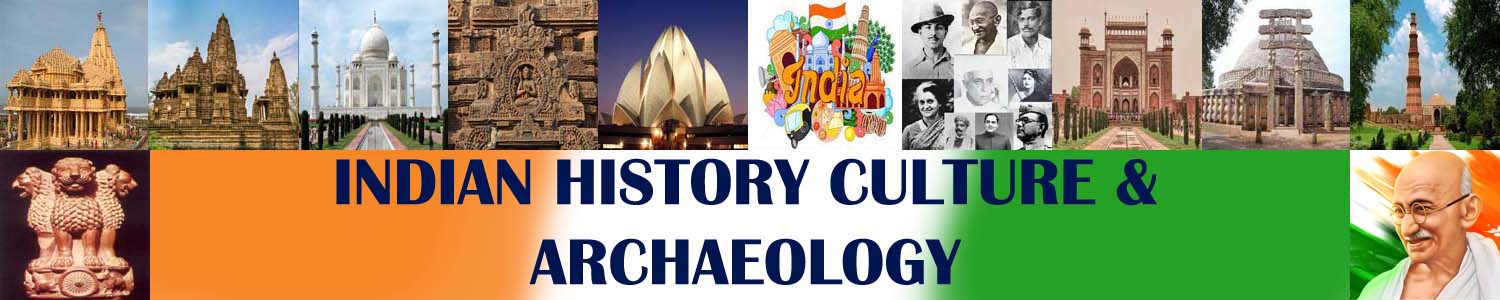| |||||||||
|
भारत पर तुर्क आक्रमण
सन् एक हजार से बारह सौ ई. तक पश्चिम के साथ-साथ मध्य एशिया और उत्तरी भारत में तीव्र गति से परिवर्तन हुए। इन्ही परिवर्तनों ने इस काल के अंत में तुर्कों के लिए भारत पर आक्रमण करने का मार्ग प्रशस्त किया था।
नौवीं शताब्दी के अंत तक अब्बासी खिलाफत पतनोन्मुख हो चली थी। उनका साम्राज्य जब छोटे-छोटे राज्यों में बँट गया था जिन पर उन तुर्कों का शासन स्थापित हो गया था जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। नौवीं शताब्दी में तुर्क, अब्बासी साम्राज्य में महल रक्षकों और पेशेवर सैनिकों के रूप में सेवा में आये थे। परन्तु शीघ्र ही वे इतना शक्तिशाली हो गए कि राजा की नियुक्ति पर भी उनका प्रभाव हो गया। केन्द्रीय सरकार की शक्ति क्षीण होते ही प्रान्तीय शासक अपने को स्वतन्त्र समझने लगे। फिर भी उन सफल सरदारों को जो किसी क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व जमाने में सफल हो जाते थे, खलीफा द्वारा औपचारिक रूप से ‘अमीर-उल-उमरा’ (अमीरों का अमीर) की उपाधि प्रदान करके, एकता की परिकल्पना को बनाये रखने का प्रयास किया गया। ये नये शासक पहले अमीर की फिर बाद में सुल्तान की उपाधि धारण करने लगे। मध्य एशिया से तुर्की जनजातियों के लगातार आक्रमण, पेशावर की राजसत्ता पलटने और अयोग्य राजाओं को निसंकोच गद्दी से उतारने की प्रवृत्ति, विभिन्न क्षेत्रों तथा मुसलमानों के विभिन्न सम्प्रदायों के बीच होने वाले संघर्ष के कारण इस काल में बराबर अशांति एवं अस्थिरता बनी रही। एक-एक करके साम्राज्य स्थापित होते चले गये और शीघ्र ही उनका पतन भी होता गया। ऐसी परिस्थिति में केवल वहीं व्यक्ति उभर कर आ सकता था, जिसमें साहस, नेतृत्व क्षमता व युद्ध कौशल के साथ ही साथ षड़यन्त्रों का सामना करने की भी क्षमता थी। तुर्क कबीले के लोग अपने साथ लूटपाट की निर्मम प्रथा को भी लाये। उनकी मुख्य युद्ध प्रणाली तेजी से आगे बढ़ना और पीछे हटना, बिजली की गति से छापा मारने और छिटपुट ढंग से उभरने वाले दलों पर आक्रमण करने की थी। ये उपयफ्रक्त दोनों कार्य इसलिए आसानी से सम्पन्न कर सकते थे, क्योंकि उनके पास उत्तम श्रेणी के घोड़े थे और वे स्वयं साहसी थे। ये लोग घोड़ों पर बहुत लम्बी दूरियाँ तय कर सकते थे। इसी बीच गुर्जर प्रतिहारों का साम्राज्य भी दिन प्रतिदिन छिन्न-भिन्न होता जा रहा था जिसके कारण उत्तर भारत में राजनीतिक अस्थिरता और प्रभुत्व के लिए नया संघर्ष उत्पन्न हो गया। इस संघर्षजनित स्थिति का परिणाम यह हुआ कि भारत की उत्तरी-पश्चिमी सीमा पर स्वभाव से आक्रामक एवं विस्तारवादी तुर्क राज्य के उदय की ओर ध्यान देने का किसी को अवसर न मिला। गजनवीनौवीं शताब्दी के अंत तक मावराउन्नहर (ट्रांस आक्सियाना) खुरासान तथा ईरान के कुछ भागों पर सामानी शासकों का राज्य था जो मूलतः ईरानी थे। सामानियों को तुर्की जनजातियों से उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर लगातार युद्ध करना पड़ा था। इसी युद्ध के दौरान नये प्रकार के योद्धा गाजी का उदय हुआ। अधिकतर तुर्क प्राकृतिक शक्तियों के पुजारी थे अतः वे मुसलमानों की दृष्टि से काफिर थे। इसलिए उनके विरुद्ध युद्ध, राज्य की रक्षा के साथ-साथ धर्म की रक्षा की दृष्टि से भी वांछनीय था। इस प्रकार गाज़ी योद्धा तथा धर्म-प्रचारक दोनों ही था। स्थायी सेना में वह एक सहायक अंग की भाँति काम करता था व इसकी आय का जरिया लूटमार था। गाजियों की सामर्थ्यशीलता तथा धर्म के लिए कोई भी खतरा मोल लेने की तत्परता के कारण ही नवोदित मुस्लिम राज्यों को तुर्कों के आक्रमण का मुकाबला करने में सफलता प्राप्त हो सकी। कालान्तर में बहुत से मुसलमान बन गये फिर भी गैर-मुस्लिम तुर्की जनजातियों के साथ मुसलमानी राज्यों का संघर्ष जारी रहा। इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाली तुर्की जनजातियाँ इस्लाम के सबसे बड़े रक्षक एवं धार्मिक योद्धा के रूप में उभर कर सामने आयी। लेकिन इस्लाम की रक्षा के साथ ही साथ लूटपाट के प्रति उनका अनुराग बना रहा।सामानी राज्य के प्रान्तीय शासकों में अलप्तगीन नामक एवं तुर्क गुलाम था जिसने आगे चलकर एक स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की। इस स्वतन्त्र राज्य की राजधानी गजनी थी। सामानी साम्राज्य का शीघ्र ही अंत हो गया और गज़नी के शासकों ने मध्य एशिया की जनजातियों से इस्लामी क्षेत्रों की रक्षा करने का भार संभाला। ऐसी परिस्थिति में महमूद (998-1030) गज़नी के सिंहासन पर बैठा। मध्ययुगीन इतिहासकारों ने मध्य एशिया के जनजातीय आक्रमणकारियों के विरुद्ध वीरता से संघर्ष करने के कारण महमूद को इस्लाम का प्रथम सरदार माना है। उसके शासन काल में गाज़ी भावना और सुदृढ़ हुई। इसके अतिरिक्त इस काल में हुई ईरानी संस्कृति के पुनर्जागरण से महमूद का गहरा संबंध था। स्वाभिमानी ईरानियों ने कभी भी अरबी भाषा और संस्कृति को स्वीकार नहीं किया। सामानी साम्राज्य ने फारसी भाषा और साहित्य को भी प्रोत्साहित किया था। फिरदौसी का शाहनामा ईरानी पुनर्जागरण की एक विशिष्ट पहचान है। फिरदौसी महमूद के दरबार का प्रमुख कवि था। उसने ईरान और तुरान के मध्य हुए युद्ध का काल्पनिक वर्णन ओर प्राचीन ईरानी वीरों का गुणगान किया है। ईरानियों की देश भक्ति का पुनरुत्थान हुआ और फारसी भाषा तथा संस्कृति अब गजनवी साम्राज्य की ऐसी भाषा और साहित्य समझी जाने लगी कि महमूद ने स्वयं प्राचीन ईरानी दंतकथाओं में चर्चित बादशाह अफरासियाव का वंशज होने का दावा किया। इस प्रकार तुर्क न केवल मुसलमान वरन् फारसी भी बन गये, इसी संस्कृति को वे दो शताब्दियों के पश्चात् भारत लाए थे। महमूद ने ईरानियों के सांस्कृतिक तथा इस्लामी राज्यों की तुर्क जनजातियों के आक्रमणों से रक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, किन्तु भारत में उसकी स्मृति लुटेरे और मन्दिर-विध्वंशक के रूप में शेष है। कहा जाता है कि महमूद ने भारत पर सत्रह आक्रमण किए थे। प्रारंभिक आक्रमण हिन्दू राज्यों के विरुद्ध किया गया था जिनका आधिपत्य उन दिनों पेशावर और पंजाब पर था। उसने दूसरे सम्प्रदाय के मुल्तानी मुसलमान शासकों के विरुद्ध भी संघर्ष किया जिनका वह घोर विरोधी था। हिन्दू राज्यों के राजा गजनवियों के विरुद्ध महमूद के पिता के समय से ही युद्ध करते चले आ रहे थे। हिन्दू राजाओं का साम्राज्य पंजाब से लेकर आधुनिक अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। गजनी की बुनियाद पर एक स्वतन्त्र राज्य का उदय हिन्दू राज्यों के लिए शीघ्र ही एक खतरा दिखायी पड़ने लगा। सामानी शासन काल में गजनी के भूतपूर्व प्रान्तीय शासक के पुत्र से संधि करके हिन्दू राजा जयपाल को पराजय का मुख देखना पड़ा। उसने आगामी वर्षों में भी युद्ध जारी रखा और पुनः पराजित हुआ था। युवराज के रूप में महमूद ने इन युद्धों में सक्रिय भाग लिया था। गद्दी पर आने के बाद महमूद ने हिन्दू राज्य के राजाओं के विरुद्ध आक्रमण का रुख अपनाया। युद्ध होने पर मुलतान के मुसलमान शासकों ने जयपाल का साथ दिया था। सन् 1001 में जयपाल को पराजित कर पहले बंदी बना लिया गया बाद में उसे छोड़ दिया गया। लेकिन अपमानित होने के कारण उसने आत्मदाह करने का निश्चिय किया। उसका पुत्र आनंदपाल उसका उत्तराधिकारी बना। सन् 1008-1009 में हिन्दू राज्य की राजधानी वैहिन्द (पेशावर के निकट) से महमूद और आनंदपाल के बीच एक निर्णायक युद्ध हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि कन्नौज और राजस्थान के राजाओं के सहित उत्तर-पश्चिम भारत के अनेक राजकुमारों ने इस युद्ध में भाग लिया था। मुल्तान के मुसलमान बादशाहों ने भी आनंदपाल की सहायता की। यद्यपि भारतीय सेनाएँ संख्या में अधिक थी और पंजाब की बहादुर युद्ध प्रिय जनजाति खोखर भी उसमें शामिल थी फिर भी धुड़सवार धनुधंरों के बल पर महमूद को विजय प्राप्त हुई। यद्यपि हिन्दू राजाओं को सन् 1020 तक साम्राज्य के कुछ भागों पर शासन करने के लिए अनुमति दी गयी थी, किन्तु व्यवहारिक रूप से पंजाब अब सभी कार्यों के लिए ग़ज़नियों के अधिकार में चला गया था। वैहिन्द युद्ध के चलते मुल्तान भी अधीन कर लिया गया था। मध्य एशिया में अपने शत्रुओं के विरुद्ध आक्रमण जारी रखने के उद्देश्य से महमूद ने बाद में उत्तरी भारत में समृद्ध मन्दिरों और शहरों में निरंतर लूटमार मचाने का निश्चय किया था। महमूद भारतीय राजाओं को अपने विरुद्ध संगठित होने और दलबंदी करने का भी अवसर नहीं देना चाहता था। भारत में लूटमार तथा मध्य एशिया में युद्ध बारी-बारी से चलते रहे। भारत में लूटपाट के लिए उसे गाजी सैनिकों का मुक्त सहयोग मिला। इस्लाम के गौरव के लिए उसने अपने को एक महान बुत-शिकन या मूर्तिभंजक के रूप में प्रस्तुत किया। पंजाब से महमूद ने पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र नगरकोट और कुरुक्षेत्र के निकट थानेश्वर पर आक्रमण किया। उसने सन् 1018 और 1025 में क्रमशः कन्नौज और गुजरात पर साहसिक आक्रमण किया था। कन्नौज के विरुद्ध अभियान में मथुरा और कन्नौज दोनों जगहों में उसने लूटपाट और लूटमार मचाई और अपार समृद्धि के साथ बुदेलखंड में कालिंजर होते हुए लौटा। बिना किसी को दंडित किये वह, यह सब कुछ कर सका क्योंकि इस समय उत्तर भारत में किसी शक्तिशाली राज्य का अस्तित्व नहीं था। इन क्षेत्रों में से किसी को भी उसने अपने साम्राज्य में मिलाने का कोई प्रयास नहीं किया। मार्ग में किसी गंभीर प्रतिरोध का सामना किये बिना वह मुल्तान से राजपूताना को पार करते हुए सोमनाथ के मन्दिर पर पहुँचा, जो अपनी अपार धन राशि के लिये विख्यात था। भारत में पंजाब के बाहर उसका यह अन्तिम अभियान था। सन् 1030 में उसकी गजनी में मृत्यु हो गई। महमूद को आक्रमणकारी और लुटेरा कहकर उपेक्षा करना अनुचित है। गजनवी के पंजाब और मुल्तान के आक्रमण ने उत्तरी भारत की राजनीतिक स्थिति में आमूल परिवर्तन कर दिया। उत्तर पश्चिम से भारत को सुरक्षा प्रदान करने वाली पर्वत श्रंखलाओं को तुर्कों ने पार कर लिया था और वे गंगाघाटी की मध्य भूमि पर किसी भी समय गंभीर आक्रमण कर सकते थे। इस काल में भारत के अतिरिक्त मध्य एशिया में तीव्रगति से परिवर्तन होने के कारण तुर्क लोग डेढ़ सौ वर्षों में भी इस क्षेत्र में अपने आक्रमण कर विस्तार करने में असफल ही रहे। महमूद की मृत्यु के साथ-साथ सल्जूक नाम एक शक्तिशाली साम्राज्य अस्तित्व में आया। सल्जूक साम्राज्य में सीरिया, ईरान और मावराउन्नहर सम्मिलित थे। इस साम्राज्य ने खुरासान पर आधिपत्य जमाने के लिए गज़नवियों से संघर्ष किया। एक प्रसिद्ध युद्ध में महमूद का पुत्र मसूद पराजित हुआ और उसने लाहौर में शरण ली। गजनी साम्राज्य अब गजनी और पंजाब तक ही सीमित रह गया। फिर भी गजनवियों ने गंगाघाटी में आक्रमण और लूटपाट का क्रम जारी रखा। राजपूत लोग भारत पर होने वाले भारी सैनिक खतरे का सामना करने की स्थिति में नहीं थे। उत्तर भारत में एक ही समय में कुछ नये राज्यों का उदय हुआ जो गजनवियों के आक्रमण का सामना कर सकते थे। राजपूत राज्यराजपूतों के एक नये वर्ग के उदय तथा उनकी उत्पत्ति से सम्बन्धित मतभेद के बारे में पहले चर्चा हो चुकी है। प्रतिहार साम्राज्य के विघटन होते ही उत्तर भारत में कुछ नये राजपूत राज्यों का जन्म हुआ। इनमें से कन्नौज के गहड़वाल, मालवा के परमार और अजमेर के चौहान सबसे प्रसिद्ध थे। उन दिनों कुछ अन्य छोटे राजवंश भी थे जो भारत के विभिन्न भागों में स्थित थे जैसे - आधुनिक जबलपुर के निकट कलचुरि, बुदेलखंड के चंदेल, गुजरात के चालुक्य, दिल्ली के तोमर आदि। बंगाल पालों के अधिकार में रहा और कालान्तर में सेनों के अधिकार में चला गया। कन्नौज के गहड़वालों ने पालों को धीरे-धीरे बिहार से बाहर कर दिया और बनारस को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। चौहानों ने अपने को अजमेर में स्थापित कर लिया था और धीरे-धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार गुजरात के अतिरिक्त दिल्ली और पंजाब की तरफ भी कर लिया। इस परिस्थिति में उनका संघर्ष गहड़वालों के साथ हुआ। इस प्रतिद्वन्दता के कारण गजनवियों को पंजाब से खदेड़ने के लिए राजपूत शासकों का एकजुट होना असंभव था। वस्तुतः गजनवी उज्जैन तक भी युद्ध करने के लिए पूर्ण सक्षम थे।राजपूत समाज का आधार कुल था। प्रत्येक राजपूत वंश, अपनी उत्पत्ति का स्रोत किसी न किसी योद्धा के वंश से चाहे वह काल्पनिक हो अथवा वास्तविक, मानते हैं। सामान्यतः इन वंशों का प्रभुत्व एक विशिष्ट क्षेत्र पर होता था। कभी-कभी इनका निर्धारण बारह या चौबीस या अड़तालिस या चौरासी गाँवों की इकाइयों पर होता था। सरदार अपने अधीनस्थ सरदारों को गाँवों की भूमि सौंपता था तथा वे इस भूमि को विभिन्न राजपूत योद्धाओं के सम्मान के अनुरूप एवं पारिवारिक निर्वाह के लिये सौंप देते थे। भूमि, परिवार और मर्यादा के प्रति मोह राजपूतों की विशेषता थी। प्रत्येक राजपूत राज्य पर ऐसे ही सरदारों की मदद से शासन किया जा सकता था जो प्रायः कुलबंधु हुआ करते थे। यद्यपि उनकी जगीरें राजा की इच्छा पर निर्भर करती थी। राजा द्वारा भूमि को पुनः लौटा लेने से भूमि की पवित्रता नष्ट हो जाती थी। यह विशेष परिस्थितियों में होता था, जबकि जागीरदार राजा के विरुद्ध बगावत न कर दे या उसका कोई उत्तराधिकारी न हो इत्यादि। राजपूत समाज के संगठन में गुण-दोष दोनों थे। पहला गुण भाई-चारा और समानतावादी भावना थी जो राजपूतों की विशेषता थी। लेकिन उसी गुण विशेष ने राजपूतों के बीच अनुशासन कायम रखना मुश्किल कर दिया। पुश्तैनी शत्रुता कई पीड़ितों तक चलती रहती थी। राजपूतों की दूसरी दुर्बलता दलबंदी की भावना थी। प्रत्येक वंश अपने को एक-दूसरे से श्रेष्ठ मानता था। वे गैर राजपूतों से भाईचारे की भावना के संबंध का विस्तार करने के लिए तैयार न थे। इससे राजपूत शासक वर्ग और जनता के, जिनमें अधिकांश संख्या गैर राजपूतों की थी, बीच की खाई गहरी होने लगी। राजस्थान में आज भी राजपूतों की संख्या दस प्रतिशत है। ग्यारहवीं और बारहवीं शताब्दियों में राजपूत जिन क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व रखते थे, वहाँ की कुल जन-संख्या से राजपूतों की संख्या का प्रतिशत अधिक नहीं रहा होगा। राजपूत युद्ध को खेल समझते थे। युद्ध के खेल समझने की प्रवृत्ति तथा भूमि और पशुओं पर अधिकार के प्रश्न को लेकर विभिन्न राजपूत राज्यों में निरन्तर संघर्ष बना रहता था। राजपूत राज्यों के बीच की भूमि और पशुओं को लेकर निरन्तर युद्ध हुआ करते थे। वही आदर्श राजा माना जाता था जो दशहरे के पश्चात् अपनी सेना का नेतृत्व कर अपने पड़ोसियों के क्षेत्रों पर आक्रमण करता था। इस नीति से गाँवों और शहरों की जनता को दुख भोगना पड़ा। इस समय के अधिकांश राजपूत शासक हिन्दू धर्म के समर्थक थे। उनमें से कुछ जैन धर्म के भी संरक्षक थे। उन्होंने ब्राह्मणों और मन्दिरों को भारी चन्दा और भूमि अनुदान दिया था। राजपूत ब्राह्मणों की सुविधाओं और जाति व्यवस्था की रक्षा के लिए आगे आए। अतः दूसरों की तुलना में ब्राह्मणों से भू-राजस्व कम दर पर लिया जाता था। राजपूत राज्यों में यह व्यवस्था तब तक चलती रही जब तक कि उनका विलयन भारतीय संघ में नहीं हो गया। इनके बदले में तथा अन्य सुविधाओं के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराने चन्द्रवंशी और सूर्यवंशी राजपूतों के रूप में मान्यता दी, जो पहले समाप्त हो चुकी थी। आठवीं शताब्दी के बाद और विशेषकर दसवीं और बाहरहवीं शताब्दियों के मध्य का काल उत्तर भारत में मन्दिर निर्माण का कार्य चरमोत्कर्ष माना जा सकता है। मन्दिर निर्माण की प्रख्यात शैली को नागर शैली कहकर पुकारा जाता था। यद्यपि ये संपूर्ण भारत में पाई जाती थी, फिर भी उत्तर और दक्षिण भारत इस निर्माण शैली के प्रधान केन्द्र थे। इसकी प्रमुख विशेषता मुख्य प्रतिमा के ऊपर बड़ी टेढ़ी सर्पाकार छत थी, जिसे गर्भगृह या देवल कहा जाता था। इसका प्रधान कमरा प्रायः वर्गाकार होता था, यद्यपि इसके हर तरफ प्रक्षेप हो सकते थे। प्रतिभा-कक्ष (मंडप) से लगा मन्दिर होता था और कभी-कभी मन्दिर ऊँची दीवारों से घिरे होते थे, जिसके दरवाजे ऊँचे होते थे। इस प्रकार के मन्दिरों का प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश में खजुराहो और उड़ीसा में भुवनेश्वर के मन्दिर करते हैं। पार्श्वनाथ तथा विश्वनाथ और खजुराहो का कंदरिया मन्दिर इस शैली के उत्कृष्ट और सुन्दरतम उदाहरण हैं। इन मन्दिरों की प्रचुर नक्काशी से पता चलता है कि इस काल में मूर्ति कला अपनी उन्नति के शिखर पर थी। इनमें से अधिकांश मन्दिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने किया था, जो नौवीं शताब्दी के आरम्भ से लेकर तेरहवीं शताब्दी के अंत तक शासन करते रहे। उड़ीसा में लिंगराज का मन्दिर (ग्यारहवीं शताब्दी) और कोणार्क का सूर्य मन्दिर (तेरहवीं शताब्दी) स्थापत्य कला के विशाल और सुन्दर उदाहरण हैं। पुरी का प्रसिद्ध मन्दिर भी इसी काल का है। उत्तर भारत में मथुरा, बनारस, दिलवाड़ा (आबू) आदि अन्य स्थानों में बड़ी संख्या में मन्दिरों का निर्माण किया गया था। दक्षिण भारत में मन्दिरों की तरह उत्तर भारत में भी मन्दिरों का विस्तार अधिकाधिक होता गया। वे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केन्द्र भी थे। उनमें से कुछ, जैसे सोमनाथ का मन्दिर बहुत समृद्ध शाली हो गया। वे अनेक गाँवों पर शासन करते और व्यापारिक क्रियाकलापों में हाथ बँटाते थे। राजपूत राजाओं ने भी कला और विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। इस काल में उनके संरक्षण में संस्कृत में अनेक पुस्तकें और नाटक लिखे गये। चालुक्य राजा भीम का प्रसिद्ध मन्त्री वस्तुपाल एक लेखक और विद्वानों का संरक्षक था। उसने आबू में एक सुन्दर जैन मन्दिर का निर्माण कराया था। परमार राजाओं की राजधानी उज्जैन और धार संस्कृत भाषा के अध्ययन के दूसरे केन्द्र थे। अपभ्रंश और प्राकृत की अनेक रचनाएँ इस क्षेत्र की भाषाओं में उपलब्ध हैं। जैन विद्वानों का इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान है। उनमें सबसे मशहूर थे हेमचन्द्र, जिन्होंने संस्कृत और अपभ्रंश दोनों में रचनाएँ की थी। ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान के साथ उच्च वर्ग में संस्कृत ने अपभ्रंश और प्राकृत का स्थान ग्रहण कर लिया। फिर भी ऐसी भाषा जो बोलचाल की भाषा के निकट थी, प्रचलित रही और उसमें रचनाएँ होती रही। इस काल में इन लोकप्रिय भाषाओं से हिन्दी, बंगाली, मराठी आदि जैसी उत्तर भारत की आधुनिक भाषाओं का विकास आरम्भ हो गया था। तुर्कों द्वारा उत्तर भारत की विजयगजनवी द्वारा पंजाब विजय के उपरान्त हिन्दुओं और मुसलमानों के मध्य दो विशिष्ट रूपों में सम्बन्ध विकसित हुये। एक का आधार लूटमार का आकर्षण था जिसके परिणामस्वरूप महमूद के उत्तराधिकारियों ने गंगाघाटी और राजपूताने पर आक्रमण किया। राजपूत राज्यों के शासकों ने इन आक्रमणों का डटकर सामना किया और तुर्कों के विरुद्ध उन्हें अनेक बार विजय मिली। लेकिन अब गजनी राज्य बहुत शक्तिशाली नहीं रह गए थे और तुर्कों को अनेक स्थानीय युद्धों में पराजित कर राजपूतों ने आत्मसंतोष कर लिया। किन्तु दूसरे स्तर पर मुसलमान व्यापारियों को न केवल स्वीकृति दी गई वरन् देश में उनका स्वागत भी किया गया क्योंकि उनके माध्यम से मध्य और पश्चिमी एशिया के साथ भारत के व्यापार को बहुत बढ़ावा मिलता था और इससे राज्यों की आय भी बढ़ती थी। इससे उत्तरी भारत के नगरों में मुसलमान व्यापारियों की बस्तियाँ स्थापित हो गयी। इन व्यापारियों के पीछे अनेक मुसलमानों के धर्म-प्रचारक गये जिन्हें सूफी कहते हैं। सूफीयों ने प्रेम पर विश्वास करने और एक ईश्वर पर विश्वास करने और एक ईश्वर के प्रति समर्पण के सिद्धान्त का प्रचार किया। यद्यपि उनका धर्म प्रचार मुसलमानों के लिए ही था तथापि हिन्दू भी उससे प्रभावित हुए बिना न रह सके। इस प्रकार इस्लाम तथा हिन्दू धर्म और समाज के बीच एक दूसरे को प्रभावित करने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। लाहौर अरबी और फ़ारसी भाषा तथा साहित्य का केन्द्र बन गया। तिलक जैसे हिन्दू सेनापतियों ने गजनवियों की सेना का नेतृत्व किया। गजनवियों की सेना में हिन्दू सैनिक भी भर्ती किए जाते थे।ये दोनों प्रक्रियाएं अनिश्चित काल तक चलती रहती, यदि इसी बीच मध्य-एशिया की राजनीतिक स्थिति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन न होता। बारहवीं शताब्दी के मध्य तक तुर्की जनजातियों के एक अन्य दल ने जो कुछ हद तक बौद्ध और कुछ हद तक गैर मुसलमान थे, सल्जूक तुर्कों को उखाड़ फेंका। इस तरह जो स्थान रिक्त हुआ उसमें ख्वारिज्मी और गोरी दो नयी शक्तियों का उदय हुआ। ख्वारिज़्मी साम्राज्य का आधार ईरान तथा गोरी साम्राज्य का आधार उत्तर-पश्चिम अफगानिस्तान था। गोरी आरम्भ में गजनी के सामन्त थे लेकिन शीघ्र ही वे इस बोझ को उतार फेंकने में सफल हो गए। सुल्तान अलाउद्दीन के अधीन गोरियों की शक्ति में अभिवृद्धि हुई। उसे विश्व ‘दाहक’ (जहाज सोज़) की संज्ञा दी गई है क्योंकि उसने अपने भाइयों के साथ किए गए व्यवहार के कारण गजनी का विध्वंश किया और जला दिया। साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के कारण गोरियों को मध्य एशिया की ओर बढ़ने की महात्वाकांक्षा को आघात पहुँचा। खुरासान जो इन दोनों के मध्य झगड़े की जड़ था, पर ख्वारिज्म के शाह ने अधिकार कर लिया। इससे गोरियों के लिए भारत की तरफ बढ़ने के अलावा और कोई चारा न था। शहाबुद्दीन महमूद (जिसे मुइज्जुद्दीन बिनसाम के नाम से भी जाना जाता है) सन् 1173 में गजनी के सिंहासन (1173-1206 ई.) पर बैठा जबकि उसका अग्रज गोर पर शासन कर रहा था। गोमल दर्रे से होता हुआ मुहज्जुद्दीन मुहम्मद ने मुल्तान और उच्च पर अपना अधिकार जमा लिया। सन् 1178 में उसने राजस्थान की मरुभूमि को पार करता हुआ गुजरात में प्रवेश करने का प्रयास किया। लेकिन गुजरात के शासक के हाथों आबू के निकट युद्ध में उसे बुरी तरह मुँह की खानी पड़ी। भाग्य से मुइज्जुद्दीन की जान बच गई। अब उसने भारत पर आक्रमण करने से पूर्व पंजाब में अपना अनुकूल आधार बनाने की आवश्यकता का अनुभव किया। इस प्रकार उसने पंजाब में गजनवियों के अधिकार के विरुद्ध एक अभियान छेड़ दिया। सन् 1190 तक मुइज्जुद्दीन मुहम्मद ने पेशावर, लाहौर और सियालकोट को जीत लिया। पुनः उसने अपने को संतुलित कर दिल्ली और गंगा के दोआब पर आक्रमण किया। इसी बीच उत्तर भारत की घटनाएँ ज्यों कि त्यों बनी रहीं। चौहानों की शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी। चौहानों ने राजस्थान पर पंजाब की तरफ से आक्रमण करने वाले तुर्कों को पराजित किया और भारी संख्या में तुर्कों को मार डाला। उन्होंने इस शताब्दी के मध्य तक तोमरों से दिल्ली को अपने अधिकार में ले लिया। चौहान शक्ति का पंजाब की ओर विस्तार के कारण उस क्षेत्र के गजनवी शासकों से संघर्ष होना अनिवार्य था। मुइज्जद्दीन मुहम्मद (मुहम्मद गोरी) जब मुल्तान और उच्च पर अधिकार करने की चेष्टा कर रहा था, एक चौदह वर्षीय बालक अजमेर की गद्दी पर बैठा। यह पृथ्वीराज था, जिसके विषय में अनेक जनश्रुतियाँ और कथाएँ प्रचलित हैं। किशोर राजा ने विजय को ही जीवन वृत्ति के रूप में अपनाया। अपने सगे-संबंधियों के विरोध को समाप्त कर उसने राजस्थान के अनेक छोटे राज्यों को अपने अधीनस्थ कर लिया। उसने बुदेलखंड पर आक्रमण किया और महोबा के निकट एक युद्ध में चंदेल राजाओं को पराजित किया। इसी युद्ध में आल्हा और ऊदल नामक दो प्रसिद्ध भाईयों ने महोबा की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। फिर भी पृथ्वीराज ने उस राज्य को अपने में मिलाने का प्रयास नहीं किया व पुनः उसने गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात के राजा भीम द्वितीय ने जिसने मुइज्जुद्दीन मुहम्मद को पहले हराया था, पृथ्वी को भी पराजित किया। इस पराजय से बाध्य होकर पृथ्वीराज का ध्यान पंजाब और गंगा की घाटी की ओर गया। तराइन का युद्धइस प्रकार मुइज्जुद्दीन मुहम्मद और पृथ्वीराज जैसे दो महत्वाकांक्षी राजाओं के बीच युद्ध अपरिहार्य हो गया। संघर्ष तबर हिन्द (भंटिडा) पर दोनों के दावों को लेकर आरम्भ हुआ। सन् 1191 में तराइन में जो युद्ध हुआ था उसमें गोरी की फौज के पैर उखड़ गये और मुइज्जुद्दीन मुहम्मद का जीवन एक ख़लजी घुड़सवार युवक ने बचाया था। पृथ्वीराज अब भटिंडा की ओर बढ़ा और बारह मास के घेरे के पश्चात् उसे अपने अधिकार में कर लिया। पंजाब से गोरियों को खदेड़ने के लिए पृथ्वीराज ने बिल्कुल प्रयास नहीं किया। संभवतः उसे ऐसा अनुभव हुआ कि तुर्कों के बार-बार हो रहे आक्रमणों में से यह भी एक हो और गोरी शासक पंजाब पर शासन कर संतुष्ट रहे। बताया जाता हे कि तराइन के दूसरे युद्ध के पूर्व वह मुइज्ज़द्दीन को दिए गए एक प्रस्ताव में पंजाब को मुइज्जुद्दीन के हाथों में छोड़ने के लिए तैयार था।सन् 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। मुइज्जुद्दीन मुहम्मद ने संघर्ष के लिए सावधानी से तैयारियाँ की थीं। कहा जाता है कि इसकी सेना में बख्तरबन्द घुड़सवार और 10,000 धनुर्धारी घुड़सवार शामिल थे। यह सूचना गलत है कि पृथ्वीराज अपने राज्य की घटनाओं से बेखबर थे और उनकी नींद तब खुली, जबकि बहुत देर हो चुकी थी। सत्य तो यह है कि उस समय पिछले अभियान का विजयी सेनापति स्कन्द कहीं अन्यत्र व्यस्त था। ज्यों ही पृथ्वीराज को गोरियों के खतरे की आशंका हुई, उसने उत्तरी भारत के समग्र राजाओं से सहायता के लिए अनुरोध किया। बताया जाता है कि बहुत से राजाओं ने उसकी मदद के लिए सेनाओं की टुकड़ियाँ भेजी। लेकिन कन्नौज का राजा जयचन्द्र अलग रहा। किवंदन्ती के अनुसार पृथ्वीराज ने जयचन्द्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था, क्योंकि यह पृथ्वीराज से प्रेम करती थी। अधिकांश इतिहासकार अब इस मत से सहमत नहीं हैं। वस्तुतः यह प्रेमकथा बहुत बाद में कवि चन्द्रवरदायी ने लिखी थी व उसके वर्णन में कई असम्भाव्य घटनाओं का समावेश है। इन दो राज्यों के बीच एक पुराने समय से गहरी शत्रुता चली जा रही थी। इसलिए जयचन्द ने अपने को इस युद्ध की गतिविधियों से अलग रखा। कहा जाता है कि पृथ्वीराज ने 300,000 फौजियों को, जिनमें बड़ी संख्या में घुड़सवार और तीन सौ हाथी थे, रणभूमि में उतारा था। दोनों पक्षों की सैन्य शक्ति के वर्णन में अतिशयोक्ति हो सकती है। संख्या के हिसाब से भारतीय फौजें संभवतः बड़ी थीं, लेकिन तुर्कों की सेना सुसंगठित थी और उनका नेतृव्य भी बढ़िया था। युद्ध मुख्य रूप से घुड़सवारों के बीच ही था। तुर्कों की विजय घुड़सवार सेना के सुसंगठन, दक्षता और गतिशीलता के कारण ही हुई। भारी संख्या में भारतीय सैनिक मारे गये। पृथ्वीराज ने भागकर बचने की कोशिश की लेकिन उन्हें सरस्वती के निकट बंदी बना लिया गया। तुर्की सेनाओं ने हाँसी, सरस्वती और समाना के किलों पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने अजमेर पर आक्रमण किया और उसे अपने अधिकार में ले लिया। इस समय के सिक्कों में एक तरफ तिथि और पृथ्वीराज का चित्र और दूसरी ओर भी मुहम्मद साम शब्द अंकित है। इससे पता चलता है कि पृथ्वीराज को अजमेर पर कुछ समय तक शासन करने के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन इसके तुरंत बाद षड़यंत्र का आरोप लगाकर पृथ्वीराज को मार डाला गया। पृथ्वीराज का पुत्र उसका उत्तराधिकारी बना। दिल्ली को भी उसके शासक को लौटा दिया गया। लेकिन यह नीति शीघ्र ही बदल दी गई। दिल्ली के शासक तोमर नरेश को हटा दिया गया और दिल्ली को तुर्की सेना के लिए गंगा घाटी को ओर बढ़ने का आधार बनाया गया। एक विद्रोह में मुस्लिम सेना ने अजमेर पर आधिपत्य जमा लिया और वहाँ एक तुर्की सेनाध्यक्ष को शासक नियुक्त कर दिया। पृथ्वीराज का पुत्र रणथम्भौर की ओर बढ़ा और एक नये शक्तिशाली चौहान साम्राज्य की उसने स्थापना की। इस प्रकार दिल्ली तथा पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र तुर्कों के शासन के अधीन हो गये। गंगाघाटी, बिहार और बंगाल पर तुर्कों की विजयसन् 1192 और 1206 के बीच तुर्की शासन का विस्तार गंगा यमुना के दोआब पर उसके निकटवर्ती क्षेत्रों तक हो गया। बिहार और बंगाल भी जीत लिए गए। दोआब में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए सर्वप्रथम तुर्कों को कन्नौज की शक्तिशाली राजधानी गहड़वाल पर अधिकार जमाना पड़ा। उस समय गहड़वाल का राजा जयचन्द भारत का सबसे शक्तिशाली राजा था। वह दो दशकों से बड़ी शान्तिपूर्वक शासन करता आ रहा था। संभवतः वह कोई बहुत योग्य योद्धा नहीं था क्योंकि बंगाल के सेन राजा के हाथों उसकी भारी पराजय हुई थी।तराइन युद्ध के उपरान्त मुइज्जुद्दीन अपने विश्वासी गुलाम कुतुबुद्दीन के हाथों भारतीय मामलों को सौंप कर गजनी लौट गया। आगामी दो वर्षों के भीतर तुर्कों ने ऊपरी दोआब के हिस्सों को जीत लिया। गहड़वालों ने इसका किंचित विरोध नहीं किया। सन् 1194 में मुइज्जुद्दीन भारत लौटा। उसने 50,000 घुड़सवारों के साथ यमुना पार की और कन्नौज की ओर अग्रसर हुआ। कहा जाता है कि जयचंद लगभग जीत चुका था कि एक तीर लगने से वीरगति को प्राप्त हुआ और उसकी सेना पूर्णरूपेण पराजित हो गयी। मुइज्जुद्दीन अब बनारस की ओर बढ़ा और उसे उजाड़ दिया। वहाँ के बहुत से देवालय नष्ट कर दिए गए। तुर्कों ने अब दिल्ली से बिहार की सीमा तक के विस्तृत क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया था। इस प्रकार तराइन और चन्दवाड़ा के युद्धों ने उत्तर भारत में तुर्कों के शासन की स्थापना की। विजित साम्राज्य को संगठित करना कठिन कार्य था जिसमें तुर्कों को लगभग पचास वर्ष लग गए। इसका अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। मुइज्जुद्दीन सन् 1206 तक जीवित रहा। इस काल में दिल्ली के दक्षिणी भाग की सुरक्षा के लिए उसने बथाना और ग्वालियर के शक्तिशाली किलों को अपने अधिकार में कर लिया। इसके पश्चात् ऐबक ने इस क्षेत्र के चन्देल राजाओं से कालिंजर, महोबा और खजुराहो जीत लिया। दोआब को आधार बनाकर तुर्कों ने निकटवर्ती क्षेत्रों पर निरन्तर आक्रमण किया। ऐबक ने गुजरात और अन्हिलवाड़ा के राजा भीम द्वितीय को पराजित किया और अनेक नगरों को उखाड़ा और लूटा। यद्यपि एक मुसलमान प्रान्तीय शासक को उसकी जगह शासन करने के लिए नियुक्त किया गया, किन्तु उसे शीघ्र ही हटा दिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि दूरवर्ती क्षेत्रों पर तुर्कों में शासन करने की शक्ति नहीं थी। किन्तु तुर्कों ने पूर्व में सफलता हासिल की। बख्तियार खलजी नामक एक खलजी पदाधिकारी जिसके चाचा ने तराइन के युद्ध में भाग लिया था, बनारस के पार के कुछ क्षेत्रों पर शासन करने के लिए नियुक्त किया गया। उसने इस बात का लाभ उठाया और बिहार पर बारम्बार आक्रमण किया जो उस समय किसी के अधिकार में नहीं था। इन आक्रमणों के दौरान उसने कुछ बौद्ध मठों पर आक्रमण किया और उन्हें नष्ट कर दिया। नालंदा और विक्रमशिला का अब कोई संरक्षक नहीं रहा। उसने विपुलधन और अपने समर्थकों को अपने चारों तरफ एकत्र कर लिया था। इन आक्रमणों के दौरान उसने बंगाल पहुँचने के मार्गों का भी पता लगा लिया। उन दिनों बंगाल अपने धन एवं सम्पदा के कारण विख्यात था। प्रचुर आंतरिक संसाधनों एवं विदेशी व्यापार के कारण बंगाल अत्यंत ही समृद्ध हो चुका था। अच्छी तरह से तैयारी कर बख्तियार खलजी ने एक सेना के साथ बंगाल के सेन राजाओं की राजधानी नदिया की ओर कूच किया। खलजी सरदार ने चोरी-चोरी, घोड़े के व्यापारी का छद्मवेश धारण कर अपने अठारह सैनिकों के एक दल के साथ सेन राजा की राजधानी में प्रवेश किया। उन पर किसी प्रकार शक नहीं किया गया क्योंकि उन दिनों तुर्की घोड़े के व्यापारियों का देखा जाना आम बात थी। राजमहल के निकट पहुँचकर बख्तियार खलजी ने अचानक धावा बोल दिया, जिससे चारों तरफ खलबली मच गई। संभवतः अचानक हमले से सेन राजा घबड़ा गया। यह सोचकर कि तुर्कों की मुख्य सेना पहुँच चुकी है, पीछे के दरवाजे से भागकर उसने सोनार गाँव में शरण ली। तुर्की सेना निश्चित रूप से निकट रही होगी, क्योंकि वह शीघ्र ही वहाँ पहुँच गयी और रक्षक सेना को उसने धराशयी कर दिया। लक्ष्मण सेन की सारी सम्पत्ति, यहाँ तक कि उसकी पत्नियों तथा बच्चों को भी कब्जे में कर लिया गया। इस क्षेत्र में बड़ी नदियों की संख्या अधिक होने के कारण बख्तियार खलजी को नदिया पर अधिकार बनाए रखना कठिन हो गया। इसलिए वह पीछे हट गया और उत्तर बंगाल में उसने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। लक्ष्मण सेन और उसके उत्तराधिकारी सोनार गाँव से दक्षिण बंगाल पर शासन करते रहे। यद्यपि बख्तियार खलजी औपचारिक रूप से मुइज्जुद्दीन द्वारा प्रान्तीय शासक नियुक्त किया गया था किन्तु वास्तव में वह एक स्वतन्त्र शासक के रूप से शासन करता रहा। लेकिन उसकी स्थिति बहुत समय तक मजबूत न रह सकी। उसने असम में ब्रह्मपुत्र घाटी पर आक्रमण करने की मूर्खता की। लेखकों का कथन है कि वह तिब्बत तक जाना चाहता था। असम का शासक माघ पीछे हटता गया और तुर्कों की सेना जितना अंदर जा सकती थी जाने दिया गया। अंत में थकान की मार से सेना आगे बढ़ने में असमर्थ हो गई। अतः उसने लौटाने का निश्चय किया। मार्ग में उन्हें रसद नहीं मिल सकी और असमी सैनिकों द्वारा उन पर हमले किये जाते रहे। भूख और बीमारी से क्लान्त और दुर्बल तुर्की सेना को युद्ध का सामना करना पड़ा। युद्ध के समय उनके सामने एक चौड़ी नदी थी और पीछे असम की सेना। तुर्की सेना बुरी तरह पराजित हुई। बख्तियार खलजी अपने अनुचरों के साथ पहाड़ी जनजातियों की सहायता से लौट सकने में सफल हुआ। लेकिन उसका उत्साह भंग हो गया था और स्वास्थ्य गिर चुका था। ऐसी दशा में सोते समय एक अमीर ने छुरे से प्रहार कर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। जब ऐबक, तुर्की और खलजी सरदार उत्तर भारत में तुर्की द्वारा अर्जित क्षेत्रों के विस्तार और संगठन की चेष्टा कर रहे थे, मुइज्जुद्दीन और उसका भाई मध्य एशिया में गोरी साम्राज्य का विस्तार करने में लगे थे। गोरियों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के कारण उन्हें शीघ्र ही शक्तिशाली ख्वारिज्म साम्राज्य से मुठभेड़ लेनी पड़ी। सन् 1203 में ख्वारिज्म के शासक के हाथों मुइज्जुद्दीन की भीषण पराजय हुई। यह पराजय तुर्कों के लिए वरदान सिद्ध हुई क्योंकि इसके कारण उन्हें मध्य एशिया में विस्तार की आशंका की तिलांजलि देनी पड़ी और उन्होंने अपनी शक्ति को एकमात्र भारत में केन्द्रित करने में लगा दिया। इससे विकास का मार्ग अवरुद्ध हो गया। कुछ समय के बाद भारत तुर्की साम्राज्य का एकमात्र आधार बन गया। इसका तात्कालिक परिणाम यह हुआ है कि मुइज्जुद्दीन की पराजय से उसके विरोधियों ने भारत में विद्रोह करने का साहस किया। पश्चिमी भारत पंजाब की लड़ाकू जनजाति खोखरों ने लाहौर और गजनी के बीच यातायात के साधनों को गुप्त रूप से काट दिया। विद्रोही खोखरो से निपटने के लिए मुइज्जुद्दीन ने सन् 1206 में भारत में अपने अंतिम विद्रोह का नेतृत्व किया। उसने बड़े पैमाने पर खोखरो का कत्ल किया और उन्हें दबा दिया। गजनी वापस लौटते समय किसी विरोधी मुस्लिम सम्प्रदाय के कट्टार समर्थक द्वारा जान से मार डाला गया। मुइज्जुद्दीन मुहम्मद बिन साम की तुलना अक्सर महमूद गजनी से की जाती है। महमूद गजनी एक योद्धा के रूप में मुइज्जुद्दीन से अधिक सफल रहा क्योंकि उसे भारत या मध्य एशिया में पराजय का मुख कभी देखना नहीं पड़ा। उसने भारत के बाहर भी एक बड़े साम्राज्य पर शासन किया। लेकिन यह स्मरण रखना चाहिए कि मुहम्मद की तुलना में मुइज्जुद्दीन को भारत में बड़े और सुसंगठित राज्यों का सामना करना पड़ा था। यद्यपि वह मध्य एशिया में उतना सफल नहीं रहा फिर भी भारत में उसकी बड़ी राजनीतिक उपलब्धियाँ थीं। लेकिन पंजाब पर महमूद की विजय ने भारत में मुइज्जुद्दीन के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। दोनों को विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था, अतः इन दोनों की तुलना से कोई लाभ नहीं हो सकता। महत्वपूर्ण बातों को लेकर भारत में दोनों के राजनीतिक और सैनिक उद्देश्य भी भिन्न थे। वस्तुतः इस्लाम का प्रसार दोनों का ही उद्देश्य नहीं था। यदि कोई राजा उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता तो उसे अपने क्षेत्र पर शासन करने दिया जाता था। केवल विशेष परिस्थितियों में उनके पूरे राज्य या उसके किसी भाग को पूरी तरह से अपने अधिकार में लाना आवश्यक हो जाता था। महमूद के अतिरिक्त मुइज्जुद्दीन ने भी हिन्दू पदाधिकारियों और सैनिकों की सेवाओं का उपयोग किया। लेकिन दोनों में से किसी ने अपने स्वार्थों को सिद्ध करने तथा भारतीय शहरों और मन्दिरों की लूट को उचित ठहराने के लिए इस्लाम के नारों का सहारा लेने में हिचकिचाहट का अनुभव नहीं किया। पन्द्रह वर्षों की अल्पावधि में तुर्की सेना द्वारा उत्तर भारत के अग्रगण्य राज्यों की पराजय से सम्बन्धित तथ्य के पुनर्विश्लेषण की भी आवश्यकता है। सूक्ति रूप में यह स्वीकार किया जा सकता है कि एक देश दूसरे पड़ोसी देश से तभी जीता जाता है जबकि उसमें सामाजिक और राजनीतिक दुर्बलता हो या आर्थिक, सैनिक दृष्टि से पिछड़ापन हो। आधुनिक शोध प्रमाणित करते हैं कि भारतीयों की तुलना में तुर्कों के पास श्रेष्ठ हथियार नहीं थे। पहले ही इस बात का उल्लेख हो चुका है कि लोहे के पावदान ने यूरोप की युद्ध पद्धति को परिवर्तित कर दिया था। भारत में भी इसका प्रचार आठवीं शताब्दी से ही हुआ था। तुर्की धनुष पर चलाए गए बाण लम्बी दूरी तक मार सकते थे। लेकिन भारतीय धनुषों का निशाना अचूक और प्राणघातक होता था। बाणों के सिर साधारणतः विषैले होते थे। तलवारबाजी के लिए भारतीय तलवार विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी। भारतीयों को हाथियों का भी लाभ मिलता था। भारत में जिन घोड़ों का आयात किया जाता था उसकी तुलना में तुर्की घोड़े संभवतः फुर्तीले और अधिक तगड़े होते थे। इस प्रकार तुर्कों की श्रेष्ठता सामाजिक और संगठनात्मक मामलों में थी। सामंतशाही के विकास अर्थात् स्थानीय भूमिधरों और सरदारों के उदय ने भारतीय राज्यों के प्रशासनिक ढाँचे और सैनिक संगठन को निर्बल बना दिया था। राजाओं को अनेक सरदारों पर अधिक निर्भर रहना पड़ता था जिनमें सहयोग की भावना का अभाव था। युद्धोपरान्त शीघ्र ही ये अपने-अपने क्षेत्रों को लौट जाते थे। दूसरी तरफ, तुर्की समुदाय की जनजातीय संरचना और इक्ता और खलिसा पद्धतियों, जिनकी चर्चा बाद में की जायेगी, के विकास के कारण तुर्क लोग बड़ी संख्या में सैनिकों की भर्ती करते और ये सैनिक मैदान में अधिक समय तक टिके रहते थे। परन्तु तुर्की सेना की विशेषता के बावजूद भी ऐसे बहुत से राजपूत राज्य थे जो मौलिक एवं मानवीय संसाधनों से गजनवियों और गोरियों की अपेक्षा अधिक समृद्ध होने के कारण युद्ध में पराजित नहीं किए जा सकते थे और पराजित हो जाने के बाद वे शीघ्र ही अपनी स्थिति सुदृढ़ कर लेने में सक्षम थे। | |||||||||
| |||||||||