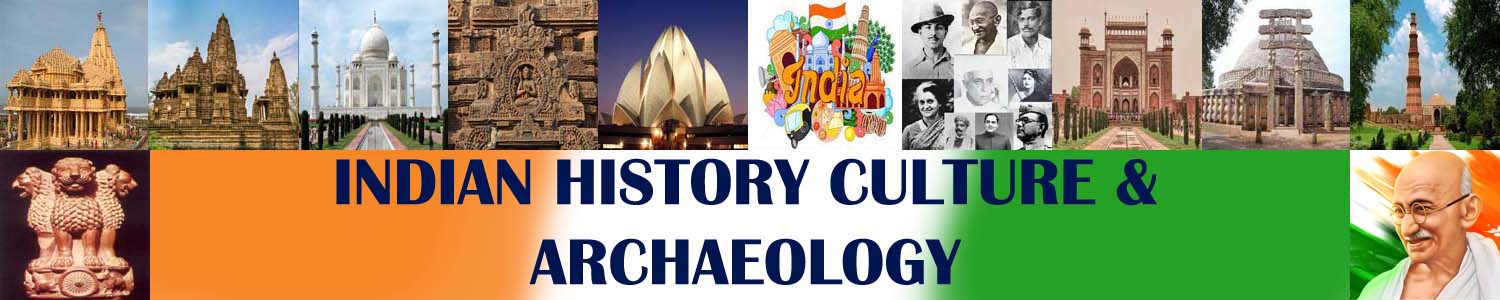| |||||||||
|
पूर्वमध्यकाल में दक्षिणी भारत - चोल राजवंश
नौवीं शताब्दी में चोल साम्राज्य का उदय हुआ। तुंगभद्रा नदी तक फैले हुए प्रायद्वीप के विशाल क्षेत्र पर इसका आधिपत्य था। चोल राजाओं ने एक शक्तिशाली नौसेना का विकास किया जिसने उन्हें हिन्द महासागर में सामुद्रिक व्यापार बढ़ाने और श्रीलंका तथा मालद्वीप पर अधिकार करने योग्य बनाया। उनका प्रभुत्व दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में भी माना जाता था। इस प्रकार दक्षिण भारतीय इतिहास में चोल साम्राज्य के चरमोत्कर्ष पर होने का संकेत मिलता है।
चोल साम्राज्य का उदयचोल साम्राज्य की स्थापना विजयांचल ने की थी जो पहले पल्लवों का एक सामंत था। उसने सन् 850 में तंजौर पर आधिपत्य जमाया। नौवीं शताब्दी के अंत में चोल राजाओं ने कांची के पल्लवों को पराजित कर तथा पांड्यों को निर्बल बनाकर दक्षिणी तमिल प्रदेश को अपने अधिकार में ले लिया। लेकिन चोल राजाओं को राष्ट्रकूटों के विरुद्ध अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए कठिन प्रयास करना पड़ा था। विगत अध्याय में इसका उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय ने चोल राजा को पराजित कर चोल साम्राज्य के उत्तरी भाग को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। यह चोल राजाओं के लिए भारी आघात साबित हुआ। परन्तु सन् 965 में कृष्ण तृतीय की मृत्यु एवं राष्ट्रकूट साम्राज्य के पतन के बाद, इस क्षति की पूर्ति उन्होंने बड़ी शीघ्रता से कर ली।राजराजा तथा राजेन्द्र प्रथम का कालचोल वंश के सबसे महान शासक राजराजा (985-1014) और उसका पुत्र राजेन्द्र प्रथम (1014-1044) थे। राजराजा अपने पिता के जीवन काल में ही उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया गया था। सिंहासनारोहण के पूर्व ही उसे प्रशासन और युद्ध का गहरा अनुभव था। राजराजा ने त्रिवेन्द्रम में चेर नौसेना को नष्ट कर दिया और कुइलान पर आक्रमण किया। तत्पश्चात् उसने मदुरई को जीता और पाण्ड्य राजा को बंदी बना लिया। उसने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया और उसके उत्तरी भाग को अपने साम्राज्य में मिला लिया। कुछ वर्ष तक दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार को अपने अधिकार में लाने के उद्देश्य से उसने यह कार्यवाही की। कोरोमंडल तट और मालाबार, भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के मध्य होने वाले व्यापार केन्द्र थे। मालद्वीप की विजय उसकी नौसेना की अद्भुत उपलब्धि थी।उत्तर में, राजराजा ने उत्तर-पश्चिम कर्नाटक के गंगा क्षेत्र के उत्तर-पश्चिमी भाग को अपने राज्य में मिला लिया और बेंगी को कुचल दिया। राजेन्द्र प्रथम ने राजराजा की अधिनहनवादी नीति को आगे बढ़ाया। पाण्ड्य और चेर प्रदेशों को जीत कर उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया। श्रीलंका की विजय को भी पूर्ण किया गया। एक युद्ध में श्रीलंका के राजा और रानी के राजमुकुट और राजचिन्ह अधिकार में ले लिए गये। अगले पचास वर्षों तक श्रीलंका चोलों के अधिकार से अपने को मुक्त नहीं कर पाया। राजराजा और राजेन्द्र प्रथम ने अनेक स्थानों में शिव और विष्णु के मन्दिरों का निर्माण कर अपनी विजय को सुस्पष्ट किया। इनमें से सबसे प्रसिद्ध तंजोर स्थित राज राजेश्वर का मन्दिर था जिसका निर्माण सन् 1010 में पूर्ण हुआ। चोल राजाओं ने उनकी दीवारों पर अपनी ऐतिहासिक विजयों के विवरणों के लम्बे अभिलेखों को अंकित करने की रीति अपनायी। यही कारण है कि हमें चोल राजाओं के विषय में उनके पूर्ववर्ती शासकों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। राजेन्द्र प्रथम के काल का सबसे स्मरणीय कारनामा था गंगा नदी पार कर चोल सैनिकों की कलिंग से बंगाल तक यात्रा और दो स्थानीय राजाओं की पराजय। सन् 1022 में इस अभियान का नेतृत्व एक चोल सेनाध्यक्ष के द्वारा किया गया जिसने उसी मार्ग का अनुसरण किया जिस पर से होकर महान विजेता समुद्रगुप्त उत्तरी दिशा की ओर से गुजरा था। उस अवसर की स्मृति बनाये रखने के लिए राजेन्द्र प्रथम ने गंगाई कोन्डचोल (या गंगा का चोल विजेता) उपाधि धारण की। उसने कावेरी तट के निकट एक नयी राजधानी बनायी और इसे गंगई कोंड चोलपुरम् (गंगा विजेता चोल का शहर) कहा। पुनर्जीवित श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध राजेन्द्र प्रथम की नौसेना का आक्रमण उसके काल की एक अन्य उल्लेखनीय घटना थी। उस समय श्री विजय साम्राज्य मलाया, प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और निकटवर्ती द्वीपों तक फैला था और चीन तक के समुद्री मार्गों पर उसका नियंत्रण था। शैलेन्द्र वंश के राजा बौद्धधर्म के मानने वाले थे और चोलों के साथ उनका मैत्रीपूर्ण संबंध था। शैलेन्द्र राजा ने नागपट्टम में एक बौद्ध मठ का निर्माण किया था। उसके अनुरोध पर राजेन्द्र प्रथम ने मठ के सहायतार्थ एक गाँव भेंट किया था। चोलों ने भारतीय व्यापारियों की बाधाओं के दूर कर चीन तक अपने व्यापार का विस्तार किया। आगे चलकर श्रीविजय और चोल शासकों के बीच संबंध विच्छेद का यह एक महत्वपूर्ण कारण बना। नौसेना के अभियान के द्वारा मलाया प्रायद्वीप और सुमात्रा के कई स्थानों एवं कादरम या केदार पर विजय प्राप्त की गयी। कुछ समय के लिये चोल राजाओं की नौसेना उस क्षेत्र की सबसे शक्तिशाली सेना थी और बंगाल की खाड़ी चोलों के लिए एक झील बन गई। चोल राजाओं ने भी कुछ राजदूतों को भेजा। सन् 1077 में सत्तर व्यापारियों का एक दल दूतों के रूप में चीन पहुँचा। एक चीनी विवरण के अनुसार उन्हें 81,000 कास्य मुद्राओं की मालाएँ आर्थात् बदले में उतना ही धन मिला जितना शीशे का समान, कपूर, बहुमूल्य वस्त्र, गैंडे के सींग, हाथी दाँत आदि वस्तुएँ उपहार में दी गयी थीं। व्यापार हेतु बाहर ले लायी गई सभी वस्तुओं के लिए चीनी ‘भेंट‘ शब्द का व्यवहार करते थे। राष्ट्रकूटों के पूर्ववर्ती चालुक्यों ने चोल राजाओं से निरन्तर संघर्ष किया। ये उत्तर कालीन चालुक्य कहलाये और इनकी राजधानी कल्याणी थी। बेंगी (रायलसीमा), तुंगभद्रा का दोआब और कर्नाटक के उत्तर-पश्चिम गंग प्रदेश पर आधिपत्य के लिए चोल शासकों एवं चालुक्यों के मध्य आपस में टकराव हुआ। इस संघर्ष में किसी को भी निर्णायक विजय नहीं मिली और दोनों साम्राज्य अंततः चकनाचूर हो गए। ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध उन दिनों भयानक हो गए थे। चोल शासकों ने चालुक्यों के शहरों में जिनमें कल्याणी शामिल था, लूटपाट मचायी और निवासियों जिनमें ब्राह्मण और बच्चे सम्मिलित थे हत्याएँ कीं। उन्होंने पाण्ड्य प्रदेशों में यही नीति अपनायी। सैनिक बस्तियाँ स्थापित कर जनता को आतंकित किया। श्रीलंका के शासकों की प्राचीन राजधानी अनुराधापुर को उन्होंने नष्ट कर दिया और उनके राजा और रानी के साथ निष्ठुर व्यवहार किया। चोल साम्राज्य के इतिहास पर ये कलंक है। फिर भी चोल जब किसी देश पर अपना आधिपत्य जमा लेते थे तो उसमें सुसंगठित प्रशासन कायम करते थे। अपने सम्पूर्ण साम्राज्य के गाँवों में स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित करना चोल-प्रशासन की विशेषता थी। चोल साम्राज्य बारहवीं शताब्दी तक चरमोत्कर्ष स्थित में बना रहा। लेकिन तेरहवीं शताब्दी के आरम्भ में उसका पतन आरम्भ हो गया। अंततः बारहवीं शताब्दी में, महाराष्ट्र के क्षेत्रों पर उनका बचा खुचा साम्राज्य भी समाप्त हो गया। चोल साम्राज्य का स्थान दक्षिण में पांड्य और होयसल सम्राटों तथा उत्तरकालीन चालुक्यों का स्थान यादवों तथा काकतियों ने ले लिया। इन राज्यों ने कला और स्थापत्य को संरक्षण प्रदान किया। दुर्भाग्यवश निरन्तर आपस में झगड़कर उन्होंने अपने को निर्बल बना लिया। नगरों में वे लूटपाट करते और मन्दिरों को भी नहीं छोड़ते थे। अंततः चौदहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में वे दिल्ली के सुलतानों द्वारा नष्ट कर दिए गये। चोल प्रशासनचोल प्रशासन में राजा सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। संपूर्ण सत्ता उसके हाथों में थी। लेकिन परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद् होती थी। प्रशासन से जुड़े योग्य व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करने के लिए राजा कभी-कभी दौरे पर जाया करता था। चोलों के पास एक विशाल सेना थी जिसके तीन अंग थे - गज सेना, अश्वारोही सेना और पैदल सेना। पैदल सेना सामान्यतः भालों से लैस होती थी। अधिकांश राजाओं के पास अंगरक्षक थे, जो शपथ लेते थे कि अपनी जान की बाजी लगाकर राजा की रक्षा करेंगे। बेनिश यात्री मार्को पोलो जिसने तेरहवीं शताब्दी में केरल की यात्रा की थी, कहता है कि राजा की मृत्यु के उपरान्त उसके सभी अंगरक्षक चिता के साथ जलकर मर जाया करते थे। यह कथन अतिश्योक्तिपूर्ण प्रतीत होता है। जैसा कि हम देख चुके हैं, चोलों के पास एक शक्तिशाली नौ-सेना भी थी, जिसका आधिपत्य मालाबार और कोरोमंडल तट पर था। कुछ समय तक यह नौ सेना संपूर्ण बंगाल की खाड़ी पर छायी हुई थी।चोल साम्राज्य मंडलमों अर्थात् प्रान्तों में विभाजित था और पुनः ये बलनाडू और नाडू में विभक्त थे। यदाकदा राजपरिवार के युवराज प्रान्तीय शासक नियुक्त किये जाते थे। सामान्यतः पदाधिकारियों को वेतन के रूप में कर मुक्त भूमि दी जाती थी। चोल राजाओं ने शाही सड़कों का जाल बिछा दिया, जो व्यापार के अतिरिक्त सेना आवागमन के लिए बड़ी उपयोगी थीं। चोल साम्राज्य में व्यापार और वाणिज्य की अभिवृद्धि हुई। उन दिनों कुछ बड़े व्यापारिक संघ थे जो जावा और सुमात्रा के साथ व्यापार करते थे। चोलों ने सिंचाई की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया। इस काम के लिए कावेरी तथा अन्य नदियों का उपयोग किया जाता था। सिंचाई के लिए अनेक सरोवर भी बनाए गये थे। लगान भू-राजस्व की दर निश्चित करने के लिए कुछ चोल राजाओं ने भूमि का व्यापक सर्वेक्षक कराया। लेकिन यह हमें पता नहीं लगता है कि लगान की ठीक-ठीक दर क्या थी। भूमि कर के अतिरिक्त चोल राजा व्यापार कर, पेशावर और निकटवर्ती क्षेत्रों की लूटपाट से अपनी आय बढ़ाते थे। चोल राजा समृद्ध थे और वे कुछ शहरों और भव्य स्मारकों को बना सकने में समर्थ हो सके। राष्ट्रकूट साम्राज्य के कुछ गाँवों स्थानीय स्वशासन का उल्लेख पहले किया जा चुका है। कुछ अभिलेखों द्वारा चोल साम्राज्य प्रशासन के विषय में अधिक जानकारी मिलती है। हमें ऊर और सभा या महासभा नामक दो समितियों की जानकारी मिलती है। ऊर गाँव की प्रधान समिति होती थी। हमें महासभा के कार्यों के विषय में अधिक जानकारी है। यह गाँवों के वरिष्ठ ब्राह्मणों की सभा थी जिन्हें अग्रहार कहा जाता था। इन गाँवों में ब्राह्मण बसे हुए थे जिनकी अधिकांश भूमि कर मुक्त थी। ये गाँव अधिकांशतः स्वायत्तता का उपभोग करते थे। गाँव के कारोबार की देख-रेख एक प्रबंधकारिणी समिति करती थी जिसके लिए गाँव के शिक्षित धनवान व्यक्तियों में से सदस्यों का निर्वाचन पर्चें डालकर या क्रम से होता था। सदस्य प्रत्येक तीन वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते थे। भू-राजस्व निर्धारण और वसूली, कानून और व्यवस्था बनाये रखने तथा न्याय करने के लिए अन्य समितियाँ थीं। इन महत्वपूर्ण समितियों में एक सरोवर समिति भी थी जो खेतों की सिंचाई के लिए जल वितरण की देखरेख करती थी। महासभा नयी भू-व्यवस्था भी कर सकती थी और उसके ऊपर मालिकाना अधिकार का प्रयोग भी। यह गाँव हेतु ऋण उगाह सकती थी और कर लगा सकती थी। चोल गाँवों की स्वशासन व्यवस्था एक बहुत ही सुन्दर व्यवस्था थी। यह व्यवस्था कुछ हद तक अन्य गाँवों में भी थी। लेकिन सामन्तशाही के विकास से गाँवों का स्वायत्तशासन सीमित हो गया जिसका विवेचन बाद के अध्याय में किया गया है। सांस्कृतिक जीवनचोल साम्राज्य के विस्तार और द्रव्यसाधनों ने उनके शासकों को तंजौर, गंगई कोंड चोलपुरम, काँची इत्यादि जैसे बड़े नगरों को बनाने का सामर्थ्य प्रदान किया। शासकों ने अपने बड़े परिवारों के लिए भोजन-गृहों के साथ राजमहल, विशाल उद्यान और चबूतरे बनावाए। हमें पता चलता है कि उनके सरदारों के महल भी पाँच या सात मंजिले होते थे। दुर्भाग्य की बात है कि उन दिनों के महलों में से एक भी विद्यमान नहीं है। चोलों की राजधानी गंगई कोंड चोलपुरम्, तंजौर के निकट अब मात्र एक छोटे से गाँव के रूप में रह गया है। लेकिन इस युग के साहित्य में हमें चोल शासकों और उनके मन्त्रियों तथा बड़े व्यापारियों के विशाल महलों और उनके वैभव का वर्णन मिल जाता है।दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य के अंतर्गत मन्दिर स्थापत्यकला उन्नति के शिखर पर पहुँच गई थी। इस काल की स्थापत्यकला की शैली द्रविड़ शैली कहलायी क्योंकि यह विशेष रूप से दक्षिण भारत में सीमित थी। इसकी प्रमुख विशेषता यह थी कि मुख्य प्रतिमा-कक्ष या (गर्भ गृह) के ऊपर एक के ऊपर एक मंजिल का निर्माण होता था। इन मंजिलों की संख्या पाँच से सात तक होती थी। ये एक विशेष शैली में बनी होती थीं जिन्हें विमान कहते थे। स्तम्भों वाला बड़ा कमरा मंडप कहलाता था। प्रायः प्रतिमा कक्ष के सामने बारीक खुदाई वोल स्तम्भों पर टिकी सपाट छत वाला एक बड़ा कक्ष होता था, जिसे मंडप कहते थे। मंडप में सभाएँ होतीं और अनेक तरह के क्रिया-कलाप होते रहते थे, जिनमें देवदासियों का अनुष्ठानिक नृत्य शामिल था। देवदासियाँ ऐसी स्त्रियाँ होती थीं जो देवताओं की सेवा के लिए समर्पित थीं। भक्तों के परिक्रमा करने के लिए कभी-कभी पवित्र मन्दिर गर्भ के चारों तरफ एक गलियारा बना दिया जाता था। इस गलियारे में अनेक देवताओं की प्रतिमाएँ रखी जा सकती थीं। समग्र ढाँचा एक प्रांगण के अन्दर ऊँची दीवारों से घिरा होता था, जिसमें ऊँचे प्रवेश द्वार थे, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था। समय के साथ और ऊँचे विमान बनते गये, प्रांगणों की संख्या बढ़कर दो या तीन होती गयी और गोपुरम् अधिकारिक अंलकृत होते गये। इस प्रकार मन्दिर ने एक छोटे शहर या राजमहल का रूप धारण कर लिया जिसमें पुजारी तथा अन्य अनेक लोगों के निवास के लिए कमरे बने होते थे। मन्दिरों के खर्च के लिए राजस्वमुक्त भूमि की सुविधा थी। समृद्ध व्यापारियों से उन्हें अनुदान और प्रचुर चंदा मिलता था। इससे कुछ मन्दिर इतने धनवान बन गये थे कि वे व्यापार के क्षेत्र में प्रवेश कर ऋण देने और व्यापारिक कार्यों में सहायता करने लगे। आठवीं शताब्दी में बना मन्दिर स्थापत्यकला की द्रविड़ शैली का प्रारम्भिक उदाहरण, कांचीपुरम् का कैलाश मन्दिर है। इस शैली का उत्कृष्टतम और भव्य उदाहरण हमें तंजौर में राजराजा द्वारा निर्मित वृहदेश्वर मन्दिर में मिलता है। यह राजराजा मन्दिर के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि चोलों का स्वभाव था कि वे देवी-देवताओं की मूर्तियों के अतिरिक्त मन्दिरों में राजा और रानी की मूर्तियाँ भी स्थापित करते थे। गंगई कोंड चोलपुरम का मन्दिर यद्यपि जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, तथापि यह चोल साम्राटों के काल के मन्दिर-स्थापत्यकला का दूसरा उत्तम उदाहरण माना जा सकता है। दक्षिण भारत के अन्य स्थानों में भी बड़ी संख्या में मन्दिरों का निर्माण हुआ। यहाँ पर यह स्मरण रखना उचित होगा कि इन कार्यकलापों के लिए धन की प्राप्ति चोल साम्राटों द्वारा इस क्षेत्र की जनता को लूटने से होती थी। चोल साम्राज्य के पतन के पश्चात् चालुक्य और होयसल राजाओं के काल में भी मन्दिर निर्माण कार्य चलता रहा। धारवाड़ जिले और होयसलों की राजधानी हालेविड में भी बड़ी संख्या में मन्दिर हैं। इनमें से सबसे अधिक भव्य होयसलेश्वर का मन्दिर है। यह चालुक्य शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है इस मन्दिर में देवी-देवताओं की मूर्तियों के अतिरिक्त उनके सेवकों की मूर्तियाँ तथा स्त्री-पुरुषों (यक्ष और यक्षणी) की प्रतिमाएँ हैं। साथ ही साथ मंदिर के पटों पर व्यस्त जीवन के चित्र अत्यंत सुंदर ढंग से तराशे गये हैं जिनमें नृत्य, संगीत, युद्ध और प्रणय के दृश्य शामिल हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जीवन पूर्ण रूप से धर्म से जुड़ा हुआ था। जनसाधारण के लिए मन्दिर मात्र एक पूजा-स्थान ही नहीं वरन् सामाजिक और सांस्कृति जीवन का केन्द्र था। इस काल में दक्षिण भारत में मूर्तिकला उच्च स्तर तक पहुँची हुई थी। इसका एक उदाहरण श्रवण बेलगोला स्थित, जैन संत, गोमतेश्वर की विशालकाय प्रतिमा है। मूर्ति निर्माण कला का दूसरा पक्ष भी उन्नति की पराकष्ठा पर पहुँचा हुआ था जिसे हम नटराज शिव की नृत्य-मुद्राओं देखते हैं। नटराज की प्रतिमाएँ विशेषकर जो कास्य की हैं, इस काल की श्रेष्ठ कृति मानी जाती हैं। इसके अनेक उत्कृष्ठ उदाहरण भारत और विदेशों के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। इस काल में विभिन्न वंशों के राजाओं ने भी कला और साहित्य को संरक्षण प्रदान किया। संस्कृत उच्च संस्कृति की भाषा मानी जाती थी और कुछ नृपतियों के अतिरिक्त विद्ववानों और दरबारी कवियों ने इस भाषा में रचनाएँ कीं। क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्यिक विकास इस काल की असाधारण विशेषता थी। छठी और नौवीं शताब्दी के मध्य में शिव और विष्णु भक्त कुछ लोकप्रिय संत जिन्हें नयनार और अलवार कहा जाता है, तमिल क्षेत्र में फलते-फूलते थे। उन्होंने तमिल और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में रचनाएँ कीं। बारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में तीरूमूराई के नाम से ग्यारह खंडों में संग्रहित इन संतों की रचनाओं को पावन और पंचम वेद माना जाता है। ग्यारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध और बारहवीं शताब्दी के आरम्भ को कंबन का काल माना जाता है, जिसे तमिल साहित्य का स्वर्ग युग समझा जाता है, ‘कंबन की रामायण’ तमिल साहित्य का गौरव ग्रंथ माना जाता है। यह विश्वास किया जाता है कि कंबन चोल राजा के दरबार में रहते थे। अन्य कई साहित्यकारों ने रामायण और महाभारत को अपनी विषय वस्तु बनाकर इन गौरव ग्रन्थों को जनमानस तक पहुँचाया। तमिल के बाद कन्नड़ साहित्य भी इस काल की साहित्यिक भाषा बन गई। कन्नड़ के अतिरिक्त तेलुगू को भी राष्ट्रकूट, चालुक्य और होयसल राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया। राष्ट्रकूट राजा ‘अमोघवर्ष’ ने कन्नड़ में काव्य शास्त्र पर एक पुस्तक लिखी। अनेक जैन विद्वानों ने भी कन्नड़ साहित्य के विकास में योगदान दिया। पम्पा, पोन्ना और रन्ना कन्नड़ काव्य के तीन रत्न माने जाते हैं। यद्यपि वे जैन धर्म से प्रभावित थे फिर भी उन्होंने रामायण और महाभारत के प्रसंगों के आधार पर रचनाएँ कीं। चालुक्य राजा के दरबार में रहने वाले कवि नन्नैया ने महाभारत का अनुवाद तेलुगू में आरम्भ किया। इसके द्वारा आरम्भ किया गया यह कार्य तिकन्ना ने तेरहवीं शताब्दी में पूरा किया। तमिल रामायण की भाँति तेलुगू महाभारत भी गौरव ग्रन्थ माना जाता है। जिसने अनेक परवर्ती साहित्यकारों को प्रोत्साहित किया। इन साहित्यों में भी अनेक लोक प्रचलित प्रसंग पाये जाते हैं। ऐसी विषय-वस्तुएँ जो संस्कृत से नहीं ली गयी हैं, लेकिन वे लोकप्रिय मनोभावों और संवेगों को प्रतिबिंबित करती हैं, उन्हें तेलुगू में देशी या ग्रामीण कहा जाता है। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि आठवीं से बारहवीं शताब्दी तक का काल केवल दक्षिण भारत में राजनीतिक एकता के लिए ही स्मरण योग्य नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक विकास के लिए भी स्मरणीय है। इस काल में व्यापार और वाणिज्य की भी उन्नति हुई जिसके फलस्वरूप यह काल दक्षिण भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। | |||||||||
| |||||||||