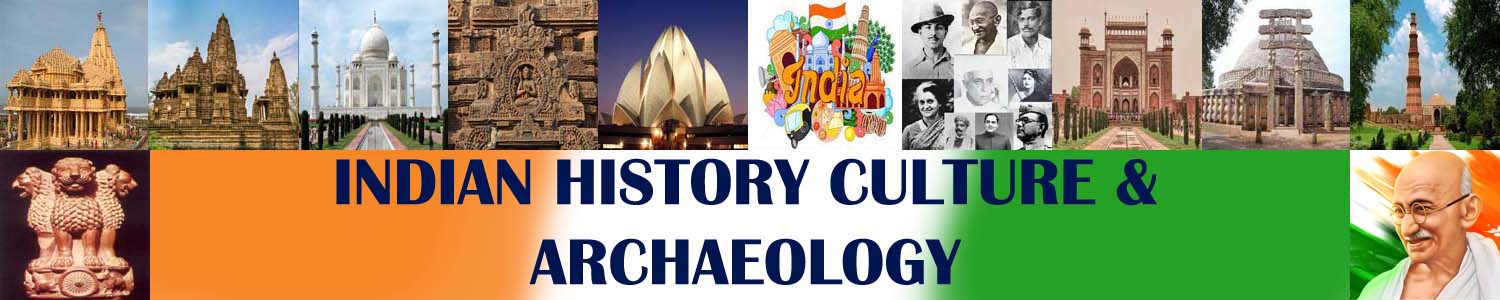| |||||||||
|
19वीं सदी में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण
जबर्दस्त बौद्धिक और सांस्कृतिक उथल पुथल उन्नीसवीं सदी के भारत की विशेषता थी। आधुनिक पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव और विदेशी शक्ति द्वारा पराजित होने की चेतना के चलते लोगों में नई जागृति पैदा हुई। जनता में इस बात का एहसास हो चुका था कि भारतीय सामाजिक ढाँचे और सांस्कृतिक दुर्बलताओं की वजह से मुट्ठी भर विदेशियों ने भारत को उपनिवेश में बदल दिया है। समझदार भारतीय लोगों ने अपने समाज की शक्ति तथा कमजोरी को जाना और इसकी कमजोरियों को दूर करने के उपाय भी खोजने लगे। भारत की बहुसंख्यक जनता ने पश्चिम के साथ समझौता करना अस्वीकार कर दिया। इन लोगों ने परंपरागत भारतीय विचारों और संस्थाओं में अपनी आस्था व्यक्त की। दूसरी बात यह थी कि लोग धीरे-धीरे यह मानने लगे कि अपने समाज में फिर से प्राण फूँकने के लिए आधुनिक पश्चिमी विचारों के कुछ तत्वों को आत्मसात करना पड़ेगा। मानवतावाद, विवेक पर आधारित सिद्धांतों और आधुनिक विज्ञान ने उन्हें खास तौर से प्रभावित किया, क्योंकि इस बात पर लोगों में मतभेद था कि किस प्रकार के सुधार किए जाएँ तथा कितना सुधार किया जाना चाहिए। लेकिन उन्नीसवीं शताब्दी के सभी बुद्धिजीवी इस विश्वास के थे कि सामाजिक और धार्मिक सुधारों की तत्काल जरूरत है।
राजा राममोहन रायइस जागरण के मुख्य नेता राममोहन राय थे जिन्हें आधुनिक भारत का प्रथम नेता मानना एकदम उचित है। अपने देश और जनता के प्रति गहरे प्रेम से प्रेरित होकर आजीवन उसके सामाजिक, धार्मिक, बौद्धिक और राजनीजिक नवोत्थान के लिए राममोहनराय ने कठिन परिश्रम किया। समसामयिक भारतीय समाज की जड़ता और भ्रष्टाचार से उन्हें काफी कष्ट हुआ। उस समय भारतीय समाज में जाति और परंपरा का बोलबाला था। लोकर्धम अंधविश्वासों से भरा हुआ था। इसका फायदा अज्ञानी लोग और भ्रष्ट पुरोहित उठाते थे। उच्च वर्ग के लोग स्वार्थी थे और उन लोगों ने अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए सामाजिक हितों की बलि दी। राममोहन राय के मन में प्राच्य दार्शनिक विचार-धाराओं के प्रति गहन प्रेम और आदर था। लेकिन वे यह भी सोचते थे कि केवल पश्चिमी संस्कृति से ही भारतीय समाज का पुनरूत्थान संभव था।खास तौर पर वे चाहते थे कि उनके देश के लोग विवेकशील दृष्टि और वैज्ञानिक सोच अपनाएँ तथा नर-नारियाँ मानवीय प्रतिष्ठा और सामाजिक समानता के सिद्धांत को स्वीकार कर लें। वे यह भी चाहते थे कि देश में आधुनिक पूँजीवादी उद्योग आंरभ किए जाएँ। राममोहन राय प्राच्य और पाश्चात्य चिंतन के संश्लिष्ट (मिलेजुले) रूप के प्रतिनिधि थे। वे विद्वान थे और संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, ग्रीक और हिब्रू सहित एक दर्जन से अधिक भाषाएँ जानते थे। युवावस्था में उन्होंने वाराणासी में संस्कृत साहित्य और हिंदू दर्शन तथा पटना में कुरान और फारसी तथा अरबी साहित्य का अध्ययन किया था। वे जैन धर्म और भारत के अन्य धार्मिक आंदोलनों तथा पंथों से अच्छी तरह परिचित थी। बाद में उन्होंने पाश्चात्य चिंतन और संस्कृति का गहरा अध्ययन किया। मूल बाइबिल का अध्ययन करने के लिए उन्होंने ग्रीक और हिब्रू भाषाएँ सीखीं। उन्होंने 1809 में फारसी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “एकेश्वरवादियों को उपहार” (Gift to Monotheists) लिखी जिसमें उन्होंने अनेक देवताओं में विश्वास के विरुद्ध और एकेश्वरवाद के पक्ष में वजनदार तर्क दिए। वे 1814 में कलकत्ता में बस गए और उन्होंने जल्द ही नौजवानों के एक समूह को अपनी ओर आकर्षित कर लिया जिनके सहयोग से उन्होंने आत्मीय सभा आरंभ की। तब से लेकर जीवन भर बंगाल के हिंदुओं में प्रचलित धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने एक जोरदार संघर्ष चलाया। विशेष रूप से उन्होंने मूर्तिपूजा, जाति की कट्टरता और निरर्थक धार्मिक कृत्यों के प्रचलन का जोरदार विरोध किया। इन रिवाजों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने पुरोहित वर्ग की निंदा की। उनकी धारणा थी कि सभी प्रमुख प्राचीन हिंदू धर्मग्रंथों ने एकेश्वरवाद की शिक्षा दी है। अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने वेदों औार पाँच प्रमुख उपनिषदों के बंगला अनुवाद प्रकाशित किए। उन्होंने एकेश्वरवाद के समर्थन में कई पुस्तक-पुस्तिकाएँ लिखीं। यद्यपि अपने दार्शनिक विचारों के समर्थन में उन्होंने प्राचीन विशेषज्ञों को उद्धत किया तथापि अंततोगत्वा उन्होंने मानवीय तर्क शक्ति का सहारा लिया जो, उनके विचार से, किसी भी सिद्धान्त-प्राच्य या पाश्चात्य-की सच्चाई की अंतिम कसौटी है। उनकी धारणा थी कि वेदांत-दर्शन मानवीय तर्क शक्ति पर आधारित है। किसी भी स्थिति में आदमी को तब पवित्र ग्रंथों, शस्त्रों और विरासत में मिली परंपराओं से हट जाने में नहीं हिचकिचाना चाहिए जब मानवीय तर्क शक्ति का वैसा तकाजा हो और वे परंपराएँ समाज के लिए हानिकारक सिद्ध हो रही हों। इस बात का उल्लेख जरूरी है कि राममोहन राय ने अपने विवेकशील दृष्टिकोण का प्रयोग केवल भारतीय धर्मों और परंपराओं तक ही सीमित नहीं रखा। उससे उनके अनेक ईसाई धर्मप्रचारक मित्रों को निराशा हुई जिन्होंने उम्मीद लगाई थी कि हिंदू धर्म की विवेकशील समीक्षा उन्हें ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए प्रेरित करेगी। राममोहन राय ने ईसाई धर्म, विशेषकर उसमें निहित अंध आस्था के तत्वों को भी विवेक शक्ति के अनुसार देखने पर जोर दिया। उन्होंने 1820 में ‘प्रीसेप्ट्स आफ जीसस’ (Precepts of Jesus) नाम की पुस्तक प्रकाशित की जिसमें उन्होंने ‘न्यू टेस्टामेंट’ के नैतिक और दार्शनिक संदेश को उसकी चमत्कारी कहानियों से अलग करने की कोशिश की। उन्होंने ‘न्यू टेस्टामेंट’ के नैतिक और दार्शनिक संदेश की प्रशंसा की। वे चाहते थे कि ईसा मसीह के उच्च नैतिक संदेश को हिंदू धर्म में समाहित कर लिया जाए। इससे ईसाई धर्म प्रचारक उनके विरोधी बन गए। इस प्रकार राममोहन राय का मानना था कि न तो भारत के भूतकाल पर आँखें मूँदकर निर्भर रहा जाए और न ही पश्चिम का अंधानुकरण किया जाए। दूसरी ओर, उन्होंने ये विचार रखे कि विवेक बुद्धि का सहारा लेकर नए भारत को सर्वोत्तम प्राच्य और पाश्चात्य विचारों को प्राप्त कर संजो रखना चाहिए। अतः उन्होंने चाहा कि भारत पश्चिमी देशों से सीखे, मगर सीखने की यह क्रिया एक बौद्धिक और सर्जनात्मक प्रक्रिया हो जिसके द्वारा भारतीय संस्कृति और चिंतन में जान डाल दी जाए। इस प्रक्रिया का अर्थ भारत पर पाश्चात्य संस्कृति को थोपना नहीं हो। इसलिए वे हिंदू धर्म में सुधार के हिमायती और हिंदू धर्म की जगह ईसाई धर्म लाने के विराधी थे। उन्होंने ईसाई धर्म प्रचारकों को हिंदू धर्म और दर्शन पर आज्ञापूर्ण आलोचनाओं का जवाब दिया। साथ ही उन्होंने अन्य धर्मों के प्रति अत्यंत मित्रतापूर्ण रूख अपनाया। उनका विश्वास था कि बुनियादी तौर पर सभी धर्म एक ही संदेश देते हैं कि उनके अनुयायी भाई-भाई हैं। जिंदगी भर राममोहन राय को अपने निडर धार्मिक दृष्टिकोण के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। रूढ़िवादियों ने मूर्ति पूजा की आलोचना तथा ईसाई धर्म और इस्लाम की दार्शनिक दृष्टिकोण से प्रशंसा करने के कारण उनकी निंदा की। उन्होंने उनका सामाजिक तौर पर बहिष्कार किया। उनकी माँ ने भी बहिष्कार करने वालों का साथ दिया। उन्हें विधर्मी और जातिबहिष्कृत कहा गया। उन्होंने 1829 में ब्रह्मसमाज नाम की एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की जिसको बाद में ब्रह्मसमाज कहा गया। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना और एकेश्वरवाद की शिक्षा देना था। नई संस्था को दो आधार थे, तर्क शक्ति और वेद तथा उपनिशद। उसे अन्य धर्मों की शिक्षाओं को भी समाहित करना था। ब्रह्मसमाज ने मानवीय प्रतिष्ठा पर जोर दिया, मूर्तिपूजा का विरोध किया तथा सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों की आलोचना की। राममोहन राय एक महान चिंतक थे और कर्मठ व्यक्ति थे। राष्ट्र-निर्माण का शायद ही कोई पहलू था जिसे उन्होंने अछूता छोड़ा हो। वस्तुतः जैसे उन्होंने हिंदू धर्म के अंदर रहकर सुधारने का काम आरंभ किया, वैसे ही उन्होंने भारतीय समाज के सुधार के लिए आधार तैयार किया। सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध उनके आजीवन जेहाद का सबसे बढ़िया उदाहरण अमानवीय सती प्रथा के खिलाफ ऐतिहासिक आंदोलन था। उन्होंने 1818 में इस प्रश्न पर जनमत खड़ा करने का काम आरंभ किया। एक ओर पुराने शास्त्रों का प्रमाण देकर दिखलाया कि हिंदू धर्म सती प्रथा के विरोध में था, दूसरी ओर उन्होंने लोगों की तर्क शक्ति, मानवीयता और दया भाव की दुहाई दी। वे कलकत्ता के शमशानों में जाते और विधवाओं के रिश्तेदारों से उनके आत्मदाह के कार्यक्रम को त्याग देने के लिए समझाते-बुझाते। उन्होंने समान विचार वाले लोगों को संगठित किया जो इन कृत्यों पर कढ़ी निगाह रखें और विधवाओं को सती होने के लिए मजबूर करने की हर कोशिश को रोकें। जब रूढ़िवादी हिंदुओं ने संसद को याचिका दी कि वह सती प्रथा पर पाबंदी लगाने संबंधी बैंटिक की कार्रवाई को मंजूरी न दे तब उन्होंने बैंटिक की कार्रवाई के पक्ष में प्रबुद्ध हिंदुओं की ओर से एक याचिका दिलवाई। वे औरतों के पक्के हिमायती थे। उन्होंने औरतों की परवशता की निंदा की तथा इस प्रचलित विचार का विरोध किया कि औरतें पुरूषों से बुद्धि में या नैतिक दृष्टि से निकृष्ट हैं। उन्होंने बहुविवाह तथा विधवाओं की अवनत स्थिति की आलोचना की। औरतों की स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने माँग की कि उन्हें विरासत और संपत्ति संबंधी अधिकार दिए जाए। राममोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से थे। वे आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रचार का प्रमुख साधन समझते थे। डेविड हेअर ने 1817 में कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की। वह 1800 में एक घड़ीसाज के रूप में भारत आया था, मगर उसने अपनी सारी जिंदगी देश में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में लगा दी। हिंदू कॉलेज की स्थापना और उसकी अन्य शिक्षा संबंधी परियोजनाओं के लिए राममोहन राय ने हेअर को अत्यंत जोरदार समर्थन दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने कलकत्ता में 1817 से अपने खर्च से एक अंग्रेजी स्कूल चलाया जिसमें अन्य विषयों के साथ ही यांत्रिकी (Mechanics) और वाल्तेयर के दर्शन की पढ़ाई होती थी। उन्होंने 1825 में एक वेदान्त कालेज की स्थापना की जिसमें भारतीय विद्या और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञानों की पढ़ाई की सुविधाएँ उपलब्ध थीं। राममोहन राय बंगाल में बंगला को बौद्धिक संपर्क का माध्यम बनाने के लिए समान रूप से उत्सुक थे। उन्होंने बंगला व्याकरण पर एक पुस्तक की रचना की। अपने अनुवादों, पुस्तिकाओं तथा पत्र-पत्रिकाओं के जरिए बंगला भाषा की एक आधुनिक और सुरूचिपूर्ण शैली विकसित करने में उन्होंने सहायता दी। भारतीय में राष्ट्रीय चेतना के उदय की पहली झलक का राममोहन प्रतिनिधित्व करते थे। एक स्वतंत्र और पुनरूत्थानशील भारत का स्वप्न उनके चिंतन और कार्यों का मार्गदर्शन करता था। उनका विश्वास था कि भारतीय धर्मों और समाज से भ्रष्ट तत्वों को जड़मूल से उखाड़ फेंकने की कोशिश कर और एकेश्वरवाद का वैदांतिक संदेश देकर वे भिन्न-भिन्न समूहों में बँटे भारतीय समाज की एकता का आधार तैयार कर रहे थे। उन्होंने जातिप्रथा की कट्टरता का विशेष रूप से विरोध किया, जो, उनके अनुसार, “हमारे बीच एकता के अभाव का स्रोत रहा है।” उनका ख्याल था कि जतिप्रता दोहरी कुरीति है - उसने असमानता पैदा की है और जनता को विभाजित किया है और उसे “देशभक्ति की भावनाओं से वंचित रखा है।” इस प्रकार, उनके अनुसार, धार्मिक सुधार का एक लक्ष्य राजनीतिक उत्थान था। राममोहन राय भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत थे। जनता के बीच वैज्ञानिक, साहित्यिक और राजनीतिक ज्ञान के प्रचार, तात्कालिक दिलचस्पी के विषयों पर जनमत तैयार करने और सरकार के सामने जनता की माँगों और शिकायतों को रखने के लिए उन्होंने बंगला, फारसी, हिंदी और अंग्रेजी में पत्र-पत्रिकाएँ निकालीं। वे देश के राजनीतिक प्रश्नों पर जन-आंदोलन के प्रवर्तक भी थे। बंगाल के जमींदारों की उत्पीड़क कार्रवाइयों की उन्होंने निंदा की, जिन्होंने किसानों को दयनीय स्थिति में पहुँचा दिया था। उन्होंने माँग की कि वास्तविक किसानों द्वारा दिए जाने वाले अधिकतम लगान को सदा के लिए निश्चित कर दिया जाना चाहिए जिससे वे भी 1793 के स्थायी बंदोबस्त से फायदा उठा सकें। उन्होंने लाखिराज (rent-free) जमीन पर लगान निर्धारित करने के प्रयासों के प्रति भी विरोध प्रकट किया। उन्होंने कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को खत्म करने तथा भारतीय वस्तुओं पर से भारी निर्यात शुल्कों को हटाने की भी माँग की और उच्च सेवाओं के भारतीयकरण कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से अलग करने, जूरी के जरिए मुकदमों की सुनवाई और भारतीयों तथा यूरोपवासियों के बीच न्यायिक समानता की भी उन्होंने माँग की। अंतर्राष्ट्रीयता और राष्ट्रों के बीच मुक्त सहयोग में राममोहन का पक्का विश्वास था। कवि रवींद्रनाथ ठाकुर ने ठीक ही लिखा है, “राममोहन अपने समय में, संपूर्ण मानव समाज में एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को पूरी तरह समझा। वे जानते थे कि मानव सभ्यता का आदर्श अलग-अलग रहने में नहीं बल्कि चिंतन और क्रिया के सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों तथा राष्ट्रों के आपसी भाई चारे में निहित है।” राममोहन राय ने अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में गहरी दिलचस्पी ली और हर जगह उन्होंने स्वतंत्रता, जनतंत्र और राष्ट्रीयता के आंदोलन का समर्थन तथा हर प्रकार के अन्याय, उत्पीड़न और जुल्म का विरोध किया। 1821 में नेपल्स में क्रांति की विफलता की खबर से वे इतने दुखी हो गए कि उन्होंने अपने सारे सामाजिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया। दूसरी ओर, स्पेनिश अमरीका में 1823 में क्रांति की सफलता पर उन्होंने एक सार्वजनिक भोज देकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। आयरलैंड की दूरस्थ जमींदारों के उत्पीड़क राज में दयनीय स्थिति की उन्होंने निंदा की। उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि अगर संसद रिफार्म बिल पास करने में असफल रही तो वे ब्रिटिश साम्राज्य छोड़कर चले जाएँगे। सिंह की तरह राममोहन निडर थे। किसी उचित उद्देश्य का समर्थन करने में वे कभी नहीं हिचकिचाए। सारी जिंदगी व्यक्तिगत हानि और कठिनाई सहकर भी उन्होंने सामाजिक अन्याय और असमानता के खिलाफ संघर्ष किया। समाजसेवा करते हुए उनका बहुधा अपने परिवार, धनी जमींदार और शक्तिशाली धर्म प्रचारकों, उच्च अफसरों और विदेशी अधिकारियों से टकराव हुआ। मगर वे न तो कभी डरे और न ही कभी अपने अपनाए हुए रास्ते से विचलित हुए। उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्ध में वे भारतीय आकाश के सबसे चमकीले सितारे जरूर थे मगर वे अकेले सितारे नहीं थे। उनके अनेक विशिष्ट सहयोगी, अनुयायी और उत्तराधिकारी थे। शिक्षा के क्षेत्र में डच घड़ीसाज डैविड हेअर और स्कॉटिश धर्म प्रचारक अलेक्जेंडर डफ्फ ने उनकी बड़ी सहायता की। अनेक भारतीय सहयोगियों में द्वारका नाथ टैगोर सबसे प्रमुख थे। उनके अन्य प्रमुख अनुयायी थे, प्रसन्न कुमार टैगोर, चंद्रशेखर देव और ब्रह्मसभा के प्रथम मंत्री ताराचंद चक्रवर्ती। डेरोजिअन और यंग बंगालउन्नीसवीं सदी के तीसरे दशक के अंतिम वर्षों तथा चौथे दशक के दौरान बंगाली बुद्धिजीवियों के बीच एक आमूल परिवर्तनकारी प्रवृत्ति पैदा हुई। यह प्रवृत्ति राममोहन राय की अपेक्षा अधिक आधुनिक थी और उसे यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जाना जाता हैं। उसका नेता और प्रेरक नौजवान एंग्लो इंडियन हेनरी विवियन डेरोजिओं था। डेरोजिओ का जन्म 1809 में हुआ था। उसने 1826 से 1831 तक हिन्दू कॉलेज में पढ़ाया। डेरोजिओ में आश्चर्यजनक प्रतिभा थी। उसने महान फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा ग्रहण की और अपने जमाने के अत्यंत क्रांतिकारी विचारों को अपनाया। वह अत्यन्त प्रतिभाशाली शिक्षक था जिसने अपनी युवावस्था के बावजूद अपने इर्द-गिर्द अनेक तेज और श्रद्धालु छात्रों को विवेकपूर्ण और मुक्त ढंग से सोचने सभी आधारों की प्रामाणिकता की जाँच करने, मुक्ति, समानता और स्वतंत्रता से प्रेम करने तथा सत्य की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। डेरोजिओं और उसके प्रसिद्ध अनुयायी जिन्हें डेरोजिअन और यंग बंगाल कहा जाता था, प्रचंड देशभक्त थे। डेरोजिओं आधुनिक भारत का शायद प्रथम राष्ट्रवादी कवि था। उदाहरण के लिए, उसने 1827 में लिखा -My country ! in the days of glory past Land of the Gods and lofty name; But woe me ! I never shall live to behold, डेरोजिओ को उसकी क्रांतिकारिता के कारण 1831 में हिंदू कॉलेज से हटा दिया गया और वह उसके तुरंत बाद 22 वर्ष की युवावस्था में हैजे से मर गया। उसके अनुयायियों ने पुरानी और हृासोन्मुख प्रथाओं, कृत्यों और रिवाजों की घोर आलोचना की। वे नारी अधिकारों के पक्के हिमायती थे। उन्होंने नारी-शिक्षा की माँग की किंतु वे किसी आंदोलन को जन्म देने में सफल नहीं हुए क्योंकि उनके विचारों को फलने-फूलने को लिए सामाजिक स्थितियाँ उपयुक्त नहीं थी। उन्होंने किसानों के मसायल के सवाल को नहीं उठाया और उस समय भारतीय समाज में ऐसा कोई और वर्ग या समूह नहीं था जो इनके प्रगतिशील विचारों का समर्थन करता। यही नहीं, वे जनता के साथ अपने संपर्क नहीं बना सके। वस्तुतः उनकी क्रांतिकारिता किताबी थी, वे भारतीय वास्तविकता को पूरी तरह से समझने में असफल रहे। इतना होते हुए भी, डेरोजिओ के अनुयायियों ने जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रश्नों पर सामाचारपत्रों, पुस्तिकाओं और सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा शिक्षित करने की राममोहन राय की परंपरा को आगे बढ़ाया। उन्होंने कंपनी के चार्टर (सनद) के संशोधन, प्रेस की स्वतंत्रता, विदेश स्थित ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीय मजदूरों के साथ बेहतर व्यवहार, जूरी द्वारा मुकदमों की सुनवाई, अत्याचारी जमींदारों से रैयतों की सुरक्षा और सरकारी सेवाओं के उच्चतर वेतनमानों में भारतीयों को रोजगार देने जैसे सार्वजनिक प्रश्नों पर आम आंदोलन चलाए। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसिद्ध नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरोजिओं के अनुयायियों को “बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत, हमारी जाति के पिता कहा जिनके सद्गुण उनके प्रति श्रद्धा पैदा करेंगे और जिनकी कमजोरियों पर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा।” देवेन्द्रनाथ टैगोर और ईश्वरचन्द्र वि़द्यासागरब्रह्मसमाज बना रहा मगर उसमें कोई खास दम नहीं था। रवींद्रनाथ ठाकुर के पिता देवेन्द्रनाथ ठाकुर ने उसे पुनर्जीवित किया। देवेंद्रनाथ भारतीय विद्या की सर्वोत्तम परंपरा तथा नवीन पाश्चात्य चिंतन की उपज थे। उन्होंने राममोहन राय के विचारों के प्रचार के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। उसमें राममोहन राय और डेरोजिओ के प्रमुख अनुयायी तथा ईश्वरचंद्र विद्यासागर और अक्षय कुमार दत्त जैसे स्वतंत्र चिंतक शामिल हो गए। तत्वबोधिनी सभा और उसके मुख्य पत्र ‘तत्वबोधिनी’ पत्रिका ने बंगला भाषा में भारत के सुव्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दिया। उसने बंगाल के बुद्धिजीवियों को विवेकशील दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। 1843 में देवेंद्रनाथ ठाकुर ने ब्रह्मसमाज का पुनर्गठन किया और उसमें नया जीवन डाला। समाज ने सक्रिय रूप से विधवा पुनिर्विवाह, बहुविवाह के उन्मूलन, नारीशिक्षा, रैयत की दशा में सुधार और आत्म संयम के आंदोलन का समर्थन किया।भारत में उस समय एक दूसरा बड़ा व्यक्तित्व उभर कर सामने आया। यह व्यक्तित्व पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर का था। विद्यासागर महान विद्वान और समाज-सुधारक थे। उन्होंने अपना सारा जीवन समाज सुधार के कार्य में लगा दिया। उनका जन्म 1820 में एक गरीब परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने को शिक्षित करने के लिए कठिनाइयों से संघर्ष किया और अंत में वे संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल के पद पर पहुँचे। यद्यपि वे संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे तथापि उनके दिमाग के दरवाजे पाश्चात्य चिंतन में जो कुछ सर्वोत्तम था उसके लिए खुले हुए थे। वे भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति के एक सुखद संयोग का प्रतिनिधित्व करते थे। इन सब के अलावा उनकी महानता उनकी सच्चरित्रता और प्रखर प्रतिभा में निहित थी। उनमें असीम साहस था तथा उनके दिमाग में किसी प्रकार का भय नहीं था। जो कुछ भी उन्होंने सही समझा उसे कार्यान्वित किया। उनकी धारणाओं और कार्य, तथा उनके चिंतन और व्यवहार के बीच कोई खाई नहीं थी। उनका पहनावा सादा, उनकी आदतें स्वाभाविक और व्यवहार सीधा था। वे एक महान मानवतावादी थे। उनमें गरीबों, अभागों और उत्पीड़ित लोगों के लिए अपार सहानुभूति थी। बंगाल में आज भी उनके उदात्त चरित्र, नैतिक गुणों और अगाध मानवतावाद के संबंध में अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं। उन्होंने सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे दिया क्योंकि वे अनुचित सरकारी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं कर सके। गरीबों के प्रति उनकी उदारता अचंभे में डालने वाली थी। शायद ही कभी उनके पास कोई गर्म कोट रहा क्योंकि निरपवाद रूप से उन्होंने अपना कोट जो भी नंगा सड़क पर पहले मिला, उसे दे दिया। आधुनिक भारत के निर्माण में विद्यासागर का योगदान अनेक प्रकार का था। उन्होंने संस्कृत पढ़ाने के लिए नई तकनीक विकसित की। उन्होंने एक बंगला वर्णमाला लिखी जो आज तक इस्तेमाल में आती है। उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा बंगला में आधुनिक शैली के विकास में सहायता दी। उन्होंने संस्कृत कॉलेज के दरवाजे गैर-ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए खोल दिए क्योंकि वे संस्कृत के अध्ययन पर ब्राह्मण जाति के तत्कालीन एकाधिकार के विराधी थे। संस्कृत अध्ययन को स्वगृहीत अलगाव के नुकसानदेह प्रभावों से बचाने के लिए उन्होंने संस्कृत कॉलेज में पाश्चात्य चिंतन का अध्ययन आरंभ किया। उन्होंने एक कॉलेज की स्थापना में सहायता दी जो अब उनके नाम पर है। सबसे अधिक, विद्यासागर को उनके देशवासी भारत की पद्दलित नारी जाति को ऊँचा उठाने में उनके योगदान के कारण आज भी याद करते हैं। इस क्षेत्र में वे राममोहन राय के सुयोग्य उत्तराधिकारी सिद्ध हुए। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए एक लंबा संघर्ष चलाया। उनके मानवतावाद को हिंदू विधवाओं के कष्टों ने पूरी तरह उभारा। उन्होंने उनकी दशा को सुधारने के लिए अपना सब कुछ दे दिया और अपने को वस्तुतः बर्बाद कर लिया। उन्होंने 1855 में विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में अपनी शक्तिशाली आवाज उठाई और इस काम में अगाध परंपरागत विद्या का सहारा लिया। जल्द ही विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में एक शक्तिशाली आंदोलन आरंभ हो गया जो आज तक चल रहा है। 1855 के अंतिम दिनों में बंगाल, मद्रास, बंबई, नागपुर और भारत के अन्य शहरों से सरकार को बड़ी संख्या में याचिकाएँ दी गईं। जिनमें विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी बनाने के लिए एक ऐक्ट पास करने का अनुरोध किया। यह आंदोलन सफल रहा और एक कानून बनाया गया। हमारे देश की उच्च जातियों में पहला कानूनी हिंदू विधवा पुनर्विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 को विद्यासागर की प्रेरणा से और उनकी ही देख-रेख में हुआ। देश के विभिन्न भागों में अनेक अन्य जातियों की विधवाओं को प्रचलित कानून को तहत यह अधिकार पहले से ही प्राप्त था। एक प्रत्यक्ष-दृष्टा ने उपर्युक्त विधवा पुनर्विवाह समारोह का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में किया है - “मैं वह दिन कभी नहीं भुला पाऊँगा जब पंडित विद्यासागर अपने मित्र, दूल्हे के साथ एक बड़ी बारात में आगे-आगे आए तब दर्शकों की भीड़ इतनी बड़ी थी कि घूमने-फिरने के लिए एक इंच जगह भी नहीं थी और कई लोग बड़े नालों में गिर गए, उन दिनों कलकत्ता की सड़कों के किनारे नाले बने होते थे। समारोह के बाद हर जगह चर्चा का यह विषय बन गया, बाजारों और दुकानों में, सड़कों पर, सार्वजनिक चौराहों पर, छात्रवासों में, भद्र लागों की बैठकों में, दफ्तरों और दूर ग्रामीण घरों में इसकी चर्चा होने लगी, जहाँ औरतों ने भी बड़ी गंभीरता से उस पर आपस में विचार-विमर्श किया। शांतिपुर के बुनकरों ने एक विचित्र प्रकार की स्त्रियों की साड़ी तैयार की जिसके किनारों पर एक नव-रचित गीत की पंक्ति बुनी गई थी जिसमें कहा गया था “विद्यासागर चिरंजीवी हों।” विधवा पुनर्विवाह की वकालत करने के कारण विद्यासागर को पोंगापंथी हिंदुओं की कटु शत्रुता का सामना करना पड़ा। कभी-कभी उनकी जान लेने की धमकी दी गई। किंतु निडर होकर वे अपने रास्ते पर आगे बढ़े। उनके इस काम में जरूरतमंद दंपत्तियों की आर्थिक सहायता भी शामिल थी। उनके प्रयासों से, 1855 और 1860 के बीच 25 विधवा पुनर्विवाह हुए। विद्यासागर ने 1850 में बालविवाह का विरोध किया। उन्होंने जीवन भर बहुर्विवाह के विरूद्ध आंदोलन चलाया। वे नारी-शिक्षा में भी गहरी दिलचस्पी रखते थे। स्कूलों के सरकारी निरीक्षक की हैसियत से उन्होंने 25 बालिका विद्यालयों की स्थापना की जिनमें से कई को उन्होंने अपने खर्च से चलाया। बेथुन स्कूल के मंत्री की हैसियत से वे उच्च नारी-शिक्षा के अग्रदूतों में से थे। पश्चिमी भारत में सुधारों के प्रणेताबेथुन स्कूल की स्थापना 1849 में कलकत्ता में हुई। वह नारी-शिक्षा के लिए उन्नीसवीं सदी के पाँचवें और छठे दशकों में चलाए गए शक्तिशाली आंदोलन का पहला परिणाम था। यद्यपि नारी-शिक्षा भारत के लिए कोई नई चीज नहीं थी, यद्यपि उसके विरूद्ध काफी पूर्वाग्रह व्याप्त था। कुछ लोगों की यह भी धारणा थी कि शिक्षित औरतें अपने पतियों को खो बैठेंगी। लड़कियों को आधुनिक शिक्षा देने की दिशा में सबसे पहले 1821 में ईसाई धर्म प्रचारकों ने कदम उठाए। मगर ईसाई धार्मिक शिक्षा पर जोर देने के कारण उनके प्रयास सफल नहीं हो सके। बेथुन स्कूल को विद्यार्थी प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई हुई। युवा छात्राओं के खिलाफ नारे लगाए गए और उन्हें गालियाँ दी गईं। कई बार उनके अभिभावकों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। अनेक लोगों का ख्याल था कि पाश्चात्य शिक्षा पाने वाली लड़कियाँ अपने पतियों को अपना गुलाम बना देंगी।बंगाल पर पाश्चात्य विचारों का असर काफी पहले महसूस किया गया था, पश्चिमी भारत में यह असर अपेक्षाकृत बाद में महसूस किया गया था। 1818 में ही बंगाल प्रभावशाली ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया था। बंबई के बालशास्त्री जांबेकर प्रथम सुधारकों में से थे जिन्होंने ब्राह्मणवादी कट्टरता की आलोचना की और हिंदुओं की आम प्रथाओं में सुधार लाने की कोशिश की। 1832 में उन्होंने ‘दर्पण’ नाम के एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था। इस पत्रिका के उद्देश्य इस प्रकार थे - “अज्ञान और त्रुटियों के धुंध को दूर भगाना, जिनके कारण लोगों के दिमाग बंद हो गए थे तथा लोगों पर ऐसा प्रकाश डालना जिस प्रकाश से दूसरे देशों की तुलना में यूरोप के लोग दुनिया में आगे बढ़ चुके थे।” 1849 में महाराष्ट्र में “परमहंस मंडली” की स्थापना की गईं। इसके संस्थापक आस्तिक थे तथा मूल रूप से उनकी दिलचस्पी जातपात के बंधनों को तोड़ने में थी। जब इसकी बैठक होती थी तब इसके सदस्य तथाकथित नीच जातियों के हाथ का पकाया हुआ भोजन करते थे। विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा में भी वे विश्वास करते थे। इस मंडली की शाखाएँ पूना, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य नगरों में भी स्थापित की गई। नौजवानों के ऊपर इस मंडली के प्रभाव को याद करते हुए प्रसिद्ध इतिहासकार आर. जी. भंडारकर लिखते हैं : “शाम के समय जब हम लोग बाहर टहलने के लिए निकलते थे तब जातपात के भेदभाव के विषय में आपस में बातचीत करते थे और इस पर भी बात होती थी कि ऊँच नीच के भेदभाव की वजह से देश का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हैं। इस बात की भी चर्चा होती थी कि इनको दूर किए बिना देश की असली तरक्की हो ही नहीं सकती है।” कुछ पढ़े लिखे युवकों ने मिलकर 1848 में छात्रों की एक साहित्यिक और वैज्ञानिक संस्था बनाई। इसकी दो शाखाएँ थीं - गुजराती और मराठी ध्यान प्रसारक मंडलियाँ। यह मंडलियाँ सामाजिक प्रश्नों और आम वैज्ञानिक विषयों पर व्याख्यान आयोजित किया करती थीं। महिलाओं की शिक्षा के लिए स्कूल आरंभ करना भी इस संस्था के लक्ष्यों में एक लक्ष्य था। 1851 में ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी ने पूना में लड़कियों का एक स्कूल खोला। इसके तत्काल बाद और कई स्कूल खुल गए। इन स्कूलों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने वालों में जगन्नाथ सेठ और भाऊ दाजी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। फुले महाराष्ट्र में विधवा विवाह आंदोलन की अगली पंक्ति के नेता थे। 1850 में विष्णु शास्त्री पंडित ने “विधवा-विवाह समाज” स्थापित किया। करसोनदास मलजी इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण कार्यकर्ता थे। 1852 में उन्होंने गुजराती भाषा में विधवा विवाह के समर्थन के लिए “सत्य प्रकाश” नाम की पत्रिका निकाली। महाराष्ट्र में नई शिक्षा और नए सामाजिक सुधारों के प्रवक्ता गोपाल हरि देशमुख थे, जो आगे चलकर ‘लोकहितवादी’ उपनाम से विख्यात हुए। आधुनिक, मानवतावादी तथा धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और विवेकसंगत सिद्धांतों को आधार पर भारतीय समाज के पुनर्गठन की उन्होंने वकालत की। ज्योतिबा फुले नीची मानी जाने वाली माली जाति में पैदा हुए थे। महाराष्ट्र के गैर-ब्राह्मण और अछूत जातियों की दयनीय सामाजिक स्थिति को वे भी अच्छी तरह समझते थे। ऊँची जातियों के प्रभुत्व और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के खिलाफ वे जीवन भर अभियान चलाते रहे। दादाभाई नौरोजी बंबई के दूसरे प्रमुख समाज सुधारक थे। ‘पारसी धर्म सुधार संगठन’ के संस्थापकों में वे थे। पारसी कानून संघ के जन्मदाताओं में भी वे थे। इस संगठन ने महिलाओं को कानूनी हक दिलाने के लिए तथा पारसी लोगों की शादी और उत्तराधिकार संबंधी समान कानून बनाने के लिए आंदोलन किए। सुधारकों ने शुरु से अपना संघर्ष मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं के अखबारों और साहित्य के माध्यम से चलाया। भारतीय भाषाएँ अपनी भूमिका सफलतापूर्वक निभा सकें, इसके लिए उन्होंने प्रारंभिक पाठ्यपुस्तकें बनाने जैसा काम भी अपने हाथ में लिया। उदाहरण के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर तथा रवींद्रनाथ ठाकुर, दोनों ही महानुभावों ने बंगला की प्रारंभिक कक्षाओं के लिए पाठ्य-पुस्तकें तैयार कीं। इन पुस्तकों को आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वास्तव में आम जनता के बीच आधुनिक तथा सुधारवादी विचारों का प्रसार मूलतः भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही हुआ। यह बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए कि उन्नीसवीं शताब्दी के सुधारकों का महत्व उनकी संख्या के आधार पर नहीं तय किया जाना चाहिए। वास्तव में वे लोग तो नई धारा के प्रवर्तक थे। उन्हीं के विचारों और क्रियाकलापों का नए भारत की रचना पर निर्णायक असर पड़ा। | |||||||||
| |||||||||