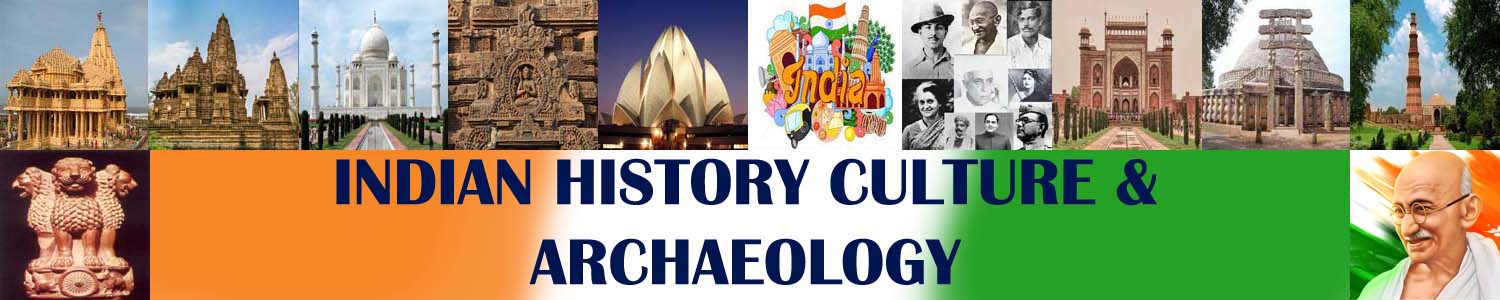| |||||||||
|
भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
राष्ट्रवादी आंदोलन, 1858-1905उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना बहुत तेजी से विकसित हुई और भारत में एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ हुआ। दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव पड़ी। आगे चल कर इसी के नेतृत्व में विदेशी शासन से स्वतंत्रता के लिए भारतीयों ने एक लंबा और साहसपूर्ण संघर्ष चलाया और अंत में 15 अगस्त 1947 को भारत मुक्त हो गया।विदेशी प्रभुत्व के परिणामआधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद बुनियादी तौर पर विदेशी आधिपत्य की चुनौती के जवाब़ रूप में उदित हुआ। स्वयं ब्रिटिश शासन की पीरिस्थितियों ने भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावना विकसित करने में सहायता दी। ब्रिटिश शासन तथा उनके प्रत्यक्ष और परोक्ष परिणाम ने ही भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के लिए भौतिक नैतिक और बौद्धिक परिस्थितियाँ तैयार कीं।इस आंदोलन की जड़े भारतीय जनता के हितों तथा भारत में ब्रिटिश हितों के टकराव में थीं। अंगेजों ने अपने हितों को पूरा करने के लिए ही भारत को अधीन बनाया था इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर वे भारत का शासन चलाते थे। वे अक्सर ब्रिटेन के लाभ के लिए भारतीयों की भलाई को भी ध्यान में नही रखते थे। धीरे-धीरे भारतीयों ने अनुभव किया कि लंकाशायर के उद्योगपतियों तथा अंगेजों के दूसरे प्रमुख वर्गों के हितों के लिए उनके अपने हितों का बलिदान दिया जाता रहा है। स्वयं ब्रिटिश शासन भारत के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण बनता गया और भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का आधार यही तथ्य था। यह भारत के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक तथा राजनीतिक विकास में प्रमुख बाधक तत्व बन चुका था। इससे भी बढ़ी बात यह है कि अधिक संख्या में भारतीय इस तथ्य को स्वीकार करने लगे थे और उनकी यह संख्या बढ़ती जा रही थी। भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक समूह ने धीरे-धीरे यह देखा कि उसके हित अंग्रेज शासकों के हाथों में असुरक्षित हैं। किसान देख रहे थे कि सरकार जमीन की मालगुजारी के नाम पर उनकी उपज का एक बड़ा हिस्सा उनसे ले लेती थी। सरकार और उसकी पुलिस, उसकी अदालतें और उसके अधिकारी, सभी उन जमींदारों और भूस्वामियों के समर्थक और रक्षक जो किसान से कसकर लगान वसूलते थे, वे उन व्यापारियों तथा सूदखोंरों के रक्षक थे जो तरह-तरह से किसान को धोखा देते, उसका शोषण करते तथा उसकी जमीन उससे छीन लेते थे। जब कभी किसान जमींदारों और सूदखोरों के दमन के खिलाफ उठ खड़े होते, पुलिस तथा सेना कानून और व्यवस्था के नाम पर उनको कुचल दिया करती थी। दस्तकार और शिल्पी यह महसूस कर रहे थे कि सरकार विदेशी प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर उनको तबाह कर रही थी और उनके पुनर्वास के लिए कुछ नहीं कर रही थी। आगे चलकर बीसवीं शताब्दी में आधुनिक कारखानों, खदानों तथा बागानों के मजदूरों ने भी पाया कि सारी जबानी हमदर्दी के बावजूद सरकार पूँजीपतियों का, खासकर विदेशी पूँजीपतियों का ही साथ देती थी। जब कभी मजदूर ट्रेड यूनियन बनाने तथा हड़तालों, प्रदर्शनों और दूसरे संघर्षों के द्वारा अपनी स्थिति को सुधारने के प्रयत्न करते, सरकार का पूरा तंत्र उनके खिलाफ उठ खड़ा होता। इसके अलावा उन्होंने यह भी महसूस किया कि बढ़ती बेरोजगारी का समाधान केवल तीव्र औद्योगीकरण से संभव है, और यह कार्य केवल एक स्वाधीन सरकार कर सकती है। भारतीय समाज के दूसरे समूह भी कुछ कम संतुष्ट नहीं थे। शिक्षित भारतीयों का उभरता हुआ वर्ग अपने देश की दयनीय आर्थिक व राजनीतिक स्थिति को समझने के लिए नए-नए प्राप्त आधुनिक ज्ञान का उपयोग कर रहा था। पहले जिन लोगों ने 1857 में ब्रिटिश शासन का इस आशा से समर्थन किया था कि विदेशी होने के बावजूद यह शासन देश को एक आधुनिक तथा औद्योगिक देश बनाएगा, वे अब धीरे-धीरे निराश होने लगे थे। आर्थिक दृष्टि से उन्हें आशा थी कि ब्रिटिश पूँजीवादी ने जैसे ब्रिटेन में उत्पादक शक्तियों को विकसित किया था, उसी प्रकार वह भारत की उत्पादक शक्तियों को भी विकसित करेगा। लेकिन उन्होंने यह पाया कि ब्रिटेन के पूँजीवाद के इशारों पर भारत में ब्रिटिश शासन ने जो नीतियाँ अपनाई थीं वे देश को आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा या अल्पविकसित बनाए हुए थीं और उसकी उत्पादक शक्तियों के विकास में बाधक हो रही थीं। राजनीतिक स्तर पर शिक्षित भारतीय समुदाय को यह लगा कि अंग्रेजों ने पहले भारत को स्वशासन का मार्ग दिखाने के जो भी दावे किए थे, उन सबको वे भूल चुके थे। अधिकांश ब्रिटिश अधिकारियों तथा राजनीतिक नेताओं ने खुली घोशणा की थी कि अंग्रेज भारत में बने रहेंगे। इसके अलावा भाषण, प्रेस तथा व्यक्ति को और अधिक स्वतंत्रता देने की जगह अंग्रेज उन पर अधिकाधिक प्रतिबंध लगाते जा रहे थे। अंग्रेज अधिकारियों तथा लेखकों ने भारतीयों को जनतंत्र या स्वशासन की दृष्टि से अयोग्य घोषित कर दिया था। संस्कृति के क्षेत्र में भी शासक उच्च शिक्षा और आधुनिक विचारों के प्रसार के बारे में अधिकाधिक नकारात्मक, बल्कि शत्रुतापूर्ण रवैया अपना रहे थे। उभरते हुए भारतीय पूँजीपति वर्ग में बहुत धीरे-धीरे राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना विकसित हुई। लेकिन इस वर्ग ने भी धीरे-धीरे पाया कि वह साम्राज्यवाद के कारण नुकसान उठा रहा था। सरकार की व्यापार, चुंगी कर तथा यातायात संबंधी नीतियों के कारण इसके विकास में भारी बाधाएँ आ रही थीं। नया तथा कमजोर वर्ग होने के नाते इसे अपनी कमजोरियों की भरपाई के लिए सरकार की सक्रिय सहायता की जरूरत थी। इसके बजाए सरकार और उसकी नौकरशाही उन विदेशी पूँजीपतियों का साथ दे रही थी जो अपने विशाल संसाधनों के साथ भारत आकर यहाँ के सीमित औद्योगिक क्षेत्र को हथिया रहे थे। भारतीय पूँजीपतियों का विशेष विरोध विदेशी पूँजीपतियों की सख्त प्रतियोगिता के प्रति था। इस तरह भारतीय पूँजीपतियों ने भी महसूस किया कि उनके अपने स्वतंत्र विकास तथा साम्राज्यवाद के बीच एक अंतर्विरोध था और यह कि एक राष्ट्रीय सरकार ही भारतीय व्यापार और उद्योगों के तीव्र विकास की परिस्थितियाँ तैयार कर सकती थी। जैसा कि हमने इसके पहले देखा है, भारतीय समाज में केवल जमींदार, भूस्वामी तथा राजे-महाराजे ही ऐसे वर्ग थे जिनके हित विदेशी शासकों के हितों से मेल खाते थे और इसीलिए वे अंत तक विदेशी शासन का साथ देते रहे। लेकिन इन वर्गों से भी बहुत से लोग राष्ट्रवादी वातावरण में देशभक्ति की भावना ने बहुतों को प्रभावित किया। इसके अलावा प्रजातीय भेदभाव तथा श्रेष्ठता की नीतियों ने प्रत्येक विचारशील, स्वाभिमानी भारतीय में घृणा जगाकर उसे उठ खड़ा किया, चाहे वह किसी भी वर्ग का क्यों न रहा हो। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वयं ब्रिटिश शासन के विदेशी चरित्र ने भी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया को जन्म दिया। कारण यह है कि विदेशी दासता गुलाम जनता के दिलों में हमेशा ही देशभक्ति की भावनाएँ पैदा करती है। संक्षेप में, विदेशी साम्राज्यवाद का अपना चरित्र तथा भारतीय जनता पर उसका हानिकारक प्रभाव, इन बातों के कारण ही भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्यवाद-विरोधी आंदोलन का धीरे-धीरे जन्म और विकास हुआ। यह आंदोलन एक राष्ट्रीय आंदोलन था क्योंकि यह समाज के विभिन्न वर्गों और समुदायों के लोगों को प्रेरित कर रहा था कि वे अपने मतभेद भुलाकर अपने शत्रु के खिलाफ एकजुट हों। देश का प्रशासकीय और आर्थिक एकीकरणउन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में भारत का एकीकरण हो चुका था और वह एक राष्ट्र के रूप में उभर चुका था। इसलिए भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावनाओं का विकास आसानी से हुआ। अंग्रेजों ने धीरे-धीरे पूरे देश में सरकार की एकसमान, आधुनिक प्रणाली लागू कर दी थी और इस तरह इसका प्रशासकीय एकीकरण हो चुका था। ग्रामीण और स्थानीय आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के विनाश तथा अखिल भारतीय पैमाने पर आधुनिक व्यापार तथा उद्योग की स्थापना के कारण भारत का आर्थिक जीवन निरंतर एक इकाई के रूप में ढलता चला गया तथा देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के आर्थिक हित परस्पर संबद्ध हुए। उदाहरण के लिए, भारत के किसी एक भाग में अकाल फूटता या वस्तुओं की कमी होती तो दूसरे सभी भागों में भी खाद्य-सामग्री की कीमतों तथा उपलब्धता पर उसका प्रभाव पड़ता था। इसके अलावा, रेलवे, तार, तथा एकीकृत डाक व्यवस्था के समांरभ ने भी देश को एकजुट बना दिया था और जनता, खासकर नेताओं के पारस्परिक संपर्क को बढ़ावा दिया था।इस सिलसिले में भी, विदेश शासन का अस्तित्व ही एकता का कारण बन गया, हालाँकि यह शासन सामाजिक वर्ग, जाति, धर्म या क्षेत्र का भेद किए बिना पूरी भारतीय जनता का दमन करता था। पूरे देश के लोगों ने देखा कि वे एक ही शत्रु अर्थात ब्रिटिश शासन के हाथों पीड़ित थे। एक तरफ तो एक भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का एक प्रमुख कारण बन गया और दूसरी तरफ साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष तथा उस संघर्ष के दौरान उपजी एकजुटता की भावना ने भारतीय राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पश्चिमी विचार और शिक्षाउन्नीसवीं सदी में आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा और विचारधारा के प्रसार के फलस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में भारतीयों ने एक आधुनिक, बुद्धिसंगत, धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक तथा राष्ट्रवादी राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाया। वे यूरोपीय राष्ट्रों के समसामयिक राष्ट्र वादी आंदोलनों का अध्ययन, उसकी प्रशंसा तथा उनका अनुकरण करने के प्रयत्न भी करने लगे। रूसो, पेन, जान स्टुअर्ट मिल तथा दूसरे पाश्चात्य विचारक उनके राजनीतिक मार्गदर्शक बन गए जबकि मैजिनी, गैरीबाल्डी तथा आयरलैंड के राष्ट्रवादी नेता उनके राजनीतिक आदर्श हो गए।विदेशी दासता के अपमान की चुभन को सबसे पहले इन्हीं शिक्षित भारतीयों ने महसूस किया। विचारों से आधुनिक बनकर इन लोगों ने विदेशी शासन की बुराईयों के अध्ययन की योग्यता भी प्राप्त कर ली। उन्हें एक आधुनिक, मजबूत समृद्ध और एकताबद्ध भारत की कल्पना से प्रेरणा प्राप्त होती रही। कालांतर में, इन्हीं में से बेहतरीन तत्व राष्ट्रीय आंदोलन के नेता और संगठनकर्ता बने। हमें यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि राष्ट्रीय आंदोलन आधुनिक शिक्षा प्रणाली की उपज नहीं था, बल्कि वह ब्रिटेन तथा भारत के हितों के टकराव से उत्पन्न हुआ था। इस प्रणाली ने किया यह कि शिक्षित भारतीयों को पाश्चात्य विचार अपनाकर राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व संभालने तथा उसे एक जनतांत्रिक और आधुनिक दिशा देने में समर्थ बनाया। वास्तविकता यह है कि स्कूलों तथा कॉलेजों में अधिकारीगण विदेशी शासन के प्रति विनम्रता और सेवा का भाव ही जगाने के प्रयत्न करते थे। राष्ट्रवादी विचार तो आधुनिक विचारों के सामान्य प्रसार के कारण आए। चीन तथा इंडोनेशिया जैसे दूसरे एशियाई देशों में तथा पूरे अफ्रीका में भी आधुनिक और राष्ट्रवादी विचार फैले हालाँकि वहाँ आधुनिक स्कूलों और कॉलेजों की संख्या बहुत ही कम थी। आधुनिक शिक्षा ने शिक्षित भारतीयों के दृष्टिकोणों तथा हितों को एक सीमा तक एकजुटता और समानता पैदा की। इस सिलसिले में अंग्रेजी भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह आधुनिक विचारों के प्रसार का साधन बन गई। यह देश के विभिन्न भाषाई क्षेत्रों के शिक्षित भारतीयों के बीच विचारों के आदान-प्रदान तथा संपर्क का भी माध्यम बन गई। लेकिन जल्दी ही अंग्रेजी साधारण जनता में आधुनिक ज्ञान के प्रसार में बाधक भी बन गई। यह शिक्षित नागरिक वर्गों को साधारण जनता, खासकर ग्रामीण जनता से अलग रखने का काम भी करने लगी। भारत के राजनीतिक नेताओं ने इस तथ्य को अच्छी तरह समझा, दादाभाई नौरोजी, सैयद अहमद खान और जस्टिस रानाडे से लेकर तिलक और गाँधी जी तक सभी से शिक्षा प्रणाली में भारतीय भाषाओं को एक बड़ी भूमिका दिए जाने की माँग पर आंदोलन किए। वास्तव में, जहाँ तक साधारण जनता का सवाल था, आधुनिक विचारों का प्रसार विकासमान भारतीय भाषाओं, उनमें विकसित हो रहे साहित्य तथा सबसे अधिक तो भारतीय भाषाओं के लोकप्रिय प्रेस के कारण हुआ। प्रेस तथा साहित्य की भूमिकावह प्रमुख साधन प्रेस था जिसके द्वारा राष्ट्रवादी भारतीयों ने देशभक्ति की भावनाओं का, आधुनिक आर्थिक-सामाजिक-राजनीतिक विचारों का प्रचार किया तथा एक अखिल भारतीय चेतना जगाई। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में बड़ी संख्या में राष्ट्र वादी सामाचारपत्र निकलें। उनके पन्नों पर सरकारी नीतियों की लगातार आलोचना होती थी, भारतीय दृष्टिकोण को सामने रखा जाता था, लोगों को एकजुट होकर राष्ट्रीय कल्याण के काम करने को कहा जाता था, तथा जनता के बीच स्वशासन, जनतंत्र, औद्योगीकरण, आदि के विचारों को लोकप्रिय बनाया जाता था। देश के विभिन्न भागों में रहने वाले राष्ट्रीवादी कार्यकर्ताओं को भी परस्पर विचारों को आदान-प्रदान करने में प्रेस ने समर्थ बनाया।उपन्यासों, निबंधों, देशभक्तिपूर्ण काव्य आदि के रूप में राष्ट्रीय साहित्य ने भी राष्ट्रीय चेतना जगाने में प्रमुख भूमिका निभाई। बंगला में बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय तथा रवींद्रनाथ टैगोर, असमी में लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, मराठी में विष्णु शास्त्री चिपलुणकर तमिल में सुब्रामन्य भारती, हिंदी में भारतेंदु हरिश्चन्द्र और उर्दू में अल्ताफ हुसैन हाली इस काल के कुछ प्रमुख राष्ट्रवादी लेखक थे। भारत के अतीत की खोजअनेक भारतीय इस कदर पस्त हो चुके थे कि वे अपनी स्वशासन की क्षमता में एकदम भरोसा खो बैठे थे। इसके अलावा उस समय के अधिकांश ब्रिटिश अधिकारी और लेखक लगातार यह बात दोहराते रहते थे कि भारतीय लोग कभी भी अपना शासन चलाने योग्य नहीं थे, कि हिंदू और मुसलमान हमेशा आपस में लड़ते रहे हैं, कि भारतीयों के भाग्य में ही विदेशियों के अधीन रहना लिखा है, कि उनका धर्म और सामाजिक जीवन पतित और असभ्य रहें हैं और इस कारण वे लोकतंत्र या स्वशासन तक के काबिल नहीं हैं। इस प्रचार का जवाब देकर अनेक राष्ट्रवादी नेताओं ने जनता में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जगाने के प्रयत्न किए। वे गर्व से भारत की सांस्कृतिक धरोहर की ओर संकेत करते और आलोचकों का ध्यान अशोक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और अकबर जैसे शासकों ने विद्वानों कला, स्थापत्य, साहित्य, दर्शन, विज्ञान और राजनीति में भारत की राष्ट्रीय धरोहर की फिर से खोज करने में जो कुछ किया, उससे इन राष्ट्रवादी नेताओं को बल तथा प्रोत्साहन मिला। दुर्भाग्य से कुछ राष्ट्रवादी नेता दूसरे छोर तक चले गए तथा भारत के अतीत की कमजोरियों और पिछड़ेपन से आँखें चुराकर गैर-लोचनात्मक ढंग से उसे महिमामंडित करने लगे। खास तौर पर प्राचीन भारत की उपलब्धियों का प्रचार करने तथा मध्यकालीन भारत की उतनी ही महान उपलब्धियों का प्रचार करने तथा मध्यकालीन भारत की उतनी ही महान उपलब्धियों को अनदेखा करने की प्रवृत्ति ने भी बहुत नुकसान पहुँचाया। इसके कारण हिंदुओं में सांप्रदायिक भावनाओं के विकास को प्रोत्साहन मिला। साथ ही इसकी जवाबी प्रवृत्ति के रूप मे मुसलमान सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रेरणा पाने के लिए अरबों तथा तुर्कों के इतिहास की ओर नजर करने लगे। इसके अलावा, पश्चिम के सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की चुनौती का जवाब देते समय बहुत से भारतीय यह बात भी भूल जाते थे कि भारत की जनता कई क्षेत्रों में सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ी थी। इससे गर्व तथा आत्मसंतोष की एक झूठी भावना पनपी जो भारतीयों को अपने समाज के आलोचनात्मक अध्ययन से रोकती थी। इसके कारण सामाजिक-सांस्कृतिक पिछड़ेपन के खिलाफ संघर्ष कमजोर हुआ, तथा अनेक भारतीय दूसरी जातियों की स्वस्थ और नई प्रवृत्तियों और नए विचारों से विमुख रहे।शासकों का जातीय दंभभारत में राष्ट्रीय भावनाओं के विकास का एक गौण परंतु महत्वपूर्ण कारण जातीय श्रेष्ठता का वह दंभ था जो भारतीयों के प्रति अनेक अंग्रेजों के व्यवहार में पाया जाता था। इस जातीय दंभ का एक कड़वा और प्रचलित रूप तब देखने को मिलता था, जब कोई अंग्रेज किसी भारतीय से किसी विवाद में उलझा होता था और न्याय व्यवस्था अंग्रेज का पक्ष लेती थी। जैसा कि जी. ओ. ट्रेवेलियन ने 1864 में लिखा है : “हमारे अपने देश के एक व्यक्ति का बयान भी अदालतों में अनेक हिंदुओं से अधिक महत्व रखता है। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें शक्ति का एक भयानक साधन एक बेईमान और चालाक अंग्रेज के हाथों में पहुँच जाता है।”यह जातीय दंभ जाति, धर्म प्रांत या वर्ग का भेदभाव किए बिना तमाम भारतीयों को एक समान हीन करार देता था। वे यूरोपीय लोगों के क्लबों में नहीं जा सकते थे और अक्सर उन्हें किसी गाड़ी के उस डिब्बे में यात्रा की अनुमति नही थी जिसमें यूरोपीय यात्री जा रहे हों। इससे उनमें राष्ट्रीय अपमान का बोध हुआ तथा अंग्रेजों के मुकाबले वे अपने-आपकों एक जनगण के रूप में देखने लगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएँ1870 के दशक तक यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि भारतीय राष्ट्रवाद इतनी ताकत और गति अर्जित कर चुका है कि वह भारतीय राजनीति में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर सके।दिसंबर 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अखिल भारतीय पैमाने पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पहली संगठित अभिव्यक्ति हुई। लेकिन इसके पहले भी अनेक संस्थाएँ स्थापित हो चुकी थीं। जैसा कि हमने इसके पहले पढ़ा है, राजा राममोहन राय पहले ऐसे भारतीय नेता थे जिन्होंने भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन चलाया। 1836 के बाद देश विभिन्न भागों में अनेक सार्वजनिक समितियाँ स्थापित हुई। इन सभी समितियों पर धनी तथा अभिजात लोगों का प्रभुत्व था जिनको तब “गणमान्य व्यक्ति” कहा जाता था, और इसका चरित्र प्रांतीय या स्थानीय था। इन्होंने प्रशासन में सुधार और प्रशासन में भारतीय लोगों की भागीदारी के लिए काम किया तथा ब्रिटिश संसद को लंबे-लंबे प्रार्थनापत्र भेजे जिनमें भारतीयों की माँगें रखी जाती थीं। 1858 के बाद के काल में शिक्षित भारतीयों तथा अंग्रेजों के भारतीयों प्रशासन के बीच की खाई धीरे-धीरे बढ़ती गई। ब्रिटिश शासन के चरित्र तथा भारतीयों के लिए उसके दुष्परिणामों का अध्ययन करने के बाद ये शिक्षित भारतीय भारत में ब्रिटिश नीतियों के अधिकाधिक मुखर आलोचक बन गए। उनका असंतोष धीरे-धीरे राजनीतिक कार्यकलाप में अभिव्यक्त हुआ। उस समय तक मौजूद समितियों राजनीतिक चेतना-प्राप्त भारतीयों को संतुष्ट करने में असफल रहीं। 1866 में लंदन में दादाभाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया ऐसोसिएशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य भारतीय प्रश्नों पर विचार करना तथा भारत के कल्याण की दिशा में ब्रिटेन के नेताओं को प्रभावित करना था। बाद में उन्होंने प्रमुख भारतीय नगरों में भी इस एसोसिएशन की शाखाएँ स्थापित कीं। 1825 में जन्में दादाभाई ने अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय आंदोलन को समर्पित कर दिया। जल्द ही उन्हें भारत का पितामह (ग्रैंड ओल्ड मैन आफ इंडिया) कहा जाने लगा। वे भारत के पहले आर्थिक विचारक भी थे। अपने अर्थशास्त्रीय लेखन में उन्होंने सिद्ध किया कि भारत की गरीबी का कारण अंग्रेजों द्वारा उसका शोषण तथा यहाँ का धन ब्रिटेन भेजना था। तीन बार दादाभाई को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष चुनकर उनका सम्मान किया। वास्तव में वे भारत के उन जनप्रिय राष्ट्रवादी नेताओं की लंबी कतार के अग्रणी नेता थे जिनका नाम भर जनता के हृदय में हलचल मचाने के लिए काफी था। कांग्रेस-पूर्व राष्ट्रवादी संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण कलकत्ता का इंडियन एसोसिएशन था। बंगाल के कम अवस्था के राष्ट्रवादी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की रूढ़िवादी और जमींदार-समर्थक नीतियों से धीरे-धीरे ऊब रहे थे। वे व्यापक सार्वजनिक महत्व के सवालों पर लंबा राजनीतिक आंदोलन छेड़ना चाहते थे। प्रतिभाशाली लेखक-वक्ता सुरेंद्रनाथ बनर्जी के रूप में उन्हें एक नेता भी मिल गया। बनर्जी अपने अधिकारियों द्वारा बहुत ही अन्यायपूर्ण ढंग से इंडियन सिविल सर्विस से बाहर कर दिए गए थे क्योंकि ये अधिकारी अपनी सर्विस में किसी स्वतंत्र विचारों वाले भारतीय की उपस्थिति नहीं बर्दाश्त कर सके। बनर्जी ने 1875 में कलकत्ता के छात्रों के सामने राष्ट्रवादी विषयों पर प्रभावशाली भाषण देकर अपना राजनीतिक जीवन शुरु किया। सुरेंद्रनाथ तथा आनंदमोहन बोस के नेतृत्व में बंगाल के इन युवा राष्ट्रवादियों ने जुलाई 1876 में इंडियन एसोसिएशन की नींव रखी। इस एसोसिएशन ने अपने सामने राजनीतिक प्रश्नों पर भारतीय जनता को एकताबद्ध करने का लक्ष्य रखा। अपनी ओर बड़ी संख्या में जनता को खींचने के लिए इसने निर्धन वर्गों के लिए कम सदस्यता शुल्क निर्धारित किया। बंगाल के शहरों और गाँवों तथा बंगाल से बाहर अनेक शहरों में भी इस एसोसिएशन की कई शाखाएँ खोली गई। भारत के दूसरे भागों में भी युवक लोग सक्रिय थे। जस्टिस रानाडे तथा उनके साथियों ने 1870 के दशक में पूना सार्वजनिक सभी की स्थापना की। एम. वीर राघवचारी, जी. सुब्रामन्य अय्यर, आनंद चारुलु तथा दूसरों ने 1884 में मद्रास महाजन सभा की नींव डाली। फिरोजशाह मेहता, के. टी. तेलंग, बदरूद्दीन तैयबजी तथा दूसरों ने 1885 में बांबे प्रेसीडेंसी ऐसोसिएशन बनाया। इस तरह जो राष्ट्रवादी एक साझे शत्रु अर्थात विदेशी शासन और शोषण के खिलाफ राजनीतिक एकता की आवश्यकता महसूस कर रहे थे, उनके लिए एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन की स्थापना का समय आ चुका था। तब तक मौजूद संगठनों ने एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा किया था परंतु उनका क्षेत्र ओर कार्यकलाप बहुत सीमित थे। वे अधिकतर स्थानीय प्रश्नों को उठाते थे तथा उनकी सदस्यता और नेतृत्व एक शहर या एक प्रांत के ही थोड़े से लोगों तक सीमित थे। यहाँ तक कि इंडियन एसोसिएशन भी एक अखिल भारतीय संस्था नहीं बन सकी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसराष्ट्रवादी कार्यकताओं की एक अखिल भारतीय संगठन बनाने की योजनाएँ अनेक भारतीय जन तैयार करते आ रहे थे। लेकिन इस विचार को एक ठोस और अंतिम रूप देने का श्रेय एक सेवानिवृत अंग्रेज सिविल सवेर्ट, ए. ओ. हृयूम, को जाता है। उन्होंने प्रमुख भारतीय नेताओं से संपर्क किया और उनके सहयोग से बंबई से दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता डब्ल्यू. सी. बनर्जी ने की तथा इसमें प्रतिनिधि शामिल थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य इस प्रकार घोषित किए गए - देश के विभिन्न भागों के राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, जाति-धर्म-प्रांत का भेद किए बिना राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित तथा मजबूत करना, जनप्रिय माँगों को निरूपण तथा उन्हें सरकार के सामने रखना और सबसे महत्वपूर्ण यह कि देश में जनमत को प्रशिक्षित और संगठित करना।कहा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे ह्यूम का प्रमुख उद्देश्य शिक्षित भारतीयों में बढ़ रहे असंतोष की सुरक्षित निकासी के लिए एक ‘सेफ्टी वाल्व’ बनाना था। वे असंतुष्ट राष्ट्रवादी शिक्षित वर्गों तथा असंतुष्ट किसान जनता के आपसी मेल को रोकना चाहते थे। मगर यह ‘सेफ्टी वाल्व’ का सिद्धान्त सच्चाई का बहुत छोटा अंश है और यह पूरा अपर्याप्त तथा भ्रामक है। राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बढ़कर राजनीतिक चेतना-प्राप्त भारतीयों की इस आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करती थी कि उनकी आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के लिए कार्यरत एक राष्ट्रीय संगठन बनाया जाए। हम पहले ही देख चुके है कि कुछ जबर्दस्त शक्तियों के कार्यरत होने के परिणामस्वरूप देश में राष्ट्रीय आंदोलन पहले से ही फैल रहा था। इस आंदोलन के जन्म के लिए किसी एक व्यक्ति या कुछेक व्यक्तियों को श्रेय नहीं दिया जा सकता। ह्यूम के अपने उद्देश्य भी मिले-जुले थे। वे ‘सेफ्टी वाल्व’ बनाने के विचार से कहीं अधिक श्रेष्ठ विचारों से प्रेरित थे। वे भारत से तथा इसके गरीब किसानों से सचमुच प्यार करते थे। कुछ भी हो, राष्ट्रीय कांग्रेस को जन्म देने में जिन भारतीय नेताओं ने ह्यूम से सहयोग किया वे ऊँचे चरित्र वाले देशभक्त लोग थे। उन्होंने जान-बूझकर हृयूम की सहायता इसलिए ली कि वे राजनीतिक कार्यकलाप के आंरभ में ही अपने प्रयासों के प्रति सरकार की शत्रुता मोल लेना नहीं चाहते थे। उन्हें आशा थी कि एक सेवानिवृत सिविल सवेर्ट की उपस्थिति अधिकारियों की आशंकाओं का समाधान करेगी। अगर हृयूम कांग्रेस का उपयोग एक ‘सेफटी वाल्व’ के रूप में करना चाहते थे तो कांग्रेस के आरंभिक नेताओं को आशा थी कि वे हृयूम का उपयोग एक ‘तड़ित चालक’ के रूप में कर सकेंगे। इस तरह 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ छोटे पैमाने पर लेकिन संगठित रूप में, विदेशी शासन से भारत की मुक्ति का संघर्ष आरंभ हो गया। इसके बाद तो राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ता ही गया तथा देश और देश की जनता ने स्वाधीन होने तक आराम को हराम जाना। आरंभ से ही कांग्रेस ने एक पार्टी नहीं, बल्कि एक आंदोलन का काम किया। 1886 में कांग्रेस के 436 प्रतिनिधि विभिन्न स्थानीय संगठनों तथा समूहों द्वारा चुने गए थे। इसके बाद कांग्रेस हर वर्ष दिसंबर में और हर बार देश के एक नए भाग में अपने अधिवेशन करती रही। जल्द ही इसके प्रतिनिधियों की संख्या बढ़कर हजारों में पहुँच गई। इसके प्रतिनिधियों में अधिकांश लेग वकील, पत्रकार, व्यापारी, उद्योगपति अध्यापक और जमींदार होते थे। 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादंबिनी गांगुली ने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया। यह इस बात का प्रतीक था कि भारत का स्वाधीनता संग्राम स्त्रियों को उस पतित अवस्था से उबारेगा जिसमें वे सदियों के कालक्रम में पहुँचा दी गई थीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कोई एक धारा नहीं थी, जिसमें राष्ट्रवाद की नदी आगे बढ़ी। प्रांतीय सम्मेलन और स्थानीय समितियों और राष्ट्रवादी सामाचार पत्र भी बढ़ते हुए राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रमुख उद्घोषक थे। खासकर प्रेस राष्ट्रवादी विचारों तथा राष्ट्रवादी आंदोलन को फैलाने का प्रमुख साधन बन गया था। इस काल के अधिकांश सामाचार पत्र निश्चित ही व्यापार के रूप में नहीं चलाए जाते थे बल्कि राष्ट्रवादी गतिविधियों के मुख्यपत्र के रूप में आरंभ किए जाते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक वर्षों में इसके कुछ महान अध्यक्षों के नाम इस प्रकार थे - दादाभाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोजशाह मेहता, पी. आनंद चारुलु, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, रमेशचन्द्र दत्त, आनंदमोहन बोस और गोपाल कृष्ण गोखले। इस काल में कांग्रेस तथा राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ और प्रमुख नेता महादेव गोविन्द रानाडे, बाल गंगाधर तिलक, शिशिरकुमार तथा मोतीलाल घोष नामक दो भाई, मदनमोहन मालवीय, जी. सुब्रामन्य अय्यर, सी. विजयराघवाचारी और दिनशा ई वाचा थे। आरंभिक राष्ट्रवादियों के कार्यक्रम और कार्यकलापआरंभ के राष्ट्रवादी नेताओं का विश्वास था कि देश की राजनीतिक मुक्ति के लिए सीधी लड़ाई लड़ना अभी व्यवहारिक नहीं था। जो कुछ व्यावहारिक था, यह था कि राष्ट्रीय भावनाओं को जगाया तथा मजबूत किया जाए, बड़ी संख्या में भारतीय जनता को राष्ट्रवादी राजनीति की धारा में लाया जाए और राजनीति तथा राजनीतिक आंदोलन के लिए उन्हें शिक्षित किया जाए। इस बारे में पहला महत्वपूर्ण कार्य राजनीतिक प्रश्नों में जनता की रूचि विकसित करना तथा देश में जनमत का संगठन करना था। दूसरे, राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय माँगों का निरूपण किया जाना था ताकि उभरते हुए जनमत को एक अखिल भारतीय स्वरूप मिल सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पहले पहल राजनीतिक चेतना-प्राप्त भारतीयों तथा राजनीतिक कार्यकर्ताओं और नेताओं में राष्ट्रीय एकता पैदा की जाए।आंरभिक राष्ट्रीय नेता इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि भारत अभी हाल ही में एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में पहुँचा है, दूसरे शब्दों में, भारत अभी एक नवोदित राष्ट्र था। भारत के राष्ट्रीय स्वरूप को बहुत सावधानी से निखारने की आवश्यकता थी। भारतीयों को बहुत होशियारी से एक राष्ट्र के रूप में संगठित किया जाना था। रातनीतिक चेतना-प्राप्त भारतीयों को क्षेत्र, जाति या धर्म के भेदों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित और मजबूत करने के लिए लगातार डटकर काम करना पड़ रहा था। आंरभिक राष्ट्रवादियों ने अपनी राजनीतिक तथा आर्थिक माँगों का निर्धारण इस बात को दृष्टि में रखकर किया कि भारतीय जनता को एक साझे आर्थिक-राजनीतिक कार्यक्रम के आधार पर संगठित करना है। साम्राज्यवाद की अर्थशास्त्रीय आलोचनासाम्राज्यवाद की अर्थशास्त्रीय आलोचना आरंभिक राष्ट्रादियों का संभवतः सबसे महत्वपूर्ण रातनीतिक कार्य था। उन्होंने तत्कालीन औपनिवेशिक आर्थिक शोषण के सभी तीनों रूपों, अर्थात व्यापार, उद्योग तथा वित्त के द्वारा शोषण पर ध्यान दिया। उन्होंने अच्छी तरह समझा कि ब्रिटेन के आर्थिक साम्राज्यवाद का मूल तत्व भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के अधीन बनाना था। भारत में एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के मूल तत्वों को विकसित करने के ब्रिटिश प्रयासों को उन्होंने तीखा विरोध किया। ये तत्व थे, कच्चा माल पैदा करने वाले देश, ब्रिटिश उद्योगों में पैदा माल के लिए मंडी, तथा विदेशी पूँजी के निवेश के क्षेत्र के रूप में भारत का रूपांतरण। उन्होंने इस औपनिवेशिक ढाँचे पर आधारित सरकार की लगभग सभी महत्वपूर्ण आर्थिक नीतियों के खिलाफ एक शक्तिशाली आंदोलन खड़ा किया।आरंभिक राष्ट्रवादी भारत की बढ़ती गरीबी तथा आर्थिक पिछड़ेपन और यहाँ आधुनिक उद्योग-धंधों तथा कृषि के विकास की असफलता को लेकर दुखी थे। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। दादाभाई नौरोजी ने 1881 में ही घोषित कर दिया था कि ब्रिटिश शासन ‘‘एक स्थायी, बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण’’ है जो ‘‘धीरे-धीरे सही, मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है।’’ भारत के परंपरागत हस्त उद्योगों को नष्ट करने तथा आधुनिक उद्यागों के विकास में बाधा डालने के लिए राष्ट्रवादियों ने सरकार की अर्थिक नीतियों की आलोचना की। उनमें अधिकांश ने भारतीय रेलवे, बागानों तथा उद्योगों में विदेशी पूँजी के भारी निवेशी का विरोध किया। उनका तर्क यह था कि इससे भारतीय पूँजीपतियों का उत्पीड़न होगा और भारत की अर्थव्यवस्था तथा राजनीतिक प्रणाली पर ब्रिटेन का दबदबा और मजबूत होगा। उन्हें विश्वास था कि विदेशी पूँजी के निवेश से मौजूदा पीढ़ी ही नहीं बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए भी गंभीर आर्थिक और राजनीतिक खतरे पैदा होंगे। उन्होंने बतलाया कि भारत की निर्धनता को दूर करने का प्रमुख उपाय आधुनिक उद्योगों का तीव्र विकास है। वे चाहते थे कि सरकार चुंगी द्वारा सरंक्षण तथा प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता देकर आधुनिक उद्योगों को प्रोत्साहन दे। भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने स्वदेशी, अर्थात् भारतीय मालों के उपयोग तथा ब्रिटिश मालों के बहिष्कार के विचार को प्रोत्साहित किया। उदाहरण के लिए, 1896 में एक व्यापक स्वदेशी कार्यक्रम के अंग के रूप में पूना तथा महाराष्ट्र के दूसरे नगरों में विदेशी वस्त्रों की खुलेआम होली जलाई गई। राष्ट्रवादियों को शिकायत थी कि भारत की दौलत इंग्लैंड ले जाई जा रही है और उन्होंने माँग की कि इस दोहन को रोका जाए। किसानों पर करों का बोझ कम करने के लिए उन्होंने जमीन की मालगुजारी घटाने के सवाल पर निरंतर आंदोलन चलाया। इनमें से कुछ ने उन अर्ध-सामंती कृषि संबंधों की भी आलोचना की जिनकों अंग्रेज बनाए रखना चाहते थे। बागान-मजदूरों के काम की परिस्थितियों में सुधार के लिए भी राष्ट्रवादियों ने आंदोलन छेड़े। उन्होंने भारी करों को भारत की गरीबी का एक कारण बताया और नमक-कर खत्म करने तथा जमीन की मालगुजारी घटाने की माँग की। उन्होंने भारत सरकार के भारी फौजी खर्चों की निंदा की तथा इसे घटाने की माँग की। समय गुजरने के साथ-साथ अधिकाधिक राष्ट्रवादी इस निष्कर्ष पर पहुँचते गए कि विदेशी साम्राज्यवाद द्वारा देश का आर्थिक शोषण, उसे निर्धन बनाना तथा उसके आर्थिक पिछड़ेपन को बनाए रखना, ये ऐसी बाते थीं जो विदेशी शासन के कुछ लाभकारी पहलुओं पर पानी फेर देती थीं। उदाहरण के लिए जीवन तथा संपत्ति की सुरक्षा के लाभों के प्रश्न पर दादाभाई नौरोजी ने इस प्रकार की टिप्पणी की - मजे की बात यह है कि भारत में जीवन तथा संपत्ति की सुरक्षा प्राप्त है, मगर यथार्थ में ऐसी कोई बात नहीं है। केवल एक ही अर्थ या रूप में जीवन और संपत्ति की सुरक्षा प्राप्त है, अर्थात् लोग एक-दूसरे की या देशी तानाशाहों की हिंसा से सुरक्षित हैं . . . . . परंतु इंग्लैंड की अपनी जकड़ से संपत्ति को और परिणामस्वरूप जीवन को बिलकुल सुरक्षा प्राप्त नहीं है। भारत की संपत्ति सुरक्षित नहीं है। जो कुछ सुरक्षित और अच्छी तरह सुरक्षित है, वह यह है कि इंग्लैंड पूरी तरह सुरक्षित तथा निश्चित है और इस तरह पूरी सुरक्षा पाकर वह इस समय तीन या चार करोड़ पौंड प्रति वर्ष की दर से भारत की संपत्ति बाहर ले जा रहा है, या यहीं उसका भक्षण कर रहा है . . . . . इसलिए मैं यह कहने की जुर्रत करूँगा कि भारत की संपत्ति या उसके जीवन को सुरक्षा प्राप्त नहीं है . . . . . भारत के लाखों-लाख लोगों के लिए जीवन का अर्थ ‘आधा-पेट भोजन’, या भुखमरी, या अकाल और महामारी है। कानून और व्यवस्था के बारे में दादाभाई ने लिखा - भारत में एक कहावत प्रचलित है - “पीठ पर मार लो भैया, मगर पेट पर मत मारो।” देशी तानाशाह के अधीन जनता जो कुछ पैदा करती है उसे अपने पास रखती और उपयोग करती है, हालाँकि कभी-कभी उसे पीठ पर कुछ हिंसा झेलनी पड़ती है। ब्रिटिश भारत की तानाशाही में मनुष्य शांति के साथ रह रहा है और ऐसी कोई हिंसा यहाँ नहीं है, परंतु उसका सहारा उसे अनदेखे, शांतिपूर्ण तथा बहुत बारीक ढंग से उससे छिनता जा रहा है। वह शांति के साथ भूखा रहता है तथा शान्ति के साथ मर जाता है और यह सब पूरे कानून और व्यवस्था के साथ हो रहा है।” आर्थिक प्रश्नों पर राष्ट्रीयवादी आंदोलन के कारण अखिल भारतीय स्तर पर यह विचार फैला कि ब्रिटिश शासन भारत के शोषण पर आधारित है, भारत को गरीब बना रहा है तथा आर्थिक पिछड़ापन और अल्पविकास पैदा कर रहा है। ब्रिटिश शासन से परोक्ष ढंग से जो भी लाभ हुए हों, उनके मुकाबले ये हानियाँ कहीं बहुत अधिक थीं। सांविधानिक सुधारशुरु के राष्ट्रवादियों का आरंभ से ही यह विश्वास था कि भारत में अंततः लोकतांत्रिक स्वशासन लागू होना चाहिए। लेकिन उन्होंने इस लक्ष्य को फौरन प्राप्त किए जाने की माँग नहीं की। उनकी तात्कालिक माँगें अत्यधिक साधारण थीं। वे एक-एक कदम उठा कर स्वाधीनता की मंजिल तक पहुँचना चाहते थे। वे बहुत सावधान भी थे कि सरकार उनकी गतिविधियों को कुचल न दे। 1885 से 1892 तक वे विधायी परिषदों के प्रसार और सुधार की ही माँग उठाते रहे।उनके आंदोलन के दबाव में ब्रिटिश सरकार को 1892 में भारतीय परिषद् कानून पास करना पड़ा। इस कानून द्वारा शाही विधायी परिषद् तथा प्रांतीय परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। इनमें से कुछ सदस्यों को भारतीय अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुन सकते थे, मगर बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता। राष्ट्रवादी 1892 के कानून से पूरी तरह असंतुष्ट थे तथा उन्होंने इसे मजाक बतलाया। उन्होंने परिषदों में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाने तथा उन्हें अधिक अधिकार दिए जाने की माँग उठाई। खास तौर पर उन्होंने सार्वजनिक धन पर भारतीयों के नियंत्रण की माँग की तथा वह नारा दिया जो इससे पहले अमरीकी जनता ने अपने स्वाधीनता के युद्ध के दौरान लगाया था। यह नारा था - “प्रतिनिधित्व नहीं तो कर भी नहीं।” पर साथ ही साथ वे अपने लोकतांत्रिक माँगों के आधार को व्यापक बनाने में असफल रहे, उन्होंने जनता के लिए या स्त्रियों के लिए मताधिकार की माँग नहीं की। बीसवीं सदी के आरंभ तक राष्ट्रवादी नेता और आगे बढ़ चुके थे और उन्होंने आस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों की तर्ज पर ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर ही स्वशासन (स्वराज्य) का दावा पेश किया। कांग्रेस के मंच से इस माँग को 1905 में गोखले और 1906 में दादाभाई नौरोजी ने उठाया। प्रशासकीय और अन्य सुधारआरंभिक राष्ट्रवादी व्यक्तिवादी प्रशासकीय फैसलों के निर्भीक आलोचक थे तथा उन्होंने भ्रष्टाचार, निकम्मापन और दमन से ग्रस्त शासन प्रणाली के सुधार के लिए अथक प्रयास किए। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रशासकीय सुधार वे चाहते थे, वह यह था कि प्रशासकीय सेवाओं के उच्चतर पदों का भारतीयकरण हो। उन्होंने आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक आधारों पर यह माँग उठाई। आर्थिक, दृष्टि से उच्चतर पदों पर यूरोपीय एकाधिकार दो कारणों से हानिकारक था - (अ) यूरापीय लोगों को बहुत ऊँचे वेतन दिए जाते थे और इससे भारत का प्रशासन बहुत खर्चीला हो जाता था, जबकि समान योग्यता वाले भारतीयों को कम वेतन पर रखा जा सकता था और (ब) यूरोपीय लोग अपने वेतन का एक बड़ा भाग भारत से बाहर भेज देते थे और उनको पेंशन भी इंग्लैंड में अदा किया जाता था। इससे भारत की संपत्ति का दोहन और बढ़ता था। राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्रवादियों का मत था कि इन सेवाओं का भारतीयकरण करने पर प्रशासन भारत की आवश्यकताओं के प्रति और सजग होता। इस प्रश्न के नैतिक पक्ष को 1897 में गोपालकृष्ण गोखले ने इस प्रकार रखा -विदेशी प्रशासन का अत्यधिक खर्चीलापन बहरहाल इसकी अकेली बुराई नहीं है यह एक नैतिक बुराई भी है, बल्कि यह बड़ी बुराई है। वर्तमान व्यवस्था में भारतीय जाति का कद घटने या उसकी वृद्धि के रूकने की प्रक्रिया चल रही है। हमें अपना पूरा जीवन, उसका एक-एक दिन हीनता के वातावरण में जीना पड़ रहा है और हममें जो श्रेष्ठता है उसे भी झुकना पड़ रहा है . . . . हमारी मनुष्यता जिन महानता ऊँचाइयों को छू सकती है, वहाँ तक वर्तमान व्यवस्था में हम कभी नहीं पहुँच सकेंगे। प्रत्येक स्वशासी जनगण को जिस नैतिक ऊँचाई का अनुभव होता है, उसे हम महसूस नहीं कर सकते। हमारी प्रशासकीय और सैनिक योग्यताएँ उपयोग के बिना धीरे-धीरे नष्ट हो जाएगी और हम अपने ही देश में लकड़ी काटने वालों या कुएँ से पानी निकालने वालों के रूप में जड़ होकर रह जाएँगे। राष्ट्रवादियों की माँग थी कि न्यायिक अधिकारों को कार्यकारी अधिकारों से अलग किया जाए ताकि पुलिस तथा नौकरशाही के मनमाने अत्याचारों से जनता को कुछ सुरक्षा मिले। उन्होने जनता के साथ पुलिस या दूसरे सरकारी अमलों के दमनकारी निरंकुश व्यवहार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। उन्होंने कानूनी प्रक्रिया में लगने वाली देरी तथा न्याय-व्यवस्था के ऊँचे खर्च की आलोचना की। उन्होंने भारत के पड़ोसी देशों के प्रति आक्रामक विदेश नीति का विरोध किया। उन्होंने बर्मा के अपहरण, अफगानिस्तान पर हमले तथा पश्चिमोत्तर भारत की आदिवासी जनता के दमन का भी विरोध किया। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह राज्य की ओर से कल्याणकारी गतिविधियाँ चलाए। उन्होंने जनता में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर बहुत अधिक जोर दिया। उन्होंने तकनीकी और उच्च शिक्षा की सुविधाएँ बढ़ाने की माँग भी उठाई। सूदखोरों के चंगुल से किसानों को बचाने के लिए उन्होंने कृषि बैकों की स्थापना की माँग की। वे चाहते थे कि सरकार खेती के विकास तथा देश को अकाल से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर सिंचाई की योजनाएँ लागू करे। उन्होंने चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने तथा पुलिस को ईमानदार, कुशल तथा जनप्रिय बनाने के लिए पुलिस व्यवस्था में सुधार की माँगें भी उठाई। राष्ट्रवादी नेताओं ने उन भारतीय मजदूरों के पक्ष में भी आवाज उठाई जो गरीबी से मजबूर होकर, रोजगार की तलाश में दक्षिण अफ्रीका, मलाया, मॉरीशस, वेस्ट इंडीज या ब्रिटिश गुयाना चले जाते थे। इनमें सें अधिकांश देशों में उन्हें निर्मम दमन तथा जातीय भेदभाव का सामना करना पड़ता था। यह बात दक्षिण अफ्रीका के बारे में खास तौर पर सच थी, जहाँ भारतीयों के मूलभूत मानव अधिकारों की रक्षा के लिए मोहनदास करमचंद गाँधी एक जनसंघर्ष चला रहे थे। नागरिक अधिकारों की रक्षाआरंभ में ही राजनीति चेतना-प्राप्त भारतीय लोकतंत्र ही नहीं, बल्कि भाषण, प्रेस, विचार तथा संगठन की स्वतंत्रता जैसे आधुनिक नागरिक अधिकारों के प्रति भी आकर्षित थे। जब भी सरकार इन नागरिक अधिकारों को सीमित करने के प्रयास करती, वे जमकर उनका बचाव करते। यही वह काल था जिसमें राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्य के फलस्वरूप आम तौर पर पूरी भारतीय जनता तथा खास तौर पर शिक्षित वर्गों में लोकतांत्रिक विचार अपनी जड़े जमाने लगे। वास्तव में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का सघर्षं राष्ट्रीय का अभिन्न अंग बन गया। 1897 में बंबई की सरकार ने बाल गंगाधर तिलक, दूसरे कई नेताओं और समाचारपत्रों के संपादकों को सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काने के लिए गिरफ्तार कर लिया और उन पर मुकद्दमा चलाया। उनकों लंबी-लंबी कैद की सजाएँ दी गई। इसी के साथ पूना के दो नाटू भाईयों को बिना किसी मुकद्दमे के अंडमान भेज दिया गया। जनता की स्वतंत्रता, पर इस हमले का पूरे देश में विरोध हुआ। तिलक जिन्हे अभी तक मुख्यतः महाराष्ट्र में ही जाना जाता था, रातों-रात अखिल भारतीय नेता बन गए।राजनीतिक कार्य की विधियाँ1905 तक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर उन लोगों का वर्चस्व था जिनको प्रायः नरमपंथी राष्ट्रवादी कहा जाता था। कानून की सीमा में रहकर सांविधानिक आंदोलन तथा धीरे-धीरे, व्यवस्थित ढंग से राजनीतिक प्रगति-इन शब्दों में नरमपंथियों की राजनीतिक कार्यपद्धति को संक्षेप में रखा जा सकता है। उनका विश्वास था कि अगर जनमत को उभारा और संगठित किया जाए और प्रार्थनापत्रों, सभाओं, प्रस्तावों तथा भाषणों के द्वारा अधिकारियों तक जनता की माँगों को पहुँचाया जाए तो वे धीरे-धीरे एक-एक करके इन माँगों को पूरा करेंगे।इसलिए उनके राजनीतिक कार्य की दो दिशाएँ थीं। प्रथम, भारत की जनता में राजनीतिक चेतना तथा राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए एक शक्तिशाली जनमत तैयार करना तथा जनता को राजनीतिक प्रश्नों का शिक्षित और एकताबद्ध करना। राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव तथा प्रार्थनापत्र भी मूलतः इसी लक्ष्य द्वारा निर्देशित थे। हालाँकि देखने में तो उनके स्मरणपत्र और प्रार्थनापत्र सरकार को संबोधित थे, मगर उनका वास्तविक उद्देश्य भारतीय जनता को शिक्षित करना था। उदाहरण के लिए जब 1891 में युवक गोखले ने पूना सार्वजनिक सभा द्वारा सावधानी के साथ तैयार करके भेजे गए दो पंक्तियों के उत्तर पर अपनी निराशा व्यक्त की तो जस्टिस रानाडे ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की - आप अपने देश के इतिहास में हमारे स्थान को नहीं समझते। ये स्मरणपत्र कहने को सरकार के नाम संबोधित हैं। वास्तव में ये जनता को संबोधित हैं ताकि वह जान सकें कि इन विषयों पर कैसे विचार करना चाहिए। यह काम किसी परिणाम की आशा किए बिना अभी अनेक वर्षो तक चलाया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की राजनीति इस देश के लिए एकदम नई वस्तु है। दूसरे, आरंभिक राष्ट्रवादी ब्रिटिश सरकार तथा ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना चाहते थे ताकि जिस प्रकार के सुधार राष्ट्रवादी द्वारा सुझाव गए थे उनको लागू किया जाए। नरमपंथी राष्ट्रवादियों का विश्वास था कि ब्रिटिश जनता और संसद भारत के साथ न्याय तो करना चाहती थी, मगर उन्हें यहाँ की वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं थी। इसलिए जनमत को शिक्षित करने के साथ-साथ नरमपंथी राष्ट्रवादी ब्रिटिश जनमत को शिक्षित करने के प्रयास भी कर रहे थे। इस उद्देश्य से उन्होंने ब्रिटेन में जमकर प्रचार-कार्य किया। भारतीय पक्ष को सामने रखने के लिए प्रमुख भारतीयों के दल ब्रिटेन भेजे गए। 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति बनाई गई। इस समिति ने 1890 में इंडिया नामक एक पत्रिका भी निकालनी आरंभ की। दादाभाई नौरोजी ने अपने जीवन तथा आय का एक बड़ा हिस्सा इंग्लैंड में रहकर वहाँ की जनता में भारत की माँगों का प्रचार करने में लगा दिया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययनकर्ता कभी-कभी भ्रम में पड़ जाते हैं, जब वे पाते हैं कि प्रमुख भारतीय नेता अंग्रेजों के प्रति वफादारी की बड़ी-बड़ी कसमें खाते थे। इन कसमों का अर्थ हर्गिज यह नहीं है कि वे सच्चे देशभक्त नहीं थे या वे कायर लोग थे। उनका दिल से विश्वास था कि ब्रिटिश के साथ भारत का राजनीतिक संबंध बने रहना इतिहास के उस चरण में भारत के हित में था। इसलिए उनकी योजना अंग्रेजों को माँगने की नहीं बल्कि ब्रिटिश शासन का रूपांतरण करके उसे एक राष्ट्रीय शासन के समान बनाने की थी। बाद में जब उन्होंने ब्रिटिश शासन की बुराइयों को तथा सुधार की राष्ट्रवादी माँगों को स्वीकार करने में सरकार की असफलता को समझा तो उनमें से अनेक ने ब्रिटिश शासन के प्रति वफादारी की कसम खाना बंद करके भारत के लिए स्वशासन की माँग उठानी आंरभ कर दी। इसके अलावा उनमें से अनेक केवल इसलिए नरमपंथी थे क्योंकि वे समझते थे कि विदेशी शासकों को खुलकर चुनौती देने का समय अभी नहीं आया था। जनता की भूमिकासंकुचित सामाजिक आधार आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की बुनियादी कमजोरी थी। अभी जनता में इस आंदोलन की पैठ नहीं हुई थी। वास्तव में जनता में नेताओं की कोई राजनीतिक आस्था नहीं थी। सक्रिय राजनीतिक संघर्ष छेड़ने की समस्याओं का वर्णन करते हुए गोपालकृष्ण गोखले ने कहा कि ’’देश में विभाजन तथा उपविभाजन की एक अंतहीन श्रंखला है, जनता का अधिकांश भाग अज्ञान से भरा हुआ तथा विचार और भावना के पुराने तरीकों से कसकर चिपका हुआ है और यह जनता हर प्रकार के परिवर्तन की विरोधी है और परिवर्तन को समझती नहीं है।‘‘ इस प्रकार नरमपंथी नेताओं का विश्वास था कि औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जुझारू जन-संघर्ष तभी छेड़ा जा सकता है जबकि भारतीय समाज के बहुविध तत्वों को एक राष्ट्र के सूत्र में बाँधा जा चुका हो, परंतु वास्तव में यही तो वह संघर्ष था जिनके दौरान भारतीय राष्ट्र का निर्माण हो सकता था। जनता के प्रति इस गलत दृष्टिकोण का नतीजा यह हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभिक चरण में जनता की एक निष्क्रिय भूमिका ही रही। इससे राजनीतिक नरमी का जन्म हुआ। जनता के समर्थन के अभाव में वे जुझारू राजनीतिक उपाय नहीं अपना सकते थे। हम आगे देखेंगे कि बाद के राष्ट्र वादी लोग नरमपंथियों से ठीक इसी अर्थ में भिन्न थे।फिर भी आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन के संकुचित सामाजिक आधार से हमें यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि यह उन्हीं सामाजिक वर्गो के संकुचित हितों तक सीमित था जो इसमें शामिल थे। इसके कार्यक्रम और इसकी नीतियाँ भारतीय जनता के सभी वर्गों के हितों से जुड़ी थीं और औपनिवेशिक वर्चस्व के विरूद्ध उदीयमान भारतीय राष्ट्रीय का प्रतिनिधित्व करती थीं। सरकार का रवैयाआरंभ से ही ब्रिटिश अधिकारी उभरते हुए राष्ट्रवादी आंदोलन के खिलाफ तथा राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति शंकालु थे। वायसराय डरफिन ने हृयूम को यह सुझाव दिया कि कांग्रेस राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक मामलों को देखे और यह इस तरह उसने राष्ट्रीय आंदोलन को दिशाभ्रष्ट करना चाहा। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने ऐसा परिवर्तन करने से इनकार कर दिया, परंतु जल्दी ही यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रीय कांग्रेस अधिकारियों के हाथों का खिलौना नहीं बन सकती है और यह धीरे-धीरे भारतीय राष्ट्रवाद का केन्द्रबिंदु बनती जा रही थी। अब ब्रिटिश अधिकारी खुलकर राष्ट्रीय कांग्रेस तथा दूसरे राष्ट्रवादी प्रवक्ताओं की आलोचना और निंदा करने लगे। डरफिन से लेकर नीचे तक के सभी ब्रिटिश अधिकारी राष्ट्रवादी नेताओं को “बेवफा बाबू”, “राजद्रोही ब्राह्मण” तथा “हिंसक खलनायक” कहने लगे। कांग्रेस को “राजद्रोह का कारखाना” कहा जाने लगा। डरफिन ने 1887 में एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे ‘जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग’ का प्रतिनिधि बताकर उसकी हँसी उड़ाई।लार्ड कर्जन ने 1890 में विदेश सचिव को बतलाया कि “कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी मुख्य महत्वकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं।” भारतीय जनता की बढ़ती एकता उनके शासन के लिए एक बड़ा खतरा है, यह महसूस करके अंग्रेज अधिकारियों ने “बाँटों और राज करो” की नीति को और भी जमकर लागू किया। उन्होने सैयद अहमद खान, बनारस के राजा शिवप्रसाद तथा दूसरे ब्रिटिश-समर्थक व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया कि वे कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन चलाएँ। उन्होने हिन्दुओं और मुसलमानों में भी फूट डालने की कोशिश की। राष्ट्रवाद का विकास रोकने के लिए उन्होंने एक तरफ छोटी-छोटी छूटें देने और दूसरी तरफ निर्मम दमन करने की नीति अपनाई। फिर भी, अधिकारियों का यह विरोध राष्ट्रीय आंदोलन का विकास रोकने में असफल रहा। आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन का मूल्याँकनकुछ आलोचकों का विचार है कि राष्ट्रवादी आंदोलन और राष्ट्रीय कांग्रेस को आरंभिक चरण में अधिक सफलता नहीं मिली। जिन सुधारों के लिए राष्ट्रवादियों ने आंदोलन छेड़े उनमे से बहुत थोड़े सुधार ही सरकार ने लागू किए।इस आलोचना में बहुत कुछ सच्चाई है। मगर आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन को असफल घोषित करना भी आलोचकों के लिए सही नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखों तो जो काम उन्होंने हाथ में लिए थे, उसकी तात्कालिक कठिनाईयों को देखते हुए, इस आंदोलन का इतिहास बहुत उज्जवल है। यह अपने समय की सबसे प्रगतिशील शक्ति का सूचक था। यह एक व्यापक राष्ट्रीय जागृति लाने तथा जनता में एक ही भारतीय राष्ट्र के सदस्य होने की भावना जगाने में सफल रहा। इसने भारतीय जनता को उनके साझे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हितों से जुड़े होने तथा साम्राज्यवाद के रूप में एक साझे शत्रु के अस्तित्व के प्रति जागरूक किया और इस प्रकार उनको एक राष्ट्र में एकताबद्ध किया। इसने जनता को राजनीतिक कार्य में प्रशिक्षित किया, उनमें जनतंत्र, नागरिक स्वतंत्रताओं, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्रवाद के विचारों को लोकप्रिय बनाया, उनमें आधुनिक दृष्टिकोण जगाया तथा ब्रिटिश शासन की बुराइयों को उनके सामने रखा। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के सही चरित्र को निर्ममतापूर्वक उजागर करने में आरंभिक राष्ट्रवादियों ने अग्रगामी भूमिका निभाई। उन्होंने लगभग प्रत्येक महत्वपूर्ण आर्थिक प्रश्न को देश की राजनीतिक रूप से पराधीन स्थिति से जोड़ा। साम्राज्यवाद की उनकी शक्तिशाली अर्थशास्त्रीय अलोचना ब्रिटिश शासन के खिलाफ बाद के सक्रिय जनसंघर्ष के दौरान राष्ट्रवादी आंदोलन का एक प्रमुख अस्त्र बन गई। अपने आर्थिक आंदोलन के द्वारा ब्रिटिश शासन के निर्मम, शोषण चरित्र को बेनकाब करके उन्होंने उसके नैतिक आधारों को भी कमजोर किया। आरंभिक राष्ट्रीवादी आंदोलन ने एक साझा राजनीतिक-आर्थिक कार्यक्रम भी पेश किया जिसके आधार पर भारतीय जनता एकजुट होकर बाद में राजनीतिक संघर्ष चला सकी। इसने यह राजनीतिक सत्य सामने रखा कि भारत का शासन भारतीयों के हित में चलना चाहिए। इसने राष्ट्रवाद के प्रश्न को भारतीय जीवन का एक प्रमुख प्रश्न बना दिया। इसके अलावा, नरमपंथियों का राजनीतिक कार्य धर्म, भावुकता या खोखली भावना की दुहाई न देकर जनता के जीवन की ठोस वास्तविकता के ठोस अध्ययन और विशेषण पर आधारित था। आरंभिक आंदोलन की कमजोरियों को तो बाद की पीढ़ियों ने दूर कर दिया उसकी उपलब्धियाँ आगे के वर्षों में एक और जोरदार राष्ट्रीय आंदोलन का आधार बन गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि अपनी तमाम कमियों के बावजूद आरंभिक राष्ट्रवादियों ने वह बुनियाद बनाई जिस पर राष्ट्रीय आंदोलन आगे और भी विकसित हुआ। इसलिए उन्हें आधुनिक भारत के निर्माताओं में ऊँचा स्थान मिलना चाहिए। | |||||||||
| |||||||||