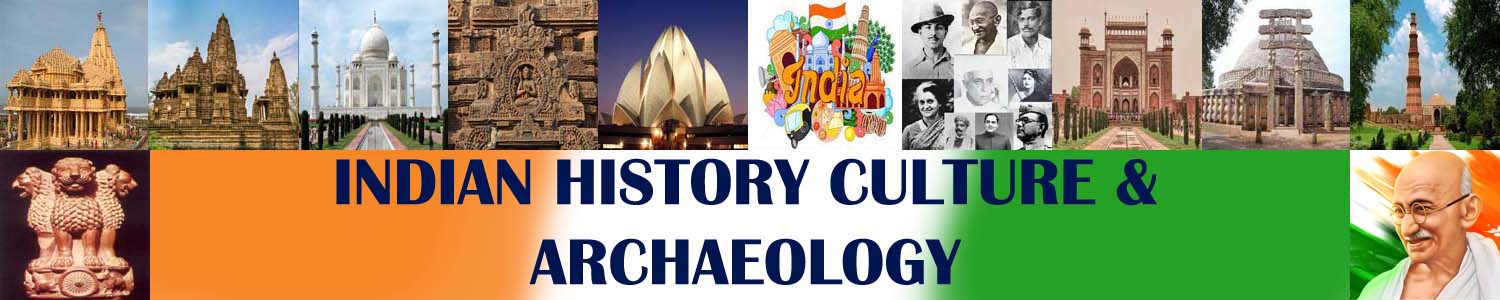| |||||||||
|
19वीं सदी में धार्मिक और सामाजिक सुधार
1858 के बाद धार्मिक और सामाजिक सुधारराष्ट्रवाद तथा लोकतंत्र की वह उठती लहर, जिसमें स्वतंत्रता के संघर्ष को जन्म दिया था उन आंदोलनों के रूप में भी सामने आई जिनका उद्देश्य सामाजिक संस्थाओं तथा भारतीय जनता के धार्मिक दृष्टिकोण का सुधार करना और उनका लोकतंत्रीकरण करना था। अनेक भारतीयों ने यह अनुभव किया कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आधुनिक ढंग से देश का चौतरफा विकास करने तथा राष्ट्रीय एकता और एकजुटता को विकसित करने के लिए आवश्यक हैं। राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास, नई आर्थिक शक्तियों का उदय, शिक्षा का प्रसार, आधुनिक पश्चिमी विचारों तथा संस्कृति का प्रभाव तथा दुनिया के बारे में पहले से अधिक जानकारी, इन सभी बातों ने भारतीय समाज के पिछड़ेपन तथा पतन के बारें में लोगों की चेतना को बढ़ाया ही नहीं बल्कि सुधार के संकल्प को और मजबूत किया। उदाहरण के लिए, केशवचंद्रसेन ने कहा -आज हम जो कुछ अपने इर्द-गिर्द देखते हैं वह एक पतित राष्ट्र है - एक ऐसा राष्ट्र जिसकी प्राचीन महानता विध्वंस होकर बिखरी पड़ी है। इसका राष्ट्रीय साहित्य और विज्ञान, इसका धर्मशास्त्र और दर्शन, इसका उद्योग और वाणिज्य, इसकी सामाजिक समृद्धि और घरेलू सरलता तथा मधुरता, यह सभी समाप्त हो चुकी बातों के साथ लगभग जा ही चुकी हैं। जब हम अपने चारों ओर बढ़ते आध्यात्मिक, सामाजिक तथा बौद्धिक सूनेपन का दुखजनक तथा निराशाजनक दृष्य देखते हैं तो हम इसमें कालिदास के, काव्य के, विज्ञान के तथा सभ्यता के देश को पहचानने का व्यर्थ प्रयत्न करते हैं। इसी तरह स्वामी विवेकानंद ने भारतीय जनता की स्थिति को इन शब्दों में व्यक्त किया - चिथड़ों में लिपटे वृद्धों और युवकों के यहाँ-वहाँ भटकते कृशकाय ढाँचे, जिनके चहरों पर सैकड़ों वर्षों की निराशा तथा गरीबी ने गहरी झुर्रियाँ डाल रखी हैं, हर जगह पाए जाने वाले गाएँ, बैल तथा भैंस जैसे पशु उनकी आँखों में वही गहरी उदासी, वही दुर्बल शरीर, सड़क के किनारे बिखरा कूड़ा और गर्द-क्या यही हमारा आज का भारत है। महलों के ठीक पड़ोस में चरमराती झोपड़ियाँ, मंदिर के ठीक पास कूड़े के ढेर, तड़क-भड़क वस्त्रों में सजे व्यक्ति के साथ-साथ चलता हुआ लंगोट पहने सन्यासी, अच्छे भोजन तथा तमाम सुविधाओं से संपन्न व्यक्ति को दया की भीख माँगती और बेचमक निगाहों से देखता हुआ एक भूख का मारा व्यक्ति-क्या हमारा अपना देश है ! भयानक प्तेग तथा कालरा के कारण भयानक तबाही, देश के पोर-पोर को चबाता हुआ मलेरिया, मनुष्य की दूसरी प्रकृति बन चुकी भुखमरी और अर्ध-भुखमरी, तांडव-नृत्य करता हुआ अकाल का दानव................. तीस करोड़ लोगों का यह समूह जो कहने भर को मनुष्य हैं, अपने की देशवासियों तथा विदेशी राष्ट्रों द्वारा पीड़ित होकर जीवनहीन............... किसी आशा, किसी अतीत, किसी भविष्य से वंचित................. ऐसे कुटिल चरित्र के लोग जो केवल गुलामों को शोभा दे, जिनके लिए अपने ही भाइयों की संपत्ति असहृय है................. उन बलवानों के तलवे चाटते हुए जो बलहीनों को प्राणघातक चोटें पहुँचा रहे हैं................. ऐसे भोंडे तथा निकृष्ट अंधविश्वासों से ग्रस्त तो स्वाभाविक तौर पर कमजोर तथा भविष्य से निराश लोगों में आ जाते हैं................किसी भी नैतिक मानदंड से रहित.................. इन तरह के तीन करोड़ प्राणी जो भारत के शरीर पर इस तरह रेंग रहे हैं जैसे कि सड़ती और बदबू देती लाशों के ऊपर कीड़े रेंगते हैं - हमारे बारे में यही वह तस्वीर है जो स्वाभाविक तौर पर अंग्रेज अधिकारियों के सामने उभरती है। इस तरह 1858 के बाद पहले की सुधारवादी प्रवृत्ति का आधार और व्यापक हुआ। राजा राममोहन राय तथा ईश्वरचंद्र विधासागर जैसे आरंभिक सुधारवादियों के काम को धार्मिक तथा सामाजिक सुधार के प्रमुख आंदोलनों ने और आगे बढ़ाया। धार्मिक सुधारविज्ञान, जनतंत्र तथा राष्ट्रवाद की आधुनिक दुनिया की आवश्यकताओं के अनुसार अपने समाज को ढालने की इच्छा लेकर तथा यह संकल्प करके कि इस रास्ते में कोई बाधा नहीं रहने दी जाएगी, विचारशील भारतीयों ने अपने पारंपरिक धर्मों के सुधार का काम आरंभ किया। कारण कि धर्म उन दिनों जनता के जीवन का एक अभिन्न अंग था और धार्मिक सुधार के बिना सामाजिक सुधार भी कुछ खास संभव नहीं था। अपने धर्मों के आधार के प्रति सच्चे रहकर भी उन्होंने उनको भारतीय जनता की नई आवश्यकताओं के अनुसार ढाला।ब्रह्म समाजराजा राममोहन राय की ब्रह्म परंपरा को 1843 के बाद देवेंद्रनाथ ठाकुर ने आगे बढ़ाया। उन्होंने इस सिद्धान्त का भी खंडन किया कि वैदिक ग्रंथ अनुल्लंघनीय हैं। 1866 के बाद इस आंदोलन को केशवचंद्र सेन ने आगे जारी रखा। ब्रह्म समाज ने हिंदू धर्म की कुरीतियों को हटाकर, उसे एक ईश्वर की पूजा पर आधारित करके, तथा वेदों को अनुल्लंघनीय न मानकर भी वेदों तथा उपनिषदों की शिक्षाओं के आधार पर उसमें सुधार लाने की कोशिश की। सबसे बड़ी बात यह है कि उसने अपना आधार मानव-बुद्धि को बनाया तथा उसे यह जानने की कसौटी बतलाया कि प्राचीन या वर्तमान धार्मिक सिद्धान्तों और व्यवहारों में क्या उपयोगी तथा क्या अनुपयोगी है। इस कारण धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग को भी ब्रह्म समाज ने अनावश्यक बताया। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार तथा क्षमता प्राप्त है कि वह अपनी बुद्धि की सहायता से यह देखे कि किसी धार्मिक ग्रंथ या सिद्धान्त में क्या गलत है और क्या सही है। इस तरह ब्रह्म समाजी मूलतः मूर्तिपूजा तथा अंधविश्वासपूर्ण कर्मकांडों के, बल्कि पूरी ब्राह्मणवादी परंपरा के विरोधी थे। वे बिना किसी पुरोहित की मध्यस्थता के एक ईश्वर की पूजा करते थे।ब्रह्म लोग महान समाज-सुधारक भी थे। उन्होंने जाति-प्रथा तथा बाल विवाह का जमकर विरोध किया विधवा-पुनर्विवाह समेत स्त्री-कल्याण के सभी उपायों के तथा स्त्री-पुरूषों के बीच आधुनिक शिक्षा के प्रसार के वे समर्थक थे। ब्रह्म समाज अपने आंतरिक कलह के कारण उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में कमजोर पड़ गया। इसके अलावा इसका प्रभाव अधिकांश नगरीय शिक्षित वर्ग तक ही सीमित था। फिर भी 19वीं और 20वीं सदी में बंगाल तथा शेष भारत के बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। महाराष्ट्र में धार्मिक सुधारबंबई प्रांत में धार्मिक सुधार-कार्य का आरंभ 1840 में परमहंस मंडली ने आरंभ किया। इसका उद्देश्य मूर्तिपूजा तथा जातिप्रथा का विरोध करना था। पश्चिमी भारत के पहले धार्मिक सुधारक संभवतः गोपाल हरि देशमुख थे जिन्हें जनता ‘लोकहितवादी’ कहती थी। वे मराठी भाषा में लिखते थे। उन्होंने हिन्दू कट्टरपंथ पर भयानक बुद्धिवादी आक्रमण किए और धार्मिक तथा सामाजिक समानता का प्रचार किया। उदाहरण के लिए, 1840 के दशक में उन्होंने लिखा -पुरोहित बहुत ही अपवित्र है क्योंकि कुछ बातों को बिना उनका अर्थ समझे दुहराते रहते हैं और ज्ञान को इसी रटंत तक भोंडे ढंग से सीमित करके रख देते हैं।............... पंडित तो पुरोहितों से भी बुरे हैं क्योंकि वे और भी अज्ञानी हैं तथा अहंकारी भी हैं................ब्राह्मण कौन हैं और किन अर्थों में वे हमसे भिन्न हैं ? क्या उनके बीस हाथ हैं और क्या हममें कोई कमी है ? अब जब ऐसे सवाल पूछे जाएँ तो ब्राह्मणों को अपनी मूर्खतापूर्ण धारणाएँ त्याग देनी चाहिए, उन्हें यह मान लेना चाहिए कि सभी मनुष्य बराबर हैं तथा हर व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर धर्म सामाजिक सुधार की अनुमति नहीं देता तो उसे बदल दिया जाना चाहिए। कारण की धर्म को मनुष्य ने ही बनाया है और बहुत पहले लिखे गये धर्मग्रंथ हो सकता हैं की बाद के काल के लिए प्रासंगिक न रह जाएँ। बाद में आधुनिक ज्ञान के प्रकाश में हिंदू धार्मिक विचारों तथा व्यवहारों में सुधार लाने के लिए प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसने ईश्वर की पूजा का प्रचार किया तथा धर्म को जाति-प्रथा की रूढ़ियों से और पुरोहितों के वर्चस्व से मुक्त करने का प्रयास किया। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान तथा इतिहासकार आर. जी. भंडारकर और महादेव गोविन्द रानाडे (1842-1901) इसके प्रमुख नेता थे। इस पर ब्रह्म समाज का गहरा प्रभाव था तेलुगू सुधारक वीरेशलिंगम के प्रयासों से इसका प्रसार दक्षिण भारत में भी हुआ। इसी समय महाराष्ट्र में गोपाल गणेश आगरकर भी कार्यरत थे जो आधुनिक भारत के महानतम बुद्धिवादी विचारकों में एक हैं। ये मानव-बुद्धि की क्षमता के प्रचारक थे। परंपरा पर अंध-श्रद्धा तथा भारत के अतीत के झूठे महिमामंडन की भी उन्होंने कड़ी आलोचना की। रामकृष्ण और विवेकांनदरामकृष्ण परमंहस (1834-1886) एक संत चरित्र व्यक्ति थे जो त्याग-ध्यान-भक्ति की पारंपरिक विधियों से धार्मिक मुक्ति पाने में विश्वास रखते थे। धार्मिक सत्य की खोज तथा स्वयं में ईश्वर का अनुभव करने के उद्देश्य से वे मुस्लिम तथा ईसाई दरवेशों के साथ भी रहे। उन्होंने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुँचने तथा मुक्ति पाने के कई मार्ग हैं और यह कि मनुष्य की सेवा ईश्वर की सेवा है, क्योंकि मनुष्य ईश्वर का ही मूर्तिमान रूप है।उनके धार्मिक संदेशों को उनके महान शिष्य स्वामी विवेकानंद (1863-1902) ने प्रचारित किया तथा उनको समकालीन भारतीय समाज की आवश्यकताओं के अनुसार ढालने का प्रयास किया। विवेकानंद का सबसे अधिक जोर सामाजिक क्रिया पर था। उन्होंने कहा कि ज्ञान अगर वास्तविक दुनिया में जिसमें हम रहते हैं, कर्म से हीन हो तो व्यर्थ है। अपने गुरू की तरह उन्होंने भी सभी धर्मों की बुनियादी एकता की घोषणा की तथा धार्मिक बातों में संकुचित दृष्टिकांण की निंदा की। जैसा कि 1898 में उन्होंने लिखा था - ’’हमारी अपनी मातृ भूमि के लिए दो महान धर्मों-हिंदुत्व तथा इस्लाम-का संयोग ही . . . . एकमात्र आशा है।‘‘ साथ ही वे भारतीय दर्शन-परंपरा के श्रेष्ठकर दृष्टिकोण में भी विश्वास रखते थे। वे खुद वेदांत के अनुयायी थे जिसे उन्होंने एक पूर्णतः बुद्धिसंगत प्रणाली बतलाया। विवेकानंद ने भारतीयों की आलोचना की कि बाकी दुनिया से कटकर वे जड़ तथा मृतप्राय हो गए हैं। उन्होंने लिखा - ‘‘दुनिया के सभी दूसरे राष्ट्रों से हमारा अलगाव ही हमारे पतन का कारण है और शेष दुनिया की धारा में समा जाना ही इसका एकमात्र समाधान है। गति जीवन का चिन्ह है।’’ विवेकानंद ने जाति-प्रथा की तथा कर्मकांड, पूजा-पाठ और अंधविश्वास पर हिंदू धर्म के तत्कालीन जोर देने की निंदा की तथा जनता से स्वाधीनता, समानता तथा स्वतंत्र चिंतन की भावना अपनाने का आग्रह किया। इस बारे में उनकी तीखी टिप्पणी इस प्रकार थी - हमारे सामने खतरा यह है कि हमारा धर्म रसोईघर में न बंद हो जाए। हम, अर्थात हममें से अधिकांश न वेदांती हैं, न पौराणिक और न ही तांत्रिक। हम केवल ‘हमें मत छुओ’ के समर्थक हैं। हमारा ईश्वर भोजन के बर्तन में है और हमारा धर्म यह है कि ‘हम पवित्र हैं, हमें छूना मत।’ अगर यही सब कुछ एक शताब्दी और चलता रहा तो हममें से हर एक व्यक्ति पागलखाने में होगा। विचारों की स्वतंत्रता के लिए कहा - विचार और कर्म की स्वतंत्रता जीवन, विकास तथा कल्याण की अकेली शर्त है। जहाँ यह न हो वहाँ मनुष्य, जाति तथा राष्ट्र सभी पतन के शिकार होते हैं। अपने गुरू की तरह विवेकानंद भी एक महान मानवतावादी थे। देश की साधारण जनता की गरीबी, बदहाली और पीड़ा से दुखी होकर उन्होंने लिखा है - मैं एक ईश्वर को मानता हूँ जो सभी आत्माओं की एक आत्मा है और सबसे ऊपर है। मेरा ईश्वर दुखी मानव है, मेरा ईश्वर पीड़ित आत्मा है, मेरा ईश्वर हर जाति का निर्धन मनुष्य है।” शिक्षित भारतीयों से वे कहते हैं - जब तक लाखों-लाख लोग भूख तथा अज्ञान से ग्रस्त हैं, मैं हर उस व्यक्ति को देशद्रोही कहूँगा जो उसके खर्च पर शिक्षा पाकर भी उन पर कोई ध्यान नहीं देता। मानवतावादी राहत-कार्य तथा समाज-कार्य को जारी रखने के लिए 1896 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। देश के विभिन्न भागों में इस मिशन की प्रमुख शाखाएँ थीं और इसने स्कूल, अस्पताल और दवाखाने, अनाथालय और पुस्तकालय, आदि खोलकर सामाजिक सेवा के कार्य किए। इस तरह इसका जोर व्यक्ति की मुक्ति नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण और समाज सेवा पर था। स्वामी दयानंद और आर्यसमाजउत्तर भारत में हिन्दू धर्म के सुधार का बीड़ा आर्यसमाज ने उठाया। इसकी स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद (1824-1883) ने की थी। उनका मानना था कि तमाम झूठी शिक्षाओं से भरे पुराणों की सहायता से स्वार्थीं व अज्ञानी पुरोहितों ने हिंदू धर्म को भ्रष्ट कर रखा था। अपने लिए दयानंद ने वेदों से प्रेरणा प्राप्त की जिनको ईश्वर-कृत होने के नाते वे अनुल्लंघनीय तथा सभी ज्ञान का भंडार मानते थे। उन्होंने उन बाद के सभी धर्मिक विचारों को रद्द कर दिया जो वेदों से मेल नही खाते थे। वेदों तथा उनकी अनुल्लंघनीयता पर इस तरह की पूर्ण निर्भरता ने उनकी शिक्षाओं को रूढ़िवादी रंग में रंग दिया क्योंकि उनकी अनुल्लंघनीयता का अर्थ यह है कि मानव-बुद्धि अंतिम निर्णायक नहीं रही।फिर भी, इस दृष्टिकोण का एक बुद्धिसंगत पक्ष भी था। कारण कि ईश्वर-प्रदत्त होने के बावजूद वेदों की व्याख्या उन्हें तथा दूसरे मनुष्यों को ही बुद्धिसंगत ढंग से करनी होगी। वे मानते थे कि प्रत्येक को ईश्वर तक सीधे पहुँचने का अधिकार है। इसके अलावा, हिंदू कट्टरपंथ का समर्थन करने की बजाए उन्होंने इस पर हमला किया तथा इसके खिलाफ एक विद्रोह छेड़ा। परिणामस्वरूप वेदों की अपनी व्याख्या से उन्होंने जो भी शिक्षाएँ ग्रहण की वे दूसरे भारतीयों द्वारा प्रचारित किए जा रहे धार्मिक व सामाजिक सुधारों से मिलती-जुलती थीं। वे मूर्तिपूजा, कर्मकांड और पुरोहितवाद के तथा खासकर जाति-प्रथा और ब्राह्मणों द्वारा प्रचलित हिंदु धर्म के विरोधी थे। उन्होंने इसी वास्तविक जगत में रह रहे मनुष्यों की समस्याओं की ओर ध्यान दिया तथा दूसरी दुनिया में परंपरागत विश्वास से लोगों का ध्यान हटाया। वे पश्चिमी विज्ञानों के अध्ययन के भी समर्थक थे। दिलचस्प बात यह है कि स्वामी दयानंद ने केशवचन्द्र सेन, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, जस्टिस रानाडे, गोपाल हरि देशमुख तथा दूसरे आधुनिक धर्म-समाज-सुधारकों से मिलकर उनसे वाद-विवाद भी किए थे। वास्तव में आर्यसमाज का इतवारी सभाओं का विचार इस बारे में ब्रह्म समाज तथा प्रार्थनासमाज के व्यवहार से मिलता-जुलता था। स्वामी दयानंद के कुछ शिष्यों ने बाद में पश्चिमी ढंग की शिक्षा के प्रसार के लिए देश भर में स्कूलों तथा कॉलेजों का एक पूरा जाल-सा बिछा दिया। इस प्रयास में लाला हंसराज की एक प्रमुख भूमिका रही। दूसरी तरफ कुछ अधिक परंपरावादी शिक्षा के प्रसार के लिए स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में हरिद्वार के निकट गुरूकुल की स्थापना की। आर्यसमाजी सुधार के प्रखर समर्थक थे। स्त्रियों की दशा सुधारने तथा उनमें शिक्षा का प्रसार करने के लिए उन्होंने बहुत से काम किए। उन्होंने छुआछूत तथा वंश-परंपरा पर आधारित जाति-प्रथा की कठोरताओं का विरोध किया। इस तरह वे सामाजिक समानता के प्रचारक थे तथा उन्होंने सामाजिक एकता को मजबूत बनाया। उन्होंने जनता में आत्मसम्मान तथा स्वावलंबन की भावना भी जगाई। इससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। साथ ही साथ, आर्यसमाज का एक उद्देश्य हिंदुओं को धर्म-परिवर्तन से रोकना भी था। इसके कारण दूसरे धर्मो के खिलाफ एक जेहाद छेड़ दिया। यह जेहाद बीसवीं सदी में भारत में सांप्रदायिकता के प्रसार में सहायक एक कारण बन गया। आर्यसमाज के सुधार-कार्य ने समाज की बुराइयाँ खत्म करके जनता को एकबद्ध करने का प्रयास किया, मगर उसके धार्मिक कार्य में संभवतः अचेतन रूप में ही विकासमान हिंदुओं, मुसलमानों, पारसियों, सिखों और ईसाइयों के बीच पनप रही राष्ट्रीय एकता को भंग करने की ही प्रवृत्ति थी। उसे यह बात स्पष्ट नहीं थी कि भारत में राष्ट्रीय एकता धर्मनिरपेक्ष आधार पर तथा धर्म से परे रहकर ही संभव है ताकि यह सभी धर्मों के लोगों को समेट सके। थियोसोफिकल सोसायटीथियोसोफिकल सोसायटी की स्थापना संयुक्त राज्य अमरीका में मैडम एच. पी. ब्लावात्सकी तथा कर्नल एच. एस. ओलकाट द्वारा की गई। बाद में ये भारत आ गए तथा 1886 में मद्रास के करीब अदियार में उन्होंने सोसायटी का हेडक्वार्टर स्थापित किया। 1893 में भारत आनेवाली श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में थियोसोफी आंदोलन जल्द ही भारत में फैल गया। थियोसोफिस्ट प्रचार करते थे कि हिंदुत्व, जरथुस्त्र मत (पारसी धर्म) तथा बौद्ध मत जैसे प्राचीन धर्मों को पुनर्स्थापित तथा मजबूत किया जाए। उन्होंने आत्मा के पुनरागमन के सिद्धांत का भी प्रचार किया। धार्मिक पुनर्स्थापनावादियों के रूप में थियोसोफिस्टों को बहुत सफलता नहीं मिली। लेकिन आधुनिक भारत के घटनाक्रमों में उनका एक विशिष्ट योगदान रहा। यह पश्चिमी देशों के ऐसे लोगों द्वारा चलाया जा रहा एक आंदोलन था। जो भारतीय धर्मों तथा दार्शनिक परंपरा का महिमामंडन करते थे। इससे भारतीयों को अपना खोया आत्मविश्वास फिर से पाने में सहायता मिलीं हालाँकि अतीत की महानता का झूठा गर्व भी इसने उनके अंदर पैदा किया।भारत में श्रीमती एनी बेसेंट के प्रमुख कार्यों में एक था बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना जिसे बाद में मदनमोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया। सैयद अहमद खान तथा अलीगढ़ आंदोलनमुसलमानों में धार्मिक सुधार के आंदोलन कुछ देर से उभरे। उच्च वर्गों के मुसलमानों ने पश्चिमी शिक्षा व संस्कृति के संपर्क से बचने की ही कोशिशें कीं। केवल 1857 के महाविद्रोह के बाद ही धार्मिक सुधार के आधुनिक विचार उभरने शुरू हुए। इस दिशा में आरंभ 1863 में कलकत्ता में स्थापित मुहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी ने किया। इस सोसाइटी ने आधुनिक विचारों के प्रकाश में धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रश्नों पर विचार-विमर्श को बढ़ावा दिया तथा पश्चिमी शिक्षा अपनाने के लिए उच्च तथा मध्य वर्गों के मुसलमानों को प्रेरित किया।मुसलमानों में सबसे प्रमुख सुधारक सैयद अहमद खान (1817-1898) थे। वे आधुनिक वैज्ञानिक विचारों से काफी प्रभावित थे तथा जीवन भर इस्लाम के साथ उनका तालमेल करने के लिए प्रयत्नरत रहे। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले यह घोषित किया कि इस्लाम की एकमात्र प्रामाणिक पुस्तक कुरान है और सभी इस्लामी लेखन गौण महत्व का है। उन्होंने कुरान की व्याख्या भी समकालीन बुद्धिवाद तथा विज्ञान का रोशनी में की। उनके अनुसार कुरान की कोई भी व्याख्या अगर मानव-बुद्धि, विज्ञान या प्रकृति से टकरा रही है तो वह वास्तव में गलत व्याख्या है। उन्होंने कहा है कि धर्म के तत्व भी अपरिवर्तनीय नहीं है। धर्म अगर समय के साथ नहीं चलाता तो वह जड़ हो जाएगा जैसा की भारत में हुआ है। जीवन भर वे परंपरा के अंध अनुकरण, रिवाजों पर भरोसा, अज्ञान तथा अबुद्धिवाद के खिलाफ संघर्ष करते रहे। उन्होंने लोगो से आलोचनात्मक दृष्टिकोण तथा विचार की स्वतंत्रता अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने घोषणा की - “जब तक विचार की स्वतंत्रता विकसित नहीं होती, सभ्य जीवन संभव नहीं है।” उन्होंने कट्टरपंथ, संकुचित दृष्टि तथा अलग-थलग रहने के खिलाफ भी चेतावनी दी, तथा छात्रों और दूसरें लोगों से खुले दिल वाला तथा सहिष्णु बनने का आग्रह किया। उन्होंने कहा की बंद दिमाग सामाजिक-बौद्धिक पिछड़ेपन की निशानी है। विश्व भर के अमर साहित्य के अध्ययन की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा - (इससे) छात्र उस मानसिकता को समझ सकेगा जिसके सहारे महान व्यक्ति महान प्रश्नों पर विचार करते हैं। उसे पता चलेगा कि सत्य के अनेक पक्ष होते हैं और यह व्यक्तिगत मत का पर्याय या मात्र समकक्ष नहीं होता और यह कि दुनिया उसके अपने पंथ, समाज या वर्ग से कहीं बहुत अधिक व्यापक है। सैयद अहमद खान का विश्वास था कि मुसलमानों का धार्मिक और सामाजिक जीवन आधुनिक पाश्चात्य, वैज्ञानिक ज्ञान और संस्कृति को अपनाकर ही सुधर सकता है। इसलिए आधुनिक शिक्षा का प्रचार जीवन-पर्यन्त उनका प्रथम ध्येय रहा। अधिकारी के रूप में उन्होंने अनेक नगरों में विद्यालय स्थापित किए थे और अनेक पश्चिमी ग्रंथों का उर्दू में अनुवाद कराया था। उन्होंने 1875 में अलीगढ़ में मुहम्मडन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना पाश्चात्य विज्ञान तथा संस्कृति का प्रचार करने वाले एक केंद्र के रूप में की। बाद में इस कॉलेज का विकास अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में हुआ। सैयद अहमद खान धार्मिक सहिष्णुता के पक्के समर्थक थे। उनका विश्वास था की सभी धर्मों में एक बुनियादी एकता मौजूद है जिसे व्यवहारिक नैतिक कहा जा सकता है। वे मानते थे कि धर्म व्यक्ति का अपना निजी मामला है और इसलिए वे वैयक्तिक संबंधों में धार्मिक कट्टरता की निंदा करते थे। वे सांप्रदायिक टकराव के भी विरोधी थे। हिंदुओं और मुसलमानों से एकता का आग्रह करते हुए उन्होंने 1883 में कहा था - ‘हम दोनों भारत की हवा में सांस लेते हैं और गंगा-यमुना का पवित्र जल पीते हैं। हम दोनों भारत की धरती का अनाज खाकर जीवित रहते हैं। जीवन और मृत्यु, दोनों में हम एक साथ हैं। भारत में हमारे निवास ने हम दोनों का खून बदल डाला है, हमारें शरीर के रंग एक हो चुके हैं, हमारें हुलिए समान हो चुके हैं। मुसलमानों ने अनेक हिंदू रिवाजों को अपना लिया है तथा हिंदुओं ने मुसलमानों के आचार-विचार की बहुत सी बातें ले ली हैं। हम इस कदर एक हो चुके हैं कि हमने एक नई भाषा उर्दू को विकसित किया हैं जो न हमारी भाषा है और न हिंदुओं की। इसलिए हम अपने जीवन के उन पक्षों को छोड़ दें जो ईश्वर से संबंधित हैं तो निःसंदेह इस आधार पर कि हम दोनों एक ही देश में रहते हैं, हम एक राष्ट्र हैं, तथा देश की, तथा हम दोनों की प्रगति और कल्याण हमारी एकता, पारस्परिक सहानुभूति और प्रेम पर निर्भर है जबकि हमारा पारस्परिक मतभेद, अकड़, विरोध तथा दुर्भावना निश्चित ही हमें नष्ट कर देंगी। इसके अलावा इस कॉलेज के कोश में हिंदुओं, पारसियों और ईसाइयों ने भी जी खोलकर दान दिया, और इसके दरवाजे भी सभी भारतीयों के लिए खुले थे। उदाहरण के लिए, 1898 में इस कॉलेज में 64 हिंदू और 285 मुसलमान छात्र थे। सात भारतीय अध्यापकों में दो हिंदू थे और इनमें एक संस्कृत का प्रोफेसर था। मगर अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अपने अनुयायियों को उभरते राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने से रोकने के लिए सैयद अहमद खान हिंदुओं के वर्चस्व की शिकायतें करने लगे थे। यह दुर्भाग्य की बात थी। फिर भी वे बुनियादी पर सांप्रदायिक नहीं थे। वह केवल यह चाहते थे कि मध्य तथा उच्च वर्गों के मुसलमानों का पिछड़ापन खत्म हो। उनकी राजनीति उनके इस दृढ़ विश्वास की उपज थी कि ब्रिटिश सरकार को आसानी से नहीं हटाया जा सकता और इसलिए तात्कालिक राजनीतिक प्रगति संभव नहीं है। दूसरी तरफ, अधिकारियों की जरा सी भी शत्रुता शिक्षा-प्रसार के प्रयास के लिए घातक हो सकती थी जबकि वे इसे वक्त की जरूरत समझते थे। उनका विश्वास था कि जब भारतीय भी विचार व कर्म में अंग्रेजों जितने आधुनिक बन जाएँगे, केवल तभी वे सफलता के साथ विदेशी शासन को ललकार सकेंगे। इसलिए उन्होंने सभी भारतीयों तथा खासकर शैक्षिक रूप से पिछड़े मुसलमानों को सलाह दी कि वे कुछ समय के लिए राजनीति से दूर रहें। उनके अनुसार राजनीति का समय अभी नहीं आया था। वास्तव में वे अपने कॉलेज तथा शिक्षा-प्रसार के उद्देश्य के प्रति इस तरह समर्पित हो चुके थे कि इसके लिए अन्य सभी हितों का बलिदान करने को तैयार थे। परिणामस्वरूप, रूढ़िवादी मुसलमानों को कॉलेज का विरोध करने से रोकने के लिए उन्होंने धार्मिक सुधार के आंदोलन को भी लगभग त्याग दिया था। इसी कारण से वे कोई ऐसा काम नहीं करते थे कि सरकार रूष्ट हो तथा, दूसरी ओर, सांप्रदायिकता और अलगाववाद को प्रोत्साहन देने लगे थे। निश्चित ही यह एक गंभीर राजनीतिक त्रुटि थी जिसके बाद में हानिकारक परिणाम निकले। इसके अलावा उनके कुछ अनुयायी उनकी तरह खुले दिल वाले नहीं रहे और वे बाद में इस्लाम का तथा उसके अतीत का महिमामंडन करने लगे तथा दूसरे धर्मों की आलोचना करने लगे। सैयद अहमद ने सामाजिक सुधार के काम में भी उत्साह दिखाया। उन्होंने मुसलमानों से मध्यकालीन रीति-रिवाज तथा विचार व कर्म की पद्धतियों को छोड़ देने का आग्रह किया। उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने के बारे में लिखा तथा पर्दा छोड़ने तथा स्त्रियों में शिक्षा-प्रसार का समर्थन किया। उन्होंने बहुविवाह प्रथा तथा मामूली-मामूली बातों पर तलाक के रिवाज की भी निंदा की। सैयद अहमद खान को सहायता उनके कुछ वफादार अनुयायी किया करते थे। इन्हें सामूहिक रूप से अलीगढ़ समूह कहा जाता है। चिराग अली, उर्दू शायर अल्ताफ हुसैन हाली, नजीर अहमद तथा मौलाना शिबली नुमानी अलीगढ़ आंदोलन के कुछ और प्रमुख नेता थे। मुहम्मद इकबालआधुनिक भारत के महानतम कवियों में एक, मुहम्मद इकबाल (1876-1938) ने भी अपनी कविता द्वारा नौजवान मुसलमानों तथा हिंदुओं के दार्शनिक एंव धार्मिक दृष्टिकोण पर गहरा प्रभाव डाला। स्वामी विवेकानंद की तरह उन्होंने भी निरंतर परिवर्तन तथा अबाध कर्म पर बल दिया और विराग, ध्यान तथा एकांतवास की निंदा की। उहोंने एक गतिमान दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया जो दुनिया को बदलने में सहायक हों। वे मूलतः एक मानवतावादी थे। वास्तव में उन्होंने मानव कर्म को प्रमुख धर्म की स्थिति तक पहुँचा दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को प्रकृति या सत्ताधीशों के अधीन नही होना चाहिए बल्कि निरंतर कर्म द्वारा इस विश्व को नियंत्रित करना चाहिए। उनके विचार में स्थिति को निश्क्रिय रूप से स्वीकार करने से बड़ा पाप नहीं है। कर्मकांड, विराग तथा दूसरी दुनिया में विश्वास की प्रवृत्ति की निंदा करते हुए उन्होंने कहा है मनुष्य को इसी जीती-जागती दुनिया में सुख प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अपनी आरंभिक कविता में उन्होंने देशभक्ति के गीत गाँए हैं हालाँकि बाद में उन्होंने मुस्लिम अलगाववाद का समर्थन किया।पारसियों में धार्मिक सुधारपारसी लोगों में धार्मिक सुधार का आरंभ बंबई में 19वीं सदी के आरंभ में हुआ। 1851 में रहमानी मज़्दायासन सभा (रिलीजस रिफार्म एसोसिएशन) का आरंभ नौरोजी फरदूनजी, दादाभाई नौरोजी, एस. एस. बंगाली तथा अन्य लोगों नें किया। इस सभी ने धर्म के क्षेत्र में हावी रूढ़ि़वाद के खिलाफ आंदोलन चलाया, और स्त्रियों की शिक्षा तथा विवाह और कुल मिलाकर स्त्रियों की सामाजिक स्थिति के बारे में पारसी सामाजिक रीति-रिवाजों के आधुनिकीकरण का आरंभ किया। कालांतर में पारसी लोग सामाजिक क्षेत्र में पश्चिमीकरण की दृष्टि से भारतीय समाज के सबसे अधिक विकसित अंग बन गए।सिखों में सामाजिक सुधारसिख लोगों में धार्मिक सुधार का आरंभ 19वीं सदी के अंत में हुआ जब अमृतसर में खालसा कॉलेज की स्थापना हुई। लेकिन सुधार के प्रयासों को बल 1920 के बाद मिला जब पंजाब में अकाली आंदोलन का आरंभ हुआ। अकालियों का मुख्य उद्देश्य गुरूद्वारों के प्रबंध का शुद्धिकरण करना था। इन गुरूद्वारों को भक्त सिखों की ओर से भारी मात्रा में जमीनें और धन मिलते थे, परंतु इनका प्रबंध भ्रष्ट तथा स्वार्थी महंतों द्वारा मनमाने ढंग से किया जा रहा था। अकालियों के नेतृत्व में 1921 में सिख जनता ने इन महंतों तथा इनकी सहायता करने वाले सरकार के खिलाफ एक शक्तिशाली सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया। जल्द ही अकालियों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वह एक सिख गुरूद्वारा कानून बनाए। यह कानून 1922 में बना और 1925 में इसमें संशोधन किए गए। कभी-कभी इस कानून की सहायता से मगर अधिकतर सीधी कार्यवाही के द्वारा सिखों ने गुरूद्वारों से भ्रष्ट महंतों को धीरे-धीरे बाहर खदेड़ दिया, हालाँकि इस आंदोलन में सैकड़ों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा।ऊपर जिन सुधार आंदोलनों तथा विशिष्ट सुधारों का वर्णन किया गया है उनसे अलग बहुत से दूसरे इसी तरह के आंदोलन और सुधारक भी 19वीं तथा 20वीं सदी में हुए हैं। आधुनिक युग के धार्मिक सुधार के आंदोलन में एक बुनियादी समानता पाई जाती है। ये सभी आंदोलन बुद्धिवाद तथा मानवतावाद के दो सिद्धांतों पर आधारित थे, हालाँकि अपनी ओर लोगों को खीचनें के लिए कभी-कभी वे आस्था तथा प्राचीन ग्रंथों का सहारा भी लेते थे। इसके अलावा, उन्होंने उभरते हुए मध्य वर्ग आधुनिक शिक्षा-प्राप्त प्रबुद्ध लोगों को सबसे अधिक प्रभावित किया। उन्होंने बुद्धिविरोधी धार्मिक कठमुल्लापन तथा अंध श्रद्धा से मानव बुद्धि की तर्क-विचार की क्षमता को मुक्त कराने का प्रयास किया। उन्होंने भारतीय धर्मों के कर्मकांडी, अंधविश्वासी, बुद्धिविरोधी तथा पुराणपंथी पक्षों का विरोध किया। उनमें से अनेक ने, किसी ने कम और किसी ने अधिक, धर्म को अंतिम सत्य का भंडार मानने से इंकार कर दिया तथा किसी भी धर्म या उसके ग्रंथों में उपस्थित सत्य को तर्क, बुद्धि तथा विज्ञान की कसौटी पर परखा स्वामी विवेकानंद ने कहा - “क्या धर्म बुद्धि के उन अधिकारों द्वारा अपना औचित्य सिद्ध करेगा जिनके द्वारा प्रत्येक विज्ञान अपना औचित्य स्थापित करता है ? क्या जाँच-पड़ताल की वे विधियाँ जो विज्ञानों तथा ज्ञान के लिए प्रयुक्त होती हैं, धर्म के विज्ञान पर भी लागू की जाएँगी ? मेरे विचार में ऐसा ही होना चाहिए और मैं यह भी मानता हूँ कि यह जितनी जल्दी हो उतना ही बेहतर है।” इनमें से कुछ धर्मसुधारकों ने परंपरा का सहारा लिया और यह दावा किया कि वे केवल अतीत के वास्तविक सिद्धान्तों, मान्यताओं और व्यवहारों को ही पुनर्जीवित कर रहे हैं। पर वास्तव में अतीत को पुर्नजीवित नहीं किया जा सका। प्रायः अतीत के बारे में सबकी समझ भी एक जैसी न थी। अतीत का सहारा लेने पर जो समस्याएँ उठती हैं उनका वर्णन जस्टिस रानाडे ने किया है, हालाँकि खुद उन्होंने अक्सर जनता से आग्रह किया था कि वह अतीत की बेहतरीन परंपराओं को पुर्नजीवित करें। वे लिखते हैं - पुर्नजीवित हम करें तो क्या ? क्या हम अपनी जनता की पुरानी आदतों को पुर्नजीवित करें सब हमारी जातियों में सबसे पवित्र जाति भी पशु के माँस तथा नशीली शराब का सेवन करती थी जिन्हें हम आज घृणित समझते हैं ? क्या हम पुत्रों की बारह श्रेणियों तथा आठ प्रकार के विवाह को पुर्नजीवित करें जिसमें राक्षस-विवाह भी शामिल था तथा जो मुक्त तथा अवैध यौन संबंध को मान्यता देता था ? . . . . . क्या हम प्रति वर्ष होने वाले शतमेघ को पुनर्जीवित करें जिसमें मनुष्यों तक का देवता के आगे बलिदान दिया जाता था ? क्या हम सती और शिशु-हत्या की प्रथाओं को पुर्नजीवित करें ? फिर रानाडे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि समाज एक निरंतर परिवर्तनशील जीवित सत्ता है और कभी अतीत की ओर नहीं पलट सकती। “मृत तथा दफनाएँ या जलाएँ जा चुके लोग हमेशा के लिए मरकर दफनाएँ या जलाएँ जा चुके हैं और इसलिए मुर्दा अतीत को पुनर्जीवित नहीं कर सकता,” ऐसा उन्होंने लिखा है। अतीत का नाम लेने वाले प्रत्येक सुधारक ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की कि वह उसके द्वारा सुझाए गए सुधारों के अनुरूप लगे। सुधार तथा उनके दृष्टिकोण प्रायः नवीन होते थे, अतीत के नाम पर केवल उनको उचित ठहराया जाता था। अनेक विचारों को जो आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान से मेल नहीं खाते थे, यह कहा गया कि ये बाद में जोड़े गए हैं यह गलत व्याख्या के परिणाम हैं। चूँकि रूढ़िवादी लोग इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं होते थे इसलिए उनसे सामाजिक सुधारकों का टकराव हुआ और ये सुधारक कम से कम आरंभिक चरण में धार्मिक और सामाजिक विद्रोहियों के रूप में सामने आए। उदाहरण के लिए, रूढ़िवादियों द्वारा स्वामी दयानंद के विरोध के बारे में लाला लाजपतराय ने यह बात लिखी है - स्वामी दयानंद को अपने जीवन में जितने निंदा वचनों तथा उत्पीड़न का निशाना बनना पड़ा उनका अंदाजा इसी एक तथ्य से लगाया जा सकता है कि रूढ़िवादी हिंदुओं ने उनकी जान लेने के अनेक प्रयास किए। उनकी हत्या के लिए हत्यारों को भाड़े पर लिया गया, उनके भाषणों तथा वाद-विवाद के बीच उन पर वस्तुएँ फेंकी गईं, उनकों ईसाइयों का भाड़े का प्रचारक, धर्म विरोधी, नास्तिक, आदि-आदि कहा गया। इसी तरह सैयद अहमद खान को भी परंपरावादियों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। उन्हें गालियाँ दी गईं, उनके फतवे जारी किए गए तथा जान से मारने की धमकियाँ तक दी गईं। धार्मिक सुधार के आंदोलनों के मानवतावादी चरित्र की अभिव्यक्ति पुरोहितवाद तथा कर्मकांड पर उनके हमलों में तथा मानव कल्याण तथा मानव बुद्धि की दृष्टि से धर्मग्रंथों की व्याख्या के व्यक्ति के अधिकार पर दिए गए जोर में हुई। इस मानवतावाद की एक खास बात एक नई मानवतावादी नैतिकता थी। इसमें यह धारणा भी शामिल थी कि मानवता प्रगति कर सकती और करती रही है और अंततः वे ही मूल्य नैतिक मूल्य हैं जो मानव-प्रगति में सहायक हों। सामाजिक सुधार के आंदोलन इस नई, मानवतावादी नैतिकता के मूर्त रूप थे। हालाँकि सुधारकों ने अपने-अपने धर्मों में ही सुधार लाने के प्रयत्न किए, मगर सामान्य दृष्टिकोण सर्वव्यापकतावादी था। राममोहन राय विभिन्न धर्मों को एक ही सर्वव्यापी ईश्वर तथा एक धार्मिक सत्य के विशिष्ट रूप समझते थे। सैयद अहमद खान ने कहा कि सभी पैगम्बरों का एक ही धर्म या दीन था, और अल्लाह ने हर कौम को अपना एक पैगंबर भेजा है। इसी बात को केशवचंद्र सेन इस प्रकार रखते हैं - “हमारा मत यह नहीं है कि सत्य सभी धर्मों में पाए जाते हैं, बल्कि यह है कि सभी स्थापित धर्म सत्य हैं।” शुद्ध रूप से धार्मिक विचारों के अलावा धर्म-सुधार के इन आंदोलनों ने भारतीयों के आत्मविश्वास, आत्मसम्मान तथा अपने देश पर उनके गर्व को बढ़ाया। उनके धार्मिक अतीत की आधुनिक बुद्धिवादी शब्दों में व्याख्या करके तथा 19वीं सदी के धार्मिक विश्वासों से अनेक भ्रामक तथा बुद्धिविरोधी तत्वों को बाहर फेंककर इन सुधारकों ने अपने अनुयायियों को अधिकारियों के इस व्यंग्य का उत्तर देने योग्य बनाया कि यहाँ के धर्म व समाज पतनशील और हीन हैं। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार - उभरते हुए मध्य वर्गों का राजनीतिक रुझान था और उन्हें धर्म की खोज उतनी नहीं थी, लेकिन उनमें इच्छा थी कि वे किसी सांस्कृतिक मूल का सहारा ले सकें-किसी ऐसी वस्तु का जो उनको उनकी अपनी शक्ति का अनुभव कराए, कोई ऐसी वस्तु जो कुंठा तथा अपमान की उस भावना को कम करें जो विदेशियों की विजय तथा उनके शासन ने उनके अंदर उपजा दिए थे। धर्म-सुधार के आंदोलनों ने अनेक भारतीयों को इस योग्य बनाया कि वे आधुनिक विश्व से तालमेल बिठा सकें। वास्तव में उनका जन्म ही पुराने धर्मों को एक नए, आधुनिक साँचे में ढालकर उनको समाज के नए वर्गों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए हुआ था। इस तरह अतीत पर गर्व करके भी भारतीयों ने आम तौर पर आधुनिक विज्ञान की मूलभूत श्रेष्ठता को मानने से इनकार नहीं किया। यह सही है कि कुछ लोगों ने दावा किया कि वे तो केवल मूल, प्राचीनतम धर्मग्रंथों का सहारा ले रहे हैं और इन ग्रंथों की उन्होंने समुचित व्याख्या की। सुधारमूलक दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप अनेक भारतीय जाति-धर्म के विचारों पर आधारित एक संकुचित दृष्टिकोण की जगह एक आधुनिक, इहलौकिक, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाने लगे, हालाँकि पहले के संकुचित दृष्टिकोण एकदम समाप्त नहीं हो सके। इसके अलावा अधिकाधिक संख्या में लोग अपने भाग्य को निष्क्रिय रहकर स्वीकार करने तथा मरकर दूसरे जीवन के सुधरने की आशा लगाने के बजाए इसी दुनिया में अपने भौतिक व सांस्कृतिक कल्याण की बाते सोचने लगे। इन आंदोलनों ने बाकी दुनिया से भारत के सांस्कृतिक और बौद्धिक अलगाव को भी कुछ हद तक खत्म किया और विश्वव्यापी विचारों में भारतीयों को भागीदार बनाया। साथ ही साथ, वे पश्चिम की हर बात के रोब में नहीं आए और जो लोग आँखें मूँदकर पश्चिम की नकल करते थे उनकी खुलकर हँसी उड़ाई गई। वास्तव में परंपरागत धर्मों व संस्कृति के पिछड़े तत्वों के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाकर तथा आधुनिक संस्कृति सकरात्मक तत्वों का स्वागत करके भी, अधिकांश धर्म-सुधारकों ने पश्चिम की अंधी नकल का विरोध भी किया और भारतीय संस्कृति व विचार परंपरा के उपनिवेशीकरण के खिलाफ एक विचारधारात्मक संघर्ष चलाया। यहाँ समस्या दोनों पक्षों के बीच संतुलन स्थापित करने की थी। कुछ लोग आधुनिकीकरण की दिशा में बहुत आगे बढ़ गए तथा संस्कृति संबंधी उपनिवेशवाद को प्रोत्साहित करने लगे। कुछ और लोग थे जो परंपरागत विचारों, संस्कृति और संस्थाओं का पक्ष लेते और उनका महिमामंडन करते थे और आधुनिक विचारों व संस्कृति के समावेश का विरोध कर रहे थे। सुधारकों में जो श्रेष्ठ थे उनका तर्क यह था कि आधुनिक विचारों तथा संस्कृति को अच्छी तरह तभी अपनाया जा सकता है जब उन्हें भारतीय सांस्कृतिक धारा का अंग बना लिया जाए। धर्म-सुधार के आंदोलनों के दो नकारात्मक पक्षों को भी ध्यान में रखना चाहिए। प्रथम, ये सभी समाज के एक बहुत छोटे भाग की यानी नगरीय उच्च और मध्य वर्गों की आवश्यकताएँ पूरी करते थे। इनमें से कोई भी बहुसंख्य किसानों तथा नगरों की गरीब जनता तक नहीं पहुँचा और ये लोग अधिकांशतः परंपरागत रीति-रिवाजों में ही जकड़े रहे। कारण यह है कि ये आंदोलन मूलतः भारतीय समाज के शिक्षित व नगरीय भागों की आकांक्षाओं को ही प्रतिबिंबित करते थे। इनकी दूसरी कमी तो आगे चलकर एक प्रमुख नकारात्मक प्रवृत्ति बन गई। यह कमी पीछे घूमकर अतीत की महानता का गुणगान करने तथा धर्मग्रंथों को आधार बनाने की प्रवृत्ति थी। यह बात इन आंदोलनों की अपनी सकारात्मक शिक्षाओं की विरोधी बन गई। इसने मानव-बुद्धि तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण की श्रेष्ठता के विचार को ही धक्का पहुँचाया। इससे नए-नए रूपों में रहस्यवाद तथा नकली वैज्ञानिक चिंतन को बल मिला। अतीत की महानता के गुणगान ने एक झूठे गर्व तथा दंभ को बढ़ावा दिया। अतीत में एक ‘स्वर्ण युग’ पाने की इच्छा के कारण आधुनिक विज्ञान को पूरी तरह नहीं अपनाया जा सका और वर्तमान को सुधारने के प्रयत्नों में बाधा पड़ी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे हिंदू, मुसलमान, सिख और पारसी फूट के शिकार होने लगे। ऊँची तथा नीची जातियों के हिंदुओं में भी दरार पड़ने लगी। अनेक धर्मों वाले एक देश में धर्म पर जरूरत से ज्यादा जोर देने से फूट की प्रवृत्ति बढ़नी स्वाभाविक थी। इसके अलावा, सुधारकों ने सांस्कृतिक धरोहर के धार्मिक-दार्शनिक पक्षों पर एकतरफा जोर दिया। फिर ये पक्ष सभी लोगों की साझी धरोहर भी नहीं थे। दूसरी तरफ, कला, स्थापत्य, साहित्य, संगीत, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आदि पर पूरा जोर नहीं दिया गया, हालाँकि इनमें जनता के सभी भागों की बराबर भूमिका रही थी। इसके अलावा हर एक हिंदू सुधारक ने भारतीय अतीत के गुणगान को प्राचीन काल तक सीमित रखा। स्वामी विवेकानंद जैसे खुले दिमाग के व्यक्ति तक ने भारत की आत्मा या भारत की उपलब्धियों की चर्चा केवल इसी अर्थ में की। ये सुधारक भारतीय इतिहास के मध्य काल को मूलतः पतन का काल मानते थे। यह विचार अनैतिहासिक ही नहीं था बल्कि सामाजिक-राजनीतिक दृष्टि से हानिकारक भी था। इससे दो कौमों की धारणा पनपी। इसी तरह प्राचीन काल और प्राचीन धर्मों की अनौपचारिक प्रशंसा को निचली जातियों के लोग भी पचा नहीं सके, जो सदियों से उसी विध्वंसक जाति-प्रथा के दमन के शिकार रहे जो ठीक उसी प्राचीन काल की उपज थी। इन सबका परिणाम यह हुआ कि सभी भारतीय अतीत की भौतिक-सांस्कृतिक उपलब्धियों पर समान रूप से गर्व करें और उससे प्रेरणा प्राप्त करें, इसके बजाय अतीत कुछेक लोगों की संपत्ति बनकर रह गया। इसके अलावा अतीत भी अनेक खंडों में विभाजित होने लगा। मुस्लिम मध्य वर्ग के अनेक लोगों ने तो अपनी परंपरा और अपनी धरोहर पश्चिमी एशिया के इतिहास में खोजना आरंभ कर दिया। हिंदू, मुसलमान, सिख और पारसी तथा बाद में निचली जाति के हिंदू-ये सब सुधार आंदोलनों से प्रभावित हुए थे, मगर अब ये एक दूसरे से कटने लगे। दूसरी तरफ, सुधार आंदोलनों के प्रभाव से दूर रहकर परंपरागत रीति-रिवाजों को मानने वाले हिंदुओं और मुसलमानों में आपसी भाईचारा बना रहा, हालाँकि वे अपने-अपने कर्मकांड का पालन करते रहे। एक समन्वित संस्कृति के विकास की वह प्रक्रिया जो सदियों से चली आ रही थी, उस पर इस कारण से कुछ अंकुश लगा, हालाँकि दूसरे क्षेत्रों में भारतीय जनता के राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया तेज हुई। इस प्रवृत्ति का दुष्परिणाम तब स्पष्ट हो गया जब यह पाया गया कि मध्य वर्गों में राष्ट्रीय चेतना के तीव्र विकास के साथ-साथ एक और चेतना, अर्थात् सांप्रदायिक चेतना, का विकास भी हो रहा था। आधुनिक काल में सांप्रदायिकता के विकास के अनेक दूसरे कारण भी थे, परंतु अपनी प्रकृति के कारण धर्म-सुधार के आंदोलनों ने निश्चय ही इसमें कुछ योगदान किया। सामाजिक सुधारउन्नीसवीं सदी के राष्ट्रीय जागरण का प्रमुख प्रभाव सामाजिक सुधार के क्षेत्र में देखने को मिला। नवशिक्षित लोगों ने बढ़-चढ़कर जड़ सामाजिक रीतियों तथा पुरानी प्रथाओं से विद्रोह किया। वे अब बुद्धिविरोधी और अमानवीयकारी सामाजिक व्यवहारों को और सहने को तैयार न थे। उनका विद्रोह सामाजिक समानता तथा सभी व्यक्तियों की समान क्षमता के मानवतावादी आदर्शों से प्रेरित था।समाज-सुधार के आंदोलन में लगभग सभी धर्म-सुधारकों का योगदान रहा। कारण यह कि भारतीय समाज के पिछड़ेपन की तमाम निशानियों जैसे जाति प्रथा या स्त्रियों की असमानता को अतीत में धार्मिक मान्यता प्राप्त रही है। साथ ही सोशल कॉन्फ्रेंस, भारत सेवक समाज जैसे कुछ अन्य संगठनों तथा ईसाई मिशनरियों ने भी समाज-सुधार के लिए जमकर काम किया। ज्योतिबा गोविन्द फुले, गोपाल हरि देशमुख, जस्टिस रानाडे, के. टी. तेलंग, बी. एम. मलाबारी, डी. के. कर्वे, शशिपद बनर्जी, बिपिनचंद्र पाल, वीरेशलिंगम, ई. वी. रामास्वामी नायकर ‘पेरियार’ और भीमराव अंबेडकर तथा दूसरे प्रमख व्यक्तियों की भी एक प्रमुख भूमिका रही। बीसवीं सदी में और खासकर 1919 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन मानव-सुधार का प्रमुख प्रचारक बन गया। जनता तक पहुँचने के लिए सुधारकों ने प्रचार-कार्य में भारतीय भाषाओं का अधिकाधिक सहारा लिया। उन्होंने अपने विचारों को फैलाने के लिए उपन्यासों, नाटकों, काव्य, लघु कथाओं, प्रेस तथा 1930 के दशक में फिल्मों का भी उपयोग किया। उन्नीसवीं सदी में कुछ मामलों में समाज-सुधार का कार्य धर्म-सुधार से जुड़ा था, मगर बाद के वर्षों में यह अधिकाधिक धर्मनिरपेक्ष होता गया। इसके अलावा रूढ़िवादी धार्मिक दृष्टिकोण वाले अनेक व्यक्तियों ने भी इसमें भाग लिया। इसी तरह आरंभ में समाज-सुधार बहुत कुछ ऊँची जातियों के नवशिक्षित भारतीयों द्वारा अपने सामाजिक व्यवहार का आधुनिक पश्चिमी संस्कृति व मूल्यों के साथ तालमेल बिठाने के प्रयासों का परिणाम था। लेकिन धीरे-धीरे इसका क्षेत्र व्यापक होकर समाज के निचले वर्गों तक फैल गया और यह सामाजिक क्षेत्र की क्रांतिकारी पुर्नरचना करने लगा। कालांतर में सुधारकों के विचारों व आदर्शों को लगभग सर्वभौमिक मान्यता मिली तथा आज वे भारतीय संविधान के अंग हैं। समाज-सुधार के आंदोलनों ने मुख्यतः दो लक्ष्यों की पूरा करने के प्रयास किए - (अ) स्त्रियों की मुक्ति तथा उनको समान अधिकार देना, तथा (ब) जाति-प्रथा की जड़ताओं को समाप्त करना तथा खासकर छूआछूत का खात्मा। स्त्रियों की मुक्तिभारत में स्त्रियाँ अनगिनत सदियों से पुरुषों की अधीन तथा सामाजिक उत्पीड़न का शिकार रही हैं। भारत में प्रचलित विभिन्न धर्मों व उन पर आधारित गृहस्थ-नियमों ने स्त्रियों को पुरुषों से हीन स्थान दिया। इस संबंध में उच्च वर्गों की स्त्रियों की स्थिति किसान औरतों से भी बदतर थी। चूँकि किसान स्त्रियाँ अपने पुरुषों के साथ खेतों में काम करती थीं, इसलिए उनको बाहर आने-जाने की कुछ अधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी और परिवार में उनकी स्थिति उच्च वर्गों की स्त्रियों से कुछ मामलों में बेहतर थीं। उदाहरण के लिए, वे शायद ही कभी पर्दे में रहती हों तथा उनमें से अनेकों को पुनर्विवाह के अधिकार प्राप्त थे।पारंपरिक विचारधारा में पत्नी और माँ की भूमिका में स्त्री की प्रशंसा तो की गई है मगर व्यक्ति के रूप में उसे बहुत हीन सामाजिक स्थान दिया गया है। अपने पति से अपने संबंधों से अलग उसका भी एक व्यक्तित्व है, ऐसा कभी नहीं माना गया। अपनी प्रतिभा या इच्छाओं की अभिव्यक्ति के लिए घरेलू महिला से भिन्न कोई अन्य भूमिका उसे प्राप्त न थी। वास्तव में, उसे पुरुष का पुछल्ला मात्र माना गया। उदाहरण के लिए, हिंदुओ में किसी स्त्री का एक ही विवाह संभव था, मगर किसी पुरुष को अनेक पत्नियाँ रखने का अधिकार था। मुसलमानों में भी यह बहुपत्नी-प्रथा प्रचलित थी। देश के काफी बड़े भाग में स्त्रियों को पर्दे में रखा जाता था। बाल-विवाह की प्रथा आम थी, आठ-नौ वर्ष के बच्चे भी ब्याह दिए जाते थे। विधवाएँ पुर्नविवाह नहीं कर सकती थीं और उन्हें त्यागी व बंदी जीवन बिताना पड़ता था। देश के अनेक भागों में सती-प्रथा प्रचलित थी जिसमें एक विधवा स्वयं को पति की लाश के साथ जला लेती थी। हिंदू स्त्री को उत्तराधिकार में संपत्ति पाने का हक नहीं था, न उसे अपने दुखमय विवाह को रद्द करने का कोई अधिकार था। मुस्लिम स्त्री को संपत्ति में अधिकार मिलता तो था, मगर पुरुषों का केवल आधा और तलाक के बारे में स्त्री और पुरुष के बीच सैद्धान्तिक समानता भी न थी। वास्तव में, मुस्लिम स्त्रियाँ तलाक से भयभीत रहती थीं। हिंदू व मुस्लिम स्त्रियों की सामाजिक स्थिति तथा उनके मान-सम्मान भी मिलते-जुलते थे। इसके अलावा, दोनों ही सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से पुरुषों पर पूरी तरह निर्भर थीं। अंतिम बात यह कि शिक्षा के लाभ उनमें से अधिकांश को प्राप्त नहीं थे। साथ ही, स्त्रियों का अपनी दासता को स्वीकार कर लेने, बल्कि इसे सम्मान का प्रतीक समझने के पाठ भी पढ़ाए जाते थे। यह सही है कि भारत में कभी-कभी रजिया सुल्ताना, चाँद बीवी तथा अहिल्याबाई होलकर जैसी स्त्रियाँ भी गुजरी हैं। मगर यह उदाहरण मात्र अपवाद हैं और इनसे सामान्य स्थिति में कोई अंतर नहीं आता। उन्नीसवीं सदी के मानवतावादी व समानतावादी विचारों से प्रेरित होकर समाज-सुधारकों ने स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन छेड़ा। कुछ सुधारकों ने व्यक्तिवाद तथा समानता के सिद्धान्तों का सहारा लिया, तो दूसरों ने घोषणा की कि हिंदू धर्म, इस्लाम या जरथुस्त्र मत स्त्रियों की हीन स्थिति के प्रचारक नहीं हैं और यह कि सच्चा धर्म उन्हें एक ऊँचा सामाजिक दर्जा देता है। अनेकानेक व्यक्तियों, सुधार समितियों तथा धार्मिक संगठनों ने स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार करने, विधवाओं के पुर्नविवाह को प्रोत्साहन देने, विधवाओं की दशा सुधारने, बाल-विवाह रोकने, स्त्रियों को पर्दे से बाहर लाने, एकपत्नी-प्रथा प्रचलित करने और मध्यवर्गीय स्त्रियों को व्यवसाय या सरकारी रोजगार में जाने के योग्य बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। 1880 के दशक में तत्कालीन वायसराय लार्ड डफरिन की पत्नी लेडी डफरिन के नाम पर जब डफरिन अस्पताल खोले गए तो आधुनिक औषधियों तथा प्रसव की आधुनिक तकनीकों के लाभ भारतीय स्त्रियों को उपलब्ध कराने के प्रयास भी किए गए। बीसवीं सदी में जुझारू राष्ट्रीय आंदोलन के उदय से स्त्री-मुक्ति के आंदोलन को बहुत बल मिला। स्वतंत्रता के संघर्ष में स्त्रियों ने एक सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बंग-भंग विरोधी आंदोलन तथा होम रूल आंदोलन में उन्होंने बड़ी संख्या में भाग लिया। 1918 के बाद वे राजनीतिक जुलूसों में भी चलने लगीं, विदेशी वस्त्र और शराब बेचने वाली दुकानों पर धरने देने लगीं। असहयोग आंदोलनों में वे जेल गईं तथा जन-प्रदर्शनों में उन्होंने लाठी, आँसू-गैस और गोलियाँ भी झेली। उन्होंने क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। वे विधानमंडलों के चुनावों में वोट देने तथा उम्मीदवारों के रूप में खड़ी भी होने लगी। प्रसिद्ध कवियत्री सरोजिनी नायडू राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बनी। अनेक स्त्रियाँ 1937 में जनप्रिय सरकारों में मंत्री या संसदीय सचिव बनीं। उनमें से सैकड़ों नगरपालिकाओं तथा स्थानीय शासन की दूसरी संस्थाओं की सदस्या तक बनीं। 1920 के दशक में जब ट्रेंड यूनियन और किसान आंदोलन खड़े हुए तो अक्सर स्त्रियाँ उनकी पहली पंक्तियों में दिखाई देतीं। भारतीय स्त्रियों की जागृति तथा मुक्ति में सबसे महत्वपूर्ण योगदान राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भागीदारी का रहा। कारण कि जिन्होंने ब्रिटिश जेलों तथा गोलियों को झेला था उन्हें ही भला कौन कह सकता था और उन्हें अब और कब तक घरों में कैद रखकर ‘गुड़िया’ या ‘दासी’ के जीवन से बहलाया जा सकता था ? मनुष्य के रूप में अपने अधिकारों का दावा उन्हें करना ही करना था। एक और प्रमुख घटनाक्रम देश में महिला आंदोलन का जन्म था। 1920 के दशक तक प्रबुद्ध पुरुषगण स्त्रियों के कल्याण के लिए कार्यरत रहे। अब आत्मचेतन तथा आत्मविश्वास-प्राप्त स्त्रियों ने यह काम संभाला। इस उद्देश्य से उन्होंने अनेक संस्थाओं और संगठनों को खड़ा किया। इनमें सबसे प्रमुख था आल इंडिया वूमेन्स कांफ्रेन्स जो 1927 में स्थापित हुआ। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद समानता के लिए स्त्रियों के संघर्ष में बहुत तेजी आई। भारतीय संविधान (1950) की धारा 14 व 15 में स्त्री व पुरूष की पूर्ण समानता की गारंटी दी गई है। 1956 के हिंदू उत्तराधिकार कानून ने पिता की संपत्ति में बेटी को बेटे के बराबर अधिकार दिया। 1955 के हिंदू विवाह कानून में कुछ विशिष्ट आधारों पर विवाह-संबंध भंग करने की छूट दी गई। स्त्री-पुरूष दोनों के लिए एक विवाह अनिवार्य बना दिया गया। लेकिन दहेज प्रथा की बुराई अभी तक जारी है हालाँकि दहेज लेने और देने, दोनों पर प्रतिबंध है। संविधान स्त्रियों को भी काम करने तथा सरकारी संस्थाओं में नौकरी करने के समान अधिकार देता है। संविधान के नीति-निर्देशक सिद्धान्त में स्त्री-पुरुष दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धान्त भी शामिल है। स्त्रियों की समानता के सिद्धान्त को व्यवहार में लागू करने में अभी भी निश्चित ही अनेक स्पष्ट और अस्पष्ट बाधाएँ हैं। इसके लिए एक समुचित सामाजिक वातावरण का निर्माण आवश्यक है। फिर भी समाज-सुधार आंदोलन, स्वाधीनता संग्राम, स्त्रियों के अपने आंदोलन तथा स्वतंत्र भारत के संविधान ने इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान किए हैं। जाति-प्रथा के विरुद्ध संघर्षजाति-व्यवस्था समाज-सुधार आंदोलन के हमले का एक और प्रमुख निशाना थी। इस समय हिंदू अनगिनत जातियों में बँटे थे। कोई व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता था उसी के नियमों से उसके जीवन का एक बड़ा भाग संचालित होता था। व्यक्ति किससे विवाह करे तथा किसके साथ भोजन करे, इसका निर्धारण उसकी जाति से ही होता था। उसके पेशे तथा उसकी सामाजिक प्रतिबद्धता का निर्धारण भी बहुत कुछ इसी से होता था। इसके अलावा जातियों को भी सावधानीपूर्वक अनेक ऊँचे-नीचे दर्जे में रखा गया था। इस व्यवस्था में सबसे नीचे अछूत आते थे जो हिंदू आबादी का लगभग 20 प्रतिशत भाग थे, इन्हीं को बाद में अनुसूचित जातियाँ कहा गया। ये अछूत अनेकों कठोर निर्योग्यताओं और प्रतिबंधों से पीड़ित थे जो विभिन्न जगहों में भिन्न-भिन्न थीं। उनके स्पर्श मात्र से किसी व्यक्ति को अपवित्र माना जाता था।देश के कुछ भागों में और खासकर दक्षिण में लोग उनकी छाया तक से बचते थे और इसलिए किसी ब्राह्मण को आता जानकर इस अछूतों को बहुत दूर हट जाना पड़ता था। अछूतों के खाने-पहनने और रहने के स्थान पर भी कड़े प्रतिबंध थे। वह ऊँची जातियों के कुओं, तालाबों से पानी नहीं ले सकता था, इसके लिए अछूतों के लिए कुछ तालाब और कुएँ निश्चित होते थे। जहाँ ऐसे कुएँ और तालाब न होते वहाँ उनको पौखरों और सिंचाई की नालियों का गंदा पानी पीना होता था। वे हिंदू मंदिरों में जा नहीं सकते और न शास्त्र पढ़ सकते थे। अक्सर उनके बच्चे ऊँची जातियों के बच्चों के स्कूल में नहीं जा पाते थे। पुलिस तथा सेना जैसी सरकारी नौकरियाँ उनके लिए नहीं थी। अछूतों को ‘अपवित्र’ समझे जाने वाले गंदे काम, जैसे झाडू-बुहारू, जूते बनाना मुर्दे उठाना, मुर्दा जानवरों की खाल निकालना, खालों तथा चमड़ों को पकाना-कमाना, आदि काम करने पड़ते थे। वे जमीन के मालिक नहीं बन सकते थे और उनमें से अनेकों को बँटाईदारी या खेत-मजदूरी करनी पड़ती थी। जाति-प्रथा की एक और बुराई भी थी। यह अपमानजनक, अमानवीय और जन्मगत असमानता के जनतंत्र-विरोधी सिद्धांत पर आधारित तो थी ही, साथ ही यह सामाजिक विघटन का कारण भी थी। इसने लोगों को अनेकों समूहों में बाँटकर रख दिया था। आधुनिक काल में यह प्रथा एकता की राष्ट्रीय भावना के विकास और जनतंत्र के प्रसार में एक प्रमुख बाधा रही है। यहाँ यह भी कह दिया जाए कि जातिगत चेतना, खासकर विवाह-संबंधों के बारे में, मुसलमानों, ईसाइयों तथा सिखों में भी रही है, तथा वे भी कम उग्र रूप में ही सही, छुआछूत का पालन करते रहे हैं। ब्रिटिश शासन ने ऐसी अनेक शक्तियों को जन्म दिया जिन्होंने धीरे-धीरे जाति-प्रथा की जड़ों को कमजोर किया। आधुनिक उधोगों, रेलों व बसों के आरंभ से तथा बढ़ते नगरीकरण के कारण खासकर शहरों में विभिन्न जातियों के लोगों के बीच संपर्क को अपरिहार्य बना दिया है। आधुनिक व्यापार-उधोग ने आर्थिक कार्यकलाप के नए क्षेत्र सभी के लिए पैदा किए हैं। उदाहरण के लिए, एक ब्राह्मण या किसी और ऊँची जाति का व्यापारी चमड़े या जूते के व्यापार का अवसर भी शायद ही छोड़े, और न ही वह डॉक्टर या सैनिक बनने का अवसर छोड़ेगा। जमीन की खुली बिक्री ने अनेक गाँवों में जातीय संतुलन को बिगाड़कर रख दिया है। एक आधुनिक औधोगिक समाज में जाति और व्यवसाय का पुराना संबंध चल सकना कठिन है क्योंकि इस समाज में मुनाफा प्रमुख प्रेरणा बनता जा रहा है। प्रशासन के क्षेत्र में, अंग्रेजों ने कानून के सामने सबकी समानता का सिद्धान्त लागू किया, जातिगत पंचायतों से उनके न्यायिक काम छीन लिए और प्रशासकीय सेवाओं के दरवाजे धीरे-धीरे सभी जातियों के लिए खोल दिए। इसके अलावा, नई शिक्षा प्रणाली पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष है और इसलिए वह मूलतः जातिगत दृष्टिकोण की विरोधी है। जब भारतीयों के बीच आधुनिक जनतांत्रिक व बुद्धिवादी विचार फैले तो उन्होंने जाति प्रथा के खिलाफ आवाज उठाना शुरु किया। ब्रह्मसमाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसोफी, सोशल कांफ्रेंस तथा उन्नीसवीं सदी के लगभग सभी महान सुधारकों ने इस पर हमले किए। हालाँकि उनमें से बहुतों ने चार वर्णों की प्रथा का पक्ष भी लिया, मगर वे भी जाति-प्रथा के आलोचक थे। उन्होंने खास तौर पर छुआछूत की अमानवीय प्रथा की निंदा की। उन्होंने यह भी महसूस किया कि राष्ट्रीय एकता तथा राजनीतिक-सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में राष्ट्रीय प्रगति तब तक असंभव है जब तक कि लाखों-लाख लोग सम्मान से जीने के अधिकार से वंचित हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के विकास ने भी जाति-प्रथा को कमजोर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय आंदोलन उन तमाम संस्थाओं का विरोधी था जो भारतीय जनता को बाँटकर रखती थी। जन-प्रदर्शनों, विशाल जनसभाओं तथा सत्याग्रह के संघर्षों में सबकी भागीदारी ने भी जातिगत चेतना को कमजोर बनाया। कुछ भी हो, वे लोग जो स्वाधीनता और स्वतंत्रता के नाम पर विदेशी शासन से मुक्ति के लिए लड़ रहे थे, जाति-प्रथा का समर्थन नहीं कर सकते थे क्योंकि यह उन सिद्धांतों की विरोधी थी। इस तरह आरंभ से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बल्कि पूरे राष्ट्रीय आंदोलन ने जातिगत विशेषाधिकारों का विरोध किया और जाति-लिंग-धर्म के भेदभाव के बिना व्यक्ति के विकास के लिए समान नागरिक अधिकारों तथा समान स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते रहे। गाँधीजी अपनी सार्वजनिक गतिविधियों में छूआछूत के खात्मे को जीवन भर एक प्रमुख काम मानते रहे। 1932 में उन्होंने इस उद्देश्य से अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की। “अस्पृश्यता का जड़-मूल से उन्मूलन का उनका आंदोलन मानवतावाद और बुद्धिवाद पर आधारित था। उनका तर्क कि हिंदू शास्त्रों में छूआछूत को कोई मान्यता नहीं दी गई है। लेकिन अगर कोई शास्त्र छूआछूत का समर्थन करे तो उसे नहीं मानना चाहिए क्योंकि यह तब मानव-सम्मान के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि सत्य किसी पुस्तक के पन्नों तक सीमित नहीं होता। उन्नीसवीं सदी के मध्य से अनेक व्यक्तियों व संगठनों ने अछूतों के बीच शिक्षा-प्रसार का काम आंरभ किया (इन अछूतों को बाद में कमजोर वर्ग या अनुसूचित जातियाँ कहा गया)। उनके लिए स्कूलों तथा मंदिरों के दरवाजे खुलवाने, सार्वजनिक कुओं और तालाबों से उन्हें पानी भरने का अधिकार दिलाने, तथा उनको उत्पीड़ित करने वाली अन्य सामाजिक निर्योग्यताओं और भेदभावों को नष्ट करने के प्रयास किए गए। शिक्षा तथा जागृति फैली तो निचली जातियों में भी हलचल होने लगी। वे अपने मूल मानव-अधिकारों के प्रति सचेत हुए तथा उनकी रक्षा के लिए उठकर खड़े होने लगे। धीरे-धीरे उन्होंने ऊँची जातियों के परंपरागत उत्पीड़न के खिलाफ एक शक्तिशाली आंदोलन खड़ा किया। महाराष्ट्र में 19वीं सदी के उत्तरार्ध में एक निचली जाति में जन्में ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणों की धार्मिक सत्ता के खिलाफ जीवन-भर आंदोलन चलाया। यह ऊँची जातियों के प्रभुत्व के खिलाफ उनके संघर्ष का एक अंग था। वे आधुनिक शिक्षा को निचली जातियों की मुक्ति का सबसे शक्तिशाली अस्त्र समझते थे। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने निचली जातियों की लड़कियों के लिए अनेक स्कूल खोले। डाक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो खुद एक अनुसूचित जाति के थे, अपना पूरा जीवन जातिगत अत्याचार विरोधी संघर्ष को समर्पित कर दिया। इसके लिए उन्होंने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की। अनुसूचित जातियों के दूसरे अनेक नेताओं ने अखिल भारतीय वंचित वर्ग संघ की स्थापना की। केरल में श्री नारायण गुरु ने जाति-प्रथा के खिलाफ जीवन भर संघर्ष चलाया। उन्होंने ही “मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर” का प्रसिद्ध नारा दिया। दक्षिण भारत में ब्राह्मणों द्वारा लादी गई निर्योग्यताओं का मुकाबला करने के लिए गैर-ब्राह्मणों ने 1920 के दशक में एक आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। पूरे भारत में मंदिरों में अछूतों के प्रवेश की मनाही तथा दूसरे प्रतिबंधों के खिलाफ ऊँची तथा निचली जातियों के लोगों ने मिलकर अनेक सत्याग्रह आंदोलन चलाए। फिर भी, छुआछूत विरोधी संघर्ष विदेशी शासन में पूरी तरह सफल नहीं हो सकता था। विदेशी सरकार समाज के रुढ़िवादी तत्वों की शत्रुता मोल लेने से डरती थी। समाज के मूलभूत सुधार का काम केवल स्वतंत्र भारत की सरकार कर सकती थी। इसके अलावा, सामाजिक कल्याण का काम राजनीतिक-आर्थिक कल्याण से गहराई से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए, कमजोर वर्गों की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए आर्थिक प्रगति आवश्यक है, शिक्षा तथा राजनीतिक अधिकारों के प्रसार के साथ भी यही बात है। इस बात को भारतीय नेताओं ने अच्छी तरह समझा था। उदाहरण के लिए, डॉ. भीमराव अंबेडकर लिखते हैं- आपके दुखों को कोई इतनी अच्छी तरह दूर नहीं कर सकता जिस तरह आप कर सकते हैं और आप इन्हें तब तक दूर नहीं कर सकते जब तक कि राजनीतिक सत्ता आपके हाथों में न आए . . . . . हमारे पास एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जिसमें सत्ता में बैठे लोग जीवन के सामाजिक व आर्थिक नियमों को संशोधित करने से न डरते हों, जिसकी न्याय और व्यवहारिकता माँग करती हैं। इस भूमिका को ब्रिटिश सरकार कभी नहीं निबाह सकती। केवल जनता की, जनता के लिए, जनता द्वारा चलाई जा रही सरकार, अर्थात् दूसरे शब्दों में, केवल एक स्वराज्य सरकार, इस काम को संभव बना सकती है।” 1950 के संविधान ने अंततः छुआछूत के खात्मे के लिए एक कानूनी आधार तैयार किया। इसने घोषणा की कि अस्पृश्यता समाप्त की जा चुकी है और किसी भी रूप में इसका पालन मना है। छुआछूत के आधार पर किसी पर कोई भी निर्योग्यता लादना एक अपराध होगा जिसके लिए कानून के अनुसार दंड दिया जाएगा। संविधान कुओं, तालाबों या नहाने के घाटों के उपयोग पर या दुकानों, रेस्तराओं, होटलों और सिनेमाघरों में किसी के प्रवेश पर रोक लगाने से भी मना करता है। इसके अलावा भावी सरकारों के मार्गदर्शन के लिए जो नीति-निर्देशक सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं उनमें से एक में यह बात कही गई है : “राज्य जनकल्याण को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा और इसके लिए जितने प्रभावी ढंग से संभव हो सके, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था लाने तथा उसकी रक्षा करने का प्रयास करेगा जिसमें राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं का आधार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो।” फिर भी जाति-प्रथा की बुराइयों के खिलाफ संघर्ष, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, अभी भी भारतीय जनता का एक प्रमुख कार्यभार है। | |||||||||
| |||||||||