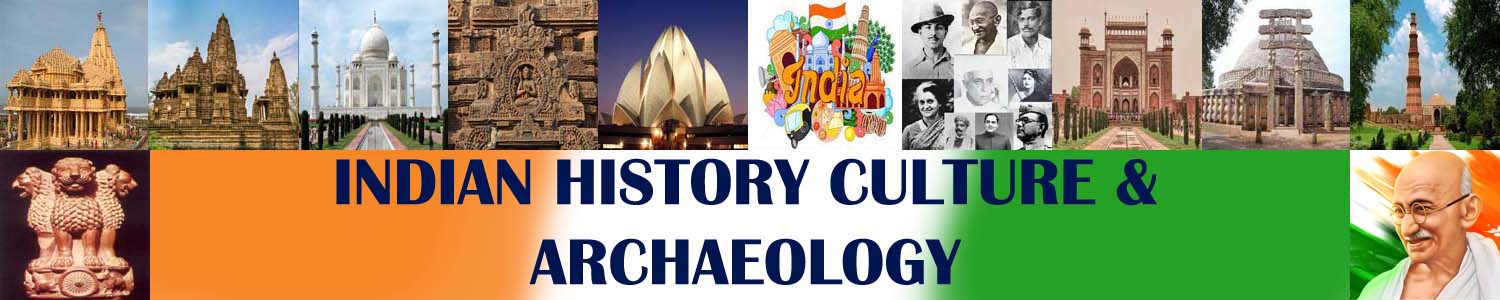| |||||||||
|
1918 से 1939 तक विश्व का राजनीतिक परिदृश्य
ऐसा विश्वास किया गया था कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद (प्रथम विश्व युद्ध को सभी प्रकार के यु़द्धों को समाप्त करने के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध माना गया था) शांति, स्वतंत्रता, लोकतंत्र और हर व्यक्ति के लिए बेहतर जीवन के युग की शुरूआत होगी। इस युद्ध में जब संयुक्त राज्य अमरीका कूदा या जो तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने घोषणा की थी, ‘‘हम उन मूल्यों के लिए लड़ेंगे जिनको हमने सदा से अपने हृदय में सँजो रखा है। हम लोकतंत्र के लिए लड़ेंगे, उन लोगों के अधिकारों के लिए लड़ेंगे जिनको अपनी बात कहने के लिए अपनी ही सरकार के अधिकारियों के समक्ष झुकना पड़ता है। हम छोटे राष्ट्रों की स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए लड़ेंगे। स्वतंत्र जातियों में सामंजस्य स्थापित कर हम अधिकारों की सार्वभौम सत्ता के लिए लडेंगे, इससे राष्ट्रों के बीच शांति और सुरक्षा कायम होगी। इससे दुनिया अंततः अपने आप स्वतंत्र हो जाएगी। ‘‘इस घोषणा के सात महीने बाद रूस में क्रांति हो गई। क्रांति के बाद नई सोवियत सरकार ने एक ‘शांति आदेश‘ जारी किया । इस संदेश में सभी युद्धरत राष्ट्रों की जनता का आह्वान किया गया था कि बिना किसी दूसरे देश या उसके भू-भाग को अपने देश में मिलाए तथा बिना किसी क्षतिपूर्ति (हरजाना दिए) के युद्धरत देश शांति वार्ता में शरीक हों। रूसी क्रांतिकारियों को इस बात की उम्मीद थी कि यूरोप के कुछ अन्य देशों के मजदूर वर्ग भी उनके आदर्शों का अनुसरण करेंगे। मित्र राष्ट्रों ने सोवियत प्रस्ताव ठुकरा दिए और रूस ने युद्ध से अपने को अलग करने के लिए जर्मनी को बहुत बड़ी कीमत चुकाई जो एक साल बाद तक जारी रही। 8 जनवरी 1918 को वुडरो विल्सन ने अपना शांति प्रस्ताव पेश किया था। इसको चौदह सूत्री प्रस्ताव कहा गया था। इन प्रस्तावों में निम्नांकित बातें शामिल थीं : गुप्त कूटनीति का अंत, समुद्रों को मुक्त रखना, हथियारों के जखीरे में कटौती और राष्ट्रीयता के सिद्धांतों के आधार पर यूरोप के देशों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण। उपनिवेशों को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया गया था। उसमें राष्ट्रों के आत्मनिर्णय वाले सिद्धांत को लागू नहीं किया गया। इस प्रश्न पर प्रस्ताव में कहा गया कि उपनिवेशों के सभी दावों (क्लेम्स) का निष्पक्ष समायोजन (इंपार्शियल एडजस्टमेंट) किया जाएगा। अंतिम सूत्र में बड़े तथा छोटे सभी राज्यों की राजनीतिक स्वतंत्रता और भूभागीय अखंडता की गारंटी की व्यवस्था के लिए ‘राष्ट्रों का एक आम संगठन‘ स्थापित करने की बात कहीं गई थी। उम्मीद की गई थी कि प्रस्ताव के ये चौदह सूत्र शांति का आधार बनेंगे।
बहरहाल, इसके बाद के बीस सालों में जो घटनाएँ घटीं, उनसे ये उम्मीदें मिथ्या साबित हुईं। चार साम्राज्यों में राजवंशों के पतन के बावजूद दुनिया के देश पहले की तुलना में अधिक लोकतांत्रिक नहीं बन सके। रूस के क्रांतिकारियों को उम्मीद थी कि यूरोप के कुछ देशों में सामाजिक क्रांतियाँ होंगी लेकिन उनकी यह उम्मीद यथार्थ का रूप नहीं ले सकी और जर्मनी तथा हंगरी में हुई बगावतों को कुचल दिया गया। यूरोप के अनेक देशों में तानाशाही शासन कायम हुए। इन्होंने उग्रराष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया और युद्ध के लिए तैयारी की। तानाशाही शासनों के कायम होने के पीछे प्रमुख कारक सामाजिक क्रांति का भय था, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक प्रणाली थी, उन्हें भी इसका भय सताता रहा। इससे उनकी आंतरिक और विदेश नीतियाँ प्रभावित हुईं। युद्ध के परिणामस्वरूप यूरोप की ताकत काफी घट गई लेकिन उपनिवेशों में इसके शासन का अंत नहीं हुआ। यूरोप में कई नए राष्ट्रों का आविर्भाव हुआ। पूरे तौर पर तो नहीं लेकिन आमतौर पर इन देशों के नक्शे पर उभरने का सैद्धांतिक आधार इनकी राष्ट्रीयता थी लेकिन यूरोप के मामलों को लेकर जो टकराव चल रहे थे, वे समाप्त नहीं हुए। टकरावों के पीछे जो कारण काम कर रहे थे, उनमें से कुछ के पीछे प्रमुख कारण युद्ध के बाद शांति समझौतों पर हुए हस्ताक्षर थे। साम्राज्यवादियों की आपसी होड़ भी युद्ध का कारण थी। होड़ खत्म नहीं हुई और अंतर्राष्ट्रीय टकरावों में पुनः वह मुख्य कारक बन गई। इस अवधि में संयुक्त राज्य अमरीका बहुत बड़ी शक्ति बन गया। अधिकांश यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्थाएँ उस पर निर्भर हो गईं। यह बात तब और साफ हो गई जब 1929 में संयुक्त राज्य अमरीका में आर्थिक मंदी का दौर शुरू हुआ और दुनिया के हर भाग के साथ, यूरोप के भी हर देश की (रूस को छोड़कर) अर्थव्यवस्था पर इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ा। औद्योगीकृत देशों के युद्ध पूर्व समाजों में सामाजिक-आर्थिक असमानता बहुत स्पष्ट थी, इस दौर में भी वे ज्यों की त्यों बनी रहीं यद्यपि लोगों के रहन-सहन के स्तर में कुछ समय के लिए नाममात्र को सुधार हुआ था। बहरहाल, 1929-33 के आर्थिक संकट के कारण मौजूदा व्यवस्था की खामियों पर लोगों का ध्यान केंद्रित हुआ। लगने लगा था कि जनसंख्या के अधिकांश हिस्से के लिए अभाव और दरिद्रता इस व्यवस्था के अनिवार्य अंग हैं। यूरोप के बाहर के देशों में और उत्तरी अमरीका में यह राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों का दौर था यद्यपि इन आंदोलनों को सफलता दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही मिलती थी। विल्सन की 14 सूत्री योजना में जिस राष्ट्र संघ की परिकल्पना की गई थी, वह शांति-समझौते के बाद ही अमल में लाई जा सकी। लेकिन विश्व को युद्ध की लपटों में झुलसने से रोकने में यह संगठन एक बार फिर पूरी तरह असफल साबित हुआ। 1930 के मध्य से ही लगने लगा था कि द्वितीय विश्व युद्ध को किसी भी तरह रोकना संभव नहीं है और 1939 में जब यह आरंभ हो गया तो पहले युद्ध को खत्म हुए मुश्किल से बीस साल हुए थे। यह पहले की तुलना में काफी व्यापक और अधिक विनाशकारी था। शांति के लिए संधियाँप्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों का मुख्य शत्रु जर्मनी था। 18 जनवरी 1919 में पेरिस में जर्मनी के साथ शांति समझौते का प्रारूप तैयार करने के लिए मित्र राष्ट्रों का शांति-अधिवेशन शुरू हुआ। इस अधिवेशन में संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्जेज क्लीमेन्स का वर्चस्व था। इस समझ के आधार पर जर्मनी से आत्मसमर्पण कराया गया था कि शांति-संधि का आधार विल्सन के चौदह सूत्री प्रस्तावों और अन्य वक्तव्यों को बनाया जाएगा। चौदह सूत्री प्रस्तावों के अलावा वुडरो विल्सन ने घोषणा की थी कि किसी भी देश के भूभाग को जबरन छीन कर किसी दूसरे देश में नहीं मिलाया जाएगा, किसी से कोई हर्जाना नहीं लिया जाएगा, किसी को दंडित नहीं किया जाएगा तथा इससे संबद्ध लोगों की स्वतंत्र सहमति ही समझौते का आधार होगी। जब संधि का प्रारूप (ड्राफ्ट) तैयार किया गया तब इस सिद्धांत का पूरी तरह उल्लंघन किया गया। संधि का प्रारूप तैयार करने में जर्मनी अथवा किसी भी केन्द्रीय शक्तियों वाले देश का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं किया गया। जब विजेता देशों ने संधि के प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया तो जर्मनी को इस निर्देश के साथ यह प्रारूप दिया गया कि 5 दिनों के अंदर या तो वह संधि पर हस्ताक्षर करे, अगर वह हस्ताक्षर नहीं करता तो मित्र राष्ट्र पुनः उस पर आक्रमण करेंगे। इस संधि पर हस्ताक्षर करने के अलावा जर्मनी के पास कोई चारा नहीं था। इस संधि को जर्मनी ने ‘‘जबरन थोपी गई संधि‘‘ कहा था। इतना ही नहीं संधि पर हस्ताक्षर समारोह के समय भी जर्मनी के प्रतिनिधियों को अपमानित किया गया। उनसे सभागार में मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के साथ बैठने के लिए नहीं कहा गया। इसके विपरीत सभागार में उनको चारों तरफ से घेर कर इस तरह से लाया तथा सभागार से समारोह के बाद बाहर ले जाया गया जैसे अपराधी को कचहरी के कटघरे में लाया और ले जाया जाता है। जर्मनी पर दबाव डाला गया कि वह अपने युद्ध अपराधों को स्वीकार करे। संधि के प्रारूप में एक अध्याय क्षतिपूर्ति को लेकर तैयार किया गया था। इसकी शुरूआत इस प्रकार की गई थी, ‘‘जर्मनी और उसके सहयोगियों द्वारा किए गए सभी तरह के नुकसान के लिए जर्मनी और उसके सहयोगी दायित्व स्वीकार करते हैं। जर्मनी तथा उसके सहयोगियों ने आक्रमण करके मित्र राष्ट्रों, उसकी सहयोगी सरकारों और उनकी जनता पर युद्ध थोपा है।‘‘ इस प्रारूप को जब जर्मनी के विदेश मंत्री को दिखाया गया तो उन्होंने कहा, ‘‘हमसे माँग की गई है कि हम इस बात को स्वीकार कर लें कि युद्ध के लिए सिर्फ हम लोग जिम्मेदार हैं.........हम किसी भी दायित्व से मुकरना नहीं चाहते........लेकिन इसको हम जोर देकर अस्वीकार करते हैं कि इसके लिए सिर्फ जर्मनी जिम्मेदार है। पिछले पचास वर्षों में सारे यूरोपीय देशों के साम्राज्यवाद ने अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों में संक्रामक रोग की तरह जहर घोल दिया है......।‘‘ संधि में ऐसी धाराओं का भी प्रावधान था जिनमें उन जर्मनों पर मुकदमा चलाने के लिए कहा गया था जिनके ऊपर मित्र राष्ट्रों ने युद्ध अपराधी होने का आरोप लगाया था। जिन लोगों पर इस तरह के आरोप थे उस सूची में जर्मनी के सम्राट का भी नाम था जो उन दिनों हालैंड में शरण लिए हुए थे।युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने आपस में कई गुप्त संधियाँ और समझौते किए थे। इस संधि मसौदे की रूपरेखा तैयार करने में उन गुप्त समझौतों और करारों को आधार बनाया गया था। इन गुप्त समझौतों का मुख्य मकसद युद्ध में प्राप्त लूट की संपत्ति का आपस में बँटवारा करना था। क्रांति के बाद रूस ने न सिर्फ उनको मानने से इनकार किया बल्कि उन गुप्त समझौतों को सार्वजनिक भी बना दिया। मित्र राष्ट्रों का दावा था कि वे स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं लेकिन रूस द्वारा रहस्योद्घाटन किए जाने पर उन सबके दावे बेनकाब हो गए। अमरीका तथा ब्रिटेन के अखबारों में ये समझौते प्रकाशित हो गए लेकिन मित्र राष्ट्र जब जर्मनी के भाग्य का निर्णय कर रहे थे तो इस भण्डाफोड़ का उन पर कोई असर नहीं हुआ था। इस भण्डाफोड़ से वे टस-से-मस नहीं हुए (बाद में टर्की तथा अन्य केंद्रीय शक्तियों के साथ हुए समझौते में भी उनका व्यवहार ऐसा ही था)। वुडरो विल्सन सब प्रकार से खुले राजनय के समर्थक थे लेकिन उन्हें भी इससे सहमत होने के लिए तैयार कर लिया गया। शांति सम्मेलन के आरंभिक कार्यों में एक काम ‘राष्ट्रसंघ‘ (विल्सन की योजना में इसकी स्थापना के लिए चौदहवें सूत्र में प्रस्ताव किया गया था) की स्थापना का था। अप्रैल 1919 में सम्मेलन ने ‘राष्ट्रसंघ‘ के इकरारनामे (या औपचारिक सत्यनिष्ठा की घोषणा और अनिवार्य समझौता) को मंजूरी दी। उसमें कहा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना संघ के मूल उद्देश्य हैं। संघ के मूल उद्देश्यों के लिहाज से इकरारनामे की तीन धाराएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। धारा VIII में कहा गया था कि ‘‘शांति कायम रखने के लिए राष्ट्रों के हथियार भंडार को कम करने की जरूरत है।‘‘ धारा X में कहा गया था, ‘‘संघ के सदस्य वचन देते हैं कि वे सभी सदस्य राष्ट्रों की मौजूदा राजनीतिक स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे और बाहरी आक्रमण से उनकी रक्षा करेंगे। ........इस प्रकार के किसी भी आक्रमण के मामले में या इस प्रकार के आक्रमण के खतरे या धमकी के मामले में परिषद् (संघ की परिषद्) उन तरीकों पर अपनी राय जाहिर करेगी। इसी राय के आधार पर इस दायित्व को पूरा किया जाएगा।‘‘ धारा XVI में अनुशासनात्मक कार्रवाई (या दण्ड विधान) का विवरण था। इस धारा में कहा गया था कि ‘‘संघ का कोई भी सदस्य यदि युद्ध का सहारा लेता है.......तो इसको अपने आप मान लिया जाएगा कि उसने संघ के अन्य सभी सदस्य देशों पर आक्रमण किया है.........।‘‘ इस धारा में यह नियम भी रखा गया कि ऐसी स्थिति में दूसरे सभी सदस्य देश आक्रमणकारी देश से अपने सारे व्यापारिक और वित्तीय संबंध तोड़ लेंगे और परिषद् की सलाह पर आक्रमणकारी देश के खिलाफ संयुक्त रूप से फौजी कार्रवाई करेंगे। जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे, शांति बनाए रखने और आक्रमणकारी देश के खिलाफ कारगर कदम उठाने में राष्ट्र संघ एकदम प्रभावहीन साबित हुआ। हथियारों की कटौती के मामले में भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। हाँ, संघ द्वारा स्थापित दो अभिकरणों (एजेंसियों) ने अवश्य ही काफी उपयोगी काम किए। ये अभिकरण थे - अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए स्थाई अदालत (यह विश्व अदालत भी कहलाता है) और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। राष्ट्र संघ के विषय में प्रमुख घटनाओं की चर्चा बाद में की जाएगी। वारसाई नामक स्थान पर 28 जून 1919 में जर्मनी के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसलिए इसे वारसाई की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के प्रावधानों के मुताबिक अलसेस लोरां को फ्रांस को वापस लौटाया जाना था, 1871 में जर्मनी ने इसको अपने कब्जे में ले लिया था। पोलैंड नाम के नए राज्य की स्थापना की गई और समुद्र तक जाने के लिए इसे रास्ता देने के उद्देश्य से 65 किलोमीटर की एक पट्टी छोड़ी गई। इस पट्टी के कारण प्रूशिया (प्रशा) जर्मनी के शेष भाग से कट गया। डानजिंग को स्वतंत्र नगर का दर्जा मिला और इसका राजनीतिक नियंत्रण राष्ट्र संघ के हाथ में और आर्थिक नियंत्रण पोलैंड के हाथ में सौपा गया। बेल्जियम, डेनमाक्र और लिथुआनिया को भी जर्मनी के भू-भाग का कुछ हिस्सा मिला। इन क्षेत्रों की सारी कोयला खदानों को पंद्रह सालों के लिए राष्ट्र संघ, के नियंत्रण में कर दिया गया और क्षतिपूर्ति के रूप में यहाँ की खदानों को फ्रांस को हस्तांतरित कर दिया गया। जर्मनी पर रोक लगा दी गई कि आस्ट्रिया के साथ उसका एकीकरण नहीं हो सकता। इस बात की भी व्यवस्था की गई कि राइनलैण्ड का स्थाई रूप से विसैन्यीकरण कर दिया जाए और इस पर 15 सालों तक मित्र राष्ट्रों का नियंत्रण बना रहे। जर्मनी की सैनिक शक्ति की सीमा एक लाख निर्धारित कर दी गई और इसकी भी व्यवस्था की गई कि वह किसी भी प्रकार से नौ सेना नहीं रखेगा (केवल कुछ नौ सैनिक जहाज रख सकता था), न ही वह पनडुब्बियाँ रख सकेगा। चूँकि अपना ‘युद्ध अपराध‘ स्वीकारने के लिए जर्मनी को मजबूर किया गया था, इसलिए उसे मित्र राष्ट्रों को क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ पैसों की अदायगी भी करनी पड़ी थी। इस क्षतिपूर्ति का हिसाब बाद में लगाया गया और इसकी राशि 66000 लाख पौंड ठहराई गई। जर्मनी से उसके सारे उपनिवेश छीन लिए गए और इन उपनिवेशों को विजेता देशों में गुप्त संधियों में किए गए करारों के मुताबिक बाँट दिया गया। जर्मनी के नियंत्रण वाले पूर्वी अफ्रीका का अधिकांश भाग - तंगानिका, ब्रिटेन को मिला। इसी का कुछ हिस्सा पुर्तगाल और बेल्जियम कांगो को दिया गया था। कामरून और तोगोलैंड को ब्रिटेन और फ्रांस में बाँटा गया था। रूआण्डा-उरूण्डी को बेल्जियम के हवाले कर दिया और दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका को दे दिया गया। जर्मनी के नियंत्रण वाले प्रशांत क्षेत्र के द्वीपों को आस्ट्रिया, न्यूजीलैण्ड और जापान में बाँटा गया। जापान ने शानतुंग पर अधिकार कर लिया। पहले यह जर्मनी के प्रभाव क्षेत्र में था। इन बँटवारों और नियंत्रणों का संदर्भ ऊपर आ चुका है। जर्मनी द्वारा शांति-संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद इन बँटवारों को राष्ट्र संघ द्वारा वैद्यता का जामा पहना दिया गया। सिद्धांत रूप में माना गया कि विजेता देशों ने इन उपनिवेशों को अपने राज्य में शामिल नहीं किया है। राष्ट्र संघ के इकरारनामे में इसके लिए रास्ता निकाला गया था तथा इसको समादेश या अधिकारपत्र (मैनडेट) कहा गया। पराजित उपनिवेशवादी देशों पर यह व्यवस्था लागू की गई। इस इकरारनामे में कहा गया था कि ‘‘इन उपनिवेशों और क्षेत्रों में ऐसे लोग रहते हैं जो आधुनिक दुनिया की तनावपूर्ण स्थितियों में अपने बलबूते पर टिक नहीं सकते हैं।‘‘ और ‘‘ऐसे लोगों की भलाई और विकास का काम सभ्य लोगों के पवित्र विश्वास का अंग है।‘‘ इकरारनामे में कहा गया था कि ‘‘इस विश्वास को अमली जामा पहनाने के लिए इन उपनिवेशों और क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विकसित राष्ट्रों के संरक्षण में रखा जाना चाहिए।‘‘ बहरहाल विकसित देश पहले से ही यह निर्णय कर चुके थे कि कौन सा उपनिवेश किस विकसित देश के संरक्षण में रहेगा। इसलिए इस विषय में ‘राष्ट्र संघ‘ को कुछ भी करना-धरना नहीं था। वारसाई की संधि ही प्रमुख संधि थी जिसका संबंध प्रमुख पराजित देश जर्मनी से था। अन्य केंद्रीय शाक्तियों के साथ अलग-अलग संधियों पर हस्ताक्षर हुए। 10 सितंबर को आस्ट्रिया ने सेंट जर्मेन की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के प्रावधानों के मुताबिक आस्ट्रिया ने हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया के स्वतंत्र अस्तित्व को मान्यता प्रदान की तथा इटली समेत इन देशों को उसे कुछ क्षेत्र देने पड़े। इसके बाद आस्ट्रिया की स्थिति एक छोटे राज्य की रह गई और इस बात पर रोक लगा दी गई कि वह जर्मनी के साथ मिल कर संघ नहीं बना सकता। हंगरी के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर हुए क्योंकि इसे अब स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिला था। इसे यूगोस्लाविया, रूमानिया और चेकोस्लोवाकिया को कुछ भूक्षेत्र देने पड़े। बल्गेरिया के साथ की गई संधि के आधार पर बल्गेरिया को अपने राज्य के कुछ क्षेत्र, रूमानिया, यूगोस्लाविया और ग्रीस को देने पड़े। अंतिम समझौते पर टर्की ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के अनुसार अरब क्षेत्रों को ब्रिटेन और फ्रांस ने पहले ही आपस में बाँट लिया था। सीरिया और लेबनान फ्रांसीसी नियंत्रण में आ गए थे और इराक, फिलिस्तीन तथा ट्रांसजोर्डन ब्रिटिश नियंत्रण में कुछ अरब क्षेत्र पहले से ही ब्रिटिश प्रभाव में आ चुके थे जैसे कुवैत, बहरीन और कातार, जबकि कुछ दूसरे क्षेत्र स्थानीय शासकों के अधीन थे और जिनको स्वायत्तता मिली हुई थी, पहले की तरह बने रहे। हेजाज को अलग राज्य बनाया गया लेकिन जल्दी ही नेज्द के शासक इब्न सऊद ने इसे जीत लिया और जीतने के बाद सऊदी अरब राज्य स्थापित किया। ऑटोमन के हाथ से अरब साम्राज्य का निकलना अवश्यंभावी हो गया। ऑटोमन के खिलाफ अरब राष्ट्रवादियों को सिर्फ इसलिए मित्र राष्ट्रों से समर्थन मिला था कि युद्ध के बाद उनके क्षेत्रों पर अधिकार किया जा सके। लेकिन टर्की के विभाजन से टर्की राष्ट्रवादी विद्रोहों का जन्म हुआ। ग्रीस और इटली ने टर्की के काफी बड़े भू-भाग पर अधिकार कर लिया था। सितंबर 1920 में टर्की के सुल्तान ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि में वह टर्की के पूर्ण विभाजन के लिए तैयार हो गया था। इस बीच देश में राष्ट्रीय विद्रोह की ऐसी आंधी चली कि उसने इस देश को पूरी-तरह झकझोर कर रख दिया। इस विद्रोह का नेतृत्व मुस्तफा कमाल ने किया था। अंकारा में उन्होंने एक सरकार बनाई। कमाल की फौजों ने इतालवियों और ग्रीकों को देश से बाहर खदेड़ दिया और जुलाई 1923 में मित्र राष्ट्रों को टर्की के साथ नए समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। टर्की को गणराज्य घोषित किया गया। यहीं से एक आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में टर्की की विकास यात्रा शुरू हुई। खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया। ऊपर से देखने में इन संधियों ने प्रथम विश्व को समाप्त कर दिया लेकिन वास्तविक अर्थों में इन संधियों के बहुत से प्रावधान नए तनावों के स्रोत बन गए। शुरू से ही रूस को सभी प्रकार के विचार विमर्श से अलग रखा गया था। इतना ही नहीं उसे राष्ट्र संघ का सदस्य भी बनाया गया था (वैसे ही जैसे जर्मनी को राष्ट्र संघ में नहीं लिया गया था)। असल बात यह थी कि जब संधियों का प्रारूप तैयार किया जा रहा था और शांति को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की जा रही थी तब कई मित्र राष्ट्रों की फौजें रूस की क्रांतिकारी सरकार के साथ युद्ध कर रही थीं। विजयी उपनिवेशवादी ताकतों की मर्जी के मुताबिक उपनिवेशों के सवाल निपटा दिए गए थे लेकिन निपटारे के दौरान उपनिवेशों की आम जनता की भावनाओं का ध्यान नहीं रखा गया था। प्रथम विश्व युद्ध में चीन भी मित्र राष्ट्रों में एक देश था और शांति सम्मेलन में उसको प्रतिनिधित्व भी मिला था लेकिन चीन का जो भू-भाग औपचारिक तौर पर जर्मनी के नियंत्रण में था, उसे जापान को सौंप दिया गया था। दो विश्व युद्धों के बीच संयुक्त राज्य अमरीका, रूस और जापानदोनों विश्व युद्धों के बीच प्रमुख शाक्तियों के रूप में तीन देशों के नाम लिए जाते थे - संयुक्त राज्य अमरीका, रूस और जापान। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूसी क्रांति के पहले तक कुछ समय के लिए तीनों सहयोगी थे। युद्ध के बाद जब रूस को बहिष्कृत कर दिया गया, तब शांति संधियों के प्रारूप तैयार करने में संयुक्त राज्य अमरीका ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और इसी नाते प्रथम विश्व युद्ध के बाद की दुनिया को बनाने में उसका मुख्य हाथ था। इसलिए वह विश्व की प्रभावशाली ताकत बनकर उभरा था। जिस समय संयुक्त सोवियत समाजवादी गणतंत्र का जन्म हुआ तो रूस उसका एक अंग था और वह युद्ध, क्रांति, गृह युद्ध और विदेशी हस्तक्षेप के चंगुल से बाहर निकला था। वह यूरोप का अत्यंत जर्जर और कमजोर देश था। लेकिन 1930 के दशक के अंत तक रूस अत्यंत शक्तिशाली औद्योगिक और सैनिक ताकत के रूप में उभर कर सामने आया। उसकी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था दुनिया के और देशों से भिन्न थी। विश्व की गतिविधियों में उसने विशेष भूमिका अदा की। इस युद्ध से जापान एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के सबसे ताकतवर देश के रूप में उभरा था और इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम करने की उसमें महत्वाकांक्षा थी।संयुक्त राज्य अमरीकावारसाई की संधि का प्रारूप तैयार करने में संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की प्रमुख भूमिका थी। लेकिन इस पूरी संधि को ही अमरीकी सीनेट ने अस्वीकार कर दिया। इसके परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमरीका ने ‘राष्ट्र संघ‘ (लीग ऑफ नेशन्स) में शामिल होने से मना कर दिया यद्यपि यह संघ मुख्य रूप से अमरीकी राष्ट्रपति विल्सन के दिमाग की उपज थी। 1920 में डेमोक्रेटिक दल (विल्सन इसी दल के राष्ट्रपति थे) के प्रत्याशी रिपब्लिकन दल के प्रत्याशियों से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हार गए। उसके बाद के 1924 तथा 1928 के चुनावों में भी रिपब्लिकन दल की जीत हुई।युद्ध के तत्काल बाद के वर्ष अमरीका में आर्थिक संकट से ग्रस्त वर्ष थे। युद्ध के दौरान जब यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं को जबर्दस्त झटका खाना पड़ा, उस समय अमरीकी अर्थव्यवस्था का खूब विस्तार हुआ, वह फलती-फूलती रही। इसकी वजह थी - संयुक्त राज्य अमरीका की धरती पर कोई युद्ध नहीं लड़ा गया। उसके नगरों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और फसलों को कोई क्षति नहीं पहुँची। लेकिन युद्ध के खत्म होते ही युद्ध के कारण होने वाला विस्तार अचानक थम गया। इसकी वजह से अमरीका में गंभीर संकट पैदा हो गया। तकरीबन एक लाख व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का दिवाला निकल गया और करीब-करीब पचास लाख लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। इसके चलते श्रमिक असंतोष पैदा हुआ और समूचा अमरीका हड़तालों के समुद्र में गोते लगाने लगा। अकेले 1919 में अमरीका में तकरीबन 3500 हड़तालें हुईं। इसमें कुछ हड़तालें तो ऐसी थीं जिसमें हजारों मजदूर शामिल थे और ये काफी लंबे समय तक चलीं। इन हड़तालों को सख्ती से कुचल दिया गया और इस बात का प्रचार करके मजदूरों के मन में भय तथा आतंक पैदा किया गया कि अमरीका भी रूस की तरह क्रांति की भयानक लपटों से झुलस सकता है। इसके उपरांत अमरीकी अर्थव्यवस्था सँभली और उसकी अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व संवृद्धि हुई। जिस दौर में पूँजीवादी दुनिया के बाकी देश विश्व युद्ध के कारण हुए भीषण विनाश से उभरने की कोशिश में लगे थे, उस दौर में उन्नत प्रौद्योगिकी के सहारे संयुक्त राज्य अमरीका ने अपना औद्योगिक विस्तार आरंभ किया। विश्व के प्रमुख ऋणदाता देश के रूप में उभरकर वह सामने आया। यूरोप के अधिकांश देश उसके कर्जदार थे। उस जमाने के प्राप्त आंकड़ों से जबर्दस्त औद्योगिक विस्तार के संकेत मिलते हैं। 1929 में अकेले संयुक्त राज्य अमरीका में 50 लाख कारें बिकीं। इस औद्योगिक विस्तार के बाद अमरीका के हाथ में और अधिक आर्थिक शक्ति केंद्रित हो गई। मुट्ठी भर बड़ी कंपनियाँ हजारों की संख्या में चलने वाले छोटे-छोटे उद्योगों को निगल गईं। विभिन्न उत्पादकों में जबर्दस्त स्पर्धा पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता थी। उस स्पर्धा का लगभग अंत हो गया। कुछ मामलों में तो देश का सारा उद्योग एक ही कंपनी के हाथ में सिमट गया, जैसे इस्पात का उद्योग। ये कंपनियाँ बहुत प्रभावशाली थीं। एक कहावत प्रचलित थी कि ‘जनरल मोटर्स‘ के लिए जो कुछ फायदेमंद है, वही अमरीका के लिए भी फायदेमंद है। आर्थिक शक्ति के जबर्दस्त केंद्रीयकरण के कारण भ्रष्टाचार खूब फला फूला और भ्रष्टाचार के अनेक मामले सामने आए। इनमें बड़े-बड़े राजनेता और उच्च पदाधिकारियों का हाथ पाया गया। यद्यपि इस अभूतपूर्व आर्थिक संवृद्धि के बावजूद मजदूर वर्ग को नाममात्र का फायदा हुआ। उनमें से अधिकांश का गरीबी और कष्टपूर्ण जीवन ज्यों-का-त्यों बना रहा। मजदूरों को मजदूरी तो कम मिलती ही थी, साथ ही नौकरी से हाथ धोने का खतरा हमेशा बना रहता था। वहाँ कोई शक्तिशाली ट्रेड यूनियन आंदोलन भी नहीं उभर सका क्योंकि कंपनियों को सरकार और अदालत दोनों से समर्थन मिलता था और ये कंपनियाँ अक्सर पुलिस बल और किराए के बदमाशों के बल पर हिंसा का इस्तेमाल करती थीं। इस अभूतपूर्व औद्योगिक विस्तार का अंत अभूतपूर्व संकट के रूप में सामने आया। 1929 के शुरूआती दौर में संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति पद पर हरबर्ट हूवर जीत कर आए। उन्होंने घोषणा की, ‘‘हमारा देश संसाधन संपन्न देश है, इसका भव्य सौंदर्य हमें प्रेरित करता है, करोड़ों सुखी परिवारों का यह देश है। यहाँ के लोगों को हर तरह की सुख सुविधाएँ और अवसर प्राप्त हैं।‘‘ उनका उस समय मानना था कि उनके देश का ‘‘भविष्य आशा और उम्मीदों से परिपूर्ण‘‘ था। उनके इस सुनहरे वक्तव्य के कुछ ही महीनों बाद 24 अक्टूबर 1929 को व्यवसाय और उद्योग की गाड़ी चरमरा उठी, इसको पूरी दुनिया महामंदी (दि ग्रेट डिप्रेशन) के नाम से जानती है। जो आर्थिक संकट का दौर वहाँ शुरू हुआ उसकी जड़ें वहाँ की अर्थव्यवस्था के भीतर ही थीं। बड़े लाभ के लिए अर्थव्यवस्था का अबाध विस्तार होता चला गया जबकि अधिकांश अमरीकी जनता को गरीबी का अभिशाप झेलने के लिए छोड़ दिया गया था। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास के कारण उत्पादन अबाध गति से बढ़ा और इसके चलते उद्योगों को काफी मुनाफा भी हुआ। इस विरोधी स्थिति के कारण हालात ऐसे हो गए कि अमरीकी समाज में उन लोगों की संख्या बहुत कम हो गई जो औद्योगों द्वारा तैयार किए गए सामान को खरीद सकें। 1920 के दशक में पाँच से सात प्रतिशत गैरकृषीय जनसंख्या (नगरीय तथा औद्योगिक) बेरोजगार रही। लगभग एक दशक की अभूतपूर्व आर्थिक संवृद्धि के बावजूद आधे से अधिक अमरीकी परिवार निम्नतर जीवन स्तर की या उससे भी निचले स्तर की जिंदगी जी रहे थे तथा जो सामान अमरीका में तैयार हो रहा था, उसे खरीदने की स्थिति में वे नहीं थे। अनुमान लगाया गया है कि 1929 में अमरीका की लगभग एक तिहाई निजी आय पाँच प्रतिशत लोगों के हाथ में पहुँचती थी। सभी लोग इस बात को मानते हैं कि ‘‘क्रयशक्ति का दोषपूर्ण वितरण इस महामंदी का आधारभूत नहीं तो मुख्य कारक अवश्य था। यह बात वे अर्थशास्त्री भी मानते हैं जो पूँजीवदी व्यवस्था के किसी भी स्वरूप की आलोचना नहीं करते। शेयर बाजार में जब शेयर के दाम नीचे आने लगे तब चारों ओर दहशत फैल गई तथा लोग अपने-अपने शेयर बेचने के लिए बाजारों की तरफ भागने लगे। इससे शेयर के बाजार भाव में और गिरावट आई। इस तरह से बाजार में मंदी की शुरूआत हुई। इसकी वजह से शेयर बाजार ढह गया। इसके बाद बैंक बंद हुए। 1929 और 1932 के बीच 5700 से ज्यादा बैंक दिवालिया हो गए तथा लगभग 3500 बैंकों ने कारोबार बंद कर दिया। बैंकों के दिवालिया होने के कारण लाखों अमरीका वासियों की जीवन भर की गाढ़ी कमाई लुप्त हो गई। इसका नतीजा यह हुआ कि अब पहले से भी कम लोगों के पास बाजार से सामान खरीदने के लिए पैसा बच रहा। उद्योगों को बैंकों से उधार मिलना बंद हो गया और उनके पास तैयार माल बाजार में, खरीददार के अभाव में बिक नहीं पाया। इसीलिए उनके उद्योग बंद होने लगे। इससे काफी लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे। इसके परिणामस्वरूप बाजार में माल की माँग में और भी कमी आई जिसके कारण और ज्यादा कारखाने बंद हुए। इस क्रम में बेरोजगारों की संख्या दिनों-दिन बढ़ती चली गई। 1929 में यह 15 लाख थी जो बढ़कर 1930 में 50 लाख, 1931 में 90 लाख तथा 1932 में 1 करोड़ 30 लाख तक पहुँच गई। बेरोजगारी की 1932 की संख्या संयुक्त राज्य अमरीका को समूची श्रम शक्ति के 25 प्रतिशत से भी ऊपर थी। अमरीकी किसानों की हालत शहर के मजदूरों से किसी भी हालत में बेहतर नहीं थी। कृषि उपजों की कीमतें काफी नीचे आ गईं और इसके चलते लाखों किसान अपनी जमीन से हाथ धो बैठे तथा उनकी स्थिति दरिद्रों जैसी हो गई। 1930 का दशक अमरीकी जनता के लिए बड़ा भयानक था। काले लोगों पर इसका सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यूरोप में दो लाख से ज्यादा लोगों ने फौजी सिपाही के रूप में काम किया था। घर लौट कर उन्होंने पाया कि नस्ल के आधार पर उनके खिलाफ भेदभाव और भी बढ़ गया है। भीड़ द्वारा सरेआम बिना अपराध बताए सजा देने (लिंचिंग) की घटनाएँ बढ़ चुकी हैं। यहाँ तक कि युद्ध से वापस आए बहादुर नीग्रो लोगों का भी अनादर और अपमान किया जाता है और तो और उनको भी ‘लिंचिंग‘ का शिकार होना पड़ता है, उन्हीं को सबसे पहले नौकरियों से बाहर किया जाता है तथा अक्सर उन्हें निकालकर उनकी जगह किसी गोरे को नौकरी दे दी जाती है। चुनाव में मतदान का अधिकार उनको अभी भी नहीं दिया गया था। यह स्थिति काफी समय तक बरकरार रही। अब नस्लीय भेदभाव और नस्ल के आधार पर अलग बस्तियों में रहने की प्रवृत्ति और भी बढ़ गई। यह प्रवृत्ति पूरे अमरीका में छूत की बीमारी की तरह फैल गई थी जबकि पहले यह दक्षिण के राज्यों तक ही सीमित थी। देश के अनेक भागों में ‘कू-क्लक्स-क्लान‘ जैसे श्वेत लोगों के आतंकवादी गुट सक्रिय हो गए थे। काले लोगों के अलावा यहूदी, विदेशी लोग तथा ऐसे लोग, आतंकवादी संगठनों के हिंसा के शिकार माने जाते थे। जो नस्लीय दृष्टि से अशुद्ध माने जाते थे। महामंदी के दौरान काले लोगों के साथ भेदभाव की स्थिति पहले की तुलना में और खराब हो गई। गोरे लोगों ने माँग की कि जब तक प्रत्येक गोरे को नौकरी (रोजगार) नहीं मिल जाती, जब तक किसी भी नीग्रो को नौकरी में नहीं लिया जाना चाहिए। हजारों की संख्या में नीग्रो दक्षिणी राज्यों को छोड़कर उत्तर के राज्यों में जा बसे लेकिन उत्तर के राज्यों में भी हालत कोई बेहतर नहीं थी। अनुमान लगाया गया है कि 1932 में काले लोगों की जनसंख्या के 1/3 लोग एकदम बेरोजगार थे और एक तिहाई को आंशिक रूप से ही काम मिल पाता था। अमरीकी समाज में 1930 का दशक आमूल सुधारवाद के विकास का दौर था। इस दौर में एक बहुत ताकतवर ट्रेड यूनियन आंदोलन उभरना शुरू हुआ। अमरीका में समाजवादी व्यवस्था की वकालत करने वाले परिवर्तनवादी राजनीतिक आंदोलन शुरू हो गए थे। अमरीका की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना इसके पहले ही हो चुकी थी। इस दौर में उसकी ताकत काफी बढ़ी और मजदूरों, काले लोगों तथा गोरों को एक साथ संगठित करने और नस्लवाद के विरूद्ध संघर्ष चलाने में उसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। काले लोगों ने भी अपने को नस्लवाद के विरूद्ध संगठित किया। एन. ए. ए. सी. सी. पी. की पहले चर्चा की जा चुकी है। इसने काले तथा गोरे मजदूरों को एकजुट करने और नस्लवाद के खिलाफ लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौर में अन्याय और दमन नंगे रूप में सामने आए। इसने अमरीका को हिलाकर रख दिया। कई दूसरे देशों की जनता ने भी इस दमन और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। इस संदर्भ में पहला मामला दो इतालवी आव्रजकों का था। इनमें एक का नाम साक्को था और दूसरे का नाम वानजेत्ती था। इन दोनों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ जो आरोप लगाए उनके प्रमाण पक्के नहीं थे अतः उन आरोपों के प्रति लोगों ने शंकाएँ जाहिर कीं। लेकिन उन्हें फाँसी पर लटका दिया गया। आमतौर पर संयुक्त राज्य अमरीका और पूरे विश्व में लोगों को विश्वास था कि ये दोनों सीधे और निर्दोष लोग थे और इनको एक जाली मामले में लपेटा गया था जिससे अमरीका में भय और आतंक का वातावरण तैयार किया जा सके और बताया जाए कि विध्वंसकारी शक्तियों द्वारा क्रांति का खतरा पैदा हो गया है। पूरे विश्व में माँग उठी थी कि इस मुकदमें की सुनवाई दुबारा होनी चाहिए। लेकिन यह माँग ठुकरा दी गई। साक्को तथा वानजेत्ती को फाँसी पर लटका दिया गया। इसी तरह का एक अन्य मामला है जिसे स्काट्सबोरो के मामले के नाम से इतिहास में याद किया जाता है। इस मामले का संबंध नस्लवाद से था। 1931 में अलाबामा में 9 नौजवान लड़कों पर दो श्वेत वेश्याओं के साथ बलात्कार का आरोप लगाकर मुकदमा चलाया गया। इनमें से आठ को फाँसी की सजा सुनाई गई। जिस न्यायपीठ (जूरी) ने सजा सुनाई थी, उसके सारे सदस्य गोरे थे। आमतौर पर लोगों ने माना था कि यह पूरा मुकदमा ही जाली है। इसलिए इन निर्दोष बच्चों को बचाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया था और इस अभियान को विश्व-जनमत का समर्थन भी मिला था। इसका परिणाम यह निकला कि इस मामले में सजा पर अमल नहीं किया जा सका था लेकिन इनमें से अधिकांश लड़के वर्षों जेल में सड़ते रहे। महामंदी की जड़ तो अमरीका था लेकिन इसकी चपेट में यूरोप का हर देश आ गया था। दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं था जो थोड़ा बहुत इससे प्रभावित न हुआ हो। यूरोप के देशों पर इसके प्रभाव अधिक घातक थे जिनकी चर्चा आगे की जाएगी। संयुक्त राज्य अमरीका के कुछ सबसे खराब प्रभावों का उपचार 1931 के बाद शुरू किया गया। यह काम फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट के राष्ट्रपतित्व काल में किया गया जिन्हें 1933 में पहली बार राष्ट्रपति चुना गया था। इसके बाद के तीन और चुनावों में भी वे विजयी हुए थे। सुधार के जो कार्यक्रम रूजवेल्ट ने शुरू किए थे उनको ‘न्यू डील‘ नाम से जाना जाता है। इसके तहत काफी बड़े पैमाने पर कल्याण कार्यक्रम शुरू किया गया। जनसंख्या के अनेक तबकों में इससे लोगों की परेशानी कुछ कम हुई, यद्यपि लोगों का विश्वास था कि काले लोगों के प्रति रूजवेल्ट का रूख सहानुभूतिपूर्ण था लेकिन काले लोगों की दशा सुधारने के लिए नाममात्र को ही कदम उठाए गए। अमरीका ने ‘राष्ट्रसंघ‘ में शामिल होने से इनकार कर दिया था। अमरीका का इनकार करना इस संगठन के लिए सबसे बड़ा आघात था। इस दौरान संयुक्त राज्य अमरीका की मुख्य चिंता दुनिया के दूसरे हिस्सों में अपना आर्थिक नियंत्रण कायम करना थी। विश्व की अर्थव्यवस्था पर संयुक्त राज्य अमरीका के बढ़ते हुए प्रभुत्व का यूरोप तथा बाकी दुनिया पर काफी बुरा असर पड़ा। 1920 में संयुक्त राज्य अमरीका ने जर्मनी और कुछ अन्य देशों को काफी बड़ी मात्रा में ऋण दिए। इससे आर्थिक संकट से उबरने में थोड़ी मदद मिली लेकिन इन देशों पर संयुक्त राज्य अमरीका के ऊपर बढ़ती निर्भरता का घातक प्रभाव पड़ा और महामंदी के दौर में ऐसा होना स्वाभाविक तथा अवश्यंभावी भी था। चीन को लेकर जापान की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा अमरीका के लिए चिंता का मुख्य विषय था क्योंकि इससे संयुक्त राज्य अमरीका को नुकसान हो सकता था। 1922 में जापान, ब्रिटेन, फ्रांस तथा इटली के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। इस संधि का मकसद इस बात को सुनिश्चित करना था कि चीन में सबके लिए दरवाजा खुला रहे ताकि चीन पर किसी एक देश का अकेला वर्चस्व कायम न हो सके। इस संधि में जापान की नौसैनिक ताकत पर भी कुछ रोक लगाई गई थी। इसके बाद भी जापान प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी ताकत था। अन्य पश्चिमी देशों की तरह 1931 में अमरीका ने स्पष्ट कर दिया था कि वह जापान के और बाद में इटली और फ्रांस के आक्रमण को रोकने के लिए हस्तक्षेप नहीं करेगा। सोलह साल तक संयुक्त राज्य अमरीका ने सोवियत रूस की क्रांतिकारी सरकार को मान्यता नहीं दी (बाद में साम्यवादी चीन को भी उसने बीस साल बाद मान्यता प्रदान की)। लैटिन अमरीका में संयुक्त राज्य अमरीका का आर्थिक प्रभुत्व और अधिक सुदृढ़ हो गया और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के राष्ट्रपति का आसन ग्रहण करने तक सीधा सैनिक हस्तक्षेप का सिलसिला चलता रहा। लैटिन अमरीका पर संयुक्त राज्य अमरीका प्रभुत्व के कारण वहाँ के लोगों में काफी व्यापक रोष था तथा लैटिन अमरीकी लोग इसको ‘‘यांकी साम्राज्यवाद‘‘ कहा करते थे। संघीय सोवियत समाजवादी गणतंत्रबहुत से इतिहास रूस की बोल्शेविक क्रांति को बीसवीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानते हैं। कुछ इतिहासकार इसको मानव इतिहास में नए युग की शुरूआत मानते हैं। हम किसी भी दृष्टि से देखें, यह क्रांति बीसवीं सदी की दुनिया के स्वरूप को निर्धारित करने में प्रमुख कारक रही है। मानव इतिहास में समाज में आधारभूत रूपांतरण लाने के लिए किसी अन्य क्रांति ने ऐसा प्रयास नहीं किया जैसा प्रयास 1917 की रूसी क्रांति ने किया है। सभ्यता के प्रारंभ से लेकर 5000 वर्षों से भी अधिक समय तक (यदि हम समूचे विश्व को ध्यान में रखें) सामाजिक और आर्थिक असमानता तथा एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण सभी सभ्य समाजों की मुख्य विशेषता रही है। राज्य का रूप चाहे जो भी रहा हो, उसका उपयोग असमानता और शोषण को बरकरार रखने के लिए किया जाता रहा है। रूसी क्रांति का लक्ष्य असमानता और शोषण को समाप्त करना तथा ऐसे समाज की रचना करना था जिसमें कोई भी व्यक्ति दूसरे के श्रम पर मौज न कर सके। शांति और भूमि संबंधी आज्ञा पत्रों की चर्चा हम पहले कर चुके हैं इसके तत्काल बाद रूस में सारे उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।रूसी जनता के अधिकारों का एक घोषणा पत्र भी जारी किया गया था। इसमें रूसी साम्राज्य में रहने वाली गैर रूसी जातियों के दमन को समाप्त करने की घोषणा की गई थी। इसमें सभी जातियों के आत्म निर्णय के अधिकार, समानता और संप्रभुत्ता की भी घोषणा की गई थी। जार की सरकार ने जितने गुप्त समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे, उन सारे समझौतों को निरस्त कर दिया गया तथा औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने के लिए पूरब के लोगों का आह्वान किया गया। जनवरी 1918 में रूस को ‘रूसी सोवियत संघात्मक गणतंत्र‘ घोषित किया गया। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तब तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के समस्त भूभाग पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। एस्टोनिया, जाटिविया और निथुआनिया स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आए थे। इन पर बोल्शेविकों का नियंत्रण नहीं था। पोलेण्ड भी स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा और इसमें वह समूचा पोलिश भूभाग शामिल कर लिया गया, जो पहले रूसी साम्राज्य का हिस्सा था। इसी बीच रूस में गृह युद्ध शुरू हो गया और इसके साथ विदेशी सैनिक हस्तक्षेप भी शुरू हो गया। भूमि और गैर रूसी जातियों के प्रति सोवियत नीति के कारण गोरे रूसियों और उनके विदेशी समर्थकों के लिए कुछ कर पाना असंभव हो गया। जो लोग रूस में पुरानी व्यवस्था को वापस लाना चाहते थे, उनको रूसी जनता या गैर रूसी जातियों का समर्थन नहीं मिल पाया और 1920 के दशक के समाप्त होते रूस में गृह युद्ध और विदेशी हस्तक्षेप का अंत कर दिया गया था। रूस में हस्तक्षेप के लिए जिन देशों की सेनाएँ भेजी गई थीं, उन देशों की जनता ने इसका विरोध किया। रूस में विदेशी सैनिक हस्तक्षेप को खत्म करने में जनता द्वारा विरोध की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी। प्रथम विश्व युद्ध और क्रांति के तत्काल बाद के गृह युद्ध तथा विदेशी सैनिक हस्तक्षेप से रूस की अर्थव्यवस्था एक दम तहस-नहस हो गई थी। इसके बाद वहाँ भयंकर अकाल पड़ा जिसमें लाखों लोग मौत के मुहँ में चले गए। 1921 में औद्योगिक उत्पादन 1914 के पहले के उत्पादन से भी 13 प्रतिशत नीचे आ गया। व्यवस्था को पूरी तरह ढहने से बचाने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए उसे ‘युद्ध साम्यवाद‘ (वार कम्युनिज्म) के नाम से जाना जाता है। भूस्वामियों से छीन कर जमीन किसानों में बाँट दी गई थी। लेकिन किसानों ने जो कुछ उपजाया था, उनकी उपज की न्यूनतम जरूरत की मात्रा को छोड़कर बाकी सारा अन्न शेष जनता के उपभोग के लिए सरकार ने उनसे वसूल लिया। कुछ भी खरीदा या बेचा नहीं जा सका। कारखानों में जो कुछ पैदा किया गया था उसे मजदूरों तथा अन्य लोगों में उनकी न्यूनतम आवश्यक जरूरतें पूरी करने के लिए मजदूरी के बदले बाँट दिया जाता था। युद्ध, गृह युद्ध और विदेशी हस्तक्षेप से पैदा हुई स्थितियों में जीवन रक्षा के लिए ये उपाय बहुत जरूरी थे। लेकिन इन उपायों से व्यापक असंतोष पैदा हुआ और कहीं-कहीं तो लोगों ने विद्रोह भी किए। 1921 में एक नई नीति अपनाई गई जिसे ‘नई आर्थिक नीति‘ कहा जाता है। ‘युद्ध साम्यवाद‘ के अंतर्गत उठाए गए कदमों को वापस ले लिया गया। किसानों की उपज पर उनका नियंत्रण वापस कर दिया गया और वेतन का नगद भुगतान किया जाने लगा। माल का व्यापार आरंभ हो गया और अर्थव्यवस्था को फिर से स्थापित करने के प्रयास किए गए। कुछ उद्योगों से निजी प्रबंध की भी छूट दी गई तथा कई छोटे मोटे उद्योगों को निजी स्वामित्व में चलाने की अनुमति दी गई। काफी बड़ी संख्या में सहकारी संघ स्थापित किए गए। 1921 में देश के बहुत बड़े हिस्से में फसल नष्ट हो गई। इसकी वजह से बड़े पैमाने पर भुखमरी की नौबत आ गई। बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पर राहत के लिए प्रयास शुरू किया गया। दूसरे कई देशों के लोगों ने सोवियत जनता की मदद के लिए राहत कार्यक्रम आयोजित किए। संयुक्त राज्य अमरीका ने सरकार को मान्यता तो नहीं दी लेकिन राहत के लिए भोजन सामग्री अवश्य भेजी। नई आर्थिक नीति से अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ और इस सुधार से वह युद्ध पूर्व की स्थिति तक पहुँच गई। इससे भावी विकास की नींव पड़ी। यह नीति 1928 तक चालू रही, जब एक के बाद एक पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए आर्थिक विकास को उच्च स्तर तक ले जाने के लिए जबर्दस्त कोशिश शुरू की गई और दूसरी 1934 में। जिस समय दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, उस समय तक सोवियत रूस (सोवियत समाजवादी गणतंत्र का 1924 से एक हिस्सा) सशक्त औद्योगीकृत सैनिक ताकत बन चुका था। कोई दूसरा देश इतनी जल्दी उद्योग प्रधान नहीं बन पाया था जितनी जल्दी सोवियत समाजवादी गणराज्य बना था। जिन स्थितियों में सोवियत रूस की अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, वे स्थितियाँ दूसरे देशों की स्थितियों से बहुत भिन्न थी। विकास का काम सोवियत संघ ने अपने आंतरिक साधनों को जुटाकर किया था। इसका संगठन-संयोजन राज्य की ओर से किया गया था और इस पर स्वामित्व भी राज्य का ही था। नई आर्थिक नीति के जमाने में जो भी निजी उद्यम मौजूद थे, उनको भी राज्य ने अपने हाथ में ले लिया था और उद्योग तथा व्यापार पर से निजी नियंत्रण एकदम हटा दिया गया था। यह बात ध्यान देने लायक है कि सोवियत संघ अकेला देश था जिस पर अमरीकी महामंदी का कोई असर नहीं पड़ा था। कृषि क्षेत्र में काफी परिवर्तन किए गए थे। मशीनों और ट्रैक्टरों के जरिए खेती के आधुनिकीकरण का जब प्रयास चल रहा था तब मानवीय दृष्टि से इसके काफी विनाशकारी नतीजे सामने आए थे। राज्य (सरकार) ने बड़े-बड़े फार्म स्थापित किए तथा खेती की बाकी जमीन को सामूहिक बनाया गया। किसानों की छोटी-छोटी व्यक्तिगत जोतों को सामूहिक रूप दिया गया और सामूहिक कृषि फार्म स्थापित किए गए। इस तरह के कृषि फार्मों को रूसी भाषा में कोल्खोजेज कहा जाता था। 1930 के दशक में तकरीबन सारी जमीन सामूहिक फार्म के अंतर्गत आ चुकी थी। इन फार्मों पर किसान लोग सामूहिक रूप से काम करते थे। इसके लिए सरकार को जोर जबर्दस्ती का अक्सर सहारा लेना पड़ा था। संपन्न किसानों का वर्ग पूरी तरह खत्म हो चुका था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि कृषि के सामूहिकीकरण के दौरान बहुत से किसान नष्ट हो गए। 1924 में नए संविधान की घोषणा की गई। इस नए संविधान के अनुसार सभी सोवियत गणराज्य जैसे रूस, जॉर्जिया, अर्मेनिया, तुर्कमेन, यूक्रेन, अज़रबैज़ान, कॉकेसिया आदि को एक संघ के अंतर्गत लाया गया। इसे सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ कहा गया। 1936 में जब दूसरा संविधान लागू हुआ तो कुल राज्यों की संख्या 11 थी। इन्हीं को मिलाकर सोवियत संघ की रचना हुई थी। सभी जातियों (नेशनलिटीज) और सभी राष्ट्रों की बराबरी के सिद्धांतों के आधार पर इन गणराज्यों का गठन किया गया था। संविधान के मुताबिक वे संघ से अलग होने के लिए भी स्वतंत्र थे। यदि मोटे तौर पर कहा जाए तो भूतपूर्व रूसी साम्राज्य की हर जाति अपनी भाषा और संस्कृति का विकास करने के लिए स्वतंत्र थी। एशिया के दूसरे देशों के लोगों के लिए सोवियत रूस के एशियाई गणराज्यों का सांस्कृतिक और आर्थिक विकास विशेष रूप से प्रभावशाली था। खास तौर पर उन देशों के लिए जो उपनिवेशवादी शासन से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहे थे। राजनीतिक परिवर्तन के बाद सोवियत संघ में जनता की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों की जबर्दस्त अवहेलना की गई। क्रांति के लिए चलाए गए संघर्ष के दौरान बनाई गई सोवियतों (पंचायतें) को ही लोकतंत्र का सच्चा और प्रामाणिक रूप घोषित किया गया था। ये सोवियतें निर्णय की प्रक्रिया में जनता के विशाल समूह को शामिल करती थीं। उनके जीवन पर इसका असर पड़ा और इसके कारण लाखों लोग सक्रिय राजनीति में भागीदार बने। इन सोवियतों के भीतर कई राजनीतिक दलों और गुटों का प्रतिनिधित्व था जैसे इसमें मैनशेविक दल के और समाजवादी क्रांतिकारी दल के लोग भी शामिल थे। गृह युद्ध और विद्रोह करने के प्रयास के दौरान इन लोगों को देश के राजनीतिक जीवन से अलग कर दिया गया। इन दलों के ज्यादातर नेता या तो देश छोड़ गए या उनको साइबेरिया में निर्वासित कर दिया गया। यहाँ तक कि जब क्रांति को संघटित कर दिया गया था और प्रतिक्रांति के सफल होने की कोई भी संभावना नहीं थी, तब भी देश के राजनीतिक जीवन में उन्हें किसी प्रकार की भूमिका अदा करने की इजाजत नहीं दी गई। बोल्शेविक पार्टी देश की एकमात्र राजनीतिक पार्टी रह गई जिसे बाद में चल कर कम्युनिस्ट पार्टी नाम दिया गया। देश पर इस राजनीतिक पार्टी का अकेला नियंत्रण कायम हो गया। यहाँ तक कि इस पार्टी के अंदर भी धीरे-धीरे सभी तरह की लोकतांत्रिक स्थितियाँ समाप्त हो गईं। निरंकुश जारशाही के अंतर्गत बोल्शेविक पार्टी का विकास हुआ था जिसमें कानूनी रूप में खुले तौर पर उसके लिए काम करना असंभव था। राजनीतिक पार्टी के रूप में बोल्शेविक पार्टी मौजूदा व्यवस्था को क्रांतिकारी ढंग से उखाड़ फेंकने के लिए काम कर रही थी। इस दौरान इसने काम करने के कुछ खास तौर तरीके विकसित कर लिए थे जिसमें बहस मुबाहिसे और वादविवाद की छूट थी, कभी-कभी ये विवाद पार्टी के भीतर काफी तीखे और गंभीर रूप भी धारण कर लेते थे लेकिन एक बार सदस्यों का बहुमत जो निर्णय लेता था, उसको अनिवार्य रूप से सबको मानना पड़ता था। रूसी क्रांति के महानायक लेनिन जब तक जीवित रहे, पार्टी के काम करने का यह तौर तरीका भी बरकरार रहा। कई अवसरों पर दूसरे कम्युनिस्ट नेताओं ने लेनिन के दृष्टिकोणों का खुल्लम खुल्ला विरोध भी किया और कुछ उदाहरण तो ऐसे भी मौजूद हैं, जब इस प्रकार की बहस में लेनिन अकेले पड़ गए थे। लेनिन इन मतभेदों को व्यक्त करने के कारण या बहुमत से अथवा नेता के दृष्टिकोण से भिन्न विचार रखने वालों का कभी दमन नहीं किया गया। इस प्रकार पार्टी के अंदर लोकतंत्र बरकरार रखा जाता था। 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद पार्टी के अंतर्गत नेतृत्व पर कब्जा करने के लिए तीव्र संघर्ष हुआ। इन मुद्दों पर गंभीर मतभेद थे कि समाजवाद के निर्णय के लिए क्या तरीके अपनाए जाएँ और किन साधनों का उपयोग किया जाए। क्या एक ही देश में समाजवाद की रचना संभव थी और क्या सोवियत सरकार का प्रारंभिक काम दुनिया में क्रांतियों को बढ़ावा देना होना चाहिए, खेती को सामूहिक फार्मों में रूपांतर तथा औद्योगीकरण के तौरतरीकों पर भी विवाद था। इन मतभेदों को बहुमत द्वारा निर्णय कराकर तथा उस पर आगे अमल करके ही हल नहीं किया गया, बल्कि जिन लोगों ने पार्टी के भीतर इसका विरोध किया था, उनको पार्टी तथा देश का शत्रु मान लिया गया। पार्टी के अंदर पहला मुख्य संघर्ष त्रात्स्की और स्तालिन के बीच हुआ था। स्तालिन पार्टी के महासचिव चुने गए थे। कई लोग ऐसा मानते हैं। कि क्रांति में उसके बाद विदेशी मंत्री के रूप में और उसके बाद युद्ध मंत्री के रूप में लेनिन के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका त्रात्स्की की ही थी लेकिन 1927 में स्तालिन विजयी होकर पार्टी में ऊपर उठे तथा त्रात्स्की को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था तथा 1929 में उनको निर्वासित कर दिया गया। ऐसा कुछ लोगों का विश्वास है कि 1940 में मैक्सिको में किसी के जरिए स्तालिन ने उनकी हत्या करवा दी। यहाँ वे कुछ सालों से रह रहे थे। बाद में अन्य कई नेताओं पर भी त्रात्स्कीवादी होने का आरोप लगाया गया, उनको कैद किया गया और सजा दी गई। स्तालिन की नीतियों से कई अवसरों पर दो अन्य नेताओं-जिनोविएव तथा बुखारिन-के भी मतभेद हुए। इनको भी, ऐसा माना जाता है, रास्ते से अलग कर दिया गया। धीरे-धीरे 1930 में जो देश नए प्रकार के समाज की और नई सभ्यता की रचना कर रहा था, जो हर प्रकार के शोषण से मुक्त होती, उसने एक व्यक्ति की तानाशाही का रूप ले लिया। सारी शक्ति स्तालिन के हाथ में केंद्रित हो गई जिसको सब तरह के विवेक और समझदारी का स्रोत माना जाता था। उसके निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता था। समाजवादी विचारों के विकास में समाजवादी निर्माण की एक मंजिल के रूप में सर्वहारा के अधिनायकत्व की परिकल्पना की गई थी। माना गया कि सभी पूँजीवादी देशों में बुर्जुआ वर्ग की तानाशाही कायम है यद्यपि इन देशों में लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्थाएँ मौजूद थीं। इसका कारण यह बताया गया कि इन देशों की सरकारें बुर्जुआ वर्ग के प्रभुत्व को बनाए रखने का उपकरण हैं। उसी प्रकार यह भी मान लिया गया कि सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व भी मजदूर वर्ग का प्रभुत्व बनाए रखने के लिए राजसत्ता का इस्तेमाल करेगा। इस अधिनायकत्व का अर्थ यह कतई नहीं था कि राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं होगी, सभी राजनीतिक दलों को समाप्त कर दिया जाएगा तथा केवल एक पार्टी का शासन कायम रहेगा। बहरहाल जिस तरीके से सोवियत संघ की राजनीतिक प्रणाली का विकास हुआ, उसका इस प्रकार अर्थ किया गया - पहले पार्टी का अधिनायकत्व और चूँकि पार्टी पर स्तालिन का नियंत्रण था, इसलिए स्तालिन का अधिनायकत्व। 1953 में स्तालिन की मृत्यु के बाद इस पूरी परिघटना को सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकांश नेताओं ने स्तालिन की ‘व्यक्ति पूजा‘ की संज्ञा दी। सोवियत संघ में समाजवाद के निर्माण में स्तालिन की ‘व्यक्ति पूजा‘ या तानाशाही के कारण भंयकर खामियाँ पैदा हुईं। 1934 में लेनिनग्राद (पहले इसका नाम पेट्रोग्राद था) में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता किरोव की हत्या कर दी गई। अब लोगों का आमतौर पर मानना है कि इसमें स्तालिन का हाथ था। बहरहाल ऐसे हर एक के विरूद्ध दमन-अभियान चलाने के लिए स्तालिन ने इस हत्या का उपयोग किया, जिसकी वफादारी पर थोड़ा बहुत भी शक था। जल्दी ही इसने जो रूप धारण किया उसको ‘ग्रेट पर्ज‘ (महान सफाई अभियान) नाम से जाना जाता है। इस महान सफाई अभियान के दौरान नष्ट हुए लोगों की संख्या के बारे में लोगों ने अब अनुमान लगाना प्रारंभ किया है। यह संख्या काफी ज्यादा थी। इनमें कई तरह के लोग शामिल थे, जैसे कुछ काफी बड़े कम्युनिस्ट नेता, क्रांति के कुछ बड़े सेनानी, लेखक, कलाकार, वैज्ञानिक, सैनिक तथा नागरिक सेवा के अधिकारी तथा दूसरे देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों के कुछ नेता आदि। लंबे अर्से तक सोवियत रूस के बाहर समाजवाद से सहानुभूति रखने वाले लोग अपने-अपने देश में उपनिवेशवादी शासन अथवा पूँजीवादी शोषण के विरूद्ध संघर्ष चलाने में व्यस्त थे इसलिए समाजवाद के नाम पर किए जाने वाले इन अपराधों की भयंकरता का उनको एहसास नहीं हो पाया था। इसका एक कारण तो यह था कि सोवियत संघ चारों तरफ से ऐसे देशों से घिरा हुआ था जो सोवियत संघ और समाजवाद, दोनों के ही खिलाफ किलाबंदी किए हुए थे। इनमें से कुछ देशों की सोवियत संघ खिलाफ आक्रामक मंशा जगजाहिर थी और इन देशों ने घोषणा की थी कि वे कम्युनिज्म (साम्यवाद) को नष्ट करके ही दम लेंगे। इनमें से अधिकांश देशों ने कई अन्य देशों पर अपना उपनिवेशवादी शासन कायम कर रखा था। इन देशों की अर्थव्यवस्था से असमानता पैदा हुई जिससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, अभाव और गरीबी फैली। सोवियत संघ के भीतर जो दमन हुआ था उसे लोगों ने दूसरे संदर्भ में देखा। लोगों ने माना कि चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ सोवियत संघ अपनी समाजवादी व्यवस्था तथा स्वतंत्रता की रक्षा करने की कोशिश में यह सब कर रहा है। सोवियत संघ विश्व रंग मंच पर अपनी अंतर्राष्ट्रीय भूमिका के कारण उस समय की तमाम बड़ी ताकतों में अलग दिखाई पड़ता था। केंद्रीय शक्तियों के साथ युद्ध के उपरांत पेरिस में शांति संधि का प्रारूप तैयार करते समय उसे अलग रखा गया था। 1921 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान और ईरान के साथ एक समझौता किया। इस समझौते का उद्देश्य इन देशों की स्वतंत्रता और संप्रभुता को सुदृढ़ करना था। मुस्तफा कमाल की सरकार अपने देश (टर्की) के भू-भाग की अखंडता को बहाल करने के लिए लड़ रही थी। रूस ने कई निःशस्त्रीकरण सम्मेलनों में भाग लिया और आम तथा समग्र का प्रस्ताव रखा। 1930 के दशक में उसने फासीवादी देशों द्वारा किए गए हमलों का खुलकर विरोध किया और फासीवादी हमलों को रोकने के लिए दूसरे देशों के साथ संयुक्त कार्रवाई का प्रयास किया। बहरहाल अधिकांश पश्चिमी देशों ने इस उम्मीद से फासीवाद को खुश करने की नीति अपनाई कि फासीवाद साम्यवाद को नष्ट कर देगा। 1934 में सोवियत संघ, राष्ट्र संघ (तीन ऑफ नेशंस) का सदस्य बना। उसने इस बात की पूरी कोशिश की कि राष्ट्रों की स्वतंत्रता और शांति को बनाए रखने के लिए राष्ट्र संघ दृढ़ता से कार्रवाई करे। विश्व की प्रमुख शक्तियों में सोवियत संघ ऐसी अकेली ताकत था जो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद बरकरार रखने का हर तरह से विरोधी था। सोवियत संघ अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत विश्व की तमाम जनता का मित्र समझा जाता था। यहाँ पर कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय की स्थापना की चर्चा प्रासंगिक और उचित जान पड़ती है। एक प्रकार से यह रूसी क्रांति का परिणाम था। युद्ध प्रारंभ होने के साथ ही ‘दूसरा अंतर्राष्ट्रीय‘ (दि सेकण्ड इण्टरनेशनल) खत्म हो चुका था। युद्ध के दौरान विभिन्न देशों की समाजवादी पार्टियों के कुछ हिस्सों को एकजुट करने के लिए कुछ कोशिशें हुईं। रूसी क्रांति के बाद कई देशों में समाजवादी पार्टियों के बाएँ बाजू के कुछ लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टियाँ गठित कीं। सभी कम्युनिस्ट पार्टियों को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन में लाने के लिए प्रयास प्रारंभ किया गया। मार्च 1919 में मास्को में एक अधिवेशन हुआ। इसमें तीस देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अधिवेशन में कोमिनटर्न (कम्युनिस्ट इण्टरनेशनल का संक्षिप्त रूप) अथवा तीसरे अंतर्राष्ट्रीय का गठन किया गया। 1930 के दशक के मध्य तक साठ से भी अधिक देशों में कम्युनिस्ट पार्टियाँ गठित हो चुकी थीं। इनमें से कुछ तो काफी ताकतवर थीं जैसे जर्मनी की कम्युनिस्ट पार्टी। यह पार्टी हिटलर के सत्ता में आने के पहले काफी शक्तिशाली थी। हिटलर ने इसको खत्म करने के लिए सुनियोजित अभियान चलाया था। इसी तरह फ्रांस की कम्युनिस्ट पार्टी भी बहुत शक्तिशाली थी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी काफी ताकतवर होकर सामने आई थी। पूँजीवादी देशों के मजदूरों में और उपनिवेशों में कम्युनिस्ट पार्टियों ने अपने लिए समर्थन का काफी शक्तिशाली आधार तैयार किया था। महामंदी के दौर में लगभग सभी देशों में पूँजीवादी प्रणाली द्वारा उत्पन्न की गई मुसीबतों के विरूद्ध मजदूरों को संगठित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उपनिवेशवादी शासन वाले कुछ देशों में स्वतंत्रता संग्राम में ये अग्रणी शक्ति के रूप में सामने आए। सभी देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन सोवियत रूप की क्रांति के प्रभाव में हुआ था, इसलिए बहुत सी कम्युनिस्ट पार्टियाँ सोवियत रूस की कम्युनिस्ट पार्टी को अपना आदर्श मानती थीं और अक्सर विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन की मुख्य शक्ति के रूप में उसकी तरफ देखती थीं। रूस की बोल्शेविक क्रांति भी अक्सर समाजवादी क्रांति का नमूना समझी जाती थी। सोवियत रूस की कम्युनिस्ट पार्टी से अपने घनिष्ट संबंधों के कारण, दूसरे लोग सभी कम्युनिस्ट पार्टियों को शक की निगाह से देखते थे। कोमिनटर्न का मुख्यालय मास्को में था, इसलिए इस पर सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था और दूसरे देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों की गतिविधियों को मास्को द्वारा निर्देशित समझा जाता था। कम्युनिस्ट पार्टियों तथा कोमिनटर्न के गठन से समाजवाद के लिए क्रांतिकारी आंदोलनों को शक्ति मिली। लेकिन समाजवादी आंदोलन को यदि हम सामजिक परिवर्तन के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो समाजवादी आंदोलन में कमजोर तत्व भी नजर आएँगे। कम्युनिस्ट पार्टियों में कई प्रकार के मतभेद थे लेकिन सहमति और कार्रवाई के समान मुद्दे खोजने की जगह ये पार्टियाँ एक दूसरे को अपना शत्रु समझने लगीं। जर्मनी की कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के बीच दरार ने नाजियों के लिए सत्ता में आने का रास्ता आसान बना दिया। यह सिर्फ समाजवाद और लोकतंत्र के लिए घातक नहीं साबित हुआ, बल्कि विश्वशांति के लिए भी विनाशकारी साबित हुआ। 1935 में बल्गेरिया के कम्युनिस्ट नेता ज्यार्जी दिमित्रोव के नेतृत्व में कोमिनटर्न ने अपनी सातवीं बैठक में फासीवाद के विरूद्ध लोकप्रिय संयुक्त मोर्चा बनाने का आह्वान किया तथा उपनिवेशों में साम्राज्यवाद विरोधी संयुक्त मोर्चा बनाने की अपील की। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। इसने समान उद्देश्यों को पाने में जनता के बड़े समूह को एक्यबद्ध करने में मदद दी जिनमें कम्युनिस्ट, समाजवादी और अन्य लोग थे। इस नीति के कारण जो लोकप्रिय मोर्चे खोले गए थे, उन्होंने कुछ देशों में सत्ता पर कब्जा करने से फासीवादियों को रोका। इस बीच विश्व एक बार पुनः युद्ध में लौटने की स्थिति में पहुँच गया। जापानउन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में अपने आधुनिकीकरण के आरंभिक समय से ही विस्तार के लिए अभियान चलाना जापानी इतिहास की प्रमुख विशेषता रही है। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में उसे मिले औपनिवेशिक लाभों की चर्चा पहले की जा चुकी है। उसने वाशिंगटन में अपनी नौसैनिक शक्ति को सीमित रखने वाली एक संधि पर हस्ताक्षर किए लेकिन इस नौसैनिक परिसीमन संधि के बाद भी वह प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी नौसैनिक ताकत बना रहा। कुछ समय तक आर्थिक माध्यमों से चीन दक्षिण-पूर्व एशिया में अपने प्रभुत्व विस्तार के लिए शांतिपूर्ण तरीकों से कोशिश करता रहा। लेकिन चीन के राष्ट्रीय एकीकरण के लिए आंदोलन के विकास तथा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभाव के कारण खतरा पैदा हो गया और उसे लगने लगा कि संभव है कि वह चीन पर अपना नियंत्रण न बढ़ा सके। चीन के राष्ट्रीय एकीकरण को रोकना उसके उद्देश्यों में से मुख्य उद्देश्य था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पहला बड़ा आक्रमण जापान ने किया और उसने मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। बाद में यहाँ उसने एक कठपुतली सरकार स्थापित कराई। इसके बाद 1937 में जापान ने चीन पर जबरदस्त आक्रमण किया। 1936 में जर्मनी के साथ जापान ने कोमिनटर्न-विरोधी संधि पर हस्ताक्षर किए। उसने संपूर्ण एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र पर प्रभुत्व कायम करने की वैसी ही योजना बनाई जैसी योजना जर्मनी और इटली ने मिलकर बाकी दुनिया पर प्रभुत्व स्थापित करने की बनाई थी।युद्ध के बाद जापान की अर्थव्यवस्था संवृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ती रही तथा सूती कपड़े, रेयन तथा कच्चे सिल्क का वह सबसे बड़ा निर्यातक देश हो गया। भोजन सामग्री, कलपुर्जों तथा कच्चे माल के लिए दूसरे देशों पर उसकी निर्भरता के चलते उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया था। उनमें से कुछ समस्याओं पर काबू पाने के लिए लोहा, इस्पात और भारी इंजीनियरिंग उद्योग का काफी अधिक विस्तार किया गया। लेकिन जापान के उद्योगपतियों तथा राजनीतिक और सैनिक नेताओं ने चीन तथा अन्य देशों के संसाधनों और बाजार पर सीधे प्रभुत्व को जरूरी माना। मजदूरों का भयानक तरीके से शोषण करके ही जापान का औद्योगिक विस्तार किया गया था। जापान का औद्योगिक विस्तार किया गया था। उद्योग और बैंक ‘जैबात्सु‘ के प्रभाव में थे, यह पैसे वालों का एक छोटा सा गुट था। जापान की सरकार और उसके राजनीतिज्ञों से ‘जैबास्तु‘ के घनिष्ठ संबंध थे। मजदूर बहुत दयनीय जिंदगी जी रहे थे। किसान भी इनसे अच्छी हालत में नहीं थे। इनमें से अधिकांश किसान बहुत छोटी जोतों के मालिक थे। जो एक एकड़ से नाममात्र को ज्यादा थी। किसानों की बहुत बड़ी संख्या किराए पर जमीन लेकर जोतती थी। जापान की बढ़ती हुई आबादी की जरूरतें पूरी करने में वहाँ की कृषि व्यवस्था असमर्थ थी। वह भोजन की भी आवश्यकता को पूरी नहीं कर सकती थी। देश में काफी व्यापक असंतोष था। चावल की ऊँची कीमतों के कारण 1919 में समूचे जापान में खलबली मची हुई थी क्योंकि मजदूरी इतनी कम मिलती थी कि आम आदमी चावल खरीदने की स्थिति में नहीं था। इस खलबली को ‘चावल विद्रोह‘ कहा जाता है। कारखानों, अमीरों के घरों तथा चावल व्यापारियों की दुकानों पर लोगों ने हमले किए और उनमें आग लगा दी। 1920 के दशक में जापान में चारों तरफ हड़तालों की लहर उठी और इस दौरान मजदूरों की यूनियनें ताकतवर बनीं। कम्युनिस्ट और सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टियाँ गठित की गई और दमनकारी अर्थव्यवस्था के खिलाफ मजदूरों और किसानों को संगठित करने का उन्होंने प्रयास किया। इन पार्टियों ने साम्राज्यवादी नीतियों और युद्ध के खिलाफ भी जापानी जनता में चेतना जगाने की कोशिश की। बहरहाल, इन पार्टियों, मजदूर युनियनों और किसान संगठनों को अत्यंत बेरहमी से कुचल दिया गया। 1925 में खतरनाक विचारों के दमन के लिए ‘शांति संरक्षण कानून‘ पारित किया गया। इस कानून के अनुसार ऐसे हर आदमी को गिरफ्तार किया जा सकता था जो ऐसा संगठन बनाता है अथवा उसका सदस्य बनता है, जो संगठन सरकार के ढाँचे में परिवर्तन की वकालत करता है या व्यक्तिगत संपत्ति के उन्मूलन की बात करता है। यहाँ तक कि इन सवालों या अन्य राजनीतिक समस्याओं पर अकादमिक विचार विमर्श करने पर भी प्रतिबंध था। 1920 के दशक में लगता था कि संसदीय प्रणाली की सरकार कायम करने की दिशा में जापान कुछ प्रगति कर रहा है। 1924 में सभी पुरूष नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया गया लेकिन महिलाएँ पहले की तरह मतदान के अधिकार से वंचित रखी गईं। कुछ समय तक ऐसा लगा कि सरकार नागरिक प्रशासकों के अंतर्गत काम कर रही है। बहरहाल, देश के नागरिक जीवन में सेना की भूमिका का महत्व बरकरार रहा और वह मुख्य शक्ति बनी रही तथा 1930 के दशक के शुरूआती दौर में सरकार में इसका दबदबा बढ़ता गया। यहाँ तक कि जब सेना का सरकार में वर्चस्व नहीं था तब भी वह सरकार का खुले आम विरोध करती रहती थी तथा इसको नियंत्रित करने के लिए सरकार कुछ नहीं कर पाती थी। जापानी समाज में जापानी सेना सबसे ज्यादा आक्रामक ताकत थी। जापान में कुछ गुप्त संगठन बने थे और जापानी सेना का इन संगठनों से घनिष्ठ संपर्क था। ये सारे संगठन उदारवाद, शांतिवाद और लोकतंत्र का विरोध करते थे और संकीर्ण तथा आक्रामक राष्ट्रवाद, जापानी सांस्कृतिक श्रेष्ठता और विदेशी प्रभाव से जापानी संस्कृति की शुद्धता की रक्षा करने जैसे विचारों की हिमायत करते थे। शांति, सामाजवाद और लोकतंत्र संबंधी विचारों को विदेशी माना जाता था और यह भी कहा जाता था कि इन विचारों से जापान को बचाना है। जापानी राष्ट्रीयता के सारतत्व के बारे में इन संगठनों के खास तरह के विचार थे। सम्राट की पूजा इन सबके विचारों में समानता का तत्व था। वे इस बात को अक्सर प्रचारित करते थे कि ‘सम्राट के लिए मरना अमरत्व प्राप्त करना‘ है। इनके अपने शस्त्रधारी गुट थे जो राजनीतिक हत्याएँ करते थे। जापान की सेना और अनेक राजनीतिक नेताओं की विचार धारा का आधार मोटे तौर पर इन गुप्त संगठनों की विचारधारा के प्रभाव में निर्मित हुआ था। कम्युनिस्टों और सोशल डेमोक्रेट लोगों के अलावा सभी राजनीतिक शक्तियाँ जापान के साम्राज्यवादी विस्तार को अपना वांछनीय उद्देश्य मानती थीं। दो युद्धों के बीच जापान सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण कम्युनिस्ट तथा सोशल डेमोक्रेट एकदम महत्वहीन स्थिति में चले गए थे। जापान में जिस राजनीतिक प्रणाली का आविर्भाव हुआ, उसे ‘‘सैनिक फासीवाद‘‘ कहा जा सकता है। इसलिए जर्मनी और इटली की फासीवादी सरकारों के साथ इसकी निकटता का बढ़ना स्वाभाविक था। 1926 में सम्राट हिरोहितो जापान के सिंहासन के उत्तराधिकारी बने। 1868 में जिस सम्राट के शासन में जापान का आधुनिकीकरण शुरू हुआ था, उसे ‘मेजी‘ नाम से जाना जाता था। जापानी भाषा में मेजी का मतलब होता है, ‘प्रबुद्ध सरकार‘। सम्राट हिरोहितो ने अपने शासन के लिए ‘शोवा‘ उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है, ‘प्रबुद्ध शांति‘। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीकाएशियादो युद्धों के बीच की अवधि में एशिया के हर देश में राष्ट्रवादी आंदोलन का विकास हुआ। भारत के स्वाधीनता आंदोलन का आप विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। इस दौर में उस आंदोलन ने नए चरण में प्रवेश किया। जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, साम्राज्यवाद विरोधी जन आंदोलन का चरण आरंभ हो गया। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियाँवाला बाग में ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने नृशंस नरसंहार का खेल खेला। इसके तत्काल बाद असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। लाखों की संख्या में आम लोग स्वतंत्रता आंदोलन की ओर आकर्षित हुए जिसमें किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएँ और भारतीय समाज के हर हिस्से के लोग शामिल थे। असंख्य भारतीय लोगों के लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद को चुनौती देना एक पवित्र आदर्श बन गया। 1929 के अंत तक ‘पूर्ण स्वराज्य‘ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य बन गया। कांग्रेस ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। 1930 में एक बहुत व्यापक जन आंदोलन शुरू किया गया और लाखों की संख्या में भारतीय जनता ने ब्रिटिश कानून तोड़ा और जेल गई। संघर्ष के दौरान ही नए भारत की परिकल्पना का विकास हुआ। यह परिकल्पना स्वतंत्रता संग्राम का ही एक हिस्सा थी। इसमें स्वतंत्र, लोकतांत्रिक धर्म निरपेक्ष और समतावादी भारत का स्वप्न नीहित था। भारत के कुछ क्षेत्रों में ब्रिटिश हुकूमत की मदद से राजा-महाराजाओं का शासन चला करता था। यह आंदोलन इन क्षेत्रों में भी फैला। यूरोपीय देशों के फासीवादी विरोधी आंदोलनों तथा दूसरे उपनिवेशों के स्वतंत्रता आंदोलनों के साथ भी भारतीय मुक्ति संग्राम का निकट संपर्क कायम हुआ। धीरे-धीरे लोगों में यह विश्वास बढ़ने लगा कि भारतीय समाज की पुनर्रचना के लिए देश की राजनीतिक आजादी एक जरूरी पूर्व शर्त है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही यह बात भी तय हो गई कि स्वतंत्र होने के बाद विश्व की गतिविधियों में भारत की भूमिका की रूपरेखा क्या होगी। विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए जनता का इस्तेमाल स्वतंत्रता आंदोलन का तात्कालिक और आधारभूत कार्य था लेकिन इसके साथ ही आंदोलन के सूत्रधारों ने सामाजिक और आर्थिक पुनर्रचना और आधुनिक राष्ट्र के निर्माण पर भी सोचा।चीनचीन की 1911 की क्रांति में सन यात-सेन की भूमिका की चर्चा पहले की जा चुकी है। इस क्रांति के परिणामस्वरूप चीन को गणतंत्र घोषित किया गया। इस बात की भी चर्चा की गई है कि युयान सिह-काई ने किस प्रकार सत्ता हथियाई थी जो सम्राट बनने का स्वप्न देख रहा था। चीन के विभिन्न क्षेत्रों पर युद्ध सरदारों का शासन था। ये सरदार आधिपत्य के लिए आपस में लड़ते रहते थे। ये तमाम विदेशी शक्तियों को तरह-तरह की सुविधाएँ दिया करते थे और बदले में इनको उन लोगों का समर्थन मिला करता था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के समय चीन में दो प्रमुख सरकारें थीं। इनमें से एक पर कोमिनतांग का आधिपत्य था तथा इस सरकार का मुख्यालय कैंटन में था। इस सरकार के राष्ट्रपति डॉ. सन यात-सेन हुए थे। दूसरी सरकार का शासनाध्यक्ष एक सैनिक जनरल था और उसका मुख्यालय बीजिंग में था। 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन में तय किया गया कि शांतुंग को जापान के हवाले कर दिया जाए। इससे साम्राज्यवाद के विरोध में आंदोलन खड़ा हो गया। 4 मई 1919 में बीजिंग विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन से इसका श्री गणेश हुआ। यह आंदोलन ‘चार मई आंदोलन‘ के नाम से विख्यात हुआ। उसके बाद जल्दी ही यह चीन के दूसरे भागों में भी फैल गया। चीनी राष्ट्रवादियों पर रूसी क्रांति का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था, इसके बाद वहाँ आमूल परिवर्तनवादी प्रवृत्तियाँ बढ़ने लगी थीं। 1921 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई और जल्दी ही यह एक प्रमुख शक्ति बन गई। इस बीच चीन को एकीकृत करने में पश्चिमी देशों ने सन यात-सेन को मदद नहीं दी। इसलिए उन्होंने सोवियत संघ से समर्थन माँगा। 1924 में कोमिनटांग और कम्युनिस्ट पार्टी एक दूसरे के निकट आईं। जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ने अलग राजनीतिक दल के रूप में अपना कार्य जारी रखा, वहाँ कम्युनिस्ट लोग भी कोमिनटांग में शामिल हो गए। राष्ट्रीय क्रांतिकारी सेना गठित करने का निर्णय लिया गया। इस काम के लिए सोवियत संघ के सैनिक तथा राजनीतिक सलाहकारों की मदद से एक सैनिक अकादमी स्थापित की गई। 1925 में चीन की राष्ट्रीय क्रांतिकारी सेना ने युद्ध सरदारों के खिलाफ अपना अभियान शुरू किया। लेकिन मार्च 1925 में सन यात-सेन का देहांत हो गया और उसके दो साल बाद चीन की स्थिति में जबरदस्त बदलाव आया। कोमिनटांग और शीघ्र ही चीन में गृह-युद्ध की हालत पैदा हो गई।चीन के राजनीतिक एकीकरण के लिए राष्ट्रीय क्रांतिकारी सेना की कार्रवाई के बाद वहाँ किसानों और मजदूरों का आंदोलन शुरू हो गया। 1925 में शंघाई में मजदूर नेताओं की हत्या के विरोध में हड़तालें और प्रदर्शन हुए। जापान के उद्योगपतियों ने नेताओं को मारने का आयोजन किया था और ब्रिटिश पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई थी। कई इलाकों में किसानों ने भू-स्वामियों की जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। 1927 के मार्च महीने में जब राष्ट्रीय क्रांतिकारी सेना नानकिंग पहुँची, तो संयुक्त राज्य अमरीका और ब्रिटेन के युद्धपोतों ने गोलीबारी की। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इसी समय कोमिनटांग में विभाजन हो गया और राष्ट्रीय क्रांतिकारी सेना के प्रमुख च्यांग काई-शेक ने नानकिंग में अपनी सरकार स्थापित की। वह किसानों और मजदूरों के आंदोलन में वृद्धि और कोमिनटांग के अंदर वामपंथी तत्वों की बढ़ती शक्ति से चौंक गया था। चीन में विदेशी प्रभुत्व की समाप्ति और उसका राजनीतिक एकीकरण उसके लिए कम चिंता के विषय थे, उसके लिए मुख्य चिंता का विषय वामपंथियों तथा कम्युनिस्टों का दमन था। शंघाई में उसकी फौजी टुकड़ियों ने मजदूरों के घरों पर छापे मारे जिसमें हजारों की संख्या में मजदूर और कम्युनिस्ट मारे गए। दिसंबर 1927 में कम्युनिस्टों ने कैंटन में एक विद्रोह का नेतृत्व किया। वहाँ सोवियत रूस की सरकार स्थापित की गई लेकिन यह विद्रोह कुचल दिया गया और लगभग 5,000 मजदूर मारे गए। इससे चीन के राष्ट्रीय आंदोलन में फूट पड़ी। सोवियत सलाहकारों को चीन से बाहर निकाल दिया गया तथा कोमिनटांग के बहुत से नेता (इसमें सन यात-सेन की विधवा पत्नी भी थी) देश से बाहर चले गए। कैंटन के विद्रोह के कुचल दिए जाने के बाद कम्युनिस्ट लोग देश के विभिन्न भागों में फैल गए तथा कुछ इलाकों को अपने नियंत्रण में कर लिया। चीन अब एक लंबे गृह युद्ध के चरण में प्रवेश कर गया। यह युद्ध चीनी कम्युनिस्टों तथा च्यांग काई-शेक की फौजों के बीच चला। जापान द्वारा मंचूरिया पर कब्जा करने के बाद पूरा चीन जापान-विरोधी लहर की चपेट में आ गया और पूरे देश में जापानी माल के बहिष्कार का आंदोलन छिड़ गया। लेकिन जापानी आक्रमण के खिलाफ च्यांग काई-शेक के नेतृत्व में कोमिनटांग और कम्युनिस्ट पार्टी संगठित नहीं हो सके। कम्युनिस्टों ने जापान के विरोध में प्रतिरोध का आह्वान किया लेकिन वे च्यांग काई-शेक के साथ हाथ मिलाने के इच्छुक नहीं थे। जहाँ-जहाँ कम्युनिस्टों की ताकत के गढ़ थे उन पर च्यांग काई-शेक की फौजों ने कार्रवाई की, उनके विरूद्ध अभियान चलाया लेकिन जापान के विरूद्ध उसने कुछ नहीं किया। इस बीच कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव, ग्रामीण इलाकों में विशेष रूप से बढ़ता जा रहा था। इस दौर में माओ जेदोंग (माओ त्से-तुंग) कम्युनिस्ट पार्टी में अत्यंत प्रभावशाली नेता के रूप में उभर रहे थे। उन्होंने इस दृष्टिकोण की वकालत की कि चीन में किसान सबसे बड़ी क्रांतिकारी ताकत हैं और किसानों की मदद से उन्होंने चीन में समाजवादी क्रांति करने की रणनीति तैयार की। 1934 में लाखों की संख्या वाली सेना की मदद से दक्षिण चीन के कम्युनिस्ट के प्रभाव क्षेत्रों पर च्यांग काई-शेक ने आक्रमण किया। कम्युनिस्टों को अपना क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा ताकि उनका सफाया न कर दिया जाए। उनमें से लगभग एक लाख कम्युनिस्ट उत्तर-पश्चिम की ओर येनान क्षेत्र में चले गए। इस आंदोलन को ‘लंबी यात्रा‘ (लांग मार्च) नाम से जाना जाता है। इसमें इन लोगों ने लगभग 10,000 किलोमीटर की यात्रा की। इससे पूरे देश में कम्युनिस्टों की लोकप्रियता बढ़ी। इस लंबी यात्रा के दौरान इन लोगों ने जमींदारों से जमीन छीन कर किसानों में बाँट दी। इस प्रकार च्यांग काई-शेक की सरकार के विरूद्ध उनकी ताकत लगातार बढ़ती चली गई। अब तक लोगों के दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि च्यांग काई-शेक की सरकार बड़े जमींदारों, सौदागरों और सूदखोरों की सरकार है। जापानी आक्रमण के विरूद्ध कम्युनिस्टों ने भी एक राष्ट्रीय युद्ध का आह्वान किया जबकि च्यांग काई-शेक की फौजों के आक्रमण के लक्ष्य केवल कम्युनिस्ट लोग थे। 1937 में चीन पर जापान का भीषण आक्रमण शुरू हुआ। जापानी आक्रमण के सामने च्यांग काई-शेक की सेना टिक नहीं सकी और वह पीछे हट गई। उनकी सरकार का मुख्यालय नानकिंग से हटाकर चंगकिंग ले जाया गया लेकिन इस समय तक जापानी आक्रमण को रोकने के लिए एक संयुक्त मोर्चा गठित किया जा चुका था। 1936 में एक नाटकीय घटना घटी। कम्युनिस्टों के विरूद्ध लड़ने के लिए अपने सैनिकों को समझाने-बुझाने के मकसद से च्यांग काई-शेक सियान गया हुआ था। उसके सैनिकों ने उसको गिरफ्तार कर लिया और उन लोगों ने उसे तब छोड़ा जब वह गृह युद्ध समाप्त करने और जापान के खिलाफ कम्युनिस्टों के साथ संयुक्त मोर्चा बनाने पर राजी हुआ। इसके बाद से जापानी आक्रमण के विरूद्ध प्रतिरोधात्मक राष्ट्रीय युद्ध का दिखावा बरकरार रहा यद्यपि दोनों ही पक्ष च्यांग काई-शेक का कोमिनटांग और माओ जेडोंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट एक दूसरे के प्रति शंकालु बने रहे और अपना-अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में लगे रहे। इस अवधि में जापानी आक्रमण के विरूद्ध चीन के राष्ट्रीय संग्राम में कम्युनिस्ट लोग सच्चे और ईमानदार प्रतिनिधि के रूप में उभरकर सामने आए। कोरियाप्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के एकदम बाद ही कोरिया में जापान के उपनिवेशवादी शासन से मुक्त होने के लिए कोरिया में आंदोलन ताकत पकड़ने लगा। कोरिया में उपनिवेशवाद विरोधी विचरों को फैलाने में रूसी क्रांति से भी मदद मिली। 1918 में कोरिया के राष्ट्रवादियों ने स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का एक प्रारूप तैयार किया। मार्च 1919 में सीओल की एक जन-सभा में इसे पढ़कर सुनाया गया। इसके बाद प्रदर्शन हुए। इनमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। इन प्रदर्शनों ने जल्दी ही देशव्यापी विद्रोह का रूप ले लिया। इसमें डेढ़ लाख से भी अधिक लोगों ने भाग लिया। इस विद्रोह को जापानी फौज ने कुचल दिया। इसमें लगभग 8,000 लोग मौत के मुँह में चले गए और 16,000 लोग घायल हुए। लगभग 50,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बहरहाल किसान विद्रोह और मजदूरों की हड़तालें चलती रहीं। कोरिया में जापान विरोधी संघर्ष को मजबूत बनाने में चीन, जापान, सोवियत संघ और दूसरे देशों में बसे कोरिया के लोगों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी। 1931 के बाद जापान द्वारा मंचूरिया पर कब्जा करने पर कोरिया के लोगों ने मंचूरिया तथा कोरिया में जापान के विरूद्ध सशस्त्र संघर्ष संगठित करना आरंभ किया। जापानियों ने कोरिया को सैनिक कार्रवाई का अड्डा बनाया। यह कार्रवाई पहले चीन के विरूद्ध की गई। उन कोरिया वासियों के संगठन स्थापित करने का उन्होंने प्रयास किया जो उनके प्रति वफादार थे। दूसरे देशों के खिलाफ आक्रमण में भी उन्होंने कोरियाई लोगों का उपयोग किया।दक्षिण-पूर्व एशियाई देशसंयुक्त राज्य अमरीका के औपनिवेशिक शासन के दौरान फिलीपीन्स द्वीपों को संयुक्त राज्य अमरीका का दुमछल्ला बनाकर छोड़ दिया गया था। अपने निर्यात का 80 प्रतिशत यह संयुक्त राज्य अमरीका को भेजता था जिसमें चीनी, नारियल और तंबाकू मुख्य थे और अपने 70 प्रतिशत आयात के लिए यह अमरीका पर निर्भर था। संयुक्त राज्य अमरीका के अधीन उसके आर्थिक विकास का ढाँचा उसी प्रकार का था जैसा अधिकांश लैटिन अमरीकी देशों का था यानी उपनिवेशवादी देश की जरूरतों को ध्यान में रख कर कुछ थोड़ी सी फसलों का उत्पादन किया जाता था जिसका मुख्य उद्देश्य निर्यात होता था। इसी प्रकार ज्यादातर लैटिन अमरीकी देशों तरह भूमि के मालिक बड़े-बड़े भूस्वामी थे। किसानों के बीच अशांति ने क्रांतिकारी राजनीतिक आंदोलनों को जन्म दिया था। इन आंदोलनों का मकसद उपनिवेशवादी शासन तथा सामंतीय शोषण का अंत करना था। 1930 के दशक के शुरू में एक किसान विद्रोह हुआ। इसको कुचल दिया गया। कुछ दूसरे राजनीतिक आंदोलन चलाए गए थे जिनका उद्देश्य देश को आजाद कराना था। 1935 में फिलीपींस को स्वायत्तता दी गई और इसके साथ वादा किया गया कि दस साल बाद इसको पूर्ण स्वतंत्रता दी जाएगी।हिंद-चीन स्वतंत्रता आंदोलन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता न्यूगुएन अई क्वोक थे। इनको बाद में हो ची मिन्ह नाम से जाना गया। हिंद-चीन में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लगभग 100,000 वियतनामी फ्रांस भेजे गए थे। इनमें से कुछ तो सैनिक के रूप में गए थे लेकिन अधिकांश श्रमिकों के रूप में गए थे। फ्रांस में उनका संपर्क समाजवादी और अन्य क्रांतिकारी आंदोलनों के साथ हुआ। हो ची मिन्ह फ्रांस की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना से काफी सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। 1925 में उन्होंने वियतनामी युवा क्रांतिकारियों का एक संघ बनाया। 1930 में विभिन्न कम्युनिस्ट गुटों ने मिलकर वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। आगे चलकर इसका नाम ‘हिन्द-चीन की कम्युनिस्ट पार्टी‘ रखा गया। फ्रांसीसी शासन के विरूद्ध स्वतंत्रता संग्राम में इस दल ने नेतृत्वकारी भूमिका अदा की। एक दूसरी राजनीतिक पार्टी भी थी। इसका नाम वियतनाम नेशनल पार्टी था। यह कोमिनटांग के ढाँचे पर बनाई गई थी। इस पार्टी ने 1930 में एक विद्रोह संगठित किया था जिसे बाद में दबा दिया गया था। उपनिवेशवादी शासक इण्डोनेशिया को डच ईस्ट इंडीज कहा करते थे। इण्डोनेशिया में बीसवीं सदी के आंरभिक वर्षों में डच शासन के विरूद्ध स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक आंदोलन तथा मजदूरों और किसानों के संगठनों का आविर्भाव हुआ। इनमें इस्लामिक एलाएंस और सोशल डेमोक्रेटिक एसोशिएशन के नाम महत्वपूर्ण हैं। 1920 में इण्डोनेशिया की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। इसने जावा और सुमात्रा में विद्रोह का संगठन किया। डच अधिकारियों ने नृशंस पुलिस कार्रवाई के जरिए इन विद्रोहों को दबा दिया। 1927 में अहमद सुकर्णो के नेतृत्व में एक नेशनलिस्ट पार्टी स्थापित की गई (जो बाद में स्वतंत्र इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति बने) इस पार्टी ने स्वतंत्रता के लिए संयुक्त अभियान चलाने के मकसद से विभिन्न प्रकार के दूसरे संगठनों और दलों को एक मंच पर संगठित किया। एक बार यदि देश आजाद हो गया तो इस पार्टी ने उसके बाद समाजवाद की स्थापना के उद्देश्य को स्वीकार किया। राष्ट्रवादी आंदोलनों की बढ़ती हुई ताकत से डच अधिकारी चौंक गए और उन्होंने नेशनलिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया तथा इसके कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों में सुकर्णो भी थे। दमन कई सालों तक चला और यहाँ तक कि स्वतंत्रता की माँग को लेकर होने वाले विचार विमर्श पर भी प्रतिबंध लगाए गए। ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने के बाद भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। 1937 में उसे भारत से अलग कर दिया गया। बीसवीं सदी की शुरुआत में 1924 में बर्मा में यंग मेन्स बुद्धिस्ट एसोशिएशन की स्थापना के साथ वहॉं राष्ट्रवादी आंदोलन प्रारंभ हो गया। बर्मा के राष्ट्रवादी आंदोलन पर भारत में साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष के विकास का जबर्दस्त असर था। तथा दोनों देशों के स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं ने आपस में घनिष्ठ संपर्क कायम कर लिया था। 1921 में ’जनरल एसोशिएशन ऑफ बर्मीज कोंसिल’ की स्थापना हुई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरह उसने बर्मा में स्वशासन के स्थापना की माँग रखी। 1930 के दशक में ’थाक्रिन्स’ नाम का नौजवानों का एक संगठन बना जिसका अर्थ था ’अपने देश के मालिक’। इस संगठन ने पूर्ण स्वतंत्रता की माँग रखी। इस संगठन के सबसे प्रभावशाली नेता आंग सान थे जो बाद में बर्मा की कम्युनिस्ट पार्टी के भी नेता हुए। भारत से अलग होने के बाद बर्मा भी भरतीय अधिनियम 1935 की तरह संवैधानिक सुधार लागू किए गए लेकिन इन सुधारों से बर्मा के राष्ट्रीवादी नेता संतुष्ट नहीं हुए। चारों ओर जबर्दस्त ब्रिटिश विरोधी जनान्दोलन प्रारंभ हो गया तथा पूरे देश में विरोध में जुलूस निकाले गए और हड़तालें हुईं। मलाया का ब्रिटिश उपनिवेश कई राज्यों से मिल कर बना था। इनमें से कुछ तो सीधे ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत थे जबकि कुछ अन्य राज्यों को स्थानीय शासकों के आधीन रखा गया था और एक हद तक स्वायत्त थे। ब्रिटिश शासक इसका शोषण मुख्य रुप से रबर तथा टिन के लिए करते थे। इनके बागान और इनकी खानों के मालिक ब्रिटिश लोग थे लेकिन इनमें काम करने वाले मजदूर भारतीय मूल के थे। एशिया में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए सिंगापुर अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था क्योंकि सामरिक तथा व्यापारिक दृष्टि से इसको बहुत उपयोगी माना गया था। मलय और भारतीय मूल के लोगों के अलावा मालाया में काफी बड़ी संख्या चीनी मूल के लोगों की थी। ये लोग ज्यादातर वाणिज्य और व्यवसाय में लगे हुए थे। अलग-अलग प्रजाति के लोगों ने अपने अलग राजनीतिक संगठन बना रखे थे। मलेशिया में संगठित राष्ट्रवादी आंदोलन के उभार को रोकने के लिए ब्रिटिश अधिकारी इनके आपसी मतभेदों का इस्तेमाल किया करते थे। श्रीलंका की आबादी मुख्यतः सिंहलियों की थी। इसके अलावा वहाँ पर तमिल लोग और कुछ भारतीय मूल के मजदूर थे। ब्रिटिश अधिकारियों ने वहाँ कुछ संवैधानिक परिवर्तन किए। इससे देश के प्रशासन में श्रीलंका के उच्च वर्ग को थोड़ा प्रतिनिधित्व मिला। 1931 में नए संविधान के तहत प्रौढ़ मताधिकार प्रणाली लागू की गई और एक विधायिका की स्थापना की गई। विधान मंडल के सदस्य ब्रिटिश सचिवों के साथ मिलकर सरकार चलाते थे। 1930 के दशक में कई राजनीतिक दलों का गठन हुआ और कई विख्यात राजनीतिक नेता उभर कर सामने आए। स्वंतत्र श्रीलंका के राजनीतिक जीवन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। पश्चिम एशिया के देशसत्ता पर कब्जा करने के तुरंत बाद अमानुल्ला खाँ ने अफगानिस्तान की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अफगानिस्तान की नई सरकार के साथ सोवियत संघ की संधि की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। इस संधि की मदद से अफगानिस्तान ने अपनी स्वतंत्रता को और अधिक संगठित किया था। देश के आधुनिकीकरण के लिए अमानुल्ला खाँ ने कुछ कदम उठाए। 1929 में उनको हटा दिया गया और मुहम्मद नादिरशाह को राजा बनाया गया। नादिर शाह के शासन काल में एक नया संविधान लागू किया गया। इसका उददेश्य अफगानिस्तान को राजतंत्र का संवैधानिक रूप देना था।अक्टूबर क्रांति के बाद रूस ने 1907 के आंगल रूसी समझौते का परित्याग कर दिया। इस समझौते के अनुसार ईरान का एक भाग रूसी प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा माना गया था। क्रांतिकारी विचारों के प्रसार और ईरान में अपने तेल के हित के कारण ब्रिटिश लोग काफी चिंतित हुए। इसलिए उन्होंने सारे देश पर कब्जा करने की धमकी दी। 1919 में ईरान सरकार के साथ उन्होंने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के कारण ईरान की फौजों तथा अर्थव्यवस्था पर ब्रिटेन का नियंत्रण कायम हो गया। ब्रिटेन के कब्जे तथा ब्रिटेन के साथ समझौते के खिलाफ ईरान के विभिन्न भागों में विद्रोह हुए। ईरान के कम्युनिस्टों ने इन विद्रोह को सोवियत गणतंत्र कायम करने के लिए इस्तेमाल करना चाहा लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही। लेकिन 1921 में ईरान की ब्रिटिश समर्थक सरकार को एक सैनिक अधिकारी रजा खाँ ने गिरा दिया। नई सरकार ने भी ब्रिटेन के साथ किए गए 1919 के समझौते को रद्द कर दिया यद्यपि इसने क्रांतिकारी विद्रोहों को भी निर्ममतापूर्वक कुचल दिया था। बहुत से ईरानी रजा खाँ को ईरान का मुस्तफा कमाल समझते थे तथा जब उन्होंने अपने हाथ में निरंकुश शक्ति चाही तो उसका उन्होंने समर्थन किया। 1925 में ईरान की संविधान सभा (जिसे वहाँ मजलिस कहा जाता है) ने ईरान के शासक को सिंहासन से हटा कर उसकी जगह पर रजा खाँ को ईरान का बादशाह बना दिया। उद्योग और परिवहन का विकास किया गया। आधुनिक शिक्षा को शुरू करने का प्रयास किया गया साथ ही मुल्लाओं के प्रभाव को भी कम करने की कोशिश की गई। न्याय प्रणाली में कई सुधार किए गए। महिलाओं को बुर्का पहनने से मना कर दिया गया। जहाँ आंग्ल ईरानी तेल कंपनी का महत्व बना रहा, अब इसके लाभ का बहुत बड़ा हिस्सा ईरान को मिलने लगा। बहरहाल, इन उपायों के बाद भी शाह का शासन आतंक फैलाने वाला था और ईरान की आम जनता को इस शासन से कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। उल्लिखित किया जा चुका है कि इराक, फिलिस्तीन और ट्रांस जोर्डन को अधिकार पत्र के रूप में ब्रिटेन को दिया गया था। इराक को ब्रिटेन के हवाले कर देने के निर्णय से इराक के लोगां में विद्रोह भड़क उठा। लेकिन इसको ब्रिटिश फौजों ने कुचल दिया। 1921 में ब्रिटिश शासकों ने फैजल को इराक की गद्दी पर बैठाया जिनको फ्रांसीसियों ने सीरिया की गद्दी से उतार दिया था। लेकिन अंग्रेजों ने सैनिक, राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण अपने हाथ में रखा। इराक के संपन्न तेल संसाधनों को भी अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण में कर लिया। 1930 में इराक को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई और इसके तुरंत बाद वह राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया। फिर भी अंग्रेजी फौजें इराक में बनी रहीं और इराक की अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजी राज की पकड़ भी बनी रही। ब्रिटेन समर्थक सरकार वाला इराक संवैधानिक राजतंत्रीय व्यवस्था वाला इराक बना। 1936 में, सेना के एक हिस्से की मदद से नेशनल रिफार्म पार्टी ने ब्रिटिश-समर्थक सरकार का तख्ता पलट दिया और कृषि सुधार लागू करने और इराकी अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया। लेकिन 1937 में इस सरकार का भी तख्ता पलट दिया गया तथा नूरी सईद नामक ब्रिटिश-समर्थक व्यक्ति नई सरकार का नेता बना। ब्रिटिश लोगों ने ट्रांस जोर्डन में भी वही नीति जारी रखी। उन्होंने फैजल के भाई अब्दुल्ला को 1928 में राजगद्दी पर बैठाया, उस देश को आजादी दी लेकिन सैनिक और वित्तीय नियंत्रण अपने हाथ में रखा। लेकिन फिलिस्तीन में ब्रिटिश नीति को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और यह क्षेत्र तनावों और संघर्षों का स्रोत बन गया। उन्नीसवीं सदी के अंत में पश्चिमी देशों में यहूदीवाद आंदोलन की शक्ल में उभर कर सामने आया। वे यूरोप और संयुक्त राज्य अमरीका में समान अधिकार तथा भेदभाव को खत्म करने के लिए लड़ते आ रहे थे। अक्सर उनके साथ भेदभाव बरता जाता था। उनमें से कइयों ने क्रांतिकारी राजनीतिक आंदोलन में भाग लेना शुरू किया था लेकिन यहूदीवादी इसकी घोषणा करता था कि यहूदी एक राष्ट्र है चाहे वे जिस किसी देश में रह रहें हों और फिलीस्तीन में उनको अपना राज्य मिलना चाहिए जहाँ ढाई हजार साल से भी पहले उनका साम्राज्य था। यहूदियों में यहूदीवादी आंदोलन का दायरा काफी छोटा था लेकिन ब्रिटिश सरकार इसका समर्थन करती थी। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने फिलिस्तीन में यहूदी जनता के लिए ‘गृह राष्ट्र‘ देने का वादा किया था। युद्ध के दौरान अरब राष्ट्रवाद विकसित हो चुका था और जैसे ही फिलिस्तीन में ब्रिटिश राज्यादेश लागू किया गया वैसे ही गंभीर उथल-पुथल शुरू हो गई। लेकिन एक ओर फिलिस्तीनियों की राष्ट्रीय भावनाओं को जहाँ दबाया गया, वहीं बहुत बड़़ी संख्या में यहूदी पश्चिमी देशों से फिलिस्तीन में आकर बसे। यहूदियों ने फिलिस्तीनियों से उनकी सबसे अच्छी भूमि ले ली और वे लोग भूमिहीन हो गए। 1919 में फिलिस्तीन में यहूदियों की जनसंख्या 58,000 थी लेकिन 1934 में बढ़कर यह 9,60,000 पहुँच गई। 1929 में अरबों ने फिलिस्तीन की मुक्ति के लिए विद्रोह किया था। उन्होंने फिलिस्तीन में यहूदियों के आब्रजन के विरूद्ध आवाज उठाई थी। विद्रोह कुचल दिया गया और ब्रिटिश पुलिस और सेना ने सैकड़ों अरबों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अरब फिलिस्तीनी कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रवादी संघर्ष जारी रहा। 1937 में ब्रिटिश रॉयल कमीशन ने फिलिस्तीन को तीन राज्यों में बाँटने की सिफारिश की जिनमें से एक को अरबों के नियंत्रण में होना था, दूसरे को यहूदियों के तथा तीसरे राज्य को ब्रिटिश लोगों के नियंत्रण में रखने की सिफारिश की गई थी। सबने इस सिफारिश को नामंजूर कर दिया। फिलिस्तीन तथा दूसरे देशों के अरब लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया। 1939 में ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेतपत्र जारी किया इसमें दस साल बाद फिलिस्तीनियों को आजादी देने का वादा किया गया था। इसमें यहूदियों और अरब दोनों को गांरटी दी गई थी। इसी बीच यहूदियों के आब्रजन को सीमित किया जाना था तथा इसके बाद उसे पूरी तरह रोका जाना था। भूमि की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने पर इस मुद्दे में गंभीर मोड़ आया जिसके पश्चिमी एशिया की शांति और स्थिरता के लिए गंभीर परिणाम निकले। सीरिया और लेबनान फ्रांसीसी अधिदेश हो चुके थे और भयानक प्रतिरोध के बावजूद फ्रांसीसी सैनिकों ने इस भूभाग पर कब्जा कर लिया। फ्रांसीसी मदद से पहले फैजल सीरिया के बादशाह बने थे लेकिन फ्रांसीसियों ने उनको गद्दी से हटा दिया। इन दोनों देशों की जनता ने शुरू से ही फ्रांसीसी शासन लादने का प्रतिरोध किया। 1925 में सीरिया में एक विद्रोह फूट पड़ा और विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क के साथ पूरे देश को अपने कब्जे में ले लिया। यह विद्रोह लेबनान के भी कुछ भागों में फैला। इस विद्रोह के दौरान दमिश्क पर जबर्दस्त बमबारी हुई। इस बमबारी में लगभग 25000 लोग मौत के मुँह में चले गए। फिर भी, फ्रांसीसी अधिदेश को खत्म करने के लिए हड़तालें, प्रर्दशन और सशस्त्र संघर्ष चलते रहे। 1936 में फ्रांस में जब लोकप्रिय मोर्चा (पापुलर फ्रंट) सत्ता में आया तब फ्रांस की सरकार ने सीरिया और लेबनान के प्रतिनिधियों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसमें तीन साल के बाद स्वतंत्रता देने का वादा किया गया था। बाद में फ्रांसीसी सरकार अपने वादे से मुकर गई और सीरिया तथा लेबनान अपनी आजादी हासिल करने में असफल रहे। अफ्रीकाप्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने तक अफ्रीका में तकरीबन 50 राज्य थे। इसमें लाइबेरिया और इथयोपिया यूरोप के उपनिवेश थे। राष्ट्रवादी आंदोलनों के झटके हर जगह महसूस किए गए लेकिन राजनीतिक संघर्ष का स्तर हर देश में अलग-अलग था। यदि आमतौर पर देखें तो दो विश्व युद्धों के दौरान, उपनिवेशवादी शासन के आंरभिक दौर में जिस प्रकार के प्रतिरोध और विद्रोह देखने को मिले, बाद में अफ्रीकी लोगों ने संघर्ष के उस रूप को बदल दिया। ऊपर से देखने में लगता था कि उपनिवेशवाद अपने को पूर्ण रूप से स्थापित कर चुका है और उपनिवेशवादी शासन की ऊपरी स्थिरता को देखते हुए कुछ लोगों ने इस दौर को उपनिवेशवादी शासन का ‘स्वर्ण युग‘ भी कहा था। लेकिन यह स्थिरता दिखावटी अधिक थी और वास्तविक कम क्योंकि उपनिवेशवाद-विरोधी नई ताकतों का रूप धीरे-धीरे प्रकट होने लगा था। उत्तर अफ्रीका के कुछ देशों में इसी काल में शक्तिशाली राष्ट्रवादी आंदोलन और संघर्ष देखने को मिलते हैं। दक्षिण अफ्रीका के अधिकांश देशों समेत अन्य देशों में यह दौर राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी राजनीतिक आंदोलनों के उभार का काल माना जाता है।उत्तरी अफ्रीका में सबसे शक्तिशाली आंदोलनों में से एक आंदोलन मिस्र में खड़़ा हुआ था। 1918 में वफ्द नाम का एक संगठन स्थापित किया गया। इसने मिस्र में स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व किया। शांति सम्मेलन के दौरान मिस्र के लिए स्वतंत्रता का मांग पत्र देने के उद्देश्य से मिस्र के राष्ट्रवादियों का एक प्रतिनिधि मंडल फ्रांस जाने के लिए तैयार हुआ लेकिन प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को ब्रिटिश लोगों ने गिरफ्तार कर लिया तथा वफ्द के नेता सद जगलुल पाशा को निर्वासित कर दिया गया। इससे मिस्र में विद्रोह भड़क उठा लेकिन उसे कुचल दिया गया। लेकिन ब्रिटिश विरोधी आंदोलन चलते रहे और 1922 में मजबूर होकर ब्रिटिश सरकार ने मिस्र के संरक्षित राज्य का दर्जा खत्म कर दिया। मिस्र को स्वतंत्र साम्राज्य का दर्जा देकर अहम फौद को उसका राजा बनाया गया। 1923 में वहाँ एक संविधान लागू किया गया जिसके जरिए मिस्र में संसदीय प्रणाली की सरकार स्थापित की हुई। फिर भी मिस्र तथा स्वेज नहर की सुरक्षा के नाम पर ब्रिटेन की फौज वहाँ जमी रही। इन फौजों के वहाँ बने रहने का मकसद सूडान में ब्रिटिश शासन को कायम रखना भी था, यद्यपि सूडान नाम के लिए ब्रिटिश-मिस्र के संयुक्त नियंत्रण में था। संसद के चुनाव में जगलुल पाशा की वफ्द पार्टी भारी बहुमत से विजयी हुई तथा उसने अपनी सरकार बनाई। सरकार ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। मिस्र के राजा ने संसद भंग का दी। हर निष्पक्ष चुनाव में वफ्द पार्टी भारी मतों से जीतती थी और ब्रिटिश लोगों के इशारे पर राजा उसको भंग कर देता था। छः साल की अवधि में राजा ने चार बार इस प्रकार संसद भंग की थी। जगलुल पाशा की मौत के बाद उसका बेटा नहस पाशा वफ्द पार्टी का नेता बना और इस पार्टी ने ब्रिटिश-विरोध की अपनी पुरानी नीति जारी रखी। 1930 में एक नया संविधान घोषित किया गया जिसके अनुसार राजा की शक्ति बढ़ गई और संसद की शक्ति कम हो गई। चारों तरफ इसका जनता में विरोध हुआ और 1935 में 1923 वाला संविधान पुनः लागू किया गया। 1936 में चुनाव कराए गए। वफ्द पार्टी इस चुनाव में फिर सत्ता में आ गई। इससे राष्ट्रवादी शक्तियों की विजय हुई। नई सरकार ने ब्रिटिश सरकार के साथ एक समझौता किया। इस समझौते के अनुसार मिस्र पर ब्रिटिश अधिकार समाप्त हो गया लेकिन ब्रिटेन को 10,000 सिपाही स्वेज नहर क्षेत्र में रखने की इजाजत मिल गई। ब्रिटेन की फौजों का मिस्र में मौजूद रहना कुछ सालों के बाद ब्रिटेन और मिस्र के बीच टकराव का मुख्य स्रोत बना। ट्यूनीशिया, लीबिया, अल्जीरिया और मोरक्को में भी शक्तिशाली राष्ट्रवादी आंदोलन आरंभ हो चुके थे। 1921 में अब्दुल करीम के नेतृत्व में स्पेन के अधीन वाले मोरक्को में विद्रोह भड़क उठा। यह विद्रोह रिफ जनजाति का था। उन्होंने स्पेन की फौज को जबर्दस्त मात दी और उसको रिफियन गणतंत्र वाला राष्ट्र घोषित किया। इसके तत्काल बाद फ्रांस ने रिफियन गणतंत्र के खिलाफ अपनी सेना भेजी लेकिन उन्हें पीछे ढकेल दिया गया। अंततः स्पेन और फ्रांस ने मिलकर संयुक्त फौजी कार्रवाई की जो दो सालों तक चली। इसमें उनकी सेना की संख्या 400,000 थी, जो अनुपात में बहुत ज्यादा थी। 1962 में अब्दुल करीम को आत्म समर्पण करना पड़ा और 1927 में स्पेन और फ्रांस दोनों ही मोरक्को में अपने-अपने हिस्से पर काबिज हो गए। पूरे अफ्रीकी देशों के लिए रिफ विद्रोह साम्राज्यवाद-विरोधी आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बन गया। जब रिफ गणतंत्र के खिलाफ फ्रांस युद्ध चला रहा था, बहुत से फ्रांसीसियों, मसलन फ्रांस की कम्युनिस्ट पार्टी तथा ट्रेड यूनियनों के रिफ लोगों को अपना समर्थन दिया था। मोरक्को में फ्रांसीसी नीति के विरूद्ध 12 अक्टूबर 1925 को फ्रांस के मजदूरों ने हड़ताल और प्रदर्शन किए। फ्रांस की कम्युनिस्ट पार्टी और वहाँ के मजदूर वर्ग ने भी अल्जीरिया और ट्यूनीशिया की स्वतंत्रता का समर्थन किया और इन देशों में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना में उनकी सहायता की। दक्षिण अफ्रीकी देशों में राष्ट्रीय आंदोलन का विकास एक जैसा नहीं हुआ था। दक्षिणी अफ्रीका में उपनिवेशवादी शासकों ने जो राज्य स्थापित किए थे, उनके नागरिकों में से अधिकांश की कोई साझी इकाइयाँ थी। एशिया के अधिकांश देशों से वह स्थिति भिन्न थी या यूरोप के पुराने देशों से भी वह स्थिति अलग किस्म की थी। दो युद्धों के दौरान इन राज्यों के लोगों में राष्ट्रीय अस्मिता की चेतना का विकास महत्वपूर्ण बात थी। प्रत्येक में किसानों, मजदूरों बुद्धिजीवी वर्ग और समाज के अन्य तबकों में परेशानी और बेचैनी थी। इस वजह से मजदूर यूनियनें और दूसरे प्रकार के संगठन स्थापित हुए। इन संगठनों का स्वरूप राजनीतिक और उपनिवेशवाद-विरोधी होना अवश्यंभावी था क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ तत्काली उपनिवेशवादी शासन था। राष्ट्रीय राजनीतिक संगठनों की स्थापना करने में और लोगों में राजनीतिक चेतना लाने में बुद्धिजीवियों की भूमिका नेतृत्वकारी थी। दक्षिण अफ्रीका में शैक्षिक सुविधाएँ बहुत सीमित थी और यहाँ तक कि उपनिवेशवादी शासन को बनाए रखने के लिए माध्यमिक शिक्षा को भी बहुत खतरनाक माना जाता था। बहुत से अफ्रीकी इतिहासकारों का मत है कि अफ्रीका के उपनिवेशवादी शासकों ने भारत में उपनिवेशवादी शासन के अनुभव के कारण जानबूझ कर शिक्षा के स्तर तथा सुविधाओं को बहुत ही नीचा रखा। भारत में काफी बड़ी संख्या में भारतीय लोग शिक्षा लेने में समर्थ थे। इन लोगों ने ब्रिटिश सत्ता को भारत की धरती से उखाड़ फेंकने के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली आंदोलन चलाया। बहरहाल कुछ अफ्रीकी लोगों को तो शिक्षा मिली ही, क्योंकि उपनिवेशवादी शासक सभी कामों के लिए अपने देश से लोगों को लाकर प्रशासन नहीं चला सकते थे। शिक्षित अफ्रीकियों में से बहुत से उपनिवेशवादी प्रशासन के काम में लगाए गए थे। उनके साथ उपनिवेशवादी शासक भेदभाव का बर्ताब करते थे, इसका इनको एहसास हुआ। उन्हें अपनी जनता के शोषण का भी एहसास हुआ। इनमें से कई तो विदेशों में, खास तौर पर ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमरीका में उच्च अध्ययन के लिए जहाँ इन लोगों का सम्पर्क क्रांतिकारी और लोकतांत्रिक विचारों और आंदोलनों से हुआ। इनमें से कुछ तो अफ्रीका के भावी नेता थे जिनको विदेश प्रवास के दौरान ही ख्याति मिल चुकी थी, जैसे केनिया के जोमा केन्याटा, नाइजीरिया के नाम्दी अजीकीवे, गोल्ड कोस्ट (घाना) के क्वामे नुक्रूमा और सेनेगल के लियोपोल्ड सेंगोर। 1920 के दशक में दक्षिणी अफ्रीकी देशों में कई संगठन स्थापित किए गए। जिन देशों में कुछ प्रतिनिधि संस्थाओं का सूत्रपात किया गया था, उनमें नियमित रूप से काम करने वाले राजनीतिक दल अस्तित्व में आए। जैसे देश में संवैधानिक सुधार लागू होने के बाद नाइजीरिया में नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की गई। इस बीच कुछ और संगठन भी बने जैसे ‘यंग किकूयू एसोशिएशन’, ‘दि गोल्ड कोस्ट यूथ कानफरेंस’, ‘दि लीग फार दि राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजेनशिप’ तथा अंगोला में ‘लीगा अफ्रीकाना’। इस अवधि में अफ्रीकी में उपनिवेशवाद आंदोलनों के आविभार्व में कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और आंदोलनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनमें से कई आंदोलनों का सूत्रपात अमरिका में समानता के लिए काले लोगों के संघर्ष से जुड़े नेताओं ने किया था। इनमें से कुछ लोग कैरीबियन क्षेत्र के ब्रिटिश और फ्रांसीसी उपनिवेशों के काले लोगों की संतान थे। सभी काले लोगों की एकजुटता और एकता की वकालत इन सभी आंदोलनों की आम खूबी थी। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण पैन अफ्रीकन कांग्रेस थी जिसे डब्ल्यू. ई. बी. दु बोई ने संगठित किया था। काले लोगों की तरक्की के लिए राष्ट्रीय संगठन स्थापित करने के संदर्भ में हम पहले इनकी चर्चा कर चुके हैं। 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान दु बोई ने पैन अफ्रीकन कांग्रेस की पहली बैठक बुलाई। संयुक्त राज्य अमरीका तथा दुनिया के दूसरे भागों में रहने वाले काले लोगों को समान अधिकार देने की माँग करती हुई कांग्रेस की इस बैठक ने प्रस्ताव पारित किए। अफ्रीकी लोगों को आत्म निर्णय के अधिकार की माँग का प्रस्ताव भी पारित किया गया। यूरोपीय देशों की विभिन्न राजधानियों में 1921,1923 और 1927 में पैन अफ्रीकन कांग्रेस के अधिवेशन हुए इससे अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमरीका और कैरेबियन देशों के काले बुद्धिजीवी एक-जुट हुए। मार्कुस गार्वे नामक नेता ने दूसरा पैन अफ्रीकन आंदोलन प्रारंभ किया। यह जमैका में पैदा हुआ था। 1914 में उसने एक संगठन बनाया था। इसका नाम यूनीवर्सल नीग्रो इम्प्रूवमेंट एसोशिएशन था। उसने काले अमरीकियों को अमरीका छोड़कर अफ्रीका में बसने को प्रोत्साहित करने के लिए एक अभियान चलाया। हर जगह के काले लोगों में गर्व की चेतना जगाने में उसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी। 1920 और 1930 के दशक में एक सांस्कृतिक आंदोलन उठ खड़ा हुआ। इससे काले लोगों में अस्मिता के बोध को बढ़ावा मिला, उनमें गर्व का भाव जगा, साथ ही उनमें औपनिवेशिक प्रभुत्व को अस्वीकार करने की चेतना भी पैदा हुई। इसको नीग्रो जाति के गौरव बोध (नेग्री ट्यूड) का आंदोलन कहा जाता है। यह काली संस्कृति, अफ्रीकी कला के सौंदर्य, संगीत सौंदर्य और इस विश्वास पर आधारित था कि सभी अफ्रीकियों और उनकी संतानों की सांस्कृतिक विरासत समान है। इसके कुछ विख्यात व्यक्तियों के नाम हैं। कैरेबियन में फ्रांसीसी उपनिवेश के निवासी एमे सिजेरे मार्तिनी, सेनेगल के लियोपोल्ड सेदार सेंगोर (सही बाद में सेनेगल के राष्ट्रपति बने) और संयुक्त राज्य अमरीका के लैंग्स्टन हॉफ। ये तीनों ही अत्यंत विख्यात कवि थे। इनमें से पहले दो फ्रांसीसी भाषा के और तीसरे व्यक्ति अंग्रेजी के विख्यात कवि थे। जमैका मूल के तीसरे कवि क्लाउद मैक्के थे। इन्होंने काले लोगों को उनकी आम कठिनाइयों के विरूद्ध आवाज उठाने तथा अपने सम्मान के लिए दवाब डालने के लिए प्रेरित किया। यूरोप में जो साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था, उसने अफ्रीका में भी राष्ट्रवादी आंदोलन को बढ़ावा दिया। 1927 में ब्रुसेल्स में एक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस हुई। उसमें साम्राज्यवाद विरोधी एक संघ बनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि की हैसियत से जवाहरलाल नेहरू इसमें शामिल हुए थे। इसके अलावा क्रांतिकारी बुद्धिजीवी तथा वामपंथी आंदोलन से जुड़े यूरोप के नेता और एशिया और अफ्रीका के उन देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया जो उपनिवेशवादी शासन के अंतर्गत थे। इनमें मिस्र केनिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधि थे जिनमें जोमो केन्याटा तथा ला गुमा जी आए थे। इटली ने इथयोपिया पर आक्रमण किया था और समूची दुनिया में इसका विरोध हुआ था। इससे अफ्रीका में उपनिवेशवादी विरोधी भावनाओं को बल मिला था। दो विश्व युद्धों के बीच के वर्षों में दक्षिण अफ्रीका नस्ली (प्रजातीय) दमन व्यवस्था और सुदृढ़ हुई लेकिन उसी अनुपात में इसके खिलाफ संघर्ष तेज हुआ। 1910 में नैटाल तथा केप कॉ लोनी, बोअर राज्य, ओरेंज फ्री राज्य तथा ट्रांसवाल के ब्रिटिश उपनिवेशों को मिलाकर, एक स्वशासित राज्य बनाया गया था। इसे ब्रिटिश साम्राज्य का दक्षिण अफ्रीकी संघ कहा जाता था। प्रथम युद्ध के बाद दक्षिण अफ्रीका में गोरों की आबादी 18 लाख थी। यह उनकी जनसंख्या की 20 प्रतिशत के करीब थी। गोरों में ब्रिटिश मूल के लोग थे तथा बोअर में डच मूल के। लेकिन बहुसंख्यक जनसंख्या अफ्रीकी लोगों की थी। 200,000 लोग एशियाई थे जिनमें प्रमुखता भारतीय लोगों की थी। सरकार पर पूरी तरह से गोरे लोगों का नियंत्रण था। भारतीय लोगों के साथ अफ्रीका में जातीय आधार पर भेदभाव बरता जाता था और गाँधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में विरूद्ध संघर्ष चलाया था, इसका परिचय आपको पहले दिया जा चुका है। 1912 में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसने दक्षिण अफ्रीका में प्रजातीय दमन के विरूद्ध प्रमुख भूमिका निभाई। 1921 में दक्षिण अफ्रीका की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। नेशनलिस्ट पार्टी में बोअर्स लोग थे यहाँ अतिवादी गोरी प्रजातीयता वाले विचारों की प्रमुखता थी। गोरों की राजनीतिक और राजनीतिक श्रेष्ठता को बनाए रखने के उद्देश्य से यह रंग भेद की नीति की वकालत करती थी। ये मानते थे कि काले लोगों सेगोरों को खतरा हैं। 1920 के दशक के मध्य से नस्लवादी विचारों के प्रभाव में आकर गोरे शासकों ने अनेक कानून बनाए जिनके चलते कुशल कार्यों से, काले लोगों को पृथक रखा गया अथवा कुशल कार्यों के प्रशिक्षण से उनको वंचित रखा गया या जिन इलाकों में गोरे लोग रहते थे वहाँ उनके रहने पर प्रतिबंध लगाया गया। सारी अच्छी उपजाऊ जमीन पर गोरे लोग पहले से काबिज थे। कुछ इलाके जनजातियों के लिए सुरक्षित थे, काले लोगों को उन इलाकों में जाने के लिए कहा गया, शहरों में अथवा गोरे लोगों के खेतों में काम करने के लिए उनको इजाजत लेनी पड़ती थी। शहरों में उनको पहचान पत्र या पास रखना होता था जिसका आशय यह सिद्ध करना था कि वहाँ जाने की उनको इजाजत मिली है। यदि उनके पास ये चीजें न हों तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था शहरों में उनको ऐसे इलाकों में रहने के लिए विवश किया जाता था जो उनको दिए गए थे जहाँ की रहने की स्थिति बड़ी भयानक थी। एक गोरे मजदूर की औसत मजदूरी उसी के समकक्ष के काले मजदूर से दस गुना अधिक होती थी। काले लोगों के ट्रेड यूनियन बनाने पर तो प्रतिबंध था ही, वे गोरे लोगों की यूनियन के सदस्य भी नहीं बन सकते थे। उनको मतदान का कोई अधिकार नहीं था और अपने देश के राजनीतिक जीवन में उनका किसी प्रकार दखल नहीं था और न ही उनकी कोई बात मानी जाती थी। 1930 के दशक में जर्मनी के नाजियों की तर्ज पर गोरे नस्लवादियों ने एक फासीवादी आंदोलन आयोजित किया। नस्लवादी नीतियों के विरूद्ध व्यापक असंतोष पैदा हुआ तथा इस अनैतिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए संगठित संघर्ष की तैयारी होने लगी। लैटिन अमरीकाअधिकांश लैटिन अमरीकी देशों में ऐसी सरकारें बरकरार रहीं जिनमें बड़े भूस्वामी और सेना का वर्चस्व था। लेकिन तकरीबन हर देश में लोकतांत्रिक और वामपंथी आंदोलन और मजदूरों तथा किसानों के संगठन मजबूत हुए। इस दौर में अधिकांश लैटिन अमरीकी देशों में कम्युनिस्ट पार्टियाँ भी गठित हुइंर्। निकारागुआ में कठपुतली सरकार के विरूद्ध अगस्तो सीजर सैंडिनों के नेतृत्व में एक जन विद्रोह हुआ। उस सरकार को संयुक्त राज्य अमरीका की सैनिक मदद से सत्ता में बैठाया गया था। यह जन विद्रोह कई साल तक चला और 1933 में संयुक्त राज्य अमरीका ने अपनी सेनाएँ हटा लीं। लेकिन सैंडिनो की हत्या कर दी गई तथा अनास्तासियो सोमोजा ने सत्ता हथिया ली और निकारागुआ में उसने अपने तानाशाही शासन की स्थापना की। सभी लैटिन अमरीकी देशों में सैडिनो के नेतृत्व में चलने वाले विद्रोहों को जनता की सहानुभूति और उनका समर्थन प्राप्त हुआ। इसके कारण लैटिन अमरीका में अपनी फौजें भेजकर हस्तक्षेप करने की नीति में संयुक्त राज्य अमरीका को परिवर्तन करना पड़ा। 1929 के आर्थिक संकट ने सभी लैटिन अमरीकी देशों की अर्थ-व्यवस्था पर असर डाला था। इनमें से अधिकांश देशों की अर्थ-व्यवस्था निर्यात पर निर्भर थी और जब संयुक्त राज्य अमरीका ने विदेशी आयात पर प्रतिबंध लगाया तो इनको जबर्दस्त आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इसका नतीजा यह हुआ कि उद्योगों में काम करने वाले लोगों की बहुत बड़ी संख्या बेरोजगार हो गई। जो लोग खेती के काम में लगे हुए थे, उन पर इसका और खराब असर पड़ा और इन देशों की जनसंख्या में इन लोगों की अधिकता थी।दोनों विश्वयुद्धों के दौरान मैक्सिको में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। लैटिन अमरीकी देशों में मैक्सिको पहला ऐसा देश था जिसने संयुक्त राज्य अमरीका से स्वतंत्र होने के लिए जबर्दस्त दबाव डाला, साथ ही किसानों के हित में सामाजिक और आर्थिक नीति अपनाने के लिए भी उसने ऐसा किया। सोवियत संघ के साथ कूटनीतिक संबंध बनाने वाले अमरीकी महाद्वीप का वह पहला देश था। 1934 से 1940 के बीच लजारों कार्डिनास मैक्सिको के राष्ट्रपति थे। बड़े भूस्वामियों की ताकत को कम करने के लिए तथा अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए उसने कई क्रांतिकारी कदम उठाए। बहुत सारी भूसंपत्ति जब्त कर ली गई और जब्त करने के बाद किसानों में बाँट दी गई उन्होंने रेलों तथा कुछ अन्य उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और अंततः संपूर्ण पैट्रोलियम उद्योग को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। इन उद्योगो पर पहले ब्रिटिश तथा अमरीकी कंपनियों का अधिकार था। पैट्रोलियम उद्योगों के राष्ट्र्रीयकरण के दूरगामी परिणाम हुए क्योंकि इसका अर्थ यह था कि जनता देश की संपत्ति और संसाधनों पर अपने अधिकार का दावा कर रही हैं। बाद में समय गुजरने के साथ दूसरे लैटिन अमरीकी देशों ने भी मैक्सिको का रास्ता अख्तियार किया। इस दौर की दो खास बातें हमें दिखाई देती हैं, विदेशी हस्तक्षेप से मुक्त होने के लिए लैटिन अमरीकी देशों को अपने अधिकारों के लिए दबाव डालना, दूसरा विश्व की गतिविधियों में उनकी स्वतंत्र भूमिका। राष्ट्र संघ का सदस्य बनने के पीछे उनका यही मुख्य उद्देश्य था। साम्राज्यवाद विरोधी एक अखिल अमरीकी संघ की स्थापना की गई थी और 1927 में ब्रूसेल्स में इसके प्रतिनिधियों ने इसके अधिवेशन में भाग लिया था। यहीं पर साम्राज्यवाद के विरूद्ध संघ की स्थापना हुई थी। पैन अमरीकी संघ पर अमरीकी प्रभुत्व के विरोध में सभी लैटिन अमरीकी देश एकजुट थे जिसकी स्थापना संयुक्त राज्य अमरीका की पहल पर पहले ही की जा चुकी थी। अमरीकी महाद्वीप के दूसरे देशों के मामले में हस्तक्षेप के अमरीकी दावे का इन देशों ने विरोध किया। 1933 में पैन अमरीकी संघ का एक अधिवेशन हुआ। इसमें संयुक्त राज्य अमरीका को इस घोषणा के समर्थन में स्वीकार पूर्वक कहना पड़ा था कि “किसी दूसरे राज्य के आंतरिक या विदेशी मामले में किसी राज्य को हस्तक्षेप करने का कोई हक नहीं है।” लैटिन अमरीकी देशों के प्रति अमरीकी नीति में कुछ उल्लेखनीय तबदीली आई। सन् 1920 के दशक से लैटिन अमरीकी देशों में उसने अपना निवेश बढ़ाया तथा उनकी अर्थ-व्यवस्था को काबू में रखा। इसे ‘डालट कूटनीति’ कहा जाता है। इसके लिए प्रत्यक्ष सैनिक हस्तक्षेप का अमरीका ने सहारा नहीं लिया। निकारागुआ से अमरीका ने अपनी फौजें हटा ली थीं, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। फ्रैंकलिन डॉ. रूजवेल्ट के राष्ट्रपतित्व के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका की लैटिन अमरीकी देशों के प्रति नीति को ‘अच्छे पड़ोसी की नीति‘ की संज्ञा दी गई है। कुछ मामलों में तो नीति में परिवर्तन काफी महत्वपूर्ण थे। संयुक्त राज्य अमरीका ने एक नियम बनाया जिसे “प्लाट संशोधन” (प्लाट अमेंडमेंट) कहा जाता है। इससे उसे क्यूबा में अपने सैनिक भेजने का स्व-आरोपित अधिकार प्राप्त हो गया। पनामा कनाल क्षेत्र को छोड़कर उसने पनामा से अपनी सेनाएं वापस बुला लीं। पनामा लगातार संयुक्त राज्य अमरीका के नियंत्रण में था। फिर भी इन उपायों से लैटिन अमरीकी देशों पर से संयुक्त राज्य अमरीका का प्रभुत्व समाप्त नहीं हुआ और बाद के वर्षों में भी अहस्तक्षेप की नीति का पालन नहीं किया गया। यूरोपीय देशों में फासीवादी संगठनों के अस्तित्व में आने के बाद, कुछ लैटिन अमरीकी देशों में भी फासीवादी गुट और राजनीतिक दल गठित किए जाने लगे। इनमें से कुछ में जर्मनी इटली और स्पेन से जाकर बसे प्रवासी लोग थे। लैटिन अमरीका की जनता को फासीवाद के खतरे के विरूद्ध जागरूक बनाया गया। फासीवादी समूहों और दलों की गतिविधियों को कम करने के लिए संयुक्त मोर्चा बनाने के प्रयास किए गए। फासीवादी देशों तथा जापान के आक्रमणकारी करतूतों की निंदा की गई। लगातार मैक्सिको की नीति फासीवाद विरोधी बनी रही। मंचूरिया में जापानी आक्रमण की, इटली द्वारा इथयोपिया पर हमला कर उसे हड़पने की तथा जर्मनी द्वारा आस्ट्रिया को अपने राज्य में मिला लेने की मैक्सिको ने निंदा की थी। हजारों स्पेनी रिपब्लिकन लोगों (गणतंत्रवादियों) को उसने शरण दी, जब इटली तथा जर्मनी की मदद से फ्रैंको ने स्पेन गणंतत्र को नष्ट कर दिया था। यूरोप की प्रगति1919 से 1923 के बीच यूरोपयह उल्लिखित किया जा चुका है कि प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद बहुत से यूरोपीय राष्ट्रों का स्वतंत्र राज्य के रूप में उदय हुआ। इन स्वंतत्र राज्यों में एस्टोनिया, लाटाविया, लिथुआनिया, फिनलैंड, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया शामिल हैं। पहले से ही एक राज्य अस्तित्व में था उसमें कुछ नए क्षेत्रों को शामिल करके यूगोस्लाविया राज्य बनाया गया। आयरलैंड स्वतंत्रता के लिए ब्रिटेन से संघर्ष कर रहा था, उसे 1922 में अलग कर दिया गया। स्वतंत्र आइरिश राज्य को स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा दिया गया जबकि छः जिलों वाले उत्तरी आयरलैंड का ब्रिटेन से संबंध बना रहा। कुछ सालों बाद स्वंतत्र आइरिश राज्य ने अपने को पूरी तरह इंग्लैंड से (ब्रिटिश कामनवेल्थ से) अलग कर लिया और अपने को आयर घोषित कर लिया। आस्ट्रिया-हंगरी साम्राज्य के अंत हो जाने पर आस्ट्रिया और हंगरी अलग-अलग स्वतंत्र राज्य हो गए।शांति समझौतों के कारण यूरोप में विभिन्न राज्यों की सीमा रेखाएं निर्धारण कर दी गईं। ये सीमा रेखाएँ तनाव और संघर्ष की जड़ बन गईं। सीमा निर्धारण से मध्य, दक्षिणी और पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश इस सीमा निर्धारण से संतुष्ट नहीं थे। इनमें बहुत से देश असुरक्षित महसूस करते रहे। इस दौरान और इसके बाद भी बहुत से समझौते, गठजोड़, मैत्री संधियों और अनाक्रण संधियों पर विभिन्न देशों के बीच हस्ताक्षर हुए और इन संधियों और गठजोड़ों में कई परिवर्तन भी हुए। बीस साल के बाद यूरोप के अंदर के कुछ भू-भाग विषयक झगड़े दूसरे महायुद्ध के लिए तात्कालिक कारण बने। लगभग सभी यूरोपीय देशों में युद्ध के बाद वाले वर्ष बहुत उथल-पुथल के दौर थे। युद्ध के दौरान अर्थव्यवस्था का अस्तव्यस्त होना एक समस्या थी। शांति की जरूरतें पूरी करने के लिए इसका पुनर्गठन आवश्यक था, इसकी भी समस्या गंभीर थी। इसके अलावा अन्य अनेक समस्याएँ थीं जैसे युद्ध में लाखों के मरने से उत्पन्न समस्या, जो बच गए थे उनको नौकरी/रोजगार दिलाने और उनके पुनर्वासक की समस्या तथा युद्ध से पैदा हुई बेरोजगारी की समस्याएँ यूरोप में मौजूद थीं। इन सब समस्याओं के कारण लोगों में भीषण असंतोष व्याप्त था। यूरोप के प्रत्येक देश में हड़तालों की लहर आई हुई थी तथा कुछ देशों में वर्तमान व्यवस्था को क्रांति के जरिए उखाड़ फेंकने के प्रयास भी किए गए थे। बहुत से देशों के मजदूर वर्ग के लिए रूस का उदाहरण प्रेरणा का स्रोत था। कम्युनिस्ट पार्टियाँ और समाजवादी लोकतंत्र-वादियों के एक तबके ने रूस जैसी क्रांति संगठित करने का प्रयास भी किया। सबसे गंभीर क्रांतिकारी विस्फोट जर्मनी में देखने को मिला। 1919 में बेला कुन के नेतृत्व में एक क्रांतिकारी सरकार सत्ता में आई थी लेकिन 1923 तक यूरोप दूसरे हिस्सों में क्रांति की सफलता की संभावनाएँ कम हो गईं क्योंकि हंगरी की क्रांति मुश्किल से पाँच महीने जीवित रह सकी थी। बहुत से देशों में, प्रायः विभिन्न समाजवादी संगठनों तथा क्रांतिकारी गुटों में एकता के अभाव में क्रांति की आशाएँ धूमिल पड़ गई, इसलिए अधिनायकवादी और लोकतंत्र विरोधी ताकतें मजबूत हुई और 1930 के दशक के एकदम शुरू में यूरोप के सिर्फ चंद देश ही अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं की तथा लोकतांत्रिक सरकारों की रक्षा कर पाए थे। हंगरी में एक निरंकुश सरकार सत्ता में आई, इसका रीजेंट होर्थी था। रूमानिया और यूगोस्लाविया में निरंकुश राजतंत्र शासन में आया। जोसेफ पिल्स्दस्की के अंतर्गत पोलैण्ड में एक अधिनायकवादी सरकार कायम की गई। ग्रीस में राजतंत्रीय सरकार की सत्ता पुनः स्थापित हो चुकी थी, वहाँ कई साल तक राजनितिक परिस्थतियाँ डाँवाडोल बनी रहीं। राजा बदलते रहे और सेना के जनरल तख्ता पलटने का खेल खेलते रहे। जोनेस मेटाक्सास के नेतृत्व में 1936 में वहाँ एक फासीवादी तानाशाही सरकार स्थापित की गई। स्पेन में राजतंत्र था। वहाँ 1923 में जनरल मिगनेल प्राइमो द रिवेरा ने सैनिक तानाशाही की स्थापना की थी। यह तानाशाही 1930 तक चली थी और 1931 में जब राजतंत्र विरोधी ताकतें भारी बहुमत से चुनाव में विजयी हुई, स्पेन एक गणतंत्रात्मक राज्य बन गया। इस दौरान सबसे गंभीर घटना इटली में फासीवादी तानाशाही सरकार की स्थापना थी। इस पर हम अलग से विचार करेंगे। जिन देशों ने निरंकुशतावादी सरकार का मार्ग प्रशस्त नहीं किया उनमें स्कैण्डनेविया के देशों के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस और चेकोस्लोवाकिया शामिल हैं। लेकिन इन देशों ने भी गंभीर समस्याओं का सामना किया। 1921 में ब्रिटेन में लगभग 20 लाख लोग बेरोजगार थे। 1923 के आम चुनाव में लेबर पार्टी की विजय हुई। यह दल बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए कदम उठाने, प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीकरण करने, धनी वर्ग पर भारी कर लगाने, मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने, बड़े पैमाने पर मकान बनाने का कार्यक्रम चलाकर आवास की कमी दूर करने के लिए अभियान चला रहा था। लेकिन लेबर की सरकार 1924 की शुरूआत में सत्ता में आई और अधिक दिनों तक सत्ता में टिक नहीं पाई। इसने बहुत थोड़े से वादे पूरे किए। इस दौर में फ्रांस की सरकार में बड़े-बड़े उद्योगपतियों और बैंक मालिकों का प्रभुत्व था। यूरोप की महत्वपूर्ण शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा का यह शिकार थी। इसके लिए जर्मनी के संसाधनों पर कब्जा करने की इसने कोशिश की। चेकोस्लोवाकिया दुनिया के नक्शे पर नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। इसको गणतंत्र घोषित किया गया था। तथा टामस मसरीक इसके राष्ट्रपति बने थे। 1919 में चेकोस्लोवाकिया ने लोकतांत्रिक संविधान स्वीकार किया था और इस देश में कई महत्वपूर्ण सुधार लागू किए गए। जबकि दो विश्व युद्धों के बीच और दक्षिणी यूरोप के अधिकांश देश आर्थिक दृष्टि से पीछे रह गए थे। चेकोस्लोवाकिया तेज औद्योगिक विकास के दौर से गुजरा। 1919 में जर्मनी संसदीय गणतंत्र कहा जाता है। वेमार एक स्थान का नाम है जहाँ पर संविधान सभा की बैठक हुई थी और नए संविधान की घोषणा की गई थी। इस संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्रपति का प्रावधान था जिसके अनेक विशेषाधिकार थे। एक चांसलर की व्यवस्था थी जो संसद (जिसे रीचस्टैग कहा जाता था) के प्रति उत्तरदायी था जिसका निर्वाचन आम वयस्क मताधिकार द्वारा किया जाता था। उस संविधान में आम जनता के अधिकार तथा स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भी प्रावधान थे। ‘थोपी गई शांति‘ के विरूद्ध जर्मनी में भारी असंतोष व्याप्त था और इसके अधिकांश प्रावधान सार्वभौम रूप से अन्यायपूर्ण माने गए थे। इसके बावजूद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और कम्युनिस्ट बड़ी ताकत के रूप में उभरी यद्यपि इन दोनों ने आक्रामक राष्ट्रवाद का विरोध किया था। 1930 तक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जर्मनी की शासक पार्टियों में थी। 1923 में कम्युनिस्ट पार्टी ने जर्मनी में क्रांति करने का एक और प्रयास किया था। लेकिन इसको सफलता हाथ नहीं लगी थी। इस बीच निरंकुशतावादी गुट उभरने लगे। इन लोगों ने लोकतंत्र की भर्त्सना करनी शुरू की, वारसाई की संधि को छोड़ने की वकालत की, युद्ध की प्रशंसा की तथा लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए षड्यंत्र रचे ताकि कोई तानाशाही व्यवस्था लागू की जा सके। बड़े उद्योगपतियों तथा जर्मन सेना के एक बहुत बड़े हिस्से ने इनका समर्थन किया। युद्ध में जर्मनी की पराजय के लिए उन्होंने यहूदियों और कम्युनिस्टों को जिम्मेदार ठहराया। उनके प्रभाव से देश को मुक्त करने के लिए उन्होंने संगठित रूप से आतंक फैलाया और लोगों की हत्या की। सत्ता पर कब्जा करने के लिए 1920 में एक षड़यंत्र रचा गया। षड्यंत्रकारी संगठन के स्वयंसेवकों ने बर्लिन पर अधिकार कर लिया। सेना में इनके समर्थक लोगों ने भी इस काम में उनकी मदद की। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार भंग कर दी गई तथा ’काण’ के अंतर्गत एक नई सरकार को सत्ता में बैठा दिया गया। इस घटना से सभी लोकतांत्रिक और समाजवादी पार्टियाँ एकजुट हो गईं। जर्मनी में आम हड़ताल हुई और षड्यंत्रकारियों से लड़ने के लिए मजदूरों न अपने को हथियारों से लैस किया। ’पुश्चिस्ट’ लोगों को तत्काल सत्ता से हटा दिया गया। 1919 में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी (संक्षिप्त नाम नाजी पार्टी) स्थापित की गई। एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में इस पार्टी ने भी 1923 में सत्ता पलटने की कोशिश की लेकिन इसको दबा दिया गया। वाइमार गणतंत्र ने गंभीर आर्थिक समस्याओं का सामना किया यद्यपि इसने जर्मनी में लोकतांत्रिक सरकार बनाने में सफलता हासिल की थी। वारसाई की संधि के कुछ प्रावधानों और कुछ अन्य यूरोपीय शक्तियों के रूख के चलते ये समस्या और उग्र हो गई। मित्र राष्ट्रों को जर्मनी द्वारा दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि 6600 मिलियन पौंड निर्धारित की गई थी। 1921 में उसने इस हर्जाने की पहली किश्त 50 मिलियन पौण्ड अदा की लेकिन अगली किश्त अदा करने में वह असमर्थ था। इस वायदे को पूरा करने के लिए जर्मनी के पास संसाधन नहीं थे। इस बीच जर्मनी की अर्थव्यवस्था ढहने के कगार पर पहुँच गई। इसकी वजह अकल्पनीय मुद्रास्फीति थी। 1921 के समाप्त होते-होते जर्मनी की मुद्रा मार्क का मूल्य 50 गुना नीचे आ गया। पहले एक पौण्ड में 20 मार्क हुआ करते थे अब एक पौण्ड में 1000 मार्क मिलने लगे। 1922 में इसका और अवमूल्यन हो गया। जनवरी 1923 में बेल्जियम तथा फ्रांस की फौजों ने रूहर घाटी पर कब्जा कर लिया। यह घाटी जर्मनी के कोयला और धातु उद्योग का केंद्र था। कोयला तथा इस्पात पर कब्जा करके अपने हर्जाने को वसूल करना इसका उद्देश्य था लेकिन जर्मनी के मजदूरों ने उनसे सहयोग करने से मना कर दिया। विरोध में उन्होंने हड़ताल कर दी। उन्होंने शांतिपूर्वक प्रतिरोध का सहारा लिया। उनकी सरकार ने इसमें उनका समर्थन किया। जर्मनी की सरकार काफी अधिक संख्या में कागजी मुद्रा छापने लगी, इससे विनाशकारी स्थिति उत्पन्न हो गई। 1923 तक जर्मन मुद्रा एक दम व्यर्थ हो गई। ब्रिटेन के एक पौण्ड का मूल्य पचास हजार मिलियार्ड मार्क हो गया। (एक मिलियार्ड =एक हजार मिलियन)। 1923 के अंत तक मुद्रा सुधार लागू किया गया। इस स्थिति में उसके अलावा और कोई चारा नहीं था लेकिन जर्मन जनता के कई तबकों के लिए इसके विनाशकारी नतीजे निकले। एक नई मुद्रा शुरू की गई। इसका अर्थ यह था कि लाखों लोगों की जिंदगी भर की बचत पर पानी फिर गया। इससे सबसे अधिक प्रभावित, मध्यवर्ग, निम्न मध्यवर्ग तथा वेतन भोगी लोग थे। लाखों लोग अचानक अकिंचन हो गए। इस भंयकर स्थिति से सबसे ज्यादा लाभ नाजी पार्टी को हुआ। अपनी परेशानी के हल की तलाश में बहुत से लोगों ने इस पार्टी का मुँह जोहना शुरू किया। इस बीच क्षतिपूर्ति की समस्या को एक अन्य योजना के तहत सुलझाने की कोशिश की गई। इसको डेब्स योजना (इसका नाम अमरीकी जनरल डेब्स के नाम पर पड़ा है। वे बहुराष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष थे जो इस समस्या की समीक्षा के लिए बनाई गई थी) कहा जाता है। युद्ध के दौरान सारे मित्र राष्ट्रों ने संयुक्त राज्य अमरीका से ऋण लिया था तथा संयुक्त राज्य अमरीका दुनिया में सबसे बड़े ऋण दाता देश के रूप में सामने आया था। इससे पता चलता है कि यूरोप किस सीमा तक संयुक्त राज्य अमरीका पर निर्भर था। अधिकांश देश यदि और कर्ज न लेते तो कर्ज की रकम अदा करने की स्थिति में नहीं थे। डेब्स योजना के अंतर्गत जर्मनी ने अमरीका से बहुत अधिक कर्ज लिया, साथ में उसने दूसरे देशों से भी कर्ज लिए तथा ऊँची किश्तों में क्षतिपूर्ति की रकम देने का वायदा किया। इन भुगतानों को 1988 तक पूरा किया जाना था। इन कर्जों से जर्मनी को अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण आरंभ करने में मदद मिली। उसने क्षतिपूर्ति की किश्तें भी अदा करनी शुरू कर दीं। 1932 में अंतिम रूप से इन भुगतानों को रोक दिया गया क्योंकि उस समय विश्वव्यापी आर्थिक संकट के कारण जर्मनी और अन्य देशों की अर्थव्यवस्था लगभग नष्ट हो चुकी थी। लेकिन इस बीच अधिकांश यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था में थोड़ा सुधार आया लेकिन यह सुधार कुछ ही सालों तक कायम रहा। इससे संयुक्त राज्य अमरीका पर यूरोप की बढ़ती हुई निर्भरता भी उजागर हुई। यूरोप के दूसरे देशों की तरह युद्ध के बाद वाले वर्षों में इटली में भी जबर्दस्त बेरोजगारी रही और काफी जन-आंदोलन हुए। समाजवादी आंदोलन काफी शक्तिशाली होकर उभरा था, यद्यपि अनेक आंतरिक विभाजनों के चलते उसकी प्रभाव शक्ति कमजोर पड़ गई थी। इसी बीच एक जबर्दस्त उग्र लोकतंत्र-विरोधी फासीवादी आंदोलन इटली में उठ खड़ा हुआ। लोगों में दहशत पैदा करने के लिए सशस्त्र गुट बनाए गए। इनको ’फासेज’ कहा जाता था। मुख्य रूप से समाजवादियों, कम्युनिस्टों तथा मजदूर-किसान आंदोलनों के नेताओं को ये अपना शत्रु मानते थे। प्राचीन रोमन साम्राज्य की महान् कीर्ति से इनको प्रेरणा मिलती थी तथा इटली की महानता को वापस लेने के लिए ये लोग हिंसा और युद्ध की शिक्षा देते थे। देश के शासक वर्ग ने युद्ध में अपने देश को मित्र राष्ट्रों के पक्ष में रखा था। उनको ऐसा लगा कि युद्ध के अंत में उनके साथ धोखा किया गया है। मित्र राष्ट्र इटली की औपनिवेशिक शक्ति अर्जित करने की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं कर पाए। यद्यपि आस्ट्रिया की कीमत पर यूरोप में उसे कुछ भाग मिले लेकिन जिन उपनिवेशों को पाने की उसमें आकांक्षा थी, वे उसे नहीं मिल सके। अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए इटली के शासक वर्ग को फासीवादी आंदोलन के रूप में एक हथियार मिल गया। देश के भीतर उन्हें समाजवादी-क्रांति से उबारने वाली एक मात्र शक्ति फासीवादी आंदोलन को माना गया। 1921 में बानितो मुसोलिनी के नेतृत्व में ’नेशनल फासिस्ट पार्टी’ का गठन हुआ। हजारों की संख्या में काली कमीज वाले सदस्यों की भर्ती की गई ताकि हड़तालें तोड़ी जा सकें तथा समाजवादी और कम्युनिस्ट नेताओं की हत्या कराई जा सके। फासीवादी आंदोलन की लोकप्रियता इन हथियारबंद गिरोहों तथा शासक वर्ग अर्थात् उद्योगपतियों और भूस्वामियों से अधिक आगे नहीं बढ़ सकी। लेकिन हड़तालों को तुड़वाने और प्रदर्शनों को रोकने में उन्हें सफलता मिली। इनका आयोजन बढ़ते हुए फासीवाद खतरे के खिलाफ किया जाता था। बढ़ती हुई फासीवादी हिंसा के प्रति चुप्पी साधकर सरकार मूक दर्शक बनी रही। 1919 में संसद में फासीवादियों को एक भी स्थान नहीं मिला। 1921 में उनको पैंतीस स्थान मिले। लेकिन फासीवादियों को जनसमर्थन न मिलने के बाद भी इटली के शासक वर्ग ने उनके साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। फासीवादीयों ने जबरन बोलोगना और मिलान शहरों पर कब्जा कर लिया। 24 अक्टूबर 1922 को उन लोगों ने रोम के लिए यात्रा का एक कार्यक्रम बनाया। इन सशस्त्र यात्राओं को कुचलने के बजाए सरकार ने उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इटली के राजा ने मुसोलिनी को आमंत्रित किया यद्यपि मुसोलिनी ने इस यात्रा में भाग नहीं लिया था और उससे सरकार बनाने के लिए कहा गया। उसने तत्काल निरंकुश सत्ता अपने हाथ में ली तथा ‘काली कमीज वाले’ लोगों द्वारा जबर्दस्त आंतक फैलाया गया। इस आतंक और दहशत के बीच 1924 में चुनाव कराए गए। चुनाव के दौरान फासिस्ट लोगों द्वारा की गई हिंसा के खिलाफ संसद में जब समाजवादी नेता गियाकोमो मैतिऔत्ती ने भाषण दिया, तो उसकी हत्या कर दी गई। इसके तत्काल बाद सुनियोजित रूप से समाजवादियों, कम्युनिस्टों तथा दुसरे राजनीतिक विरोधियों की हत्याएँ की गई और 1926 में सभी गैर-फासीवादी संगठन और दल गैर कानूनी घोषित कर दिए गए तथा उनको भंग कर दिया गया। इटली के फासीवादियों ने जो तरीके अपनाए उनकी नकल दूसरे देशों में भी की गई, कुछ देशों में इनको सफलता भी मिली। 1924 से 1936 के बीच यूरोप1924 से महामंदी के बीच का समय आमतौर पर आर्थिक पुनर्स्थापना और आर्थिक संवृद्धि का दौर था। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से पैदा हुए सामाजिक तनावों पर काबू नहीं पाया जा सका, हालाँकि मौजूदा व्यवस्था को क्रांतिकारी तरीके से समाप्त करने का खतरा टल गया था।1920 के दशक के मध्य में आर्थिक पुनर्स्थापना का समय प्रारंभ हुआ था, वह आकर 1929 में खत्म हो गया। 1929-30 के बीच की अवधि को ’दुःस्वप्न’ की शुरूआत का समय कहा गया है, जो 1933 तक चला उसके बाद दुबारा आर्थिक पुनर्स्थापना का समय शुरू हो गया। यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं का संकट महामंदी का सीधा नतीजा था। इस महामंदी ने संयुक्त राज्य अमरीका को 1929 में ग्रस लिया था। इससे यह भी दिखा कि यूरोप कितना अधिक संयुक्त राज्य अमरीका पर निर्भर हो चुका है। यूरोप के लिए अमरीकी ऋण पूरी तरह रोक दिए गए। इससे उन अर्थव्यवस्थाओं को सबसे अधिक आघात लगा जो लगातार ऋण की आपूर्ति के कारण विकसित हुई थी और जर्मनी भी इस तरह के प्रभावित देशों में था। इस समय संयुक्त राज्य अमरीका में औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद होने लगे थे और लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे। उन्हें नौकरियों से बाहर निकाल दिया गया था। 1932 में जर्मनी में लगभग साठ लाख लोग बेकार थे और लगभग आधी आबादी दरिद्र हो गई थी। ब्रिटेन में बेरोजगारों की संख्या तीस लाख के आसपास थी। यूरोप के जो देश मूलतः कृषि प्रधान रह गए थे, वे भी बुरी तरह प्रभावित हुए थे अपनी सारी कृषि उपज के लिए वे निर्यात पर निर्भर थे। कृषि उत्पादों की कीमतों में तेजी से गिरावट आने के कारण उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हुई थी। हर देश ने विदेश से आयात पर रोक लगा रखी थी, जिसके काफी गंभीर नतीजे हुए थे। यूरोप में आर्थिक संकट का लोकतंत्र पर काफी घातक राजनीतिक असर पड़ा था। इस काल के समाप्त होने के पहले ही यूरोप के अधिकांश देशों में निरंकुश, अर्धफासीवादी, फासीवादी शक्तियाँ सत्ता में आ चुकी थीं। यहाँ तक कि जिन देशों में लोकतंत्र बचा हुआ था, वहाँ भी फासीवादी शक्तियों को ताकत मिल रही थी। जर्मनी में आधुनिक युग की सर्वाधिक बर्बर सरकार सत्ता पर काबिज हो चुकी थी। इस अवधि की समाप्ति के करीब यूरोप और विश्व पुनः युद्ध की स्थिति में लौटने लगे थे। जनवरी 1924 में पहली लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आई जिसने यह वायदा किया था कि अर्थव्यवस्था में वह आमूल सुधार लाएगी। यह सरकार कुछ कर नहीं पाई और दस महीने में ही इसके शासन का अंत हो गया। एक जाली चिट्ठी भय पैदा करने के लिए लिखी गई थी। इस पत्र की लेबर पार्टी की हार में अहम भूमिका थी। जीनोविएव के नाम से एक जाली पत्र तैयार किया गया था जो उस समय कोमिनटर्न के अध्यक्ष थे। इस पत्र में ब्रिटिश कम्युनिस्टों को ब्रिटेन में विद्रोह करने और ब्रिटिश सेना और नौ सेना में तोड़ फोड़ की कार्रवाई के लिए हिदायत दी गई थी। अक्टूबर में कनजर्वेटिव पार्टी सत्ता में आई जिसने लेबर पार्टी पर आक्रमण करने के लिए जाली पत्र का उपयोग किया था जिसमें लेबर पार्टी पर कम्युनिस्टों के साथ दोस्ताना संबंध का आरोप लगाया गया था। यह पार्टी 1929 एक सत्ता में बना रही। ब्रिटेन के इतिहास में सबसे बड़ी हड़ताल इसी काल में हुई थी यद्यपि यह हड़ताल अंततः असफल रही। मई 1926 में मजदूरी में कटौती तथा काम के घण्टों में बढ़ोत्तरी की धमकी के विरोध में ब्रिटेन के खान मजदूरों ने हड़ताल कर दी। ब्रिटिश सरकार ने पूरी तरह खान के मालिकों का पक्ष लिया। 4 मई 1926 को तीस लाख मजदूरों ने खान मजदूरों के समर्थन में काम बंद रखा। इनमें रेल कर्मचारी, परिवहन कर्मचारी, इस्पात के कारखानों के मजदूर तथा कई अन्य उद्योगों में काम करने वाले मजदूर शामिल थे। इसको ’आम हड़ताल’ के नाम से जाना जाता है। इस हड़ताल ने सरकार को चौंका दिया। इससे ब्रिटेन के उद्योगपति भी चौंक उठे थे। इसको तोड़ने की हर तरह से कोशिश की गई सरकार के शत्रुतापूर्ण रवैये के कारण तथा सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर इसके खिलाफ प्रचार करके जनता में इस हड़ताल के विरूद्ध उत्तेजना फैलाने के कारण 12 मई को यह हड़ताल वापस ले ली गई। बहरहाल, खान मजदूरों की हड़ताल कई महीने चली लेकिन इसका अंत पूर्ण असफलता में हुआ और मजदूरों को घटी दर पर मजदूरी लेकर काम पर जाने के लिए मजबूर किया गया। उनके काम के घण्टे भी बढ़ाए गए। इसके बाद सरकार ने आम हड़तालों को गैर कानूनी घोषित कर दिया। 1929 में लेबर पार्टी पुनः सत्ता में लौटी लेकिन लेबर पार्टी की सरकार ने श्रमिक विरोधी कानूनों को वापस लेने के लिए कोई नहीं उठाया। ऐसे कानून जो हड़तालों की असफलता के बाद बनाए और लागू किए गए थे। जब ब्रिटेन आर्थिक संकट की चपेट में आया तो मजदूरी में कटौती तथा बेरोजगारी भत्ते की दर में कमी और अन्य कई कल्याणकारी कार्यक्रमों के खर्चों में कटौती करके लेबर पार्टी के प्रधान मंत्री ने इस संकट से उबरने की कोशिश की। अधिकांश मंत्रियों ने उसकी बात मानने से इनकार किया और उसने इस्तीफा दे दिया जिससे नई सरकार बनाई जा सके। इसे राष्ट्रीय सरकार कहा गया। इस सरकार में ज्यादातर मंत्री कंजर्वेटिव पार्टी के थे। राष्ट्रीय सरकार को समर्थन देने वाली पाटियाँ 1935 के चुनावों के बाद भी सत्ता में बनी रहीं लेकिन उनका बहुमत घट गया था। लेबर पार्टी की ताकत बढ़ी और 1935 के चुनावों में इसे अस्सी लाख मत प्राप्त हुए। इस बीच ब्रिटेन में एक फासीवादी आंदोलन का उदय हो चुका था जो यहूदियों के विरूद्ध हिंसा के प्रयोग की वकालत करता था। इसने दंगे कराए और अव्यवस्था फैलाई। 1933 के बाद ब्रिटेन आर्थिक संकट से उबरने लगा था यद्यपि बेरोजगारों की संख्या अभी भी लगभग 15 लाख बनी रही। उपनिवेशों में राष्ट्रवादी आंदोलनों की बढ़ती हुई ताकत के कारण इस दौर में ब्रिटेन की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा घटी। 1931 में ब्रिटेन के सारे श्वेत उपनिवेश पूर्णतः स्वतंत्र हो गए। आज जिसे राष्ट्र कुल कहा जाता है, ये राष्ट्र उसके सदस्य भर बने रहे, लेकिन उन पर कोई ब्रिटिश कानून लागू नहीं होता था। अपनी स्वतंत्र नीतियाँ उन्होंने निर्धारित करनी शुरू कीं। 1936 तक फासीवादी देशों ने आक्रमण कर युद्ध की शुरूआत कर दी थी जिसके कारण दूसरे विश्व युद्ध का विनाश घटित हुआ। अन्य पश्चिमी देशों की तरह ब्रिटिश सरकार ने भी फासीवाद को संतुष्ट करने की नीति अख्तियार की यद्यपि फासीवाद विरोधी पार्टियों और संगठनों ने इस नीति के भयंकर नतीजों के विरूद्ध आम जनता को जागृत करने का प्रयास किया। फ्रांस में यह अस्थिरता का समय था। यूरोप का प्रभावशाली राष्ट्र बनने की फ्रांस की महत्वाकांक्षा थी इसलिए शस्त्रास्त्र निर्माण का बहुत बड़ा कार्यक्रम उसने शुरू किया था। इसका जिक्र किया जा चुका है कि जर्मनी के रूहर घाटी में उसके कोयला और इस्पात उद्योग पर फ्रांस ने अधिकार कर लिया था। डेब्स योजना के कार्यान्वयन के बाद फ्रांस को रूहर घाटी से हटना पड़ा। फ्रांस की सरकार में व्यापारी वर्ग तथा भ्रष्ट राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व था और दोनों में जबर्दस्त साठगाँठ थी। यह हर महीने बनती और गिरती थी। आर्थिक संकट के दौरान बेरोजगारों की संख्या बढ़कर 15 लाख के करीब पहुँच गई तथा कृषि और औद्योगिक, दोनों ही क्षेत्रों में उत्पादन 30 प्रतिशत गिर गया। इस दौर में समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टियों की शक्ति में वृद्धि हुई। लेकिन इसी समय एक शक्तिशाली फासीवादी आंदोलन भी उठा खड़ा हुआ और सत्ता पर कब्जा करने के लिए हिंसक और आतंक का तरीका अख्तियार किया। 1933 में एक भारी घोटले ने फ्रांस को हिला दिया। अलैक्जेंडर स्टाविस्की नाम के एक सटोरिया ने जनता को ठग कर और धोखाधड़ी से छः सौ मिलियन फ्रैंक (फ्रांस की मुद्रा) कमाया था। जब इस घोटाले का रहस्य खुला तो पता चला कि कई राजनीतिक लोग इसमें शामिल थे जिनमें कुछ तो महत्वपूर्ण सरकारी पदों की शोभा बढ़ाने वाले व्यक्तित्व थे और ये लोग स्टाविस्की के लाभ में भागीदार थे। इस घोटाले का उपयोग कर फासीवादी लोगों ने पेरिस पर कब्जा करने, सरकार को भंग करने और सत्ता हथियाने की कोशिश की। लेकिन समाजवादियों और कम्युनिस्टों ने मजदूरों को लामबंद कर फासीवादियों को पेरिस पर कब्जा नहीं करने दिया। फासीवादियों और मजदूरों के बीच उग्र संघर्ष हुए और फासीवादियों का सत्ता पर अधिकार करने का प्रयास विफल कर दिया गया। 1936 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। फासीवादी खतरे का मुकाबला करने के लिए तथा बहु प्रतीक्षित आर्थिक सुधार के लिए (जिसमें मजदूरों के कल्याणकारी कार्यक्रम शामिल थे) एक व्यापक जन मोर्चा बनाया गया जिसमें सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी शामिल हुई थीं। जन मोर्चे की चुनावों में भारी विजय हुई और लिओन ब्लुम के नेतृत्व में सोशलिस्ट और रेडिकल सोशलिस्ट पार्टियों ने मिल कर सरकार बनाई। यह सरकार लगभग एक वर्ष तक चली और इसको कम्युनिस्ट पार्टी का भी समर्थन प्राप्त था। इसने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए-हथियार निर्माण उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, वेतन और मजदूरी में की जाने वाली कटौती को समाप्त कर दिया गया तथा मजदूरों के लिए सप्ताह में चालीस घण्टे काम के बाँधे गए। फ्रांस की विदेश नीति के उद्देश्य इस प्रकार थे - महान शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा की पूर्ति तथा किसी भी संभावित जर्मन आक्रमण के खतरे से बचाव। उसने ऐसे समझौतों को प्रोत्साहित किया जिसे ’छोटा समझौता’ कहा जाता है। इसके अंतर्गत उसने रूमानिया, यूगोस्लाविया और चैकोस्लोवाकिया के साथ समझौते किए तथा इस उम्मीद में उनको हथियार दिए कि यदि भविष्य में जर्मनी ने उसके विरूद्ध आक्रमण किया तो वह फ्रांस पर केंद्रित नहीं हो पाएगा, ये देश उसकी मदद करेंगे तथा जर्मनी की शक्ति कई मोर्चों पर बँट जाएगी। 1920 दशक में फ्रांस ने अपनी सुरक्षा को सुदृढ़ करना आरंभ किया था ताकि फ्रांस की धरती पर जर्मनी को बढ़ने से तत्काल रोका जा सके जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। इस सुरक्षा प्रणाली को मैगिनो लाइन के नाम से जाना जाता था। 1935 में फ्रांस ने सोवियत संघ के साथ आपसी मदद के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया और सोवियत संघ ने फ्रांस के सहयोगी चैकोस्लोवाकिया के साथ इस प्रकार के समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस तरह एक प्रकार से त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। जब जन मोर्चा (पॉपुलर फ्रंट गवर्नमेंट) सरकार गठित हुई तो उम्मीद की गई थी कि फासीवादी आक्रमण के विरूद्ध फ्रांस का रूख प्रत्यक्ष और स्पष्ट होगा। लेकिन जन मोर्चा की सरकार 1938 में भंग हो गई। इसके बाद जो सरकार सत्ता में आई उसके नेता एडुअर्ड डैलेडियर थे। फासीवादी देशों को प्रसन्न करने की ब्रिटिश नीति का फ्रांस की नई सरकार ने अनुसरण किया। इस प्रकार अपने सहयोगी मित्र चेकोस्लोवाकिया के साथ धोखा किया। पूर्व में उल्लिखित किया जा चुका है कि हंगरी, पोलैंड, रूमानिया, यूगोस्लाविया तथा और कई देशों में निरंकुश तथा अर्ध-फासीवादी सरकारें सत्ता पर काबिज थीं। सेना की मदद से 1930 के दशक में पुर्तगाल में सालाजार ने फासीवादी तानाशाही सरकार कायम की थी। इटली और जर्मनी की फासीवादी सरकारों के प्रति उसका रूख सहानुभूतिपूर्ण था और ब्रिटेन के साथ दोस्ताना संबंध बरकरार रखते हुए भी स्पेन की रिपब्लिक पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने में उसने मदद की थी। अपने को गणतंत्र घोषित करने के बाद स्पेन को कई दिक्कतों से गुजरना पड़ा। 1932 में एक फौजी जनरल के नेतृत्व में एक विद्रोह हुआ था जिसको दबा दिया गया था। इस दौरान ’फैलांज’ नाम का फासीवादी आंदोलन बढ़ने लगा था और कैथोलिक चर्च ने इसका समर्थन किया था। स्पेन के फासीवादी संगठन राजनीतिक हत्याएँ आयोजित करते थे और इनके कई समर्थक सेना में भी थे। मुसोलिनी ने राजतंत्रवादियों तथा फासीवादियों की मदद का वायदा किया था। फासीवादविरोधी शक्तियों को एकजुट करने के लिए एक विद्रोह भी हुआ था जो बाद में कुचल दिया गया था। अक्टूबर 1935 में आस्टुरिया के खान मजदूरों ने विद्रोह कर दिया था और जनरल फ्रैंसिस्को फ्रैंको को बदनाम सरकार के विरोध में हुए इस विद्रोह को दबाने के लिए कहा गया। 1936 में स्पेन में चुनाव हुए। जो जन मोर्चा (पॉपुलर फ्रंट) फासीवादी खतरे को रोकने के लिए बनाया गया था, इन चुनावों में उसकी विजय हुई। इसमें सभी समाजवादी पार्टियाँ, कम्युनिस्ट पार्टी, अराजकतावादी दल तथा वातपंथी रिपब्लिकन दल शामिल थीं। जन मोर्चा सरकार ने हजारों की संख्या में राजनीतिक बंदियों को रिहा किया तथा प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक सुधारों की शुरूआत हुई। लेकिन थोड़े दिनों बाद स्पेन गृह युद्ध की लपेटों में आ गया जब स्पेन के फासीवादी फ्लांगे नाम के संगठन ने रिपब्लिकन सरकार का तख्ता पलटने के उद्देश्य से सेना के जनरलों और विदेश की फासीवादी सरकारों की मदद ली। गृह युद्ध तथा उसके परिणामों का वर्णन हम पृथक रूप से करेंगे। इस दौरान की सबसे बड़ी और गंभीर घटना थी - जर्मनी में फासीवाद की विजय। हम पहले नाजी पार्टी के गठन और पुत्श में उसके प्रयासों की चर्चा कर चुके हैं, यह प्रयास उसी प्रकार का था जैसा इटली में सत्ता हथियाने के उद्देश्य से मुसोलिनी ने किया था। युद्धोत्तर मुद्रा स्फीति और 1929 के आर्थिक संकट से पैदा हुई भयंकर कठिनाइयों की चर्चा हम कर चुके हैं। नाजीवाद (जर्मन फासीवाद का रूप ) फासीवाद का सबसे बर्बर और घिनौना रूप था। इटली के फासीवाद की तरह नाजीवाद भी राजनीतिक लोकतंत्र और नागरिक स्वाधीनता से घृणा करता था तथा युद्ध का महिमा मण्डन करता था। जैसे इटली के फासीवादी रोमन साम्राज्य के गौरव को लौटाना चाहते थे, उसी प्रकार जर्मनी के नाजी टेम्पटोनिक साम्राज्य की महानता को पुनरूज्जीवित करना चाहते थे। नाज़ी लोग सामी विरोधी (एंटी सेमेटिक) भावनाओं को उत्तेजित करते थे-यहूदियों के प्रति घृणा का प्रचार करते थे गैर यहूदी जर्मन लोगों में इस बात का प्रचार किया जाता था कि जर्मनी की पराजय के लिए यहूदी लोग जिम्मेदार हैं। जर्मनवासियों के सारे दुःखों-कठिनाइयों के लिए यहूदियों को उत्तरदायी ठहराया जाता था। उन्होंने जर्मन जाति की शुद्धता का गुणगान किया। इसे उन्होंने ’शुद्ध सौम्य आर्य’ की संज्ञा दी और दूसरी नस्ल के लोगों से इसे श्रेष्ठ माना और इसलिए यह भी माना कि दूसरों पर शासन करने का इस जाति (नस्ल) को अधिकार है। जर्मन जाति के सारे लोगों को एक राज्य में संगठित करना इन्होंने अपना लक्ष्य माना ताकि ’वृहत्तर जर्मनी’ का निर्माण किया जा सके तथा ’अपने लोगों के पालन पोषण और अतिरिक्त आबादी को बसाने के लिए भू-भाग’ का दावा किया। एक महान नेता के विचार को बढ़ावा दिया गया, ऐसा महान नेता जो सारी गड़बड़ियों को दुरूस्त कर देगा और जर्मनी को महानता की ऊँचाई तक ले जाएगा। कम्युनिज्म (साम्यवाद) नाजियों की दृष्टि में उनका सबसे बड़ा दुश्मन था और इसका विनाश उनका मुख्य उद्देश्य था। युद्ध में पराजय से जर्मन जनता के मन में अपमान बोध पैदा हुआ था। इस अपमान बोध का नाजियों ने इस्तेमाल किया। जर्मन जनता को बताया गया कि उनके ऊपर शांति जबरन लादी गई है। शांति संधि की कई धाराएँ न्यायोचित नहीं हैं। इन धाराओं में युद्ध अपराध स्वीकारना तथा हरजाने के रूप में मोटी रकम की अदायगी जैसी बातें भी शामिल थीं। नाजियों ने वायदा किया कि वे जर्मन जनता का खोया हुआ राष्ट्रीय सम्मान उन्हें वापस दिलाएँगे। इन विचारों को सेना में भी काफी समर्थन मिला क्योंकि इसके बड़े अधिकारी अधिकांशतः बड़े जमींदार परिवारों के हुआ करते थे। ये अपनी हार का बदला लेना चाहते थे। इन सब के ऊपर, नाजियों को जर्मनी के उद्योगपतियों से भी पूरा समर्थन मिला क्योंकि वे समाजवादी तथा कम्युनिस्ट पार्टियों की बढ़ती हुई ताकत से चौंक गए थे। इनसे नाजी लोग ही उनकी रक्षा कर सकते थे। इटली के फासीवादियों की तरह नाजी लोगों ने भी सशस्त्र स्वयं-सेवकों के गिरोह बनाए थे, जिन्हें ’एस. ए.’ कहा जाता था। इसको आम लोग ’भूरी कमीज वाले’ नाम से जानते थे। इनके द्वारा फासीवाद विरोधी और यहूदी लोगों की हत्या की वारदातें दिनों दिन बढ़ती चली गई। उनकी जायदादें नष्ट की गई और तरह-तरह से उनको सरेआम अपमानित किया गया। 1930 तक ‘भूरी कमीज वालों’ की संख्या एक लाख हो गई। नाजियों (भूरी कमीज वाले) और कम्युनिस्टों के बीच बहुधा उग्र तथा हिंसक टकराव होते थे लेकिन नाजियों की बढ़ती हुई नृशंसता को रोकने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन 1929 के आर्थिक संकट के पूर्व नाजियों को बहुत सीमित जन समर्थन हासिल था। 1928 में जर्मन संसद ’रीचस्टैग’ में उनको कुल 12 स्थान मिले थे और उनको कुल 8 लाख मत मिले थे। इसके विपरीत सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को 90 लाख मत मिले थे और 30 लाख से अधिक मत कम्युनिस्ट पार्टियों के उम्मीदवारों को प्राप्त हुए थे। लेकिन 1930 के निर्वाचन में नाजियों को प्राप्त मतों की संख्या बढ़ कर तकरीबन 65 लाख पहुँच गई जबकि सोशल डेमोक्रेटिक दल के मतों की संख्या 85 लाख और कम्युनिस्टों को 45 लाख मत प्राप्त हुए। 1932 में राष्ट्रपति के चुनाव हुए। इसमें फील्ड मार्शल पॉल वान हिंडन बर्ग प्रत्याशी थे। इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन सेना का नेतृत्व किया था और जब अस्सी वर्ष के करीब उनकी आयु हो गई थी। इस निर्वाचन में वे राष्ट्रपति चुने गए तथा उनको एक करोड़ पच्चीस लाख मत मिले थे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने इनका समर्थन किया था। हिटलर को इसमें एक करोड़ दस लाख मत मिले थे और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी अंर्स्ट तालमान को 37 लाख के ऊपर मत प्राप्त हुए थे। जुलाई 1932 में जर्मन संसद रीचस्टैग के लिए चुनाव हुए। नाजी पार्टी अकेली सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। उसे 1 करोड़ 37 लाख मत मिले। इसके विपरीत डेमोक्रेटिक पार्टी को 80 लाख और कम्युनिस्ट प्रत्याशियों को 52 लाख मत मिले थे। उसी वर्ष नवंबर में जर्मन संसद के लिए दूसरा चुनाव हुआ जिसमें नाजियों को 20 लाख कम मत मिले तथा कम्युनिस्टों के मत बढ़कर 60 लाख हो गए। लेकिन इस समय दूसरी शक्तियाँ भी काम कर रहीं थीं जो नाजियों को सत्ता में लाईं थीं। 30 जनवरी 1933 में हिंडेन बर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया। इस प्रकार हिटलर का सत्ता में प्रवेश न तो चुनावों में उसकी विजय के कारण हुआ और न मौजूदा सरकार का हिंसक तरीके से तख्ता पलटकर उसे सत्ता में बैठाया गया बल्कि यह चोरी से पर्दे के पीछे किए गए दक्षिण पंथी राजनीतिकों के समझौते का नतीजा था। जर्मनी की दक्षिण पंथी पार्टियाँ, बैंकों के मालिक, उद्योगपति, बड़े भूस्वामी आदि ने मिलकर हिडेंन बर्ग को इस बात के लिए मनाया कि वे हिटलर को चांसलर नियुक्त करें। सत्ता में आने के तत्काल बाद उसने अपनी भूमिका को मजबूत बनाने का उपक्रम शुरू किया। उसने हिंडेन बर्ग को रीचस्टैग (जर्मन संसद) को भंग करने के लिए तथा 5 मार्च 1933 को दुबारा चुनाव कराने के लिए राजी कर लिया। 28 फरवरी 1933 को यानी चुनावों से ठीक पाँच दिन पहले रीचस्टैग (संसद) भवन में आग लगा दी गई। आमतौर पर लोगों का मानना है कि नाजियों ने खुद आग लगाई थी। आतंक पैदा करने तथा मतदाताओं को धमकाने के लिए ऐसा किया गया था। इस आग लगाने के कार्य के लिए सरकार ने कम्युनिस्टों पर आरोप लगाया। तत्काल हजारों लोगों को कैद कर लिया गया। कैद किए गए लोगों में जार्जी दिमित्रोव भी थे जो बल्गेरियाई कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे और उन दिनों जर्मनी में थे। इस प्रकार की घटनाओं के बीच चुनाव हुए। लेकिन इन सबके बावजूद हिटलर बहुमत प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ। लेकिन कुछ ही महीनों में हिटलर ने अपना तानाशाही शासन सुदृढ़ बना लिया। इसके लिए उसने आतंक पैदा किया और सोशल डेमोक्रेटिक दल के लोगों, कम्युनिस्टों, ट्रेड यूनियन नेताओं तथा नाजी-विरोधियों की हत्या करवाई। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 60,000 से भी अधिक लोगों को गिरफ्तार कर जेल या यातना शिविरों में भेज दिया गया। 1933 के मध्य तक अन्य सभी दलों भंग कर दिया गया अथवा उन्होंने स्वयं अपने को भंग कर लिया। 1934 में हिटलर जर्मनी का राष्ट्रपति भी बन गया। सत्ता में आने के चंद महीनों में अपनी आतंक फैलाने वाली मशीनरी को दुरस्त कर लिया था और जर्मन जनता के ऊपर उसका निरंकुश नियंत्रण स्थापित हो गया था। सारा देश सैनिक शिविर में बदल दिया गया था। सत्ता संभालने के तत्काल बाद गुप्त रूप से देश को शस्त्रास्त्रों से लैस करने लगा तथा वारसाईकी की संधि का उल्लंघन करते हुए इसके लिए उसने एक के बाद दूसरा कई कदम उठाए। अक्टूबर 1933 में जर्मनी ने राष्ट्र संघ से अपने को अलग कर लिया। वायु सेना के एक भवन को ले लिया गया जिस पर संधि में रोक लगाई गई थी। मार्च 1935 में हिटलर ने घोषणा की कि जर्मनी की सैनिक क्षमता को लेकर संधि में जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं, जर्मनी अब उनको नहीं मानता और इसके बाद उसने सैनिक शक्ति के साथ वायु सेना तथा नौसेना को भी संगठित करना आरंभ कर दिया। रीनेलैण्ड को विसैन्यीकृत किया गया था, 1936 में जर्मन फौजों ने उस पर कब्जा कर लिया। ये सारी चालें संधि का पूर्ण रूप से उल्लंघन थीं लेकिन इस कार्रवाई का किसी भी पश्चिमी शक्ति ने विरोध नहीं किया। इन सारे उल्लंघनों के बावजूद ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ एक नौसैनिक संधि पर हस्ताक्षर किए। संधि में जर्मनी की नौसैनिक क्षमता पर जो रोक लगी थी, ब्रिटेन की संधि से उसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हुआ था। 1936 तक जर्मनी ने अपनी सैनिक शक्ति पूरी तरह बढ़ा ली थी तथा आक्रमण का मंच तैयार हो चुका था जिसके चलते द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। राष्ट्रसंघइस प्रसंग में यहाँ राष्ट्र संघ पर विचार करना अधिक उपयुक्त लगता है। यद्यपि सभी महाद्वीपों के देश इसके सदस्य थे, इसके भाग्य का अंतिम रूप से निर्णय यूरोपीय देशों द्वारा किया गया था जिनका इस पर प्रभुत्व था। इसके गठन के समय इसके सदस्यों की संख्या 44 थी। इनमें से अधिकांश यूरोपीय देश थे सिर्फ रूस और जर्मनी को इसके बाहर रखा गया था। इसके अलावा लैटिन-अमरीका के ज्यादातर देश, ईरान, जापान, चीन, थाईलैंड और भारत (जो अभी उपनिवेश था) आदि एशियाई देश, दक्षिण अफ्रीका संघ, ईथोपिया और लाइबेरिया जैसे अफ्रीकी देश तथा आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसके सदस्य देशों में शामिल थे। इस संघ में एक असेंबली, एक परिषद और एक सचिवालय था। असेंबली में सभी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व था और हर देश का एक मत था। परिषद् में पाँच सदस्य थे, इनमें पाँच-ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमरीका स्थाई सदस्य थे और बाकी चार अस्थाई सदस्य थे। संयुक्त राज्य अमरीका संघ में शामिल नहीं हुआ, इसलिए उसकी जगह जर्मनी को लिया गया जब 1926 में उसने सदस्यता ग्रहण की थी। स्विट्जरलैंड के लोकार्नो नामक नगर में अक्टूबर 1925 में एक बैठक हुई, उसके बाद ही जर्मनी को परिषद् में लिया गया। इस बैठक में सात यूरोपीय देशों ने भाग लिया था। इनमें जर्मनी तो था लेकिन इसमें सोवियत रूस नहीं था। इस बैठक में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें जर्मनी और फ्रांस की मौजूदा चौहद्दी की रक्षा की गारंटी दी गई थी। साथ में जर्मनी और बेल्जियम की सीमाओं की रक्षा की भी गारंटी दी गई थी। साथ में जर्मनी और बेल्जियम की सीमाओं की रक्षा की भी गारंटी दी गई थी। इन तीनों देशों ने वायदा किया कि आपस में कोई किसी के विरूद्ध आक्रमण नहीं करेगा। 1928 तक यूरोप के सभी देश राष्ट्र संघ के सदस्य हो चुके थे। 1934 में सोवियत संघ को भी सदस्यता मिल गई। उस समय तक जापान और जर्मनी दोनों ही राष्ट्र संघ के बाहर चले गए थे।पूर्व में उल्लिखित किया जा चुका है कि राष्ट्र संघ में प्रमुख यूरोपीय देशों का प्रभुत्व था जैसे ब्रिटेन और फ्रांस। राष्ट्र संघ छोटे-छोटे देशों के मामूली झगड़ों का निपटारा तो कर देता था लेकिन जब किसी बड़ी शक्ति का मामला आता था, जैसे आक्रमण रोकना, सदस्य राष्ट्र की भू-भागीय अखण्डता और स्वतंत्रता को कायम रखना तथा शांति की रक्षा करना तो संघ इनका निपटारा नहीं कर पाता था। इस मामले में संघ का रिकार्ड काफी निराशाजनक था। यह बड़े राष्ट्रों द्वारा अपनाई गई तुष्टीकरण की नीति का प्रतिबिंब था। यह नीति फासीवादी तथा सैनिकवादी शक्तियों के विषय में अपनाई जाती थी। जैसा पहले बताया जा चुका है कि संघ के प्रतिज्ञा पत्र में इस प्रकार के प्रावधान थे जो आक्रमण को रोकने के लिए कारगर माध्यम प्रदान करते थे लेकिन इन माध्यमों का उपयोग नहीं किया गया। जापान ने मंचूरिया पर कब्जा कर लिया उसके बाद उसने वहाँ मांचूकुओ नाम की एक कठपुतली सरकार स्थापित करवा दी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद खुलेआम आक्रमण की यह पहली बड़ी घटना थी। जापान राष्ट्र संघ को छोड़कर अलग हो गया और बाद में इस मामले में कुछ नहीं पता चला। इसके कुछ ही सालों के बाद जापान ने चीन पर जबर्दस्त आक्रमण किया। अक्टूबर 1935 में इटली ने इथयोपिया पर हमला कर दिया। इसमें उसने 6 लाख सैनिक झोंक दिए थे। नवंबर में राष्ट्रसंघ ने इटली के खिलाफ सीमित आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा की। लेकिन 1936 में इथयोपिया के कड़े प्रतिरोध के बावजूद, राष्ट्र संघ इस सदस्य देश को इटली ने अपने देश में मिला लिया। जुलाई 1936 में इटली पर थोड़े बहुत जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे, उन्हें भी वापस कर लिया गया। जिन देशों का राष्ट्र संघ में दबदबा था उन्होंने इस आक्रमण को रोकने के प्रति पूरी अनिच्छा दिखाई। संयुक्त राज्य अमरीका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था, उसने भी उस घटना पर चुप्पी साधने की नीति अपनाई। आक्रमण रोकने के लिए आर्थिक प्रतिबंधों की हिमायत करने वाला रूस अकेला देश था। उसने ब्रिटेन, फ्रांस तथा खुद को उसमें शामिल कर फासीवाद विरोधी मोर्चा बनाने के लिए आह्वान किया। सारी दुनिया के फासीवाद विरोधी विचार के लोगों ने सोवियत संघ का समर्थन किया। बहरहाल, पश्चिमी देश फासीवाद और उसके आक्रमण के प्रति तुष्टीकरण का रवैया इस विश्वास के आधार पर अपनाए हुए थे कि फासीवादी आक्रमणों का रूख अंततः सोवियत संघ की ओर हो जाएगा। आगामी तीन वर्षों के दौरान दुबारा दुनिया धीरे-धीरे विश्व युद्ध की स्थिति की ओर लौटने लगी थी। 1936 में इटली और जर्मनी के बीच राजनीतिक सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसे ’रोम बर्लिन धुरी’ कहा जाता है। 1937 के नवंबर में इटली और जर्मनी ने कोमिनटर्न विरोधी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यही समझौता पहले नंवबर 1936 में जर्मनी तथा जापान के साथ हो चुका था। 1937 में इटली ने राष्ट्र संघ से अपने को अलग कर लिया। यहाँ तक कि ’रोम बर्लिन धुरी’ के अस्तित्व में आने के पहले ही स्पेन में तानाशाही सरकार स्थापित करने के मकसद से जर्मनी और इटली ने आपस में सहयोग करना आंरभ कर दिया था। आक्रमण और तुष्टीकरण1936-37 के दौरान आक्रामक शक्तियों का एक गुट उभरकर सामने आया जिसमें जर्मनी, जापान और इटली शामिल थे। यूरोप की अन्य प्रमुख शक्तियों की तुष्टीकरण की नीति पर ब्रिटेन और फ्रांस चल रहे थे। इन देशों ने जब कई बार आक्रमण की कार्रवाई की तो संयुक्त राज्य अमरीका ने भी तटस्थता का रूख अख्तियार किया। तुष्टीकरण की नीति जारी रही। हिटलर को विश्वास हो चला था कि पोलैण्ड पर उसके आक्रमण से उत्तेजित होकर ब्रिटेन और फ्रांस हरकत में नहीं आएँगे यद्यपि इसने युद्ध की प्रक्रिया को सितंबर 1939 में तेज कर दिया। इन तीनों देशों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा युद्ध का आधारभूत कारण था। जर्मनी यूरोप को जीतकर विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनने के फिराक में था, इटली बाल्कन क्षेत्रों, अरबों के बहुत बड़े हिस्से और अफ्रीका पर कब्जा करना चाहता था और जापान एशिया और प्रशांत क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था।स्पेन का गृह युद्धजर्मनी और इटली के संयुक्त आक्रमण का पहला शिकार स्पेन हुआ। फरवरी 1936 के चुनावों में जनमोर्चा (पॉपुलर फ्रण्ट) की विजय हुई थी, इसकी चर्चा की जा चुकी है। राजनीतिक स्वतंत्रता बहाल कर, बड़े जमीदारों की भूसंपत्ति को टुकड़े कर, किसानों की माँग को पूरा कर तथा खान मजदूरों और दूसरे औद्योगिक मजदूरों की हालत में सुधार कर नई सरकार ने सुधारों को लागू करना शुरू कर दिया था। शैक्षिक विकास का भी एक काम हाथ में लिया गया था। फलांगे तथा दूसरे दक्षिण पंथी दल और गुट उन लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करते थे जिन्होंने स्पेन के पिछड़ेपन को कायम रखा था। इसके साथ इनके सहयोगी के कुछ अन्य लोग भी थे जैसे सेना के जनरल आदि। इन लोगों ने जनमोर्चा (पॉपुलर फ्रण्ट) सरकार को अपदस्थ कर उसकी जगह फासीवादी शासन कायम करने की योजना बनाई। जुलाई 1936 में फासीवादी लोगों ने विद्रोह कराए। इन विद्रोहों को सेना का समर्थन प्राप्त था। ये विद्रोह स्पेन के भीतर तथा बाहर उसके उपनिवेशों में भी कराए गए। विद्रोहियों का मुख्य नेता जनरल फ्रैंको था। वह स्पेन के उपनिवेश मोरक्को से विद्रोहियों का नेतृत्व करता हुआ स्पेन में आकर यहाँ के विद्रोहियों से मिल गया। इसके बाद तीन साल तक खूनी युद्ध चलता रहा। राष्ट्रवादियों (रिपब्लिकन विरोधी फासीवादी ताकतों और उनके सहयोगियों को इस नाम से पुकारा जाता था) ने इस बीच रिपब्लिकन सरकार को अपदस्थ करने के लिए जर्मनी और इटली से मदद प्राप्त कर ली थी। वस्तुतः स्पेन के गृह युद्ध से यूरोप के दो फासीवादी देश आपस में घनिष्ठ हो गए थे और स्पेन के फासीवादियों की मदद में बहुत बड़ी मात्रा में शस्त्रास्त्र, हवाई जहाज तथा सैनिक उन्होंने स्पेन में ठेल दिए। विदेशी मदद से विद्रोहियों ने देश के कई भागों पर कब्जा कर लिया और किसानों तथा उन लोगों को आतंकित किया गया जिन पर रिपब्लिकन दल को समर्थन देने का शक किया गया था। इस अवसर पर ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमरीका ने हस्तक्षेप की नीति अपना ली थी। इसका मतलब यह था कि रिपब्लिकन सरकार को किसी प्रकार की मदद नहीं पहुँच सकती थी जबकि फ्रैंको को जर्मनी और इटली की सैनिक सहायता बेरोक-टोक जारी रही। रिपब्लिकन सरकार की मदद में आगे आने वाला एक मात्र देश सोवियत संघ था। नागरिकों की मदद से रिपब्लिकन लोगों ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था संगठित की थी। इन नागरिकों ने अपनी सेना संगठित की थी और कई जबर्दस्त लड़ाईयाँ लड़ी थीं। नवंबर 1936 में वहाँ की राजधानी मैड्रिड की बहादुरी पूर्वक उन्होंने रक्षा की थी तथा फ्रैंको को इस पर कब्जा नहीं करने दिया था।स्पेन के गृह युद्ध ने समूचे विश्व की चेतना को आंदोलित कर दिया था। स्पेन की रिपब्लिक की रक्षा में लड़ने के लिए पचास से भी अधिक देशों के स्वयं सेवकों ने अपना नाम दर्ज कराया था। एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रिग्रेड बनाई गई थी। इसमें 40 हजार से भी ज्यादा स्वयंसेवक भर्ती हुए थे जिन्होंने स्पेन में युद्ध लड़ा। हजारों स्वयंसेवक लड़ते हुए स्पेन की धरती पर मारे गए थे। इन स्वयंसेवकों में फासीवाद विरोधी जर्मनी और इटली के भी लोग थे। टालमान के नाम पर जर्मन बटालियन का नाम रखा गया था। टालमान जर्मनी के विख्यात कम्युनिस्ट नेता थे जिनको नाजियों ने यातना शिविर में बंद कर रखा था तथा बाद में उनकी हत्या कर दी थी। अमरीका बटालियन का नाम अब्राहम लिंकन था। लिंकन संयुक्त राज्य अमरीका के ऐसे राष्ट्रपति थे। जिन्होंने वहाँ दास प्रथा का उन्मूलन किया था स्पेनी रिपब्लिकन लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एक जुटता में समूचे विश्व में फासीवाद के उत्थान को लेकर बढ़ते हुए सरोकार की झलक दिखाई पड़ती है। स्पेन के गृह युद्ध को केवल स्पेन का मामला नहीं माना गया था। बल्कि यह ऐसा मामला था जिससे से सारे विश्व को फासीवाद और उसके आक्रमण से खतरा पैदा हो गया था। रिपब्लिकन लोगों के साथ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक-जुटता दर्शाने के लिए जवाहरलाल नेहरू स्पेन गए। विश्व के ’विभिन्न भागों से लेखक’ कवि और कलाकार स्पेन के गृह युद्ध में लड़े तथा रिपब्लिकन लोगों के समर्थन में विश्व जनमत तैयार करने में उनकी मदद की। बीसवीं सदी के महान चित्रकार पाब्लो पिकासो ने ’ग्वेर्निका’ नाम का चित्र तैयार किया जो महान कलाकृति मानी जाती है। ग्वेर्निका स्पेन का एक कस्बा था जिसको फासीवाद हवाई जहाजों ने बम से तहस-नहस कर दिया था। फासीवाद जिस नृशंस शक्ति का प्रतीक था ’ग्वेर्निका’ का चित्रण उसके विरूद्ध जबर्दस्त प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता था। फरवरी 1939 तक फ्रांस का अधिकांश हिस्सा फासीवादियों के कब्जे में आ चुका था तथा ब्रिटेन और फ्रांस ने फ्रैंको की सरकार को मान्यता दे दी थी। इसके थोड़े दिनों के बाद संयुक्त राज्य अमरीका ने भी इसे मान्यता प्रदान कर दी। मार्च के अंत तक मैड्रिड शहर का प्रतिरोध जारी रहा लेकिन इस शहर पर जब फासीवादियों का कब्जा हो गया तो समूचा स्पेन उनके अधिकार में आ गया। स्पेन के गृह युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध का ’पूर्वाभ्यास’ कहा जाता है, जब फासीवादी देशों ने स्पेन के मैदान में अपने नए हथियारों का परीक्षण किया था। चीन पर जापानी हमलाजापान ने मंचूरिया को जीतने के बाद अपनी स्थिति को और सुदृढ़ किया और जुलाई 1937 में उसने चीन पर बहुत जबर्दस्त हमला किया। कुछ ही महीनों में उत्तरी चीन का बहुत बड़ा हिस्सा जापानी फौजों के कब्जे में आ गया जिसमें बीजिंग, नानकिंग और शंघाई जैसे महत्वपूर्ण नगर भी शामिल थे। जापानियों ने चीन के उन नगरों पर भी बम गिराए जिनका कोई सामरिक (सैनिक) महत्व नहीं था तथा चीन की निर्दोष आबादी पर बर्बरतापूर्ण कहर ढाए। 1938 में एक घोषणा में उन्होंने इसे ’पूर्वी एशिया की नई व्यवस्था’ की संज्ञा दी जिसमें जापान, चीन तथा मंचूरिया को एक राजनीतिक इकाई में बँधना था। इस समय तक संगठित राष्ट्रीय चीनी प्रतिरोध का उदय हो चुका था। राष्ट्र संघ ने चीनी आक्रमण की भर्त्सना तो की लेकिन इसको समाप्त करने के लिए कुछ नहीं किया गया।आस्ट्रिया का हड़पा जानाजर्मनी और आस्ट्रिया के बीच हुई संधियों के कारण दोनों देशों के एकीकरण पर रोक लगी हुई थी लेकिन हिटलर के सत्ता में आने के बाद जर्मनी द्वारा आस्ट्रिया को हड़प लेने के खतरे बढ़ गए। आस्ट्रिया में नाजी आंदोलन भी सिर उठाने लगा था। इसका उद्देश्य आस्ट्रिया और जर्मनी को एक करना था। 1930 के दशक के शुरू में आस्ट्रिया में एंगेलबर्ट डोलफुस का तानाशाही शासन कायम हो गया था। उसने आस्ट्रिया में समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी को कुचल दिया था लेकिन आस्ट्रि्रया और जर्मनी के एकीकरण के भी वह खिलाफ था। मुसोलिनी ने उसका समर्थन किया था क्योंकि तब तक जर्मनी से उसका मेलमिलाप नहीं हुआ था तथा और अधिक शक्तिशाली होने की महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए अकेले कोशिश कर रहा था। 1934 में डोलफुस की हत्या कर दी गई तथा आस्ट्रिया के नाजियों ने पुत्श के जरिए सत्ता पर काबिज होने की कोशिश की। नाजियों और कम्युनिस्टों तथा नाजी विरोधियों में भयानक खूनी संघर्ष हुए लेकिन पुत्श (सत्ता पलट) का प्रयास विफल रहा। मुसोलिनी ने भी आस्ट्रिया से लगी अपनी सीमा पर फौजें भेज दीं और चूँकि हिटलर अभी तक अपनी ताकत के बारे में आश्वस्त नहीं था, इसलिए इस मामले में उसने तटस्थ रहने का निर्णय लिया। 1938 तक आते-आते परिस्थिति एकदम बदल गई। इटली द्वारा इथयोपिया पर कब्जा करने और स्पेन में गृह युद्ध के बाद ’बर्लिन रोम धुरी’ और कोमिनटर्न विरोधी समझौते के माध्यम से इटली और जर्मनी में निकटता बढ़ी थी। 11 मार्च 1938 को मुसोलिनी की मिलीभगत से हिटलर ने अपनी सेनाओं को आस्ट्रिया में कूच करा दिया और आस्ट्रिया के नाजियों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। हिटलर ने घोषणा की कि ’’विपत्ति में फँसे जर्मन भाइयों की मदद’’ के लिए सेनाओं को वहाँ भेजा गया है। ये जर्मन लोग आस्ट्रिया सरकार के कुशासन और दमन का दुख भोग रहे थे। बिना पश्चिमी ताकतों के किसी विरोध के आस्ट्रिया को हड़पने का काम पूरा हो गया यद्यपि यह कार्रवाई शांति संधि का पूरी तरह उल्लंघन थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविली चैंबरलेन का मानना था कि जर्मनी का पूरब की ओर विस्तार और कुछ भू-भाग प्राप्त करने की न्यायोचित माँग पश्चिमी यूरोप की शांति रक्षा में मददगार साबित होगी।म्यूनिख समझौतानिकृष्ट कोटि के तुष्टीकरण और शर्मनाक विश्वासघात की घटना उस समय घटी जब चैकोस्लोवाकिया के सहयोगी पश्चिमी देशों ने उसे जर्मनी के हवाले कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद चैकोस्लोवाकिया का स्वतंत्र राज्य के रूप में उदय हुआ था। वह उन थोड़े से राज्यों में था जिन्होंने अपनी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली को बचा रखा था जबकि पूर्वी, दक्षिणी और मध्य यूरोप के अधिकांश हिस्से निरंकुश शासन के शिकार हो चुके थे। पूर्वी यूरोप का वह सबसे ज्यादा औद्योगीकृत देश था। चैकोस्लोवाकिया का एक हिस्सा ’सुदेतेन लैण्ड’ कहलाता था, यहाँ पर बड़ी संख्या में जर्मन लोग रहते थे। यह चैकोस्लोवाकिया के कुछ सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योगों का केंद्र भी था। आस्ट्रिया को हड़पने के बाद हिटलर के आक्रमण इरादों का अगला लक्ष्य चैकोस्लोवाकिया ही था। शुरू में जर्मनी की माँग थी कि ’सुदेतेन लैण्ड’ उसे सौंपा जाना चाहिए। 1920 के दशक से ही फ्रांस चैकोस्लोवाकिया का मित्र देश था। चैकोस्लोवाकिया ने जर्मनी की यह माँग ठुकरा दी कि सुदेतेन लैण्ड उसके हवाले किया जाना चाहिए और सोवियत संघ ने इस मुद्दे पर चैकोस्लोवाकिया का समर्थन किया। सोवियत संघ ने चैकोस्लोवाकिया के साथ 1935 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। सोवियत संघ ने चैकोस्लोवाकिया के सामने प्रस्ताव रखा कि यदि वह जर्मन आक्रमण का प्रतिरोध करना चाहता है तो सोवियत संघ उसकी तत्काल मदद करेगा।किनारे परअब यह बात भी साफ हो गई है कि अगर नाजियों के खिलाफ एक शक्तिशाली शांति मोर्चा कायम किया गया होता या फासीवादी आक्रमण के विरूद्ध मोर्चा कायम किया गया होता तो इस युद्ध को रोककर शांति को सुनिचित किया जा सकता था। सोवियत संघ, फ्रांस इंग्लैंड और चैकोस्लोवाकिया को मिलाकर यह शांति मोर्चा बन सकता था जिसमें संयुक्त राज्य अमरीका की सद्भावना को साथ लिया जा सकता था। फिर अपने आप इस शांति मोर्चे की तरफ पोलैंड, रूमानिया और यूरोप की अन्य छोटी-छोटी ताकतें आकर मिलतीं, इटली और जर्मनी के विरूद्ध यह जबर्दस्त संगठन होता (यद्यपि इटली ने जर्मनी से हाथ मिलाया, यह पहले निश्चित नहीं था)। यदि कहीं ऐसा हुआ होता तो आक्रांता की भूमिका में प्रवेश करना नाजी सरकार का पागलपन होता और शांति सुनिश्चित की गई होती।यह सरल और स्पष्ट नीति ब्रिटिश सरकार को अच्छी नहीं लगी, जिससे अपने आप शांति कायम हुई होती। लेकिन ऐसा इसलिए संभव नहीं हो सका क्योंकि ऐसा होने का अर्थ था सोवियत संघ के साथ सहयोग करना। इसका यह भी अर्थ था कि सोवियत संघ इससे मजबूत होता तथा दुनिया की तमाम जन शक्तियाँ बंधन मुक्त होतीं। ब्रिटिश सरकार अपनी वर्ग सहानुभूति के कारण सोवियत संघ को खौफ की नजर से देखती थी और इसलिए उसका झुकाव नाजीवाद और फासीवाद की तरफ था और फिर इसका परिणाम यह हुआ कि बात तो वे लोकतंत्र और शांति की करते थे। उन्होंने फासीवाद को खुश रखने की नीति अपनाई थी जो सीधे युद्ध की ओर ले गई। चैंबरलेन बर्चेसगाडेन में है। इससे ज्यादा कलंक की बात क्या हो सकती है, इससे बड़ा धोखा और क्या होता है ? अविश्वसनीय घटनाएँ पहले ही घट चुकी हैं, किसी की चौंकने की सामर्थ्य पहले ही खत्म हो गई है। एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री हिटलर और फासीवाद के जासूस के रूप में काम करता है तथा यूरोप पर फासीवादी प्रभुत्व कायम करने के लिए काम करता है। एक फ्रांसीसी विदेश मंत्री एम. बोनेट तो एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं तथा अपने मित्र चैकोस्लोवाकिया के विरूद्ध सक्रिया रूप से काम करते हैं। वे हिटलर को अधिक महिमा मण्डित करने के लिए काम करते हैं। अचानक एक झटके में इन महान राजनेताओं की वास्तविक मनशा बिजली की तरह चमक उठती हैं। उनका वास्तविक रूप सामने आ जाता है। शासक वर्ग के लिए महान् नराधम लोगों के लिए स्वतंत्रता और लोकतंत्र का कोई उपयोग नहीं है। इनको स्वतंत्रता और लोकतंत्र, दोनों से भय लगता है और हिटलर में उनको प्रतिक्रियावाद के महान विजेता के दर्शन होते हैं। यद्यपि उसे बर्दाश्त करना बहुत कठिन है लेकिन वह वास्तविक लोकतंत्र से उनके लिए लाख दर्जे अच्छा है। बहुत आसानी से वे यह भूल जाते हैं कि हिटलर का उद्देश्य इसको नष्ट करना और यूरोप पर पूरी तरह प्रभुत्व कायम करना है। वे यह भी भूल जाते हैं कि चैकोस्लोवाकिया यूरोप में लोकतंत्र का एकमात्र गढ़ है। यदि चैकोस्लोवाकिया का पतन होता है तो फ्रांस का भी पतन होता है। इससे क्या फर्क पड़ता है यदि एम. बोनेट और श्री चैंबरलेन का अपना वर्गस्वार्थ सुरक्षित है। हम देख रहे हैं कि किस तरह वर्गभावनाएँ किसी संकट का सामना करने का अंतिम मानदण्ड बनती हैं। फ्रांस और अंग्रेज जनता का मस्तक शर्म से झुका हुआ है। घटनाओं के इस नाटकीय मोड़ से विस्मित हैं लोग, केवल अपमान की बात नहीं है बल्कि उनका देश, जिस पर उनको गर्व हैं, भंयकर विनाश का सामना कर रहा है और चैंबरलेन और बोनेट चैकवासियों को बार बार अंतिम चेतावनी दे रहे हैं। हिटलर की माँगें मानो नहीं तो हम लोग भी तुम्हारे खिलाफ उसके साथ खड़े हो जाएँगे। इस पर ध्यान दीजिए : यह केवल एक सहयोगी तथा मित्र का साथ छोड़ना नहीं है, बल्कि यह एक शत्रु को समर्थन देने की धमकी भी है। आत्मा की कचोट और पीड़ा के साथ चैकोस्लोवाकिया की मंत्रिपरिषद की बैठक होती है। यह बैठक लगातार 48 घण्टे चलती हैं। उत्तर पाने में देर होने पर फोन चैबरलेन क्रोधित हो जाते हैं और उनके तथा फ्रांस के मंत्री रातभर चैकोस्लोवाकिया के मंत्रियों को फोन खटखटाते रहते हैं और धमकी पर धमकी देते जाते हैं और चैकोस्लोवाकिया की सरकार आत्मसमर्पण कर देती है। इसकी व्याख्या हम कैसे करेंगे ? किसी ने इसकी सांगोपांग व्याख्या की है। यह चैकोस्लोवाकिया के साथ जर्मनी द्वारा बलात्कार था, इनमें इंग्लैंड और फ्रांस उसको पकड़कर जबरन जमीन पर पटके हुए हैं। उसमें संसदों से विचार-विमर्श नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि उनकी बैठकें तक नहीं बुलाई जाती हैं। चैंबरलेन का कहना है कि संसद की बैठक बुलाना उस समय असुविधाजनक होगा जब बातचीत नाजुक दौर में हो। फ्रांस में सभाओं और प्रदर्शनों पर रोक लगा दी जाती है। हम देख रहे हैं कि इंग्लैंड और फ्रांस में भी फासीवादी तरीके विकसित हो रहे हैं। अंग्रेज कहते हैं कि उनको अंग्रेज कहलाने में शर्म महसूस होती है। फ्रांस में किसी एक सत्कर्म की सूचना बिजली की कौंध की तरह चमकती है और मोहभंग हुई जनता को कुछ गर्व महसूस होता है। प्राग के फ्रांसीसी सैनिक मिशन में नियुक्त एक फ्रांसीसी जनरल घोषणा करता है कि उसके देश ने चैक जनता के साथ धोखा किया है, इससे वह घुटन का अनुभव करने लगा है और फ्रांस की नागरिकता छोड़कर चैक नागरिकता ले लेता है और कसम खाता है कि कभी वह फ्रांस नहीं लौटेगा। इसके बाद से वह अपने को चैक नागरिक मानता है। ताज्जुब है कि फ्रांसीसी नागरिकता को त्यागने की इस कार्रवाई का बड़ी संख्या में फ्रांसीसी गर्व का अनुभव करते हैं क्योंकि इसको उन्होंने अपमान समझा था। उनको इस बात पर गर्व है कि एक बहादुर फ्रांसीसी जो सोचता था उसे उसने कह भी दिया तथा उसका परिणाम भुगतने के लिए बहादुरी से तैयार है। चैंबरलेन हिटलर से मिल रहे हैं। इस बीच जनसमूह में खलबली है तथा फ्रांस और ब्रिटेन में गड़गड़ाहट सुनाई पड़ रही है। जनता को काफी समय तक उनकी सरकारों और मंत्रियों ने बेवकूफ बनाया है लेकिन उनका संकट बहुत कठिन है। वे युद्ध तो कतई नहीं चाहते हैं। वे, उनके बेटे, भाई और पति इस युद्ध में मरेंगे। उनके बच्चों, माताओं, पत्नियों और बहनों पर बम गिराए जाएँगे। वे अब करें क्या ? यह सब कुछ बहुत आसानी से रोका जा सकता था यदि शांति के पक्ष में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस एक साथ डट कर खड़े होते लेकिन चैंबरलेन और बोनेट हिटलर को प्राथमिकता देते हैं। (जवाहर लाल नेहरू द्वारा पेरिस में लिखे गए एक लेख का अंश, पोलैण्ड का सवाल और सोवियत संघ के साथ बातचीतजर्मनी की ओर से अगला खतरा पोलैण्ड पर आया। जर्मनी ने डानजिग तथा उस गलियारे को वापस करने की माँग रखी जो पूर्वी प्रशिया को जर्मनी के शेष हिस्से से अलग करता था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह गलियारा पोलैण्ड को दिया गया था और ’डानजिग’ को स्वतंत्र नगर बना दिया गया था। ब्रिटेन और फ्रांस की सरकारों ने घोषणा की कि यदि किसी भी कार्रवाई से पोलैण्ड की स्वतंत्रता को खतरा पैदा होता है तो वे लोग पोलैण्ड को हर संभव सहायता देंगे। पोलैण्ड से किए जाने वाले इन वायदों को जर्मनी ने बहुत गम्भीरता से नहीं लिया।बहरहाल जिस समय से फासीवादी ताकतों ने आक्रमण करना शुरू किया तब से पहली बार जर्मनी के विरूद्ध मैत्री संधि के लिए ब्रिटेन और फ्रांस ने सोवियत संघ से बातचीत शुरू की। ब्रिटेन और फ्रांस दोनों की ही सीमा पोलैण्ड के साथ लगी हुई नहीं थी, इसलिए यदि जर्मनी पोलैण्ड पर आक्रमण करता तो ये दोनों सीधे पोलैण्ड की मदद के लिए नहीं पहुँच सकते थे। सोवियत संघ के साथ पोलैण्ड की सीमा काफी लंबी थी और फ्रांस ब्रिटेन और सोवियत संघ का गठजोड़ ही जर्मनी के आक्रमण से पोलैण्ड की रक्षा कर सकता था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद पोलैण्ड ने रूस की जमीन पर कब्जा जमाए रखा तथा लगातार उसकी नीतियाँ सोवियत विरोधी रही थीं। वह नहीं चाहता था कि सोवियत संघ की फौजें पोलैण्ड की धरती पर पाँव रखें चाहे उसके देश को कितना ही खतरा क्यों न हो। 12 से 21 अगस्त के बीच ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ के सैनिक मिशनों की बातचीत हुई। इस बातचीत में पोलैण्ड के उपर्युक्त रूख से रूकावट आई। बातचीत बीच में ही टूट गई जब फ्रांस तथा ब्रिटेन के सैनिक मिशनों ने यह बताया कि उनकी सरकारों ने उनको यह अधिकार नहीं दिया है कि वे सोवियत संघ के साथ किसी कारगर संधि को अंजाम दे सकें। 23 अगस्त 1939 में जर्मनी और सोवियत संघ ने एक अनाक्रमण संधि पर हस्ताक्षर किए और 1 सितंबर को जर्मनी ने पोलैण्ड पर आक्रमण कर दिया। 3 सितंबर को ब्रिटेन ने और उसके बाद फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। | |||||||||
| |||||||||