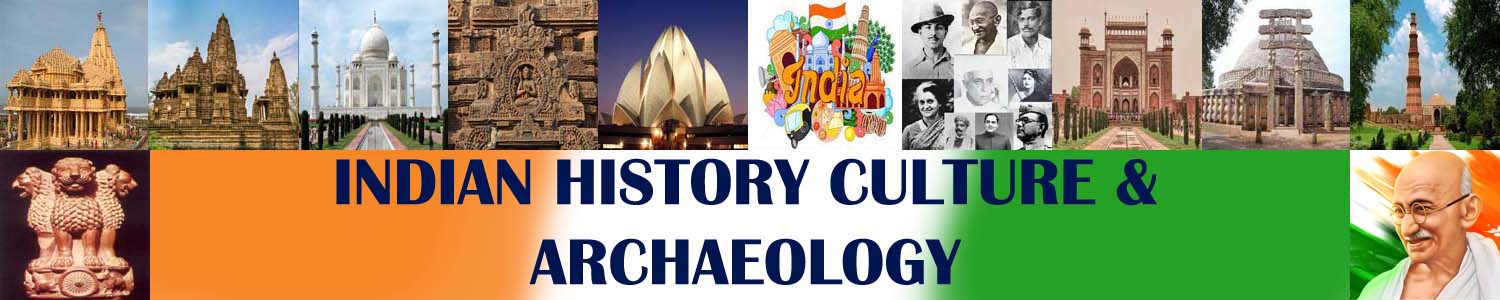| |||||||||
|
जहांगीर और शाहजहां तथा मुगल सैन्य संगठन
भारत की राजनीतिक स्थिति तथा प्रशासनिक प्रगतिभारत में सत्रहवीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध कुल मिलाकर प्रगति तथा विकास का काल था। इस अवधि में मुगल साम्राज्य दो कुशल शासकों, जहाँगीर (1605-27) तथा शाहजहाँ (1628-58) ने राज्य किया। जैसा कि हम देख चुके हैं कि दक्षिण भारत में भी बीजापुर तथा गोलकुण्डा में यह युग आंतरिक शान्ति तथा सांस्कृतिक विकास का युग था। मुगल शासकों ने अकबर द्वारा विकसित प्रशासनिक व्यवस्था का और प्रसार किया। उन्होंने राजपूतों के साथ मैत्री बनाए रखी तथा अफगानों और मराठों जैसे शक्तिशाली वर्गों की मित्रता हासिल कर साम्राज्य की राजनीतिक नींव को वृहद् आधार प्रदान किया। उन्होंने अपनी राजधानियों में सुन्दर भवनों का निर्माण किया जिनमें से कई संगमरमर से निर्मित थे। इसके अलावा उन्होंने मुगल राजदरबार को देश का सांस्कृतिक केन्द्र बनाने की चेष्टा की। इन शासकों ने ईरानियों, तुर्कों तथा उजबेकों जैसी पड़ोसी शक्तियों के साथ भारत के सम्बन्ध अच्छे बनाने में सक्रिय योगदान दिया। इससे भारत के विदेश व्यापार की संभावनाएँ बढ़ी। उन्होंने विभिन्न यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को जो छूट दी, उससे भी भारत का विदेश व्यापार काफी बढ़ा। लेकिन इसी अवधि में कुछ हानिकारक तत्व भी उभर कर सामने आये। शासक वर्ग के बीच की समृद्धि काश्तकारों तथा मजदूरों तक नहीं पहुँची। मुगल शासक वर्ग पश्चिम के विज्ञान तथा तकनीक के विकास से भी अनजान रहा। सिंहासन के उत्तराधिकार की समस्या को लेकर राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई, जिससे राजनीतिक व्यवस्था के अलावा देश की आर्थिक तथा उसके सामाजिक विकास पर भी प्रभाव पड़ा।अकबर का सबसे बड़ा पुत्र जहाँगीर बिना किसी बाधा के सम्राट बन सका, क्योंकि उसके अन्य छोटे भाई अकबर के ही जीवनकाल में अत्याधिक मद्यपान के कारण मर गए थे। लेकिन जहाँगीर ने सम्राट बनने के कुछ ही समय बाद उसके बड़े लड़के खुसरो ने विद्रोह कर दिया। उस काल में सिंहासन के लिए पिता तथा पुत्र के बीच संघर्ष होना बहुत अनोखी बात नहीं थी। जहाँगीर ने स्वयं अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठा रखा था और कुछ समय तक सारे साम्राज्य में अशान्ति फैल गयी। खुसरों का विद्रोह अधिक दिनों तक नहीं चल सका। जहाँगीर ने लाहौर के निकट युद्ध में उसे पराजित किया और शीघ्र ही उसे बंदी बना लिया। बंगालहम देख चुके हैं कि किस प्रकार जहाँगीर ने मेवाड़ के साथ चले आ रहे चार दशकों के संघर्ष को समाप्त किया। इसके अलावा दकन में मलिक अम्बर जो अकबर के प्रस्तावित समझौते को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, के साथ संघर्ष की समाप्ति के सिलसिले में भी उसकी कूटनीतिक कुशलता भली-भाँति प्रकट होती है। पूर्व में भी संघर्ष की स्थिति थी। यद्यपि अकबर ने उस क्षेत्र में शक्तिशाली अफगानों की रीढ़ तोड़ दी, थी फिर भी पूर्वी बंगाल के कई हिस्सों में अफगान अमीर अभी भी शक्तिशाली बने हुये थे। उन्हें जैसोर, कामरूप (पश्चिम असम) कछार आदि क्षेत्रों में हिन्दू राजाओं का समर्थन भी प्राप्त था। अपने शासन के अन्तिम दिनों में अकबर ने बंगाल के सूबेदार राजा मानसिंह को वापस दरबार में बुला लिया था और इसका लाभ उठाकर उस्मानखाँ तथा अन्य अफगान अमीरों ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था। जहाँगीर ने कुछ समय बाद मानसिंह को वापस वहाँ भेजा, लेकिन स्थिति बिगड़ती ही गई। 1608 में जहाँगीर ने प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के पोते इस्लामखाँ को बंगाल भेजा। इस्लामखाँ ने वहाँ बड़े उत्साह और दूरदर्शिता से काम लिया। उसने जैसोर के राजा तथा अन्य जमींदारों को अपने पक्ष में कर लिया और विद्रोहियों का मुकाबला करने के लिए ढाका को अपना अड्डा बनाया जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। उसने सबसे पहले सोनार गाँव की विजय की ओर ध्यान दिया जो मूसाखाँ तथा उसके साथियों के जिन्हें ‘‘बारह भुइया’’ पुकारा जाता था, नियन्त्रण में था। तीन वर्ष के लम्बे अभियान के बाद सोनार गाँव पर मुगलों का कब्जा हो गया। शीघ्र ही मूसाखाँ ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसे बन्दी बनाकर मुगल राजदरबार में भेज दिया गया। उसके बाद उस्मानखाँ की बारी थी, जिसे एक भीषण युद्ध में इस्लामखाँ ने पराजित किया। इन पराजयों से अफगान विद्रोहियों की हिम्मत टूट गई और बाकियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। जैसोर तथा कामरूप के क्षेत्रों को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया और इसके साथ ही पूर्वी बंगाल पर मुगलों की सत्ता भलीभाँति कायम हो गई। इस क्षेत्र को पूरी तरह नियन्त्रण में रखने के लिए राजमहल के स्थान पर ढाका को सूबे की राजधानी बनाया गया। जिसका अब बहुत तेजी से विकास आरम्भ हुआ।अकबर की तरह जहाँगीर भी इस बात को समझना था कि किसी भी क्षेत्र को अधिक समय तक बल प्रयोग से नहीं बल्कि वहाँ के लोगों का मन जीतकर उसे अधीन रखा जा सकता है। उसने पराजित अफगान अमीरों तथा उनके समर्थकों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया। कुछ समय के बाद बंगाल के कई जमींदारों और राजकुमारों को रिहा कर दिया गया और उन्हें बंगाल वापस जाने की स्वीकृति दे दी गई। यहाँ तक कि मूसाखाँ को भी छोड़ दिया गया और उसकी जागीरें उसे वापस दे दी गईं। इस प्रकार एक लम्बी अवधि के बाद बंगाल में शान्ति तथा समृद्धि के युग का फिर प्रारम्भ हुआ। इस प्रक्रिया में सहायता देने के लिए कुछ अफगान अमीरों को मुगल उमरा वर्ग में भी शामिल किया गया। जहाँगीर के शासनकाल में प्रमुख अफगान अमीर खान-ए-जहाँ लोदी था जिसने दकन में बड़ी बहादुरी दिखाई थी। 1622 तक जहाँगीर मलिक अम्बर को परास्त करने, बंगाल में शान्ति स्थापित करने तथा मेवाड़ के साथ चल रहे लंबे संघर्ष को समाप्त करने में सफल हो गया। जहाँगीर अभी भी जवान था (51)। लगता था कि उसके आगे शान्ति समृद्धि का एक लम्बा युग है। लेकिन दो कारणों से स्थिति बिल्कुल ही बदल गई। इनमें से पहला कारण कंधार पर फारस की विजय थी, जिससे मुगल प्रतिष्ठा को गहरा धक्का पहुँचा और दूसरा कारण जहाँगीर का स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण उत्पन्न होने वाली वाली परिस्थिति थी। उसकी बीमारी के कारण उसके बेटों में उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष आरम्भ हो गया था और अमीर अपनी शक्ति बढ़ाने की ताक में लगे थे। इन कारणों से अब नूरजहाँ राजनीतिक क्षेत्र में उतर गई। नूरजहाँनूरजहाँ के जीवन वृत्त, शेर अफगान नामक एक ईरानी के साथ उसका विवाह और एक लड़ाई में उसकी मृत्यु, जहाँगीर के एक वरिष्ठ सम्बन्धी के साथ नूरजहाँ का आगरा में ठहरना और चार साल बाद (1611) जहाँगीर के साथ उसके विवाह की घटनाओं से हम अच्छी तरह परिचित हैं और उन्हें विस्तार में दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इतिहासकार इस बात पर विश्वास नहीं करते कि नूरजहाँ के पहले पति की मृत्यु के लिए जहाँगीर उत्तरदायी था। मीना बाजार में जहाँगीर से नूरजहाँ की अचानक मुलाकात और बाद में शादी, कोई विचित्र बात नहीं थी। नूरजहाँ का परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार था और उसका पिता एतमाद्दुदौला जहाँगीर के शासन काल के प्रथम वर्ष में ही दीवान बन गया था। उसके एक लड़के ने खुसरो के विद्रोह में भाग लिया था और इसलिए नूरजहाँ के पिता को भी उसके पद से हटा दिया गया था, लेकिन शीघ्र ही उसे उसका पद वापस मिल गया। अपनी कार्यकुशलता तथा जहाँगीर के साथ अपनी पुत्री के विवाह के बाद एतमाद्दुदौला को प्रमुख दीवान बना दिया गया। इसके अलावा इस विवाह से परिवार के अन्य सदस्यों को भी लाभ पहुँचा और उनका मनसब बढ़ा दिया गया। एतमाद्दुदौला कुशल, कर्तव्यनिष्ठ तथा सम्राट के प्रति निष्ठावान था और दस वर्ष बाद अपनी मृत्यु तक राज्य के मामलों में उसका काफी प्रभाव था। नूरजहाँ का भाई आसफखाँ भी एक योग्य तथा विद्वान व्यक्ति था उसे खान-ए-सामाँ नियुक्त किया गया। खान-ए-सामाँ का पद एक ऐसे अमीरों को दिया जाता था जो सम्राट के अत्यधिक विश्वासपात्र होते थे। एक वर्ष बाद आसफखाँ ने अपनी पुत्री का विवाह खुर्रम (शाहजहाँ) से किया। खुसरो के विद्रोह और उसकी गिरफ्तारी के बाद खुर्रम अब अपने पिता का सबसे प्रिय पुत्र बन गया था।कुछ आधुनिक इतिहासकारों का मत है कि अपने पिता तथा भाई के साथ मिलकर और खुर्रम की सहायता से नूरजहाँ ने अपना एक ऐसा छोटा सा दल बना लिया था, जिसका जहाँगीर पर इतना नियंत्रण हो गया था कि उसके समर्थन के बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता था। इसी कारण बाद में दो गुट हो गए थे। एक गुट नूरजहाँ का था तथा दूसरा उसके विरोधियों का। यह भी कहा जाता है कि नूरजहाँ की महत्वाकांक्षाओं के कारण ही शाहजहाँ से उसका मतभेद हो गया और इसी कारण 1622 में शाहजहाँ अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह पर उतर आया। उसे यह अनुभव होने लगा कि जहाँगीर पूरी तरह नूरजहाँ के प्रभाव में है। कुछ अन्य इतिहासकार इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि जैसा कि जहाँगीर और आत्मकथा से स्पष्ट है, 1622 में अपने स्वास्थ्य के गिरने तक जहांगीर स्वयं सभी राजनीतिक निर्णय लेता था। इस अवधि में नूरजहाँ की राजनीतिक भूमिका क्या रही, यह स्पष्ट नहीं है। उसका प्रभाव अधिकतर शाही घराने पर था और उसने फारसी परम्पराओं पर आधारित नये फैशनों का प्रचलन किया। उसके प्रभाव के कारण ही राजदरबार में फारसी कला तथा संस्कृति को प्रतिष्ठा मिली। नूरजहाँ वास्तविक अर्थों में जहाँगीर की संगिनी थी। वह उसके साथ शिकार पर भी जाती थी। क्योंकि वह स्वयं एक कुशल घुड़सवार और निशानेबाज थी। इसलिये उसको बराबर बादशाह के साथ रहने का मौका मिलता था और इसी कारण वह जहाँगीर को प्रभावित अवश्य कर सकती थी और कई लोग सम्राट के साथ अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए उसकी सिफारिश का अनुरोध करते थे। इसके बावजूद जहाँगीर, नूरजहाँ या उसके दल पर निर्भर नहीं था। यह इस बात से भी स्पष्ट है कि ऐसे अमीर जो इस विशेषदल के प्रिय नहीं थे, उनकी भी पदोन्नति हुई। शाहजहाँ भी अपने व्यक्तिगत गुण तथा उपलब्धियों के कारण आगे बढ़ा, न कि नूरजहाँ की सिफारिश से शाहजहाँ स्वयं भी महत्वाकांक्षी था पर जहाँगीर को इस बात का आभास नहीं था। जो भी हो, उन दिनों कोई भी शासक अपने पुत्र या किसी अमीर को शक्तिशाली होने का मौका नहीं दे सकता था, क्योंकि बाद में वे ही उसके लिए काल बन जाते थे। जहाँगीर तथा शाहजहाँ के बीच संघर्ष का यही मूल कारण था। शाहजहाँ का विद्रोहविद्रोह का तत्कालिक कारण शाहजहाँ का कंधार जाने से, जो ईरान की सेना के घेरे में था, इन्कार करना था। शाहजहाँ को डर था कि यह अभियान बड़ा कठिन तथा लम्बा होगा और उसकी अनुपस्थिति में उसके विरुद्ध षड़यंत्र रचे जायेंगे। इसलिए उसने कई माँगे रखीं, जिनमें ऐसी शक्तिशाली सेना का पूर्ण नेतृत्व था, जिसमें दकन के कई बहादुर शामिल थे। इसके अलावा वह कई महत्वपूर्ण किलों तथा सारे पंजाब पर अपना प्रभुत्व चाहता था। उसके इस व्यवहार से जहांगीर क्रोधित हो गया। उसे विश्वास हो गया कि शाहजहाँ विद्रोह करने की सोच रहा है और उसने उसे कड़ी चिट्ठियाँ लिखीं तथा ऐसे कदम उठाये जिससे स्थिति अधिक खराब हो गई। दोनों के बीच की खाई और गहरी हो गई। शाहजहाँ उन दिनों माण्डू में था। वहाँ से वह आगरा आया ताकि वहाँ के खजाने को अपने बस में कर सके। शाहजहाँ को दकन की सेना वहाँ के अमीरों का पूरा समर्थन प्राप्त था। गुजरात तथा मालवा ने भी उसका साथ दिया। इसके अलावा उसे अपने ससुर आसफखाँ तथा दरबार के अन्य अमीरों का भी समर्थन प्राप्त था। दिल्ली के पास होने वाले युद्ध में शाहजहाँ महाबतखाँ द्वारा पराजित हुआ और मेवाड़ के एक दल की बहादुरी के कारण ही बच सका। सेना की एक अन्य टुकड़ी को शाहजहाँ के हाथों से गुजरात वापस लेने के लिए भेजा गया। इस प्रकार शाहजहाँ को मुगल क्षेत्रों से खदेड़ दिया गया और उसे अपने पहले के शत्रुओं, दकन के राजाओं, की शरण लेनी पड़ी। कुछ ही समय बाद शाहजहाँ दकन पार कर उड़ीसा पहुँच गया और वहाँ के सूबेदार को अचानक हमले से अचम्भित कर दिया। जल्दी ही बंगाल और बिहार शाहजहाँ के नियन्त्रण में आ गये। किन्तु महाबतखाँ की सैनिक योग्यता के सामने एक बार फिर शाहजहाँ को हारकर दकन को लौटना पड़ा। इस बार उसने मलिक अम्बर के साथ सन्धि की जो फिर मुगलों से लोहा लेने पर तुल गया था। शीघ्र ही उसने जहाँगीर को एक पत्र लिखकर क्षमा माँगी। जहाँगीर भी अपने योग्य तथा उत्साही पुत्र को क्षमा करने के लिए उत्सुक था। इसके बाद सन्धि के अन्तर्गत शाहजहाँ को अपने दो पुत्रों, दारा तथा औरंगजेब को राजदरबार में बंधक के रूप में रखना पड़ा। शाहजहाँ को खर्च के लिए दकन का एक क्षेत्र जागीर के रूप में सौंप दिया गया। ये घटनाएँ 1626 की हैं।महाबतखाँशाहजहाँ के विद्रोह के कारण चार वर्षों तक साम्राज्य में अशान्ति बनी रही। इसके परिणामस्वरूप कन्धार मुगलों के हाथ से जाता रहा तथा दकन के शासकों के हाथ से सभी क्षेत्रों को अपने अधिकार में वापस से लिया जो उन्हें अकबर के जीवनकाल में छोड़ने पड़े थे। इससे व्यवस्था की एक और कमजोरी उभरकर सामने आई। कोई भी शक्तिशाली राजकुमार बादशाह की शक्ति का प्रतिद्वन्दी बन सकता था। विशेषकर उस परिस्थिति में जबकि बादशाह सर्वोच्च शक्ति को अपने नियन्त्रण में बनाये रखने में असमर्थ या अनिच्छुक प्रतीत होता था। शाहजहाँ का मुख्य आरोप यह था कि जहाँगीर ने अपने गिरते स्वास्थ्य के कारण राज्य का कार्यभार देखना बंद कर दिया था और सारी शक्ति नूरजहाँ के हाथों में चली गई थी। यह आरोप स्वीकार करना इसलिए कठिन है, क्योंकि शाहजहाँ का ससुर आसफखाँ स्वय प्रमुख दीवान था। इसके अलावा यद्यपि जहाँगीर का स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं था, फिर भी वह बहुत सतर्क था और उसकी इच्छा के बिना कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता था। जहाँगीर की बीमारी से यह भी खतरा बढ़ गया था कि कोई भी महत्वाकांक्षी अमीर स्थिति का लाभ उठाकर सर्वोच्च शक्ति अपने हाथों में केन्द्रित करने की कोशिश कर सकता था। यह बात एक ऐसी घटना के माध्यम से सामने आई जिसकी किसी को आशा नहीं थी। महाबतखाँ ने शाहजहाँ के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन वह इस बात को लेकर क्षुब्ध था कि विद्रोह की समाप्ति के बाद दरबार के कुछ लोग उसकी शक्ति समाप्त कर देने पर तुल गये थे। यह महसूस किया जाने लगा कि शहजादे परवेज के साथ उसकी मित्रता कभी भी खतरनाक साबित हो सकती है। जब महाबतखाँ को हिसाब-किताब देने के लिए राजदरबार में बुलाया गया तब वह राजपूतों के एक ऐसे दल के साथ आया जो उसका कट्टर समर्थक था। जब सम्राट अपने लोगों के साथ काबुल जाने के लिए झेलम नदी पार कर रहा था, महाबतखाँ ने मौका देखकर उसे अपने कब्जे में कर लिया। नूरजहाँ नदी पार कर भाग निकलने में सफल हुई किन्तु उसने आसफखाँ के साथ मिलकर महाबतखाँ के विरुद्ध अभियान किया जो असफल हो गया। नूरजहाँ ने अब अन्य उपायों का सहारा लिया। उसने महावतखाँ के सामने आत्मसमर्पण कर दिया ताकि वह जहाँगीर के पास रह सके। उसने मकाबतखाँ के सन्देह को मिटाने की पूरी चेष्टा की, पर अन्दर ही अन्दर अवसर की ताक में रहने लगी। महाबतखाँ एक कुशल सैनिक तो था, किन्तु योग्य कूटनीतिक या प्रशासक नहीं। उधर वह धीरे-धीरे राजपूत सैनिकों का समर्थन भी खोता जा रहा था। नूरजहां ने स्थिति का लाभ उठाया तथा छः महीनों के अन्दर-अन्दर वह अमीरों को महाबतखाँ के खिलाफ भड़कने में सफल हो गई। अपनी नाजुक स्थिति को देखकर महाबतखाँ जहाँगीर को छोड़कर राजदरबार से भाग निकला। कुछ समय बाद वह शाहजहाँ के साथ मिल गया, जो समय अपने हाथ होने की ताक में था। महाबतखाँ की पराजय नूरजहाँ की सबसे बड़ी विजय थी। यह उसकी धीर बुद्धि तथा साहस के कारण ही संभव हो सकी। इसके बावजूद नूरजहाँ की विजय चिरस्थायी नहीं रह सकी क्योंकि एक वर्ष के अन्दर-अन्दर जहाँगीर ने लाहौर के पास (1627) आखिरी साँस ली। चालाक आसफखाँ ने मौके का फायदा उठाया। जहाँगीर ने उसे अपना वकील नियुक्त किया था। लेकिन वह धीरे-धीरे अपने दामाद शाहजहाँ के शहंशाह बनाने की नींव तैयार कर रहा था। आसफखाँ अब खुलकर सामने आया। दीवान, प्रमुख अमीरों और सेना की सहायता से उसने नूरजहाँ को बंदी बना लिया और दकन में शाहजहाँ को इस महत्वपूर्ण घटना की सूचना भेजी। इसके अलावा उसने खुसरो के एक लड़के को कठपुतली के रूप में खाली गद्दी पर बैठा दिया। शाहजहाँ का छोटा भाई परवेज अत्यधिक मद्यपान के कारण पहले ही मर चुका था। उसके दूसरे भाई शहरयार ने गद्दी के लिए प्रयास तो किया पर उसे बड़ी आसानी से मात दे दी गई और अंधा बनाकर कैद में डाल दिया गया। इसके शीघ्र बाद शाहजहाँ आगरा पहुँचा जहाँ हर्षोल्लास के बीच वह सिंहासन पर बैठा। इसके पहले ही उसके कहने पर उसके सभी प्रतिद्वन्द्वियों को जिसमें बंदी बनाये गये उनके भाई शामिल थे, को मौत के घाट उतार दिया गया। इस प्रकार घटना, जिसमें पुत्र ने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था, जहाँगीर के साथ शुरू हुई और शाहजहाँ के बाद तक चली। इससे कटुता फैली और मुगल वंश के लिए इसके घातक परिणाम हुआ। शाहजहाँ ने अपने बोये हुये बीज का परिणाम स्वयं चखा। जहाँ तक नूरजहाँ का सवाल है, शाहजहां ने गद्दी पर बैठने के बाद उसके लिए एक निश्चित राशि तय कर दी और नूरजहाँ अठारह साल बाद अपनी मृत्यु तक शान्ति का जीवन व्यतीत करती रही।शाहजहाँ का शासनकाल (1628-58) बहुमुखी गतिविधियों का काल था। उसकी दकन नीति का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। जब हम मुगलों की विदेश नीति की चर्चा करेंगे जो शाहजहाँ के काल में अपने शिखर पर थी। मुगलों की विदेश नीतिहम देख चुके हैं कि पन्द्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में तैमूरी साम्राज्य के विघटन के बाद किस प्रकार तीन शक्तिशाली साम्राज्यों उजबेक, सफवी तथा उस्मानी का मध्य एशिया में उदय हुआ। उजबेक आरम्भ से ही मुगलों के शत्रु थे और उन्होंने मुगलों तथा अन्य तैमूरवंशी राजकुमारों को समरकन्द तथा उसके पास के क्षेत्र खुरासान से बहिस्कृत किया था। साथ उजबेकों का संघर्ष नवोदित सफवी से हो गया जो खुरासान पर अपना दावा कर रहा था। खुरासान पठार ईरान तथा मध्य एशिया को जोड़ता था तथा चीन और भारत के व्यापार-मार्ग इसी के रास्ते में पड़ते थे। सफवियों के लिए यह स्वाभाविक था कि उजबेकों के खतरे का सामना करने के लिए ये मुगलों से हाथ मिलाएँ। यह इसलिए भी संभव था क्योंकि उजबेकों तथा मुगलों के बीच कंधार को छोड़कर अन्य कोई सीमा विवाद नहीं था। उजबेकों ने ईरान के सफवी शासकों से धार्मिक मतभेद का फायदा उठाने की कोशिश की। सफवी शासक शिया थे तथा सुन्नियों पर निर्ममता से अत्याचार कर रहे थे। उजबेक तथा मुगल शासक दोनों ही सुन्नी मुसलमान थे। लेकिन उजबेक समझते थे कि इसके कारण मुगल उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ायेंगे। लेकिन मुगल इतने संकीर्ण दृष्टिकोण के नहीं थे कि वे धार्मिक मतभेदों से प्रभावित हों। शिया समर्थक ईरान के साथ मुगलों की सन्धि को देखकर उजबेक क्षुब्ध हो उठे। उन्होंने पेशावर तथा काबुल के बीच के उत्तर-पश्चिमी सीमा क्षेत्र में बसे अफगानों तथा बलूची कबीलों को मुगल शासन के खिलाफ भड़कना आरंभ किया। पश्चिम एशिया में इस काल में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य संभवतः उस्मानी तुर्कों का था। उस्मानी तुर्कां का नाम उनके प्रथम शासक उस्मान (मृत्यु 1326) के नाम पर था। उन्होंने एशिया माइनर तथा पूर्वी यूरोप पर विजय प्राप्त कर ली थी तथा 1529 तक सीरिया, मिश्र अरब तथा ईरान पर भी कब्जा कर लिया था। काहिरा के शक्तिहीन खलीफा ने उन्हें ‘रूस के सुल्तान’ की उपाधि दी थी। बाद में उन्होंने ‘बादशाह-ए-इस्लाम’ की पदवी ग्रहण कर ली।ईरान के शिया शक्ति के उदय से उस्मानी सुल्तानों को अपनी पश्चिमी सीमा पर खतरे का आभास होने लगा था। उन्हें डर था कि ये उनके क्षेत्रों में शिया सम्प्रदाय को बढ़ावा देंगे। 1512 में तुर्की के सुल्तान ने एक प्रसिद्ध लड़ाई में ईरान के शाह को पराजित किया। तुर्कां तथा ईरानियों में बगदाद तथा एरीवान के आसपास के उत्तरी ईरान के क्षेत्रों को लेकर संघर्ष आरम्भ हुआ। तुर्कां ने धीरे-धीरे अरब के आसपास के तटवर्ती क्षेत्रों पर अपना अधिकार कायम किया तथा फारस की खाड़ी से पुर्तगालियों को निकाल देने का प्रयास किया। पश्चिम में उस्मानी तुर्कों के खतरे को देखकर ईरान के शासक मुगलों की मैत्री हासिल करने के लिए उत्सुक थे। यह अब और भी आवश्यक हो गया था क्योंकि पूर्व में उजबेकों का खतरा बना हुआ था। ईरान के खिलाफ तुर्कां तथा उजबेक शासकों का जो गुट था उसमें मुगल सम्मिलित नहीं होना चाहते थे, क्योंकि इससे एशिया का शक्ति संतुलन बिगड़ रहा था। इसके आलावा ईरान की मैत्री से मध्य एशिया से उनके व्यापार की संभावना बढ़ सकती थीं। यदि मुगलों के पास एक शक्तिशाली नौसेना होती तब वे शायद तुर्कां से मैत्री करते क्योंकि तुर्कों के पास नौसेना थी और वे भूमध्यसागर में यूरोपीय शक्तियों से संघर्ष कर रहे थे। लेकिन दूसरी ओर मुगल तुर्कां के साथ मैत्री बढ़ाने में इसलिए हिचकिचा रहे थे क्योंकि वे तुर्की सुल्तानों को खलीफों के उत्तराधिकारियों के रूप में मान्यता देने के लिए तैयार नहीं थे। मुगलों की विदेश नीति का निर्धारण उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर ही किया गया। अकबर तथा उजबेकसफवी शासकों के हाथों उजबेक सरदार शैबानीखाँ की 1511 में पराजय के बाद बाबर कुछ समय के लिए समरकन्द पर एक बार फिर अपना अधिकार कायम रखने में सफल हो गया था। यद्यपि बाबर को उजबेकों द्वारा ईरानियों की पराजय के बाद समरकन्द छोड़ना पड़ा था तथापि ईरानी बादशाह ने बाबर की जो मदद की उससे मुगलों तथा सफवी स्थायी शासकों के बीच स्थाई मैत्री की नींव पड़ी। बाद में शेरशाह द्वारा भारत से निकाले जाने के बाद हुमायूँ को भी सफवी सम्राट शाह तहमास्प से मदद मिली थी और उसने ईरान के राजदरबार में शरण ली थी।उजबेक सरदार अब्दुलखाँ ने 1570 और 1579 के बीच साम्राज्य का वृहद् विस्तार कर लिया था। 1572-73 में अब्दुल्लखाँ उजबेक ने बल्ख पर कब्जा कर लिया था। बल्ख एवं बदख्शां की मुगलों तथा उजबेकों के मध्य मध्यवर्ती क्षेत्र की सी स्थिति थी। 1577 में अब्दुल्लाखाँ ने अकबर के पास अपना राजदूत भेजकर ईरान को परस्पर बाँट लेने का प्रस्ताव रखा था। शाह तहमास्प (मृत्यु 1576) के बाद ईरान में अशान्ति तथा अराजकता फैल गई थी। अब्दुल्ला उजबेक ने अकबर को इस बात पर राजी करने की चेष्टा की कि वह हिन्दुस्तान से अपने नेतृत्व में ईरान पर अभियान करे तथा दोनों संगठित रूप से इराक तथा खुरासान को शाह के चंगुल से निकालने का प्रयास करें। इस संकीर्ण धार्मिक तर्कों से अकबर जरा भी प्रभावित नहीं हुआ। इसके अलावा उजबेकों को शांत बनाये रखने के लिए एक शक्तिशाली ईरान की आवश्यकता थी। लेकिन साथ ही साथ अकबर उजबेकों से उस समय तक नहीं उलझना चाहता था जब तक वह काबुल अथवा भारतीय क्षेत्रों के लिए खतरा पैदा न करते हों। अकबर की विदेश नीति का यही आधार था। अब्दुल्ला उजबेक ने उस्मानी सुल्तानों के सामने भी ईरान के खिलाफ त्रिगुटीय सुन्नी शक्तियों के संगठन का प्रस्ताव रखा। इसके उत्तर में अकबर ने अब्दुल्ला उज़बेक को अपना एक राजदूत भेजकर यह स्पष्ट कर दिया कि आक्रमण के लिए कानूनी अथवा धार्मिक मतभेदों को पर्याप्त कारण नहीं माना जाना चाहिए। मक्का जाने वाले तीर्थ यात्रियों की दिक्कतों के बारे में अकबर ने स्पष्ट कर दिया कि गुजरात की विजय के बाद उनके लिए एक नया मार्ग खुल गया है। इसके अलावा उसने ईरान से अपनी पुरानी दोस्ती की चर्चा की तथा अब्दुल्लाखाँ उजबेक को सफवियों के बारे में अपमानजनक बाते कहने के लिए भर्त्सना की और उसे बताया कि वे सैयद तथा स्वतन्त्र बादशाह हैं। अकबर की मध्य एशिया की राजनीति में बदली हुई दिलचस्पी का प्रमाण यह भी था, कि उसने अपने दरबार में तैमूरी राजकुमार, मिर्जा सुलेमान को शरण दी, जिसे उसके पोते ने बदख्शां से बहिष्कृत कर दिया था। अबुलफजल के अनुसार खैबर दर्रा पहियों वाले वाहनों के लिए किया गया तथा मुगलों के डर के कारण बल्ख के द्वार अधिकतर बंद ही रखे जाते थे। बदख्शां पर किसी प्रकार का आक्रमण न हो, इसके लिए अब्दुल्ला उजबेक ने उत्तर-पश्चिम सीमा क्षेत्र में बसे कबालियों को मुगलों के खिलाफ उकसाने की चेष्टा भी की। यह काम उसने अपने धर्मांध प्रतिनिधि जलाल के माध्यम से किया था। इसके परिणामस्वरूप वहाँ की स्थिति इतनी गम्भीर हो गई कि अकबर को अटक आना पड़ा। इन्हीं अभियानों के दौरान अकबर ने अपने प्रिय मित्र राजा बीरबल को खो दिया था। अब्दुल्ला उजबेक ने 1585 में अचानक बदख्शां पर कब्जा कर लिया। मिर्जा सुलेमान तथा उसका पोता, दोनों ही अकबर के दरबार में शरण मांगने आये। अकबर में उन्हें उचित मनसब प्रदान किया। इसी बीच अपने सौतेले भाई मिर्जा हकीम की मृत्यु (1585) का लाभ उठाकर अकबर ने काबुल पर कब्जा कर उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब मुगल तथा उजबेक सीमाएँ समीपस्थ हो गईं। अब्दुल्लाखाँ उजबेक ने अकबर के पास एक और राजदूत भेजा जो अकबर से उस समय मिला जब वह सिन्धु नदी के पास अटक में था। वहाँ अकबर को अपनी सीमा के इतनी नजदीक देखकर अब्दुल्ला उजबेक चिन्तित हो गया था। लम्बे पत्र व्यवहार के बावजूद भी अब्दुल्लाखाँ उजबेक अकबर को अपने पक्ष में नहीं कर सका था और उसे बराबर मुगलों द्वारा सफवियों की मदद के लिए आने की आशंका बनी रही। ऐसी स्थिति में अब्दुल्लाखाँ उजबेक ने बुद्धिमानी दिखाई और और खुरासान पर चढ़ाई कर दी और उन प्रदेशों पर कब्जा कर लिया जिन पर पहले से ही उसकी नजर थी। इस स्थिति में अकबर ने अब्दुल्लाखाँ उजबेक के साथ समझौता करने में ही भलाई समझी और उसने अब्दुल्लाखाँ उजबेक के पास अपने राज्य के हकीम हूमान के माध्यम से एक पत्र तथा मौखिक संदेश भेजा। ऐसा लगता है कि इन दोनों में हिन्दुकुश की सीमा निर्धारित करने से सम्बन्धित एक सन्धि भी हुई। इस सन्धि के अन्तर्गत मुगलों ने 1585 तक तैमूर वंशी शासकों द्वारा शासित प्रदेश बदख्शां तथा बलख में अपना हस्तक्षेप समाप्त कर दिया। बदले में उजबेकों ने काबुल तथा कंधार पर दावा करना पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया तथापि सन्धि के कारण मुगलों को हिन्दुकुश में एक सुरक्षित सीमा मिल गई जिसका लाभ उठाकर 1595 में कंधार जीतकर अकबर ने एक सुनियोजित सीमा की स्थापना की जो भौगोलिक आधार पर लक्षित थी। इसके आलावा 1586 के बाद स्थिति की देखरेख के लिए अकबर स्वयं लाहौर में ठहर गया और 1598 में अब्दुल्लाखाँ उजबेक की मृत्यु के बाद ही आगरा आया। अब्दुल्ला की मृत्यु के बाद उजबेक साम्राज्य ऐसे छोटे राज्यों में बँट गया जो बराबर आपस में लड़ते रहते थे। इसके परिणामस्वरूप एक लम्बे अर्सें के लिए मुगलों पर से इसका खतरा टल गया। कंधार का मामला तथा ईरान के साथ सम्बन्धमुगलों तथा सफवी शासकों के मध्य विवाद की सम्भावना कन्धार को लेकर हो सकती थी। जिस पर दोनों अपना-अपना दावा कर रहे थे। कंधार सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के अलावा आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। यह दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रतीक भी बना हुआ था। कंधार अब तक तैमूरी साम्राज्य का हिस्सा रहा था और इस पर हिरात के शासकों तथा बाबर के भाई-भतीजों का 1507 तक अधिकार रहा जब उजबेकों ने उन्हें पराजित कर वहाँ से निकाल दिया। 1507 में कंधार पर बाबर का भी कुछ समय तक अधिकार रहा था। उजबेकों द्वारा ईरानी शिया मतावलम्बी शासकों के विरोध में प्रचार तथा मुगलों द्वारा सफवी शासकों की असहिष्णुता पूर्ण नीति को नापसंद किये जाने के बावजूद सफवी और मुगल शासकों के मध्य मैत्री सम्बन्ध स्थापित हुए। इसका कारण मुख्यतः उजबेक शक्ति का आतंक ही था।काबुल की सुरक्षा के लिए सामरिक दृष्टि से कंधार का बहुत महत्व था। कंधार के किले को इस क्षेत्र के सबसे मजबूत किलों में गिना जाता था और उसमें पानी की अच्छी व्यवस्था थी। काबुल तथा हिरात जाने वाली सड़कें इसी स्थान पर जाकर मिलती थीं। यहाँ से सारे दक्षिण अफगानिस्तान पर नज़र रखी जा सकती थी। इस प्रकार इस किले का अत्यधिक सामरिक महत्व था। एक आधुनिक लेखक के अनुसार ‘‘काबुल’’, गजनी तथा कंधार रेखा उससे सामरिक और सुनियोजित सीमा रेखा का बोध होता था। जो भौगोलिक आधार पर लक्षित थी। काबुल तथा खैबर के आगे कोई भी प्राकृतिक सुरक्षा सीमा नहीं थी। इसके अलावा कंधार के नियंत्रण से अफगान तथा बलूची कबीलों पर भी नियंत्रण आसान हो जाता था।’’ सिंध तथा बलूचिस्तान पर अकबर की विजय के बाद मुगलों के लिए कंधार का सामरिक तथा आर्थिक महत्व और भी बढ़ गया था। कंधार एक समृद्ध तथा उपजाऊ भूमि वाला प्रान्त था, जहाँ भारत और मध्य एशिया के बीच लोगों तथा वस्तुओं का समागम मध्य एशिया से कंधार द्वारा मुल्तान तक का स्थल मार्ग तथा वहाँ से सिन्धु नदी द्वारा समुद्र का जल मार्ग धीरे-धीरे व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता गया। ऐसा विशेषकर इसलिए था क्योंकि ईरान होकर जाने वाली सड़क युद्धों तथा आंतरिक गड़बड़ी के कारण बहुधा असुरक्षित रहते थीं। अतः अकबर इसी मार्ग से व्यापार बढ़ाना चाहता था और उसने अब्बदुल्ला उज्बेक को बताया भी था कि मक्का जाने के लिए यह तीर्थ यात्रियों तथा वस्तुओं के किये एक सुरक्षित मार्ग बन सकता है। इन सभी बातों पर गौर करने से ऐसा लगता है कि कंधार का ईरानियों के लिए उतना महत्व नहीं था, जितना कि मुगलों के लिए। ईरान के लिए कंधार एक बाहरी सीमा चौकी के समान था, जिसका महत्व तो था, पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए इसकी विशेष आवश्यकता नहीं थी। आरम्भ में कंधार की समस्या को लेकर मुगलों तथा ईरानियों के सम्बन्धों को बिगड़ने नहीं दिया गया। 1522 में कंधार बाबर के नियन्त्रण में उस समय आया जब उजबेक एक बार फिर खुरासान पर धावे की तैयारी कर रहे थे। इस स्थिति में कंधार पर मुगलों के कब्जे पर ईरानियों ने कोई गंभीर आपत्ति नहीं की। लेकिन हुमायूँ शाह तहमास्प के दरबार में शरण माँगने आया तब ईरान के साम्राट ने उसे इस शर्त पर सहायता देना मंजूर किया कि वह कंधार को अपने सौतेले भाई कामरान से हासिल कर उसे ईरानियों को सौंप देगा। हुमायूँ के लिए इसे स्वीकार करने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। इसके बावजूद कंधार पर विजय के बाद उस पर अपना नियंत्रण बनाये रखने के लिए हुमायूँ को बहाने मिल गये। वास्तव में काबुल में कामरान के खिलाफ अभियानों के लिए कंधार ही हुमायूँ का अड्डा था। शाह तहमास्प ने हुमायूँ की मृत्यु के बाद फैली अशांति और गडबड़ी का लाभ उठाकर कंधार को अपने कब्जे में कर लिया। अकबर ने कंधार को वापस लेने का उस समय तक प्रयास नहीं किया जब तक अब्दुल्ला उजबेक के नेतृत्व में उजबेकों ने ईरान तथा मुगलों के लिए खतरा पैदा नहीं किया। जैसा कि कुछ आधुनिक इतिहासकारों का मत है, मुगलों की कंधार विजय (1595) उस संधि का हिस्सा नहीं थी जो ईरान के साम्राज्य को आपस में बाँटने के लिए अकबर तथा उज़बेकों के बीच हुई थी। उस समय तक खुरासान पर उजबेकों का नियंत्रण हो जाने के कारण कंधार ईरान से कट गया था। अकबर की कंधार विजय उजबेक आक्रमण की खिलाफ उत्तर-पश्चिम में एक सुरक्षा सीमा कायम करने के लिए थी। कंधार पर मुगलों के आधिपत्य के बावजूद ईरान तथा मुगलों के बीच अच्छे सम्बन्ध बने रहे। अकबर की मृत्यु के बाद ईरानियों ने कंधार को अपने कब्जे में करने की चेष्टा की पर असफल रहे। शाह अब्बास प्रथम (शासन 1588-1629) जो सबसे महान सफवी सम्राट था, जहाँगीर के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने के लिए उत्सुक था। उसने कंधार पर चड़ाई की योजना रद्द कर दी। जहाँगीर और उनके बीच राजदूतों तथा कीमती भेटों का आदान-प्रदान बराबर बना रहा। शाह अब्बास ने दकन के राज्यों के साथ राजनीतिक तथा व्यापारिक सम्बन्धों को स्थापित किया, लेकिन इस पर जहाँगीर ने आपत्ति नहीं की। दोनों देश एक दूसरे के प्रभाव से आतंकित नहीं थे, वरन् उनमें एक-दूसरे के प्रति सौहर्द की भावना थी, जिसका प्रतीक जहाँगीर के चित्रकार द्वारा कल्पना से बनाया गया वह चित्र है जिसमें जहाँगीर तथा शाह अब्बास एक-दूसरे को गले लगा रहे हैं और उनके पैरों के नीचे संसार का एक ग्लोब है। इस कार्य में दोनों देश सांस्कृतिक दृष्टि से भी एक-दूसरे के काफी करीब आ गये। इसमें नूरजहाँ के पिता का जो स्वयं ईरान से आये थे, काफी योगदान था। इस मैत्री से जहाँगीर से अधिक लाभ शाह अब्बास को हुआ, क्योंकि जहाँगीर ने शाह अब्बास की मैत्री के कारण उजबेक सरदारों के साथ मैत्री पर अधिक ध्यान नहीं दिया। क्योंकि वह अपने ‘‘बिरादर‘‘ की मैत्री में अपने आपको सुरक्षित समझता था और इस कारण शाह अब्बास उजबेकों के आतंक से मुक्त रहा, क्योंकि उजबेकों और मुगलां की सम्मिलित शक्ति ईरान के लिए खतरा सिद्ध हो सकती थी। जबकि मुगलों ने उजबेकों के मैत्री के प्रयास को ठुकरा कर दूरदर्शिता का परिचय नहीं दिया और यह बात शीघ्र ही सामने आई। 1620 में शाह अब्बास ने जहाँगीर से कंधार वापस लौटाने का अनुरोध किया और साथ में उस पर चढ़ाई करने की योजना भी बनाई। जहाँगीर इस हमले के लिये जरा भी तैयार नहीं था। वह राजनीतिक दृष्टि से अकेला पड़ गया था और न ही वह सामरिक दृष्टि से तैयार था। उसने कंधार को वापस लेने के लिए जल्दी-जल्दी तैयारियाँ की, लेकिन इसी समय शहजादे शाहजहाँ ने वहाँ जाने के पहले ऐसी माँगें रखीं जो पूरी नहीं की जा सकती थीं। परिणामस्वरूप कंधार ईरानियों के हाथ में चला गया (1622)। शाह अब्बास ने कंधार के प्रश्न पर जहाँगीर से हुई कटुता को कीमती उपहार देकर मिटाने की चेष्टा की। उसने जहाँगीर के सामने इस कार्य के लिए कई कारण भी रखे, जिन्हें जहाँगीर ने औपचारिक रूप से स्वीकार भी कर लिया। लेकिन इसके बाद मुगल तथा ईरानियों के सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध समाप्त हो गये तथा ईरान के विरुद्ध कूटनीतिक तैयारियाँ होनी प्रारम्भ हो गईं। 1598 में अब्दुल्लाखाँ उजबेक की मृत्यु के बाद मध्य एशिया की राजनीति में दूरगामी परिवर्तन हुए। आंतरिक कबीलाई झगड़ों के कारण उजबेक साम्राज्य का विघटन हो गया और इस स्थिति का लाभ उठाकर ईरान ने खुरासान पर कब्जा कर लिया। कंधार पर कब्जा करने के कुछ ही समय बाद शाह अब्बास पश्चिम की ओर प्रवृत्त हुआ और तुर्कों से बगदाद को वापस लेने में सफल हो गया। इस प्रकार उजबेक, मुगल तथा तुर्क, जो सुन्नी थे, एक बार फिर ईरान के विरुद्ध त्रिगुटीय संगठन कायम करने की सोचने लगे तथा जहाँगीर और उजबेकों के बीच संधि को अंतिम रूप देने के लिए राजदूतों के कई आदान-प्रदान हुए। जहाँगीर की मृत्यु के बाद संधि के प्रयास शाहजहाँ के शासनकाल में भी जारी रहे। किन्तु शाहजहाँ ने कूटनीति का सहारा लिया। शाह अब्बास की मृत्यु (1629) के बाद ईरान में अराजकता फैल गई थी। उधर शाहजहाँ दकन के मामलों से मुक्त हो गया। ईरान की स्थिति का लाभ उठाकर शाहजहाँ ने कंधार के ईरानी प्रशासक अली मर्दानखाँ को मुगलों के पक्ष में आ जाने के लिए उकसाया और उसमें सफल भी हो गया। शाहजहाँ का बल्ख अभियानकंधार की विजय शाहजहाँ के लिए एक विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति का आयाम मात्र थी। शाहजहाँ उजबेकों के काबुल पर हमलों तथा बलूची और अफगान कबीलों के साथ उनके षड़यन्त्रों के बारे में बहुत चिन्तित था। इस समय तक बुखारा और बल्ख ईमामकुली के छोटे भाई नजर मोहम्मद के हाथों में आ गए। नजर मोहम्मद तथा उसका लड़का अब्दुल अजीज दोनों ही महत्वाकांक्षी थे। काबुल तथा गजनी पर अपना प्रभाव कायम करने के लिए उन्होंने अफगान कबाइलियों की मदद से कई अभियान किये, पर शीघ्र ही अब्दुल अजीज ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा किया। इसके बाद नजर मुहम्मद के नियन्त्रण में केवल बल्ख रह गया और उसने शाहजहाँ से सहायता माँगी। शाहजहाँ ईरानियों की ओर से निश्चिंत था अतः उसने सहायता की माँग को शीघ्रता से स्वीकार कर लिया। वह लाहौर से काबुल आया तथा नजर मोहम्मद की मदद के लिए राजकुमार मुराद के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी। इस सेना में पचास घोड़े, दस हजार प्यादे जिनमें तोपची भी थे, के अलावा राजपूतां का एक दल भी शामिल था। यह सेना 1646 के मध्य में काबुल से रवाना हुई। शाहजहाँ ने राजकुमार मुराद को आदेश किया कि वह नजर मोहम्मद के साथ विनम्रता से पेश आये और आत्मसमर्पण कर दे तो उसे बल्ख लौटा दे तथा यह भी यदि नजर मोहम्मद समरकन्द तथा बुखारा पर कब्जा करने की इच्छा करे तब राजकुमार मुराद उसे हर प्रकार से सहायता करे। स्पष्ट है कि शाहजहाँ बुखारा के शासक के साथ जो मुगलों की सहायता और समर्थन का आकांक्षी था, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहता था। लेकिन मुराद के उतावलेपन के कारण शाहजहाँ की सारी योजना असफल हो गई। मुराद नजर मोहम्मद के निर्देश के बिना ही बल्ख की तरफ बढ़ा, उसने अपने सैनिकों को बल्ख के किले में घुसने का आदेश दिया। नजर मोहम्मद उस समय उसी किले में था। मुराद ने सख्ती से उसे अपने सामने हाजिर होने का आदेश दिया। नजर मोहम्मद राजकुमार के उद्देश्य से अवगत न होने के कारण वहा से भाग खड़ा हुआ। मुगलों को अब बाध्य होकर बल्ख पर कब्जा करना पड़ा और वहाँ की क्षुब्ध और क्रोधित जनता के विरोध के बावजूद अपना नियंत्रण कायम रखना पड़ा। उधर नजर मोहम्मद के लिए भी कोई आसान विकल्प सामने नहीं था। उसके लड़के अब्दुल अजीज ने मावराउन्नहर में उजबेक कबीलों को मुगलों के खिलाफ भड़का दिया तथा 120,000 सैनिकों की एक सेना खड़ी कर आमू दरिया आक्सस नदी को पार कर गया। इसी बीच राजकुमार मुराद की, जो घर लौटने का इच्छुक था, जगह औरंगजेब ने ली। मुगलों ने आमू दरिया को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। इसके बदले उन्होंने सामरिक महत्व की जगहों पर सैनिकों दल नियुक्त किये तथा सेना का मुख्य भाग एक साथ रखा ताकि वह किसी भी जगह पर आक्रमण की दशा में आसनी से जा सके। इस प्रकार मुगलों की स्थिति बड़ी अच्छी थी। अबुल अजीज आमू दरिया पार तो कर गया पर एक विशाल मुगल सेना को सामने पाकर उसके सामने पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस पलायन युद्ध में मुगलों ने उजबेकों को बल्ख के दरवाजों तक खदेड़ दिया (1647 के मध्य)।बल्ख पर मुगलों की विजय से उजबेकों के साथ सन्धि वार्ता का रास्ता साफ हो गया। अब्दुल अजीज के उजबेक समर्थक इधर-उधर भाग खड़े हुए और उसने भी अपने स्वयं को शांत करने के प्रयास किये। नजर मोहम्मद जो इस समय तक ईरान में शरण ले चुका था। उसने भी अपने साम्राज्य की वापसी के लिए मुगलों से अनुरोध किया। काफी सोच-विचार के बाद शाहजहाँ ने नजर मोहम्मद का साथ दिया। लेकिन उसने नजर मोहम्मद को सबसे पहले औरंगजेब से माफी माँगने के लिए कहा। यह शाहजहाँ की गलती थी, क्योंकि गर्वीला उजबेक शासक इस प्रकार नहीं झुक सकता था, विशेषकर जब कि वह जानता था कि मुगल बल्ख में अधिक समय तक नहीं बने रह सकते थे। मुगल व्यर्थ ही नजर मोहम्मद की व्यक्तिगत उपस्थिति की प्रतीक्षा करते रहे। इसी बीच सर्दी का मौसम आ रहा था और बल्ख में रसद नहीं थी अतः मुगलों ने अक्टूबर 1647 में वापस लौटना शुरू किया। लेकिन उन्हें वापसी बड़ी मँहगी पड़ी क्योंकि चारों तरफ विद्रोही उजबेकों ने छापामार हमले शुरू किए। जिसके कारण मुगलों को काफी नुकसान उठाना पड़ा और औरंगजेब की दृढ़ता से ही स्थिति पूरी तरह बिगड़ने से बच सकी। शाहजहाँ के बल्ख अभियान को लेकर आधुनिक इतिहासकारों में बहुत मतभेद है। ऊपर के वृतांत से स्पष्ट है कि शाहजहाँ की दृष्टि सुनियोजित व सुरक्षित मुगल साम्राज्य की भौगोलिक सीमा समझी जाने वाली आमू दरिया तक प्रशस्त करने के लिए प्रयत्नशील नहीं था। वैसे भी हम देख चुके हैं कि आमू दरिया सुरक्षित सीमा रेखा हो ही नहीं सकती थी। यद्यपि मुगल बादशाह बराबर अपने स्वदेश की चर्चा करते थे। किन्तु शाहजहाँ ने इस अभियान का लक्ष्य मुगलों के स्वदेश समरकन्द तथा परगना पर कब्जा करने के उद्देश्य से संबंधित नहीं था। ऐसा लगता है कि शाहजहाँ का लक्ष्य काबुल के सीमवर्ती क्षेत्रों बल्ख और बदख्शां में किसी मित्र शासक को बैठाना था। ये प्रदेश 1585 से ही तैमूरवंशी शासकों के अधीन रहे थे। शाहजहाँ का विश्वास था कि ऐसा करने से गजनी तथा खैबर दर्रे के आसपास रहने वाले विद्रोही अफगान कबीलों पर भी नियंत्रण रखा जा सकेगा। सामरिक दृष्टि से मुगलों का यह अभियान सफल रहा। मुगलों ने बल्ख पर कब्जा कर लिया था तथा उजबेकों के उन्हें वहाँ से बाहर निकालने के प्रयत्नों को असफल कर दिया। इस क्षेत्र में भारतीय सेना की यह पहली महत्वपूर्ण विजय थी और शाहजहाँ द्वारा इस जीत पर खुशियाँ मनाना स्वाभाविक ही था। लेकिन बल्ख पर अधिक समय के लिए अपना प्रभाव कायम रखना मुगलों के बस के बाहर की बात थी। ईरान के कड़े विरोध तथा स्थानीय आबादी के असन्तोष के कारण राजनीतिक दृष्टि से भी यह कार्य बड़ा कठिन था। कुल मिलाकर बल्ख अभियान से मुगल सेना की प्रतिष्ठा तो बड़ी, लेकिन इससे कोई विशेष राजनीतिक लाभ नहीं हुए। शायद मुगलों के लिए अकबर द्वारा बड़ी चेष्टा के बाद स्थापित काबुल, गजनी, कंधार सीमा पर बने रहना अधिक लाभकारी होता और इसमें सैनिक तथा दौलत का भी नुकसान नहीं होता। जो भी हो जब तक नजर मोहम्मद जीवित रहा मुगलों के साथ उसके संबंध अच्छे रहे और दोनों के बीच राजदूतों का बराबर आदान-प्रदान रहा। ईरान के साथ मुगलों के संबंधों का अन्तिम चरणबल्ख में मुगलों की पराजय से काबुल क्षेत्र में उजबेकों तथा खैबर-गजनी क्षेत्र में अफगान कबीलों का विद्रोह फिर शुरू हो गया। स्थिति का लाभ उठाकर ईरानियों ने कंधार पर हमला कर उसे अपने कब्जे में कर लिया (1649)। यह शाहजहाँ की प्रतिष्ठा पर एक बड़ा आघात था और उसने कंधार को वापस लेने के लिए शहज़ादों के नेतृत्व में एक-एक कर तीन अभियान भेंजे। इनमें से पहला बल्ख के विजेता औरंगजेब के नेतृत्व में था जो 50,000 सैनिकों के साथ वहाँ गया। यद्यपि मुगलां ने ईरानियों को किले के बाहर पराजित कर दिया लेकिन ईरानियों के कड़े प्रतिरोध के कारण वे किले पर पूरी तरह विजय नहीं हासिल कर सके।तीन वर्ष बाद औरंगजेब ने दूसरा प्रयास किया लेकिन फिर असफल रहा। सबसे बड़ा अभियान शाहजहाँ के प्रिय पुत्र दारा के नेतृत्व में हुआ (1653)। दारा ने बड़ी-बड़ी बातें की थीं लेकिन वह अपनी विशाल सेना के बावजूद किले की रसद को समाप्त करने तथा उस पर कब्जा करने में असफल रहा। इस हमले में साम्राज्य की दो सबसे बड़ी तोपें कंधार ले जायी गईं थीं, लेकिन उनका भी कोई खास असर नहीं हुआ। जैसा कि कुछ इतिहासकारों का मत है, कंधार में मुगलों की असफलता मुगल सेना की कमजोरी की निशानी नहीं है। इसके विपरीत इससे यह स्पष्ट होता है कि कुशल सेनापति के नेतृत्व में यह किला दुर्जेय था। इसके अलावा इस अभियान से मजबूत किलों को फतह करने में मध्य युगीन तोपखाने की अक्षमता भी प्रकट हो जाती है। (दकन में भी मुगलों का यही अनुभव रहा था।) एक तर्क यह अवश्य है कि शाहजहाँ की कंधार विजय व्यवहारिकता की अपेक्षा भावुकता से प्रेरित थी। सफवी तथा उजबेक शक्तियों के कमजोर पड़ जाने के बाद कंधार का अब वह सामरिक महत्व नहीं रहा था, जो पहले था। मुगलों की प्रतिष्ठा को जो आघात पहुँचा वह इसलिए नहीं था कि वे कंधार को अपने कब्जे में रखने में असफल रहे, बल्कि इसलिए कि उन्हें वहाँ बार-बार असफलता का समाना करना पड़ा, जिससे उनकी प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ा। परन्तु इस तथ्य पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा अपनी परकाष्ठा पर थी। यहाँ तक कि गर्वीले उस्मानी सुल्तान ने भी 1680 में औरंगजेब की सहायता प्राप्त करने के लिए अपना राजदूत भेजा था। औरंगजेब ने कंधार विजय के असफल प्रयासों पर रोक लगा दी और ईरान से राजनीतिक संबंध पुनः स्थापित किए। लेकिन सन् 1668 में ईरान के शासक, शाह अब्बास द्वितीय ने मुगल राजदूत का अपमान किया, उसके सामने औरंगजेब के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कहीं और आक्रमण की धमकी भी दी। इसके कारण स्पष्ट नहीं हैं। संभवतः शाह अब्बास द्वितीय की अस्थिर बुद्धि के कारण ही ऐसा हुआ हो। किन्तु इससे ईरान और मुगलों के संबंधों में दरार आना स्वाभाविक ही था। पंजाब तथा काबुल में मुगल गतिविधियाँ बढ़ गईं, लेकिन इसके पहले कि हमला किया जा सके, शाह अब्बास की मृत्यु हो गई। उसके उत्तराधिकारी महत्वहीन थे और 50 वर्षों के बाद जब नादिरशाह शासन में आया, तब तक भारत की सीमा पर ईरानियों का खतरा समाप्त हो गया। मुगलों की विदेशी नीति पर समग्र रूप में दृष्टिपात करने पर ज्ञात होता है कि मुगल एक ओर तो हिन्दुकुश को आधार बनाकर उत्तर-पश्चिम में तथा दूसरी ओर काबुल-गजनी सीमा पर कंधार तक एक सुनियोजित सीमा, जो भौगोलिक आधार पर लक्षित थी, स्थापित करने में सफल हो गये थे। इस प्रकार उनकी विदेश नीति का मुख्य आधार भारत की सुरक्षा थी। इस सीमा को राजनीतिक तरीकों से अधिक सुरक्षित बनाया गया। यद्यपि कंधार के मामले को लेकर दोनों में कभी-कभी अनबन हो जाती थी। मुगलों के पूर्वजों के देश को वापस लेने की बात अधिकतर राजनीतिक कारणों से दोहराई जाती थी पर इस पर कभी भी गम्भीरता से अमल नहीं किया गया। सैनिक तथा राजनीतिक उपायों से मुगल भारत को विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित रखने में बहुत हद तक सफल रहे। मुगलों की विदेश नीति की एक विशेषता यह कि उन्होंने प्रमुख एशियाई शक्तियों के साथ बराबरी का सम्बन्ध कायम रखा। विशेष रूप से सफवी तथा उस्मानी साम्राज्य से जो उस काल के सशक्त साम्राज्य थे। यह तथ्य उस स्थिति में और महत्वपूर्ण हो जाता है कि उपरोक्त दोनों साम्राज्यों के शासक अपनी-अपनी श्रेष्ठता का दावा करते थे। सफवी शासक पैगम्बर मुहम्मद से विशेष संबंध के आधार पर अपने को श्रेष्ठ समझते थे और दूसरी ओर उस्मानी सुल्तानों ने स्वयं को बगदाद के खलीफे का उत्तराधिकारी मानकर बादशाह-ए-इस्लाम की पद्वी ग्रहण कर ली थी। इसके अलावा मुगलों ने अपनी विदेश नीति का उपयोग भारत के व्यापारिक हितों को बढ़ाने के लिए किया। भारत तथा मध्य एशिया के बीच होने वाले व्यापार के लिए काबुल तथा कंधार महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार थे। मुगल साम्राज्य के लिए इस व्यापार के आर्थिक महत्व की समीक्षा होना बाकी है। प्रशासन व्यवस्था का विकास - मनसबदारी व्यवस्था तथा मुगल सेनाअकबर द्वारा विकसित प्रशासनिक तथा राजस्व व्यवस्था जहाँगीर तथा शाहजहाँ ने मामूली परिवर्तनों के साथ कायम रखी, लेकिन मनसबदारी व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गए। रख-रखाव के लिए मनसबदार को आरम्भ में 240 रूपये प्रति वर्ष प्रति सवार मिल जाते थे। बाद में जहाँगीर के शासनकाल में यह राशि घटाकर दो सौ रूपये प्रति वर्ष कर दी गई। सवारों को उनकी राष्ट्रीयता के हिसाब से वेतन मिलता था। मुगल सवार को किसी भी भारतीय मुसलमान अथवा राजपूत सवार से अधिक वेतन मिलता था। इस संबंध में घोड़े की श्रेणी का भी ध्यान रखा जाता था। मनसबदार को अपने विभिन्न खर्चों के लिए सवारों के लिए मिली राशि में से 5 प्रतिशत रखने की स्वीकृति रहती थी। मुगल मिली-जुली सेना के पक्ष में थे। उनकी सेना में इरानी तथा तूरानी मुगल, भारतीय मुसलमान (हिन्दुस्तानी) तथा राजपूत एक विशेष तादाद में रखे जाते थे। इसका उद्देश्य कबीलाई तथा जातीय भेदभाव को पनपने देने से रोकना था। परन्तु विशेष परिस्थितियों में मुगल या राजपूत मनसबदारों को केवल मुगल अथवा राजपूत सैनिकों के दल को संगठित करने की स्वीकृति दी जाती थी। इस काल में कुछ परिवर्तन भी किए गए। जात-वेतन को घटाने की प्रवृत्ति इस काल में स्पष्ट नजर आती है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि जहाँगीर ने सवार के औसत वेतन को घटा दिया था। जहाँगीर ने एक अन्य व्यवस्था शुरू की जिससे चुने हुए अमीर जात-पदवी में उन्नति के बिना सैनिकों की एक बड़़ी टुकड़ी रख सकते थे। इस व्यवस्था को दु-अस्पाह सी-अस्पाह व्यवस्था (अर्थात् दो या तीन घोड़ों वाला सैनिक) कहा जाता था। इसका अर्थ यह था कि इस व्यवस्था के अन्तर्गत मनसबदार को उसके सवार में निर्दिष्ट संख्या से दुगुनी मात्रा में सवार रखने पड़ते थे तथा उसी अनुपात से उनको दुगुना वेतन भी मिलता था। इस प्रकार 3000 जात ओ सवार (दु-अस्पाह सी-अस्पाह) मनसब के अन्तर्गत 6000 सवारों की टुकड़ी रखनी होती थी। सामान्यतः किसी भी मनसबदार को सवार की ऐसी पद्वी नहीं दी जाती थी जो उसकी जात की पदवी से अधिक हो। शाहजहाँ के शासन काल में इस व्यवस्था में एक अन्य परिवर्तन हुआ वह यह कि मनसबदारों के सवार पद में निर्दिष्ट संख्या के अनुपात में भारी कमी की गई। अब मनसबदार को अपनी सवार पदवी के आधार पर निश्चित संख्या के एक तिहाई सवारों को रखना पड़ता था। यहाँ तक कि कुछ परिस्थितियों में यह संख्या एक चौथाई अथवा 1/5 रहती थी। 3000/3000 जात ओ सवार के मनसबदार को अब 1000 से अधिक सैनिकों को नहीं रखना पड़ता था। लेकिन यदि उस सरदार की पदवी 3000 सवार दु-अस्पाह सी-अस्पाह हो तो यह संख्या दुगुनी अर्थात् 2000 सैनिकों तक पहुँच जाती थी। यद्यपि मनसबदारों का वेतन रूपयों में निश्चित किया जाता था, किन्तु उनके वेतन की अदायगी जागीर के रूप में की जाती थी। मनसबदार भी रूपयों के स्थान पर जागीर ही पसन्द करते थे क्योंकि रूपयों की अदायगी में प्रायः देर हो जाती थी और इससे परेशानी भी उठानी पड़ती थी। इसके अलावा जमीन पर अधिकार सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक था। यद्यपि निश्चित वर्गीकरण तथा कड़े नियमों से मुगलों ने वर्ग को एक अफसरशाही का रूप दे दिया था फिर भी वे जमीन के प्रति उनके सामन्ती मोह को समाप्त नहीं कर सके। जैसा कि हम देखेंगे मुगल सरदारों के लिए यह बहुत बड़ी समस्या बना हुआ था। जागीर देने के उद्देश्य से कर-विभाग को विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली आय का अनुमानित ब्यौरा (जमा) रखना पड़ता था। इस आय को रूपयों के स्थान पर दामों से आँका जाता था। चालीस दामों का मूल्य एक रूपये के बराबर होता था। इस ब्यौरे को जमा-दामी कहते थे। जैसे-जैसे मनसबदारों की संख्या बढ़ती गई, साम्राज्य की आर्थिक क्षमता कम होती गई। जिसके बहुत से कारण थे। उक्त परिस्थितियों में उपरोक्त संशोधन पर्याप्त नहीं थे। वेतनों में कटौती होने पर सरदारों में असन्तोष फैल जाता और मुगल सम्राट यह खतरा मोल नहीं ले सकते थे। इसलिए उनके लिए निश्चित सैनिकों तथा घोड़ों की संख्या पुनः घटा दी गई। मनसबदारों को वेतन अब दस महीनों, आठ महीनों, छह महीनों या उससे भी कम अवधि के आधार पर मिलने लगा और उसी अनुपात में उनके द्वारा रखे जाने वाले सवारों की संख्या भी कम कर दी गई। इस प्रकार अकबर द्वारा आरम्भ किये गये नियमों के अनुसार 3000 जात 3000 जात-ओ-सवार की पदवी वाले मनसबदार को एक हजार सवार और 2200 घोड़े रखने पड़ते थे। यदि अब उसका वेतन दस महीनों के आधार पर निश्चित होता था तब उसे केवल 1800 घोड़े रखने पड़ते थे और यदि छह महीनों के लिए निश्चित होता था तो केवल 1100 घोड़े रखने पड़ते। साधारणतया वेतनों को निश्चित करने के लिए पाँच महीनों से कम तथा दस महीनों से अधिक की अवधि नहीं रखी जाती थी। जागीर से होने वाली आय में हृास का महीनों के आधार पर वेतन (Month Scale) निर्धारण से कोई सम्बन्ध नहीं था। क्योंकि यह प्रणाली नकद वेतन तथा जागीर दोनों प्रकार के भुगतान के लिये लागू होती थी। शाहजहाँ के काल में काश्त की भूमि के क्षेत्र में विस्तार हुआ था। साथ ही तिजारती फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई थी। इस प्रकार जमा-दामी अर्थात् जागीर से होने वाली आय में भी वृद्धि हुई थी। परन्तु यह वृद्धि अधिकांशतः तत्कालीन मूल्य वृद्धि के स्तर पर ही रही। इसी कारण जमा दामी में वृद्धि का विशेष फायदा न हुआ। यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि मुगल सेवा में जिन मराठों को नियुक्त किया गया था उनमें से अधिकतर के मनसब पाँच महीनों या उससे कम के आधार पर तय किए गए थे। इस प्रकार यद्यपि उनका पद ऊँचा था, उनके द्वारा रखे गये घोड़ों तथा सवारों की संख्या उनके पदों में निर्दिष्ट संख्या से बहुत कम थी। जैसा कि हम देख चुके हैं कि अच्छी घुड़सवार सेना के लिए यह आवश्यक था कि घोड़े पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों। शाहजहाँ के शासनकाल में घोड़ों की कमी से मुगल घुड़सवार सेना पर अवश्य ही बुरा प्रभाव पड़ा होगा। मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था बड़ी पेचीदा थी। इसकी सफलता कई तत्वों पर निर्भर थी, जिसमें जागीरदारी व्यवस्था तथा घोड़ों को दागने की व्यवस्था का कुशल संचालन भी महत्वपूर्ण है। यदि दाग व्यवस्था का अच्छी तरह पालन नहीं होता था, तो साम्राज्य को नुकसान पहुँचता था। यदि जमा दामी को बढ़ा दिया जाता था या फिर जागीरदारों को उनका निश्चित वेतन नहीं मिलता था, तब उनका असंतोष बढ़ जाता था और वे निश्चित संख्या के सवारों अथवा घोड़ों को रखना छोड़ देते थे। कुल मिलाकर मनसबदारी व्यवस्था शाहजहाँ के शासनकाल में सफल रही क्योंकि शाहजहाँ स्वयं सूक्ष्मता से प्रशासन की देख-रेख करता था तथा बड़े योग्य व्यक्तियों को वजीरों के रूप में नियुक्त करता था। कुशल और योग्य व्यक्तियों की सेवा में नियुक्ति, कड़े अनुशासन तथा पदोन्नति व पुरूस्कार के लिये निश्चित नियमों के पालन के कारण मुगल उमरा वर्ग एक ऐसे वर्ग के रूप में ढल गया जो वफादार और भरोसेमंद था तथा जिसमें प्रशासनिक कार्यां और साम्राज्य की सुरक्षा को बनाये रखने के लिए पर्याप्त योग्यता थी। मुगल सेनाजैसा कि हम देख चुके हैं कि घुड़सवार मुगल सेना के प्रमुख अंग थे और इन्हें उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व अधिकतर मनसबदारों पर था। मनसबदारों के अलावा मुगल बादशाह अलग से भी वीर घुड़सवार रखते थे, जिन्हें अहदी पुकारा जाता था। अहदियों को बहुत ऊँचा वेतन मिलता था। इनकी नियुक्ति सम्राट स्वयं करता था और इनका अपना सेना अध्यक्ष होता था। यह सैन्यदल अत्यन्त विश्वसनीय था। एक अहदी पाँच घोड़े तक रखता था। यद्यपि कभी-कभी दो अहदी मिलकर एक घोड़ा भी रखते थे। अहदियों के कर्तव्य विविध प्रकार के होते थे। सरकारी दफ्तरों के अधिकतर लिपिक, राजदरबार के चित्रकार तथा कारखानों के फोरमैन इसी वर्ग से नियुक्त होते थे। इनमें से कई राजसी आदेशों को ले जाने के लिए नियुक्त किये जाते थे। शाहजहाँ के शासन काल में अहदियों की संख्या 7000 थीं। इन्हें कई बार लड़ाई के मैदान में भी भेजा जाता था। जहाँ उन्हें विविध स्थानों पर तैनात किया जाता था। इनमें से कई कुशल तीरंदाज और वरकन्दाज होते थे।अहदियों के अलावा सम्राट अंगरक्षकों की एक टुकड़ी भी रखते थे। (इन्हें वालाशाही पुकारा जाता था)। इसके अलावा महलों की सुरक्षा के लिए भी सैनिक दल रहते थे। ये वास्तव में घुड़सवार होते थे लेकिन महल तथा किलों की देख-रेख पैदल ही करते थे। एक अन्य वर्ग पियादगानों का था। ये संख्या में बहुत थे और इनके कर्तव्य भी विविध प्रकार के होते थे। इनमें से बहुत से बन्दूकची होते थे और इन्हें तीन से सात रूपये प्रतिमाह तक वेतन मिलता था। वास्तव में मुगल सेना के प्यादे यही थे। प्यादों में कुली, नौकर, पहलवान, तलवार बाज तथा गुलाम शामिल थे। इस काल में गुलामों की संख्या सल्तनत काल से कम थी और इन्हें सम्राट अथवा राजकुमार की ओर से खाना कपड़ा मिलता था। कभी-कभी गुलामों की पदोन्नति अफसरों के पद तक हो जाती थी लेकिन आमतौर पर प्यादों का स्तर निम्न ही रहता था। मुगल सम्राट बड़ी संख्या में हाथी भी रखते थे तथा उनका तोपखाना बड़ा सुसंगठित रहता था। तोपखाने के दो विभाग थे - किलों की रक्षा अथवा उन पर हमला करने के लिए भारी तोपें जो इतनी भारी होती थीं कि उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बड़ा कठिन होता था। इनके अलावा छोटी व हल्की तोपें थीं जो कहीं भी आसानी से ले जायी जा सकती थीं। मुगल अपने तोपखाने के सुधार के लिए बराबर प्रयत्नशील रहते थे और उन्होंने आरम्भ में इस विभाग में रूमियों तथा पुर्तगालियों की नियुक्ति भी की थी। औरंगजेब के समय तक मुगल तोपखाना अत्यन्त विकसित हो गया था और विदेशियों को इस विभाग में मुश्किल से नियुक्ति मिलती थी। बड़ी तोपों का आकार कभी-कभी जरूरत से ज्यादा ही बड़ा होता था। उनको लाना ले जाना अत्यन्त दुष्कर होता था। जबकि उनसे फायदे उस अनुपात में नहीं होते थे। जैसा कि एक लेखक ने कहा है - ‘‘इन तोपों से आवाज अधिक और नुकसान कम होता था। ये दिन में कई बार दागी नहीं जा सकती थीं और यह खतरा बना रहता था कि ये फटकर दागने वालों को ही मार देंगी’’, लेकिन दूसरी ओर शाहजहाँ के साथ लाहौर तथा कश्मीर जाने वाले फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने हल्की तोपों की बहुत प्रशंसा की और कहा कि ये वस्तुतः ‘‘रकाब की तोपें थी।’’ उसका कहना है कि ‘ये तोपें पीपल के पचास छोटे टुकड़ों से बनी होती थीं तथा हर तोप एक सुन्दर व रंगीन गाड़ी पर रखी जाती थी। जिस पर बारूद के दो बक्से भी रखे जाते थे। इस गाड़ी को दो उत्तम घोड़े खीचते थे तथा एक घोड़ा अतिरिक्त होता था। हल्की तोपों को हाथियों तथा ऊँटों की पीठ पर भी रखा जाता था। मुगल सेना की शक्ति का सही अनुमान लगाना कठिन है। शाहजहाँ के शासनकाल में इसमें 200000 घुड़सवार थे, जिनमें प्रान्तों तथा फौजदारों के साथ काम करने वाले सैनिक शामिल नहीं थे। औरंगजेब के शासन में यह संख्या बढ़कर 240000 हो गई। शाहजहाँ के शासनकाल में पैदल सेना की संख्या 40000 और संभव है कि औरंगजेब के शासनकाल में भी इनकी संख्या इतनी ही रही हो। पश्चिम अैर मध्य एशिया तथा यूरोपीय राज्यों की सेनाओं के मुकाबले में मुगल सेना कैसी थी ? इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। यद्यपि बर्नियर जैसे कई यूरोपीय यात्रियों ने मुगल सेना के बारे में बहुत अच्छे विचार व्यक्त नहीं किये हैं। परन्तु उनकी बातों का सावधानी से विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी बातें अधिकतर मुगल पैदल सेना पर लागू होती हैं। जिनमें कोई अनुशासन नहीं था और न ही वे अच्छी तरह संगठित थीं। उनका नेतृत्व भी बेतरतीब था और ऐसा लगता था कि एक भीड़ जमा हो गयी हो। जबकि यूरोप में पैदल सेना का विकास अन्य ढंग से हुआ था। सत्रहवीं शताब्दी में बन्दूक के विकास के बाद पैदल सेना की शक्ति बहुत बढ़ गई थी और कभी-कभी तो यह घुड़सवार सेना को भी मत दे देती थी। भारतीयों को इस तथ्य का आभास अठारहवीं शताब्दी में बहुत बड़ा मूल्य चुका कर हुआ। बल्ख अभियान के समय उजबेकों के खिलाफ मुगलों की सफलता से पता चलता है कि मुगल सेना मध्य एशिया तथा ईरानी सेनाओं से खुले युद्ध में बहुत कमजोर नहीं पड़ती थी। मुगल सेना की मुख्य कमजोरी नौसेना के क्षेत्र में व विशेष रूप से सामुद्रिक युद्धों में व्यक्त हुई। उच्च कोटि का तोपखाना न होने पर भी मुगल सेना औरंगजेब के समय तक एशिया की अन्य शक्तियों के मुकाबले हो गई थी। यह और बात है कि यह यूरोपीय शक्तियों की सेनाओं जैसी शक्तिशाली नहीं थी। क्योंकि उनकी शक्ति का मुख्य आधार नौ सेना थी। कुल मिलाकर सेना की व्यवस्था और विशेषकर घुड़सवारों की उपलब्धि जगीरदारी व्यवस्था पर निर्भर थी जो देश में प्रचलित भूमि संबंधों पर आधारित सामन्ती व्यवस्था पर निर्भर थी। कुल मिलाकर एक की शक्ति और सफलता दूसरे की शक्ति पर निर्भर करती थी। | |||||||||
| |||||||||