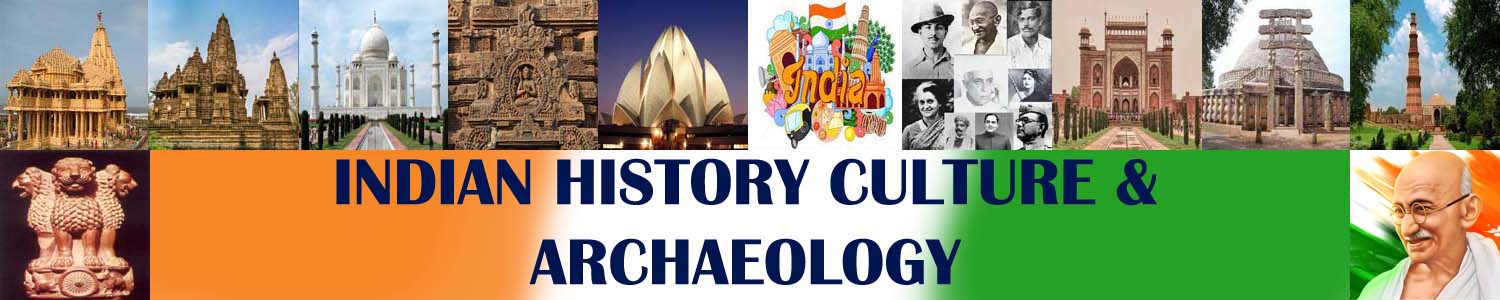| |||||||||
|
प्राचीन भारत की विरासत
धर्मप्रकृति के साथ मानव का सामना होने के परिणामस्वरूप बहुत-सी विलक्षण घटनाएँ हुईं। लोगों को अपनी जीविका प्राप्त करने में जंगल, पहाड़, कड़ी मिट्टी, सूखा, बाढ़, पशु आदि से होने वाली कठिनाइयों से निपटना पड़ा। लेकिन कई कठिनाइयों पर काबू पाना असम्भव मालूम हुआ और प्रकृति की लीलाएँ समझ के बाहर प्रतीत हुर्इं। इसलिए अगत्या लोगों को प्रकृति के साथ समझौता कर लेना पड़ा। अपने सारे प्रयासों के बावजूद लोगों को प्रकृति के विविध वरदानों पर निर्भर रहना पड़ा, जैसे मिट्टी की उर्वरता, समय पर वर्षा होना आदि। प्रकृति की कृपालुता और क्रूरता दोनों ने मानव को धर्म और अलौकिक शक्ति के विषय में सोचने को बाध्य किया।भारत में ब्राह्मण धर्म या हिन्दू धर्म पूर्व काल में प्रभावशाली रूप में विकसित हुआ। इसने कला और साहित्य को तथा समाज को भी प्रभावित किया। हिन्दू धर्म के साथ-साथ भारत में जैन और बौद्ध धर्म भी उदित हुए। यद्यपि ईसाई धर्म इस देश में ईसा की पहली सदी के आसपास ही आया, फिर भी प्राचीन काल में यह अधिक आगे नहीं बढ़ सका। बौद्ध धर्म भी धीरे-धीरे इस देश से गायब हो गया, हालाँकि यह बढ़ते-बढ़ते पूरब में जापान तक और पश्चिमोत्तर में मध्य एशिया तक फैल चुका था। अपने प्रचार-प्रसार के क्रम में बौद्ध धर्म ने पड़ोसी क्षेत्रों को भारतीय कला, भाषा और साहित्य से उद्भासित किया। जैन धर्म भारत में टिका रहा और यहाँ की कला और साहित्य के विकास में प्रेरणा देता रहा। आज भी इस धर्म के अनुयायी लोग विशेष कर व्यापारी वर्गों में, राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक में भारी संख्या में छाए हुए हैं। वर्ण-व्यवस्थाभारत में धर्म के प्रभाव से एक विशेष प्रकार के सामाजिक वर्गों का गठन हुआ। अन्य प्राचीन मानव समाजों में विभिन्न सामाजिक वर्गों के कर्तव्यों का निर्धारण कानून के जरिए हुआ और उसे अमल में लाने वाला राज्य था। परन्तु भारत में वर्णसम्बन्धी नियमों को राज्य और धर्म दोनों का समर्थन प्राप्त था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णां के कर्तव्य तो विधि द्वारा सुपरिसीमित किए हुए थे, परन्तु ऐसा विश्वास प्रचलित था कि यह वर्णव्यवस्था ईश्वर की बनाई हुई है। जो कोई अपने निर्धारित कर्तव्यों से च्युत होता था और अपराधी पाया जाता था उसे लौकिक दंड तो भोगना ही पड़ता था, साथ-साथ प्रायश्चित अर्थात् धार्मिक शुद्धि भी करनी पड़ती थी और ये दंड अपराधी के वर्ण के अनुसार भिन्न-भिन्न कोटि के होते थे। हर वर्ण की न केवल सामाजिक पहचान, बल्कि धार्मिक पहचान भी थी। धीरे-धीरे कानून और धर्म दोनों ने वर्णों और जातियों के कर्ममूलक से जन्ममूलक या आनुवंशिक बना दिया। यह सब इसलिए किया गया कि वैश्य उत्पादन करते और कर चुकाते रहें और शूद्र मजदूरी में खटते रहें ताकि ब्राह्मण पुरोहितों के पद पर बने रहें और क्षत्रिय शासकों के पद पर। श्रम-विभाजन और व्यवसाय के विशेषीकरण के सिद्धांत पर टिकी यह अद्भुत वर्णव्यवस्था आरम्भिक अवस्था में अवश्य ही सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायक हुई। वर्णव्यवस्था का हाथ राज्य के विकास में भी रहा। उत्पादक वर्ग और श्रमिक वर्ग अर्थात् वैश्य और शूद्र दोनों अस्त्रहीन कर दिए गए और धीरे-धीरे हर जाति दूसरी जाति के विरूद्ध इस तरह खड़ी कर दी गई कि शोषित वर्ग सुविधाभोगी वर्गो के खिलाफ एकजुट न होने पाएँ।अपने-अपने कर्तव्यों में लगे रहने में ही कल्याण है ऐसी धारणा विभिन्न वर्गों के मन में इस तरह बद्धमूल हो गई थी कि सामान्यतः वे अपने धर्म से विचलित होने की बात सोच भी नहीं सकते थे। भगवद्गीता सिखाती है कि अपना कर्म करते हुए मर जाना भी दूसरे का कर्म हड़पने से कहीं अच्छा है। निम्न वर्णों के लोग अपने कठिन कर्तव्य का पालन इस दृढ़ विश्वास के साथ करते रहे कि अगले जन्म में वे सुख की जिन्दगी पाएंगे। इस विश्वास के फलस्वरूप एक ओर पैदा करके सबको खिलाने वालों और दूसरी ओर बिना कुछ किए मुफ्त का खाने वाले राजाओं, पुरोहितों, अधिकारियों, सेनानियों और बड़े-बड़े श्रेष्ठ व्यक्तियों के बीच लड़ाई-झगड़े बहुत ही कम हुए। इसीलिए निम्न वर्णों को दबाने-सताने की कार्रवाई प्राचीन भारत में आवश्यक नहीं हुई। जो कुछ भी यूनान और रोम में गुलामों और अन्य उत्पादक वर्गों से कोड़े का डर दिखाकर कराया जाता था वह यहाँ के वैश्य और शूद्र स्वतः करते थे, क्योंकि ब्राह्मण धर्म और वर्ण-व्यवस्था ने उनके दिमाग में ऐसी ही धारणा जमा दी थी। दार्शनिक पद्धतियाँभारतीय चिन्तकों ने संसार को माया समझा तथा आत्मा और परमात्मा के बीच के सम्बन्धों की गम्भीर विवेचना की। वास्तव में इस विषय का जितना गहन चिन्तन भारतीय दार्शनिकों ने किया उतना किसी अन्य देश के दार्शनिकों ने नहीं। परन्तु भारत में जगत् के विषय में भौतिकवादी विचारधारण भी विकसित हुई। भारत में उदित छह दार्शनिक पद्धतियों के बीच हम भौतिकवादी दर्शन के तत्व सांख्य में पाते हैं, जिसके संस्थापक कपिल 580 ई. पू. के आसपास उत्पन्न हुए थे। उनके अनुसार आत्मज्ञान के साधन हैं - प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। सांख्यदर्शन में ईश्वर का अस्तित्व नहीं माना गया है। इसके अनुसार संसार की सृष्टि ईश्वर ने नहीं, प्रकृति ने की है तथा संसार और मानव-जीवन की नियामिका स्वयं प्रकृति है।भौतिकवादी दर्शन को ठोस बनाने का सबसे बड़ा श्रेय चार्वाक को है, जो ईसापूर्व छठी सदी के आसपास हुए थे। उन्होंने जिस दर्शन की स्थापना की वह लोकायत कहलाता है। उनका मत है कि जिसका अनुभव मनुष्य अपनी इन्द्रियों द्वारा नहीं कर सकता है उसका वास्तव में अस्तित्व नहीं हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि ईश्वर नामक कोई वस्तु नहीं है। लेकिन व्यापार, शिल्प और नगरीकरण में हृास होने के साथ ही दर्शन में प्रत्ययवाद की प्रमुखता हो गई। प्रत्ययवादी दर्शन बताता है कि संसार माया और भ्रम है। उपनिषदों में लोगों को उपदेश दिया गया है कि सांसारिक विषयों से दूर रहें और ज्ञान पाने की चेष्टा करें। पाश्चात्य चिन्तकों ने उपनिषदों के उपदेशों को अपनाया क्योंकि वे आज के यान्त्रिक युग द्वारा पैदा की गई समस्याओं का समाधान कर पाने में असमर्थ थे। प्राख्यात जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर ने अपनी दार्शनिक विचारधारा में वेदों और उपनिषदों को भी स्थान दिया है। वह कहा करते थे कि उपनिषदों ने उन्हें इन जन्म में दिलासा दी है मृत्यु के बाद भी देती रहेंगी। शिल्प और प्रौद्योगिकीयह कहना गलत होगा कि भारतीयों ने भौतिक संस्कृति में कोई प्रगति नहीं की। उन्होंने उत्पादन के कई क्षेत्रों में निपुणता प्राप्त की। भारतीय शिल्पी रंगाई करने तथा तरह-तरह के रंग बनाने में परम दक्ष थे। भारत में बनाए गए मूल रंग इतने चमकीले और पक्के होते थे कि अजन्ता और ऐलोरा के मोहक चित्र आज भी ज्यों के त्यों हैं।इसी तरह भारत के लोग ईस्पात बनाने में भी परम कुशल थे। ईस्पात बनाने की कला सबसे पहले भारत में विकसित हुई। भारतीय ईस्पात का अन्य देशों में निर्यात ईसा-पूर्व चौथी सदी से होने लगा और बाद में आकर वह उट्ज (Wootz) कहलाने लगा। विश्व का कोई अन्य देश ईस्पात की वैसी तलवारें नहीं बना सकता था जैसी भारतीय शिल्पी बनाते थे। पूर्वी एशिया से लेकर पूर्वी यूरोप तक इन तलवारों की भारी माँग थी । राज्यतंत्रकौटिल्य के अर्थशास्त्र से इस बात में कोई शंका नहीं रह गई है कि भारत के लोग विशाल साम्राज्य का प्रशासन चला सकते थे और जटिल समाज की समस्याओं को हल कर सकते थे। देश ने अशोक के रूप में एक महान शासक पैदा किया, जिसने कलिंग पर शानदार विजय पाकर भी शान्ति और अनाक्रमण की नीति अपनाई। अशोक और कई अन्य भारतीय राजाओं ने धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया और बताया कि अन्य धर्मों के अनुयायियों की भावना का आदर किया जाए और यूनान के अलावा भारत ही एक ऐसा देश था जहाँ किसी न किसी प्रकार के गणतंत्र का प्रयोग-परीक्षण किया गया हो।विज्ञान और गणितभारत का विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान है। प्राचीन काल में धर्म और विज्ञान आपस में गुँथे-से थे। इस देश में खगोल-विद्या में इसलिए बहुत प्रगति हुई कि ग्रह देवता माने जाने लगे थे और उनकी गति का गहन अवलोकन आरम्भ हो गया। ग्रहों का अध्ययन इसलिए भी आवश्यक हो गया कि उनका सम्बन्ध ऋतुओं और मौसमों के परिवर्तनों से था और इन परिवर्तनों की जानकारी खेती के काम में आवश्यक थी। व्याकरण और भाषाविज्ञान का उद्भव इसलिए हुआ कि ब्राह्मण पुरोहित वेद की ऋचाओं और मन्त्रों के उच्चारण की शुद्धता को महत्व देते थे। वास्तव में भाषा के सम्बन्ध में भारतीयों की वैज्ञानिक दृष्टि का प्रथम फल संस्कृत व्याकरण की रचना। ईसा पूर्व चौथी सदी में संस्कृत भाषा के नियमों को सुव्यवस्थित रूप से संचित करके पाणिनि ने एक व्याकरण लिखा जो अष्टाध्यायी के नाम से प्रख्यात है।ईसा-पूर्व तीसरी सदी में आकर गणित, खगोल-विद्या और आयुर्विज्ञान तीनों का विकास अलग-अलग आरम्भ हुआ। गणित के क्षेत्र में प्राचीन भारतीयों ने तीन विशिष्ट योगदान किए - अंकनपद्धति, दाशमिक पद्धति और शून्य का प्रयोग। दाशमिक पद्धति के प्रयोग का सबसे पुराना उदाहरण ईसा की पाँचवीं सदी के आरम्भ का है। भारतीय अंकन पद्धति को अरबों ने अपनाया और उसको पश्चिमी दुनिया में फैलाया। अंग्रेजी में भारतीय अंकमाला को अरबी अंक (अरेबिक न्यूमरल्स) कहते हैं, किन्तु अरब लोग स्वयं इसे हिन्दसा कहते हैं। पश्चिम में इस अंकमाला का प्रचार होने के सदियों पहले से भारत में इसका प्रयोग हुआ। इसका प्रयोग अशोक के अभिलेखों में पाया जाता है, जो ईसा-पूर्व तीसरी सदी में लिखे गए। दाशमिक पद्धति का प्रयोग सबसे पहले भारतीयों ने किया। प्रख्यात गणितशास्त्री आर्यभट (376-500 ई.) इससे परिचिति थे। चीनियों ने यह पद्धति बौद्ध धर्मप्रचारकों से सीखी और पश्चिम जगत ने अरबों से सीखी, जबकि वे भारत के सम्पर्क में आए। शून्य का आविष्कार भारतीयों ने ईसा-पूर्व दूसरी सदी में किया। जबसे इसका आविष्कार हुआ, भारतीय गणितज्ञ इसको एक पृथक अंक समझने लगे और इस रूप में इसका प्रयोग अंकगणना में होने लगा। अरब देश में शून्य का प्रयोग सबसे पहले 873 ई. में पाया जाता है। अरबों ने इसे भारत से सीखा और यूरोप में फैलाया। बीजगणित में भारतीय और यूनानी दोनों का योगदान रहा है परन्तु पश्चिम यूरोप में उसका ज्ञान यूनान से नहीं, बल्कि अरब से मिला, जो अरब ने भारत से प्राप्त किया था। हड़प्पा में बनी र्इंट की इमारतों से प्रकट होता है कि पश्चिमोत्तर भारत में लोगों को मापन और ज्यामिति का अच्छा ज्ञान था। बाद में वैदिक लोगों ने इस ज्ञान से लाभ उठाया होगा, जो ईसा-पूर्व पाँचवीं सदी के आसपास के शुल्बसूत्रों में दिखाई देता है। ईसापूर्व दूसरी सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञवेदी बनाने के लिए आपस्तम्ब ने एक व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की। इसमें न्यूनकोण, अधिककोण और समकोण का वर्णन किया गया है। आर्यभट ने त्रिभुज का क्षेत्रफल जानने का नियम निकाला जिसके फलस्वरूप त्रिकोणमिति का जन्म हुआ। इस काल की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है सूर्यसिद्धान्त। पूरब में इस तरह की कोई दूसरी समकालीन कृति नहीं पाई गई है। खगोल शास्त्र में आर्यभट और वराहमिहिर दो महान् विद्वान हुए। आर्यभट पाँचवीं सदी में हुए और वराहमिहिर छठी सदी में। आर्यभट ने बेबिलोनियाई विधि से ग्रह-स्थिति की गणना की। उन्होंने चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहण के कारण का पता लगाया। उन्होंने अनुमान के आधार पर पृथ्वी की परिधि का मान निकाला जो आज भी शुद्ध माना जाता है। उन्होंने बताया कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमती है। आर्यभट की पुस्तक का नाम आर्यभटीय है। वराहमिहिर की सुविख्यात कृति है बृहत्संहिता। यह ईसा की छठी सदी की है। वराहमिहिर ने बताया कि चन्द्र पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। उन्होंने ग्रहों के संचार और अन्य खगोलीय समस्याओं के अध्ययन में यूनानियों की अनेक कृतियों का सहारा लिया। यद्यपि भारतीय खगोल-शास्त्रियों ने यूनानियों के ज्ञान से लाभ उठाया तथापि उन्होंने इस ज्ञान को आगे बढ़ाया और ग्रहों की गति के अवलोकन में इस ज्ञान का प्रयोग किया। प्रायौगिक विज्ञान के क्षेत्र में, भारतीय शिल्पियों ने रसायनविद्या की प्रगति में बहुत योगदान दिया। भारतीय रंगरेजों ने टिकाऊ रंगों का विकास किया और नील का आविष्कार किया। पहले बताया जा चुका है कि भारतीय लोहारों ने किस प्रकार दुनिया में सबसे पहले इस्पात का निर्माण किया। आयुर्विज्ञानप्राचीन भारत के वैद्यों को शरीर-रचना (एनेटॉमी) का ज्ञान था। उन्होंने रोगों के निदान की विधियाँ बनाई और इलाज के लिए औषध (दवा) बताई। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। परन्तु अन्य प्राचीन समाजों की भाँति, बताए गए उपचारों में जादू-टोना और तंत्र-मंत्र भी भर गए और आयुर्विज्ञान का विकास वैज्ञानिक रीति से नहीं हुआ।ईसा की दूसरी सदी में भारत में आयुर्वेद के दो महान् विद्वान उत्पन्न हुए - सुश्रुत और चरक। अपनी सुश्रुतसंहिता में सुश्रुत ने मोतियाबिन्द, पथरी तथा और कई रोगों का शल्योपचार बताया है। उन्होंने शल्य-क्रिया के बहुत सारे उपकरणों का उल्लेख किया है, जिनकी संख्या 121 तक हैं। रोगों से मुक्ति के लिए उन्होंने आहार और सफाई पर जोर दिया है। चरकसंहिता भारतीय चिकित्साशास्त्र का विश्वकोष है। इसमें ज्वर, कुष्ठ, मिरगी और यक्ष्मा के अनेक भेदोपभेदों का वर्णन है। शायद चरक यह नहीं जानते थे कि कुछ बीमारियाँ छूत से भी फैलती हैं। इनकी पुस्तक में भारी संख्या में उन पेड़-पौधों का वर्णन है जिनका प्रयोग दवा के रूप में होता है। इस प्रकार यह पुस्तक न केवल भारतीय आयुर्विज्ञान के अध्ययन के लिए, बल्कि प्राचीन भारत के वनस्पति और रसायन के अध्ययन के लिए भी उपयोगी है। बाद की सदियों में भारत में आयुर्विज्ञान का विकास चरक के बताए मार्ग पर होता रहा। भूगोलभूगोल के अध्ययन में भी प्राचीन भारत के लोगों का कुछ योगदान है। उन्हें भारत से बाहर की दुनिया का भौगोलिक ज्ञान अत्यल्प था, परन्तु देश के विभिन्न प्रदेशों की नदियों, पर्वतों और तीर्थ स्थलों का विशद वर्णन रामायण, महाभारत और पुराणों में मिलता है। यद्यपि भारत के लोग चीन और पश्चिमी देशों के बारे में कुछ-कुछ जानते थे, पर वे नहीं जानते थे कि ये देश कहाँ और भारत से कितना दूर हैं।पूर्व काल में प्राचीन भारतीयों को समुद्रयात्रा का कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने जहाज बनाने की कला में कुछ योगदान दिया। परन्तु चूँकि बड़ी-बड़ी राजनैतिक शक्तियों के केन्द्रस्थल समुद्रतट से बहुत दूर थे और समुद्र की ओर से कोई खतरा नहीं था, इसलिए प्राचीन भारत के राजाओं ने नौपरिवहन की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। कला और साहित्यप्राचीन भारत के राजमिस्त्री और शिल्पी सुन्दर-सुन्दर कलाकृतियाँ बनाते थे। अशोक द्वारा बनवाए गए अखंड प्रस्तर के स्तम्भ अपनी चमकदार पालिश के लिए प्रसिद्ध हैं और उनकी पालिश की तुलना उत्तरी काले पालिशदार मृद्भांड की पालिश से की जा सकती है। यह अब भी एक रहस्य बना हुआ है कि शिल्पकारों ने स्तम्भों और मृद्भांडों पर कैसे इस तरह की पालिश की। मौर्यकालीन पालिशदार स्तम्भों के शीर्ष पर पशुओं, विशेषकर सिंहों की मूर्तियाँ हैं। सिंह की मूर्ति वाले स्तम्भशीर्ष को भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिह्न स्वीकार किया है। अजन्ता के गुहा-मन्दिरों और विख्यात चित्रों का उल्लेख यहाँ गौरव के साथ किया जा सकता है, जो ईस्वी सन् के आरम्भ काल के हैं। इस प्रकार से अजन्ता एशियाई कला का जन्मस्थान है। वहाँ ईसा-पूर्व दूसरी और सातवीं सदियों के बीच अनेक गुहा-मन्दिर बने जिनकी संख्या 30 तक है। चित्रों की रचना ईसा की दूसरी सदी में शुरू हुई। अधिकतर चित्र गुप्तकाल के बने हैं। उनके विषय जातक कथाओं और प्राचीन साहित्यों में लिए गए हैं। अजन्ता के चित्रकारों की उपलब्धियों की सराहना सभी कला-मर्मज्ञों ने मुक्त कंठ से की है। अजन्ता की रेखाएं और रंग ऐसी निपुणता प्रदर्शित करते हैं जो यूरोपीय पुनर्जागरण के पहले संसार भर में कहीं नहीं पाई गई हैं। इतना ही नहीं, भारतीय कला भारत के भीतर ही नहीं समाई रही, वह एक ओर मध्य एशिया और चीन तक तथा दूसरी ओर दक्षिण-पूर्व एशिया तक फैल गई। अफगानिस्तान और मध्य एशिया के पड़ोसी भाग में भारतीय कला के प्रसार का केन्द्र-बिन्दु गन्धार था। भारतीय कला और यूनानी कला दोनों के तत्वों के सम्मिश्रण से एक नई कला-शैली का जन्म हुआ, जो गन्धार शैली के नाम से प्रसिद्ध है। बुद्ध की पहली प्रतिमा इसी शैली में बनी है। उनके नाक-नक्शा तो भारतीय हैं, लेकिन उनके आकार में तथा सिर की रचना और वस्त्र-विन्यास में यूनानी प्रभाव दिखाई देता है। इसी प्रकार दक्षिण भारत में बने मन्दिर तो दक्षिण-पूर्व एशिया में मन्दिर-निर्माण के आदर्श ही बन गए। हम कम्बोडिया में अंकोरवट के मन्दिर और जावा में बोरोबुदुर के मन्दिर की चर्चा कर चुके हैं।शिक्षा के क्षेत्र में नालन्दा का विशाल बौद्ध विहार उल्लेखनीय है। वहाँ न केवल भारत के विभिन्न भागों से, बल्कि तिब्बत और चीन से भी छात्र पढ़ने के लिए आते थे। परीक्षा का मानदण्ड कड़ा था। इसमें प्रवेश केवल उन्हीं का होता था जो द्वारपण्डित द्वारा ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण होते थे। नालन्दा का विहार आवासीय सह-शिक्षण संस्थान का सबसे प्राचीन उदाहरण है, जहाँ विद्या, दर्शन और ध्यान के प्रति समर्पित हजारों भिक्षु रहते थे। साहित्य के क्षेत्र में प्राचीन भारतीयों ने ऋग्वेद की रचना की जो भारतीय आर्य साहित्य की सबसे पुरानी कृति है और जिसके आधार पर आर्यसंस्कृति का स्वरूप अवधारित करने की चेष्टा की गई है। गुप्त काल में हम कालिदास की कृतियाँ पाते हैं, जिनमें एक अभिज्ञान शाकुन्तल का अनुवाद विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं में हुआ है। | |||||||||
| |||||||||