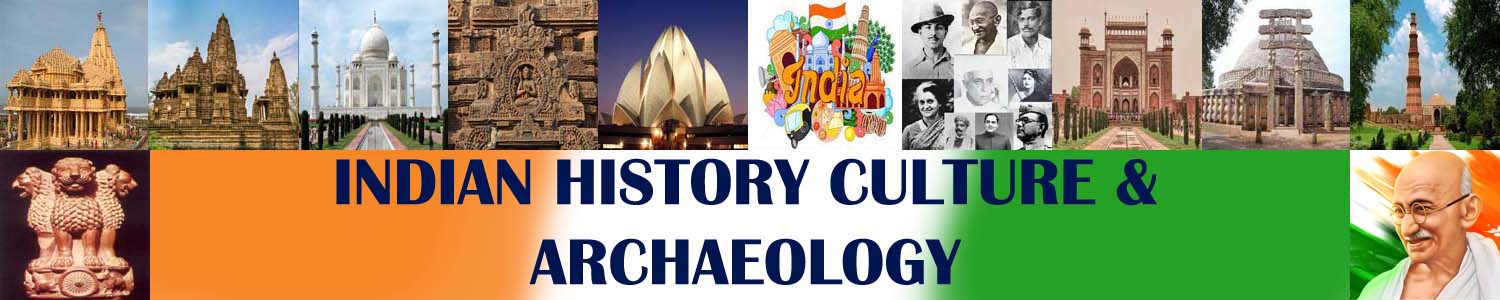| |||||||||
|
स्वतंत्रता आन्दोलन का विकास एवं भारतीय स्वतंत्रता
नई शक्तियों का अविर्भाववर्ष 1927 में राष्ट्रीय आंदोलन में फिर से शक्ति पाने के अनेक संकेत देखे गए। इसी वर्ष समाजवाद की नई प्रवृत्ति का भी उदय हुआ। मार्क्सवाद और दूसरे समाजवादी विचार बहुत तेजी से फैले। राजनीतिक दृष्टि से इस शक्ति की अभिव्यक्ति कांग्रेस के अंदर एक वामपंथ के उदय के रूप में हुई। इस नई प्रवृति के नेता जवाहरलाल नेहरु और सुभाषचन्द्र बोस थे। इस वामपंथ ने अपना ध्यान साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष तक ही सीमित नहीं रखा। साथ ही साथ उसने पूँजीपतियों और जमींदारों के आंतरिक वर्गीय शोषण का सवाल भी उठाया।भारत के नौजवान सक्रिय हो रहे थे। पूरे देश में नौजवान सभाएँ बन रही थीं और छात्रों के सम्मेलन हो रहे थे। पहला अखिल-बंगाल छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 में जवाहरलाल नेहरु की अध्यक्षता में हुआ। इसके बाद देश में अनेक दूसरे छात्र संगठन बने तथा सैकड़ों छात्र-युवा सम्मेलन आयोजित किए गए। इसके अलावा भारत के युवा राष्ट्रवादी धीरे-धीरे समाजवाद की तरफ आकर्षित होने लगे और देश जिन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बुराइयों से पीड़ित था, उनके लिए दूरगामी हल सुझाने लगे। उन्होंने पूर्ण स्वाधीनता का कार्यक्रम भी सामने रखा तथा उसे लोकप्रिय बनाया। तीसरे, देश में समाजवादी और कम्युनिस्ट गुटों की स्थापना हुई। रुसी क्रांति की विख्यात घटना ने अनेक युवा राष्ट्रवादियों को आकर्षित किया था। उनमें से अनेक गाँधीवादी राजनीतिक विचारों और कार्यक्रमों से असंतुष्ट थे। वे मार्गदर्शन पाने के लिए समाजवादी विचारधारा की ओर मुड़े मानवेंद्रनाथ राय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व-वर्ग में चुने गए, इसके लिए चुने जाने वाले वे पहले भारतीय थे। 1924 में सरकार ने मुजफ्फर अहमद और श्रीपाद अमृत डांगे को गिरफ्तार करके उन पर कम्युनिस्ट विचारों के प्रचार का आरोप लगाया और उन्हें तथा कुछ और लोगों को लेकर कानपुर षड़यंत्र का मुकदमा चलाया। 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। इसके अलावा देश के अनेक भागों में मजदूर-किसान पार्टियाँ बनीं। इन पार्टियों और समूहों ने मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट विचारों का प्रचार किया। लेकिन साथ ही वे लोग राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय कांग्रेस के अभिन्न अंग भी थे। किसान और मजदूरों में भी पुनः हलचल मच रही थी। संयुक्त प्रांत में बँटाईदारी के कानूनों में संशोधन के लिए बँटाईदारों ने बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाया। ये बँटाईदार लगान में कमी, बेदखली से सुरक्षा तथा कर्ज में राहत चाहते थे। गुजरात के किसानों ने जमीन की मालगुजारी बढ़ाने के सरकारी प्रयासों का विरोध किया। बारदोली का प्रसिद्ध सत्याग्रह इसी समय हुआ। 1928 में सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने टैक्स न देने का आंदोलन चलाया और अंत में अपनी माँगें मनवाने में सफल रहे। अखिल-भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेतृत्व में मजदूर संघों का तेजी से विकास हुआ। 1928 में अनेक हड़तालें हुईं। खड़गपुर के रेलवे वर्कशाप में दो माह तक एक लंबी हड़ताल चली। दक्षिण भारतीय रेल मजदूरों ने भी हड़ताल की। जमशेदपुर में टाटा के लोहा-इस्पात कारखाने में भी एक हड़ताल हुई। इस हड़ताल के समाधान में सुभाष चंद्र बोस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस काल की सबसे प्रमुख हड़ताल बंबई की कपड़ा मिलों में हुई, जहाँ लगभग डेढ़ लाख मजदूर पाँच महीनों से अधिक समय तक हड़ताल पर रहे। यह हड़ताल कम्युनिस्टों के नेतृत्व में हुई। 1928 में हुई हड़तालों में पाँच लाख से अधिक मजदूरों में भाग लिया। इस नई लहर का एक और संकेत क्रांतिकारी आतंकवाद के आंदोलन की गतिविधियों में देखने को मिला। अब यह आंदोलन भी साम्राज्यवाद की ओर झुक रहा था। प्रथम असहयोग आंदोलन की असफलता के कारण रूका हुआ आतंकवाद आंदोलन फिर से उठ खड़ा हुआ था। एक अखिल भारतीय सम्मेलन के बाद अक्टूबर 1924 में सशस्त्र क्रांति के लिए संगठन के उद्देश्य से हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की स्थापना हुई। सरकार ने इस पर एक कड़ा प्रहार किया। आतंकवादी युवकों को बड़ी संख्या में गिरफ्तार करके उन पर काकोरी षड़यंत्र केस (1925) नामक मुकदमा चलाया गया। सत्रह लोगों को लंबी-लंबी जेल की सजाएँ हुईं, चार को आजीवन कारवास का दंड मिला, तथा रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह समेत चार लोगों को फाँसी दे दी गई। आतंकवादी जल्द ही समाजवादी विचारों के प्रभाव में आ गए और 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में उन्होंने अपने संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ (हिसप्रस) कर दिया। वे अब धीरे-धीरे व्यक्तिगत वीरता के कामों और आतंकवाद से भी दूर हटने लगे। लेकिन 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन विरोधी एक प्रदर्शन पर पुलिस के बर्बर लाठी चार्ज के कारण एक आकस्मिक परिंवर्तन आया। इसमें लाठियों की चोट खाकर पंजाब के महान नेता लाला लाजपतराय शहीद हो गए। युवक इससे कुद्ध हो उठे और 17 दिसंबर 1928 को भगतसिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरू ने लाठी चार्ज का नेतृत्व करने वाले ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सांडर्स को गोलियों से भून दिया। हिसप्रस के नेताओं ने यह भी निर्णय किया कि अपने बदले हुए राजनीतिक उद्देश्यों तथा जन-क्रांति की आवश्यकता के बारे में जनता को बतलाएँ। परिणामस्वरूप 8 अप्रैल 1929 को भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय धारा-सभा में एक बम फेंका। बम से किसी को नुकसान नहीं पहुँचा, उसे जान-बूझकर ऐसा बनाया गया था कि किसी को चोट न आए। इस काम का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, बल्कि आतंकवादियों के एक पर्चे के अनुसार “बहरों को सुनाना” था। भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त चाहते तो बम फेंकने के बाद आसानी से भाग निकलते, मगर उन्होंने जान-बूझकर अपने को गिरफ्तार कराया वे क्रांतिकारी प्रचार के लिए अदालत का एक मंच के रूप में उपयोग करना चाहते थे। बंगाल में भी क्रांतिकारी आतंकवाद की गतिविधियाँ एक बार फिर उभरीं। अप्रैल 1930 में चटगाँव के सरकारी शस्त्रागार पर क्रांतिकारियों ने योजनाबद्ध ढंग से एक बड़ा छापा मारा। इसका नेतृत्व मास्टर सूर्यसेन कर रहे थे। अलोकप्रिय सरकारी अधिकरियों पर हुए हमलों में यह पहला हमला था। बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन की एक उल्लेखनीय विशेषता उसमें युवतियों की भागीदारी थी। चटगाँव के क्रांतिकारी आंदोलन के विकास के सूचक थे। उनका काम व्यक्तिगत नहीं सामूहिक था और उसका उद्देश्य औपनिवेशिक शासन के अंगों पर प्रहार करना था। सरकार ने क्रांतिकारी आतंकवादियों पर एक तीखा प्रहार किया। उनमें से अनेकों गिरफ्तार कर लिए गए और उन पर अनेकों प्रसिद्ध मुकदमे चलाए गए। भगतसिंह तथा कुछ और लोगों पर सांडर्स की हत्या का मुकद्दमा भी चला। इन युवक क्रांतिकारियों ने अदालतों में दिए गए अपने बयानों से तथा अपने निर्भीक और अवज्ञापूर्ण, व्यवहार से जनता का दिल जीत लिया। उनके बचाव के लिए कांग्रेसी नेता आगे आए जो वैसे अहिंसा के समर्थक थे। जेलों की अमानवीय परिस्थितियों के विरोध में उनकी भूख हड़तालें खास तौर पर प्रेरणाप्रद थीं। राजनीतिक बंदियों के रूप में उन्होंने जेलों में अपने साथ सम्मानित तथा सुसंस्कृत व्यवहार किये जाने की माँग की। ऐसी ही एक भूख हड़ताल में 63 दिनों की एतिहासिक भूख-हड़ताल के बाद एक दुबले-पतले युवक क्रांतिकारी जतीनदास शहीद हुए। जनता के देशव्यापी विरोध के बावजूद भगतसिंह सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फाँसी दे दी गई। फाँसी से कुछ दिन पहले जेल सुपरिटेंडेंट को लिखे गए एक पत्र में इन तीन क्रांतिकारियों ने कहा था - “बहुत जल्द ही अंतिम संघर्ष की दुंदुभि बजेगी। इसका परिणाम निर्णायक होगा। हमने इस संघर्ष में भाग लिया है और हमें इस पर गर्व है।” अपने दो अंतिम पत्रों में 23 वर्षीय भगतसिंह ने समाजवाद में अपनी आस्था भी व्यक्त की। वे लिखते हैं : “किसानों को केवल विदेशी शासन ही नहीं बल्कि जमींदारों और पूँजीपतियों के जुए से भी स्वयं को मुक्त कराना होगा।” 3 मार्च 1931 को भेजे गए अपने अंतिम संदेश में उन्होंने घोषणा की कि भारत में संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि “मुट्ठी भर शोषक अपने स्वार्थों के लिए साधारण जनता की मेहनत का शोषण करते रहेंगे। इससे कोई बहस नहीं है कि ये शोषक शुद्ध रूप से ब्रिटिश पूँजीपति हैं, ब्रिटिश और भारतीय मिलकर शोषण करते हैं, या ये शुद्ध रूप से भारतीय हैं।” भगतसिंह ने समाजवाद की एक वैज्ञानिक परिभाषा की कि इसका अर्थ पूँजीवाद तथा वर्गीय शासन का अंत। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 1930 के बहुत पहले ही उन्होंने तथा उनके साथियों ने आतंकवाद का त्याग कर दिया था। 2 फरवरी 1931 को लिखे गए अपने राजनीतिक वसीयतनामें में उन्होंने घोषणा की - “देखने में मैंने एक आतंकवादी की तरह कार्य किया है। लेकिन मैं आतंकवादी नहीं हूँ.......... मैं अपनी पूरी शक्ति से यह घोषणा करना चाहूँगा कि मैं आतंकवादी नहीं हूँ और शायद अपने क्रांतिकारी जीवन के आरंभिक दिनों को छोड़कर मैं कभी आतंकवादी नहीं था। और मुझे पूरा विश्वास है कि इन विधियों से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते।” भगतसिंह पूरी तरह और चेतन रूप से धर्मनिरपेक्ष भी थे। वे अकसर अपने साथियों से कहते थे कि सांप्रदायिकता भी उतना ही बड़ा शत्रु है जितना कि उपनिवेशवाद और इसका सख्ती से मुकाबला करना होगा। 1926 में उन्होंने पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना में भाग लिया था और इसके प्रथम सचिव बने थे। भगतसिंह ने सभा के जो नियम तैयार किए थे उनमें दो नियम इस प्रकार थे - “सांप्रदायिक विचार फैलाने वाले सांप्रदायिक संगठनों या अन्य पार्टियों से कोई संबंध न रखना” और “लोगों को यह समझाना कि धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है तथा इस प्रकार उनमें सामान्य सहिष्णुता की भावना जगाना तथा इसी विचार के अनुसार कार्य करना।” क्रांतिकारी आतंकवाद का आंदोलन बहुत जल्द समाप्त हो गया, हालाँकि इक्की-दुक्की घटनाएँ अनेक वर्षों तक जारी रहीं। चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के एक पार्क में पुलिस से मुकाबला करते हुए मारे गए। बाद में इस पार्क का नाम आजाद पार्क रखा गया। सूर्यसेन फरवरी 1933 में गिरफ्तार कर लिए गए और कुछ समय बाद उन्हें फाँसी दे दी गईं। सैंकड़ों दूसरे क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें लंबी-लंबी सजाएँ दीं गईं। इनमें से अनेकों को अंडमान के सेलुलर जेल में भेज दिया गया। इस तरह तीसरे दशक के अंत तक एक नई राजनीतिक परिस्थिति उभरने लगी थी। वायसराय लार्ड इर्विन ने बाद में इन वर्षों के बारे में लिखा, “कोई ऐसी नई शक्ति अब कार्यरत थी जिसके महत्व को अभी तक उन लोगों ने भी पूरी तरह नहीं समझा है जिनका भारत संबंधी ज्ञान बीस-बीस या तीस-तीस साल पुराना है।”। सरकार इस नई प्रवृत्ति को कुचलने पर आमादा थी। जैसा कि हमने देखा, आतंकवादियों को निर्ममता के साथ कुचल दिया गया। उभरते मजदूर और कम्युनिस्ट आंदोलनों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव किया किया गया। मार्च 1929 में 31 प्रमुख मजदूर और कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, इनमें तीन अंग्रेज भी थे। फिर भी इन पर चार वर्षों तक मुकद्दमा चलाया गया, जिसे मेरठ षड़यंत्र का मुकद्दमा कहा जाता है और मुकद्दमें की समाप्ति पर इनको लंबी-लंबी जेल-सजाएँ दी गईं। साइमन कमीशन का बहिष्कारआंदोलन के इस नए चरण को बल तब मिला, जब नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन का गठन किया, जिसे आम तौर पर साइमन कमीशन कहा जाता है जो इसके अध्यक्ष थे। इसका उद्देश्य आगे सांविधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था। “इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। सभी वर्गों के भारतीयों ने इस घोषणा का विरोध किया। इस बात पर उन्हें सबसे अधिक क्रोध था कि कमीशन में एक भी भारतीय को नहीं रखा गया था और इसके पीछे यह धारणा काम कर रही थी कि स्वशासन के लिए भारतीयों की योग्यता-अयोग्यता का फैसला विदेशी करेंगे। दूसरे शब्दों में, सरकार के इस काम को आत्म-निर्णय के सिद्धांत का उल्लंघन समझा गया तथा ऐसा माना गया कि भारतीयों के आत्मसम्मान को जान-बूझ कर चोट पहुँचाई गई है। 1927 के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन कि अध्यक्षता डॉ. अंसारी साहब कर रहे थे, उसमें राष्ट्रीय कांग्रेस ने “हर कदम पर और हर रूप में “इस कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किया। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने भी कांग्रेस के फैसले का समर्थन किया। वास्तव में अस्थायी तौर पर ही सही, साइमन कमीशन ने देश के सभी वर्गों और दलों को एक बार फिर एकताबद्ध कर दिया। राष्ट्रवादियों के साथ एकजुटता जतलाने के लिए मुस्लिम लीग ने मिले-जुले चुनाव मंडलों के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया, इस शर्त के साथ कि मुसलमानों के लिए कुछ सीटें आरक्षित रखी जाएँ।सभी महत्वपूर्ण भारतीय नेताओं और दलों ने परस्पर एकजुट होकर तथा सांविधानिक सुधारों की एक वैकल्पिक योजना बनाकर साइमन कमीशन की चुनौती का जवाब देने का प्रयास किया। प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ताओं के दर्जनों सम्मेलन और साझी बैठकें आयोजित की गईं। इसका परिणाम नेहरू रिपोर्ट के रूप में सामने आया जिसके प्रमुख निर्माता मोतीलाल नेहरू थे। इसे अगस्त में अंतिम रूप दिया गया। दुर्भाग्य से कलकत्ता में दिसंबर 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन रिपोर्ट को स्वीकार न कर सका। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और सिख लीग के कुछ सांप्रदायिक रूझान वाले नेताओं ने इसे लेकर आपत्तियाँ कीं। इस तरह सांप्रदायिक दलों ने राष्ट्रीय एकता का दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद निरंतर सांप्रदायिकता का विकास हुआ। यह भी ध्यान रहे कि राष्ट्रवादियों की राजनीति और सांप्रदायवादियों की राजनीति में एक बुनियादी खाई मौजूद थी। राष्ट्रवादी देश के लिए राजनीतिक अधिकार तथा स्वाधीनता पाने के लिए विदेशी सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक संघर्ष चला रहे थे। हिंदू या मुस्लिम सांप्रदायवादियों के साथ बात नहीं थी। उनकी माँगें राष्ट्रवादियों को ही संबोधित थीं, दूसरी ओर वे समर्थन और सहायता के लिए आम तौर पर विदेशी सरकार का ही मुँह ताकते थे। ऐसा अक्सर देखा गया कि वे काग्रेस से लड़ते थे किंतु अंग्रेजी सरकार से सहयोग करते रहते थे। सर्वदलीय सम्मेलन का कार्यवाही से कहीं बहुत अधिक महत्वपूर्ण साइमन कमीशन के विरोध में जनता का उभार था। कमीशन के भारत पहुँचने पर एक शक्तिशाली राष्ट्रव्यापी विरोध आंदोलन उठ खड़ा हुआ और राष्ट्रवादी उत्साह तथा एकता नई ऊँचाइओं तक पहुँची। 3 फरवरी को कमीशन के बंबई पहुँचने पर एक अखिल भारतीय हड़ताल की गई। कमीशन जहाँ-जहाँ भी गया, वहीं हड़तालें और काले झंडे दिखाकर तथा “साइमन, वापस जाओ” के नारे के साथ उसका स्वागत किया गया। इस अवसर पर जनता के विरोध को कुचलने के लिए सरकार ने निर्मम दमन तथा पुलिस-कार्यवाहियों का सहारा लिया। साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन तात्कालिक रूप में एक व्यापक राजनीतिक संघर्ष को जन्म न दे सका। कारण की राष्ट्रीय आंदोलन के अघोषित मगर सर्वमान्य नेता, अर्थात् गाँधीजी को विश्वास न था कि संघर्ष का समय आ गया है। पर जनता के उत्साह को अधिक समय तक बांधकर नहीं रखा जा सका। अब एक बार फिर देश संघर्ष के लिए कमर कस चुका था। पूर्ण स्वराजजनता की इस नई भावना को जल्द ही राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना लिया। गाँधीजी सक्रिय राजनीति में वापस लौट आए और दिसंबर 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता सम्मेलन में शामिल हुए। कांग्रेस का पहला काम जुझारू वामपंथ से मेल-मिलाप करना था। 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इस घटना का एक रोमानी पहलू भी था। मातीलाल नेहरू 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे और राष्ट्रीय आंदोलन के आधिकारिक प्रमुख के रूप में उनका स्थान अब उनके पुत्र ने ले लिया था। इस तरह आधुनिक इतिहास में विशिष्ट परिवार की विजय हुई।कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में इस नई, जुझारू भावना को आवाज मिली। इस अधिवेशन में पारित एक प्रस्ताव ने पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया। 31 दिसंबर 1929 को स्वाधीनता का नया-नया स्वीकृत तिरंगा झंडा लहराया गया। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया। उसके बाद यह दिवस हर साल मनाया जाने लगा, जब लोग यह शपथ लेते थे कि ब्रिटिश शासन की “अधीनता अब और आगे स्वीकार करना मानवता और ईश्वर के प्रति अपराध” होगा। इस अधिवेशन ने एक नागरिक अवज्ञा आंदोलन भी छेड़ने की घोषणा की। लेकिन इसने संघर्ष का कोई कार्यक्रम नहीं तैयार किया। यह काम महात्मा गाँधी पर छोड़ दिया गया और पूरे कांग्रेस संगठन को उनकी आज्ञा के अधीन कर दिया गया। गाँधीजी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन एक बार फिर सरकार के मुकाबले खड़ा हुआ। देश अब एक बार फिर आशा, उल्लास और मुक्त होने की दृढ़ भावना से भर उठा। नागरिक अवज्ञा आंदोलनदूसरा नागरिक अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को गाँधीजी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ आरंभ हुआ। इस दिन 78 चुने हुए अनुयायियों को साथ लेकर गाँधीजी साबरमती आश्रम से चले और लगभग 200 किलोमीटर दूर, गुजरात के समुद्र-तट पर स्थित दांडी गाँव पहुँचे। उनकी यात्रा, उनके भाषणों तथा जनता पर उनके प्रभाव की रिपोर्टें प्रतिदिन समाचारपत्रों में छपती रहीं। रास्ते में पड़ने वाले गाँवों के सैकड़ों अधिकारियों ने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिए। गाँधीजी 6 अप्रैल को दांडी पहुँचे, समुद्र-तट से मुट्ठी भर नमक उठाया और इस प्रकार नमक-कानून को तोड़ा। यह इस बात का प्रतीक था कि भारतीय जनता अब ब्रिटिश कानूनों और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जीने के लिए तैयार नहीं है। गाँधीजी ने घोषणा की -भारत में ब्रिटिश शासन ने इस देश को नैतिक, भौतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विनाश के कगार तक पहुँचा दिया है। मैं इस शासन को एक अभिशाप मानता हूँ। मैं इस शासन-प्रणाली को नष्ट करने पर आमादा हूँ.............. अब राजद्रोह मेरा धर्म बन चुका है। हमारा संघर्ष एक अहिंसक युद्ध है। हम किसी की हत्या नहीं करेंगे, मगर इस शासन रूपी अभिशाप को नष्ट होते देखना हमारा धर्म है। आंदोलन अब तेजी से फैल चला। पूरे देश में नमक-कानून तोड़े गए। फिर उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य भारत में जंगल-कानून तोड़े गए और पूर्वी भारत में ग्रामीण जनता ने चौकीदारी कर अदा करने से इनकार कर दिया। देश में हर जगह जनता हड़तालों, प्रदर्शनों और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में भाग लेने लगी और कर अदा करने से इनकार करने लगी। लाखों भारतीयों ने सत्याग्रह किया। देश के अनेक भागों में किसानों ने जमीन की मालगुजारी और लगान देने से इनकार कर दिया। उनकी जमीनें जब्त कर लीं गईं। इस आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता स्त्रियों की भागीदारी थी। हजारों स्त्रियाँ घरों के अंदर से बाहर निकलीं और सत्याग्रह में भाग लिया। विदेशी वस्त्र या शराब बेचने वाली दुकानों पर धरना देने में उनकी सक्रिय भूमिका रही। जुलूसों में वे पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलीं। आंदोलन बढ़कर भारत के एकदम उत्तर-पश्चिमी छोर तक भी पहुँचा और बहादुर और शेरदिल पठानों में ऐसा जोश सा भर गया। “सीमांत गाँधी” के नाम से जाने जाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में पठानों ने खुदाई खिदमतगार (ईश्वर के सेवक) नामक संगठन बना लिया, जो जनता के बीच “लाल कुर्ती वाले” कहलाते थे। ये लोग अहिंसा और स्वाधीनता संघर्ष को समर्पित थे। इस समय पेशावर में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। गढ़वाली सिपाहियों के दो प्लाटूनों ने अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया इसके नेता चंद्र सिंह गढ़वाली थे। इसके बदले में उनका कोर्ट मार्शल किया गया और लंबी-लंबी जेल-सजाएँ दी गईं। इस घटना से स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रवाद की भावना भारतीय सेना तक में फैलने लगी थी जो ब्रिटिश शासन का प्रमुख आधार थी। इसी तरह आंदोलन की गूँज देश के एकदम पूर्वी कोनों में सुनाई पड़ी। इसमें मणिपुरी जनता की बहादुरी से भरपूर भागीदारी रही। नागालैंड ने रानी गिडालू जैसी वीरांगना को जन्म दिया। इस वीर बाला ने मात्र 13 वर्ष की आयु में कांग्रेस और गाँधीजी के आह्वान पर विदेशी शासन के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठा लिया। 1932 में यह युवा रानी पकड़ी गई और उसे आजीवन कारावास की सजा मिली। रानी की पूरी जवानी असम के विभिन्न जेलों की अंधेरी कोठरियों में गुजर गई और उसे मुक्ति केवल 1947 में स्वतंत्र भारत की सरकार द्वारा मिली। उसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में लिखा था - ‘‘एक दिन वह आएगा जब भारत उसे याद करेगा और उसका सम्मान करेगा।’’ सरकार ने इस राष्ट्रीय संघर्ष के साथ पहले जैसा ही व्यवहार किया। निर्मम दमन, निहत्थे स्त्री-पुरूषों पर लाठी और गोली की बौछार, आदि के द्वारा इसे कुचलने के प्रयास किए गए। गाँधीजी तथा दूसरे कांग्रेसी नेताओं समेत 30,000 से अधिक सत्याग्रही गिरफ्तार किए गए। कांग्रेस को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पुलिस की गोलीबारी में 110 से अधिक लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। गैरसरकारी आंकड़ों के अनुसार मृतकों की संख्या इससे कहीं बहुत अधिक थी। फिर लाठी चार्ज में हजारों लोगों के सर फूटे और हड्डियाँ टूटीं। खासकर दक्षिण भारत में भयानक किस्म का दमन देखने को मिला। पुलिस अकसर लोगों को खादी या गाँधी टोपी पहने देखकर भी पीट देती थी। अंततः जनता ने आंध्र में एलौरा नामक स्थान पर प्रतिरोध किया और वहाँ पुलिस की गोलियों से अनेकों लोग मारे गए। इसी बीच 1930 में ब्रिटिश सरकार ने लंदन में भारतीय नेताओं और सरकारी प्रवक्ताओं का पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। इसका उद्देश्य साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना था। लेकिन कांग्रेस ने सम्मेलन का बहिष्कार किया और उसकी कार्यवाहियाँ बेकार गईं। भारत के बारे में कांग्रेस के बिना सम्मेलन यूँ ही था जैसे राम के बिना कोई रामलीला। अब सरकार ने कांग्रेस से किसी सहमति पर पहुँचने के लिए बातचीत शुरु की ताकि कांग्रेस इस सम्मेलन में भाग ले। अंत मे लार्ड इर्विन और गाँधीजी के बीच मार्च 1931 में एक समझौता हुआ। सरकार अहिंसक रहने वाले राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर तैयार हो गई। उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार तथा विदेशी वस्त्रों तथा शराब की दुकानों पर धरना देने का अधिकार भी मान लिए गए। तब कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन रोक दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन मे भाग लेने पर तैयार हो गई। अनेक कांग्रेसी नेता और खासकर युवक वामपंथी गाँधी-इर्विन समझौते के विरोधी थे, क्योंकि सरकार ने एक भी प्रमुख राष्ट्रवादी माँग नहीं मानी थी। सरकार ने यह माँग तक नहीं मानी थी कि भगतसिंह तथा उनके दो साथियों की फाँसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। लेकिन गाँधीजी को विश्वास था कि लार्ड इर्विन और ब्रिटिश भारतीय माँगों पर बातचीत के बारे मे गंभीर थे। सत्याग्रह की उनकी धारणा में यह भी शामिल था कि प्रतिपक्षी को हृदय-परिवर्तन का प्रदर्शन करने का अवसर दिया जाए। उनकी रणनीति इस समझ पर आधारित थी कि कोई भी जन-आंदोलन निश्चित ही बहुत संक्षिप्त होगा और बहुत दिनों तक जारी न रह सकेगा क्योंकि जनता की बलिदान की क्षमता अनंत नहीं होती। परिणामस्वरूप कानून विरोधी जनसंघर्ष के बाद एक निष्क्रिय चरण का आरंभ हुआ जिसमें आंदोलन को कानून की सीमाओं में रहकर ही चलाया जाना था। इसके अलावा गाँधीजी ने बराबरी के आधार पर बातचीत की थी और इस प्रकार कांग्रेस की प्रतिष्ठा को सरकार की प्रतिष्ठा के बराबर ला दिया था। इसलिए वे कांग्रेस के करांची अधिवेशन में इस समझौते का अनुमोदन कराने में सफल रहे। इस बीच देश के अनेक भागों मे किसानों में असंतोष की लहर फैल चुकी थी। विश्वव्यापी मंदी के कारण खेतिहर पैदावारों के दाम गिर गए थे और लगान और मालगुजारी का बोझ उनके लिए असह्य हो चला था। संयुक्त प्रांत में लगान में कमी और बँटाईदारी की बेदखली के खिलाफ कांग्रेस ने आंदोलन चलाया। दिसंबर 1930 में कांग्रेस ने “न लगान, न टैक्स” का अभियान चलाया। उत्तर में सरकार ने 26 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरु को गिरफ्तार कर लिया। पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत में सरकार की मालगुजारी संबंधी नीति के खिलाफ खुदाई खिदमतगार किसान आंदोलन चला रहे थे। 24 दिसंबर को उनके नेता खान अब्दुल गफ्फार खान भी धर लिए गए। किसान आंदोलन बिहार, अंध्र, मध्य प्रांत, बंगाल और पंजाब में भी फैल रहे थे। भारत वापस आने पर गाँधीजी के सामने नागरिक अवज्ञा आंदोलन को दोबारा आरंभ करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। अब सरकार के प्रमुख नए वायसराय लार्ड वेलिंगडन थे जिनका मत था कि कांग्रेस के साथ समझौता करना बहुत बड़ी गलती थी। उनकी सरकार कांग्रेस को कुचलने के लिए आमादा और तैयार थी। वास्तव में भारतीय नौकरशाही नरम तो कभी पड़ी ही नहीं थी। गाँधी-इर्विन समझौते पर हस्ताक्षर के फौरन बाद आंध्र को पूर्वी गोदावरी जिले में एक भीड़ पर गोली चली थी और चार लोग मारे गए थे - सिर्फ इसलिए कि उन्होंने गाँधीजी का एक चित्र लगाया था। 4 जनवरी 1932 को गाँधीजी तथा दूसरे कांग्रेसी नेता फिर धर लिए गए और कांग्रेस गैरकानूनी घोषित कर दी गई। सामान्य कानून निलंबित कर दिए गए और प्रशासन विशेष अध्यादेशों के सहारे चलने लगा। पुलिस ने आंतक का नंगा खेल खेला और स्वाधीनता-सेनानियों पर अनगिनत अत्याचार किए गए। एक लाख से ऊपर सत्याग्रही गिरफ्तार किए गए और हजारों की जमीनों, मकानों और दूसरी जायदादों को जब्त किया गया। राष्ट्रवादी साहित्य प्रतिबंधित कर दिया गया। राष्ट्रवादी समाचारपत्रों पर दोबारा सेंसरशिप लागू कर दिया गया। अंत में सरकारी दमन सफल रहा क्योंकि सांप्रदायिक और दूसरे प्रश्नों पर भारतीय नेताओं के बीच मतभेद होने से सहायता मिली। नागरिक अवज्ञा आंदोलन धीरे-धीरे बिखर गया। कांग्रेस ने आधिकारिक रूप में मई 1933 में इसे निलंबित कर दिया और मई 1934 में इसे वापस ले लिया। गाँधीजी एक बार फिर सक्रिय राजनीति से अलग हो गए। राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच एक बार फिर निराशा फैल गई। बहुत पहले, 1933 में ही सुभाष चंद्र बोस और विट्ठलभाई पटेल ने घोषणा कर दी थी कि ‘‘एक राजनीतिक नेता के रूप में महात्माजी असफल रहे हैं।’’ वायसराय वेलिंगडन ने भी कहा कि “कांग्रेस 1930 की तुलना में निश्चित ही कम अच्छी स्थिति में है और जनता पर उसका प्रभाव घटा है।” मगर वास्तव में ऐसा न था। यह सही है कि स्वाधीनता लाने में आंदोलन असफल रहा था, लेकिन जनता का और राजनीतिकरण करने और स्वाधीनता संघर्ष के सामाजिक आधारों को और मजबूत बनाने में वह सफल रहा था। जैसा कि एक ब्रिटिश पत्रकार एच. एन. ब्रेल्सफोर्ड ने लिखा है, हाल के संघर्ष के फलस्वरूप भारतीयों ने “अपने मन को मुक्त कर लिया है और अपने दिलों में स्वाधीनता प्राप्त कर ली है।” नागरिक अवज्ञा आंदोलन के वास्तविक परिणाम और वास्तविक प्रभाव का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि राजनीतिक बंदी जब 1934 में रिहा हुए तो जनता ने उनका वीरों के रूप में स्वागत किया। राष्ट्रवादी राजनीति, 1935-39
1935 का भारत सरकार कानूननवंबर 1932 में जब कांग्रेस संघर्ष के मंझधार में थी तब लंदन में एक बार फिर कांग्रेस के बिना तीसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें हुए विचार-विमर्ष का परिणाम अंततः 1935 के भारत सरकार कानून के रूप में सामने आया। इस कानून में एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता के आधार पर एक नई शासनप्रणाली की व्यवस्था थी। यह संघ (फेडरेशन) ब्रिटिश भारत के प्रांतों तथा रजवाड़ों पर आधारित था। केंद्र में दो सदनों वाली एक संघीय विधायिका की व्यवस्था थी जिसमें रजवाड़ों को भिन्न-भिन्न प्रतिनिधित्व दिया गया था। मगर रजवाड़ों के प्रतिनिधियों का चुनाव जनता द्वारा नहीं किया जाता बल्कि उन्हें वहाँ के शासक मनोनीत करते। ब्रिटिश भारत की केवल 14 प्रतिशत जनता को मताधिकार प्राप्त था। इस विधायिका में राष्ट्र वादी तत्वों को काबू में रखने के लिए राजा-महाराजाओं का उपयोग किया गया था, मगर फिर भी इसे कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी गई थी। रक्षा तथा विदेश विभाग इसके अधिकार-क्षेत्र से बाहर थे। जबकि दूसरे विषयों पर गवर्नर-जनरल का विशेष नियंत्रण था। गवर्नर-जनरल और गवर्नरों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार करती और वे उसी के प्रति उत्तरदायी थे। प्रांतों को अधिक स्थानीय अधिकार दिए गए थे। प्रांतीय विधान सभाओं के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों का प्रांतीय प्रशासन के हर विभाग पर नियंत्रण था। उन्हें कानूनी गतिविधियों पर निशेधाधिकार तथा अपने कानून बनाने के अधिकार थे। इसके अलावा नागरिक प्रशासन और पुलिस पर उनका पूरा नियंत्रण था। यह कानून राष्ट्रवादियों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका, क्योंकि आर्थिक और राजनीतिक शक्ति अभी भी ब्रिटिश सरकार के हाथों में केंद्रित थी। विदेशी शासन पहले की तरह ही जारी था, हाँ कुछेक लोकप्रिय और चुने हुए नेता भारत के ब्रिटिश प्रशासन के ढाँचे में और जुड़े। कांग्रेस ने “पूरी तरह निराशाजनक” कहकर इस कानून की निंदा की।इस कानून के संघीय पक्ष को कभी लागू नहीं किया गया, पर प्रांतीय पक्ष जल्द ही लागू कर दिया गया। इस 1935 के नए कानून का कड़ा विरोध करने के बावजूद कांग्रेस ने इसके अंतर्गत होने वाले चुनावों में भाग लेने का निर्णय किया और इस घोषित लक्ष्य के साथ कि वह इस कानून की अलोकप्रियता सिद्ध करेगी। कांग्रेस के तूफानी चुनाव-प्रचार को जनता का व्यापक समर्थन मिला, हालाँकि गाँधीजी ने एक भी चुनाव-सभा को संबोधित नहीं किया। फरवरी 1937 में हुए इन चुनावों में यह बात निश्चित रूप से सिद्ध हो गई कि जनता का एक बड़ा भाग कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस ने अधिकांश प्रांतों भारी जीत हासिल की। ग्यारह में से सात प्रांतों में जुलाई 1937 में कांग्रेसी मंत्रीमंडल बने। बाद में कांग्रेस ने दो प्रांतों में साझी सरकारें भी बनाईं। केवल बंगाल और पंजाब प्रांत में ही गैरकांग्रेसी मंत्रीमंडल बन सके। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी ने और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई। कांग्रेसी मंत्रिमंडलस्पष्ट है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल भारत में ब्रिटिश प्रशासन के बुनियादी साम्राज्यवादी चरित्र को बदलने और एक नया युग आरंभ करने में असफल रहे। फिर भी 1935 के कानून के अंतर्गत उन्हें जो सीमित अधिकार प्राप्त थे उनके सहारे उन्होंने जनता की दशा सुधारने के सचमुच प्रयास किए। कांग्रेसी मंत्रियों ने अपना वेतन खुद घटाकर 500 रुपये प्रति माह कर दिया। उनमें से अधिकांश रेलों में दूसरे या तीसरे दर्जे में चलते। ईमानदारी और जनसेवा के नए मानदंड उन्होंने स्थापित किए। अनेक क्षेत्रों में उन्होंने सकारात्मक निर्णय लिए। उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया, प्रैस और अतिवादी संगठनों पर लगे प्रतिबंध हटाए, मजदूर संघों और किसान सभाओं को उन्होंने काम करने और बढ़ने की छूट दी, पुलिस के अधिकार कम किए और क्रांतिकारी आतंकवादियों समेत राजनीतिक कैदियों को बड़ी संख्या में रिहा कर दिया। बँटाईदारों के अधिकारों और बँटाईदारों की सुरक्षा के लिए उन्होंने अनेक कृषि-कानून बनाए। मजदूर संघों ने पहले से अधिक मुक्त महसूस किया और मजदूरों की मजदूरी बढ़वाने में सफल रहे। कांग्रेसी सरकारों ने चुने हुए क्षेत्रों में नसबंदी लागू की, हरिजन-कल्याण के काम किए, तथा प्राथमिक, उच्च और तकनीकी शिक्षा तथा जन-स्वास्थ्य पर पहले से अधिक ध्यान दिया। खादी और दूसरे ग्रामीण उद्योगों को समर्थन दिया गया। आधुनिक उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिला। सांप्रदायिक दंगों से सख्ती से निपटना कांग्रेसी मंत्रिमंडल की एक प्रमुख उपलब्धि थी। सबसे बड़ा लाभ तो मानसिक लाभ था। लोगों को लगा कि वे विजय और स्वशासन की हवा में सांस ले रहे हैं। जो लोग अभी हाल तक जेलों में बंद थे, अब वे मंत्री के रूप में शासन कर रहे थे। क्या यह एक बड़ी उपलब्धि नहीं थी ?1935-39 के काल में कुछ में कुछ और महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएँ भी घटीं जिन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन और कांग्रेस को एक तरह से नया मोड़ दिया। सामाजवादी विचारों का प्रसारइस सदी के चौथे दशक में कांग्रेस के अंदर और बाहर समाजवादी विचारों का तेजी से प्रसार हुआ। 1929 में अमरीका में एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई जो धीरे-धीरे पूरी दुनिया में छा गई। दूसरे पूँजीवादी देशों में उत्पादन और विदेशी व्यापार में बहुत बड़ी गिरावट आई। इससे जनता की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैली। एक समय ऐसा हो गया था जब ब्रिटेन में 30 लाख, जर्मनी में 60 लाख और अमरीका में 120 लाख लोग बेरोजगार थे। दूसरी ओर सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति इसके ठीक विपरीत थी। वहाँ गिरावट तो नहीं आई बल्कि 1929 और 1936 के बीच पहली दो पंचवर्षीय योजनाएँ सफलतापूर्वक लागू की गई जिससे सोवियत औद्योगिक उत्पादन चार गुना से भी अधिक हो गया। इस तरह विश्वव्यापी मंदी के कारण पूँजीवादी प्रणाली बदनाम हो गई, और लोगों का ध्यान मार्क्सवाद, समाजवाद और आर्थिक योजना के विचार की ओर गया। परिणामस्वरूप अधिकाधिक लोग, खासकर युवक, मजदूर और किसान समाजवादी विचारों की ओर खिंचने लगे।राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभिक दिनों से ही उसका झुकाव निर्धन जनता की ओर था। 1917 की रूसी क्रांति के प्रभाव से, राजनीतिक मंच पर गाँधीजी के उदय से, तथा दूसरे और तीसरे दशकों में शक्तिशाली वामपंथी गुटों के बनने से यह प्रवृत्ति और मजबूत हुई। राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर और पूरे देश के पैमाने पर एक समाजवादी भारत की तस्वीर को लोकप्रिय बनाने में जवाहरलाल नेहरु ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस के अंदर वामपंथी प्रवृत्ति के मजबूत होने का प्रमाण यह था कि 1929, 1936 और 1937 में जवाहर लाल नेहरु तथा 1938 और 1939 में सुभाषचन्द्र बोस कांगेस अध्यक्ष पद के लिए विजयी हुए। नेहरु का तर्क था कि राजनीतिक स्वाधीनता का अर्थ जनता की आर्थिक शक्ति, खासकर मेहनती किसानों की सामंती शोषण से मुक्ति होनी चाहिए। 1936 में लखनऊ अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में नेहरु ने कांग्रेस से आग्रह किया कि वह समाजवाद को अपना लक्ष्य बनाए तथा खुद को किसान और मजदूर वर्गों के और भी पास लाए। उनका विश्वास था कि मुस्लिम जनता को उनके प्रतिक्रियावादी सांप्रदायिक नेताओं से दूर हटाने का यही सबसे अच्छा उपाय था। उन्होंने कहा - मेरा विश्वास है कि विश्व की समस्याओं और भारत की समस्याओं का एकमात्र समाधान समाजवाद है और जब मैं इस शब्द का उपयोग करता हूँ तो इसे अस्पष्ट मानवतावादी नहीं बल्कि वैज्ञानिक, आर्थिकअर्थ में करता हूँ..... इसका मतलब है हमारे राजनीतिक और सामाजिक ढाँचे में व्यापक तथा क्रांतिकारी परिवर्तन, कृषि और उद्योग के निहित स्वार्थों का उन्मूलन, तथा भारत के सामंती और निरंकुश रजवाड़ों की प्रणाली की समाप्ति। इसका अर्थ है कि एक संकुचित अर्थ को छोड़कर निजी संपत्ति का उन्मूलन तथा वर्तमान मुनाफा प्रणाली की जगह सहकारी सेवा के उच्चतर आदर्श की स्थापना। अंततः इसका अर्थ है हमारी सहज वृत्तियों, आदतों और इच्छाओं में परिवर्तन। संक्षेप में, इसका अर्थ है वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्था से मूलगामी अर्थ में भिन्न एक नई सभ्यता। देश में मूलगामी शक्तियों के प्रसार का प्रमाण जल्द ही कांग्रेस के कार्यक्रम तथा नीतियों में भी देखा गया। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रस्थान-बिंदू मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति पर वह प्रस्ताव था जिसे कांग्रेस ने करांची अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरु के आग्रह पर पारित किया। प्रस्ताव में घोषणा की गई कि “जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए राजनीतिक स्वाधीनता में लाखों-लाख भूखे लोगों की वास्तविक आर्थिक स्वाधीनता भी सम्मिलित होनी चाहिए। प्रस्ताव में जनता को मूल नागरिक अधिकारों, जाति-पंथ-लिंग के भेद के बिना कानून के आगे सबकी समानता, सार्वभौमिक बालिग मताधिकार के आधार पर चुनाव, तथा मुक्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की जमानत दी गई थीं। लगान व मालगुजारी में काफी कमी, लाभहीन जोतों के लिए लगान माफी, खेतिहरों के कर्जों में तथा सूदखोरों के नियंत्रण से राहत, जीवनयापन-योग्य मजदूरी समेत मजदूरों के लिए बेहतर दशाओं, महिला मजदूरों के लिए काम के सीमित घंटों और सुरक्षा, मजदूरों तथा किसानों के लिए संगठित होने और यूनियन बनाने के अधिकार, तथा प्रमुख उद्योगों, खदानों और यातायात के साधनों पर राज्य का स्वामित्व या नियंत्रण जैसे वादे भी इस प्रस्ताव में किए गए थे। कांग्रेस के अंदर मूलगामी प्रवृत्ति का एक और प्रमुख रूप कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन के प्रस्तावों व 1936 के चुनाव घोषणापत्र में देखने को मिला। इसमें कृषि-प्रणाली का मूलगामी रूपांतरण करने, लगान और मालगुजारी मे काफी कमी करने, ग्रामीण ऋण कम करने तथा आसान शर्तों पर ऋण देने के वादे किए गए थे इसके साथ ही सामंती वसूलियों को समाप्त करने, बँटाईदारों की बँटाईदारी की सुरक्षा देने, खेत मजदूरों को जीवनयापन-योग्य मजदूरी दिलाने, तथा मजदूर संघ और किसान सभाएँ बनाने तथा हड़ताल करने के अधिकार देने के भी वादे किए गए थे। 1945 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित करके जमींदारी उन्मूलन का भी अनुमोदन किया था। 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाषचंद्र बोस थे। इस समय कांग्रेस ने आर्थिक योजना का विचार अपनाया और जवाहरलाल नेहरु की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति बनाई। नेहरु, दूसरे वामपंथियों तथा गाँधी ने भी चंद लोगों के हाथों मे धन का केंद्रीकरण रोकने के लिए बड़े उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में रखने की बात की। वास्तव में, चौथे दशक की एक प्रमुख घटना यह थी कि गाँधीजी ने भी मूलगामी आर्थिक नीतियों को अधिकाधिक स्वीकार किया। 1933 में नेहरु से सहमत होकर उन्होंने कहा कि “निहित स्वार्थों में एक बड़े परिवर्तन के बिना जनता की स्थिति को कभी नहीं सुधारा जा सकता।” उन्होंने “जमीन जोतने वाले की” का सिद्धान्त भी मान लिया और 1942 में घोषणा की कि “जमीन उनकी है जो उस पर मेहनत करते हैं और किसी की नहीं।” कांग्रेस के बाहर समाजवादी प्रवृत्ति का एक परिणाम यह भी था कि 1935 के बाद पूरनचंद्र जोशी के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी का प्रसार हुआ और 1934 में आचार्य नरेंद्रदेव तथा जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। 1939 में गाँधीजी के विरोध के बावजूद सुभाषचंद्र बोस दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर गाँधीजी और उनके समर्थकों के विरोध के कारण बोस अप्रैल 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने को मजबूर हो गए। फिर उन्होंने और उनके अनेक वामपंथी समर्थकों ने फारवर्ड ब्लाक की स्थापना की। 1939 तक आते-आते कांग्रेस के अंदर मौजूद वामपंथ सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एक-तिहाई वोट जुटा सकने में समर्थ हो चुका था। इसके अलावा चौथे और पाँचवें दशक में समाजवाद भारत के अधिकांश राजनीतिक चेतना-प्राप्त युवकों का विश्वास अपना रूप ले चुका था। चौथे दशक में आल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन तथा अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की भी स्थापना हुई। किसान और मजदूर आंदोलनचौथे दशक में भारत के किसानों और मजदूरों में राष्ट्रव्यापी जागरण देखने को आया। 1920-20 तथा 1930-34 के दो राष्ट्रव्यापी आंदोलनों ने किसानों और मजदूरों का बड़े पैमाने पर राजनीतिकरण किया था। 1929 के बाद भारत तथा शेष विश्व पर जिस आर्थिक मंदी की मार पड़ी उसने भारतीय किसान-मजदूरों की दशा भी बिगाड़ दी थी। 1932 के अंत तक खेतिहर पैदावार की कीमतें 50 प्रतिशत से अधिक गिर चुकी थीं। अब पूरे देश में किसान भूमि सुधारों, मालगुजारी और लगान में कमी, तथा कर्ज से राहत की माँग करने लगे थे। कारखानों और बागानों के मजदूर अब काम की बेहतर परिस्थितियों तथा ट्रेड यूनियन अधिकार दिए जाने की बढ़-चढ़ कर माँग कर रहे थे।नागरिक अवज्ञा आंदोलन तथा वामपंथी पार्टियों और गुटों ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं की एक ऐसी नई पीढ़ी पैदा की जो किसानों और मजदूरों के संगठन के लिए समर्पित थी। परिणामस्वरूप शहरों में ट्रेड यूनियनों का तथा पूरे देश में, खासकर संयुक्त प्रांत, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और पंजाब में किसान सभाओं का तेजी से प्रसार हुआ। 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में पहला अखिल भारतीय किसान संगठन अखिल भारतीय किसान सभा के नाम से बना। कांग्रेस और विश्व की घटनाएँ1935-39 के काल की तीसरी प्रमुख बात थी कि कांग्रेस विश्व की घटनाओं में बढ़-चढ़कर दिलचस्पी लेने लगी थी। 1885 में अपनी स्थापना के समय से ही कांग्रेस ने कहा था कि अमरीका और एशिया में ब्रिटेन के हितों की रक्षा करने के लिए भारतीय सेना और भारत के संसाधानों का प्रयोग न किया जाए। धीरे-धीरे इसने साम्राज्यवाद प्रसार के विरोध पर आधारित एक विदेश नीति विकसित कर ली थी। फरवरी 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरु ने ब्रुसेल्स में आयोजित उत्पीड़ित जातीयताओं के सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन का आयोजन आर्थिक या राजनीतिक साम्राज्यवाद से पीड़ित एशियाई, अफ्रीकी और लातीनी अमरीकी देशों के निर्वासित राजनीतिक कार्यकर्ताओं और क्रांतिकारियों ने किया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य इन सबके साझे साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष में तालमेल बिठाना और उन्हें योजनाबद्ध रूप देना था। यूरोप के अनेक वामपंथी बुद्धिजीवियों और राजनीतिक नेताओं ने भी सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए नेहरु ने कहा-हम समझते हैं कि विभिन्न पराधीन, अर्धपराधीन और उत्पीड़ित जनगण आज जो संघर्ष चला रहे हैं उसमें बहुत कुछ साँझा है। उनके दुश्मन भी प्रायः एक ही होते हैं, हालाँकि वे कभी-कभी विभिन्न रूपों में सामने आते हैं और उनके उत्पीड़न के लिए प्रयोग किए जाने वाले साधन भी अकसर मिलते-जुलते होते हैं। नेहरू इसी सम्मेलन में स्थापित “लीग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म” की एक्जीक्यूटिव कौंसिल” के भी सदस्य चुने गए। 1927 में राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में सरकार को चेतावनी दी गई कि ब्रिटेन अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अगर कोई युद्ध छेड़ेगा तो भारत की जनता उसका समर्थन नहीं करेगी। चौथे दशक में कांग्रेस ने दुनिया के किसी भी भाग में जारी साम्राज्यवाद के खिलाफ एक कड़ा रूख अपनाया और एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रीय आंदोलनों को समर्थन दिया। इसने उस समय इटली, जर्मनी और जापान में उभरते हुए फासीवाद की निंदा की जो साम्राज्यवाद और नस्लवाद का सबसे भयानक रूप था, और इथियोपिया, स्पेन, चेकोस्लोवाकिया तथा चीन पर फासीवादी ताकतों के हमले के खिलाफ संघर्ष में वहाँ की जनता का पूरा-पूरा समर्थन किया। 1937 में जब जापान ने चीन पर हमला किया तो कांग्रेस ने एक प्रस्ताव के द्वारा भारतीय जनता से आग्रह किया कि वे “चीन की जनता के प्रति अपनी सहानुभूति जताने के लिए जापानी वस्तुओं के प्रयोग से बचें।” 1938 में कांग्रेस ने डॉ. एम. अटल के नेतृत्व में डाक्टरों का एक दल भी चीनी सेनाओं के साथ काम करने के लिए भेजा। राष्ट्रीय कांग्रेस को पूरा-पूरा विश्वास था कि भारत का भविष्य उस संघर्ष से घनिष्ठतापूर्वक जुड़ा हुआ है जो एक तरफ फासीवाद तथा दूसरी तरफ स्वाधीनता, समाजवाद और जनतंत्र की शक्तियों के बीच छिड़ने वाला है। विश्व की घटनाओं के प्रति कांग्रेस में उभरते हुए दृष्टिकोण तथा दुनिया में भारत की स्थिति की चेतना को जवाहरलाल नेहरु ने 1936 के लखनऊ अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में सामने रखा था - हमारा संघर्ष वास्तव में स्वाधीनता के एक और बड़े संघर्ष का भाग था और जो शक्तियाँ हमें प्रेरित कर रहीं थीं वे पूरी दुनिया में लाखों दूसरे लोगों को भी प्रेरित कर रही तथा कर्मक्षेत्र में ला रही थीं। संकट की स्थिति में पूँजीवाद ने फासीवाद का रूप लिया पराधीन औपनिवेशिक देशों में साम्राज्यवाद जो कुछ बहुत पहले से रहा है, स्वयं को जन्म देने वाले कुछ देशों में ही पूँजीवाद ने भी वैसा ही रूप धारण कर लिया। फासीवाद और साम्राज्यवाद इस तरह पतनशील पूँजीवाद के दो रूप बनकर सामने आए......... पश्चिम में समाजवाद ने तथा पूर्वी तथा अन्य पराधीन देशों में उदीयमान राष्ट्रवाद ने फासीवाद और साम्राज्यवाद के इस गठजोड़ का विरोध किया। कांग्रेस साम्राज्यवादी शक्तियों के किसी भी आपसी युद्ध में भारत सरकार की किसी भी रूप में भागीदारी का विरोध करेगी, इस बात पर जोर देते हुए नेहरु ने “विश्व की प्रगतिशील शक्तियों के प्रति, स्वाधीनता के लिए तथा राजनीतिक और सामाजिक बंधन तोड़ने के लिए लड़ने वालों के प्रति” अपने पूरे सहयोग का वचन दिया क्योंकि “साम्राज्यवाद और फासीवादी प्रतिक्रिया के विरोध में उनके संघर्ष से हमें यह लगता है कि हमारा संघर्ष एक साझा संघर्ष है।” रजवाड़ों की जनता का संघर्षइस काल का चौथा प्रमुख घटनाक्रम यह था कि राष्ट्रीय आंदोलन रजवाड़ों तक भी फैल गया। इन रजवाड़ों में से अधिकांश में आर्थिक से राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ नरक जैसी थीं। किसान दमन के शिकार थे, मालगुजारी और कर बहुत अधिक तथा असह्य थे, शिक्षा का कोई खास प्रसार न था, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक सेवाएँ एकदम पिछड़ेपन की हालत में थीं और प्रेस की स्वतंत्रता तथा दूसरे नागरिक अधिकारों का शायद ही कोई मान हो। रजवाड़े की आय का बहुत बड़ा भाग राजा और उसके परिवार के भोग-विलास पर खर्च होता था। अनेक रजवाड़ों में भूदास-प्रथा, गुलामी और बेगार का बोलबाला था। पहले के पूरे इतिहास में आंतरिक विद्रोह या बाहरी आक्रमण की चुनौतियाँ इन भ्रष्ट और पतित राजा-महाराजाओं की मनमानी पर कुछ हद तक नियंत्रण रखती थीं, परंतु ब्रिटिश शासन ने राजाओं को इन दोनों खतरों से सुरक्षित बना दिया और अब वे खुलकर अपने शासन का दुरुपयोग करने लगे।इसके अलावा राष्ट्रीय एकता के विकास में बाधा डालने तथा उदीयमान राष्ट्रीय आंदोलन का मुकाबला करने के लिए ब्रिटिश अधिकारी भी राजाओं का इस्तेमाल करने लगे। राजा-महाराजा भी, अपनी बारी में, किसी जनविद्रोह के आगे अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सत्ता पर निर्भर थे और उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति दुश्मनी का रवैया अपनाया। 1921 में चेंबर आफ प्रिंसेज की स्थापना की गई ताकि महाराजे मिल-बैठ सकें और ब्रिटिश मार्गदर्शन में अपने साझे हित के विषयों पर विचार कर सकें। 1935 के भारत सरकार कानून में भी प्रस्तावित संघीय ढाँचे की योजना इस प्रकार रखी गई थी कि राष्ट्रवादी शक्तियों पर नियंत्रण बना रहे। इसमें व्यवस्था थी कि ऊपरी सदन में कुल सीटों के 2/5 पर तथा निचले सदन में 1/3 पर रजवाड़ों का प्रतिनिधित्व रहेगा। अनेक रजवाड़ों की जनता अब जनतांत्रिक अधिकारों और लोकप्रिय सरकारों की माँग को लेकर आंदोलन करने लगी। विभिन्न रजवाड़ों में राजनीतिक गतिविधियों के तालमेल के लिए दिसंबर 1927 में ही आल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कांफ्रेंस की स्थापना हो चुकी थी। दूसरे असहयोग आंदोलन ने रजवाड़ों की जनता पर काफी गहरा प्रभाव डाला और उन्हें राजनीतिक गतिविधियों के लिए प्रेरित किया। अनेक रजवाड़ों, खासकर राजकोट, जयपुर, कश्मीर, हैदराबाद और ट्रावनकोर में जनसंघर्ष चलाए गए। राजाओं ने इन संघर्षों का सामना निर्मम दमन के द्वारा किया। इनमें से कुछ ने सांप्रदायिकता का सहारा भी लिया। हैदराबाद के निजाम ने जन-आंदोलन को मुस्लिम-विरोधी और कश्मीर के महाराजा ने उसे हिंदू-विरोधी घोषित किया, जबकि ट्रावनकोर के महाराजा का दावा था कि जन-आंदोलन के पीछे ईसाइयों का हाथ है। राष्ट्रीय कांग्रेस ने रजवाड़ों की जनता के संघर्ष का समर्थन किया और राजाओं से आग्रह किया कि वे जनतांत्रिक प्रतिनिधि सरकार स्थापित करें और जनता को मूलभूत नागरिक अधिकर दें। 1938 में जब कांग्रेस ने अपने स्वाधीनता के लक्ष्य को परिभाषित किया तो इसमें रजवाड़ों की स्वाधीनता को भी शामिल किया। अगले साल त्रिपुरी अधिवेशन में रजवाड़ों की जनता के आंदोलनों में और भी सक्रिय रूप से भाग लेने का उसने फैसला किया। ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को 1939 में आल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कांफ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया। रजवाड़ों की जनता के आंदोलन ने उस जनता में राष्ट्रीय चेतना पैदा की। इससे पूरे भारत में एकता की नई चेतना भी फैली। सांप्रदायिकता का विकासपाँचवाँ महत्वपूर्ण घटनाक्रम सांप्रदायिकता का विकास था। सीमित मताधिकार तथा अलग-अलग चुनाव मंडलों के आधार पर विधान सभाओं के लिए जो चुनाव हुए उससे एक बार फिर अलगाववादी भावनाएँ पैदा हो गईं। इसके अलावा कांग्रेस अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित अनेक सीटें जीतने में असफल रही। मुसलमानों के लिए कुल 482 सीटें आरक्षित थीं मगर कांग्रेस को इनमें केवल 26 मिलीं और उसमें भी 15 केवल पश्चिमोत्तर सीमा सीमा-प्रांत में मिलीं, हालाँकि इनमें ज्यादा सीटें मुस्लिम लीग को भी नहीं मिली। हिंदू महासभा भी बुरी तरह हारी। इसके अलावा जमींदारों और सूदखोरों की पार्टियाँ भी चुनाव में धूल चाटतीं नजर आईं। कांग्रेस ने एक मूलगामी कृषि कार्यक्रम अपना लिया था और किसान आंदोलन फैल रहे थे - इन दो बातों को देखकर जमींदार और सूदखोर अब सांप्रदायिक पार्टियों को अपना समर्थन देने लगे। उन्होंने समझ लिया कि आम जनता की व्यापक राजनीतिक भागीदारी के युग में उनके हितों की खुलकर वकालत कर सकना अब संभव नहीं होगा। अब सांप्रदायिक पार्टियाँ मजबूत होने लगीं। जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग कांग्रेस की घोर विरोधी हो गई। अब उसने यह प्रचार शुरू कर दिया कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक हिंदुओं में समा जाने का खतरा है। उसने इस अवैज्ञानिक और अनैतिहासिक सिद्धांत का प्रचार किया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग-अलग राष्ट्र है और उनका एक साथ रह सकना असंभव है। 1940 में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित करके माँग की कि स्वाधीनता के बाद देश के दो भाग कर दिए जाएँ और पाकिस्तान नाम का एक अलग राज्य बनाया जाए।हिंदुओं के बीच हिंदू महासभा जैसे सांप्रदायिक संगठनों के अस्तित्व के कारण मुस्लिम लीग के प्रचार को और बल मिला। हिंदू एक अलग राष्ट्र है और भारत हिंदूओं का देश है, यह कहकर हिंदू संप्रदायवादियों ने मुस्लिम संप्रदायवादियों की ही बात दोहराई। इस तरह उन्होंने भी दो राष्ट्रों के सिद्धांत को मान लिया। उन्होंने इस बात का जमकर विरोध किया कि अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त सुरक्षा-व्यवस्था की जाए ताकि उन्हें बहुमत के प्रभुत्व का भय न रहे। एक तरफ से हिंदू संप्रदायवाद का औचित्य और भी कम था। हर देश में धार्मिक, भाषायी या जातीय अल्पसंख्यकों को कभी न कभी ऐसा लगता रहा है कि उनकी संख्या कम होने के कारण उनके सामाजिक और सांस्कृतिक हितों को हानि पहुँच सकती है। लेकिन बहुसंख्यक संप्रदाय ने जब भी वचन और कर्म से यह सिद्ध किया है कि ये भय निराधार है तो अल्पसंख्यकों का भय समाप्त हो गया है, परंतु जब बहुसंख्यक जनता का कोई भाग सांप्रदायिक और संकीर्ण हो जाता है और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बोलने या कुछ करने लगता है तो अल्पसंख्यक अपने को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। तब अल्पसंख्यकों का सांप्रदायिक और संकीर्ण नेतृत्व भी मजबूत होता है। उदाहरण के लिए चौथे दशक में मुस्लिम लीग वहीं मजबूत थी, जहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक थे। इसके विपरीत पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, पंजाब, सिंध और बंगाल में जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक थे और इसलिए अपने को कुछ सुरक्षित महसूस करते थे, वहाँ मुस्लिम लीग कमजोर थी। दिलचस्प बात यह है कि हिंदू और मुस्लिम संप्रदायवादियों ने कांग्रेस के खिलाफ एक-दूसरे से हाथ मिलाने में कोई संकोच नहीं किया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, पंजाब, सिंध और बंगाल में हिंदू संप्रदायवादियों ने कांग्रेस के विरोध मे मुस्लिम लीग तथा दूसरे संप्रदायवादियों ने कांग्रेस के विरोध में मुस्लिम लीग तथा दूसरे सांप्रदायिक संगठनों का मंत्रिमंडल बनवाने में सहायता की। सरकार-समर्थक रवैया अपनाना भी तमाम सांप्रदायिक संगठनों की एक साझी विशेषता थी। यहाँ हम कह दें कि हिंदू और मुस्लिम राष्ट्रवाद की बात करने वाले किसी भी सांप्रदायिक संगठन या दल ने विदेशी शासन विरोधी संघर्ष में कभी कोई सक्रिय भाग नहीं लिया। दूसरे धर्मों की जनता तथा राष्ट्रवादी नेताओं को ही वे अपना वास्तविक शत्रु समझते थे। सांप्रदायिक संगठन और दल जनता की सामाजिक और अर्थिक माँगे उठाने से भी कतराते रहे जबकि राष्ट्रवादी आंदोलन, जैसा कि हमने देखा है, बढ़-चढ़कर इन माँगों को उठाता रहा। इस संबंध में वे ऊँचे वर्गों के निहित स्वार्थों का ही प्रतिनिधित्व करने लगे। बहुत पहले 1933 में ही इस बात को जवाहरलाल नेहरु ने समझ लिया था - आज सांप्रदायिकता का आधार राजनीतिक प्रतिक्रिया है और इसलिए हम देखते हैं कि सांप्रदायिक नेता बिना किसी अपवाद के राजनीतिक और आर्थिक मामलों में प्रतिक्रियावादी बन बैठते हैं। ऊँचे वर्गों के लोगों के संगठन यह दिखाकर कि वे धार्मिक अल्पसंख्यकों या बहुसंख्यकों की सामुदायिक माँगों के पक्षधर हैं, अपने स्वयं के वर्गीय हितों को छिपाने के प्रयास करते हैं। हिंदुओं, मुसलमानों तथा दूसरों की ओर से रखी गई विभिन्न सामुदायिक माँगों को आलोचनात्मक विश्लेषण करने पर पता चलेगा कि इनका जनता से कुछ भी लेना-देना नहीं है। राष्ट्रीय आंदोलन ने सांप्रदायिक ताकतों का हमेशा दृढ़ता से विरोध किया और धर्मनिरपेक्षता से उसकी प्रतिबद्धता हमेशा गहरी और संपूर्ण रही। फिर भी वह सांप्रदायिक चुनौती का सामना करने में पूरी तरह सफल न हो सका। अंत में सांप्रदायिकता देश का विभाजन कराने में सफल रही। इस असफलता की व्याख्या कैसे की जाए ? इसका एक उत्तर जो प्रायः दिया जाता है, वह यह है कि राष्ट्रवादी नेताओं ने सांप्रदायिक नेताओं से बातचीत करने और उन्हें साथ लेने के पर्याप्त प्रयास नहीं किए। हमारा विचार इसके ठीक विपरीत है। आरंभ से ही राष्ट्रवादी नेताओं ने सांप्रदायिक नेताओं से बातचीत पर बहुत अधिक भरोसा किया। लेकिन संप्रदायवाद से समझौता कर सकना या उसे संतुष्ट कर सकना संभव न था। इसके अलावा, एक तरह की सांप्रदायिकता को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है, प्रतिक्रिया के रूप में दूसरे तरह की सांप्रदायिकता हमेशा ही फलने-फूलने लगती। 1937 और 1939 के बीच कांग्रेस के नेताओं ने बार-बार जिन्ना से मुलाकात करके उसे मनाने का प्रयास किया। लेकिन जिन्ना ने कभी कोई ठोस माँग सामने नहीं रखी। इसके बजाए उन्होंने यह असंभव माँग रखी कि कांग्रेस माने कि वह हिंदुओं की पार्टी है और केवल हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है, केवल तभी वह कांग्रेस के लिए यह माँग स्वीकार करना संभव न था, क्योंकि ऐसा करके वह अपने बुनियादी धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रवादी चरित्र को ही छोड़ देती। वास्तविकता यह है कि संप्रदायवाद को संतुष्ट करने के जितने भी प्रयास किए गए, उतनी ही अधिक उसमें उग्रता आती गई। वास्तव में सांप्रदायिकता को संतुष्ट करने की जरूरत नहीं थी बल्कि उसके खिलाफ एक निर्मम राजनीतिक और विचारधारात्मक संघर्ष चलाने की जरूरत थी। आवश्यकता सांप्रदायिकता के खिलाफ एक व्यापक मुहिम चलाने की थी जैसी मुहिम 1880 के बाद के दशक में औपनिवेशिक विचारधारा के खिलाफ चलाई गई थी। लेकिन कभी-कभार को छोड़कर राष्ट्रीवादियों ने ऐसा नहीं किया। फिर भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद की सफलताओं को कम करके नहीं आँका जाना चाहिए। 1946-47 में विभाजन के आगे और पीछे हुए दंगों तथा सांप्रदायिक शक्तियों के पुनरूत्थान के बावजूद स्वतंत्रता के बाद भारत एक धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाने में तथा मूल रूप से एक धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक व्यवस्था और समाज खड़ा कर सकने में सफल रहा। हिंदू सांप्रदायिकता समाज में और राष्ट्रवादियों की कतारों तक में भी गहरे पैठी, फिर भी यह हिंदुओं के बीच इसकी शक्ति मामूली ही बनी रही। 1946-47 के दौरान धार्मिक कट्टरता तथा सांप्रदायिकता की लहर में अनेक मुसलमान बह गए, मगर कुछ दूसरे मुसलमान सांप्रदायिकता के सामने चट्टान की तरह खड़े रहे। अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, जोशीले भाषण देने वाले समाजवादी नेता युसूफ मेहरअली, निर्भीक पत्रकार एस. ए. बरेलवी, इतिहासकार मुहम्मद हबीब और कुंवर मुहम्मद अशरफ उर्दू शायरी के तुफानी पितरैल जैसे जोश मलीहाबादी, फैज अहमद फैज, सरदार जाफरी, साहिर लुधियानवी और कैफी आजमी और मौलाना मदनी - ये सब ऐसे नाम हैं जो इस संबंध में हमारे सामने मिसाल बनकर उभरते हैं। दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान राष्ट्रीय आंदोलनदूसरा विश्वयुद्ध सिंतबर 1939 में आरंभ हुआ जब जर्मन प्रसारवाद की हिटलर की नीति के आनुसार नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इसके पहले मार्च 1938 में वह अस्ट्रिया और मार्च 1939 में चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर चुका था। ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर को खुश रखने के लिए सब कुछ किया था, मगर अब वे पोलैंड की सहायता करने को बाध्य हो गए। भारत की सरकार राष्ट्रीय कांग्रेस या केंद्रीय धारा सभा के चुने हुए सदस्यों से परामर्श किए बिना फौरन युद्ध में शामिल हो गई।राष्ट्रीय कांग्रेस को फासीवादी (फासिस्ट) आक्रमण के शिकार देशों से पूरी सहानुभूति थी। वह फासीवाद विरोधी संघर्ष में लोकतांत्रिक शक्तियों की सहायता करने को तैयार थी। मगर कांग्रेस के नेताओं का सवाल यह था कि एक गुलाम राष्ट्र द्वारा दूसरों के मुक्ति-संघर्ष में साथ देना किस प्रकार सभव था ? इसलिए उन्होंने माँग की कि भारत को स्वाधीन घोषित किया जाए या कम से कम भारतीयों को समुचित अधिकार दिए जाए ताकि वे युद्ध में सक्रिय भाग ले सकें। ब्रिटिश सरकार ने इस माँग को मानने से इनकार कर दिया तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों और राजा-महाराजाओं को कांग्रेस के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास किया। इसलिए कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडलों को आदेश दिया कि वे त्यागपत्र दे दें। अक्टूबर 1940 में गाँधीजी ने कुछ चुने हुए व्यक्तियों को साथ लेकर सीमित पैमाने पर सत्याग्रह चलाने का निर्णय किया। सत्याग्रह को सीमित इसलिए रखा गया कि देश में व्यापक उथल-पुथल न हो और ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में बाधा न पड़े। वायसराय के नाम एक पत्र में गाँधीजी ने इस आंदोलन के उद्देश्यों की व्याख्या इस प्रकार की - कांग्रेस नाजीवाद की विजय की उतनी ही विरोध है जितना कि कोई अंग्रेज हो सकता है। लेकिन उसकी आपत्ति को युद्ध में उसकी भागीदारी की सीमा तक नहीं खींचा जा सकता और चूँकि आपने तथा भारत-सचिव महोदय ने घोषणा की है कि पूरा भारत स्वेच्छा से युद्ध प्रयास में सहायता कर रहा है, इसलिए यह स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है कि भारत की जनता का विशाल बहुमत इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखता। वह नाजीवाद तथा भारत पर शासन कर रही दोहरी निरंकुशता में कोई अंतर नहीं करता। सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे थे। 15 मई 1941 तक 25,000 से अधिक सत्याग्रही गिरफ्तार किए जा चुके थे। 1941 में विश्व की राजनीति में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। पश्चिमी यूरोप तथा अधिकांश पूर्वी यूरोप में पोलैंड, बेल्जियम, हॉलैंड, नॉर्वे और फ्रांस पर अधिकार कर चुकने के बाद नाजी जर्मनी ने 22 जून 1941 को सोवियत संघ पर हमला बोल दिया। 7 दिसंबर को जापान ने पर्ल हार्बर में एक अमरीकी समुद्री बेड़े पर आकस्मिक हमला किया तथा जर्मनी और इटली की ओर से युद्ध में शामिल हो गया। उसने तेजी से फिलीपीन, हिंदचीन, इंडोनेशिया, मलाया और बर्मा पर अधिकार कर लिया। मार्च 1942 में रंगून पर उसका अधिकार हो गया। इससे युद्ध भारत की सीमाओं तक आ पहुँचा। हाल में रिहा हुए कांग्रेसी नेताओं ने जापानी आक्रमण की निंदा की और कहा कि अगर ब्रिटेन फौरन प्रभावी शक्ति भारतीयों को सौंप दे और युद्ध के बाद पूर्ण स्वाधीनता का वचन दे तो वे भारत की रक्षा तथा राष्ट्रों के हितों के लिए सहयोग को तैयार हैं। अब ब्रिटिश सरकार को युद्ध प्रयासों में भारतीयों के सक्रिय सहयोग की पूरी तरह आवश्यकता थी। ऐसा सहयोग पाने के लिए उसने एक कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा। क्रिप्स पहले लेबर पार्टी के उग्र सदस्य और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पक्के समर्थक थे। हालाँकि क्रिप्स ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य यहाँ “जितनी जल्दी संभव हो स्वशासन की स्थापना करना” था, फिर भी उनके तथा कांग्रेसी नेताओं की लंबी बातचीत टूट गई। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की यह माँग मानने से इनकार कर दिया कि वास्तविक शक्ति तत्काल भारतीयों को सौंपी जाए। दूसरी तरफ भारतीय नेता इस बात से संतुष्ट नहीं हुए कि उनसे भविष्य के लिए केवल वादे किए जाएँ और फिलहाल वायसराय के हाथों में निरंकुश शक्तियाँ बनी रहें। वे युद्ध प्रयासों में सहयोग के लिए तैयार थे, खासकर इसलिए कि जापानी आक्रमणकारियों से भारत के लिए ही खतरा पैदा हो गया था। लेकिन उन्हें लगता था कि वे यह काम तभी कर सकेंगे जब देश में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो जाए। क्रिप्स मिशन की असफलता से भारत की जनता रूष्ट हो गई। उसे फासीवाद-विरोधी शक्तियां से अभी भी पूरी सहानुभूति थी, मगर उसे लगता था कि देश की राजनीतिक स्थिति अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। युद्ध के दौरान वस्तुओं की कमी और बढ़ती कीमतों ने उसके असंतोष को और भी गहरा दिया था। अप्रैल-अगस्त 1942 के काल में तनाव लगातार बढ़ता गया। जैसे-जैसे जापानी फौजें भारत की ओर बढ़ती गईं तथा जापानी विजय का भय जनता और नेताओं को त्रस्त करने लगा और गाँधीजी उनके ही अधिक जुझारू होते गए। कांग्रेस ने अब फैसला किया कि अंग्रेजों से भारतीय स्वाधीनता की माँग मनवाने के लिए सक्रिय उपाय किए जाएँ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मीटिंग 8 अगस्त 1942 को बंबई में हुई जिसमें प्रसिद्ध “भारत छोड़ो” प्रस्ताव स्वीकार किया गया तथा इस उद्देश्य को पाने के लिए गाँधीजी के नेतृत्व में एक अहिंसक जनसंघर्ष चलाने का फैसला किया गया। प्रस्ताव में घोषणा की गई कि - भारत के लाभ तथा संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों की सफलता, दोनों के लिए भारत में ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति आवश्यक हो गई है.......... आधुनिक साम्राज्यवाद का प्रमुख शिकार होने के नाते भारत अब समस्या के केंद्र में आ चुका है क्योंकि भारत की स्वाधीनता से ही ब्रिटेन तथा संयुक्त राष्ट्र को परखा जाएगा और एशिया तथा अफ्रीका के जनगण में आशा और उत्साह का संचार होगा। इस तरह इस देश में ब्रिटिश शासन की समाप्ति एक जीवंत और तात्कालिक प्रश्न है जिस पर युद्ध का भविष्य तथा स्वाधीनता और जनतंत्र की सफलता निर्भर है। एक स्वाधीन भारत स्वाधीनता के संघर्ष में तथा नाजीवाद, फासीवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ अपने तमाम विशाल संसाधनों को झोंककर यह सफलता सुनिश्चित करेगा।” 8 अगस्त की रात में कांग्रेसी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए गाँधीजी ने कहा - इसलिए मैं अगर हो सके तो तत्काल, इसी रात, प्रभात से पहले स्वाधीनता चाहता हूँ.......... आज दुनिया में झूठ और मक्कारी का बोलबाला है......... आप मेरी बात पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं मंत्रिमंडल या ऐसी दूसरी वस्तुओं के लिए वायसराय से सौदा करने वाला नहीं हूँ। मैं पूर्ण स्वाधीनता से कम किसी चीज से संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ......... अब मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ, आप इसे अपने दिलों में संजोकर रख लें और हर एक साँस में इसका जाप करें। वह मंत्र यह है - ‘करो या मरो।’ हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएँगे या इस प्रयास में मारे जाएँगे, मगर हम अपनी पराधीनता को जारी रहते देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन कांग्रेस आंदोलन चला सके, इसके पहले ही सरकार ने कड़ा प्रहार किया। 9 अगस्त को बहुत तड़के ही गाँधीजी तथा दूसरे कांग्रेसी नेता गिरफ्तार करके अनजानी जगहों पर ले जाए गए और कांग्रेस को फिर एक बार गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। इन गिरफ्तारियों की खबर ने पूरे देश को सकते में डाल दिया और हर जगह विरोध में एक स्वतःस्फूर्त आंदोलन उठ खड़ा हुआ जिसमें जनता का अभी तक दबा हुआ गुस्सा झलक रहा था। नेताविहीन और संगठन विहीन जनता ने जिस ढंग से भी ठीक समझा, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। पूरे देश में कारखानों में, स्कूलों और कॉलेजों में हड़तालें और कामबंदी हुईं और प्रदर्शन हुए जिन पर लाठी चार्ज और फायरिंग भी हुईं। बार-बार की गोलीबारी और दमन से क्रुद्ध होकर जनता ने अनेक जगहो पर हिंसक कार्यवाहियाँ भी कीं। उसने पुलिस थानों, डाकखानों, रेलवे स्टेशनों आदि ब्रिटिश शासन के तमाम प्रतीकों पर हमले किए। उन्होंने टेलीफोन के तार उखाड़ दिए, तार के खंभे गिरा दिए, रेल लाइनें उखाड़ दीं और सरकारी इमारतों मे आग लगा दी। इस संबंध में मद्रास और बंगाल सबसे अधिक प्रभावित हुए। अनेक जगहों पर अनेक शहरों, कस्बों और गाँवों में विद्रोहियों का अस्थायी कब्जा भी हुआ। संयुक्त प्रांत, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के अनेक भागों में ब्रिटिश शासन लुप्त हो गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले, बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक और बंबई के सतारा जिले जैसे कुछ क्षेत्रों में क्रांतिकारियों ने ‘समानांतर सरकार’ भी बना ली। आम तौर पर छात्र, मजदूर और किसान ही इस ‘विद्रोह’ के आधार थे जबकि उच्च वर्गों के लोग तथा नौकरशाही सरकार के वफादार रहे। सरकार ने अपनी ओर से 1942 के आंदोलन को कुचलने के लिए सब कुछ किया। उसके दमन की कोई सीमा नहीं रही। प्रेस का पूरी तरह गला घोंट दिया गया। प्रदर्शन कर रही भीड़ों पर मशीनगनों से गोलियाँ तथा हवा में बम भी बरसाए गए। कैदियों को यातनाएँ दी गईं। पुलिस और खुफिया पुलिस का राज चारों ओर था। अनेक नगरों और कस्बों को सेना ने अपने नियंत्रण में ले लिया। पुलिस और सेना की गोलीबारी में 10,000 से अधिक लोग मारे गए। विद्रोही गाँवों को जुर्माना के रूप में भारी-भारी रकमें देनी पड़ीं और गाँव वालों पर सामूहिक रूप से कोड़े बरसाए गए। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में इतना निर्मम दमन कभी देखने को नहीं मिला था। सरकार अंततः आंदोलन को कुचलने में सफल रही। 1942 का यह विद्रोह वास्तव मे बहुत संक्षिप्त रहा। इसका महत्व इस बात में था कि इसने दिखाया कि देश में राष्ट्रवादी भावनाएँ किस गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुकी थीं। और जनता संघर्ष और बलिदान की कितनी बड़ी क्षमता प्राप्त कर चुकी थी। यह स्पष्ट था कि जनता की इच्छा के विरुद्ध भारत पर शासन कर सकना अब अंग्रेजों को संभव नहीं लगता। 1942 के विद्रोह के दमन के बाद, 1945 में युद्ध की समाप्ति तक देश में राजनीतिक गतिविधियाँ लगभग ठप रहीं। राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वमान्य नेता जेलों में बंद थे और कोई नया नेता उनकी जगह नहीं ले सका था और न ही देश को नेतृत्व दे सका था 1943 में बंगाल में आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा अकाल फूट पड़ा। कुछ ही महीनों में तीस लाख से अधिक लोग भूख से मर गए। इससे जनता एक भयानक गुस्से से भर उठी क्योंकि सरकार अगर चाहती तो इतने लोगों को अकाल से मरने से बचा सकती थी। फिर भी इस गुस्से को पर्याप्त राजनीतिक अभिव्यक्ति न मिल सकी। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन को देश के बाहर एक नई अभिव्यक्ति मिली। सुभाषचंद्र बोस मार्च 1941 में देश से बाहर निकल गए थे और सहायता के लिए सोवियत संघ जाना चाहते थे। लेकिन जून 1941 में सोवियत संघ भी जब मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में उतरा तो वे जर्मनी चले गए। वहाँ से वे फरवरी 1943 में जापान के लिए चल पड़े ताकि जापानी सहायता से वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष चला सकें। भारत की स्वाधीनता के लिए सैनिक अभियान चलाने के उद्देश्य से उन्होंने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की। इसमें उनकी सहायता एक पुराने आतंकवादी क्रांतिकारी रासबिहारी बोस ने की। सुभाष चन्द्र बोस के वहाँ पहुँचने से पहले एक सेना बनाने के लिए कुछ काम जनरल मोहनसिंह कर चुके थे जो ब्रिटिश भारत की सेना में कप्तान थे। दक्षिण-पूर्व एशिया में रहने वाले भारतीय तथा मलाया, सिंगापुर और बर्मा में जापानी सेनाओं द्वारा बंदी बनाए गए भारतीय सैनिक और अधिकारी बड़ी संख्या में आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। सुभाष चंद्र बोस ने, जिन्हें अब आजाद हिंद फौज के सिपाही “नेताजी” कहते थे, अपने अनुयायियों को “जय हिंद” का मूलमंत्र दिया। बर्मा से भारत पर आक्रमण करने में आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना का साथ दिया। अपनी मातृ भूमि को स्वाधीन कराने के विचार से प्रेरित हाकर आजाद हिंद फौज के सैनिक अधिकारी यह आशा करने लगे थे कि वे स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का प्रमुख सुभाष चंद्र बोस को बनाकर उनके साथ भारत में उसके मुक्तिदाताओं के रूप में प्रवेश करेंगे। 1944-45 में युद्ध में जापान की पराजय के बाद आजाद हिंद फौज की भी हार हुई और सुभाष चंद्र बोस टोकियो जाते हुए रास्ते में एक वायुयान दुर्घटना में मारे गए। उस समय भारत के अधिकांश राष्ट्रवादी नेताओं ने उनकी इस रणनीति की आलोचना की कि फासीवादी ताकतों के साथ सहयोग करके स्वाधीनता जीती जाए, फिर भी आजाद हिंद फौज की स्थापना करके उन्होंने देशभक्ति का एक प्रेरणाप्रद उदाहरण भारतीय जनता और भारतीय सेना के सामने रखा। पूरे देश ने उन्हें “नेताजी” का सम्मानित नाम दिया। युद्धोत्तर काल का संघर्षअप्रैल 1945 में यूरोप में युद्ध समाप्त हुआ। इसी के साथ भारत के स्वाधीनता संघर्ष के एक नए चरण में प्रवेश किया। 1942 के विद्रोह तथा आजाद हिंद फौज की मिसाल ने भारतीय जनता की बहादुरी और दृढ़ता को स्पष्ट कर दिया था। जेलों से राष्ट्रीय नेता जब रिहा हुए तो जनता स्वाधीनता और उसे आपसी समझौतां के द्वारा अपनी कुछ शक्तियाँ सौंप सकते थे। लेकिन दोनों एक ऐसी अंतरिम सरकार की योजना पर सहमत न हो सके जो एक स्वतंत्र और संघीय भारत के लिए एक संविधान बनाने के उद्देश्य से एक संविधान सभा का गठन करती। कैबिनेट मिशन की जिस योजना पर दोनों पहले सहमत हो चुके थे उसके बारे में भी दोनों ने अलग-अलग व्याख्याएँ सामने रखीं। अंततः सितंबर 1946 में कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरु के नेतृत्व में एक अंतरिम मंत्रि मंडल का गठन किया। कुछ हिचक के बाद अक्टूबर में मुस्लिम लीग भी इस मंत्रिमंडल में शामिल हो गई मगर उसने संविधान सभा का बहिष्कार करने का फैसला किया। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि ब्रिटेन जून 1948 तक भारत का शासन छोड़ देगा।लेकिन मिलने वाली स्वाधीनता की खुशियों पर अगस्त 1946 के बाद भड़कने वाले व्यापक सांप्रदायिक दंगों ने पानी फेर दिया। हिंदू और मुस्लिम संप्रदायवादियों ने इन जघन्य हत्याओं का दोशी एक दूसरे को ठहराया और क्रूरता से एक दूसरे का मुकाबला करते रहे। न्यूनतम मानव-मूल्यों का इस तरह उल्लंघन होते और सत्य-अहिंसा को ताक पर रखा जाते देखकर महात्मा गाँधी दुख से भर उठे। उन्होंने दंगे रोकने के लिए पूर्वी बंगाल और बिहार की पदयात्रा की। सांप्रदायिकता की आग को बुझाने में दूसरे अनेक हिंदू-मुसलमानों ने भी प्राणों से हाथ धोए। लेकिन इसके बीज सांप्रदायिक तत्वों ने, विदेशी सरकार की सहायता से बहुत गहरे बोए थे। गाँधीजी और दूसरे राष्ट्रवादी नेता सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों और भावनाओं से जूझते रहे मगर बेकार। अंत में मार्च 1947 में वायसराय बनकर भारत आए लार्ड लुई माउंटबेटन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से लंबी-लंबी बातचीतों के बाद समझौते का एक रास्ता निकाला कि देश स्वाधीन तो होगा मगर एक नहीं रहेगा। भारत का विभाजन होगा और भारत के साथ पाकिस्तान नामक एक नया राज्य भी स्थापित होगा। बड़े पैमाने पर खून-खराबा और सांप्रदायिक दंगों का अंदेशा सामने था, इसलिए राष्ट्रवादी नेताओं ने मजबूर होकर भारत का विभाजन स्वीकार कर लिया। लेकिन उन्होंने दो राष्ट्रों का सिद्धांत नहीं माना। उन्होंने यह नहीं माना कि देश का एक-तिहाई भाग दे दिया जाए जिसकी माँग भारत की जनसंख्या में मुसलमानों के भाग के आधार पर मुस्लिम लीग कर रही थी। वे केवल वही क्षेत्र देने पर राजी हुए जहाँ मुस्लिम लीग का व्यापक प्रभाव था। इस तरह पंजाब, बंगाल और असम का भी विभाजन आवश्यक हो गया। मुस्लिम लीग को एक “घुन-लगा” पाकिस्तान ही मिला। पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत तथा असम के सिलहट जिले में लीग का प्रभाव संदिग्ध था, इसलिए वहाँ जनमत-संग्रह कराने का निश्चय हुआ। दूसरे शब्दों में, देश का विभाजन तो हुआ, मगर हिंदू धर्म और इस्लाम के आधार पर नहीं। भारतीय राष्ट्रवादियों ने विभाजन को स्वीकार तो किया मगर इसलिए नहीं कि यहाँ दो (हिंदू और मुस्लिम) राष्ट्र रहते थे, बल्कि इसलिए कि पिछले लगभग 70 वर्षों के दौरान हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिकता का विकास इस प्रकार हुआ था कि विभाजन न होता तो वहशियाना और बर्बर सांप्रदायिक दंगों में लाखों लोगों का संहार होता। अगर ये दंगे देश के किसी एक वर्ग तक सीमित होते तो कांग्रेस के नेता उन्हें दबाने और विभाजन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने के प्रयास करते। लेकिन दुर्भाग्य से यह आपसी मार-काट हर जगह हो रही थी और इसमें हिंदू-मुसलमान, दोनों की सक्रिय भागीदारी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि देश पर अभी भी विदेशियों का शासन था जिन्होंने दंगों के रोकने के लिए उँगली तक नहीं उठाई। उल्टे, अपनी फूट डालने वाली नीतियों से विदेशी सरकार ने इन दंगों को प्रोत्साहन ही दिया, शायद इस आशा में कि वह दोनों नवस्वतंत्र राष्ट्रों को आपस में लड़ा सकेगी।’ यहाँ तक कि अंत में जिन्ना को भी मजबूर होकर अपने दो राष्ट्रों के सिद्धांत में फेर बदल करना पड़ा जो कि सांप्रदायिकता की जड़ था। भारत में रहने का फैसला करने वाले मुसलमानों ने जब उनसे पूछा कि वे क्या करें, जो जिन्ना ने कहा कि उन्हें भारत का वफादार नागरिक बनना चाहिए। 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की संविधान सभा के आगे उन्होंने कहा था : “आपका धर्म या जाति या पंथ कोई भी हो सकता है, इसका राज्य के कारोबार से कुछ भी लेना-देना नहीं है।” वास्तव में अपनी सांप्रदायिक राजनीति के लिए जिस जिन्न को उन्होंने बोतल से बाहर निकाल दिया था, अब वे उसको फिर से बोतल में बंद करने की बेकार कोशिश कर रहे थे। भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा 3 जून 1947 को की गई। रजवाड़ों को यह छूट दी गई कि इनमें से किसी भी राज्य में वे शामिल हो जाएँ। रजवाड़ों की जनता के व्यापक आंदोलनों के दबाव में और गृहमंत्री सरदार पटेल की सफल कूटनीति के कारण अधिकांश रजवाड़ों ने भारत में शामिल होने का फैसला किया। जूनागढ़ के नवाब, हैदराबाद के निजाम, तथा जम्मू-कश्मीर के महाराजा कुछ समय तक अगर-मगर करते रहे। काठियावाड़ के समुद्र तट पर स्थित छोटे से रजवाड़े जूनागढ़ की जनता ने भारत में शामिल होने की घोषणा की मगर वहाँ के नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। अंततः भारतीय सेना ने राज्य पर कब्जा कर लिया और वहाँ एक जनमत-संग्रह कराया गया जिसका परिणाम भारत में शामिल होने के पक्ष में निकला। हैदराबाद के निजाम ने स्वतंत्र राज्य घोषित करने की कोशिश की, मगर वहाँ तेलंगाना क्षेत्र में हुए एक आंतरिक विद्रोह तथा वहाँ भारतीय सेनाओं के पहुँचने के बाद उसे भी 1948 में भारत में शामिल होना पड़ा। कश्मीर के महाराजा ने भी भारत या पाकिस्तान में शामिल होने में देर की, मगर वहाँ की जनता, जिसका नेतृत्व नेशनल कांफ्रेन्स कर रही थी, भारत में शामिल होना चाहती थी। मगर कश्मीर पर पाकिस्तान के पठानों तथा अनियमित फौजी दस्तों के हमले के बाद उसे भी अक्टूबर 1947 में भारत में शामिल होना पड़ा। 15 अगस्त 1947 को भारत ने उल्लास के साथ अपना पहला स्वाधीनता - दिवस मनाया। देशभक्तों की कई पीढ़ियों के बलिदानों तथा अनगिनत शहीदों के खून का फल आखिर हमें मिला। उनका सपना अब सच्चाई बन चुका था। 14 अगस्त की रात में संविधान सभा के आगे दिए गए अपने एक स्मरणीय वक्तव्य में जवाहरलाल नेहरू ने जनता की भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए कहा - वर्षों पहले हमने भविष्य के साथ और समय आ गया है कि पूरी तरह न सही तो भी बहुत काफी सीमा तक हम अपने वचन का पालन करें। रात को बारह का घंटा जब बजे़गा और जब पूरा विश्व सो रहा होगा, तब भारत जीवन और स्वाधीनता की ओर अग्रसर होगा। इतिहास में कभी-कभी ही वह क्षण आता है, तगर आता अवश्य है, जब हम पुराने से निकलकर नए को अपनाते हैं, हम जब एक युग का अंत होता है और जब किसी राष्ट्र की लंबे समय से दबी हुई आत्मा मुखर हो उठती है। उचित यही है कि हम इस पुनीत क्षण में भारत की एक और सभवतः अंतिम संघर्ष की आशा की जाय। यह नया संघर्ष आजाद हिंद फौज के सैनिकों और अधिकारियों पर चलाए गए मुकद्दमें के विरोध में एक व्यापक आंदोलन के रूप में उभरा। सरकार ने आजाद हिंद फौज के जनरल शाहनवाज, जनरल गुरदयाल सिंह ढिल्लों और जनरल प्रेम सहगल पर दिल्ली के लाल किले में मुकद्दमा चलाने का फैसला किया। ये लोग पहले ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी थे। उन पर ब्रिटिश सिंहासन के प्रति निष्ठा की शपथ भंग करने और इस प्रकार ‘गद्दार‘ होने का आरोप लगाया गया। दूसरी ओर जनता ने उनका स्वागत राष्ट्रीय नायकों के रूप में किया। पूरे देश में उनकी रिहाई की माँग को लेकर विशाल जन-प्रदर्शन हुए। पूरा देश उत्तेजना से और इस आशा से भरा था कि अबकी बार का संघर्ष विजयी होगा। इसलिए वे इन नायकों को सजा दिए जाने की छूट नहीं दे सकती थी। ब्रिटिश सरकार भी इस समय भारतीय जनमत को अनदेखा करने की स्थिति में नहीं थी। हालाँकि कोर्ट मार्शल में आजाद हिंद फौज के इन बंदियों को दोषी पाया गया, मगर सरकार ने उन्हें छोड़ देने में ही भलाई समझी। ब्रिटिश सरकार के इस बदले रवैए के अनेक कारण थे। प्रथम, युद्ध के कारण विश्व में शक्तियों का संतुलन बदल गया था। युद्ध के बाद अब ब्रिटेन की जगह अमरीका और सोवियत संघ बड़ी शक्तियों के रूप में उभरे। ये दोनों भारत की स्वतंत्रता की माँग के समर्थक थे। द्वितीय, ब्रिटेन युद्ध में जीतने वाले पक्ष में था अवश्य, मगर अब उसकी आर्थिक और सैनिक शक्ति बिखर चुकी थी। ब्रिटेन को अब अपने को संभालने में ही वर्षों लग जाते। इसके अलावा, ब्रिटेन में सरकार भी बदल चुकी थी। कंजर्वेटिव पार्टी की जगह अब लेबर पार्टी की सरकार थी और उसके अनेक सदस्य कांग्रेस की माँगों के समर्थक थे। ब्रिटिश सैनिक युद्ध में थक-हार चुके थे। लगभग छः वर्षों तक लड़ने और खून बहाने के बाद अब वे और कई साल घर से दूर भारत में रहकर वहाँ की जनता के स्वाधीनता-संघर्ष को कुचलने के लिए तैयार नहीं थे। तृतीय, ब्रिटिश भारतीय सरकार को राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए यहाँ के नागरिक प्रशासन के भारतीय सदस्यों और सशस्त्र सेनाओं पर भरोसा नहीं रह गया था। आजाद हिंद फौज की घटना ने दिखा दिया था कि देशभक्ति की भावना भारतीय सेना में भी फैल चुकी थी जो भारत में ब्रिटिश शासन का प्रमुख आधार थी। आग में तेल छिड़कने का काम फरवरी 1946 में बंबई में भारतीय नौसेना के जहाजियों के विद्रोह ने किया। ये जहाजी सेना और नौसेना से सात घंटों तक लड़ते रहे और उन्होंने समर्पण तभी किया जब राष्ट्रीय नेताओं ने उनसे ऐसा करने के लिए कहा। दूसरी कई जगहों पर भी जहाजियां ने उनकी सहानुभूति में हड़ताल की। इसके अलावा भारतीय वायु सेना में भी व्यापक हड़तालें हुईं। ब्रिटिश शासन के दो और प्रमुख आधारों अर्थात पुलिस और नौकरशाही में भी राष्ट्रवादी झुकाव के चिह्न दिखाई देने लगे थे। अब राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए उनका भरोसे के साथ उपयोग नहीं किया जा सकता था। उदाहरण के लिए बिहार और दिल्ली के पुलिस बलों ने हड़तालें कीं। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि भारतीय जनता अब आत्मविश्वास से भरपूर और टकराने के लिए तैयार नजर आ रही थी। वह अब विदेशी शासन के अपमान को और झेलने को तैयार न थी। अब आजादी मिलने तक आराम उसके लिए हराम था। नौसेना का विद्रोह तथा आजाद हिंद फौज के कैदियों की रिहाई के लिए हड़ताल हो चुकी थी। इसके अलावा 1945-46 में अनेकों आंदोलन, हड़तालें, कामबंदियाँ और प्रदर्शन पूरे देश में और हैदराबाद, ट्रावनकोर और कश्मीर जैसे अनेक रजवाड़ों तक में भी हुए। उदाहरण के लिए नवंबर 1945 में आजाद हिंद फौज के कैदियों की रिहाई की माँग को लेकर कलकत्ता में लाखों लोगों ने प्रदर्शन किया। तीन दिन तक नगर में सरकार नाम की कोई चीज रही ही नहीं थी। फिर 12 फरवरी 1946 को भी आजाद हिंद फौज के एक और बंदी, अब्दुर्रशीद की रिहाई की माँग को लेकर नगर में एक और जन-प्रर्दशन हुआ। 22 फरवरी को बंबई में एक पूर्ण हड़ताल हुई तथा कारखानों और दफतरों में काम ठप्प रहा। यह सब विद्रोही जहाजियों के समर्थन में था। इस जन-उभार को दबाने के लिए सेना बुलानी पड़ी। 48 घंटों के अंदर सड़कों पर 250 से अधिक लोग गोली के शिकार हुए। पूरे देश में बड़े पैमाने पर मजदूर-असंतोष भी फैल रहा था। शायद ही कोई उद्योग रहा हो जिसमें हड़ताल न हुई हो। जुलाई 1946 में डाक-तार मजदूरों ने देशव्यापी हड़ताल की। अगस्त 1946 में दक्षिण भारत में रेल मजदूरों की हड़ताल हुई। 1945 के बाद, जैसे-जैसे स्वाधीनता का समय पास आया, किसान आंदोलनों में एक नया उबाल आया। युद्ध के बाद किसानों का सबसे जुझारू संघर्ष बंगाल के बँटाईदारों का तेभागा संघर्ष था, जिसमें घोषणा की गई कि वे अब जमींदारों को फसल का आधा नहीं, बल्कि एक-तिहाई भाग ही देंगे। जमीन के लिए तथा ऊँचे लगानों के खिलाफ हैदराबाद, मलाबार, बंगाल, उत्तरप्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में भी संघर्ष हुए। कामबंदी, हड़तालों और प्रदर्शनों का आयोजन करने में स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों ने प्रमुख भूमिका निभाई। हैदराबाद, ट्रावनकोर, कश्मीर और पटियाला आदि रजवाड़ों में भी जन-उभार और संघर्ष फैल उठे। 1946 के आरंभ में प्रांतीय विधान सभाओं के चुनाव एक और प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम सिद्ध हुए। सामान्य सीटों में से अधिकांश सीटें कांग्रेस ने जीतीं जबकि मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों में से अधिकांश मुस्लिम लीग को मिलीं। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1946 में एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा कि भारतीय नेताओं से भारतीयों को सत्ता सौंपने की शर्तों के बारे में बातचीत की जाए। कैबिनेट मिशन ने दो स्तरों वाली एक संघीय योजना का प्रस्ताव किया जिससे आशा की गई कि बड़ी मात्रा में क्षेत्रीय स्वायत्तता देकर भी राष्ट्रीय एकता को बनाए रखा जा सकेगा। इस योजना में प्रांतों और रजवाड़ों का एक संघ होता और संघीय केंद्र का केवल प्रतिरक्षा, विदेशी मामलों और संचार विषयों पर नियंत्रण होता। साथ ही प्रांत अपने-अपने क्षेत्रीय संगठन भी बना सकते थे। उसकी जनता की सेवा के प्रति और उससे भी व्यापकतर मानवता के हित में समर्पित होने का संकल्प करें।........ आज हमारे दुर्भाग्य का काल समाप्त होता है और भारत ने पुनः अपने-आपको पा लिया है। आज हम जिस उपलब्धि की खुशी मना रहे हैं वह निंरतर प्रयत्न चाहती है जाबकि हम वे संकल्प पूरे कर सके जो हम प्रायः करते आए हैं। परंतु यह उल्लास जिसे असीम और अबाध होना चाहिए था, दुख और उदासी से भरा हुआ था। भारत की एकता का सपना चकनाचूर हो चुका था। और भाई-भाई से बिछड़ चुका था। इससे भी बुरी बात यह थी कि स्वतंत्रता के इस क्षण में भी अवर्णनीय बर्बरता के साथ सांप्रदायिकता का दानव भारत और पाकिस्तान, दोनों में लाखों लोगों की बलि ले रहा था। अपने पूर्वजों की धरती से नाता तोड़कर लाखें-लाख शरणार्थी इन दो नए राज्यों में पहुँच रहे थे।’ राष्ट्र की विजय के इस क्षण में घटित इस त्रासदी के प्रतीक वही गाँधीजी थे जिन्होंने भारतीय जनता को अहिंसा-सत्य-प्रेम - साहस-शूरवीरता का संदेश दिया था, जो भारतीय संस्कृति के उत्कृष्टतम तत्वों के प्रतीक थे। राष्ट्रीय हर्ष के इन दिनों में भी वे घृणा से चूर बंगाल के गाँवों में चक्कर लगा रहे थे और उन लोगों को राहत पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे जो उस समय भी वहशियाना सांप्रदायिक हत्याकांडों के द्वारा स्वतंत्रता की कीमत चुकाने का काम कर रहे थे। और उन खुशियों की गूँज अभी थमी भी न थी कि 30 जनवरी 1948 को एक हत्यारे, घृणा से चूर एक हिंदू-कट्टरपंथी ने उस चिराग को बुझा दिया जो 70 वर्षों से हमारे इस देश में उजाला फैलाता आ रहा था। इस तरह गाँधीजी ‘‘एकता के जिस उद्देश्य के प्रति हमेशा समर्पित रहे उसी के लिए शहीद हो गये।‘‘’ एक अर्थ में स्वाधीनता की प्राप्ति के रूप में देश ने अभी सिर्फ पहला कदम उठाया था, अर्थात् विदेशी शासन को उखाड़ फेंककर उसने राष्ट्रीय पुनर्जन्म की प्रमुख बाधा को दूर किया था। सदियों के पिछड़ापन, पूर्वाग्रह, असमानता और अज्ञान अभी भी देश पर हावी थे और पुनर्रचना का लंबा काम अभी शुरु ही हुआ था। जैसा कि 1941 में अपने निधन से तीन माह पहले रवींद्रनाथ ठाकुर ने कहा था - ”भाग्य का चक्र किसी न किसी अंग्रेज जाति को बाध्य करेगा कि वह अपने भारतीय साम्राज्य से हाथ धो ले। लेकिन वे अपने पीछे किस तरह का भारत, कितनी बुरी बदहाली छोड़ जाएँगे ? जब उनके सदियों पुराने प्रशासन का सोता अंततः सूखेगा तब कितना कूड़-करकट और कीचड़ वे अपने पीछे छोड़ जाएँगे।” लेकिन स्वाधीनता के संघर्ष ने औपनिवेशिक शासन को ही नहीं उखाड़ फेंका था, इसकी एक तस्वीर भी सामने रखी थी। यह तस्वीर एक लोकतांत्रिक नागरिक स्वतंत्रताओं से भरपूर और धर्मनिरपेक्ष भारत की थी। यह तस्वीर एक स्वाधीन आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, सामाजिक और आर्थिक समानता और राजनीतिक रूप से जागरूक और सक्रिय जनता पर आधारित भारत की थी। यह तस्वीर थी एक ऐसे भारत की जो अपने पड़ोसियों और शेष विश्व के साथ शांतिपूर्वक रहता हो और जिसका आधार एक स्वतंत्र विदेश नीति हो। इस तस्वीर को मूर्त रूप देने का पहला प्रयास जवाहरलाल नेहरु और भीमराव अंबेडकर के मार्गदर्शन में संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत का नया संविधान बनाकर किया। 26 जनवरी 1950 को लागू होने वाले इस संविधान ने कुछ बुनियादी सिंद्धान्त और मूल्य सामने रखे। इसके अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष और जनतांत्रिक गणराज्य होगा जिसमें बालिग मताधिकार (सभी बालिग स्त्री-पुरुषों के लिए मत देने का अधिकार) पर आधारित एक संसदीय प्रणाली होगी। यह एक संघीय व्यवस्था होगी जिसमें संघ सरकार और संघ बनाने वाले राज्यों के अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से अलग-अलग होंगे। संविधान ने सभी भारतीय नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकर दिए, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सभा करने और संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संपत्ति जुटाने और उसका उपयोग करने की स्वतंत्रता आदि। संविधान ने सभी नागरिकों को कानून के सामने बराबरी तथा सरकारी रोजगार के अवसर की समानता की जमानत दी। यह निश्चित हुआ कि राज्य धर्म, जाति, लिंग या जन्म-स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं करेगा। ‘अस्पृश्यता’ का उन्मूलन कर दिया गया तथा किसी भी रूप में इसके व्यवहार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सभी भारतीयों को स्वतंत्रतापूर्वक किसी भी धर्म को मानने, उसके अनुसार कार्य करने तथा उसका प्रचार करने का अधिकार दिया गया। साथ ही पूरी तरह राज्य के खर्च पर चलने वाले किसी भी शैक्षिक संस्थान में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा देने पर रोक लगा दी गई। संविधान मे कुछ “राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत” भी निश्चित किए गए जिन्हें किसी अदालत द्वारा तो लागू नहीं कराया जा सकता मगर जो कानून बनाने में राज्य का मार्गदर्शन करेंगे। इसमें ये सिद्धांत शामिल हैं - राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित एक सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को प्रोत्साहन, धन और उत्पादन के साधनों का कुछ हाथों में केंद्रीकरण रोकना, स्त्री-पुरुष, दोनों के लिए समान काम का समान वेतन, ग्राम पंचायतों की स्थापना, काम और शिक्षा का अधिकार, बेरोजगारी, बुढ़ापे और बीमारी में सार्वजनिक सहायता, पूरे देश मे एकसमान पारिवारिक कानून तथा जनता के कमजोर वर्गों, खासकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, के शैक्षिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन। अपनी क्षमताओं पर भरोसा करके तथा मन में सफलता की आकांक्षा लेकर अब भारतीय जनता अपने देश का कायाकल्प करने तथा एक न्यायप्रिय, श्रेष्ठ समाज और एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समतावादी भारत का निर्माण करने के काम में जुट गई। | |||||||||
| |||||||||