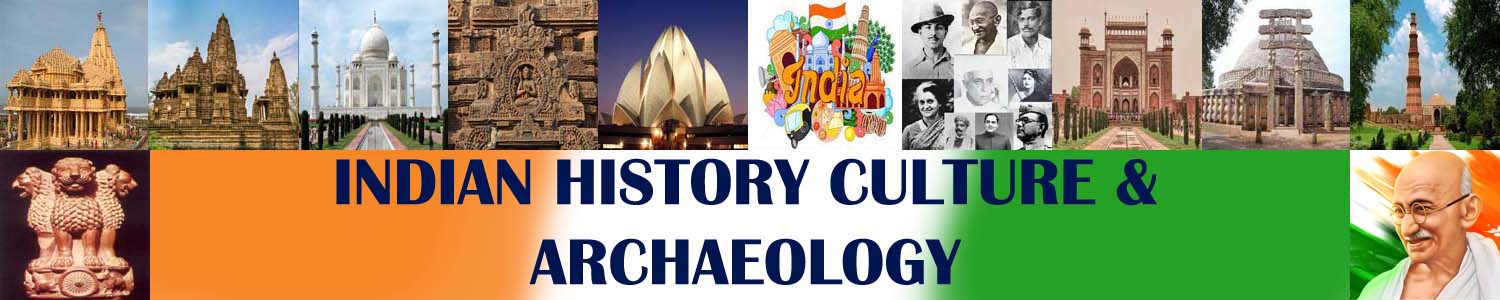| |||||||||
|
भारत में उग्रवादी आन्दोलन का विकास एवं साम्प्रदायिकता का उदय
उग्र राष्ट्रवाद का विकासवर्षा के कालक्रम में देश में धीरे-धीरे उग्र राष्ट्रवाद (जिसे गरमपंथ भी कहते हैं) का विकास होता आ रहा था। यह 1905 के बंगाल-विभाजन-विरोधी आंदोलन में अभिव्यक्त हुआ।अपने आरंभिक काल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने अधिकाधिक लोगों को विदेशी प्रभुत्व की बुराइयों तथा देशभक्ति की भावना विकसित करने की आवश्यकता के प्रति जागरूक बनाया था। उसने शिक्षित भारतीयों को आवश्यक राजनीतिक प्रशिक्षण दिया था। वास्तव में उसने जनता की भावना को ही बदल दिया था तथा देश में एक नए जीवन का संचार किया था। साथ ही साथ, राष्ट्रवादियों की एक माँग मानने में ब्रिटिश सरकार की असफलता ने राजनीतिक चेतना-प्राप्त लोगों में उस समय वर्चस्व प्राप्त नरमपंथी नेतृत्व के सिद्धान्तों व विधियों के प्रति असंतोष पैदा कर दिया था। नरमपंथी राष्ट्रवादियों की माँगें मानने की जगह ब्रिटिश शासक उनकी हँसी उड़ाते और उन्हें नीची निगाहों से देखते थे। परिणामस्वरूप सभाओं, प्रार्थनापत्रों, स्मरणपत्रों और विधायिकाओं में भाषणों की जगह और भी जोरदार राजनीतिक कार्रवाइयों और तरीकों की माँगें उठने लगी। ब्रिटिश शासन के सही चरित्र की पहचाननरमपंथी राष्ट्रवादियों की राजनीति इस विश्वास पर आधारित थी कि ब्रिटिश शासन को अंदर से सुधारा जा सकता है। लेकिन राजनीतिक और आर्थिक प्रश्नों से संबंधित ज्ञान जब फैला तो धीरे-धीरे यह विश्वास टूट गया। इसके लिए काफी बड़ी हद तक नरमपंथियों का आंदोलन स्वयं उत्तरदायी था। राष्ट्रवादी लेखकों और आंदोलनकारियों ने जनता की निर्धनता का दोषी ब्रिटिश शासन को ठहराया। राजनीतिक रूप से चेतन भारतीय को विश्वास था कि ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारत का आर्थिक शोषण करना, अर्थात् भारत की संपत्ति से इंग्लैंड को समृद्ध बनाना है। उन्हें महसूस हुआ कि जब तक भारतीयों द्वारा नियंत्रित और संचालित कोई सरकार ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जगह नहीं ले लेती, आर्थिक क्षेत्र में भारत शायद ही कुछ प्रगति कर सके। राष्ट्रवादियों ने खासकर यह भी देखा कि भारत के उद्योग तब तक फल-फूल नहीं सकते जब तक कि उन्हें सुरक्षा और प्रोत्साहन देने वाली कोई भारतीयों की सरकार न हो। भारत में 1896 और 1900 के बीच जो भयानक अकाल फूटे और जिनमें 90 लाख से ऊपर लोग मरे, वे जनता की दृष्टि में विदेशी शासन के आर्थिक दुष्परिणामों के जीते-जागते प्रतीक थे।1892 और 1905 के बीच घटित राजनीतिक घटनाओं ने भी राष्ट्रवादियों को निराश करके उन्हें और भी उग्र राजनीति के बारे में सोचने को बाध्य किया। 1892 का इंडियन कौंसिल एक्ट, जिसका वर्णन हम कर चुके हैं, घोर निराशा का कारण सिद्ध हुआ। दूसरी ओर, जनता को जो थोड़े से राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे, उन पर भी हमले किए गए। 1898 में एक कानून बनाया गया जिसमें विदेशी शासन के प्रति “असंतोष की भावना” फैलाने को अपराध घोषित किया गया। 1899 में कलकत्ता नगर निगम में भारतीय सदस्यों की संख्या घटा दी गई। 1904 में इंडियन ऑफिशियल सेक्रेट्स एक्ट बना जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया। 1897 में नाटू भाइयों को बिना मुकदमा चलाए देशबाहर कर दिया गया और उन पर लगाए गए आरोपों तक को भी जनता को नहीं बतलाया गया। उसी वर्ष लोकमान्य तिलक और दूसरे समाचारपत्र-संपादकों को विदेशी सरकार के प्रति जनता को भड़काने के लिए लंबी-लंबी जेल-सजाएँ दी गईं। इन सबसे जनता को लगा कि सरकार और भी अधिक राजनीतिक अधिकार देने के बजाए उन्हें मिले थोड़े से अधिकार भी छीन ले रही थी। लार्ड कर्जन के कांग्रेस-विरोधी दृष्टिकोण ने अधिकाधिक लोगों को विश्वास दिलाया कि भारत में ब्रिटिश शासन के रहते राजनीतिक और आर्थिक प्रगति की आशा करना व्यर्थ है। यहाँ तक कि नरमपंथी नेता गोखले को भी शिकायत थी कि “नौकरशाही खुलकर स्वार्थी और राष्ट्रीय आकांक्षाओं की शत्रु बनती जा रही है।” सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी ब्रिटिश शासन अब प्रगतिशील नहीं रहा था। प्राथमिक और तकनीकी शिक्षा में कोई प्रगति नहीं हो रही थी। साथ ही अधिकारीगण उच्च शिक्षा के प्रति शंकित हो रहे थे और देश में उसके प्रसार में बाधा डालने की कोशिश तक कर रहे थे। 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय कानून से राष्ट्रवादियों को लगा कि भारत के विश्वविद्यालयों पर और भी सख्त सरकारी नियंत्रण स्थापित करने तथा उच्च शिक्षा का प्रसार रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह अधिकाधिक संख्या में भारतीयों को विश्वास होता जा रहा था कि देश की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रगति के लिए स्वशासन आवश्यक है और राजनीतिक पराधीनता का मतलब भारतीय जनता के विकास का अवरुद्ध होना है। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का प्रसार19वीं सदी के अंत तक भारतीय राष्ट्रवादियों का आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बहुत बड़ा था। उन्हें अपना शासन आप कर सकने तथा देश का विकास कर सकने की अपनी क्षमता में विश्वास हो चुका था। तिलक, अरविंद घोष और बिपिनचंद्र पाल जैसे नेताओं ने राष्ट्रवादियों को आत्मविश्वास का संदेश दिया और उसने आग्रह किया कि वे भारतीय जनता के चरित्र क्षमताओं पर भरोसा करें। उन्होंने जनता को बतलाया कि उनकी दुर्दशा का हल उनके अपने हाथों में हैं और इसके लिए उन्हें निर्भय और बलवान होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कोई राजनीतिक नेता न थे, मगर यह संदेश उन्होंने बार-बार दिया। उन्होंने घोषणा की-दुनिया में अगर कोई पाप है तो वह निर्बलता है। निर्बलता का त्याग करो, निर्बलता पाप है और निर्बलता मृत्यु है . . . . . सत्य की कसौटी यह है - कोई भी वस्तु अगर तुम्हें शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से निर्बल बनाती है तो उसे विश समझ उसका त्याग करो कि उसमें कोई जीवन नहीं है और वह सत्य नहीं हो सकती। उन्होंने जनता से यह भी कहा कि वह अतीत के महिमामंडन के भरोसे जीना छोड़ें और मर्दों की तरह भविष्य का निर्माण करें। उन्होंने कहा, “हे भगवान, हमारा यह देश अतीत के ऊपर अपनी शाश्वत निर्भरता से कब मुक्त होगा ?” आत्मप्रयास में इस विश्वास के कारण राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार करने की आकांक्षा भी जागी। यह विचार फैला कि अब राष्ट्रवाद के उद्देश्य को ऊँचे वर्गों के थोड़े से शिक्षित भारतीयों तक अब और सीमित नहीं रहना चाहिए। इसके बजाए, जनता की राजनीतिक चेतना को उभारा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, स्वामी विवेकानंद ने लिखा : “भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता है। ऊँचे वर्ग शारीरिक और नैतिक दृष्टि से मृतप्राय हैं।” यह महसूस किया जाने लगा था कि स्वाधीनता पाने के लिए जो व्यापक बलिदान आवश्यक है वह केवल जनता ही कर सकती है। शिक्षा और बेरोजगारी में वृद्धि19वीं सदी के अंत तक शिक्षित भारतीयों की संख्या में स्पष्ट वृद्धि हुई थी। इनका एक बड़ा भाग प्रशासन में बहुत कम वेतन पर काम कर रहा था और दूसरे बहुत से लोग बेरोजगार घूम रहे थे। अपनी आर्थिक स्थिति के कारण ये लोग ब्रिटिश सरकार के चरित्र को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने लगे। उनमें से अनेक उग्र राष्ट्रवादी नीतियों से आकर्षित हुए।इससे भी महत्वपूर्ण था शिक्षा-प्रसार का विचारधारात्मक पक्ष। शिक्षित भारतीयों की संख्या जितनी बड़ी, उतना ही लोकतंत्र, राष्ट्रवाद और आमूल परिवर्तन के पश्चिमी विचारों का प्रभाव भी फैला। ये शिक्षित भारतीय उग्र राष्ट्रवाद के बेहतरीन प्रचारक और अनुयायी सिद्ध हुए। इसके दो कारण थे- वे कम वेतन पाने वाले या बेरोजगार थे और साथ ही आधुनिक विचार प्रणाली और राजनीति की तथा यूरापीय और विश्व इतिहास की शिक्षा भी उन्हें मिली थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रभावइस काल की अनेक विदेशी घटनाओं ने भी भारत में उग्र राष्ट्रवाद के विकास को प्रोत्साहित किया। 1868 के बाद एक आधुनिक जापान के उदय ने दिखा दिया कि एक पिछड़ा हुआ एशियाई देश भी बिना किसी पश्चिमी नियंत्रण के अपना विकास कर सकता है। कुछ ही दशकों के काल में जापान के नेताओं ने अपने देश को पहले दर्जे की औद्योगिक और सैनिक शक्ति बना दिया था, व्यापक प्राथमिक शिक्षा का आरंभ किया था और एक सक्षम और आधुनिक प्रशासन खड़ा किया था। 1896 में इथियोपिया के हाथों इटली की सेना तथा 1905 में जापान के हाथों रुस की हार ने यूरोपीय श्रेष्ठता के भ्रम को तोड़कर रख दिया। एशिया में हर जगह एक छोटे से एशियाई देश के हाथों यूरोप की सबसे बड़ी सैनिक शक्ति की पराजय की खबर को उत्साह के साथ सुना।18 जून 1905 को ‘कराची क्रोनिकल’ नामक सामाचारपत्र ने जनता की भावनाओं को इस प्रकार व्यक्त किया - जो कुछ एक एशियाई देश ने किया है वह दूसरे भी कर सकते हैं. . . . . अगर जापान रूस की धुनाई कर सकता है तो भारत भी उतनी ही आसानी से इंग्लैंड को धुन सकता है. . . . . आइए, हम अंग्रेजों को समुद्र में फेंक दें और विश्व की महान शक्तियों के बीच जापान के बराबर अपना स्थान ग्रहण करें। आयरलैंड, रूस, मिश्र, तुर्की और जापान के क्रांतिकारी आंदोलनों तथा दक्षिण अफ्रीका के बोअर युद्ध ने भारतीयों को विश्वास दिला दिया कि अगर जनता एकजुट और बलिदान के लिए तैयार हो तो शक्तिशाली निरंकुश सरकारों को भी चुनौती दे सकती है। जिस बात की सबसे अधिक आवश्यकता थी वह थी देशभक्ति और आत्मबलिदान की भावना। उग्र राष्ट्रवादी विचार-संप्रदाय का अस्तित्वराष्ट्रीय आंदोलन के लगभग आरंभ से ही उग्र राष्ट्रवाद का एक संप्रदाय देश में मौजूद था। इस संप्रदाय के प्रतिनिधि बंगाल में राजनारायण बोस और अश्विनीकुमार दत्त तथा महाराष्ट्र में विष्णु शास्त्री चिपलुंकर जैसे नेता थे। इस संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि बाल गंगाधर तिलक थे जिन्हें आम तौर पर लोकमान्य तिलक कहते हैं। उनका जन्म 1856 में हुआ था। बंबई विश्वविद्यालय से स्नातक-परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद से ही उन्होंने पूरा जीवन देश-सेवा के लिए समर्पित कर दिया। 1880 के बाद के दशक में उन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना में भाग लिया, यही स्कूल बाद में फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने अंग्रेजी में ‘मरहठा तथा मराठी में ‘केसरी’ नामक पत्रों की स्थापना की। 1889 से वे ‘केसरी’ का संपादन करने लगे और इस पत्र के पृष्ठों में वे राष्ट्र वाद का प्रचार करने लगे। उन्होंने जनता को भारत की स्वाधीनता के लिए साहसी, स्वावलंबी और निःस्वार्थ योद्धा होने का पाठ पढ़ाया। 1893 में उन्होंने एक परंपरागत धार्मिक उत्सव, अर्थात् गणपति उत्सव का उपयोग गीतों और भाषणों के द्वारा राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार के लिए करना आरंभ कर दिया। 1895 में उन्होंने शिवाजी उत्सव का आयोजन आंरभ किया। इसका उद्देश्य महाराष्ट्रीय युवकों के आगे अनुकरण के लिए शिवाजी का उदाहरण सामने रखकर उनमें राष्ट्रवाद की भावना पैदा करना था। 1896-97 में उन्होंने महाराष्ट्र में कर न चुकाने का अभियान चलाया। उन्होंने महाराष्ट्र के अकाल-पीड़ित किसानों से कहा कि अगर उनकी फसल चौपट हो जाए तो वे मालगुजारी न दें। जब सरकार के खिलाफ घृणा और असंतोष भड़काने के आरोप में अधिकारियों ने उन्हें 1897 में गिरफ्तार किया तो उन्होंने दिलेरी और बलिदान का एक शानदार उदाहरण सामने रखा। उन्होंने सरकार से क्षमा माँगने से इंकार कर दिया जिस पर उन्हें 18 महीनों की कड़ी कैद की सजा हुई। इस तरह वे आत्मबलिदान की नई राष्ट्रीय भावना के जीते-जागते प्रतीक बन गए।20वीं सदी के आरंभ में उग्र राष्ट्रवादी संप्रदाय को एक अनुकूल राजनीतिक वातावरण प्राप्त हुआ। अब इसके समर्थक भी राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़े। तिलक के अलावा उग्र राष्ट्रवाद के दूसरे महत्वपूर्ण नेता विपिनचंद्र पाल, अरविंद घोष और लाला लाजपतराय थे। उग्र राष्ट्रवादियों के कार्यक्रम के विशिष्ट राजनीतिक पहलू इस प्रकार थे - उनका मत था कि भारतीयों को मुक्ति स्वयं अपने प्रयासों से प्राप्त करनी होगी तथा उन्हें अपनी पतित स्थिति से उबरने के प्रयत्न करने होंगे। उन्होंने घोषणा की, कि इस कार्य के लिए बड़े-बड़े बलिदान करने होंगे और तकलीफें सहनी होगी। उनके भाषण, लेख और राजनीतिक कार्य दिलेरी और आत्मविश्वास से भरपूर थे और अपने देश की भलाई के लिए किसी भी व्यक्तिगत बलिदान को कम समझते थे। भारत अंग्रेजों के “कृपापूर्ण मार्गदर्शन” और नियंत्रण में प्रगति कर सकता है, इसे मानने से उन्होंने इंकार कर दिया। वे विदेशी शासन से दिल से नफरत करते थे और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य स्वराज्य या स्वाधीनता है। उन्हें जनता की शक्ति में असीम विश्वास था और उनकी योजना जनता की कार्रवाई के द्वारा स्वराज्य प्राप्त करने की थी। इसलिए उन्होंने जनता के बीच राजनीतिक कार्य पर और जनता की सीधी राजनीतिक कार्रवाई पर जोर दिया। प्रशिक्षित नेतृत्व1905 तक भारत में ऐसे अनेक नेता थे जो पीछे के काल में राजनीतिक आंदोलनों के मार्गदर्शन तथा राजनीतिक संघर्षों के नेतृत्व संबंधी बहुमूल्य अनुभव प्राप्त कर चुके थे। राजनीतिक कार्यकर्ताओं की एक प्रशिक्षित टुकड़ी के बिना राष्ट्रीय आंदोलन को एक उच्चतर राजनीतिक स्तर तक ले जाना बहुत कठिन होता।बंगाल का विभाजन (बंग-भंग)इस तरह 1905 में जब बंगाल को दो टुकड़ों में बाँट दिया गया तब उग्र राष्ट्रवाद के उदय की परिस्थितियाँ विकसित हो चुकी थीं। इसी के साथ भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण आरंभ होता है। 20 जुलाई 1905 को लार्ड कर्जन ने एक आज्ञा जारी करके बंगाल को दो भागों में बाँट दिया। पहले भाग में पूर्वी बंगाल और असम थे और उसकी आबादी 3.1 करोड़ थी, जबकि दूसरे भाग में शेष बंगाल था और उसकी जनसंख्या 5.4 करोड़ थी जिसमें 1.8 करोड़ बंगाली और 3.6 करोड़ बिहारी और उड़िया थे। तर्क यह दिया था कि बंगाल का प्रांत इतना बड़ा था कि एक प्रांतीय सरकार उसका प्रशासन चला सकना असंभव था। लेकिन जिन अधिकारियों ने यह योजना तैयार की उनके दूसरे, राजनीतिक उद्देश्य भी थे। बंगाल तब भारतीय राष्ट्र वाद का केंद्र माना जाता था और इस कदम के द्वारा अधिकारीगण बंगाल में राष्ट्रवाद के प्रसार को रोकना चाहते थे। भारत सरकार के गृहसचिव रिसले ने 6 दिसंबर 1904 को एक अधिकारिक टिप्पणी में लिखा -एकजुट बंगाल अपने-आप में एक शक्ति है। बंगाल अगर विभाजित हो तो सभी भागों की दिशाएँ अलग-अलग होंगी। यही बात कांग्रेस के नेता महसूस करते हैं, उनकी आशंकाएँ पूरी तरह सही हैं और इस योजना का महत्व इसी में है. . . . . हमारा एक उद्देश्य हमारे शासन के विरोधियों को तोड़ना और इस प्रकार उन्हें कमजोर करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बंगाल के राष्ट्रवादियों ने विभाजन का जमकर विरोध किया। बंगाल के भीतर भी जमींदार, व्यापारी, वकील, छात्र, नगरों के गरीब लोग और स्त्रियाँ तक, समाज के विभिन्न वर्ग अपने प्रांत के विभाजन के विरोध में स्वतःस्फूर्त ढंग से उठ खड़े हुए। राष्ट्रवादियों ने बंगाल के विभाजन को एक प्रशासकीय उपाय ही नहीं, बल्कि भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक चुनौती समझा। उन्होंने इसे बंगाल को क्षेत्रीय और धार्मिक आधार पर बाँटने का प्रयास माना, धार्मिक आधार पर इसलिए कि पूर्वी भाग में मुसलमानों और पश्चिमी भाग में हिंदुओं का बहुमत था। उन्होंने समझा कि इस प्रकार बंगाल में राष्ट्र वाद को कमजोर और नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे बंगाली भाषा और संस्कृति को जबर्दस्त धक्का लगता। उनका तर्क था कि प्रशासन में कुशलता लाने के लिए हिंदी भाषी बिहार और उड़ीया भाषी उड़ीसा को प्रात के बंगाली भाषी क्षेत्र से अलग किया जा सकता है। इसके लिए सरकार ने यह कदम जनमत की पूरी तरह उपेक्षा करके उठाया था। विभाजन के खिलाफ बंगाल के विरोध की तीव्रता का कारण यह कि इसने एक बहुत संवेदनशील व साहसी जनता की भावनाओं को चोट पहुँचाई थी। बंग-भंग-विरोधी आंदोलनबंग-भंग-विरोधी आंदोलन या स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन बंगाल के पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रयासों के कारण था, न कि आंदोलन के किसी एक भाग के। आरंभ में इसके प्रमुखतम नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मित्र जैसे नरमपंथी नेता थे, मगर बाद में इसका नेतृत्व उग्र और क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने संभाल लिया। वास्तव में आंदोलन के दौरान नरमपंथी और उग्र राष्ट्रवादियों, दोनों ने एक दूसरे से सहयोग किया।विभाजन-विरोधी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को आरंभ हुआ। उस दिन कलकत्ता को टाउनहाल में विभाजन के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। इस सभा के बाद प्रतिनिधि आंदोलन को फैलाने के लिए पूरे प्रांत में फैल गए। विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया आंदोलन के नेताओं ने इस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। उस दिन लोगों ने उपवास रखे। कलकत्ता में हड़ताल हुई। लोग बहुत तड़के ही नंगे पैर चलकर गंगा में स्नान करने पहुँचे। इस अवसर के लिए रवींद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत “आमार सोनार बंगला” लिखा जिसे सड़कों पर चलने वाली भीड़ गाती। बाद में इस गीत को बंगलादेश ने 1971 में अपनी मुक्ति के बाद अपने राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। कलकत्ता की सड़कें “वंदे मातरम” की आवाज से गूँज उठीं और यह गीत रातों-रात बंगाल का राष्ट्रीय गीत बन गया, बाद में यही पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का राष्ट्रगान बन गया। रक्षाबंधन के उत्सव का एक नए ढंग से उपयोग किया गया। बंगालियों और बंगाल के दो टुकड़ों की अटूट एकता के प्रतीक के रूप में हिंदू-मुसलमान ने एक-दूसरे की कलाइयों पर राखियाँ बाँधीं। दोपहर को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया और वयोवृद्ध नेता आनंदमोहन बोस ने बंगाल की अटूट एकता जतलाने के लिए फेडरेशन हाल की बुनियाद रखी। इस अवसर पर उन्होंने 50,000 लोगों की सभा को संबोधित किया। स्वदेशी और बहिष्कारबंगाल के नेताओं को लगा कि केवल प्रदर्शनों, सार्वजनिक सभाओं और प्रस्तावों से शासकों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसके लिए और भी सकरात्मक उपाय करने होंगे जिनसे जनता की भावनाओं की तीव्रता का अच्छी तरह पता चले। इसका परिणाम था स्वदेशी और बहिष्कार। पूरे बंगाल में जनसभाएँ की गई जिनमें स्वदेशी अर्थात् भारतीय वस्तुओं का उपयोग तथा ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार के निर्णय किए और शपथ लिए गए। अनेक जगहों पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और विदेशी कपड़े बेचने वाली दुकानों पर धरने दिए गए। स्वदेशी आंदोलन को व्यापक सफलता मिली। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के अनुसार -स्वदेशीवाद जब शक्तिमान था तब उसने हमारे सामाजिक व पारिवारिक जीवन के पूरे ताने-बाने को प्रभावित किया। अगर विवाहों में ऐसी विदेशी वस्तुएँ उपहार में दी जातीं जिनके समान वस्तुएँ देश में बन सकती हों, वे लौटा दी जाती थीं। पुरोहित अक्सर ऐसे समारोहों में धार्मिक कार्य करने से इंकार कर देते जिनमें ईश्वर को भेंट में विदेशी वस्तुएँ दी जाती थीं। जिन उत्सवों में विदेशी नमक या विदेशी चीनी का उपयोग किया जाता उसमें भाग लेने से मेहमान लोग इनकार कर देते थे। स्वदेशी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पक्ष आत्मनिर्भरता या आत्मशक्ति पर दिया जाने वाला जोर था। आत्मनिर्भरता का मतलब था राष्ट्र की गरिमा, सम्मान और आत्मविश्वास की घोषणा। आर्थिक क्षेत्र में इसका अर्थ देशी उद्योगों व अन्य उद्योगों को बढ़ावा देना। अनेक कपड़ा मिलें, साबुन और माचिस के कारखाने, हैंडलूम के उद्यम, राष्ट्रीय बैंक और बीमा कंपनियाँ खुलीं। आचार्य पी. सी. राय ने प्रसिद्ध बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की। महान कवि रविंद्रनाथ ठाकुर तक ने एक स्वदेशी स्टोर खुलवाने में सहायता की। संस्कृति के क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन के अनेक परिणाम सामने आए। राष्ट्रवादी काव्य, गद्य और पत्रकारिता का विकास हुआ। इस समय रवींद्रनाथ ठाकुर, रजनीकांत सेन, सैयद अबू मुहम्मद और मुकुंद दास ने देशभक्ति के जो गीत लिखे वे बंगाल के आत्मनिर्भरता के लिए रचनात्मक उपाय किए गए। साहित्यिक, तकनीकी और शारीरिक शिक्षा देने के लिए राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाएँ स्थापित कीं क्योंकि वे शिक्षा की तत्कालीन प्रणाली को राष्ट्र वाद से विमुख करने वाली या कम से कम अपर्याप्त मानते थे। 15 अगस्त 1906 को एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् की स्थापना की गई कलकत्ता में एक राष्ट्रीय कॉलेज का आरंभ हुआ जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। छात्रों, स्त्रियों, मुसलमानों और जनता की भूमिकाएँस्वदेशी आंदोलन में एक प्रमुख भूमिका बंगाल के युवकों ने निभाई। उन्होंने स्वदेशी का प्रयोग और प्रचार किया तथा विदेशी वस्त्र बेचने वाली दुकानों के आगे धरने आयोजित करने में आगे-आगे रहे। सरकार ने छात्रों को दबाने की हर संभव कोशिश की। जिन स्कूलों और कॉलेजों के छात्र स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय हों उन्हें दंडित करने के आदेश जारी किए गए और उन्हें प्राप्त सहायताएँ व विशेषाधिकार छीन लिए गए और उन्हें विश्वविद्यालय से असंबद्ध कर दिया गया। उनके छात्रों को छात्रवृत्ति की परीक्षाओं में बैठने से रोक दिया गया, तथा उन्हें हर सरकारी नौकरी से वंचित रखने का निर्णय किया गया। राष्ट्रवादी आंदोलन में भाग लेने के दोषी छात्रों के खिलाफ अनुशासन की कार्यवाहियाँ की गई। अनेकों पर जुर्माने किए गए, अनेक स्कूलों वा कालेजों से निकाल दिए गए, गिरफ्तार किए गए और कभी-कभी पुलिस द्वारा लाठियों से पीटे भी गए। फिर भी छात्रों ने झुकने से इंकार कर दिया।स्वदेशी आंदोलन की एक महत्वपूर्ण बात इसमें स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी थी। शहरी मध्य वर्ग की सदियों से घरों में कैद महिलाएँ जुलूसों और धरनों में शामिल हुई। इसके बाद से राष्ट्रवादी आंदोलन में वे बराबर सक्रिय रहीं। अनेकों प्रमुख मुसलमान नागरिकों ने भी स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया। इनमें प्रसिद्ध वकील अब्दुर्रसूल, लोकप्रिय आंदोलनकारी लियाकत हुसैन और व्यापारी गजनवी प्रमुख थे। मौलाना अबुलकलाम आजाद एक क्रांतिकारी आतंकवादी संगठन में शामिल हुए। फिर भी मध्य और उच्च वर्गों के अनेकों दूसरे मुसलमान आंदोलन से अलग रहे या ढाका के नवाब के नेतृत्व में (जिसे भारत सरकार ने 14 लाख रुपयों का एक ऋण दिया था) उन्होंने इस आधार पर विभाजन का समर्थन किया कि पूर्वी बंगाल में मुसलमानों का बहुमत होगा। ढाका के नवाब और दूसरों को यह सांप्रदायिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए अधिकारियों ने प्रोत्साहित किया। ढाका में भाषण देते हुए लार्ड कर्जन ने कहा कि बंगाल के विभाजन का एक कारण था कि “पूर्वी बंगाल के मुसलमानों में एसी एकता स्थापित की जाए जैसी कि पुराने मुसलमान सूबेदार और सम्राटों के समय से देखने को नहीं मिली है।” आंदोलन का अखिल भारतीय चरित्रस्वदेशी और स्वराज की गूँज जल्द ही देश के दूसरे प्रांतों में भी गूँजने लगी। बंबई, मद्रास और उत्तर भारत में बंगाल की एकता के समर्थन में तथा विदेशी मालों के बहिष्कार के लिए आंदोलन चलाए गए। स्वदेशी आंदोलन को देश के दूसरे भागों तक पहुँचाने में प्रमुख भूमिका तिलक की रही। तिलक ने जल्द ही समझ लिया कि बंगाल में इस आंदोलन के उभरने के कारण भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास का एक नया अध्याय आरंभ हुआ है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनसंघर्ष चलाने तथा आपसी सहानुभूति के बंधन में पूरे देश को बांधने की चुनौती सामने थी और यह एक अच्छा अवसर था।उग्र राष्ट्रवाद का विकासविभाजन-विरोधी आंदोलन की कमान जल्द ही तिलक, विपिनचन्द्र पाल और अरविंद घोष जैसे उग्र राष्ट्रवादियों के हाथों में पहुँच गई। इसके अनेक कारण थे।प्रथम, नरमपंथियों के नेतृत्व में पहले के विरोध आंदोलन का कोई खास परिणाम नहीं निकला था। यहाँ तक कि नरमपंथी जिस उदारवादी भारत-सचिव लार्ड मार्ले से बहुत आशाएँ लगाए बैठे थे उसने भी कह दिया कि विभाजन अब एक अंतिम सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। दूसरे, बंगाल के दोनों भागों, खासकर पूर्वी बंगाल की सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने के बड़े प्रयत्न किए। बंगाल में हिंदू-मुस्लिम वैमनस्य के बीज संभवतः इसी समय पड़े। इससे राष्ट्रवादियों का जी खट्टा हो गया। लेकिन जनता को जुझारू और क्रांतिकारी राजनीति की ओेर जिस बात ने सबसे अधिक धकेला वह थी सरकार की दमन की नीति। खासकर पूर्वी बंगाल की सरकार ने राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाने की बहुत कोशिश की। स्वदेशी आंदोलन में छात्रों को भाग लेने से रोकने के लिए सरकार के प्रयासों का वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं। पूर्वी बंगाल में सड़कों पर “वंदे मातरम्” का नारा लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जनसभाओं को सीमित कर दिया गया और कभी-कभी उनकी अनुमति भी नहीं दी जाती थी। प्रेस पर नियंत्रण के लिए भी कानून बनाए गए। स्वदेशी कार्यकर्ताओं पर मुकदमें चलाए गए और उन्हें लंबी-लंबी जेल-सजाएँ दी गई। अनेक छात्रों को शारीरिक दंड तक दिए गए। 1906 से 1909 के बीच बंगाल की अदालतों में 550 से अधिक राजनीतिक मुकदमें आए। बहुत से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों पर मुकदमें चलाए गए और प्रेस की स्वतंत्रता पूरी तरह समाप्त कर दी गई। अनेक शहरों में सैनिक पुलिस लगा दी गई जहाँ जनता से उसकी झड़पें हुईं। दमन की सबसे बदनाम मिसालों में से एक है अप्रैल 1906 में बारीसाल में आयोजित बंगाल प्रांतीय सम्मेलन पर पुलिस का हमला। अनेक युवक स्वयंसेवकों को बुरी तरह पीटा गया और सम्मेलन को जबर्दस्ती भंग कर दिया गया। दिसंबर 1908 में बंगाल के नौ नेताओं को देशबाहर कर दिया गया, इनमें आदरणीय नेता कृष्ण कुमार मित्र और अश्विनी कुमार दत्त भी थे। इसके पहले पंजाब के नहरी इलाकों मे हुए दंगों के बाद लाला लाजपतराय और सरदार अजीतसिंह देशबाहर कर दिए गए थे। 1908 में महान नेता तिलक को दोबारा गिरफ्तार करके 6 वर्ष जेल की वहशियाना सजा दी गई। मद्रास में चिदंबरम पिल्लै और आंध्र में हरि सर्वोत्तम राव तथा दूसरे लोग बंदी बनाए गए। जब उग्र राष्ट्रवादियों ने मोर्चा संभाला तो उन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार के अलावा निष्क्रिय प्रतिरोध का आह्वान भी किया। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि वह सरकार के साथ सहयोग न करे और सरकारी सेवाओं, अदालतों सरकारी स्कूल-कॉलेजों, नगरपालिकाओं और विधानमंडलों का बहिष्कार करें, अर्थात् अरविंद घोष के शब्दों में “वर्तमान परिस्थितियों में प्रशासन चला सकना असंभव बना दें।” उग्र राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी और विभाजन-विरोधी आंदोलन को जन-आंदोलन बनाने की कोशिश की और विदेशी शासन से मुक्ति का नारा दिया। अरविंद घोष ने खुलकर घोषणा की कि “राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की प्राण वायु है।” इस तरह बंगाल के विभाजन का प्रश्न गौण हो गया और भारत की स्वतंत्रता का प्रश्न भारतीय राजनीति का केंद्रीय प्रश्न बन गया। उग्र राष्ट्रवादियों ने आत्मबलिदान का आह्वान भी किया कि इसके बिना कोई भी महान उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर भी यह बात याद रखनी चाहिए कि उग्र राष्ट्रवादी भी जनता को सकरात्मक नेतृत्व देने में असफल रहे। वे आंदोलन चलाने के लिए आवश्यक कुशल नेतृत्व और कुशल संगठन नहीं दे सके। उन्होंने जनता को जागृत तो कर दिया मगर यह नहीं समझ सके कि जनता की इस नई-नई निकली शक्ति का उपयोग कैसे करें या राजनीतिक संघर्ष के नए रूप क्या हों। निष्क्रिय प्रतिरोध और असहयोग विचार मात्र बनकर रह गए। वे देश की वास्तविक जनता, अर्थात किसानों तक पहुँचने में भी असफल रहे। उनका आंदोलन नगरों के निम्न और मध्य वगों तथा जमींदारी तक सीमित रहा। 1908 के अंत तक उनकी राजनीति एक बंद गली में समा चुकी थी। फलस्वरूप उन्हें दबाने में सरकार काफी हद तक सफल रही। उनका आंदोलन उनके प्रमुख नेता तिलक की गिरफ्तारी का तथा विपिनचंद्र पाल और अरविंद घोष द्वारा सक्रिय राजनीति से संन्यास का धक्का नहीं झेल सका। लेकिन राष्ट्रवादी भावनाओं का उभार दब न सका। जनता सदियों पुरानी नींद से जाग चुकी थी और राजनीतिक में निर्भीक तथा दिलेर रवैया अपनाना सीख चुकी थी। उसने आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ लिया था और जनता की लामबंदी तथा राजनीतिक कार्यवाही के नए रूपों को समझ लिया था। अब उसे एक नया आंदोलन उभरने की प्रतीक्षा थी। इसके अलावा अपने अनुभव से जनता ने कीमती सबक सीखे। गाँधीजी ने बाद में लिखा था कि ‘‘विभाजन के बाद जनता ने समझ लिया कि प्रार्थनापत्रों के पीछे कुछ शक्ति भी होनी चाहिए और यह कि उसे कष्ट उठाने में समर्थ बनना चाहिए।‘‘ वास्तव में विभाजन-विरोधी आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रवाद में एक महान और क्रांतिकारी परिवर्तन आया। बाद के राष्ट्रीय आंदोलन ने इस पूँजी का खूब उपयोग किया। क्रांतिकारी आंतकवाद का विकाससरकार का दमन और साथ में जनता को कुशल नेतृत्व देने में नेताओं की असफलता के कारण उपजी कुंठा जैसी बातों ने क्रांतिकारी आंतकवाद को जन्म दिया। बंगाल के युवकों ने देखा कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध और राजनीतिक कार्यवाही के सारे रास्ते बंद हैं। हताश होकर उन्होंने व्यक्तिगत बहादुरी के कार्यों और बम की राजनीति का सहारा लिया। अब उन्हें यह भरोसा नहीं रहा था कि निष्क्रिय प्रतिरोध से राष्ट्रवादी उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि बारीसाल सम्मेलन के बाद समाचारपत्र ‘युगांतर’ ने 22 अप्रैल 1906 को लिखा - ‘‘समस्या का समाधान जनता के अपने हाथों में है। उत्पीड़न के इस अभिशाप को रोकने के लिए भारत के तीस करोड़ लोगों को अपने 60 करोड़ हाथ ऊपर उठाने होंगे। ताकत का सामना ताकत से करना होगा।’’ लेकिन इन क्रांतिकारी युवकों ने जनक्रांति लाने की कोई कोशिश नहीं की। इसके बजाए उन्होंने आयरलैंड के आतंकवादियों और रूसी ध्वंसवादियों की विधियाँ अपनाने का फैसला किया कि अलोकप्रिय अधिकारियों का वध किया जाए। इस सिलसिले का आंरभ 1897 में ही हो चुका था जब चाफेकर भाइयों ने पूना में दो बदनाम ब्रिटिश अधिकारियों का वध कर डाला था। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने ‘‘अभिनव भारत’’ नाम से क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन बनाया था। 1905 के बाद अनेकों समाचारपत्र क्रांतिकारी आंतकवाद की पैरवी करने लगे थे। इनमें बंगाल के ’’संध्या‘‘ और ’’युगांतर‘‘ तथा महाराष्ट्र के ’’काल‘‘ सबसे प्रमुख थे।दिसंबर 1907 में बंगाल के लेफ्टिनेंट-गवर्नर को जान से मारने की कोशिश की गई। अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में एक बग्घी पर बम फेंका जिसमें वे समझते थे कि बदनाम जज, किंग्सफोर्ड बैठा है। बाद में प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को गोली मार ली, जबकि खुदीराम बोस पर मुकद्दमा चलाकर फाँसी दे दी गई। क्रांतिकारी आतंकवाद का आंदोलन अब आरंभ हो चुका था। आतंकवादी युवकों की अनेक गुप्त संस्थाएँ अब बन गई इनमें सबसे प्रमुख थी अनुशीलन समिति जिसके ढाका खंड की ही अकेली 500 शाखाएँ थीं। क्रांतिकारी आतंकवादी समितियाँ जल्द ही देश के दूसरे भागों में भी सक्रिय हो उठीं। उनका हौसला इतना बढ़ चुका था कि जब वायसराय लार्ड हार्डिग्ज दिल्ली में एक सरकारी जुलूस में हाथी पर बैठा था तब उस पर भी उन्होंने बम फेंका। इस हमले में वायसराय घायल हो गया। क्रांतिकारियों ने अपनी गतिविधियों के केंद्र विदेशों में भी खोले। इसकी पहल लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा. विनायक दामोदर सावरकर और हरदयाल ने की जबकि यूरोप में उनके प्रमुख नेता मादाम भीखाजी कामा और अजीतसिंह थे। आतंकवादी आंदोलन भी धीरे-धीरे ठंडा पड़ गया। वास्तव में एक राजनीतिक अस्त्र के रूप में आतंकवाद की असफलता निश्चित थी। इसने जनता को गतिमान नहीं बनाया और वास्तव में जनता में इसका कोई आधार न था। लेकिन भारत में राष्ट्रवाद के विकास में आतंकवादियों का बहूमूल्य योगदान रहा है। जैसा कि एक इतिहासकार ने कहा हे, “उन्होंने हमें अपने मनुजत्व पर गर्व करना फिर से सिखाया।” हालाँकि राजनीतिक रूप से चेतन अधिकांश लोग आतंकवादियों के राजनीतिक दृष्टिकोण से सहमत न थे, फिर भी ये आतंकवादी अपनी वीरता के कारण अपने देशवासियों में बेहद लोकप्रिय हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (1905-1914)बंग-भंग विरोधी आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा। विभाजन का विरोध करने के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी भाग एक हो गए। 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष गोखले ने विभाजन की और कर्जन के प्रतिक्रियावादी शासन की खुलकर निंदा की। राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल के स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का भी समर्थन किया।नरमपंथी व गरमपंथी राष्ट्रवादियों के बीच जमकर सार्वजनिक बहसें हुईं और मतभेद उभरे। गरमपंथी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल से बाहर देश में भी फैलाया तथा औपनिवेशिक सरकार के साथ किसी भी रूप में जुड़ने का बहिष्कार करना चाहते थे। नरमपंथी बहिष्कार को बंगाल तक और वहाँ भी केवल विदेशी मालों तक सीमित रखना चाहते थे। उस साल राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष-पद के लिए दोनों दलों में रस्साकशी हुई। अंत में समझौता दादा भाई नौरोजी के नाम पर हुआ जिन्हें सभी राष्ट्रवादी एक महन देशभक्त मानते थे। दादा भाई ने अपने अध्यक्षीय भाषण में घोषणा की कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य “ग्रेट ब्रिटेन या उपनिवेशों की तरह का स्वशासन या स्वराज्य है।” इस घोषणा ने राष्ट्रवादियों में बिजली की लहर सी दौड़ा दी। लेकिन राष्ट्रवादी आंदोलन के दोनों भागों के मतभेदों को बहुत समय तक दबाकर नहीं रखा जा सका। अनेक नरमपंथी राष्ट्रवादी घटनाओं के साथ ताल-मेल बिठाकर नहीं चल सके। वे यह नहीं समझ सके कि उनके जिस दृष्टिकोण और जिन विधियों ने पीछे एक ठोस लक्ष्य प्राप्त किया था, अब आगे के लिए पर्याप्त नहीं रह गए थे। वे राष्ट्रीय आंदोलन के नए चरण तक नहीं पहुँच सके। दूसरी ओर उग्र राष्ट्रवादियों को रोका जाना पसंद न था। अंत में दिसंबर 1907 में सूरत अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए। नरमपंथी नेता कांग्रेस संगठन पर कब्जा करने तथा उससे गरमपंथियों को निष्कासित करने में सफल रहे। लेकिन अंततः इस विभाजन से लाभ किसी भी दल को नहीं हुआ। नरमपंथी नेताओं का राष्ट्रवादियों की नई पीढ़ियों से संपर्क टूट गया। ब्रिटिश सरकार ने भी “बाँटों और राज करो” का खेल खूब खेला। उन्होंने गरमपंथी राष्ट्रवादियों का दमन किया तथा इसके लिए उन्होंने नरमपंथी राष्ट्रवादियों को अपने पक्ष में लाने का प्रयत्न किए। नरमपंथी राष्ट्रवादियों को खुश करने के लिए उन्होंने 1909 के इंडियन कौंसिल्स एक्ट के रूप में सांविधानिक सुधारों की घोषणा की, इसी कानून को 1909 के मार्ले-मिण्टों सुधारों के नाम से भी जाना जाता है। 1911 में सरकार ने बंगाल का विभाजन समाप्त कर देने की घोषणा भी की। पश्चिमी और पूर्वी बंगाल फिर से मिला दिए गए तथा बिहार और उड़ीसा नाम से दो प्रांत इससे अलग बना दिए गए। इसी के साथ केंद्र सरकार की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली लाई गई। मार्ले-मिंटों सुधारों में इंपीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल और प्रांतीय परिषदों में चुने हुए सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। लेकिन ऐसे अधिकांश सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होना था, अर्थात् इंपीरियल कौंसिल के मामले में प्रांतीय परिषदों के द्वारा और प्रांतीय परिषदों के मामले में नगरपालिकाओं और जिला परिषदों द्वारा चुने हुए सदस्यों में कुछ सीटें जमींदारों और भारत में रह रहे ब्रिटिश पूँजीपतियों के लिए आरक्षित थीं। उदाहरण के लिए, इंपीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल के 68 सदस्यों में 36 अधिकारी होते और 5 ऐसे नामजद सदस्य होते जो अधिकारी न हों। शेष 27 सदस्य चुने हए होते जिनमें 6 बड़ें जमींदारों के और 2 ब्रिटिश पूँजीपतियों के प्रतिनिधि होते। इसके अलावा, सुधार के बाद भी ये परिषदें वास्तविक शक्ति से वंचित होतीं और केवल सलाहकार समितियों का काम करतीं। इन सुधारों से ब्रिटिश शासन के लोकतंत्र-विरोधी और विदेशी चरित्र में या विदेशियों द्वारा देश के आर्थिक शोषण में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। वास्तव में भारतीय प्रशासन को लोकतांत्रिक स्वरूप देना उनका उद्देश्य था ही नहीं। इस समय मार्ले ने खुलकर कहा कि “अगर यह कहा जा रहा हो कि वर्तमान सुधार प्रत्यक्ष या अनिवार्य रूप से भारत में एक संसदीय प्रणाली की स्थापना की ओर हमें ले जाएगे, तो कम से कम मेरा इनसे कुछ भी लेना-देना नहीं होगा” भारत-सचिव के रूप में उसका स्थान लेने वाले लार्ड क्रेव ने 1912 में स्थिति और भी साफ कर दी - “भारत मे एक वर्ग ऐसा है जो स्वशासन की आशा लिए हुए है जैसा कि दूसरे डोमिनियनों को दी गई है। मैं भारत के लिए इस तरह का कोई भविष्य नहीं देखता।” 1905 के सुधारों का वास्तविक उद्देश्य नरमपंथियों को भ्रमित करना, राष्ट्रवादियों में फूट डालना और भारतीय के बीच एकता को बढ़ने से रोकना था। इन सुधारों ने अलग-अलग चुनाव मंडलों की प्रणाली भी आरंभ की। इसमें सभी मुसलमानों को मिलाकर उनके अलग चुनाव क्षेत्र बनाए गए थे और इन क्षेत्रों से केवल मुसलमान ही चुने जा सकते थे। यह काम अल्पसंख्यक मुस्लिम संप्रदाय की सुरक्षा के नाम पर किया गया, पर वास्तव में यह हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने और भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने की नीति का ही अंग था। अलग-अलग चुनाव मंडलों की यह प्रणाली इस धारणा पर आधारित थी कि हिंदुओं और मुसलमानों के राजनीतिक और आर्थिक हित अलग-अलग हैं। यह एक अवैज्ञानिक धारणा थी, क्योंकि धर्म कभी राजनीतिक या आर्थिक हितों का या राजनीतिक संगठन का आधार नहीं हो सकता। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रणाली के व्यवहार में बहुत घातक परिणाम निकले। इसने भारत के एकीकरण की निरंतर ऐतिहासिक प्रक्रिया में बाधा खड़ी की। यह प्रणाली देश में हिंदू और मुस्लिम, दोनों तरह की सांप्रदायिकता के विकास का प्रमुख कारण सिद्ध हुई। मध्यवर्गीय मुसलमानों के शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने तथा इस प्रकार उनको भारतीय राष्ट्रवाद की मुख्य धारा में शामिल करने के बजाए अलग-अलग चुनाव मंडलों की इस प्रणाली ने विकसित होते हुए राष्ट्रवादी आंदोलन से उनके अलगाव को और स्थायी बनाया। इससे अलगाववादी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। इसने हिंदू-मुसलमान, सभी भारतीयों की साझी आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से लोगों को रोका। नरमपंथी राष्ट्रवादियों ने मार्ले-मिंटो सुधारों को पूरा समर्थन नहीं दिया। जल्द ही उन्हें लगने लगा कि इन सुधारों से बहुत अधिक कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी सुधारों को लागू कराने के लिए उन्होंने सरकार से सहयोग का निर्णय किया। सरकार से यह सहयोग और उग्र राष्ट्रवादियों के कार्यक्रम का विरोध उनके लिए बहुत महँगा सिद्ध हुआ। धीरे-धीरे जनता में उनकी प्रतिष्ठा और समर्थन कम होते गए और वे एक मामूली से राजनीतिक समूह बनकार रह गए। संप्रदायवाद का विकाससंप्रदायवाद मूल रूप से एक विचारधारा है। सांप्रदायिक दंगे इस विचारधारा के अनेक परिणामों में से केवल एक परिणाम हैं। संप्रदायवाद इस विश्वास का नाम है कि चूँकि कुछ लोग किसी एक विशेष धर्म को मानते हैं, इसलिए उनके पार्थिव आर्थात् सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हित भी समान होते हैं। यह इस विश्वास का नाम है कि भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई अलग-अलग और विशिष्ट समुदाय हैं कि किसी धर्म के मानने वालों के धार्मिक हित ही नहीं बल्कि पार्थिव हित भी समान होते हैं कि भारतीय राष्ट्र नाम की कोई वस्तु न है और न हो सकती है बल्कि इसके बजाए यहाँ केवल हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, आदि हैं कि भारत उपरोक्त कारण से धार्मिक समुदाय का एक महासंघ मात्र है। संप्रदायवाद में यह दूसरी धारणा भी निहित है कि किसी धर्म के अनुयायियों के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक हित किसी दूसरे धर्म के मानने वालों के हितों के भिन्न होते हैं। संप्रदायवाद का तीसरा चरण तब आरंभ होता है जब विभिन्न धर्मों के अनुयायियों या विभिन्न धार्मिक ‘समुदायों’ के हितों को परस्पर विरोधी और शत्रुतापूर्ण समझा जाने लगता है। इस चरण में संप्रदायवादी यह दावा करते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों के पार्थिव हित समान नहीं हो सकते और उनके पार्थिव हितों का एक दूसरे से टकराना निश्चित है।यह बात सही नहीं है कि संप्रदायवाद मध्य काल का अवशेष है या तब से चला आ रहा है। हालाँकि धर्म लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है और धर्म को लेकर कभी-कभी वे झगड़ते भी रहे हैं, फिर भी 1870 के दर्शक के पहले तक शायद ही किसी सांप्रदायिक विचारधारा और सांप्रदायिक राजनीति का अस्तित्व रहा हो। संप्रदायवाद एक आधुनिक प्रवृत्ति है। इसकी जड़ें आधुनिक औपनिवेशिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना में निहित हैं। संप्रदायवाद का उदय जनता और उसकी भागीदारी पर आधारित एक नई, आधुनिक राजनीति का परिणाम है। इसके कारण जनता से व्यापक संबंध बनाने और उसकी आस्था जीतने तथा नई पहचान कायम करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। यह प्रक्रिया अनिवार्यता कठिन, धीमी और जटिल रही। इस प्रक्रिया के लिए राष्ट्र, वर्ग और सांस्कृतिक भाषायी पहचानों के आधुनिक विचारों का उदय और प्रसार आवश्यक था। नई और अपरिचित होने के कारण ये नई पहचाने भी धीमे-धीमे और उतार-चढ़ाव के साथ विकसित हुई। अक्सर-बेश्तर लोग नई वास्तवकिता को समझने, व्यापक संबंध बनाने और नई पहचानें कायम करने के लिए जाति, स्थान, पंथ और धर्म की पुरानी और परिचित पहचानों का उपयोग करते रहे। ऐसा पूरी दुनिया मे हुआ है। लेकिन धीरे-धीरे राष्ट्र जातीयता और वर्ग की नई, आधुनिक और ऐतिहासिक रूप से आवश्यक पहचानें स्थापित हुई हैं। दुर्भाग्य से भारत में अनेक दशकों के बाद भी यह प्रक्रिया अभी तक अधूरी है क्योंकि, जैसा कि कहा जा चुका है, भारत पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से एक निर्माणधीन राष्ट्र ही बना रहा है। खासकर धार्मिक चेतना देश के कुछ भागों और जनता के कुछ वर्गों में सांप्रदायिक चेतना बनकर रह गई है। प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों हुआ। आधुनिक राजनीतिक चेतना खास तौर पर मुसलमानों मे देर से विकसित हुई। निम्न मध्य वर्ग के हिंदुओं और पारसियों में राष्ट्रवाद का प्रसार तो हुआ पर उसी वर्ग के मुसलमानों में वह उतनी तेजी से नहीं बढ़ सका। जैसा कि हम देख आए हैं, 1857 के विद्रोह में हिंदू-मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। वास्तव में विद्रोह को कुचलने के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने मुसलमानों से खास तौर पर बदला चुकाया था। अकेले दिल्ली में 27,000 मुसलमान फाँसी से लटका दिए गए थे। इसके बाद से मुसलमानों को लगातार शंका की दृष्टि से देखा जाता रहा, पर 1870 के दशक में इस दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। राष्ट्र वादी आंदोलन के उदय के कारण ब्रिटिश राजनेता भारत में अपने साम्राज्य की सुरक्षा के प्रति चिंतित हो उठे। देश में एकजुट राष्ट्रीय भावना के विकास को रोकने के लिए उन्होंने “बाँटों और राज करो” की नीति पर और भी सक्रियता के काम करने और जनता को धार्मिक आधारों पर बाँटने का, अर्थात् दूसरे शब्दों में भारत की राजनीति में सांप्रदायिक और अलगाववादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने का फैसला किया। इस कारण से उन्होंने मुसलमानों के ‘मसीहा’ के रूप में सामने आने तथा मुसलमान जमींदारों, भूस्वामियों और नवशिक्षित वर्गों को अपनी तरफ खींचने का फैसला किया। उन्होंने भारतीय समाज में दूसरी तरह की फूटें भी डालीं। बंगाली वर्चस्व का नाम ले-लेकर उन्होंने प्रांतवाद को हवा दी। अब्राह्मणों और ब्राह्मणों और निचली जातियों को ऊँची जातियों के खिलाफ खड़ा करने के लिए उन्होंने जाति-प्रथा का इस्तेमाल करने की कोशिशें भी कीं। संयुक्त प्रांत और बिहार में हिंदू और मुसलमान हमेशा से शांतिपूर्वक रहते आए थे। वहाँ उन्होंने राजभाषा के पद से उर्दू को हटाकर हिंदी को दिए जाने के आंदोलन को खुलकर प्रोत्साहन दिया। दूसरे शब्दों में, भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों की उचित माँगों का भी भारतीय जनता में फूट डालने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। औपनिवेशिक सरकार ने हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों को अलग-अलग समुदाय माना। उन्होंने सांप्रदायिक नेताओं को उनके सहधर्मियों के वास्तविक प्रतिनिधि मानने में कोई देर नहीं लगाई। उन्होंने प्रेस, पुस्तिकाओं, पोस्टरों, साहित्य और सार्वजनिक मंचों से जहरीले सांप्रदायिक विचार और सार्वजनिक घृणा फैलाने की पूरी छूट दी। राष्ट्र वादी समाचारपत्रों और लेखकों, आदि को जिस तरह अक्सर उत्पीड़ित किया जाता था, यह बात उसके ठीक विपरीत थी। धार्मिक अलगाववाद की प्रवृत्ति के विकास में सैयद अहमद खान की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सैयद अहमद खान एक महान शिक्षाशास्त्री और समाज-सुधारक थे, मगर अपने जीवन के अंतिम दिनों में वे रुढ़िवादी विचारों के हो गए थे। 1880 के दशक में अपने विचारों को छोड़कर उन्होंने घोषणा की कि हिंदुओं और मुसलमानों के राजनीतिक हित समान न होकर भिन्न-भिन्न बल्कि एकदम अलग-अलग हैं और इस प्रकार उन्होंने मुस्लिम सांप्रदायिकता की नींव डाली। उन्होंने ब्रिटिश शासन के प्रति पूर्ण भक्ति का उपदेश भी दिया। 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उन्होंने उसका विरोध करने का और बनारस के राजा शिवप्रसाद के साथ मिलकर ब्रिटिश राज्य के प्रति वफादारी का आंदोलन चलाने का निश्चय किया। वे अब ये भी कहने लगे कि चूँकि हिंदू भारतीय जनता का बहुमत भाग है इसलिए ब्रिटिश शासन के कमजोर पड़ने या समाप्त होने पर वे मुसलमानों को दबाकर रखेंगे। उन्होंने मुसलमानों से आग्रह किया कि वे बदरुद्दीन तैयबजी की कांग्रेस में शामिल होने की अपील पर कोई ध्यान न दें। ये विचार निःसंदेह अवैज्ञानिक और वास्तविकता से दूर थे। हिंदू और मुसलमान अलग-अलग धर्मों को मानते अवश्य थे, फिर भी इसके कारण उनके आर्थिक और राजनीतिक हित अलग-अलग न थे। भाषा, संस्कृति, जाति, वर्ग, सामाजिक स्थिति, खान-पान और वस्त्र-परिधान, सामाजिक कृत्यों, आदि में हिंदू अपने साथी हिंदुओं से और मुसलमान दूसरे मुसलमानों से अलग थे। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी हिंदू और मुसलमान जनता तथा वर्गों ने समान जीवन-प्रणालियाँ विकसित कर ली थीं। एक बंगाली मुसलमान और एक पंजाबी मुसलमान की तुलना में एक बंगाली मुसलमान और एक बंगाली हिंदू में बहुत सी बाते सांझा थीं। इसके अलावा ब्रिटिश साम्राज्यवाद हिंदू-मुसलमान दोनों का बराबर और मिलकर दमन और शोषण कर रहा था। यहाँ तक कि 1884 में सैयद अहमद खान ने भी लिखा था - क्या आप एक ही देश में नहीं रहते ? क्या आप एक ही धरती पर जलाएँ और दफनाएँ नहीं जाते ? क्या आप एक ही जमीन पर नहीं चलते या एक ही धरती पर नहीं रहते ? याद रखिए कि हिंदू और मुसलमान शब्द केवल धार्मिक अंतर के लिए है, वर्ना सभी लोग, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, बल्कि इस देश में रहने वाले ईसाई भी, इस खास अर्थ में एक ही राष्ट्र के सदस्य हैं। इसलिए इन सभी विभिन्न मतों को एक राष्ट्र कहा जा सकता है और इसलिए देश के, जो सबका देश है, उसके भले के लिए एक-एक व्यक्ति को एकता के सूत्र में बँध जाना चाहिए। तो प्रश्न यह है - मुसलमानों मे सांप्रदायिक और अलगाववादी विचार- प्रवृत्ति कैसे विकसित हुई ? कुछ हद तक इसका कारण शिक्षा, व्यापार और उद्योग में मुसलमानों का तुलनात्मक पिछड़ापन था। मुस्लिम उच्च वर्गों में अधिकांशतः जमींदार और अभिजात लोग थे। चूँकि 19वीं सदी के पहले 70 वर्षां में उच्च वर्ग के मुसलमान बहुत ब्रिटिश-विरोधी, रूढ़िवादी और आधुनिक शिक्षा के दुश्मन थे, इसलिए देश में शिक्षित मुसलमानों की संख्या बहुत कम रही। फलस्वरूप आधुनिक पश्चिमी विचार जिनका विज्ञान, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद पर था, मुसलमान बुद्धिजीवियों में नहीं फैले और वे परंपरा के दास और पिछड़े बन रहे। बाद में सैयद अहमन खान, नवाब अब्दुल लतीफ, बदरूद्दीन तैयबजी और दूसरे लोगों के प्रयासों के कारण मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ। लेकिन मुसलमानों में शिक्षित लोगों का भाग हिंदुओं, पारसियों और ईसाइयों से बहुत कम रहा। इसी तरह उद्योग-व्यापार के विकास में भी मुसलमानों का बहुत कम हाथ रहा था। मुसलमानों में शिक्षितों, उद्योगपतियों और व्यापारियों की कम संख्या के कारण प्रतिक्रियावादी बड़े जमींदार मुस्लिम जनता पर अपना प्रभाव बनाए रखने में सफल रहे। जैसा कि हम देख चुके हैं, भूस्वामी और जमींदार चाहे हिंदू हों या मुसलमान, अपने स्वार्थ के कारण ब्रिटिश शासन का समर्थन करते थे, पर हिंदुओं में आधुनिक बुद्धिजीवियों तथा उभरते हुए व्यापारी और उद्योगपति वर्ग ने जमींदारों से नेतृत्व छीन लिया था। दुर्भाग्य से मुसलमानों की स्थिति इसके ठीक विपरीत रही। मुसलमानों के शैक्षिक पिछड़ेपन का एक और घातक परिणाम हुआ। चूँकि सरकारी नौकरियों या व्यवसायों के लिए आधुनिक शिक्षा आवश्यक थी, इसलिए इन क्षेत्रों में भी मुसलमान दूसरो से पीछे रहे। इसके अलावा मुसलमानों को 1857 की बगावत के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार मानकर सरकार उनके खिलाफ 1858 से ही जान-बूझकर भेदभाव करती आ रही थी। जब मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा कुछ फैली भी, तब भी एक शिक्षित मुसलमान के सामने व्यवसाय या व्यापार के बहुत कम अवसर थे। तब वह अनिवार्य रूप से सरकारी नौकरी का मुँह देखता था और कुछ भी हो, एक पिछड़ा उपनिवेश होने के कारण भारत में जनता के लिए रोजगार के बहुत कम अवसर थे। इन हालात में ब्रिटिश अधिकारियों और जी-हुजूर मुसलमान नेताओं के लिए शिक्षित मुसलमानों को शिक्षित हिंदुओं के खिलाफ भड़काना बहुत आसान था। सैयद अहमद खान और दूसरों ने यह माँग उठाई कि सरकारी नौकरियों में मुसलमानों के साथ खास व्यवहार किया जाए। उन्होंने ऐलान किया कि अगर शिक्षित मुसलमान ब्रिटिश शासन के वफादार रहें तो सरकार नौकरियों तथा दूसरी विशेष कृपाओं के रूप में उन्हें इसका समुचित पुरस्कार देगी। कुछ जी-हुजूर हिंदू और पारसी भी इसी तरह के तर्क देने की कोशिश करते थे, मगर वे हमेशा मामूली अल्पमत में बने रहे। नतीजा यह हुआ कि जब पुरे देश के पैमाने पर स्वतंत्र और राष्ट्रवादी वकील, पत्रकार, छात्र, व्यापारी और उद्योगपति राजनीतिक नेता बन रहे थे तब भी मुसलमानों में वफादार जमींदार और सेवानिवृत सरकारी नौकर ही राजनीतिक जनमत को प्रभावित करते रहे। बंबई वह पहला प्रांत था जहाँ बहुत पहले ही मुसलमानों ने व्यापार और शिक्षा को अपनाया था और वहाँ राष्ट्रीय कांग्रेस की कतारों में बदरुद्दीन तैयबजी, आर. एम. सयानी, ए. भीमजी और युवा वकील मुहम्मद अली जिन्ना जैसे प्रतिभाशाली मुसलमान मौजूद थे। समस्या के इस पक्ष को संक्षेप में सामने रखने के लिए हम जवाहरलाल नेहरु की पुस्तक “भारत एक खोज” से एक उद्धरण देते हैं - हिंदु और मुसलमान मध्य वर्गों के विकास में एक पीढ़ी या इससे कुछ अधिक समय का अंतर रहा है और यह अंतर आज भी अनेक राजनीतिक, आर्थिक और दूसरी दिशाओं में दिखाई दे रहा है। यही वह पिछड़ापन है जो मुसलमानों में भय की मानसिकता पैदा करता है। इतिहास का छात्र होने के नाते हमें यह भी जानना चाहिए कि उन दिनों स्कूलों और कॉलेजों में जिस तरह से भारतीय इतिहास की शिक्षा दी जाती थी उसके कारण भी शिक्षित हिंदुओं और मुसलमानों में सांप्रदायिक भावनाओं का विकास हुआ। ब्रिटिश इतिहासकारों और उनका अनुकरण करने वाले भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास के मध्य काल को मुस्लिम काल कहा तुर्क, अफगान और मुगल शासकों के शासन को मुस्लिम शासन कहा गया। मुस्लिम जनता भी हिंदू जनता जितनी ही पीड़ित और करों के बोझ से दबी थी और दोनों को शासक, दरबारी, सरदार और जमींदार, चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान, एक समान अपमान की दृष्टि से देखते थे तथा उन्हें कीड़े-मकोड़े समझते थे, फिर भी इन लेखकों ने ऐलान किया कि मध्यकालीन भारत में सारे मुसलमान शासक थे और सारे ही गैरमुसलमान शासित थे। वे यह बात सामने न ला सके कि हर जगह की तरह भारत में भी प्राचीन और मध्यकालीन युग में राजनीति का आधार आर्थिक और राजनीतिक हित थे, न कि धार्मिक विचार। शासकों और विद्रोहियों दोनों ने धर्म का उपयोग अपने भौतिक हितों और महत्वाकांक्षाओं को छिपाने के लिए एक बाहरी खोल के रूप में किया। इसके अलावा ब्रिटिश और सांप्रदायिक इतिहासकारों ने भारत मे एक समन्वित संस्कृति की धारणा पर भी चोट की। निश्चित ही भारत में अनेकों प्रकार की संस्कृतियाँ मौजूद थीं। लेकिन इस विविधता का कोई धार्मिक आधार न था। किसी एक क्षेत्र के लोगों तथा एक ही क्षेत्र के उच्च और निम्न वर्गों के साझे सांस्कृतिक आचार-विचार होते थे। फिर भी सांप्रदायिक इतिहासकारों का दावा था कि भारत में हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों का अलग-अलग अस्तित्व है। इतिहास के प्रति हिंदू सांप्रदायिक दृष्टिकोण इस भ्रामक धारणा का भी सहारा होता था कि भारतीय समाज और संस्कृति प्राचीन काल में महानता और आदर्श की ऊँचाइयों पर विराजमान थी, पर मध्य काल में ‘मुस्लिम’ शासन और प्रभुत्व के कारण उसका निरंतर पतन आरंभ हो गया। भारतीय अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी, धर्म और दर्शन, कला और साहित्य, संस्कृति और समाज, फलों, सब्जियों और वस्त्रों में मध्य काल का जो भी बुनियादी योगदान था, उसे नकारा जाने लगा। इस बात के अनेक समकालीन प्रेक्षकों ने देखा-समझा। उदाहरण के लिए, गाँधीजी लिखते हैं - “जब तक स्कूलों और कॉलेजों में इतिहास की पाठ्यपुस्तकों के द्वारा अत्यंत विकृत इतिहास पढ़ाया जाता है तब तक सांप्रदायिक सद्भाव स्थायी रूप से स्थापित नहीं हो सकता।” साथ ही, इतिहास के प्रति सांप्रदायिक दृष्टिकोण को कविता, नाटकों, ऐतिहासिक उपन्यासों और कहानियों, समाचार पत्रों व लोकप्रिय पत्रिकाओं, बच्चों की पत्रिकाओं, पुस्तिकाओं और सबसे बढ़कर सार्वजनिक मंचों से मौखिक रूप से, कक्षाओं में अध्यापन, परिवार द्वारा होने वाले समाजीकरण तथा आपसी बातचीत के द्वारा भी व्यापक रूप से प्रचारित किया गया। भारतीय राष्ट्रवाद के निर्माताओं ने इस बात को अच्छी तरह से समझा कि एक राष्ट्र के रूप में भारतीयों को ढ़ालना एक धीमा और कठिन काम है और इसके लिए जनता को लंबे समय तक राजनीतिक शिक्षा देनी होगी। इसलिए उन्होंने अल्पसंख्यकों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि राष्ट्रवादी आंदोलन सभी भारतीयों को साझे राष्ट्रीय, आर्थिक और राजनीतिक हितों के आधार पर एकताबद्ध करने का प्रयास करते हुए उनके धार्मिक और सामाजिक अधिकारों की सावधानीपूर्वक रक्षा करेगा। राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए दादा भाई नौरोजी ने स्पष्ट आश्वासन दिया कि कांग्रेस केवल राष्ट्रीय प्रश्न उठाएगी और धार्मिक तथा सामाजिक मामलों में दखल नहीं देगी। 1889 में कांग्रेस ने यह सिद्धांत स्वीकार किया कि अगर किसी प्रस्ताव को कांग्रेस के मुस्लिम प्रतिनिधियों का बहुमत मुसलमानों के लिए हानिकारक समझता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के आरंभिक वर्षों में अनेकों मुसलमान इसमें शामिल हुए। दूसरे शब्दों में, यह समझाकर कि राजनीति का आधार धर्म और समुदाय नहीं होने चाहिए, आरंभिक राष्ट्रवादियों ने जनता के राजनीतिक दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने की कोशिश की। दुर्भाग्य से उग्र राष्ट्रवाद जहाँ सभी दूसरी बातों में आगे की ओर बढ़ा हुआ एक कदम था, वहीं राष्ट्रीय एकता के विकास की दृष्टि से यह एक पिछड़ा हुआ कदम था। कुछ उग्र राष्ट्रवादियों के भाषण और लेखन धार्मिक और हिंदू रंगत में रंगे हुए होते थे। उन्होंने मध्यकालीन भारतीय संस्कृति को नकारकर प्राचीन भारतीय संस्कृत पर जोर दिया। उन्होंने भारतीय संस्कृति और भारतीय राष्ट्र को हिंदू धर्म और हिंदुओं से जोड़ा उन्होंने समन्वित संस्कृति के तत्वों को छोड़ने के प्रयत्न किए। उदाहरण के लिए, तिलक ने शिवाजी और गणपति उत्सवों का प्रचार किया, अरविंद घोष ने अर्धरहस्यवादी ढंग से भारत को माता और राष्ट्रवाद को धर्म बतलाया, आतंकवादी देवी काली के आगे शपथ लेते थे और बंगाल-विभाजन-विरोधी आंदोलन का आरंभ गंगा में डुबकियाँ लगाकर किया गया। ये बातें शायद ही मुसलमानों को पसंद आतीं। वास्तव में, ऐसे काम उनके धर्म के विपरीत थे और यह आशा नहीं की जा सकती थी कि वे मुसलमान होते हुए भी इन या ऐसी दूसरी गतिविधियों से अपने को जोड़ें। मुसलमानों से यह आशा भी नहीं की जा सकती थी कि वे शिवाजी और प्रताप का गुणगान उनकी ऐतिहासिक भूमिकाओं के कारण नहीं, बल्कि ‘विदेशियों’ के खिलाफ लड़ने वाले ‘राष्ट्रीय’ नायकों के रूप में किया जाता देखें और उत्साह के साथ वही काम स्वयं करें। अगर किसी का मुसलमान होना ही उसे विदेशी कहने का आधार न हो तो अकबर या औरंगजेब को किसी भी तरह विदेशी नहीं कहा जा सकता। वास्तव में, आवश्यकता इस बात की थी कि प्रताप और अकबर या शिवाजी और औरंगजेब की लड़ाई को उसकी विशिष्ट ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में एक राजनीतिक संघर्ष के रूप में देखा जाए। अकबर और औरंगजेब को ‘विदेशी’ कहने तथा प्रताप और शिवाजी को ‘राष्ट्रीय’ नायक का दर्जा देने का मतलब यह है कि हम बीसवीं सदी के भारत में प्रचलित सांप्रदायिक दृष्टिकोण को पीछे के इतिहास पर लागू कर रहे हैं। यह एक विकृति इतिहास ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता के लिए धक्का भी था। इसका मतलब यह नहीं है कि उग्र राष्ट्रीयवादी मुस्लिम विरोधी या पूरी तरह संप्रदायवादी थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। तिलक समेत उनमें से अधिकांश हिंदू-मुस्लिम एकता के समर्थक थे। उनमें से अधिकांश के लिए मातृभूमि या भारत-माता की धारणा एक आधुनिक धारणा थी जिसका धर्म से कोई संबंध न था। उनमें से अधिकांश का राजनीतिक चिंतन अतीत के मोह में ग्रस्त न होकर आधुनिक था। आर्थिक बहिष्कार का उनका प्रमुख राजनीतिक अस्त्र और उनका राजनीतिक संगठन, दोनों वास्तव में बहुत आधुनिक थे उदाहरण के लिए, 1916 में तिलक ने घोषणा की कि ’’जो भी इस देश की जनता की भलाई का काम करता है वह चाहे मुसलमान हो या अंग्रेज, विदेशी नहीं है। ’विदेशीपन‘ का संबंध हितों से है। विदेशीपन का संबंध निश्चित ही गोरी या काली चमड़ी से या धर्म से नहीं है।‘‘ यहाँ तक कि क्रांतिकारी आंतकवादी भी आयरलैंड, रूस या इटली जैसे यूरोपीय देशों के क्रांतिकारी आंदोलनों से प्रभावित थे, न कि काली-पूजा या भवानी-पूजा से, पर जैसा कि पहले कहा जा चुका है उग्र राष्ट्रवादियों के राजनीतिक कार्यो और विचारों की कुछ-कुछ हिंदू रंगत हुआ करती थी। यह बात खास तौर पर हानिकारक सिद्ध हुई क्योंकि चालाक ब्रिटिश और ब्रिटिश - समर्थक प्रचारकों ने इस हिंदू रंगत का लाभ उठाकर मुसलमानों के मन में जहर भरा। नतीजा यह हुआ कि शिक्षित मुसलमान बड़ी संख्या में उभरते राष्ट्रवादी आंदोलन से अलग रहे या उसके शत्रु बन गए। इस तरह वे आसानी से अलगाववादी दृष्टिकोण के शिकार हो गए। इस हिंदू रंगत ने हिंदू साम्प्रदायवाद को भी वैचारिक सहारा दिया और राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए अपने बीच से हिंदू-सांप्रदायिक राजनीति और विचारधारा के तत्वों का विनाश कर सकना कठिन हो गया। इससे मुस्लिम राष्ट्रवादियों पर एक मुस्लिम रंगत भी चढ़ी। तो भी वकील अब्दुर्रसूल और हसरत मोहानी जैसे प्रगतिशील मुस्लिम बुद्धिजीवी स्वदेशी आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद क्रांतिकारी आंतकवादियों में शामिल हुए और मुहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के प्रमुख युवक नेताओं में से एक के रूप में विख्यात हुए। इसका कारण यह था कि राष्ट्रीय आंदोलन दृष्टिकोण व विचारधारा में मूलतः धर्मनिरपेक्ष ही बना रहा। जब गाँधी जी, चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहर लाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, एम. ए. अंसारी, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, सुभास चंद्र बोस, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जैसे नेता सामने आए तो यह धर्मनिरपेक्षता और भी मजबूत हुई। देश के आर्थिक पिछड़ेपन ने भी, जो औपनिवेशिक अल्प विकास की देन था, संप्रदायवाद के उदय में सहायता की। आधुनिक औधोगिक विकास के अभाव में बेरोजगारी भारत में और खासकर शिक्षित लोगों के लिए एक तीखी समस्या बन गई। नतीजा यह हुआ कि जो भी नौकरियाँ थीं उनके लिए प्रतियोगिता बहुत कड़ी थी। दूरदृष्टि रखने वाले भारतीयों ने इस बीमारी को पहचाना और एक ऐसी आर्थिक-राजनीतिक प्रणाली के लिए कार्यरत रहे जिसमें देश का आर्थिक विकास हो और रोजगार की कोई कमी न रहे। लेकिन दूसरे बहुत से लोगों ने इसके लिए नौकरियों में संप्रदाय, प्रांत या जाति के आधार पर आरक्षण जैसे अल्पदर्शी और अल्पावधि वाले हल सुझाए। रोजगार के उपलब्ध और सीमित अवसरों से एक बड़ा हिस्सा पाने के लिए उन्होंने सांप्रदायिक और धार्मिक भावनाएँ तथा बाद में जातिगत और प्रांतीय भावनाएँ भी भड़काने की कोशिशें कीं। जो लोग हताश होकर रोजगार ढूँढ़ रहे थे उनके लिए ऐसे संकुचित विचारों के प्रति कुछ तात्कालिक आकर्षण अवश्य था। इस स्थिति में सांप्रदायिक हिंदू-मुसलमान नेताओं, जातियों के नेताओं और ‘बाँटों तथा राज करो’ की नीति चलाने वाले अधिकारीगण को कुछ सफलता अवश्य मिली। अनेक हिंदू हिंदुराष्ट्रवाद की और अनेक मुसलमान मुस्लिम राष्ट्रवाद की बातें करने लगे। राजनीतिक रूप से अपरिपक्व लोग यह नहीं समझ सके, कि उनकी आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक कठिनाइयाँ विदेशी शासन में उनकी साझी पराधीनता और आर्थिक पिछड़ेपन की उपज थीं और यह कि केवल साझे प्रयासों के द्वारा ही वे देश को मुक्त कर सकते हैं, उसका आर्थिक विकास कर सकते हैं और इस तरह बेरोजगारी जैसी साझी समस्याओं को हल कर सकते हैं। कुछ लोगों का मत है कि सांप्रदायिकता के विकास का एक प्रमुख कारण यह है कि देश में अनेक धर्म मौजूद हैं। ऐसा नहीं है। किसी बहुधार्मिक समाज में सांप्रदायिकता का विकास अनिवार्य है, यह बात सही नहीं है। यहाँ हमें धर्म और संप्रदायवाद में अंतर करना होगा। धर्म एक विश्वास-प्रणाली है और लोग अपने व्यक्तिगत विश्वासों के एक अंग के रूप में उसका पालन करते हैं। इसके विपरीत संप्रदायवाद धर्म पर आधारित सामाजिक और राजनीतिक पहचान की विचारधारा का नाम है। धर्म संप्रदायवाद का कारण नहीं है और न ही संप्रदायवाद धर्म से प्रेरित होता है धर्म संप्रदायवाद में वहीं तक शामिल होता है जहाँ तक धर्म से बाहर के क्षेत्रों में उपजी राजनीति के साधन के रूप में काम करता है। संप्रदायवाद का एक बहुत सही वर्णन यह किया गया है कि यह धर्म का राजनीतिक व्यापार है। 1937 के बाद धर्म का उपयोग संप्रदायवादियों ने जनता को गतिमान बनाने के लिए किया था। इसलिए धर्मनिरपेक्षता का धर्म से कोई विरोध नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ केवल यह है कि धर्म व्यक्ति के निजी जीवन तक सीमित रहे और राजनीति तथा राज्य से उसका कोई सरोकार न रहे। जैसा कि गाँधीजी ने बार-बार कहा है - “धर्म हर व्यक्ति का निजी मामला है। इसे राजनीति या राष्ट्रीय मामलों से नहीं जोड़ना चाहिए।” शिक्षित मुसलमानों और बड़ें मुस्लिम नवाबों और जमींदारों के बीच अलगाववादी और वफादारी की प्रवृत्तियाँ तब चरम सीमा पर पहुँची जब 1906 में आगा खान, ढाका के नवाब और नवाब मोहसिनुलमुल्क के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना एक वफादार, सांप्रदायिक और रूढ़िवादी राजनीतिक संगठन के रूप में हुई और उसने उपनिवेशवाद की कोई आलोचना नहीं की, बगांल के विभाजन का समर्थन किया और सरकारी नौकरियों में मुसलमानों के लिए विशेष सुरक्षा प्रावधानों कि माँग की। बाद में वायसराय लार्ड मिंटो कि सहायता से उसने अलग-अलग चुनाव मंडलों की माँग उठाई और उसे मनवा भी लिया। इस तरह जब राष्ट्रीय कांग्रेस साम्राज्यवाद-विरोधी आर्थिक और राजनीतिक प्रश्न उठा रही थी तब मुस्लिम लीग और प्रतिक्रियावादी नेता यह प्रचार कर रहे थे कि मुसलमानों के हित हिंदुओं के हित से अलग हैं। मुस्लिम लीग की राजनीतिक गतिविधियाँ विदेशी शासन के खिलाफ नहीं बल्कि हिंदूओं राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ थीं। इसके बाद लीग लगातार कांग्रेस की हर राष्ट्रवादी और लोकतांत्रिक माँग का विरोध करती रही। इस तरह वे अंग्रेजों के हाथों में कठपुतली बनी रही जो कहते रहे कि वे मुसलमानों के ‘विशेष हितों’ की सुरक्षा करेंगे। लीग जल्द ही उन प्रमुख अस्त्रों में से एक बन गई जिसकी सहायता से अंग्रेज उभरते हुए राष्ट्रपादी आंदोलन से निबटने तथा मुस्लिम शिक्षित वर्ग को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने से रोकने की आशा करते थे। मुस्लिम लीग की उपयोगिता बढ़ाने के लिए जनता से संपर्क करने तथा उनका नेतृत्व संभालने में भी अंग्रेजों ने उसे प्रोत्साहित किया। यह सही है कि उस समय राष्ट्रवादी आंदोलन पर भी शिक्षित नगर-वासियों का वर्चस्व था, मगर उसका साम्राज्यवाद विरोधी अमीर-गरीब, हिंदू-मुसलमान, सभी भारतीयों के हितों का प्रतिनिधित्व करता था। दूसरी ओर, मुस्लिम लीग और उसके उच्चवर्गीय नेताओं के हितों की मुस्लिम जनता के हितों से बहुत कम समानता थी और यह मुस्लिम जनता भी हिंदू जनता की ही तरह विदेशी साम्राज्यवाद से पीड़ित थी। लीग की यह बुनियादी कमजोरी देशभक्त मुसलमानों पर धीरे-धीरे स्पष्ट होती गई। शिक्षित मुसलमान युवक खास तौर पर उग्र राष्ट्रवादी विचारों से आकर्षित थे। इसी समय मौलाना मुहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, मौलाना जफर अली खान और मजहरूल-हक के नेतृत्व में उग्र राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन की स्थापना हुई। ये युवक अलीगढ़ संप्रदाय तथा बड़े नवाबों और जमींदारों की वफादारी की राजनीति को नापसंद करते थे। स्वशासन के आधुनिक विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के पक्ष में प्रचार किया। ऐसी ही राष्ट्रवादी भावनाएँ पारंपरिक मुसलमान उल्माओं के एक भाग में भी उभर रही थीं। इनका नेतृत्व मदरसा देवबंद करता था। इन विद्वानों में सबसे प्रमुख थे मौलाना अबुल कलाम आजाद जिन्होंने अपने समाचारपत्र ‘अल-हिलाल’ में बुद्धिवादी और राष्ट्रीय विचारों का प्रचार किया। इस पत्र की स्थापना उन्होंने 1912 में की थी, जब वे केवल 24 वर्ष के थे। मौलाना मुहम्मद अली, आजाद और दूसरे युवकों ने साहस और निर्भय का संदेश दिया और कहा कि इस्लाम और राष्ट्रवाद में कोई विरोध नहीं है। 1911 में तुर्की की उस्मानिया सल्तनत और इटली के बीच लड़ाई छिड़ गई और 1912-13 में तुर्की का बल्कान के देशों से युद्ध हुआ। उस समय तुर्की का शासक स्वयं को खलीफा यानी तमाम मुसलमानों का धर्मगुरू भी कहता था। इसके अलावा, मुसलमानों के लगभग सभी धर्म-स्थान तुर्की के साम्राज्य में स्थित थे। भारत में तुर्की के प्रति सहानुभूति की लहर दौड़ गई। डॉ. एम. ए. अंसारी के नेतृत्व में तुर्की की सहायता के लिए एक मेडिकल मिशन भेजा गया। चूँकि बल्कान युद्ध के दौरान और उसके बाद भी ब्रिटेन की नीति तुर्की के प्रति सहानुभूतिपूर्ण न थी, इसलिए तुर्की-समर्थक और खलीफा-समर्थक, यानी खिलाफत की भावनाएँ साथ ही साम्राज्यवाद-विरोधी भी हो गई। वास्तव में अनेक वर्षों तक, अर्थात 1912 से 1924 तक मुस्लिम लीगी राष्ट्रवादी युवकों के सामने पूरी तरह दबे रहे। दुर्भाग्य से बुद्धिवादी विचारों वाले आजाद जैसे कुछेक लोगों को छोड़कर अधिकांश उग्र राष्ट्रवादी मुस्लिम युवकों ने राजनीति के प्रति आधुनिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को भी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि जिस प्रश्न को सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में उन्होंने उठाया वह राजनीतिक स्वाधीनता का नहीं, बल्कि धर्मस्थानों और तुर्क साम्राज्य की रक्षा का प्रश्न था। साम्राज्यवाद के आर्थिक और राजनीतिक दुष्परिणामों को समझने और उनका विरोध करने के बजाए वे साम्राज्यवाद से इस बात पर लड़ रहे थे कि वह खलीफा और उनके धर्मस्थानों के लिए एक खतरा था। तुर्की के प्रति उनकी सहानुभूति का आधार तक भी धार्मिक था। उनकी राजनीतिक अपील धार्मिक भावनाओं को संबोधित थी। इसके अलावा जिन नायकों, कथाओं और सांस्कृतिक परंपराओं का सहारा लिया वे प्राचीन या मध्यकालीन भारतीय इतिहास की न थीं बल्कि पश्चिमी एशिया के इतिहास से ली गई थीं। यह सही है कि इस दृष्टिकोण का भारतीय राष्ट्रवाद से तत्काल कोई टकराव नहीं हुआ। बल्कि उसने अपने समर्थकों को साम्राज्यवाद-विरोधी ही बनाया और शिक्षित मुसलमानों में राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति को बल पहुँचाया। लेकिन कालांतर में यह दृष्टिकोण ही हानिकारक सिद्ध हुआ क्योंकि इसने राजनीतिक प्रश्नों को धार्मिक दृष्टिकोण से देखने की आदत को मजबूत बनाया। खैर कुछ भी हो, इस तरह की राजनीतिक गतिविधि मुस्लिम जनता में आर्थिक और राजनीतिक प्रश्नों पर एक आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के विकास में सहायक नहीं हुई। इसी के साथ हिंदू सांप्रदायिकता का भी जन्म हो रहा था और हिंदू-सांप्रदायिकता विचार फैल रहे थे। अनेक हिंदू लेखकों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम सांप्रदायिकता और मुस्लिम लीग के विचारों और कार्यक्रमों को ही दोहराया। 1870 के बाद से ही हिंदू जमींदारों, सूदखोरों और मध्यवर्गीय पेशेवर लोगों ने मुस्लिम-विरोध भावनाएँ भड़काना आरंभ कर दिया था। भारतीय इतिहास की औपनिवेशिक समझ को पूरी तरह अपनाकर ये लोग मध्य काल में ‘निरंकुश’ मुस्लिम शासन की और ‘मुसलमानों की उत्पीड़न’ से हिंदूओं को ‘बचाने’ के संबंध में अंग्रेजों की ‘मुक्तिदायी’ भूमिका की बातें करते थे और उसके बारे में लिखते थे। संयुक्त प्रांत और बिहार में उन्होंने सही तौर पर हिंदी का सवाल उठाया मगर उसे एक सांप्रदायिक रंग दे दिया और इस अनैतिहासिक धारणा का प्रचार किया कि उर्दू मुसलमानों की तथा हिंदी हिंदुओं की भाषा है। 1890 के तत्काल बाद के वर्षों में पूरे भारत में गौहत्या-विरोध प्रचार चलाया गया। यह अभियान अंग्रेजों के नहीं बल्कि मुसलमानों के खिलाफ था। उदाहरण के लिए, ब्रिटिश फौजी छावनियों को बड़े पैमाने पर गौहत्या करने के लिए खुला छोड़ दिया गया। 1909 में पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई। इसके नेताओं ने राष्ट्रीय कांग्रेस पर इस बात के लिए चोटें कीं कि वे सभी भारतीयों को एक राष्ट्र के रूप में एकजुट कराना चाहते हैं। उन्होंने कांग्रेस की साम्राज्यवाद-विरोधी राजनीति का विरोध किया। इसके बजाए, उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ संघर्ष में हिंदू विदेशी सरकार को खुश रखें। इसके एक नेता लालचंद ने घोषणा की कि हिंदू स्वंय को “पहले हिंदू और फिर भारतीय” माने। अप्रैल 1915 में कासिम बाजार के महाराजा की अध्यक्षता में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन हुआ। पर वर्षों तक यह कुछ कमजोर संगठन ही बना रहा। इसका एक कारण यह था कि आधुनिक धर्मनिरपेक्ष बुद्धिजीवियों और मध्य वर्ग का हिंदुओं में ज्यादा असर था। दूसरी ओर, मुसलमानों पर प्रमुख प्रभाव अभी भी जमींदारों, नौकरशाहों और पारंपरिक धार्मिक मुल्लाओं का ही था। इसके अलावा औपनिवेशिक सरकार हिंदू संप्रदायवाद को कम सहायता और समर्थन देती थी क्योंकि वह मुस्लिम संप्रदायवाद पर बुरी तरह निर्भर थी और एक ही साथ दोनों तरह के संप्रदायवाद को आसानी से खुश नहीं रख सकती थी। राष्ट्रवादी और प्रथम विश्वयुद्धजून 1914 में पहला विश्वयुद्ध फूट पड़ा। इसमें एक और ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस और जापान थे और अमरीका भी बाद में उनसे आ मिला और दूसरी ओर जर्मनी, आस्ट्रिया-हंगरी और तुर्की थे। युद्ध के यह वर्ष भारत में राष्ट्रवाद के परिपक्व होने के दिन थे।आरंभ में लोकमान्य तिलक समेत, जो जून 1914 में जेल से छूटे थे, भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने सरकार के युद्ध प्रयासों में सहयोग का निश्चय किया। यह निश्चय इस गलत धारणा पर आधारित था कि कृतज्ञ होकर ब्रिटेन भारत की वफादारी का पुरस्कार देगा और भारत स्वशासन की ओर एक लंबी छलांग लगाने में समर्थ होगा। उन्होंने इस बात को पूरी तरह नहीं समझा कि प्रथम विश्वयुद्ध की विभिन्न शक्तियाँ अपने उपनिवेशों को सुरक्षित रखने के लिए ही लड़ रही थी। होम रूल लीगसाथ ही, अनेक भारतीय नेताओं ने स्पष्ट रूप से समझा कि सरकार तब तक कुछ वास्तविक अधिकार नहीं देगी जब तक कि उसके ऊपर जनता का दबाव न डाला जाए। इसलिए एक वास्तविक राजनीतिक जन-आंदोलन आवश्यक था कुछ और कारण भी राष्ट्रवादी आंदोलन को इसी दिशा में धकेल रहे थे। प्रथम विश्वयुद्ध ने, जिसमें यूरोप की साम्राज्यवादी शक्तियाँ आपस में लड़ रही थीं, एशियाई जनता के मुकाबले यूरोप के राष्ट्रों के नस्ली श्रेष्ठता की भ्रामक धारणा को नष्ट कर दिया। इसके अलावा युद्ध के कारण भारत के निर्धन वर्गों की बदहाली और भयानक हुई। उनके लिए युद्ध का मतलब था करों का भारी बोझ और रोजमर्रा की जरूरतों का लगातार मँहगा होना। ये वर्ग किसी भी जुझारु विरोध आंदोलन में शामिल होने के लिए तैयार थे। परिणामस्वरुप, युद्ध के ये वर्ष तीखे राष्ट्रवादी राजनीतिक आंदोलन के वर्ष थे।लेकिन ऐसा कोई जन-आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में नहीं चल सकता था, क्योंकि वह नरमपंथियों के नेतृत्व में एक निष्क्रिय और जड़ संगठन बन चुकी थी और जनता के बीच उसका कोई राजनीतिक कार्य नहीं रह गया था। इसलिए 1915-16 में दो होम रूल लीगों की स्थापना हुई। इनमें एक के नेता लोकमान्य तिलक थे, तो दूसरा भारतीय संस्कृति और भारतीय जनता की अंग्रेज प्रशंसिका श्रीमती ऐनी बेसेंट और एस, सुब्रामन्य अय्यर के नेतृत्व में था। इन दो होम रूल लीगों ने आपसी सहयोग से पूरे देश में इस माँग को प्रचारित किया कि युद्ध के बाद भारत को होम रूल या स्वशासन दिया जाए। यही वह आंदोलन था जिसके दौरान तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा दिया था कि “होम रूल मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा।” इन दो लीगों ने बहुत तेजी से प्रगति की और होम रूल की माँग पूरे देश में गूँजने लगी। कांग्रेस की निष्क्रियता से दुखी अनेक नरमपंथी राष्ट्र वादी भी होम रूल आंदोलन में शामिल हो गए। इन होम रूल लीगों पर जल्द ही सरकार का प्रकोप टूटा। जून 1917 में एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। जनता के विरोध के कारण सरकार ने मजबूर होकर सितंबर 1917 में उन्हें छोड़ दिया। युद्ध के इस काल में क्रांतिकारी आंदोलन का भी विकास हुआ। आतंकवादी संगठन बंगाल और महाराष्ट्र से लेकर पूरे उत्तरी भारत तक फैल गए। इसके अलावा अनेक भारतीय ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाने लगे। अमरीका और कनाडा में बसे भारतीय क्रांतिकारियों ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी के अधिकांश सदस्य पंजाब के सिख किसान और भूतपूर्व सैनिक थे जो वहाँ रोजी-रोटी की तलाश में गए थे और जिनको वहाँ खुले नस्ली और आर्थिक भेदभाव का सामना करना पड़ता था। लाला हरदयाल, मुहम्मद बरकतुल्लाह, भगवान सिंह, रामचंद्र और सोहनासिंह भखना गदर पार्टी के कुछ प्रमुख नेता थे। पार्टी का आधार उसका साप्ताहिक पत्र ‘गदर’ था जिसके सिरे पर “अंग्रेजी राज का दुश्मन” शब्द लिखे होते थे पत्र ‘गदर’ ने एक विज्ञापन छापा - “भारत में विद्रोह फैलाने के लिए बहादुर सिपाहियों की आवश्यकता है। तनख्वाह-मौत, इनाम-शहादत, पेंशन-आजादी, लड़ाई का मैदान भारत है। इस पार्टी की विचारधारा बहुत ही धर्मनिरपेक्ष थी। सोहनसिंह भखना, जो बाद में पंजाब के एक प्रमुख किसान नेता बने, के शब्दों में, “हम सिख या पंजाबी नहीं थे। हमारा धर्म देशभक्ति था।” मेक्सिको, जापान, चीन, फिलीपीन, मलाया, सिंगापुर, थाईलैंड, हिंदचीन, तथा पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका जैसे दूसरे देशों में भी पार्टी के सक्रिय सदस्य मौजूद थे। गदर पार्टी ने भारत में अंग्रेजों से लड़ने के लिए क्रांतिकारी युद्ध चलाने का संकल्प किया था। 1914 में जैसे ही प्रथम विश्वयुद्ध फूटा, गदरपंथी हथियार और धन भारत भेजने लगे कि यहाँ के सैनिकों और स्थानीय क्रांतिकारियों की सहायता से विद्रोह आरंभ किया जाए। कई हजार लोगों ने भारत वापस जाने की इच्छा प्रकट की। उनके खर्च के लिए कई लाख डालर की रकम जमा हो गई। कईयों ने अपनी जीवन भर की बचाई रकम दे दी या जमीन-जायदात बेंच दी। गदरपंथियों ने सुदूर-पूर्व, दक्षिण-पूर्वी एशिया और पूरे भारत में सैनिकों से संपर्क किया अनेकों रेजीमेन्टों को विद्रोह के लिए तैयार कर लिया। अंततः पंजाब में सशस्त्र विद्रोह के लिए 21 फरवरी 1915 की तारीख निश्चित हुई। दुर्भाग्य से अधिकारियों को इन योजनाओं का पता चल गया और उन्होंने तत्काल कार्यवाही की। विद्रोही रेजीमेन्टों को तोड़ दिया गया और उसके नेताओं को जेल या फाँसी की सजाएँ दी गईं। उदाहरण के लिए, 23वें घुड़सवार दस्ते के 12 लोगों को फाँसी हुई, 114 को उम्र कैद की सजा दी गई और 93 को लंबी-लंबी जेल-सजाएँ दी गई। उनमें से अनेक ने रिहा होने के बाद पंजाब में किरती (मजदूर) और कम्युनिस्ट आंदोलनों की स्थापना की। कुछ प्रमुख गदरी नेता इस प्रकार थे - बाबा गुरमुख सिंह, करतार सिंह सराभा, सोहन सिंह भखना, रहमत अली शाह, भाई परमानंद और मौलवी बरकतुल्लाह। गदर पार्टी से प्रेरित होकर सिंगापुर में पाँचवीं लाइट इन्फैट्री के 700 लोगों ने जमादार चिश्ती खान और सूबेदार डुंडे खान के नेतृत्व में विद्रोह किया। एक तीखी लड़ाई के बाद वे कुचल दिए गए। इस लड़ाई में अनेक लोग मारे गए। दूसरे 37 लोगों को सार्वजनिक रूप से फाँसी दी गई। 41 को उम्र कैद की सजा मिली। भारत में और बाहर दूसरे क्रांतिकारी भी सक्रिय थे 1915 में एक असफल क्रांतिकारी प्रयास में जतीन मुखर्जी, जिन्हें ‘बाघा जतीन’ कहा जाता था, बालासोर में पुलिस से लड़ते हुए मारे गए। रासबिहारी बोस, राजा महेंद्रप्रताप, लाला हरदयाल, अब्दुर्रहीम, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, चंपक रमन पिल्लै, सरदार सिंह राणा और मादाम भीकाजी कामा कुछ ऐसे प्रमुख भारतीय थे जिन्होंने भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ चलाई, क्रांतिकारी प्रचार किया और समाजवादियों तथा दूसरे साम्राज्यवाद-विरोधियों का समर्थन भारत की स्वाधीनता के लिए प्राप्त किया। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन (1916)राष्ट्रवादियों को जल्द ही पता चल गया कि उनकी फूट से उनके उद्देश्य की हानि हो रही थी और इसलिए उन्हें सरकार के विरोध में एकजुट होना चाहिए। देश में बढ़ रही राष्ट्रवादी भावना और राष्ट्रीय एकता की आकांक्षा के कारण 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ऐतिहासिक महत्व की दो घटनाएँ हुईं। पहला यह कि कांग्रेस के दोनों धड़े फिर एक हो गए। पुराने विवादों का अब कोई अर्थ नहीं रह गया था और फूट के कारण कांग्रेस राजनीतिक निष्क्रियता का शिकार हो गई थी। 1914 में जेल से रिहा होने के बाद तिलक ने फौरन बदली हुई स्थिति को समझा और कांग्रेसियों के दोनों धड़ों को एकजुट करने में लग गए। नरमपंथी राष्ट्रवादियों को मानने के लिए उन्होंने यह घोषणा की - ’’मैं हमेशा-हमेशा के लिए यह बात कह दूं कि जैसा कि आयरलैंड में आयरिश होम रूलवादी कर रहे हैं, हम भी भारत में प्रशासन-प्रणाली में सुधार के प्रयास कर रहे हैं, न कि सरकार को उखाड़ फेंकने की।” मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि देश के विभिन्न भागों में हिंसा के जो काम किए गए हैं वे न केवल यह कि मुझे अरुचिकर है बल्कि मेरी राय में उन्होंने दुर्भाग्य से हमारी राजनीतिक प्रगति की गति को काफी हद तक धीमा किया है। दूसरी तरफ, राष्ट्रवाद की उभरती लहर ने पुराने नेताओं के भी मजबूर किया कि वे लोकमान्य तिलक और अन्य उग्र राष्ट्रवादियों के कांग्रेस में दोबारा आने का स्वागत करें। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1907 के बाद एकता का पहला अधिवेशन था। इसने स्वशासन के लिए और भी सांवैधानिक सुधारों की माँग की।दूसरे, लखनऊ में अपने पुराने मतभेद भुलाकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग से सरकार के सामने साझी राजनीतिक माँगें रखीं। युद्ध और दो होमरूल लीगों के कारण जब देश में एक नई भावना पैदा हो रही थी और कांग्रेस का चरित्र बदल रहा था, तब मुस्लिम लीग में भी धीरे-धीरे परिवर्तन आ रहे थे। हमने पहले ही देखा है कि शिक्षित मुसलमान युवक उग्र राष्ट्रवादी राजनीति को अपना रहा था। युद्ध के कारण इस दिशा में और भी विकास हुआ। फलस्वरूप 1914 में सरकार ने अबुल कलाम आजाद के पत्र ’अल-हिलाल’ और मौलाना मुहम्मद अली के पत्र ‘कामरेड’ को बंद कर दिया। उसने अली भाइयों (मौलाना मुहम्मद अली और शौकत अली) हसरत मोहाना और अबुल कलाम आजाद को नजरबंद कर लिया। कम से कम अंशतः ही सही युवकों की इस राजनीतिक उग्रता की अभिव्यक्ति लीग में भी हुई। धीरे-धीरे उसने अलीगढ़ संप्रदाय के सीमित राजनीतिक दृष्टिकोण के खोल से बाहर निकलना आंरभ किया और कांग्रेस की नीतियों के करीब आने लगी। कांग्रेस और लीग की यह एकता कांग्रेस-लीग समझौते पर हस्ताक्षर के साथ स्थापित हुई, इसे आम तौर पर लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। इन दोनों को करीब लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका लोकमान्य तिलक और मुहम्मद अली जिन्ना की रही क्योंकि दोनों मानते थे कि केवल हिंदू-मुस्लिम एकता के द्वारा ही भारत को स्वशासन प्राप्त हो सकता है। तब तिलक ने घोषणा की थी - “महानुभावों, कुछ लोगों ने यह बात कही है कि हम हिंदुओं ने अपने मुसलमान भाइयों को बहुत सी छूटें दी हैं। मुझे विश्वास है कि जब मैं यह कहता हूँ कि हम बहुत कुछ दे ही नहीं सकते तो मैं पूरे भारत के हिंदू समुदाय की भावना का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। अगर स्वशासन के अधिकार केवल मुस्लिम समुदाय को दिए जाएँ तो भी मुझे परवाह नहीं होगी . . . . . अगर ये अधिकार हिंदू जनता के निचले और सबसे निचले वर्गों को दिए जाएँ तो भी मुझे परवाह नहीं होगी। जब हम एक तीसरे दल से लड़ रहे हों तो यह आवश्यक है कि हम इस मंच पर नस्ल से एकजुट, धर्म से एकजुट, सभी तरह के राजनीतिक विश्वासों से एकजुट होकर खड़े हों।” कांग्रेस और मुस्लिम लीग, दोनों ने अपने अधिवेशन में एक ही प्रस्ताव पारित किए, अलग-अलग चुनाव मंडलों के आधार पर राजनीतिक सुधारों की एक साझी योजना सामने रखी और माँग की कि ब्रिटिश सरकार यथाशीघ्र भारत को स्वशासन देने की घोषणा करें। लखनऊ समझौता हिन्दू-मुस्लिम एकता के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। दुर्भाग्य से इसने हिंदू और मुस्लिम जनता को शामिल नहीं किया और अलग-अलग चुनाव मंडलों के घातक सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया। यह इस धारणा पर आधारित था कि शिक्षित हिंदुओं और मुसलमानों को दो अलग-अलग राजनीतिक इकाइयाँ मानकर फिर उनको साथ लाया जाए। दूसरे शब्दों में, उनके राजनीतिक दृष्टिकोण को धर्मनिरपेक्ष बनाने का प्रयास नहीं किया गया जिससे वे समझ सकें कि राजनीति में हिंदू या मुसलमान के रूप में उनके अलग-अलग हित नहीं हैं। इसलिए लखनऊ समझौते के बाद भी भविष्य में भारतीय राजनीति में संप्रदायवाद के फिर से सर उठाने की गुंजाइश बनी रह गई। फिर भी लखनऊ की घटनाओं का अत्यधिक तात्कालिक प्रभाव पड़ा। नरमपंथी और उग्र राष्ट्रवादियों के बीच तथा राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एकता स्थापित होने से देश बेहद राजनीतिक उत्साह से भर उठा। यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार ने भी राष्ट्रवादियों को खुश करना अब जरूरी समझा। अभी तक वह राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने के लिए भयानक दमन का सहारा लेती आ रही थी। उग्र राष्ट्रवादियों और क्रांतिकारियों को बड़ी संख्या में जेलों में डाला गया था या बदनाम भारत रक्षा कानून और ऐसे ही दूसरे कानूनों को अंतर्गत नजरबंद किया गया था। अब सरकार ने राष्ट्रवादी जनमत को संतुष्ट करने का फैसला किया और 20 अगस्त 1917 को उसने घोषणा की कि “ब्रिटिश साम्राज्य के एक अभिन्न अंग के रूप में भारत के एक उत्तरदायी सरकार की अधिकाधिक स्थापना की दृष्टि से स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक विकास करना” उसकी नीति थी। फिर जुलाई 1918 में मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों की घोषणा की गई। पर भारतीय राष्ट्रवाद इतने से ही संतुष्ट न हो सका। वास्तव में अब राष्ट्रीय आंदोलन इस स्थिति में था कि शीघ्र ही अपने तीसरे और अंतिम चरण में प्रवेश कर सके। यह चरण गाँधीवादी युग के जनसंघर्षों का चरण था। | |||||||||
| |||||||||