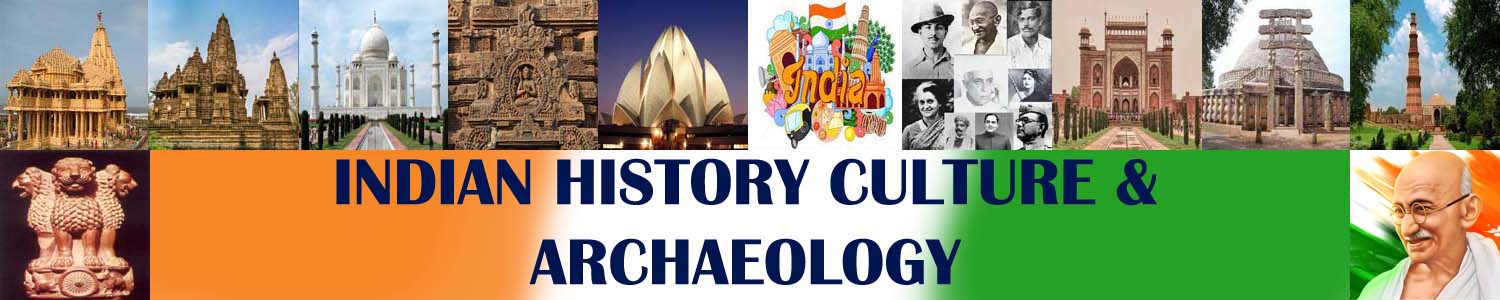| |||||||||
|
मुगल साम्राज्य का विस्तार - अकबर
अकबर का युगहुमायूँ जब बीकानेर से लौट रहा था तो अमरकोट के राणा ने उसे सहारा और सहायता देने की शिष्टता दिखाई। अमरकोट में ही 1542 में मुगलों में महानतम शासक अकबर का जन्म हुआ। जब हुमायूँ ईरान की ओर भागा तो उसके बच्चे अकबर को उसके चाचा कामरान ने रख लिया। उसने बच्चे की भली-भाँति पालन-पोषण किया। कन्धार पर हुमायूँ का फिर से अधिकार हो जाने पर अकबर फिर अपने माता पिता से मिल गया। हुमायूँ की मृत्यु के समय अकबर पंजाब में कलानौर में था और अफगान विद्रोहियों से निपटने में व्यस्त था। 1556 में कलानौर में ही अकबर की ताजपोशी हुई। उस समय उसकी आयु तेरह वर्ष और चार महीने की थी।अकबर को कठिन परिस्थितियाँ विरासत में मिली। आगरा के पार अफगान अभी भी सबल थे और हेमू के नेतृत्व में अन्तिम लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। काबुल पर आक्रमण करके घेरा डाला जा चुका था। पराजित अफगान शासक सिकंदर सूर शिवालिक की पहाड़ियों में घूम रहा था। लेकिन अकबर के उस्ताद और हुमायूँ के स्वामिभक्त और योग्य अधिकारी बैरमखाँ ने इस कठिन परिस्थिति का कुशलता व धैर्य से सामना किया। उसे खान-ए-खान की उपाधि प्रदान की गई व राज्य का वकील बनाया गया था। मुगल सेनाओं का पुनर्गठन किया। इस समय सबसे गम्भीर खतरा हेमू की ओर से था। उस समय चुनार से लेकर बंगाल की सीमा तक का प्रदेश शेरशाह के एक भतीजे आदिलशाह के शासन में था। हेमू अपना जीवन इस्लामाशाह के राज्यकाल में बाजारों के अधीक्षक के रूप में शुरू किया गया था और आदिलशाह के काल में उसकी आकस्मिक रूप से उन्नति हुई थी। हेमू बड़ा पराक्रमी था। उसने बाईस लड़ाइयों में से एक भी नहीं हारी थीं। आदिलशाह ने उसे विक्रमाजीत की उपाधि प्रदान करके वजीर नियुक्त कर लिया था। उसने उसे मुगलों को खदेड़ने का उत्तरादायित्व सौंप दिया। हेमू ने आगरा पर अधिकार कर लिया और 50,000 घुड़सवार, 500 हाथी और विशाल तोपखाना लेकर दिल्ली की ओर कूच किया। एक भीषण लड़ाई में हेमू ने मुगलों को पराजित कर दिया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। लेकिन इस कठिन परिस्थिति में बैरमखाँ ने धैर्य नहीं खोया और बिना भयभीत हुए दिल्ली की ओर बढ़ने का निश्चय किया। उसके इस साहसिक कदम से मुगल सेना में नयी शक्ति का संचार हुआ। बैरमखाँ ने हेमू को अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर दिए बिना दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। हेमू के नेतृत्व में अफगान फौज और मुगलों के बीच पानीपत के मैदान में एक बार फिर लड़ाई हुई (5 नवम्बर 1556)। यद्यपि मुगलों की एक टुकड़ी द्वारा हेमू के तोपखाने पर पहले ही अधिकार कर लिया गया था। फिर भी पलड़ा हेमू का ही भारी था। लेकिन तभी एक तीर हेमू की गर्दन में लगा और वह बेहोश हो गया। नेतृत्वहीन अफगान सेना पराजित हो गई। हेमू को बन्दी कर मार डाला गया। इस प्रकार अकबर को अपना साम्राज्य लड़ कर हासिल करना पड़ा। प्रारम्भिक दौर उमरावर्ग के साथ संघर्ष (1556-67)बैरमखाँ लगभग चार वर्ष तक साम्राज्य का सरगना रहा। इस दौरान उसने अमीरों को पूरी तौर से अपने काबू में रखा। इस दौर में काबुल पर खतरा टल गया था और साम्राज्य की सीमा का विस्तार काबुल से पूर्व में स्थित जौनपुर तक और पश्चिम में अजमेर तक हो गया था। ग्वालियर पर भी अधिकार कर लिया गया था और रणथम्भौर और मालवा को जीतने का भी भरमक प्रयास किया गया।लेकिन बैरमखाँ की यह स्थिति बरकरार न रह सकी। क्योंकि अकबर अब वयस्क हो गया था। स्पष्ट है कि वह बैरमखाँ के अनुशासन को पूर्ववत् स्वीकार नहीं कर सकता था। फिर बैरमखाँ ने अपने व्यवहार से बहुत से प्रभावशाली व्यक्तियों को नाराज कर दिया था। उन्होंने शिकायत की कि बैरमखाँ शिया है और वह अपने समर्थकों और शियाओं को उच्च पदों पर नियुक्त कर रहा है। तथा पुराने सरदारों की अवहेलना कर रहा है। वे दोषारोपण अपने आप में सही नहीं थे, लेकिन इसमें शक नहीं कि बैरमखाँ बहुत अहंकारी हो गया था और इस बात को भूल रहा था कि अकबर अब बड़ा हो रहा था। छोटी-छोटी बातों पर दोनों में मतभेद हो गया और अकबर ने यह समझ लिया कि प्रशासन के कार्यों को अब किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों में सौंपे रखना उचित नहीं है। अकबर ने बहुत होशियारी से काम लिया। वह शिकार के बहाने आगरा से निकला और दिल्ली पहुँच गया। दिल्ली से उसने बैरमखाँ को अपदस्थ करते हुए एक फरमान जारी किया और सब अमीरों को व्यक्तिगत रूप से अपने सामने हाजिर होने का आदेश दिया। एक बारगी बैरमखाँ ने जब यह महसूस किया कि अकबर सारे अधिकार अपने हाथ में लेना चाहता है, वह इसके लिए तैयार हो गया लेकिन उसके विरोधी उसे तबाह करने पर तुले हुए थे। उन्होंने उसे इतना अप्रभावित किया कि वह विद्रोह पर उतारू हो गया। इस विद्रोह के कारण साम्राज्य में 6 महीने तक अव्यवस्था रही। अन्ततः बैरमखाँ समर्पण करने पर विवश हो गया। अकबर ने उससे उदारता का व्यवहार किया और उसके सामने दो विकल्प रखे कि या तो वह उसके दरबार में बना रहे या मक्का चला जाये। बैरमखाँ ने मक्का चले जाना बेहतर समझा, लेकिन रास्ते में अहमदाबाद के निकट पाटन में एक अफगान ने व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण उसकी हत्या कर दी। बैरमखाँ की पत्नी और छोटे बच्चे को अकबर के पास लाया गया। अकबर ने बैरम की विधवा के साथ जो उसकी रिश्ते में चचेरी बहन लगती थी, विवाह कर लिया, और बच्चे को बेटे की तरह पाला। यह बच्चा बाद में अब्दुल रहीम खान ए खाना के नाम से प्रसिद्ध हुआ और साम्राज्य के महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सैनिक पद उसके पास रहे। बैरमखाँ और उसके परिवार के साथ अकबर ने जो व्यवहार किया उससे उसकी चरित्रगत एक विशेषता का भलीभाँति पता चलता है। वह यह कि एक बार कोई निर्णय ले लेने के बाद उसे कोई अपने निश्चय से डिगा नहीं सकता था तथा यह भी कि किसी प्रतिद्वन्द्वी के समर्पण कर देने पर व उसके प्रति दया भाव दिखाने से भी नहीं चूकता था। बैरमखाँ के विद्रोह के दौरान उमरा वर्ग में बहुत से व्यक्ति और दल राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गये थे। इनमें अकबर की धाय माँ महम अनगा और उसके सम्बन्धी भी थे। यद्यपि महम अनगा ने शीघ्र ही राजनीति से सन्यास ले लिया परन्तु उसका पुत्र अधमखाँ एक महत्वाकांक्षी नौजवान था। उसे मालवा के विरुद्ध एक अभियान का सेनापति बनाकर भेजे जाने से ही वह स्वतन्त्रता का व्यवहार करने लगा था। इस पर जब उसे अपदस्थ कर दिया गया तो उसने वजीर के पद की माँग की और जब उसकी माँग स्वीकार नहीं की गई तो उसने कार्यवाहक वजीर को छुरा घोंप दिया। इससे अकबर बहुत क्रोधित हुआ और अधमखाँ को किले की दीवार से फिकवा देने का आदेश दिया। इस प्रकार अधमखाँ 1561 में मर गया। परंतु अकबर को अपनी सत्ता पूरी तौर पर स्थापित करने में बहुत वर्ष लगे। उजबेकों अमीरों ने अपना एक शक्तिशाली दल बना लिया था। उनके पास पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और मालवा में महत्वपूर्ण पद थे। यद्यपि उन्होंने उन क्षेत्रों में शक्तिशाली अफगान दलों को दबाये रखकर साम्राज्य की बहुत सेवा की, परन्तु वे बहुत अहंकारी हो गये थे और तरुण शासक की हुकमउदूली करने लगे थे। 1561 और 1567 के बीच उन्होंने कई बार विद्रोह किये जिससे विवश होकर अकबर को उनके विरूद्ध सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी। प्रत्येक बार अकबर ने उन्हें क्षमा कर दिया लेकिन जब 1565 में उन्होंने फिर विद्रोह किया तो अकबर इतना उत्तेजित हुआ कि उसने प्रतिज्ञा की जब तक वह उन्हे मिटा नहीं देगा तब तक जौनपुर को राजधानी बनाये रखेगा। इसी बीच मिर्जाओं के विद्रोह ने अकबर को उलझा लिया। मिर्जा अकबर के सम्बन्धी थे और तैमूरवंशी थे। इन्होंने आधुनिक उत्तर प्रदेश के पश्चिमवर्ती क्षेत्रों में गड़बड़ मचाई। इन सब विद्रोहों से उत्साहित हो कर अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम ने काबुल पर अधिकार करके पंजाब की ओर कूच किया और लाहौर पर घेरा डाल दिया। उजबेक विद्रोहियों ने उसको विधिवत् अपना शासक स्वीकार कर लिया। हेमू के दिल्ली पर अधिकार करने के बाद अकबर के सामने यह सबसे गम्भीर संकट था। किन्तु अकबर को अपने धैर्य, साहस और कुछ हद तक भाग्य के बल पर विजय प्राप्त हुई। वह जौनपुर से लाहौर की ओर बढ़ा जिससे मिर्जा हकीम पीछे हटने पर विवश हो गया। इस बीच मिर्जाओं के विद्रोह को कुचल दिया गया और वे मालवा व वहाँ से गुजरात की ओर भाग गये। अकबर लाहौर से जौनपुर लौटा। वर्षा ऋतु में इलाहाबाद के निकट यमुना पार करके उसने उजबेक सरदारों के नेतृत्व में विद्रोहियों को आश्चर्य चकित कर दिया और उन्हें पूरी तरह पराजित किया (1567)। उजबेक नेता लड़ाई में मारे गये और इस प्रकार यह लम्बा विद्रोह समाप्त हुआ। सभी विद्रोही अमीरों के, जिसमें अपनी स्वतन्त्रता का सपना देखने वाले महत्वाकांक्षी भी शामिल थे, हौसले पस्त हो गये। अब अकबर निश्चिंत हो कर अपने साम्राज्य के विस्तार की ओर ध्यान दे सकता था। साम्राज्य का प्रारम्भिक विस्तार (1567-76)बैरमखाँ के संरक्षण के काल में मुगल साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार हुआ था। अजमेर के अतिरिक्त इस काल में मालवा और गढ़ कटंगा जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर विजय प्राप्त की गई थी। उस समय मालवा पर एक युवा राजकुमार बाजबहादुर का शासन था। वह संगीत और काव्य में प्रवीण था। बाजबहादुर और सुन्दरी रूपमती की प्रेम गथाएँ बहुत प्रसिद्ध है। सुन्दर होने के साथ-साथ रूपमती संगीत और काव्य में भी सिद्धहस्त थी। बाजबहादुर के समय में माण्डू संगीत का केन्द्र था। बाजबहादुर द्वारा सेना की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। ऐसी परिस्थितियों में मुगलों का मालवा विजय के लिये प्रेरित होना स्वाभाविक ही था। मालवा के विरुद्ध अभियान सेनापति अकबर की धाय माँ महम अनगा का पुत्र अधमखाँ था। बाजबहादुर बुरी तरह पराजित हुआ (1561) और मुगलों के हाथ रूपमती सहित बहुत कीमती सामान हाथ लगा। लेकिन रूपमती ने अधमखाँ के हरम में जाने की बजाय आत्महत्या करना उचित समझा। अधमखाँ और उसके उत्तराधिकारी के अविवेक पूर्ण क्रूरता के कारण मुगलों के विरुद्ध वहाँ प्रतिक्रिया हुई, जिससे बाजबहादुर को पुनः राज्य प्राप्त करने का अवसर मिला।बैरमखाँ के विद्रोह से निपटने के पश्चात् अकबर ने मालवा के विरुद्ध एक और अभियान छेड़ा। बाजबहादुर को वहाँ से भागना पड़ा। उसने कुछ समय के लिए मेवाड़ के राणा के पास शरण ली। एक के बाद दूसरे स्थान पर भटकने के बाद बाजबहादुर अकबर के दरबार में पहुँचा और उसे मनसबदार बना दिया गया। लगभग इसी समय मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर विजय प्राप्त की। गढ़ कटंगा के राज्य में नर्मदा घाटी और आधुनिक मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके सम्मिलित थे। इस राज्य की स्थापना पन्द्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में अमन दास ने की थीं। अमन दास ने रायेन को जीतने में गुजरात के बहादुरशाह की सहायता की थी और उसे बहादुर शाह से संग्राम शाह की उपाधि प्राप्त हुई थी। गढ़ कटंगा में कुछ गौंड और राजपूत रियासतें भी शामिल थीं। यह गौडों द्वारा स्थापित शक्तिशाली राज्य था। कहा जाता है कि राजा के सेनापतित्व में 20,000 पैदल सिपाही, एक बड़ी संख्या में घुड़सवार और 1,000 हाथी थे। लेकिन इन संख्याओं की विश्वसनीयता का कोई प्रमाण नहीं है। संग्रामशाह ने अपने एक पुत्र की शादी महोबा के सुप्रसिद्ध चंदेल शासक की राजकुमारी से करके अपनी स्थिति और सुदृढ़ कर ली थी। यह राजकुमारी, जो दुर्गावती के नाम से प्रसिद्ध है, शीघ्र ही विधवा हो गई, लेकिन उसने अपने अल्पवयस्क पुत्र को गद्दी पर बिठाया और बड़े साहस और कुशलता से राज्य किया। वह एक कुशल बंदूकची और तीरन्दाज थी। वह शिकार की शौकीन थी। एक समकालीन लेखक के अनुसार उसे जब भी आस-पास किसी बाघ के दिखाई देने की सूचना मिलती थी, वह उसका शिकार किए बिना जल भी ग्रहण नहीं करती थी। उसने आसपास के राज्यों से कई लड़ाइयाँ सफलतापूर्वक लड़ी। बाजबहादुर से भी उसका युद्ध हुआ। सीमावर्ती इलाकों के ये संघर्ष मालवा पर मुगलों का अधिकार हो जाने के बाद भी जारी रहे। इसी कारण दुर्गावती के सौन्दर्य तथा उसे राज्य की अतुल धन राशि होने की कथाएँ इलाहाबाद के मुगल सूबेदार आसफखाँ तक पहुँची। आसफखाँ 10,000 सिपाहियों को लेकर बुन्देलखण्ड की ओर से बढ़ा। गढ़ के कुछ अर्द्ध स्वतन्त्र शासकों ने गौंड का जुआ कंधों से उतार फेंकने का यह अच्छा अवसर देखा। अतः रानी के पास बहुत कम फौज रह गई। जख्मी होने पर भी, वह वीरतापूर्वक लड़ती रही। फिर यह देखकर कि पराजय अश्वयंभावी है और उसे बन्दी बनाया जा सकता है, उसने छुरा मार कर आत्महत्या कर ली। आसफखाँ ने तब आधुनिक जबलपुर के पास स्थित उसकी राजधानी चौरागढ़ पर हल्ला बोल दिया। अबुल फजल के शब्दों में ‘‘इतने हीरे जवाहरात, सोना, चाँदी और अन्य वस्तुएँ हाथ लगीं कि उनके अंश का भी हिसाब लगा पाना मुश्किल है।’’ उस भारी लूट में से आसफखाँ ने केवल 200 हाथी दरबार में भेज दिए और शेष भाग अपने पास रख लिया। रानी की एक छोटी बहन कमला देवी भी दरबार में भेज दी गईं। उजबेक सरदारों के विद्रोह को समाप्त करने के पश्चात् अकबर ने आसफखाँ को लूट का माल लौटाने के लिये विवश किया। अकबर ने गढ़ कटंगा संग्रामशाह के छोटे पुत्र चन्द्रशाह को लौटा दिया, लेकिन मालवा की सरहद पर स्थित दस किलों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अगले दस वर्षां में अकबर ने राजस्थान के अधिकांश भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया तथा गुजरात और बंगाल भी जीत लिया। राजपूत रियासतों के विरुद्ध अभियान में एक महत्वपूर्ण कदम चित्तौड़ का घेरा था। यह दुर्जेय किला जिस पर अतीत में अनेक घेरे पड़ चुके थे, मध्य राजस्थान का प्रवेश का द्वार समझा जाता था। यह आगरा से गुजरात जाने का सबसे छोटा मार्ग था। इससे भी अधिक इससे भी बढ़कर इस किले की महत्ता राजपूती संघर्ष और प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में थी। अकबर ने यह अनुभव किया कि बिना चित्तौड़ जीते, अन्य राजपूत रियासतें उसका प्रभुत्व स्वीकार नहीं करेंगी। 6 महीने के घेरे के बाद चित्तौड़ की पराजय हुई। सामन्तों की सलाह से प्रसिद्ध योद्धाओं जयमल और पट्टा को किले का भार सौंप कर राजा उदयसिंह जंगल में छिप गया था। आस-पास के इलाकों के बहुत से किसानों ने किले में शरण ले ली थी। उन्होंने भी किले की सुरक्षा में सक्रिय योगदान दिया। विजय के उपरान्त मुगलों ने किले में प्रवेश किया, तो इन किसानों और अनेक योद्धाओं का कत्ल कर दिया गया। यह पहला और अन्तिम अवसर था, जब कि अकबर ने ऐसा कत्लेआम करवाया। राजपूत योद्धाओं ने मरने से पूर्व यथा सम्भव मुकाबला किया। जयमल और पट्टा की वीरता को देखते हुए अकबर ने आगरा के किले के मुख्य द्वार के बाहर हाथी पर सवार इन वीरों की प्रस्तर प्रतिमाएँ स्थापित करवाने का आदेश दिया। चित्तौड़ के बाद राजस्थान के सबसे शक्तिशाली किले रणथम्भौर का पतन हुआ। जोधपुर पहले ही जीता जा चुका था। इन विजयों के परिणामस्वरूप बीकानेर और जैसलमेर सहित अनेक राजपूत रियासतों ने अकबर के आगे समर्पण कर दिया। केवल मेवाड़ ने ही संघर्ष करना जारी रखा। बहादुरशाह की मृत्यु के पश्चात् से गुजरात की स्थिति बहुत खराब थी। अपनी उपजाऊ भूमि, उन्नत शिल्प और बाहरी दुनिया के साथ आयात-निर्यात व्यापार का केन्द्र होने के कारण गुजरात बाहर वालों के लिये स्पर्धा का विषय बन चुका था। अकबर ने यह कह कर उस पर अपना अधिकार जमाया कि हुमायूँ उस पर कुछ समय तक राज्य कर चुका था। एक अतिरिक्त कारण यह भी था कि दिल्ली के निकट मिर्जाओं का विद्रोह समाप्त हो जाने के बाद उन्होंने गुजरात में शरण ली थी। अकबर इस बात के लिए तैयार नहीं था कि गुजरात जैसा समृद्ध प्रदेश मुकाबले की शक्ति बन जाये। 1572 में अकबर अजमेर के रास्ते से अहमदाबाद की ओर बढ़ा। अहमदाबाद ने बिना लड़े समर्पण कर दिया। अकबर ने फिर मिर्जाओं की ओर ध्यान दिया, जिन्होंने भड़ौच, बड़ौदा और सूरत पर अधिकार किया हुआ था। खम्बात में अकबर ने पहली बार समुद्र के दर्शन के किए और नाव में सैर की। पुर्तगाली व्यापारियों के एक दल ने पहली बार अकबर से आकर भेंट की। इस समय पुर्तगालियों का भारतीय समुद्रों पर पूरा नियन्त्रण था और उनकी आकांक्षा भारत में साम्राज्य स्थापित करने की थी। अकबर की गुजरात विजय से उनकी आशाओं पर तुषारापात हो गया। जब अकबर की सेनाओं ने सूरत पर घेरा डाला हुआ था, तभी अकबर ने राजा मानसिंह और आम्बेर के भगवानदास सहित 200 सैनिकों की छोटी सी टुकड़ी लेकर माही नदी को पार किया और मिर्जाओं पर आक्रमण कर दिया। कुछ समय के लिए अकबर का जीवन खतरे में पड़ गया, लेकिन उसके आक्रमण की प्रचण्डता से मिर्जाओं के पैर उखड़ गये और इस प्रकार गुजरात पर मुगलों का अधिकार स्थापित हो गया। परन्तु, जैसे ही अकबर गुजरात से लौटा, वहाँ विद्रोह फूट पड़ा। यह सुनकर अकबर लौट पड़ा। उसने ऊँटों, घोड़ों और गाड़ियों में यात्रा करते हुए नौ दिन में सारा राजस्थान पार किया और ग्यारहवें दिन अहमदाबाद पहुँच गया। यह यात्रा सामान्यतः 6 सप्ताहों में पूर्ण हो सकती थी। केवल 3,000 सिपाही ही अकबर के साथ पहुँच पाये। इसी छोटी-सी सेना की सहायता से उसने 30,000 सैनिकों की सेना को परास्त किया (1573)। इसके पश्चात् अकबर ने अपना ध्यान बंगाल की ओर केन्द्रित किया। बंगाल तथा बिहार पर अभी भी अफगानों का ही अधिकार था। बंगाल के अफगानों ने उड़ीसा को रौंद डाला था और उसके शासक को भी मार डाला था। लेकिन मुगलों को नाराज होने का मौका न देने के लिए अफ़गान शासक ने औपचारिक रूप से स्वयं को सुल्तान घोषित नहीं किया था और अकबर के नाम का खुतवा पढ़ता रहा था। अफगानों की आन्तरिक लड़ाई और नये शासक दाऊदखाँ द्वारा स्वतन्त्रता की घोषणा से अकबर को वह अवसर मिल गया, जिसकी उसे तलाश थीं। अकबर अपने साथ एक मजबूत युद्धक नावों का बेड़ा लेकर आगे बढ़ा। ऐसा विश्वास किया जाता था कि अफगान सुल्तान के पास बहुत बड़ी सेना है, जिनमें 40,000 सुसज्जित घुड़सवार 1,50,000 पैदल सैनिक, कई हजार बन्दूकें और हाथी तथा युद्धक नावों का विशाल बेड़ा था। यदि अकबर सावधानी से काम न लेता और अफगानों के पास बेहतर नेता होता, तो हो सकता है कि हुमायूँ और शेरशाह की कहानी की ही पुनरावृत्ति होती। अकबर ने पहले पटना पर अधिकार किया और इस प्रकार बिहार में मुगलों के लिए संचार के साधनों को सुरक्षित कर लिया। उसके बाद उसने एक अनुभवी अधिकारी खान-ए-खाना मुनीमखाँ को अभियान का नेता बनाया और स्वयं आगरा लौट गया। मुगल सेनाओं ने बंगाल पर आक्रमण किया और काफी संघर्ष के बाद दाऊदखाँ को शान्ति की सन्धि के लिए विवश कर दिया। उसने शीघ्र ही दुबारा विद्रोह किया। यद्यपि बिहार और बंगाल में मुगलों की स्थिति अभी कमजोर थी, तथापि उनकी सेनाएँ अधिक संगठित और बेहतर नेतृत्व वाली थी। 1576 में बिहार में एक तगड़ी लड़ाई में दाऊदखाँ पराजित हुआ और उसी समय मार डाला गया। इस प्रकार उत्तर भारत में अन्तिम अफगान शासन का पतन हुआ। इसी के साथ अकबर के साम्राज्य विस्तार का पहला दौर भी समाप्त हुआ। प्रशासनगुजरात विजय के बाद के दशक में अकबर को साम्राज्य की प्रशासनिक समस्याओं की ओर ध्यान देने का समय मिला। शेरशाह द्वारा स्थापित पद्धति में इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद व्यवधान आ गया था। इस प्रकार अकबर को प्रशासन को नये सिरे से ठीक करना था।अकबर के सामने सबसे बड़ी समस्या भी भू-राजस्व के प्रशासन की थी। शेरशाह ने ऐसी पद्धति का प्रचलन किया था, जिसमें कृषि भूमि की पैमाइश की जाती थी तथापि एक मुख्य दरतालिका (रय) निर्धारित की जाती थी। जिसके आधार पर भिन्न-भिन्न अनाजों की उत्पादकता को ध्यान में रखकर लगान तय किया जाता था। अकबर ने शेरशाह की पद्धति को ही अपनाया। लेकिन कुछ समय बाद अनुभव किया गया कि बाजार भावों को निर्धारित करने में काफी समय लग जाता है, जिससे काश्तकारों को बड़ी परेशानी होती है और फिर कीमतों का निर्धारण शाही दरबार के आस-पास की कीमतों पर आधारित होता था, जो अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों की कीमतों से अधिक होती थी। इससे काश्तकारों को अधिक अंश कर के रूप में देना पड़ता था। अतः अकबर ने वार्षिक अनुमान पद्धति को फिर से लागू किया। कानूनगो जो परम्परागत रूप से जमींदार होते थे तथा अन्य स्थानीय अफसरों, जो स्थानीय परिस्थितियों व हालात से परिचित होते थे, को वास्तविक उत्पादन, खेती की स्थिति, स्थानीय कीमतों आदि की सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया। लेकिन ज्यादातर कानूनगो ईमानदार नहीं थे तथा वे अक्सर वास्तविक आंकड़े को छिपा जाते थे। प्रतिवर्ष लगान का अनुमान लगाने की पद्धति के कारण काश्तकारों और राज्य दोनों को ही परेशानी थी। गुजरात से लौटने के पश्चात् (1573) अकबर ने भू-राजस्व पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया। समस्त उत्तर-भारत में ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की गई, जिन्हें करोड़ी कहा जाता था। एक करोड़ दाम (रू. 2,50000) कर के रूप में एकत्र करना उनका उत्तरदायित्व था। वे कानूनगो द्वारा दिये गये तथ्यों आंकड़ों की भी जाँच करते थे। वास्तविक उत्पादन, स्थानीय कीमतें, उत्पादकता आदि पर उनकी सूचना के आधार पर, अकबर ने 1580 में दहसाला नाम की नयी प्रणाली लागू की। इस प्रणाली के अन्तर्गत अलग-अलग फसलों के पिछले दस (दह) वर्ष के उत्पादन और इसी अवधि में उनकी कीमतों का औसत निकाला जाता था। इसी औसत उपज का एक तिहाई राजस्व होता था। इस औसत उत्पादन का एक तिहाई राज्य का हिस्सा होता था। किन्तु राज्य की माँग का भुगतान नकदी में होता था। राज्य के हिस्से की नकदी में गणना पिछले दस वर्षों की मूल्य-तालिका के औसत के आधार पर की जाती थी। इस प्रकार प्रति बीघे उत्पादन में राज्य के हिस्से का निर्धारण मनों में किया जाता था, जिसे कीमतों के औसत के आधार पर प्रति बीघा रूपयों में परिवर्तित कर दिया जाता था। बाद में इस प्रणाली में और सुधार किया गया। इसके लिए न केवल स्थानीय कीमतों को आधार बनाया गया, बल्कि एक ही तरह के कृषि-उत्पादन वाले परगनों को विभिन्न कर हलकों में विभाजित किया गया। इस प्रकार काश्तकार को भू-राजस्व स्थानीय कीमत और स्थानीय उत्पादन के अनुसार देना होता था। इस प्रणाली के कई लाभ थे। जैसे ही काश्तकार द्वारा बोये गये खेत की लोहे के छल्लों से जुड़े बाँसों द्वारा पैमाइश हो जाती थी, काश्तकार और राज्य दोनों को यह पता चल जाता था कि कर की राशि कितनी होगी। यदि सूखा या बाढ़ आदि के कारण फसल खराब हो जाती थी, तो काश्तकार को राजस्व में छूट मिलती थी। माप और उस पर आधारित कर-निर्धारण की प्रणाली को जब्ती प्रणाली कहा जाता था। अकबर ने इस प्रणाली को लाहौर से इलाहाबाद तक व मालवा तथा गुजरात के क्षेत्रों में लागू किया। दह-साला प्रणाली जब्ती प्रणाली का विकसित रूप थी। अकबर के शासनकाल में कर-निर्धारण की अन्य पद्धतियाँ भी अपनायी गईं। सबसे पुरानी और सामान्यतः प्रचलित प्रणाली बटाई अथवा गल्ला बख्शी कहलाती थी। इस प्रणाली के अन्तर्गत गल्ले को काश्तकारों और राज्य में निश्चित अनुपात में बाँट लिया जाता था। उत्पादन को गहाई के पश्चात् या उस समय जब काटने के पश्चात् उसके गट्ठर बाँध दिए जाते थे अथवा कटाई से पूर्व कभी भी विभाजित कर दिया जाता था। यह प्रणाली काफी सीधी और आसान थी, लेकिन इसके लिए काफी बड़ी संख्या में ईमानदार कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती थी, जिन्हें अनाज के पकते समय और बटाई के समय खेतों में उपस्थित रहना पड़ता था। कुछ परिस्थितियों में किसानों को जब्ती या बटाई प्रणाली चुनने की छूट होती थी। उदाहरण के लिए जब खेती नष्ट हो जाती थी, तो किसानों को इस प्रकार की छूट दी जाती थी। बटाई प्रणाली के अन्तर्गत किसानों को उपज या नकदी में कर-भुगतान की छूट थी, यद्यपि राज्य नकदी में कर लेना बेहतर समझता था। कपास, नील, तिलहन, ईख जैसी उपज पर तो नकद ही कर लिया जाता था। इसीलिए इन्हें तिजारती फसलें कहा जाता था। अकबर के शासनकाल में एक तीसरी प्रणाली नसक भी काफी प्रचलित थी, लेकिन इसके विषय में निश्चित जानकारी नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रणाली किसानों द्वारा पिछले वर्षों में किए गए भुगतान के आधार पर कच्चे अनुमान पर आधारित थी। इसीलिए कतिपय आधुनिक इतिहासकारों का मत है कि यह कर निर्धारण की विशिष्ट प्रणाली नहीं थी बल्कि कृषि कर का लेखा-जोखा करने की प्रणाली थी। अन्य विद्वानों के मत में यह प्रणाली खेती के निरीक्षण और पिछले अनुभवों पर आधारित अनुमानित कर निर्धारण की प्रणाली थी, जो गाँव को सामूहिक रूप से भुगतान करना होता था। कर-निर्धारण की इस कच्ची प्रणाली को कंकूत भी कहा जाता था। कर-निर्धारण की कई अन्य प्रणालियाँ भी अलग-अलग क्षेत्रों में प्रचलित रहीं। भू-राजस्व निर्धारित करते समय बुआई की निरन्तरता का भी ध्यान रखा जाता था। जिस जमीन पर हर साल बुआई होती थी, उसे पोलज कहा जाता था। जब उस पर बुआई नहीं होती थी, उसे परती कहा जाता था। परती जमीन की बुआई होने पर कर की पूरी दर (पोलज) देनी पड़ती थी। जब जमीन दो-तीन साल तक बिन बोई रहती थी, तो उसे दाचर कहा जाता था और उससे अधिक समय तक काश्त न होने पर वह बंजर कहलाती थी। इस जमीन पर कर रियायती दरों पर लगाया जाता था या उस पर पाँचवें या आठवें साल पोलज दर लगाई जाती थी। इस प्रकार राज्य परती जमीन पर खेती करने को प्रोत्साहित करता था। जमीन को उपज के आधार पर अव्वल, मध्यम और खराब इन तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता था। औसत उपज के एक तिहाई हिस्से पर राज्य का अधिकार होता था। किन्तु इस मात्रा में भूमि की उत्पदकता तथा कर निर्धारण की पद्धति के अनुसार अन्तर भी होता रहता था। अकबर काश्तकारी की उन्नति और विस्तार में बहुत रुचि लेता था। वह आमिलों को काश्तकारों से पितृवत व्यवहार करने को कहता था। आमिलों को हिदायत थी कि आवश्यकता पड़ने पर वे काश्तकारों को बीज, औजार तथा मवेशी आदि की व्यवस्था हेतु ऋण (तकावी) प्रदान करें। इन ऋणों को आसान किश्तों में वापस लिया जाता था। यह किसानों को अधिक से अधिक जमीन को जोत में लाने और घटिया फसलों के स्थान बढ़िया फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहन देना भी उसके उत्तरदायित्वों में से एक था। इसके लिए उस क्षेत्र के जमींदारों को भी सहयोग प्राप्त करने के लिए कहा जाता था। जमींदारों को पैदावार का कुछ अंश स्वयं लेने का वंशागत अधिकार प्राप्त था। किसानों को भी जुताई-बुआई का अधिकार वंशागत था और वे जब तक कर देते रहते थे, उन्हें बेदखल नहीं किया जा सकता था। दह-साला प्रणाली में दस सालों के लिए एक ही दर पर कर निर्धारित नहीं किये जाते थे। यह स्थायी भी नहीं होती थी। परन्तु, फिर भी अकबर की प्रणाली कुछ परिवर्तनों के साथ सत्रहवीं शताब्दी के अन्त तक मुगल साम्राज्य की नीति रही। जब्ती प्रणाली के प्रारम्भ का श्रेय राजा टोडरमल को जाता है और इसे राजा टोडरमल का बन्दो-बस्त भी कहा जाता है। टोडरमल एक योग्य राजस्व अधिकारी था, जो पहले शेरशाह के अधीन कार्य करता था। अकबर के शासनकाल में टोडरमल के अतिरिक्त कई अन्य सुयोग्य राजस्व अधिकारी भी विद्यमान थे। लेकिन वह योग्य राजस्व अधिकारियों में से एक था। मनसबदारी व्यवस्था तथा सेनाअकबर बिना सुदृढ़ सेना के न तो साम्राज्य का विस्तार कर सकता था और न ही उस पर अपना अधिकार बनाये रख सकता था। इसके लिए अकबर को अपने सैनिक-अधिकारियों और सिपाहियों को सुगठित करने की आवश्यकता थी। अकबर ने इन दोनों लक्ष्यों की पूर्ति मनसबदारी प्रणाली से की। इस प्रणाली में प्रत्येक सरदार और दूसरे सैन्य पदाधिकारियों को एक पद (मनसब) प्रदान किया। निम्नतम पद 10 सिपाहियों के ऊपर था और अमीरों के लिए उच्चतम पद 5,000 सिपाहियों पर था। अकबर के शासन काल में उच्चतम मनसब 5,000 से 9,000 कर दिया गया था। साम्राज्य के प्रमुख अमीरों में मिर्जा अजीज कोका तथा राजा मानसिंह ने 9,000 का मनसब प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। औरंगजेब के काल के अन्त तक उच्चतम मनसब अधिकांशतः इसी सीमा रेखा से निर्धारित होते थे। रक्त से संबद्ध राजकुमारों को बड़े मनसब दिए जाते थे। इन दो पदों को दो वर्गों-जात और सवार में विभाजित किया गया। जात का अर्थ है व्यक्तिगत। इससे व्यक्ति का पद-स्थान तथा वेतन निर्धारित होता था। सवार से घुड़सवारों की संख्या का बोध होता था जो मनसबदार अपने अधीन रखता था। जिस व्यक्ति को अपने जात-पद के अनुपात में सवार रखने का अधिकार होता था, वह प्रथम श्रेणी में आता था, यदि सवारों की संख्या आधी या आधी से अधिक रहती थी, तो वह दूसरी श्रेणी में आता था और उससे नीचे तीसरी श्रेणी होती थी।इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता था कि सवारों की भर्ती उनकी कुशलता व अनुभव के आधार पर की जाये। प्रत्येक सवार का हुलिया (चेहरा) दर्ज किया जाता था और घोड़ों पर शाही निशान दागा जाता था। प्रत्येक मनसबदार को समय-समय पर अपने सैनिकों को शहंशाह द्वारा नियुक्त अधिकारियों के सामने निरीक्षण के लिए लाना पड़ता था। घोड़ों का निरीक्षण बहुत ध्यान से किया जाता था और केवल अरबी और इसकी नस्ल के घोड़े ही रखे जाते थे। प्रत्येक 10 घुड़सवारों के पीछे मनसबदार को 20 घोड़े रखने पड़ते थे। इसका कारण यह था कि कूच के समय घोड़ों को आराम दिया जाता था और युद्ध के समय नयी कुमुक की आवश्यकता होती थी। एक घोड़े वाला आधा सवार समझा जाता था। जब तक 10 : 20 नियम का पालन किया जाता रहा, मुगल घुड़सेना सशक्त रही। इस बात की भी व्यवस्था थी कि मनसबदारों के दलों में सवार मिश्रित अर्थात् मुगल, पठान, हिन्दुस्तानी और राजपूत सभी जातियों के हों। इस प्रकार अकबर ने जाति और संकीर्ण स्थानीयता की भावना को कमजोर करने का प्रयत्न किया। केवल मुगल और राजपूत सरदारों को ही इस बात की अनुमति थी कि वे अपनी टुकड़ियों में केवल मुगल और राजपूत सवार रखें, किन्तु धीरे धीरे मिश्रित सवारों की पद्धति सामान्य रूप से अपना ली गई। घुड़सवारों के अतिरिक्त सेना में तीरन्दाज, बन्दूकची, खन्दक खोदने वाले भी भर्ती किए जाते थे। इनके वेतन अलग-अलग थे। एक सवार का औसत वेतन बीस रूपये प्रति मास था। ईरानी और तुरानियों को कुछ अधिक वेतन मिलता था। पैदल सेनिक को तीन रूपये प्रति माह मिलते थे। सिपाहियों के वेतन को मनसबदार के व्यक्तिगत वेतन में जोड़ दिया जाता था। कभी-कभी मनसबदारों को वेतन नकद भी दिया जाता था। अकबर जागीदार प्रथा को पसन्द नहीं करता था, किन्तु वह इसे समाप्त नहीं कर सका क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं, क्योंकि जागीर पर अधिग्राही का वंशगत अधिकार नहीं होता था और उसने उस क्षेत्र में विद्यमान अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं होता था, इसलिए जागीर देने का केवल यही अर्थ था कि राज्य को देय भू-राजस्व जागीदार को दिया जाता था। मुगलों के अन्तर्गत विकसित मनसबदारी एक ऐसी विशिष्ट व अनूठी प्रणाली थी, जिसकी मिसाल बाहर के देशों में नही मिलती। मनसबदारी प्रथा का उद्भव सम्भवतः चंगेज खाँ से हुआ। जिसने अपनी सेना को दशमलव पद्धति के आधार पर सुगठित किया था। उसके अन्तर्गत निम्नतम सैन्य टुकड़ियों में सैनिकों की संख्या दस तथा उच्चतम सैन्य टुकड़ी में 10,000 (तोमान) होती थी। इसका सेनापति खान कहलाता था। मंगोल पद्धति ने कुछ हद तक दिल्ली सल्तनत की सैन्य व्यवस्था को भी प्रभावित किया था। जिसका प्रमाण सदी व हजारों पद संज्ञाऐं हैं। इनके अन्तर्गत क्रमशः 100 तथा 1,000 सैनिक होते थे। मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किस समय हुआ इस विषय में काफी वाद-विवाद हैं। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि इस व्यवस्था का प्रारम्भ अकबर द्वारा अपने शासनकाल के 19वें वर्ष (1599) में किया गया था। लगभग इसी काल में उसने जात-पात सवार श्रेणी का भी प्रचलन किया। यद्यपि बहुत से इतिहासकारों के मत में सवार श्रेणी का प्रचलन अकबर द्वारा वाद में किया गया था। किन्तु आधुनिक शोधों से प्रदर्शित होता है कि दोनों ही श्रेणियाँ एक ही समय में प्रचलित हुई थीं। 500 से नीचे जात श्रेणी वालों को मनसबदार कहा जाता था। 500 से ऊपर व 2500 से नीचे जात श्रेणी होने पर अमीर कहे जाते थे तथा 2500 व उससे ऊपर के उच्चतम जात श्रेणियों के अधिकरियों को अमीर-ए-उम्दा या उम्दा-ए-आजम कहा जाता था। किन्तु मनसबदार शब्द इन तीनों ही श्रेणियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। पद-स्थिति के वर्गीकरण के अतिरिक्त इस वर्गीकरण की एक अन्य विशेषता थी वह यह कि 5000 जात श्रेणी के मनसबदार के अन्तर्गत 500 जात श्रेणी तक के मनसबदार काम कर सकते थे। इसी प्रकार जिसका मनसब 8000 जात श्रेणी होता था उसके अन्तर्गत 800 जात श्रेणी तक के ही मनसबदार रह सकते थे। उक्त श्रेणियाँ अचल नहीं थी अर्थात् उनमें पदोन्नति की काफी गुन्जाइश रहती थी। मनसबदारों की नियुक्ति साधारणतया निम्न मनसब पर होती थी। किन्तु उसकी बराबर पदोन्नति होती रहती थी। इसमें व्यक्ति के गुण तथा सम्राट की कृपा दृष्टि दोनों का ही योगदान रहता था। कभी-कभी मनसब में कमी करके मनसबदार को प्रतिदण्डित भी किया जाता था। सैन्य व प्रशासन दोनों ही प्रकार के पदों के लिए नियुक्ति और पदोन्नति के समान नियम लागू होते थे। इस प्रकार लोगों की नियुक्ति निम्न मनसब पर होती थी तथा उन्नति करते-करते अमीर या अमीर-ए-उम्दा के पद पर पहुँच जाते थे। इस प्रकार प्रतिभाशालियों के लिये कुछ हद तक उन्नति का द्वार खुला था। अपने व्यक्तिगत वेतन में से ही मनसबदार को एक निश्चित संख्या में घोड़े, हाथी वह बोझा ढोने वाले जानवर (ऊँट व खच्चर आदि) तथा गाड़ियाँ रखनी पड़ती थीं। इसके भी विशिष्ट नियम थे। जिस मनसबदार का 5000 जात का मनसब होता था, उसे 340 घोड़े, 100 हाथी, 800 ऊँट, 100 खच्चर तथा 160 गाड़ियाँ रखनी होती थीं। बाद में इन की व्यवस्था केन्द्रीय स्तर पर की जाने लगी। किन्तु उसका व्यय-मनसबदार के वेतन से ही अदा होता था। घोड़ों का 6 श्रेणियों में वर्गीकरण होता था तथा हाथियों को उनकी नस्ल के आधार पर 5 श्रेणियों में वगीकृत किया जाता था। घोड़ों तथा हाथियों की संख्या व प्रकार के बारे में अत्यन्त सावधानी पूर्वक नियम निर्धारित किये गये थे। वस्तुतः घोड़े तथा हाथियों का महत्व बहुत अधिक था। सैन्य व्यवस्था के कुशल संचालन में वे अपरिहार्य थे। उस काल में तोपखाने के महत्व में दिन ब दिन वृद्धि होने के पश्चात् भी सेना का मुख्य आधार घुड़सवार सेना तथा हाथी ही थे। भारवाहक के पशुओं की सेना के यातायात के लिये अनिवार्य रूप से आवश्यकता पड़ती थी। इन सब खर्चों को वहन करने के लिए मुगल मनसबदार को बड़ा अच्छा वेतन मिलता था। वह मनसबदार जिसका जात पद 5000 होता था 30000 हजार प्रतिमाह वेतन पाता था। 3000 जात मनसब होने पर 11000 तथा जात पर 1000 होने पर 8200 रूपया प्रतिमाह वेतन मिलता था। यहाँ तक कि 100 जात वाले सदी को भी 1000 वार्षिक वेतन मिलता था। अनुमानतः इस वेतन का एक चौथाई भाग यातायात से सम्बन्धित संसाधनों पर खर्च हो जाता था। इसके बाद भी मुगल मनसबदार को दुनिया में सबसे अच्छा वेतन मिलता था। अकबर के पास घुड़सवारों की एक बड़ी सेना थी, जो उसके अंगरक्षक का कार्य करती थी। उसके पास बहुत बड़ा अस्तबल था। उसके पास एक टुकड़ी कुलीन घुड़सवारों की भी थी। यह टुकड़ी उन सैनिकों की थी, जो उच्च वंश से सम्बन्धित थे, किन्तु जिनके पास इतनी सुविधाएँ नहीं थी कि अपनी टुकड़ी का निर्माण कर सके या इसमें वे लोग थे जिन्होंने अकबर को प्रभावित किया था। उन्हें आठ से दस घोड़े रखने का अधिकार था और उन्हें लगभग 800 रूपये प्रति मास वेतन भी मिलता था। वे केवल शहनशाह के प्रति उत्तरदायी थे और उनकी हाजिरी भी अलग होती थी। इन सैनिकों की तुलना मध्य-युगीन यूरोप के ‘‘नाइट्स’’ से की जा सकती है। अकबर को घोड़ों और हाथियों का बहुत शौक था। उसके पास एक वृहद् तोपखाना था। तोपों में उसकी विशेष रुचि थी। उसने खोली जा सकने वाली तोपों का निर्माण करवाया, जिन्हें हाथी या ऊँट ढो सकते थे। उसके पास घेरे के समय किले की दीवारों को तोड़ने वाली भारी तोपें भी थीं। इनमें से कुछ इतनी भारी थी कि उन्हें खींचने के लिए 100 या 200 बैल और बहुत से हाथी इस्तेमाल करने पड़ते थे। अकबर जब भी राजधानी से बाहर जाता था, एक मजबूत तोपखाना उसके साथ चलता था। इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि अकबर की नौ-सेना का संगठन करने की कोई योजना थी या नहीं। मजबूत नौ-सेना का अभाव मुगल साम्राज्य की हमेशा कमजोरी रही। यदि अकबर को समय मिला होता, तो सम्भवतः वह इस ओर भी ध्यान देता। उसने युद्ध के लिए नावों का एक बेड़ा अवश्य गठित किया था। जिसका प्रयोग उसने पूर्व की ओर किए गए अपने अभियानों में किया। इनमें से कुछ नावें 30 मीटर लम्बी थीं और 350 टन तक बोझ ढो सकती थीं। प्रशासन का गठनस्थानीय-प्रशासन में अकबर ने कोई परिवर्तन नहीं किया। परगना और सरकार की स्थिति पहले जैसी रही। सरकार के मुख्य अधिकारी फौजदार और अमलगुजार होते थे। फौजदार का काम न्याय और व्यवस्था बनाए रखना होता था और अमल गुजार भू-राजस्व के निर्धारण तथा वसूली का काम करता था। साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को जागीर, खालिसा और इनाम में विभाजित किया गया था। खालिसा क्षेत्रों की आय सीधी शाही खजाने में जाती थी। इनाम क्षेत्र पर जो आय होती थी, वह विद्वानों और पीरों आदि को दी जाती थी। जागीर, अमीरों, शाही परिवार के सदस्यों और बेगमों को दी जाती थीं। अमल गुजार का यह उत्तरदायित्व होता था कि प्रत्येक प्रकार की जमीन की देखभाल करे ताकि कर निर्धारण और वसूलने के नियमों का पालन समान रूप से हो सके। केवल स्वायत्ता प्राप्त राजाओं को ही अपने क्षेत्र में पारंपरिक राजस्व प्रणाली का पालन करने की छूट थी। अकबर उन्हें भी शाही प्रणाली अपनाने के लिए उत्साहित करता था। अकबर ने केन्द्रीय और प्रान्तीय प्रशासन के गठन की ओर बहुत ध्यान दिया। उसके केन्द्रीय शासन की पद्धति दिल्ली सल्तनत के केन्द्रीय शासन के ढाँचे पर ही आधारित थी, किन्तु विभिन्न विभागों के कार्यों का सावधानी से पुनर्गठन किया गया और कार्य सम्पादन के लिए बहुत स्पष्ट नियम बनाये गये। इस प्रकार अकबर ने शासन प्रणाली को नया रूप प्रदान करके उसमें नयी जान फूँक दी। मध्य एशियाई और तैमूरवंशी परम्परा में वजीर सर्वाधिक शक्तिशाली होता था और उसके अधीन विभिन्न विभागों के सर्वोच्च अधिकारी काम करते थे। वह प्रशासन और शासक के बीच सम्पर्क की प्रमुख कड़ी था। धीरे-धीरे सैनिक विभाग एक अलग विभाग बन गया। न्याय विभाग हमेशा से ही अलग विभाग होता था। इस प्रकार व्यवहार में एक सर्वशक्तिशाली वजीर रखने की परम्परा समाप्त हो गई थी, परन्तु वकील के रूप में बैरमखाँ ने सर्वशक्तिशाली वजीर के अधिकारों का ही उपयोग किया था। अकबर ने केन्द्रीय प्रशासन के ढाँचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। उसने विभिन्न विभागों को अलग-अलग अधिकार दिए ताकि एक-दूसरे से उनका सन्तुलन बना रहे और एक-दूसरे पर नजर भी रहे। यद्यपि वकील का पद समाप्त नहीं किया गया, लेकिन उसके सब अधिकार समाप्त कर दिए गए और वह केवल सम्मान सूचक पद रह गया, जो समय-समय पर महत्वपूर्ण अमीरों को प्रदान किया जाता था। किन्तु इस पद के अधिकारी का प्रशासनिक विषयों में कोई दखल नहीं होता था। राजस्व विभाग का प्रमुख वजीर होता था। यह आवश्यक नहीं था कि हमेशा इस पर पद उच्च श्रेणी का अमीर ही नियुक्त किया जाये। कई अमीरों के पास वजीर से भी ऊँचे मनसब होते थे। वस्तुतः अकबर के काल में वजीर शासक का मुख्य सलाहकार नहीं रह गया था, वरन् वह राजस्व के मामलों का विशेषज्ञ होता था। इस बात पर बल देने के लिए ही अकबर ‘‘वजीर’’ के स्थान पर दीवान या दीवान-ए-आला पद संज्ञाओं का प्रयोग करता था। कभी-कभी एक साथ कई व्यक्तियों को दीवान का कार्य संयुक्त रूप से सौंप दिया जाता था। दीवान समस्त आय और व्यय के प्रति उत्तरदायी होता था और खालिसा, जागीर और इनाम जमीनों का केन्द्रीय अधिकारी होता था। सैनिक-विभाग का प्रधान अधिकारी मीर बख्सी कहलाता था। उमरा वर्ग का प्रमुख मीर बख्सी होता था, न कि दीवान इसलिए प्रमुख अमीरों को ही यह पद दिया जाता था। मनसब पदों पर नियुक्ति और पदोन्नति आदि की सिफारिश शहंशाह के पास मीर बख्सी के माध्यम से ही की जाती थी। सिफारिश मन्जूर हो जाने पर पुष्टि के लिए तथा मनसब के अनुरूप जागीर प्रदान करने के लिए दीवान के पास भेजा जाता था। पदोन्नति के लिए भी यही पद्धति अपनायी जाती थी। साम्राज्य की गुप्तचर संस्थानों का प्रमुख भी मीर बख्सी ही होता था। साम्राज्य के प्रत्येक विभाग में गुप्तचर अधिकारी (बरीद) और सन्देश लेखक (वाकयनवीस) नियुक्त किए जाते थे। उनकी सूचनाएँ मीर बख्सी के माध्यम से दरबार में पहुँचाई जाती थी। इससे यह स्पष्ट है कि दीवान और मीर बख्सी समान पदों पर थे और एक-दूसरे के पूरक थे और एक-दूसरे के काम पर नजर रखते थे। तीसरा महत्वपूर्ण अधिकारी मीर सामाँ होता था। यह शाही परिवार के कामों को देखता था, जिसमें हरम के लिए आवश्यक भोजन-सामग्री और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति भी सम्मिलित थी। इनमें से बहुत-सी वस्तुओं का उत्पादन शाही कारखानों में होता था। सम्राट के अत्यन्त विश्वनीय सरदारों को ही इस पद पर नियुक्त किया जाता था। दरबार की मर्यादा का पालन कराने और शाही अंगरक्षकों का निरीक्षण भी इसी अधिकारी का उत्तरदायित्व था। चौथा महत्वपूर्ण विभाग न्याय-विभाग था, जिसका प्रमुख अधिकारी प्रधान काजी होता था। इसपद को कभी-कभी मुख्य सद्र के पद के साथ मिला दिया जाता था। समस्त कल्याण संस्थाओं की देखरेख तथा धार्मिक अनुदानों की व्यवस्था सद्र के ही कार्य क्षेत्र में आते थे। इस प्रकार इस पद में अपरिमित शक्ति और संरक्षण क्षमता निहित थी। यह विभाग अकबर के प्रधान काजी अब्दुलनबी के भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के कारण बदनाम हो गया। विभिन्न व्यक्तियों को प्रदत्त अनुदानों का सावधानी से अध्ययन करने के बाद अकबर ने जागीर और खालिसा जमीन से इनाम की जमीन को अलग कर दिया तथा इनाम-जमीन के वितरण और प्रशासन के लिए उसने साम्राज्य को 6 हलकों में विभाजित कर दिया। इनाम की दो विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं। पहली यह कि अकबर ने सोच समझ कर यह नीति अपनायी कि इनाम की जमीन का अनुदान बिना किसी धार्मिक भेदभाव के दिया जाए। अनेक हिन्दू मठों को दिए गए अनुदानों की सनदें अभी भी सुरक्षित हैं। दूसरी विशेषता यह थी कि अकबर ने यह नीति अपनाई कि इनाम में आधी जमीन ऐसी हो जो परती पड़ी हो, लेकिन, कृषि-योग्य हो। इस प्रकार इनाम पाने वाले को खेती के विस्तार के लिए प्रोत्साहित किया गया। प्रजा से मिलने तथा अधिकारियों से भेंट करने के लिए अकबर ने अपनी समय-सारणी बड़ी सावधानी से बनायी। उसके दिन की शुरूआत महल के झरोखे पर दर्शन देने से होती थी। शहंशाह के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होते थे और आवश्यकतानुसार अपनी फरियाद कर सकते थे। इन फरियादों पर तुरन्त या बाद में दीवान-ए-आम में कार्यवाही होती थी, जो दोपहर तक चलता था। उसके पश्चात् शहंशाह भोजन और आराम के लिए अपने कक्ष में चले जाते थे। मन्त्रियों के लिए अलग-अलग समय निर्धारित होता था। गोपनीय मन्त्रणा के लिए उनको अकबर के गुसलखाने के निकट स्थित एक कक्ष में बुलाया जाता था। धीरे-धीरे गोपनीय मन्त्रणा कक्ष गुसलखाने के नाम से मशहूर हो गया। 1580 में अकबर ने सम्पूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित कर दिया। ये थे - बंगाल, बिहार, इलाहाबाद, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, काबुल, अजमेर, मालवा और गुजरात। प्रत्येक सूबे में एक सूबेदार, एक दीवान, एक बख्शी, एक सद्र, एक काजी और वाकया-नवीस की नियुक्ति की गई। इस प्रकार नियन्त्रण और सन्तुलन के सिद्धान्त पर आधारित सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था सूबों में भी लागू की गई। राजपूतों के साथ सम्बन्धराजपूतों के साथ अकबर के सम्बन्धों को देश के शक्तिशाली राजाओं और जगीरदारों के प्रति मुगल-नीति के वृहद पृष्ठभूमि के सन्दर्भ में देखना होगा। जब हुमायूँ हिन्दुस्तान लौटा, तो उसने सोच समझ कर इन तत्वों को अपनी ओर मिलाने की नीति अपनायी। अबुल फजल कहता है कि ‘‘जमींदारों का सौहार्द्र’’ प्राप्त करने के लिए उसने वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किए।’’ उदाहरण के लिए ‘‘जब हिन्दुस्तान के बड़े जमींदारों में से एक जमालखाँ मेवाती ने हुमायूँ को समर्पण किया तो हुमायूँ ने उसकी बेटी से स्वयं विवाह किया और छोटी बहन का विवाह बैरमखाँ से किया।’’ बाद में अकबर ने इस नीति को आगे बढ़ाया।आमेर का शासक भारमल अकबर के राज्यारोहण के फौरन बाद आगरा के दरबार में उपस्थित हुआ था। तरुण शासक पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ा था क्योंकि उस समय एक पागल हाथी के भय से लोग इधर-उधर भाग रहे थे, किन्तु भारमल के नेतृत्व में सैनिक दृढ़ता से वहाँ खड़े रहे। 1562 में जब अकबर अजमेर जा रहा था तो उसे पता लगा कि स्थानीय मुगल सूबेदार भारमल को परेशान कर रहा था। भारमल स्वयं अकबर की आवभगत को आया और अपनी छोटी बेटी हरखा बाई का अकबर से विवाह करके बादशाह से अपने सम्बन्धों को पुष्ट किया। मुस्लिम शासकों और हिन्दू अधिपतियों की कन्याओं के मध्य विवाह असाधारण बात नहीं थी। चौदहवीं और पन्द्रहवीं शताब्दी में हुए इस प्रकार के अनेक वैवाहिक सम्बन्धों का उल्लेख पिछले अध्यायों में किया जा चुका है। जोधपुर के शक्तिशाली राजा मालदेव ने अपनी एक लड़की कनक बाई का विवाह गुजरात के सुल्तान महमूद के साथ किया था और दूसरी लड़की लाल बाई का विवाह सूर शासक सम्भवतः इस्लामशाह सूर के साथ किया था। इनमें से अधिकांश विवाह सम्बन्धित परिवारों के मध्य स्थायी व्यक्तिगत सम्बन्धों को स्थापित करने में सफल नहीं हुए। विवाह के पश्चात् लड़कियों को अक्सर भुला दिया जाता था और वे वापस नहीं आती थी। इसके विपरीत अकबर ने दूसरी नीति अपनायी। उसने अपनी हिन्दू पत्नियों को पूरी धार्मिक स्वतन्त्रता दी और उनके पिताओं और सम्बन्धियों को उमरा वर्ग में स्थानीय स्थान प्रदान किया। भारमल को उच्च पद प्राप्त हुआ। उसका पुत्र भगवानदास पाँच हजारी मनसब तक पहुँचा और उसका पोता मानसिंह सात हजारी तक। अकबर ने यह मनसब केवल एक और व्यक्ति को प्रदान किया था और वह था अकबर का कोका भाई (छत्रिय) अजीजखाँ कूका। अकबर ने अन्य प्रकार से भी कछवाहा शासकों से अपने विशेष सम्बन्धों की पुष्टि की। शहजादा दानियाल शैशावास्था में ही भारमल की पत्नियों के पास पालन-पोषण के लिये भेज दिया गया था। 1572 में जब अकबर ने गुजरात पर चढ़ाई की तो आगरा भारमल के सुपुर्द छोड़ दिया गया, जहाँ शाही परिवार की सब स्त्रियों की सुरक्षा का भार उसी पर था। यह सम्मान शासक के किसी सम्बन्धी या अत्यन्त विश्वसनीय अमीर को ही दिया जाता था। परन्तु अकबर ने वैवाहिक सम्बन्धों को शर्त के तौर पर नहीं रखा। रणथम्भौर के हाड़ाओं के साथ अकबर के वैवाहिक सम्बन्ध नहीं थे, फिर भी वे अकबर के कृपा-पात्र थे। राव सुर्जन हाड़ा को गढ़ कटंगा का शासन सौंपा गया था और उसका मनसब 2000 सवारों का था। इसी प्रकार सिरोही और बाँसवाड़ा के शासकों के साथ भी जिन्होंने बाद में समर्पण किया था, अकबर के वैवाहिक सम्बन्ध नहीं थे। अकबर के राजपूतों के प्रति नीति उसकी उदार सहिष्णुता की नीति के साथ सम्बद्ध हो गई। 1564 में उसने जजिया हटा दिया। जिसका प्रयोग कभी-कभी उलमा गैर-मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए किया करते थे। उससे पहले अकबर ने तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त कर दिया था और युद्ध बन्दियों के बलात् धर्म-परिवर्तन की प्रथा को भी खत्म कर दिया था। चित्तौड़ विजय के पश्चात् अधिकांश बड़े राजपूत शासकों ने अकबर के प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया था और उसे वे व्यक्तिगत रूप से सम्मान देते थे। जैसलमेर और बीकानेर के शासकों ने भी अकबर के साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किए। केवल मेवाड़ ही ऐसी रियासत थी जिसमें मुगल प्रभुत्व को मानने से बराबर इंकार किया। यद्यपि चित्तौड़ और उसके आस-पास का मैदानी इलाका मुगल-साम्राज्य के अन्तर्गत आ गया था तथापि उदयपुर और पहाड़ी इलाके, मेवाड़ का अधिकांश भाग, राणा के अधिकार में ही रहे। 1572 में राणा प्रताप उदयसिंह का उत्तराधिकारी बना। अकबर ने राणा प्रताप को मुगल प्रभुत्व स्वीकार कर लेने और दरबार में पेशकश के लिए उनके पास अनेक दूत भेजे। एक बार राणा मानसिंह भी अकबर का दूत बनकर राणा प्रताप के पास गया। राणा ने उसका हार्दिक स्वागत किया। यह कथा कि राणा प्रताप ने राजा मानसिंह का अपमान किया था, ऐतिहासिक तथ्य नहीं है और यह राणा की चारित्रिक विशेषताओं से भी मेल नहीं खाती, क्योंकि राणा साहसी था और अपने विरोधियों से भी शालीनता से पेश आता था। मानसिंह के पश्चात् भगवानदास और फिर राजा टोडरमल राणा के पास गये। राणा ने एक बार समझौते का निर्णय कर लिया था। उसने अकबर द्वारा भेजी गयी पोशाक धारण की और अपने पुत्र अमरसिंह को भगवानदास के साथ अकबर के दरबार में भेंट देने और सेवाएँ अर्पित करने के लिए भेजा। परन्तु उनमें कोई अन्तिम समझौता नहीं हो सका, क्योंकि गर्वीला राणा अकबर की इस माँग को मानने के लिए तैयार नहीं था कि वह स्वयं भेंट के लिए उपस्थित हो। ऐसा भी प्रतीत होता है कि मुगल चित्तौड़ को अपने अधिकार में रखना चाहते थे और यह भी राणा को स्वीकार नहीं था। 1576 के प्रारंभ में अकबर अजमेर की ओर बढ़ा और पाँच हजार सिपाहियों की सेना के साथ मानसिंह को राणा के विरुद्ध अभियान के लिए भेजा। अकबर की इस योजना का पूर्वानुमान करते हुए राणा ने चित्तौड़ तक के प्रदेश को नष्ट-भ्रष्ट करवा दिया था ताकि मुगल सेनाओं को भोजन और चारा न मिल सके। उसने पहाड़ी दर्रो में नाकेबन्दी भी कर ली थी। राणा की तत्कालीन राजधनी कुम्भलगढ़ के रास्ते में पड़ने वाली एक पतली भू-पट्टी हल्दी घाटी में दोनों पक्षों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। कुम्भलगढ़ उस समय राणा की राजधानी थी। चुनी हुई राजपूत सेनाओं के अतिरिक्त हकीम खाँ सूर के नेतृत्व में अफगान फौजी टुकड़ी भी राणा के साथ थी। अतः हल्दी घाटी की लड़ाई हिन्दू और मुसलमानों के बीच अथवा भारतीयों और विदेशियों के बीच का संघर्ष नहीं था। भीलों की एक छोटी सी सेना भी राणा के साथ थी। भील राणा के मित्र थे। अनुमान किया जाता है कि राणा की सेना में 3000 सेनिक थे। राजपूतों और अफगानों के आक्रमण और मारकाट ने मुगल सेना को तितर-बितर कर दिया। परन्तु अकबर के स्वयं वहाँ पहुँचने की अफवाहों को सुनकर मुगल सेना फिर एकत्र हो गई। नयी मुगल कुमुक के आने से राजपूतों का पलड़ा हल्का पड़ने लगा। यह देखकर राणा वहाँ से बचकर निकल गया। मुगल सेना इतनी थक चुकी थी कि उसने राणा का पीछा नहीं किया, परन्तु कुछ समय पश्चात् यह दर्रे से आगे बढ़ी और गोकुण्डा पर अधिकार कर लिया। गोकुण्डा सैनिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान था, जिसे राणा ने मुगल सेना के आने से पहले ही खाली कर दिया था। यह आखिरी अवसर था, जबकि राणा और मुगलों के बीच कड़ा संघर्ष हुआ। इसके बाद राणा ने छापामार युद्ध की नीति अपनाई। हल्की घाटी की लड़ाई में पराजय से स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करने की राणा की प्रतिज्ञा में कमी नहीं आई परन्तु वह जिस उद्देश्य के लिए लड़ रहा था वह पहले ही समाप्त हो चुका था क्योंकि अधिकांश राजपूत रियासतों ने मुगलों की आधीनता स्वीकार कर ली थी। राजपूत राजाओं को साम्राज्य की सेना में लेने और उसके साथ मुगल अमीरों के समकक्ष व्यवहार करने, प्रजा के प्रति विशाल धार्मिक सहिष्णुता तथा अपने भूतपूर्व विरोधियों के साथ शालीनता का व्यवहार करने की नीति से अकबर राजपूत शासकों के साथ अपने सम्बन्धों को सुदृढ़ करने में सफल हुआ था। इसीलिए मुगलों के समक्ष झुकने से राणा के इन्कार का अन्य राजपूत रियासतों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ। उन्होंने इस बात का आभास पा लिया था कि वर्तमान परिस्थितियों में छोटी-छोटी रियासतों के लिए सम्पूर्ण स्वतन्त्रता बनाये रखने का प्रयत्न अधिक समय तक संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त अकबर ने राजपूत राजाओं को पर्याप्त सीमा तक आंतरिक स्वायसत्ता प्रदान की। इस प्रकार अकबर के साम्राज्य स्थापित करने में राजपूत राजाओं को अपने स्वार्थों की कोई हानि नहीं दिखाई पड़ती थी। राणा प्रताप द्वारा अन्य राजपूत रियासतों की सहायता के बिना अकेले ही शक्तिशाली मुगल साम्राज्य का प्रतिशोध राजपूती वीरता और सिद्धान्तों के लिए बलिदान देने की गौरव गाथा है। राणा प्रताप की छापामार युद्ध की पद्धति कालान्तर में दक्खिनी सेनापति मलिक अम्बर और शिवाजी द्वारा एक सुव्यवस्थित युद्ध पद्धति के रूप में विकसित हुईं। राणा प्रताप और अकबर के संघर्ष के विषय में विस्तार में बताने की आवश्यकता नहीं है। कुछ समय तक अकबर राणा पर लगातार दबाव डालता रहा। मुगलों ने मेवाड़ के मित्र और आश्रित रियासतों डुंगरपुर, बाँसवाड़ा सिरोही इत्यादि को रौंद डाला। अकबर ने इन रियासतों के साथ पृथक सन्धियाँ की और इस प्रकार मेवाड़ को और भी अकेला कर दिया। मुगल फौजें राणा का पीछा करती रहीं तथा राणा जंगल-जंगल और घाटी-घाटी घूमता रहा। कुम्भलगढ़ और उदयपुर दोनों पर मुगलों का अधिकार हो गया। राणा को बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ीं, परन्तु भीलों की सहायता के बल पर यह निरन्तर विरोध करता रहा। 1579 में बिहार और बंगाल में अकबर द्वारा किए गए कुछ सुधारों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जबरदस्त विद्रोह हो जाने के कारण राणा पर मुगल दबाव कम कर दिया गया। अव्यवस्था के इस दौर में अकबर के सौतले भाई मिर्जा हकीम ने अवसर का लाभ उठाने के लिए पंजाब पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार अकबर को गम्भीर आंतरिक संकट का सामना करना पड़ा। 1585 में उत्तर-पश्चिम की गम्भीर हो रही स्थिति का अध्ययन करने के लिए अकबर लाहौर गया। वह बारह वर्ष तक वहाँ रहा। 1585 के बाद राणा प्रताप के विरुद्ध कोई अभियान नहीं छेड़ा गया। इस स्थिति का फायदा उठाकर राणा प्रताप ने अपने राज्य का बहुत सा भाग कुम्भलगढ़ और चित्तौड़ के आस-पास के अनेक इलाके पुनः जीत लिये, परन्तु वह चित्तौड़ पर पुनः अधिकार स्थापित न कर सका। इस दौरान उसने आधुनिक डुंगरपुर के निकट चाँवड़ में नई राजधानी स्थापित कीं। 1579 में 51 की आयु में एक सख्त धनुष की प्रत्यंचा बढ़ाते समय अन्दरूनी चोट लग जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मेवाड़ के अतिरिक्त अकबर को मारवाड़ के विरोध का सामना भी करना पड़ा। मालदेव की मृत्यु (1562) के पश्चात् उसके पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए विवाद उठ खड़ा हुआ। मालदेव की सर्वप्रिय रानी से उत्पन्न सबसे छोटा पुत्र चन्द्रसेन गद्दी पर बैठा। मुगलों के दबाव के कारण से रियासत का कुछ भाग अपने बड़े भाइयों को जागीर के रूप में देना पड़ा। किन्तु चन्द्रसेन को यह व्यवस्था पसन्द नहीं आई और कुछ समय पश्चात् ही उसने विद्रोह कर दिया जब अकबर ने मारवाड़ को सीधे मुगल प्रशासन में ले लिया। इसका एक कारण यह था कि अकबर गुजरात के लिए जोधपुर से होकर रसद ले जाने के मार्ग को सुरक्षित रखना चाहता था। विजय के पश्चात् अकबर ने जोधपुर की रक्षा का भार रायसिंह बीकानेरी को सौंपा। चन्द्रसेन ने वीरतापूर्वक मुकाबला किया और गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। लेकिन जल्दी ही उसे मेवाड़ में शरण लेनी पड़ी। वहाँ भी मुगलों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और वह इधर-उधर छिपता रहा। 1581 में उसकी मृत्यु हो गयी। दो वर्ष पश्चात् अकबर ने चन्द्रसेन के बड़े भाई उदयसिंह को जोधपुर भेज दिया। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उदयसिंह ने अपनी लड़की जगत गोसाई या जोधाबाई (जिस नाम से उसे जाना जाता है) का विवाह अकबर के बड़े लड़के सलीम के साथ कर दिया। जगत गोसाई का डोला नहीं भेजा गया था, जैसाकि इस प्रकार के पहले विवाहों में होता रहा था, बल्कि वर राजा के घर बारात लेकर गया और विवाह में अनेक हिन्दू रीतियाँ की गईं। यह कार्य अकबर के लाहौर-प्रवास के समय हुआ था। बीकानेर और बूँदी के शासकों के साथ भी अकबर के घनिष्ठ व्यक्तिगत सम्बन्ध थे। इन शासकों ने अनेक अभियानों में वीरतापूर्वक भाग लिया था। 1593 में जब बीकानेर के रायसिंह का दामाद पालकी से गिरने के कारण भर गया तो अकबर स्वयं मातमपुर्सी के लिए उनके घर गया और उसकी लड़की को सती होने से रोका क्योंकि उसके बच्चे बहुत छोटे थे। अकबर की राजपूत नीति मुगल साम्राज्य और राजपूत दोनों के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। इस मित्रता ने मुगल साम्राज्य की सेवा के लिए भारत के श्रेष्ठतम वीरों की सेवायें उपलब्ध करायीं। साम्राज्य के स्थिरीकरण और विस्तार में राजपूतों की दृढ़ स्वामिभक्त एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुई। इस मित्रता से राजस्थान में शान्ति बनी रही, जिससे राजपूत अपनी रियासतों की सुरक्षा के प्रति निश्चित होकर साम्राज्य के दूरस्थ इलाकों में सेवारत रह सकते थे। शाही सेवाओं में सम्मिलित होने के कारण साम्राज्य के महत्वपूर्ण पद राजपूत राजाओं के लिए खुले थे। उदाहरणतः आमेर के भगवानदास को लाहौर का संयुक्त सूबेदार बनाया गया, जबकि उसका पुत्र मानसिंह काबुल में नियुक्त हुआ। कालान्तर में मानसिंह को बिहार और बंगाल की सूबेदारी प्रदान की गई। अन्य राजपूत राजाओं को आगरा, अजमेर और गुजरात जैसे सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों का सर्वोच्च प्रशासनिक पद सौंपे गये। साम्राज्य के उमरा वर्ग में शामिल करने के अतिरिक्त उन्हें वंशगत राज्यों के साथ-साथ जागीरें भी प्रदान की गयीं जिससे उनकी आय के स्रोतों में वृद्धि हुई। अकबर की राजपूत नीति का अनुसरण उसके उत्तराधिकारियों - जहाँगीर और शाहजहाँ ने भी किया। जहाँगीर एक राजपूत राजकुमारी का पुत्र था और उसने स्वयं भी एक कछवाहा राजकुमारी और जोधपुर की राजकुमारी से विवाह किया। जैसलमेर और बीकानेर की राजकुमारियों के साथ भी उसका विवाह हुआ। जहाँगीर ने इन रियासतों के शासकों को उच्चतम सम्मान दिया। जहाँगीर की मुख्य उपलब्धि लम्बे समय से चले आ रहे मेवाड़ के झगड़े की समाप्ति थी। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद अमरसिंह मेवाड़ की गद्दी का उत्तराधिकारी बना। अकबर ने अमरसिंह से अपनी शर्तें मनवाने के लिए उसके विरुद्ध अभियान भेजे थे। जहाँगीर को भी दो बार उन पर आक्रमण करने भेजा गया था किन्तु उसे बहुत कम सफलता मिली थी। 1605 में गद्दी पर बैठने के पश्चात् जहाँगीर ने इस विषय में उत्साहपूर्वक कार्य किया। लगातार तीन आक्रमण किये गये किन्तु राणा के साहस को तोड़ा नहीं जा सका। 1613 में जहाँगीर स्वयं अभियान का नेतृत्व करने के लिए अजमेर पहुँचा। शहजादे खुर्रम (बाद में शाहजहाँ) को एक बड़ी सेना देकर मेवाड़ के पहाड़ी इलाकों पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। मुगल सेना के भारी दबाव, इलाके की वीरानी और खेती के विनाश ने अन्ततः अपना प्रभाव डाला। बहुत से सरदार मुगलों के पक्ष में हो गए और अनेक दूसरे सरदारों ने समझौते के लिए राणा पर दबाव डाला। राणा के पुत्र करणसिंह को जहाँगीर के दरबार में भेजा गया था, जहाँ उसका शानदार स्वागत हुआ। जहाँगीर ने अपनी गद्दी से उठकर उसे गले से लगाया और अनेक उपहार दिए। राणा का मान रखने के लिए जहाँगीर ने उसके स्वयं उपस्थित होने पर बल नहीं दिया और न ही उसे शाही सेवा में आने को बाध्य किया गया। युवराज करण को पाँच हजारी का पद दिया गया। यह पद पहले जोधपुर बीकानेर और आमेर के राजाओं को दिया गया था। करण सिंह को 1500 सवारों की टुकड़ों के साथ मुगल सम्राट की सेवा में रहने को कहा गया। चित्तौड़ सहित मेवाड़ का सारा प्रदेश राणा को लौटा दिया गया। परन्तु चित्तौड़ के सैनिक महत्व को देखते हुए यह समझौता हुआ कि किले की मरम्मत नहीं करायी जाएगी। इस प्रकार अकबर द्वारा प्रारम्भ कार्य जहाँगीर ने पूरा कर दिखाया और राजपूतों के साथ मित्रता को और भी मजबूत किया। विद्रोह तथा मुगल साम्राज्य का और अधिक विस्तारअकबर द्वारा प्रवर्तित प्रशासन व्यवस्था, जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है लागू करने का अर्थ था प्रशासन मशीनरी में सुधार लाना। उमरा वर्ग पर अधिक नियंत्रण और सामान्य जनता के हितों की अधिकाधिक रक्षा। इसीलिए यह बहुत से अमीरों को पसंद नहीं आई। क्षेत्रीय स्वतन्त्रता की भावनाएँ अभी भी बहुत से लोगों में विद्यमान थीं। विशेषरूप से गुजरात, बंगाल और बिहार जैसे स्थानों पर यह और अधिक थी, जहाँ स्वतन्त्र राज्यों की स्थापना की लम्बी परम्परा थी। राजस्थान में राणा प्रताप का स्वाधीनता के लिए संघर्ष जारी था। इन परिस्थितियों में अकबर को विद्रोहों की एक श्रंखला का सामना करना पड़ा। पुराने राजवंश के उत्तराधिकारियों द्वारा राज्य को पुनः हस्तगत करने के प्रयत्नों के कारण गुजरात में दो वर्ष तक अशान्ति रहीं, सबसे गम्भीर विद्रोह बंगाल और बिहार में हुआ, जो जौनपुर तक फैल गया। इसका प्रमुख कारण जागीरदारों के घोड़ों को दागने तथा उनकी आय के विवरण के सम्बन्ध में नियमों का सख्ती से पालन किया जाना था। जिसके कारण उनमें भारी असन्तोष उत्पन्न हुआ। धार्मिक नेताओं द्वारा उकसाये जाने के कारण उनका असन्तोष और बढ़ा। ये धार्मिक नेता अकबर के उदार विचारों तथा उस जमीन को वापिस लेने की नीति से परेशान थे। जो उन्होंने कभी गैर-कानूनी तरीकों के हाथिया ली थी और वे उस पर कर इत्यादि नहीं देते थे। अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम ने भी इस विद्रोह को इस उम्मीद में भड़काया कि वह उचित अवसर पर पंजाब पर आक्रमण कर सकेगा। मिर्जा हकीम उस समय काबुल का शासक था। पूर्वी प्रदेशों के अफगान भी विद्रोह में शामिल होने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, क्योंकि वे मुगलों द्वारा अफगान शक्ति के क्षय से विक्षुब्ध थे।इस विद्रोही ने अकबर को दो वर्षों (1580-81) तक उलझाने रखा। उसको बहुत कठिन और नाजुक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय अधिकारियों द्वारा स्थिति को गलत ढंग से संभालने के कारण बंगाल और लगभग सारा बिहार विद्रोहियों के हाथ में चला गया। जिन्होंने मिर्जा हकीम को अपना शासक घोषित कर दिया। उन्होंने किसी उल्मा से एक फतवा भी ले लिया, जिसमें मोमिनों से अकबर के खिलाफ लड़ने के लिए कहा गया था। किन्तु अकबर इस कठिन परिस्थिति से नहीं घबराया उसने टोडरमल के अधीन एक फौज बिहार और बंगाल भेज दी और दूसरी राजा मानसिंह के अधीन मिर्जा हकीम के सम्भावित आक्रमण को रोकने के लिए पश्चिम की ओर रवाना कर दी। टोडरमल साहस और चतुराई से आगे बढ़ा और मिर्जा हकीम के आक्रमण से पहले ही उसने स्थिति पर काबू पा लिया। मिर्जा हकीम 15000 घुड़सवार लेकर लाहौर की तरफ बढ़ा। किन्तु राजा मानसिंह और भगवानदास द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के कारण वह नगर पर अधिकार नहीं कर सका। मिर्जा हकीम की इस उम्मीद पर भी पानी फिर गया कि पंजाब के बहुत से सरदार उसके साथ विद्रोह में शामिल हो जायेंगे। इसी बीच 50000 अनुशासित घुड़सवारों की सेना लेकर अकबर लाहौर पहुँच गया, जिससे मिर्जा हकीम के सामने जल्दी वापस लौटने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं बचा। अकबर ने इस सफलता को यहीं तक सीमित नहीं रखा। वह काबुल की ओर बढ़ा (1581)। यह पहला अवसर था जबकि किसी भारतीय शासक ने इस ऐतिहासिक नगर में कदम रखा। क्योंकि मिर्जा हकीम ने अकबर की प्रभुत्ता स्वीकार करने या उसके सामने उपस्थित होकर स्वामिभक्ति प्रदर्शित करने से इंकार कर दिया और भारतीय सरदार और सैनिक लौटने के लिए उतावले हो रहे थे, अकबर ने काबुल का शासन अपनी बहन को सौंप दिया और भारत लौट आया। एक महिला के हाथ में शासनभार सांपना अकबर की उदारता और उसके सर्कीणता रहित मनोवृत्ति का परिचायक है। विरोधियों पर विजय अकबर की व्यक्तिगत विजय ही नहीं थी, बल्कि इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि नई व्यवस्था ने अपनी जड़ें जमाना शुरू कर दिया है। अकबर अब साम्राज्य के और विस्तार के लिए सोच सकता था। वह दकन की ओर प्रवृत हुआ जिसमें उसकी रुचि बहुत पहले से थी। लेकिन इससे पहले की वह कुछ कर पाता उत्तर-पश्चिम को समस्याओं में पुनः उसको अपना ध्यान लगाना पड़ा। मुगलों का परम्परागत शत्रु अब्दुल्ला खाँ उजबेक मध्य एशिया में शक्ति संयच कर रहा था। 1584 में उसने बदख्शां पर आक्रमण कर दिया, जिस पर तैमूरों का शासन था। लगता था कि उसके बाद काबुल की बारी है। मिर्जा हकीम और बदख्शां से खदेड़े गए तैमूर वंशी राजकुमारों ने अकबर से सहायता की प्रार्थना की लेकिन इससे पहले कि वह इस विषय में कुछ कर सके, मिर्जा हकीम अधिक शराब पीने के कारण काबुल को अव्यवस्थित छोड़ कर मर गया। अब अकबर ने मानसिंह को काबुल पर आक्रमण करने का आदेश दिया और स्वयं सिन्धु नदी की ओर बढ़े उजबेकों के सभी रास्ते बंद करने के ख्याल से उसने कश्मीर (1586) में और बलूचिस्तान की ओर भी सैन्य अभियान भेजे। लद्दाख और बाल्तिस्तान (जिसे तिब्बत खर्द और तिब्बत बुजुर्ग कहा जाता है) सहित सारा कश्मीर मुगलों के अधीन हो गया। बाल्तिस्तान के शासक की पुत्री का विवाह भी सलीम के साथ हो गया। खैबर दर्रे को मुक्त कराने के लिए भी, जिस पर विद्रोही कबीलियों ने अधिकार कर रखा था, आक्रमण किया गया। इनके विरुद्ध एक आक्रमण में अकबर का विशेष कृपा पात्र राजा बीरबल मारा गया। धीरे-धीरे अफगान विद्रोही समर्पण करने को विवश हो गए। उत्तर-पश्चिम की सुव्यवस्था एवं साम्राज्य की एक सुनियोजित सीमा रेखा, जो भौगोलिक आधार पर लक्षित थी, प्रदान करना, अकबर के ये दो महत्वपूर्ण योगदान हैं। अकबर द्वारा सिन्ध विजय (1590) किये जाने के परिणामस्वरूप सिन्धु नदी के माध्यम से पंजाब के व्यापार का मार्ग प्रशस्त हुआ। अकबर लाहौर में उस समय तक बना रहा (1598) जब तक साम्राज्य को उजबेकों का भय रहा। अब्दुल्ला खाँ की मृत्यु के पश्चात् यह भय सदैव के लिये समाप्त हो गया। उत्तर-पश्चिम की समस्याओं की ओर से निश्चित होने के पश्चात् अकबर ने अपना ध्यान पूर्व, पश्चिम और दकन की ओर प्रवृत्त किया। उड़ीसा पर उस समय अफगान सरदारों का राज्य था। उसे बंगाल के तत्कालीन गर्वनर राजा मानसिंह ने जीता। मानसिंह ने कूच कर बिहार और ढाका सहित पूर्वी बंगाल के बहुत से हिस्से जीते। अकबर के धाय पुत्र मिर्जा अजीज कोका ने पश्चिम में काठियावाड़ को विजित किया। खान-ए-खाना मुनीमखाँ को शहजादा मुराद के साथ दक्षिण की ओर भेजा गया। दक्षिण की घटनाओं का वर्णन एक अलग अध्याय में किया जाएगा। यहाँ इतना कहना पर्याप्त है कि शताब्दी के अन्त तक मुगल साम्राज्य अहमदनगर तक फैल गया था, जिससे मुगलों का मराठों से पहली बार सीधा सम्पर्क हुआ।c इस प्रकार शताब्दी के अन्त तक उत्तरी भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में पिरोया जा चुका था और मुगलों ने दक्षिण में अपना विस्तार कार्य प्रारम्भ कर दिया था। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और भावात्मक एकता थी जो धीरे-धीरे इस विशाल साम्राज्य में पनप रही थीं। एकता की ओरहम देख चुके हैं कि किस प्रकार पन्द्रहवीं शताब्दी में देश के विभिन्न भागों में अनेक शासकों ने गैर-साम्प्रदायिक और धार्मिक संस्कृत साहित्य का फारसी में अनुवाद किया था। स्थानीय भाषाओं के साहित्य को संरक्षण देकर, धार्मिक सहिष्णुता की अधिक उदार नीति अपना कर और कुछ स्थलों पर दरबार तथा सेना में हिन्दुओं को महत्वपूर्ण पद देकर हिन्दुओं और मुसलमानों में पारस्परिक समझ पैदा करने की कोशिश की। हम यह भी देख चुके हैं कि किस प्रकार चैतन्य, कबीर और नानक जैसे सन्तों ने देश के विभिन्न भागों में इस्लाम और हिन्दू धर्म के बीच मूलभूत एकता पर बल दिया और धार्मिक पुस्तकों के शाब्दिक अर्थों की बजाय प्रेम तथा भक्ति पर आधारित धर्म पर बल दिया। इस प्रकार उन्होंने ऐसा वातावरण तैयार किया, जिसमें उदार भावनाएँ और विचार पनप सकते थे तथा जिसमें धार्मिक संकीर्णत्व को अच्छा नहीं समझा जाता था। इसी का वातावरण में अकबर का जन्म और पालन पोषण हुआ।शासन-सूत्र अपने हाथ में लेने के बाद अकबर का पहला काम जजिया को समाप्त करना था। इस्लामी राज्यों में गैर-मुसलमानों को जजिया देना पड़ता था। हालाँकि यह कर भारी नहीं था फिर भी इसे नापसंद किया जाता था, क्योंकि इससे प्रजा में भेद किया जाता था। इसके साथ ही अकबर ने प्रयाग और बनारस जैसे तीर्थ स्थानों पर स्नान पर लगने वाले तीर्थयात्रा कर को भी समाप्त कर दिया। उसने युद्ध बन्दियों के जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की प्रथा को समाप्त कर दिया। इन कार्यों ने एक ऐसे साम्राज्य की आधार शिला रखी जो बिना किसी धार्मिक भेद-भाव के सभी नागरिकों के समान अधिकारों पर आधारित था। अनेक हिन्दुओं को उमरा वर्ग में शामिल करने से साम्राज्य के उदार सिद्धान्त को और भी दृढ़ आधार मिला। इनमें से अधिकांश राजपूत राजा थे, जिनमें से बहुत से अकबर, के साथ वैवाहिक सम्बन्धों से बँध गये और अकबर ने जिनके साथ व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित किये और भी बहुत से लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार मनसब दिये गये। इस दूसरे वर्ग में योग्यतम और प्रसिद्धतम व्यक्ति टोडरमल और बीरबल थे। टोडरमल राजस्व के मामलों का विशेषज्ञ था, जिसने उन्नति करके दीवान का पद प्राप्त किया था। बीरबल अकबर का विशेष कृपापात्र था। अपनी हिन्दू प्रजा के प्रति अकबर का दृष्टिकोण प्रजा के प्रति शासक के व्यवहार के सम्बन्ध में अकबर की मान्यताओं तथा आदर्शों का प्रतिनिधत्व करता है। ये विचार जिनकी अकबर के जीवनीकार अबुल फजल ने बड़ी सावधानी व सक्षमता से व्याख्या की है, तैमूरी, इरानी और भारतीय प्रभुसत्ता सम्बन्धी आदर्शों का एकीकृत रूप है। अबुलफजल के अनुसार एक सच्चे शासक का पद बड़े ही उत्तरदायित्व का है। यह पद दिव्यज्ञान (फर्र-ए-इजादी) पर निर्भर है। अतः ईश्वर और एक सच्चे शासक की पहचान प्रजा के प्रति बिना किसी वर्ग और जाति के भेद-भाव के उसके पितृवत् व्यवहार, छोटे और बड़े हर किसी की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए विशाल हदय, तथा ईश्वर जिसे वास्तविक राजा माना गया है, की प्रार्थना और भक्ति तथा उसमें रोज-ब-रोज बढ़ते विश्वास से होती है। शासक का यह कर्तव्य भी है कि वह एक पद अथवा व्यवसाय के लोगों के दूसरे वर्ग और व्यवसाय के लोगों के कार्यों में हस्तक्षेप को रोक कर समाज में सन्तुलन बनाये रखे। इन सबके अलावा साम्प्रादायिक भेदभाव की भावना की प्रचण्ड आँधी को बढ़ने से रोके। सुलह-कुल अर्थात् सब के लिए शान्ति की नीति अकबर के उपरोक्त विचारों की परिचायक है। अकबर प्रारम्भ से ही धर्म और दर्शन में गहरी रुचि रखता था। शुरु मे अकबर परम्परावादी मुसलमान था। वह राज्य के प्रमुख काजी अब्दुलनबी खाँ का बहुत आदर करता था। अब्दुलनबी उस समय सदर-उस-सदूर था और अकबर ने एक अवसर पर उसकी जूतियाँ भी उठाई थीं। लेकिन जब अकबर वयस्क हुआ तो देश भर में प्रसारित रहस्यवाद ने उसे प्रभावित करना शुरू किया। कहा जाता है कि वह पूरी-पूरी रात अल्लाह का नाम लेता हुआ उसके विचारों में खोया रहता था और अपनी सफलताओं के लिए उसका शुक्रिया अदा करने के लिए वह कई बार सुबह-सुबह आगरा में अपने महल के सामने एक पुरानी इमारत के एक सपाट पत्थर पर बैठ कर प्रार्थना और ध्यान में खो जाता था। धीरे-धीरे वह धर्म के परम्परावादी रूप से विमुख हो गया। जैसा कि हम देख चुके हैं कि उसने जजिया और तीर्थयात्रा कर पहले ही हटा दिया था। उसने अपने दरबार में उदार विचारों वाले प्रतिभाशाली विद्वानों को संरक्षण दिया। इनमें से सर्वाधिक उल्लेखनीय अबुलफजल और उसका भाई फौजी और उनके पिता हैं। महदवी विचारों के साथ सहानुभूति रखने के कारण मुल्लाओं ने इन्हें बहुत परेशान किया था। एक अन्य उल्लेखनीय व्यक्ति महेशदास नामक ब्राह्मण है, जिसे राजा बीरबल की पदवी दी गयी थी। ये हमेशा अकबर के साथ रहते थे। 1575 में अकबर ने अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी में इबादतखाना अर्थात् प्रार्थना भवन बनाया। उसने यहाँ विशेष धर्म गुरूओं, रहस्यवादियों और अपने दरबार के प्रसिद्ध विद्वानों को आमंत्रित किया। अकबर ने उनके साथ धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा की। उसने बार-बार कहा ‘‘ओ बुद्धिमान मुल्लाओं ! मेरा एक मात्र लक्ष्य सत्य की पहचान, सच्चे धर्म के सिद्धान्तों की खोज और उनको प्रकाश में लाना है।’’ यह चर्चा पहले केवल मुसलमानों तक सीमित रही। परन्तु वे अंकुशहीन सिद्ध हुए। मुल्लाओं ने आपस में झगड़ा किया। एक-दूसरे पर चिल्लाये और यहाँ तक कि अकबर की उपस्थिति में ही एक-दूसरे को गाली दी। मुल्लाओं के व्यवहार, उनके अहंकार और दम्भ ने अकबर को खीज से भर दिया। परिणामतः वह मुल्लाओं से और भी दूर हो गया। तब अकबर ने इबादतखाना सब धर्मों - ईसाई, जराथुष्ट्रवादी, हिन्दू, जैन और यहाँ तक कि नास्तिकों के लिए भी खोल दिया। इससे और अधिक विषयों पर चर्चाएँ शुरू हुईं और यहाँ तक कि उन विषयों पर भी चर्चाएँ हुई जिन पर सब मुगलमान एकमत थे जैसे कि क्या कुरान अन्तिम दैवी पुस्तक है और मुहम्मद इसके पैगम्बर है, पुनर्जन्म, ईश्वर की प्रकृति आदि। इससे धर्म गुरू भयभीत हो गये और अकबर द्वारा इस्लाम त्यागने की इच्छा की अफवाहें फैलाने लगे। एक आधुनिक लेखक का विचार है कि ‘‘अकबर के धैर्य और खुले विचारों की अलग धर्मों के लोगों ने अलग-अलग व्याख्याएँ कीं। इबादतखाने से उसे अपने विचारों के लिए श्रेय के स्थान पर बदनामी ही अधिक मिली। इसी समय मुख्य सदर अब्दुलनबी के खिलाफ तहकीकात हुई जो कल्याण कार्यों हेतु भूमि ‘‘मदद-ए-मआश’’ को बाँटने में बहुत भ्रष्ट और अत्याचारी निकला। उसने भ्रष्टाचार और अनाचार से बहुत सम्पत्ति अर्जित कर ली थी। वह धर्मान्ध था और इसलिए उसने शियाओं और मथुरा के एक ब्राह्मण को उनके विश्वासों के कारण फाँसी की सजा दे दी थी। ऐसी स्थिति में सबसे पहले अब्दुलनबी के अधिकार छीन लिए गये और मदद-ए-मआश को बाँटने के लिए प्रत्येक सूबे में एक-एक सदर की नियुक्ति की गई। जल्दी ही उसे बर्खास्त कर दिया गया और उसे हज के लिए मक्का जाने का आदेश दिया गया। लगभग इसी समय 1579-80 में पूर्व में विद्रोह हुआ। काजियों ने अकबर को धर्म-विरोधी कहते हुए अनेक फतवे दिये। अकबर ने विद्रोह को कुचल दिया और काजियों को कड़ी सजायें दीं। मुल्लाओं से निपटने के लिए अपनी स्थिति और अधिक मजबूत करने के ख्याल से मजहर की उद्घोषणा की जिसमें कहा गया कि यदि कुरान की व्याख्या में समर्थ विद्वानों (मुजतहिद) में परस्पर मतभेद हो तो अकबर ‘‘सर्वाधिक न्यायशील और विवेकी’’ होने के नाते और खुदा की नजरों में इसका दर्जा मुनत हिन्दों से ऊँचा होने के कारण उनमें से किसी भी व्याख्या को जो देश के लाभ में और बहुत संख्या के हित में’’ हो स्वीकार कर सकता है। उसमें यह भी कहा गया है कि अकबर यदि ‘‘कुरान का अनुसरण करते हुए और देश के हित में’’ कोई नया हुक्म जारी करे तो उसे सबको स्वीकार करना होगा। इस घोषणा, जिस पर प्रमुख उलेमाओं के हस्ताक्षर थे, की व्याख्या गलत ढंग से ‘‘अमोघत्व का आदेश’’ के रूप में की जाती है। अकबर ने कुरान की व्याख्या में समर्थ व्यक्तियों में परस्पर मतभेद की स्थिति में ही किसी एक विचार को सही बतलाने का अधिकार अपने हाथ में लिया था। अकबर ने ऐसे समय में जबकि देश के विभिन्न भागों में शिया, सुन्नी और महदवियों के मध्य का मतभेद खून खराबे की हद तक पहुँच चुका था, उदार धार्मिक सहिष्णुता की अपेक्षा की। इसमें सन्देह नहीं कि साम्राज्य की धार्मिक स्थिति को सामान्य बनाने में महजर का हितकर प्रभाव पड़ा। लेकिन देश के विभिन्न धर्मों और सम्प्रदायों के लोगों को एकमत करने में अकबर को बहुत कम सफलता मिली। इबादतखाने की चर्चाओं से विभिन्न धर्मों के लोगों में सामन्जस्य पैदा होने के स्थान पर और अधिक कड़वाहट पैदा हो गयी क्योंकि प्रत्येक धर्म के प्रतिनिधियों ने दूसरे धर्मों को नीचा बताकर अपने-अपने धर्म को अन्यों से बेहतर सिद्ध करने का प्रयत्न किया। इसीलिए 1582 में अकबर ने इबादतखाने की चर्चाएँ बन्द कर दीं लेकिन उसने सत्य की तलाश का काम छोड़ा नहीं। उसका घोर आलोचक बदायूँनी कहता है कि ‘‘लोग रात-दिन तर्क जिज्ञासा व खोजबीन करने के अलावा और कुछ नहीं करते’’ अकबर ने हिन्दू धर्म के सिद्धान्तों को जानने के लिए पुरुषोत्तम और देवी को आमंत्रित किया और जराथुष्ट धर्म के सिद्धान्तों की व्याख्या के लिए मेहरजी राणा को बुलवाया। ईसाई धर्म के सिद्धान्तों को और अधिक समझने लिए उसने कुछ पुर्तगाली पादरियों से भी भेंट की। उसने गोआ में अपने दूत भेजे और पुर्तगालियों से दो विद्वान धर्म प्रचारकों को अपने दरबार में भेजने की प्रार्थना की। पुर्तगालियों ने अकाबीवा और मानसरेत को भेजा, जिन्होंने लगभग तीन वर्ष अकबर के दरबार में व्यतीत किये। उन्होंने इस काल का बहुमूल्य विवरण छोड़ा है, परन्तु अकबर को ईसाई बनाने की उनकी आशा का कोई आधार नहीं था। अकबर जैनियों के सम्पर्क में भी आया और उनके आग्रह पर काठियावाड़ के प्रमुख जैन सन्त हीर विजय सूरी ने उनके दरबार में कुछ वर्ष बिताएँ। अलग-अलग धर्मों के नेताओं के सम्पर्क, उनके विद्वतापूर्वक रचनाओं के अध्ययन, सूफी सन्तों और योगियों के साथ हुई भेटों ने धीरे-धीरे अकबर को यह विश्वास दिला दिया कि सम्प्रदाय और जातिगत भेद होते हुए भी सब धर्मां में कई अच्छी बातें हैं, जो वाद-विवाद की गरमी में छिपी रह जाती हैं। उसने यह अनुभव किया कि यदि विभिन्न धर्मों की अच्छी बातों पर बल दिया जाए, तो सामन्जस्य और मित्रता का वातावरण बन सकता है, जो देश के हित में होगा। उसने यह भी अनुभव किया कि नामों और स्वरूपों की अनेकता के बावजूद ईश्वर केवल एक है। बदायूँनी के शब्दों में ‘‘शहंशाह पर सब प्रभावों के परिणामस्वरूप धीरे-धीरे अकबर के दिल में पत्थर की लकीर की तरह यह विश्वास जम गया कि सभी धर्मों के कुछ अच्छे लोग हैं। अगर हर जगह कुछ वास्तविक ज्ञान मिल सकता है, तो सत्य एक ही धर्म में क्यों सीमित रहें’’ ? बदायूँनी का दावा है कि इसी के परिणामस्वरूप अकबर धीरे-धीरे इस्लाम से दूर हो गया और उसने हिन्दू, ईसाई, पारसी धर्म आदि विद्यमान धर्मों को मिला कर एक नये धर्म की स्थापना की। परन्तु आधुनिक इतिहासकार इस मत को स्वीकार नहीं करते। उनका विचार है कि बदायूँनी ने इस बात में अतिशयोक्ति का प्रयोग किया है। इस बात कोई प्रमाण नहीं है कि अकबर ने नया धर्म चलाया या चलाने का उसका विचार था। अबुलफजल और बदायूँनी ने इस तथाकथित नये धर्म के लिये तौहीद-ए-इलाही शब्द का प्रयोग किया है जिसका शाब्दिक अर्थ है ‘‘दैवी एकेश्वरवाद’’। ‘‘दीन’’ अर्थात् शब्द का प्रयोग पहली बार आज से 80 वर्ष पूर्व किया गया था। तौहीद-ए-इलाही वास्तव में सूफी सिलसिले के सामने ही एक मार्ग था जो लोग इस में दीक्षा लेने के लिये उत्सुक होते थे। उनका दीक्षित करने के लिये जब शहंशाह अपनी सहमति दे देते थे। तभी वे इस का सदस्य बन सकते थे। दीक्षा के लिए इतवार का दिन निश्चित था। इस मार्ग में दीक्षित होने वाला व्यक्ति शहंशाह के कदमों पर अपना सिर रखता था और शहंशाह उसे उठाकर मन्त्र देता था, जिसे सूफी भाषा में (शस्त) कहा जाता था। आगन्तुक को ध्यान लगाकर इस मन्त्र की पुनरावृत्ति करनी पड़ती थी। इस सूत्र में अकबर का प्रिय उद्घोष ‘‘उल्लाह-उ-अकबर’’ अर्थात् ईश्वर महान है, सम्मिलित था। दीक्षित होने वालों को जहाँ तक सम्भव हो माँस से दूर रहना पड़ता था। कम से कम अपने जन्म के महीने में तो उसे ऐसा करना ही होता था और अपने जन्म दिन पर भोज तथा दान इत्यादि देना पड़ता था। दीक्षा के अतिरिक्त इसमें कोई रीतियाँ, आडम्बर या पूजा स्थल, कोई पुजारी वर्ग, कोई पवित्र पुस्तकें या आदेश नहीं थे। बदायूँनी का कहना है कि इसके सदस्यों की भक्ति के चार स्तर थे अर्थात् सम्पत्ति, जीवन, सम्मान और धर्म का बलिदान। ये स्तर भी सूफी मार्ग के स्तरों के सामन थे। धर्म त्याग का अर्थ वस्तुतः धर्म के संकीर्ण सिद्धान्तों पर बाह्य आडम्बरों के प्रति मोह का त्याग था और यह भी सूफी सिद्धान्तों की परम्परा में था। अकबर ने अपने शिष्य बनाने के लिए न तो बल का इस्तेमाल किया और न ही पैसे का। अकबर के अधिकांश अग्रणी अमीरों में से जिनमें लगभग सभी हिन्दू अमीर शामिल थे। किसी ने भी तौहीद-ए-इलाही में दीक्षा नहीं ली, केवल बीरबल ही इसका अपवाद था। इस मार्ग में दीक्षित होने वालों की संख्या बहुत कम थी और उनमें भी बहुत से अकबर के अपने कृपापात्र थे। अतः इस मार्ग द्वारा कोई महत्वपूर्ण राजनीतिक भूमिका अदा करने की उम्मीद नहीं थी। वस्तुतः जब अकबर ने यह मार्ग चलाया तो वह अपनी आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ कर चुका था और वह इस स्थिति में था कि किसी राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिये उसे कोई ढोंग रचने की आवश्यकता नहीं है। अकबर का उद्देश्य तब क्या था ? इस विषय में इतिहासकारों के अलग-अलग मत हैं। बदायूँनी के विचार में अयोग्य चापलूसी और अधार्मिकों द्वारा अकबर का दिमाग खराब कर दिया गया था। उसका विचार है कि उन्होंने अकबर को यह समझाया कि वह युग का ‘इंसान-ए-कामिल’ अथवा ‘परिपूर्ण मनुष्य’ है। उनके कहने पर ही अकबर ने ‘‘पाबोस’’ की परम्परा अर्थात् शहंशाह के सामने कदम बोसी शुरू करवाई। यह रीति पहले सिफ्र खुदा की इबादत के लिए अपनाई जाती थी। किन्तु यह कोई पहला उदाहरण नहीं इस तरह के बहुत से उदाहरण हैं जबकि शासकों ने अपने आप में सांसारिक और आध्यात्मिक शक्तियों को मिलाया। अबुलफजल कहता है कि यह लोगों के लिए स्वाभाविक है कि वह अपने शासक से आध्यात्मिक तथा मार्गदर्शन की आशा करें और अकबर भौतिक लोगों को आध्यात्मिक आनंद प्रदान करने और एक-दूसरे के विरोधी सम्प्रदायों में सामन्जस्य स्थापित करने में पूरी तरह समर्थ था। अकबर का लक्ष्य जो भी रहा हो, तौहीद-ए-इलाही उसके साथ ही खत्म हो गया। दीक्षित होने वालों को शस्त देने की प्रथा कुछ समय तक जहाँगीर ने भी अपनाई, लेकिन जल्दी ही इसे समाप्त कर दिया गया। फिर भी राजा को चमत्कारिक शक्तियों से युक्त मानने की प्रवृत्ति बनी रही और लोग राजा के स्पर्श या पानी से भरे बर्तन पर साँस छोड़ने से रोग मुक्त होने की कल्पनाएँ करते रहे। यहाँ तक कि औरंगजेब जैसा कठोर शासक भी इस विश्वास को तोड़ नहीं सका। अकबर ने दूसरे तरीकों से विभिन्न धर्मों में सुलह-कुल अर्थात् शान्ति और सामन्जस्य के सिद्धान्त पर बल दिया। उसने एक अनुवाद विभाग भी स्थापित किया जहाँ संस्कृत, अरबी, ग्रीक इत्यादि भाषाओं की रचनाओं का फारसी में अनुवाद होता था। सबसे पहले ‘सिंहासन बत्तीसी’’ अथर्व वेद और ‘बाइबल’ का अनुवाद किया गया। उसके बाद ‘‘महाभारत’’, ‘‘गीता’’ और ‘‘रामायण’’ का अनुवाद हुआ। ‘‘पंचतंत्र’’ जैसी अनेक रचनाओं तथा भूगोल, गणित और दर्शन पर भी अनेक रचना फारसी में अनुदित की गईं। ‘कुरान’ का भी सम्भवतः पहली बार अनुवाद हुआ। अकबर ने अनेक सामाजिक और शैक्षिक सुधार किये। उसने सती प्रथा बन्द कर दी। विधवा केवल अपनी इच्छा से ही सती हो सकती थी। छोटी आयु की विधवाओं, जिन्होंने विधवा होने तक पति के साथ सहवास नहीं किया होता था, के सती होने पर पूरी पाबन्दी लगा दी गई। विधवा-विवाह को भी कानूनी मान्यता दी गयी। अकबर एक से अधिक पत्नी रखने के हक में नहीं था। बशर्तें पहली पत्नी निःसन्तान न हो। विवाह की आयु बढ़ाकर लड़कियों के लिए चौदह वर्ष और लड़कों के लिये सोलह वर्ष कर दी थी। मदिरा की बिक्री को सीमित किया गया। लेकिन इनमें से प्रत्येक प्रयास सफल नहीं रहा। जैसा कि हम जानते हैं कि सामाजिक विधान की सफलता बहुत कुछ जनता के सहयोग पर पर निर्भर करती है। अकबर का युग अन्धविश्वासों का युग था और ऐसा लगता है कि उसके सामाजिक सुधारों को सीमित सफलता ही मिल सकी। अकबर ने शैक्षिक पाठ्यक्रम में भी काफी संशोधन किया। उसने नैतिक-शिक्षा, गणित के अतिरिक्त धर्म-निरपेक्ष विषयों जैसे कृषि, ज्यामिति, खगोल शास्त्र, प्रशासन के सिद्धान्त, तर्क शास्त्र इतिहास आदि पर अधिक बल दिया। उसने कलाकारों, कवियों, चित्रकारों और संगीतकारों को भी संरक्षण दिया। उसका दरबार प्रसिद्ध व्यक्तियों अर्थात् नवरत्नों की उपस्थिति के कारण प्रसिद्ध हो गया। इस प्रकार अकबर के शासनकाल में राज्य मूलतः धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक विषयों में उदार और प्रबुद्ध तथा सांस्कृतिक एकता को प्रोत्साहन देने वाला बन गया। | |||||||||
| |||||||||