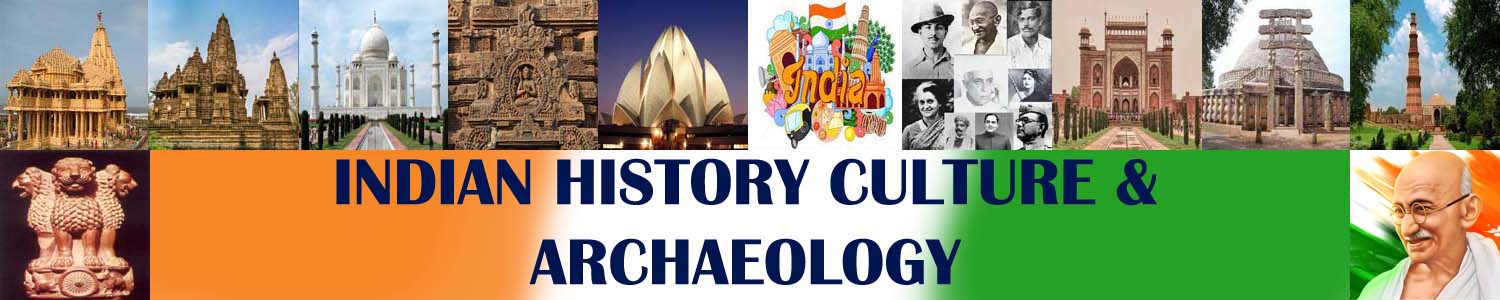| |||||||||
|
पूर्वमध्यकाल में आर्थिक, सामाजिक जीवन, एवं धार्मिक स्थिति
यद्यपि हमने अभी तक एक हजार से बारह सौ ई. तक उत्तर भारत के राजनीतिक विकास का अध्ययन नहीं किया है तो भी आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक जीवन के अध्ययन के लिए आठ सौ से लेकर बारह सौ ई. तक के काल को एक माना जा सकता है। आर्थिक और सामाजिक जीवन तथा विचार और आस्थाओं में राजनीतिक जीवन की अपेक्षा बहुत धीरे-धीरे परिवर्तन होता है। इसी वजह से अनेक प्रारम्भिक विशेषताएँ जो नौवीं शताब्दी के पहले अस्तित्व में थीं, इस काल में भी चलती रहीं। फिर भी अनेक नये तत्वों के आ जाने के कारण इस काल में कुछ विशिष्टता आ गई है। सामान्यतः प्रत्येक ऐतिहासिक काल में नये तत्वों के साथ प्राचीन तत्व भी विद्यमान रहते है, लेकिन परिवर्तन की गति तथा दिशाएँ भिन्न होती हैं।
व्यापार और वाणिज्यउत्तर भारत में यह काल स्थिरता और अवनति का काल माना गया। इसका मुख्य कारण सातवीं और दसवीं शताब्दी के मध्य व्यापार और वाणिज्य में गतिरोध आ जाना था। इसके फलस्वरूप इस क्षेत्र के नगरों और नागरिक जीवन की अवनति हुई। व्यापार और वाणिज्य में गतिरोध का मुख्य कारण पश्चिम में रोमन साम्राज्य का विध्वंश था, जिसके साथ भारत का समृद्धशाली और लाभदायक व्यापार होता था। भारत में सोना और चाँदी का उत्खनन कभी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं किया गया था। सोने और चांदी के लिए भारत की जो ख्याति थी, वह भारत के अनुकूल विदेशी व्यापार के कारण थी। अर्थात् सोना और चाँदी विदेशी व्यापार के जरिए देश में आता था। इस्लाम के उदय होने से सासानी (ईरान) जैसे प्राचीन साम्राज्यों का पतन हो गया, उसके साथ-साथ भारतीय वैदेशिक व्यापार, खासकर स्थलमार्ग द्वारा व्यापार भी प्रभावित हुआ। इसके फलस्वरूप आठवीं और दसवीं शताब्दी में उत्तर भारत में नई स्वर्ण मुद्राओं की भारी कभी हो गई। पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका में एक विस्तृत और शक्तिशाली अरब साम्राज्य के उदय से परिस्थिति में शनैः-शनैः परिवर्तन आया। अरब साम्राज्य में ऐसे अनेक क्षेत्र थे जहाँ से सोना खोदकर निकाला जाता था। अरबी समुद्री यात्रा में निपुण थे। भारतीय वस्त्रों, लोबान तथा मसालों की अमीर अरबी शासकों द्वारा माँग के कारण भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ व्यापार बढ़ा। बाद में चलकर ये क्षेत्र मसालों के द्वीप के नाम से पुकारे जाने लगे। जैसा कि हम पहले के अध्याय में देख चुके हैं, नौवीं तथा दसवीं शताब्दी में बहुत से अरब यात्री पश्चिमी तट की बंदरशाहों में आए। वे देश की तत्कालीन स्थिति के विषय में उपयोगी विवरण छोड़ गये हैं। इस प्रकार दसवीं शताब्दी के पश्चात् उत्तर भारत में वैदेशिक व्यापार और वाणिज्य धीरे-धीरे पुनर्जीवित हुआ। व्यापार के पुनर्जीवित होने से मालवा और गुजरात सबसे ज्यादा लाभान्वित हुए। इसी काल में कई नए नगर जैसे गुजरात में चम्पानेर और अन्हिलवाड़ा उभरे।उन दिनों भारत (आधुनिक पाकिस्तान और बंगला देश समेत) की जनसंख्या बहुत कम थी। यह दस करोड़ से भी कम या आज की जनसंख्या का लगभग दसांश थी। देश के अधिकांश भाग पर जंगल फैले हुए थे जिनमें बहुत अधिक संख्या में जंगली जानवर रहते थे। इन जंगलों में लड़ाकू जनजातियाँ भी रहती थीं जो अक्सर यात्रियों को लूटती थीं। आन्तरिक व्यापार के पतन ने उत्तरी भारत की श्रेणी तथा संघ नामक संघों को कमजोर बना दिया। विभिन्न जातियों के लोगों से व्यापार संघों का गठन होता था। व्यापार संघों के आवरण से संबंधित अपने नियम होते थे जिन्हें सभी सदस्य मानने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य थे और ऋण देने या लेने या दान स्वीकार करने का अधिकार रखते थे। समय बीतने के साथ-साथ कुछ पुरानी श्रेणियों ने उपजातियों का रूप धारण कर लिया, उदाहरणार्थ द्वाद्वश श्रेणी संघ वैश्यों की एक उपजाति बन गयी। अतः व्यापारी वर्ग द्वारा संरक्षित जैन धर्म की उन्नति में बाधा पहुँची। उस काल के चिंतन और विचारधाराओं में भी व्यापार और वाणिज्य के पतन का प्रतिबिम्ब मिलता है। इस अवधि में लिखे गये कुछ धर्मशास्त्रों ने लोगों को भारत के बाहर अर्थात् उन क्षेत्रों में जाने से मना कर दिया था जहाँ मूंज घास पैदा नहीं होती या काले हिरन विचरण नहीं करते हैं। लवण-समुद्र पार जाना भी अपवित्र माना जाता था। निःसन्देह इन प्रतिबन्धों को सभी लोग गंभीरता से नहीं लेते थे। हमें भारतीय सौदागरों, दार्शनिकों, चिकित्सकों तथा शिल्पकारों के विवरण मिलते हैं, जिन्होंने इस काल में बगदाद और पश्मिच एशिया के अन्य मुस्लिम नगरों की यात्रा की थी। समुद्र पार जाने का प्रतिबन्ध संभवतः ब्राह्मणों के लिए ही था। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा प्रतिबंध, धर्मशास्त्रों ने शायद इसलिए भी लगाया था ताकि लोग पश्चिम के मुस्लिम और पूर्व के बौद्ध प्रभावित क्षेत्रों की यात्रा न करें। उन्हें यह भय बना हुआ था कि धर्म विरोधी विचार पुनः भारत में लौट न आए जो कि ब्राह्मण और शासक वर्ग की निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता में बाधक बन सके। धर्मशास्त्रों द्वारा समुद्र यात्रा पर लगाये गये प्रतिबन्ध से दक्षिण-पूर्व एशिया और चीन के साथ भारत के सामुद्रिक व्यापार के विकास में बाधा नहीं पहुँची। भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के मध्य छठी शताब्दी से ही जोरदार व्यापार चल रहा था। उस क्षेत्र के देशों का विस्तृत भौगोलिक ज्ञान तत्कालीन साहित्य में प्रतिबिंबित है। हरिषेण की वृहत्कथा कोण जैसी उस काल की पुस्तकों में इस क्षेत्र की भाषाओं और पहनावे आदि की विभिन्न रूपरेखा पाते हैं। इस क्षेत्र की ऐन्द्रजलिक समुद्रों में भारतीय सौदागरों की अनेक जोखिम भरी कथाएँ हैं जो बाद में प्रसिद्ध नाविक सिंदबाद की कथाओं का आधार बनी। अनेक भारतीय व्यापारी इन देशों में बस गये और उनमें से कुछ लोगों ने स्थानीय लोगों से विवाह भी कर लिया। इस प्रकार व्यापारियों के पीछे धर्म प्रचारक भी गये और फिर बौद्ध तथा हिन्दू धार्मिक विचारों का प्रचार इस क्षेत्र में हुआ। जावा की बोरोबुदूर के बौद्ध तथा कंबोडिया में अंकोरवट के हिन्दू मन्दिरों से दोनों धर्मों के प्रचार के संबंध में जानकारी मिलती है। इस क्षेत्र के कुछ शासक परिवार हिन्दू धर्म से प्रभावित थे। उन्होंने भारत के साथ व्यापार और सांस्कृतियों के सम्मिश्रण से नवीन साहित्यिक और सांस्कृतिक स्वरूपों की स्थापना की। आधुनिक विचारकों का मत है कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों में सिंचाई द्वारा धान की खेती की तकनीक भारत से पहुँची। दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में भौतिक समृद्धि, सभ्यता के विकास एवं बड़े राज्यों के निर्माण का आधार धान की खेती की यही भारतीय तकनीक थी। बंगाल स्थित ताम्रलिप्ति के मुख्य भारतीय बंदरगाह से जावा, सुमात्रा आदि स्थानों के लिए जलयान जाते थे। इस काल की कथाओं से पता चलता है कि ताम्रलिप्ति से सौदागर स्वर्णद्वीप (आधुनिक इन्डोनेशिया) और कताहा (मलाया में केदाह) की यात्रा आरम्भ करते थे। चौदहवीं शताब्दी में जावा के एक लेखक के अनुसार वहाँ जम्बुद्वीप (भारत), कर्नाटक (दक्षिण भारत) और गौड़ (बंगाल) से लोग बड़ी संख्या में लगातार विशाल समुद्री जहाजों में आते थे। गुजरात के व्यापारी भी इस व्यापार में भाग लेते थे। रोमन साम्राज्य के पतन के साथ हिन्द महासागर में चीन, व्यापार का एक मुख्य आकर्षण केन्द्र बन गया। चीन के लोग बहुत बड़ी संख्या में मसालों का व्यापार करते थे जिसका आयात दक्षिण-पूर्व एशिया और भारत से किया जाता था। वे सर्वोत्तम हाथी दाँत भी अफ्रीका से और शीशे का समान पश्चिम एशिया से आयात करते थे। उनमें चिकित्सा की जड़ी-बूटीयाँ, लौह, लोबान और हर तरह के दुर्लभ पदार्थ शामिल थे। साधारणतः अफ्रीका और पश्चिम एशिया से लाया गया सामान दक्षिण भारत में मालाबार तक ही रहता था। चीन के जलयान भी दक्षिण-पूर्व एशिया में मलक्का के बाहर नहीं जाते थे। इस प्रकार भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया दोनों ही चीन, पश्चिम एशियाई देश और अफ्रीका के मध्य होने वाले व्यापार के केन्द्र स्थल बन गये थे। भारतीय व्यापारियों में खासतौर से तमिल, कलिंग (आधुनिक उड़ीसा और बंगाल से) फारस और बाद में अरब वालों ने इस व्यापार में सक्रिय योगदान दिया था। भारतीय जहाजों द्वारा चीन का अधिकांश व्यापार होता था। मालाबार, बंगाल और बर्मा में पायी जाने वाली सागौन की लकड़ी जलयान निर्माण की एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सामग्री थी। मानसून से पहले, जहाजों को बदरगाहों में तब तक रुके रहना पड़ता था जब तक कि पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली हवाएँ न आरम्भ हो जाए। इसी प्रकार मानसून के बाद भी पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ने वाली हवाओं के प्रारम्भ होने तक, उन्हें बंदरगाहों में ही प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सौदागर भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बंदरगाहों को चुनते थे। अरब व्यापारियों ने कहा है कि इस काल में चीन का कैंटन या कानफू वैदेशिक व्यापार के लिये एक मुख्य समुद्री बंदरगाह था। बौद्ध विद्वान समुद्र मार्ग से भारत से चीन गये थे। चीन इतिवृत्तियाँ बताती हैं कि दसवीं शताब्दी के अंत और ग्यारहवीं शताब्दी के आरम्भ में चीनी राजदरबार में जितने भारतीय भिक्षु थे, उतने चीन के इतिहास में पहले कभी नहीं थे। कुछ और पहले के काल के एक चीनी विवरण से पता लगता है कि कैंटन नदी भारत, फारस और अरब से आने वाले जहाजों से भरी रहती थी। कहा जाता है कि कैंटन में ही तीन ब्रह्मा के मन्दिरों में भारतीय ब्राह्मण निवास करते थे। चीनी समुद्र में भारतीयों की उपस्थिति को जापानी अभिलेख भी प्रमाणित करते हैं। इनके अनुसार जापान को कपास से परिचित कराने का श्रेय दो भारतीय को है जो समुद्री लहरों के साथ बहते हुए जापान पहुँच गये थे। भारतीय नरेशों, विशेषकर बंगाल के पाल और सेन तथा दक्षिण के पल्लव तथा चोल राजाओं ने चीनी सम्राटों के राजदरबार में अपने राजदूतों को भेजने का तांता बाँधकर इस व्यापार का बढ़ावा देने की चेष्टा की। चीन के साथ भारत के व्यापार में रुकावट डालने वाले मलाया तथा अन्य पड़ोसी देशों के विरुद्ध चोल नरेश राजेन्द्र प्रथम ने एक नौसेना भेजी। राजेन्द्र प्रथम द्वारा चीन को भेजे गये दूतों के दल ने भारतीय जलयान में यात्रा की थी। इस बात के प्रमाण मौजूद हैं कि दक्षिण भारत, उड़ीसा और बंगाल में अनेक जलयान निर्माण शालायें थीं जहाँ पर जहाजों का निर्माण किया जाता था। इस प्रकार के पोत-कारखाने गुजरात के साथ-साथ पश्चिम तट पर भी थे। इन क्षेत्र का भारतीय वैदेशिक व्यापार जहाज निर्माण और शक्तिशाली नौसेना के आधार पर बनी प्रभावशाली नौसेना की परम्परा तथा कुशल और साहसिक व्यापारियों पर आधारित था। चीन के साथ लगे देशों का व्यापार इतना अनुकूल था कि तेरहवीं शताब्दी में चीनी सरकार ने चीन से सोने और चाँदी के निर्यात पर रोक लगाई। धीरे-धीरे भारतीय व्यापार अरबों और चीनियों के मुकाबले में कम होता गया क्योंकि इनके जहाज भारतीय जहाजों की तुलना में विशाल द्रुतगामी थे। कहा जाता है कि चीनी जहाज कई मंजिल ऊँचे होते थे और वे चार सौ सैनिकों के अतिरिक्त छह सौ यात्री भी ले जा सकते थे। चीनी जहाजों के विकसित और सफल होने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि वे प्राचीन समुद्री नाविकों द्वारा निर्मित कपास (दिशा सूचक यंत्र) का प्रयोग करते थे। यह आविष्कार बाद में चीन से पश्चिमी देशों में पहुँचा। इस प्रकार भारतीय विज्ञान तथा तकनीक पिछड़ते जा रहे थे। दूसरी ओर जबकि पश्चिमी क्षेत्रों के साथ भारतीय व्यापार की अवनति हुई, दक्षिण-पूर्व एशिया और चीन के साथ व्यापार बारहवीं शताब्दी तक धीरे-धीरे बढ़ता ही गया। इस व्यापार का नेतृत्व दक्षिण भारत और बंगाल ने किया। इन क्षेत्रों में धन दौलत और समृद्धि के यही कारण थे। सामंतशाही का विकासइस काल में भारतीय समाज में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। उनमें से एक परिवर्तन था एक वर्ग की बढ़ती हुई शक्ति। इस वर्ग को समसामयिक लेखकों ने सामंत, रानक, रौत्त (राजपूत) आदि विविध नामों से पुकारा है। इनकी उत्पत्ति विभिन्न तरह से हुई थी। उनमें से कुछ सरकारी अधिकारी थे जिन्हें नकद वेतन की जगह गाँव दिये जाते थे, जिनसे वे राजस्व प्राप्त करते थे। दूसरे पराजित राजा और उनके समर्थक थे जो सीमित क्षेत्रों से राजस्व प्राप्त करते थे, कुछ और वंशानुगत स्थानीय सरदार या जाब़ाज सैनिक थे जिन्होंने कुछ सशस्त्र समर्थकों की मदद से अपने अधिकार क्षेत्र कायम कर लिये थे। इनके अतिरिक्त भी दूसरे कबीले या वंश का नायक थे। वे निरन्तर आपस में एक-दूसरे के विरुद्ध लड़ते-झगड़ते रहते और अपने प्रभुत्व क्षेत्र और सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास किया करते थे।राजा द्वारा दिया गया राजस्व कर भार (जिसे भोग या जागीर कहा जाता था) जो एक शासक अपने अधिकारियों या समर्थकों को प्रदान करता था, सिद्धांत रूप से अस्थायी होता था और राजा उन्हें जब चाहे वापस ले सकता था। पूर्ण विद्रोह या विश्वासघात की स्थिति को छोड़कर व्यवहारिक रूप से शायद ही कभी इसका प्रयोग किया जाता था। सामयिक धारणा के अनुसार एक पराजित राजा को भी उसकी भूमि से वंचित करना पाप समझा जाता था। परिणामस्वयप इस काल के राज्यों के विशाल क्षेत्रों पर पराजित और अधीनस्थ राजाओं का प्रभुत्व था जो निरन्तर अपनी स्वतन्त्रता को बनाए रखने की ताक में लगे रहते थे। पुनः इन क्षेत्रों के सामन्ती सरदारों के अधीनस्थ जो अधिकारी थे वे अपने पद एवं कार्य को वंशानुगत समझते थे। कालान्तर में बहुत से सरकारी पदाधिकारी भी अपने पद को पैतृक समझने लगे। पिछले एक अध्याय में हमें एक उदाहरण देखने को मिला है कि बंगाल के किसी परिवार के सदस्यों ने महामन्त्री के पद को चार पुश्तों तक सुशोभित किया था। इस प्रकार अधिकांश पदों पर कुछ परिवारों का एकाधिकार समझा जाने लगा था। वंशानुगत सरदारों ने धीरे-धीरे अनेक सरकारी कार्यों को अपने हाथों में से लिया था। उन्होंने न केवल राजस्व को निर्धारित कर वसूल करने का काम किया बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों को भी अपने हाथों में ले लिया जिनमें सज़ा देने और जुर्माना लगाने जैसे अधिकार शामिल थे और जो पहले सामान्यतः राजकीय विशेषाधिकार समझे जाते थे। उन्हें अपनी जमीन को बिना राजा की अनुमति लिए अपने समर्थकों को देने का अधिकार था। इस प्रकार भूमि पर बिना श्रम किये जीविकोपार्जन करने वाले लोगों की संख्या में अभिवृद्धि हो गयी। इस प्रकार का समाज की सामान्य विशेषता यह है कि समाज में उन्हीं की स्थिति प्रबल होती है जो बिना श्रम किए भूमि से जीविकोपार्जन करते हैं। भारत के सामन्तशाही समाज के विकास के दूरगामी प्रभाव पड़े। इसने राजा की स्थिति को निर्बल बना दिया और उन्हें सामन्ती सरदारों पर अधिक निर्भर बना दिया। उनमें से कई ने अपनी सेना तैयार कर ली जिससे वे नियमोलंघन कर सकें। भारतीय राज्यों की आंतरिक निर्बलता बाद में चलकर तुर्कों के साथ संघर्ष के समय कष्टप्रद हो गई। छोटे राज्यों ने व्यापार को निरुत्साहित किया और मितव्ययिता को बढ़ावा दिया जिससे गाँव या गाँवों का समूह अधिकांश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सके। सामन्ती सरदारों के प्रभुत्व ने भी स्थानीय ग्रामीण सरकार को कमजोर बना दिया। लेकिन सामन्ती व्यवस्था में केवल बुराईयों ही नहीं थीं। अव्यवस्था और हिन्सा के युग में शक्तिशाली सामन्ती सरदारों ने किसानों और अन्य लोगों के जीवन और धन को सुरक्षा प्रदान की जिसके बिना दैनिक जीवन चल ही नहीं सकता था। कुछ सामन्ती सरदारों ने कृषि के विस्तार और विकास में भी रुचि ली। जनता की दशाइस काल में हस्तशिल्प जैसे वस्त्र, सोना और चाँदी, धातु आदि पर किये गये उच्च स्तर के काम में कोई गिरावट नहीं आयी थी। भारतीय कृषि भी उन्नतिशील दशा में थी। कुछ अरब यात्रियों ने भूमि की उर्वरता और भारतीय कृषकों की निपुणता की पुष्टि की है।इस काल की सभी साहित्यिक रचनाओं में मन्त्रियों, अधिकारियों और सामन्ती सरदारों के ठाठ-बाट और वैभव का वर्णन मिलता है। उन्होंने राजा के मनोहर भवनों का अनुकरण किया जो ऊँचाई में तीन से पाँच मंजिल वाले होते थे। अपने शहर को सजाने के लिए वे बहुमूल्य विदेशी परिधान को धारण करते थे जिनमें ऊनी, चीनी रेशमी वस्त्र, विविध अंगराग, कीमती जवाहररात, सोने और चाँदी के बने आभूषण होते थे। इनके भवनों में बड़ी संख्या में स्त्रियाँ होती थीं और इसकी देख-रेख के लिए अनेक घरेलू नौकर होते थे। जब कभी वे बाहर निकलते तो उनके साथ बड़ी संख्या में घरेलू सेवक होते थे। ये महासामन्ताधिपति जैसी बनावटी उपाधि स्वयं धारण कर लेते थे और व्यक्तिगत सुस्पष्ट प्रतीक के रूप में झंडे, सुसज्जित छतरियाँ, मक्खियों को उड़ाने के लिए सुरागाय (याक) की पूंछ की बनी चँबर को अपना लेते थे। एक समसामयिक रचना में शाही पदाधिकारियों के एक युवा-पुत्र के प्रतिष्ठा-पोशाक धारण करने का उल्लेख है जिसे एक छोटे वर्ग का भूमि सम्पन्न सरदारों और अन्य पदाधिकारियों या प्रतिनिधित्व करने वाला माना जा सकता है। यह विशेष प्रकार की अंगूठियाँ, कुडंल और गले में एक पतला सुनहारा हार धारण किये हुए हैं। शरीर पर केसर के लेप से उसका शरीर पीले रंग का हो गया है। उसके जूते कामदार हैं। केसर से रंगे उसके वस्त्र पीले हैं, जिनमें सोने का किनारा है। जब कभी यह जनता के बीच जाता था तो उनके साथ कुछ सेवक, जिनमें एक व्यक्ति पानदान के साथ होता था और पाँच या छह सशस्त्र सैनिक होते थे। बड़े सौदागर भी राजा के रहन-सहन की नकल करते थे और कभी-कभी उनका जीवन बिल्कुल राजसी होता था। चालुक्य साम्राज्य में एक करोड़पति के विषय में कहा गया है कि उसके भवन के ऊपर बजने वाली घंटियों के साथ विशाल झंडे फहराते रहते थे और उसके पास एक बड़ी संख्या में घोड़े और हाथी थे। उसके मुख्य भवन के निकट पहुँचने के लिए स्फटिक की सीढ़ियाँ थीं। उसके मंदिर का फर्श और दीवारें स्फटिक के थे, जिन पर स्फटिक की मूर्ति और धार्मिक चित्र बने हुए थे। वस्तुपाल और तेजपाल जो गुजरात के मन्त्री थे अपने समय के सुप्रसिद्ध धनाढ्य सौदागर थे। उपयफ्रक्त विवरण से हम यह कल्पना नहीं कर सकते हैं कि सर्वत्र समृद्धि थी। यद्यपि खाद्य पदार्थ सस्ते थे फिर भी शहर में अनेक लोग ऐसे थे जिन्हें भरपेट खाना नसीब नहीं होता था। राजतरंगिणी बारहवीं शताब्दी में कश्मीर में लिखा गया ऐतिहासिक काव्य ग्रन्थ का रचयिता इन्हीं गरीबों की ओर संकेत करता है, जब वह यह कहता है कि एक तरफ दरबारी भुना माँस खाते और फूलों से सुगंधित शराब पीते थे तो दूसरी ओर साधारण जनता को चावल तथा उत्पल शाक (कमल की सब्जी या जंगली तीखी सब्जी) से संतोष करना पड़ता था। इस समय के निर्धन पुरुषों और स्त्रियों के दुर्भाग्य की अनेक कथाएँ मिलती हैं। इसमें से कुछ लोग डकैती और लूटमार करके जीवन व्यतीत करते थे। जहाँ तक गाँवों का सम्बन्ध है, वहाँ बड़ी संख्या में लोग निवास करते हैं। किसानों के जीवन के विषय हमें साहित्यिक रचनाओं, भूमि-अनुदान अभिलेखों आदि से जानकारी मिलती है। धर्मशास्त्र के व्याख्याकारों का कथन है कि किसानों से पहले ही जैसा उपज का छठा भाग राजस्व के रूप में लिया जाता था। अनुदानों से बड़ी संख्या में अतिरिक्त उपकरों या छोटे करों के विषय में पता चलता है - जैसे चारागाह-कर, सरोवर कर आदि। किसानों को भू-राजस्व के अतिरिक्त इन करों को भी देना पड़ता था। कुछ अनुदानों से जमीन के मालिक को यह अधिकार प्राप्त हो जाता था कि वह उस जमीन पर निश्चित या अनिश्चित, उचित या अनुचित करों को किसानों पर लगा सकता था। किसानों को बेगार या बलात् श्रम करना पड़ता था। कहीं-कहीं, जैसे मध्य भारत तथा उड़ीसा में मध्य युगीन यूरोप के कृषि दासों की तरह गाँवों के साथ-साथ वहाँ बसे हुए कारीगारों, चरवाहों और किसानों को भी दे दिया जाता था। साहित्यिक रचनाओं में हम ऐसे सामन्ती सरदारों के विषय में पढ़ते हैं जो मुद्रा वसूल करने का कोई भी अवसर हाथ से जाने नहीं देते थे। बताया गया है कि एक राजपूत सरदार मंत्रियों, मृतपक्षियों, सूअर की लीद, मुर्दे के कफन से भी कमाता था। एक दूसरा लेखक बताया कि एक सामन्ती सरदार के अत्याचारों से एक गाँव जनशून्य हो गया था। इस दिशा में शायद बार-बार पड़ने वाले अकालों और युद्धों का भी योगदान था। युद्ध में जल के साधनों को नष्ट कर देना, गाँवों को जला देना, बलपूर्वक पशुओं या बाजारों के अन्नभंडारों पर कब्जा कर लेना और शहरों को विनष्ट कर देना साधारण बात थी। यहाँ तक कि इस काल के लेखकों ने इन कार्यों को उचित ठहराया है। इस प्रकार सामन्ती समाज के विकास ने जनसाधारण की दिक्कतों को बढ़ा दिया। समाज जाति-व्यवस्थाजाति व्यवस्था जो पहले से ही स्थापित हो चुकी थी, सामाजिक ढाँचे का मूलाधार बन गयी। इस काल में मूर्तिकारों ने ब्राह्मणों के विशेषाधिकार को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बताया और शूद्रों को धार्मिक एवं सामाजिक दृष्टि से घोर आयोग्य साबित करने में अपने पूर्ववर्ती लेखकों को भी पीछे छोड़ दिया। लेखक पाराशर के अनुसार शूद्रों द्वारा बनाया भोजन करना, उनके साथ उठना-बैठना और उनसे सीखना ऐसे कार्य हैं जो कुलीन व्यक्ति को भी नीच बना देते हैं। यहाँ तक कि शूद्रों की छाया तक दूषित थी या नहीं, हम ऐसी भी चर्चा पाते हैं। यह कहना कठिन है कि स्मृतिकारों के विचारों का किस हद तक दैनिक जीवन में पालन किया जाता था। लेकिन इसमे कोई सन्देह नहीं कि निम्नवर्गीय लोगों की स्थिति इस काल में और भी खराब हो गयी। अंतर्जातीय विवाह को हेय दृष्टि से देखा जाता था। यदि कोई कुलीन पुरुष अकुलीन स्त्री से विवाह करता था तो उसकी संतान की जाति माँ की जाति के आधार पर निर्धारित की जाती थी। लेकिन यदि स्त्री कुलीन हो और पुरुष अकुलीन तो ऐसी स्थिति में संतान की जाति पिता की जाति के आधार पर निर्धारित की जाती थी। समकालीन लेखकों ने अनेक तत्कालीन जातियों का उल्लेख किया है, जिनमें कुम्हार, जुलाहा, सुनार, संगीतज्ञ, नाई, रस्सीवाट, चमार, मछुआ, बहेलिया आदि शामिल थे। इनमें से कुछ मजदूरों के संघ थे जिनका वर्गीकरण अब जातियों के रूप में हो गया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस काल के स्मृतिकारों ने हस्तशिल्पों को निम्न जाति का पेशा माना है। इस प्रकार अधिकांश श्रमिकों और भीलों जैसे आदिवासियों की अछूतों की श्रेणी में गणना होने लगी।इस काल में नयी राजपूत जाति के अस्तित्व का भी पता चलता है। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद हैं। अनेक राजपूत अपने को महाभारत के सूर्य और चन्द्रवंशी क्षत्रियों के वंशज मानते हैं। कुछ अन्य अपनी उत्पत्ति का स्रोत उस यज्ञ को मानते हैं जिसे ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर किया था। बहरहाल हम राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित इन सिद्धान्तों में से किसी पर निर्भर नहीं रह सकते क्योंकि आबू पर्वत की यज्ञ-अग्नि से राजपूतों के उद्भव का उल्लेख बाद के चरण साहित्य में पहली बार आया है। हम इन सिद्धांतों से केवल इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि विभिन्न राजपूत वंशों की उत्पत्ति के अलग-अलग स्रोत थे। कुछ भारतीय और विदेशी विद्वान यह मानते हैं कि इन राजपूतों के पूर्वज सीथियन और हूण लोग थे जो हर्ष के बाद भारत में आकर बस गये। कुछ अन्य वंशों की उत्पत्ति भारतीय जनजातियों से हुई। क्षत्रियों के अतिरिक्त ब्राह्मणों और वैश्य परिवार के लोगों ने अनेक कालों में देश पर शासन किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि कालान्तर में विविध जातियों के शासकों के वंशजों को राजपुत या राजपूत यानी शाही कहा गया और उन्हें क्षत्रियों का दर्जा प्रदान किया गया। यह विचारणीय है कि जाति वर्गीकरण इतना कठोर नहीं था जैसा कि कभी-कभी माना जाता है। व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप में लोग उच्च वर्ग में सम्मिलित हो सकते थे और निम्न जाति में गिर भी सकते थे। कभी-कभी नयी जातियों को वर्ण की श्रेणी में रखना कठिन हो जाता था। इसका एक उदाहरण कायस्थ जाति है जिसका उल्लेख विशिष्ट रूप में इस काल में प्रारम्भ होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आरम्भ में विविध जातियों के लोग, जिनमें ब्राह्मण और शूद्र शामिल थे और जिन्होंने राजकीय व्यवस्था में हाथ बटाया था, कायस्थ नाम से पुकारे गये। कालान्तर में वे एक पृथक जाति के रूप में उभरे। इस काल में हिन्दू धर्म का तीव्रगति से विस्तार हो रहा था। इसने न केवल एक बड़ी संख्या में बौद्धों और जैनियों को आत्मसात् किया वरन् अनेक स्वदेशी जनजातियों और विदेशियों को भी हिन्दू बना लिया। इन नये वर्गों ने नयी जातियों और उपजातियों को नया रूप दिया और प्रायः अपनी प्रथाओं, शास्त्रीय पद्धति से विवाह, उत्सवों और अपने जनजातियों देवों एवं देवियों की पूजा करना भी जारी रखा। इस प्रकार, समाज और धर्म अधिकाधिक जटिल हो गये। नारियों की स्थितिपहले की तरह इस काल में भी नारियाँ साधारणत बौद्धिक स्तर में पिछड़ी समझी जाती थीं। उनका कर्तव्य अपने पति की आज्ञा का आँख मूँदकर, बिना सोचे समझे पालन करना था। एक लेखक, पत्नी को अपने पति के प्रति कर्तव्य का बोध कराता है कि उसे पति के पैर की मालिश और इसी प्रकार के अन्य कार्यों को करना चाहिए जो नौकरों के लिए उचित हैं। लेकिन आगे वह शर्त लगाता है कि पति को सदाचारी मार्ग पर चलना चाहिए और उसे अपनी पत्नी के प्रति घृणा और ईर्ष्या भी नहीं करनी चाहिए। मत्स्य पुराण में पथभ्रष्ट पत्नी के पति को सिर तथा छाती को छोड़कर कोड़े या बाँस की छड़ी से मारने का अधिकार दिया है। नारियों को वेदाध्ययन अधिकार से वंचित रखना अभी भी जारी रहा। इसके अतिरिक्त लड़कियों की शादी की उम्र कम कर दी गयी जिसके कारण उनकी उच्च शिक्षा की सुविधा समाप्त हो गयी। तत्कालीन शब्दकोषों में शिक्षिकाओं का उल्लेख न होना नारी उच्च शिक्षा की दयनीय स्थिति का परिचायक है। फिर भी इस काल के कुछ नाटकों से हमें पता चलता है कि राजमहल की स्त्रियाँ और रानी की दासियाँ भी संस्कृत और प्राकृत में उत्कृष्ट कविताओं की रचना करने में समर्थ थीं। ललित कला, विशेष रूप से चित्रकला और संगीत में राजकुमारियों की दक्षता का उल्लेख अनेक कथाओं में मिलता है। उच्च पदाधिकारियों की पुत्रियाँ, वैश्याएँ और रखैल भी विविध कलाओं के साथ काव्य में भी विशेष पारंगत समझी जाती थीं।शादी के विषय में स्मृतिकारों ने कहा कि लड़कियों की शादी छह और आठ वर्ष की आयु के बीच या आठ वर्ष से रजस्वला होने के पूर्व तक कर देनी चाहिए। पुनर्विवाह कुछ विशेष परिस्थिति में स्वीकृत था जबकि पति ने पत्नी का त्याग कर दिया हो (अर्थात् जब उसका कोई पता न हो) या पति मर गया हो, सन्यासी हो, नंपुसक होता या निर्वासित हो। सामान्यतः स्त्रियाँ अविश्वसनीय समझी जाती थीं वे एकान्त मे रखी जाती थीं और उनका जीवन पुरुष, संबंधियों, पिता, भाई, पति और पुत्र द्वारा नियंत्रित किया जाता था। फिर भी घर में उनका आदर था। यदि कोई पति अपनी दोषी पत्नी को परित्याग करता था तो उसे पत्नी को भरण-पोषण का खर्च देना पड़ता था। भू-सम्पत्ति अधिकार के विकास के साथ-साथ स्त्रियों के सम्पत्ति संबंधी अधिकार में वृद्धि हुई। पारिवारिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए स्त्रियों को अपनी सम्पत्ति किसी पुरुष संबंधियों को उत्तराधिकार में देने का अधिकार प्रदान किया गया। यदि किसी पुरुष की मृत्यु बिना पु़त्र की प्राप्ति के हो जाती थी तो कुछ मामलों को छोड़कर उसकी पत्नी को अपने पति की पूरी जायदाद का अधिकार मिल जाता था। किसी विधवा की सम्पत्ति पर उसकी पुत्रियों का अधिकार होता था। इस प्रकार सामन्ती समाज ने निजी सम्पत्ति की धारण को मजबूत बनाया। कुछ लेखकों ने सती प्रथा को अनिवार्य बताया था, लेकिन दूसरों ने इसकी भर्त्सना की। अरब लेखक सुलेमान के अनुसार राज-पत्नियाँ कभी-कभी अपने पतियों की चिता पर जल मरती थीं, पर यह उनकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता था। ऐसा प्रतीत होता है कि सामन्ती सरदारों द्वारा एक बड़ी संख्या में स्त्रियों को रखने की प्रथा के विकास के साथ सम्पत्ति पर बढ़ते हुए झगड़ों के फलस्वरूप सती प्रथा फैली। पहनावा, भोजन, मनोरंजन आदिइस काल में पुरुषों और स्त्रियों की पोशाक में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था। धोती और साड़ी पुरुषों और स्त्रियों की सामान्य पोशाक बने रहे। इसके अतिरिक्त उत्तर भारत में पुरुष मिरजई और स्त्रियाँ चोली पहनती थीं। मूर्तियों को दखने से यह प्रकट होता है कि उत्तर भारत के उच्च वर्गीय पुरुष लम्बे कोट, पैंट और जूते पहनते थे। राजतरंगिनी के अनुसार हर्ष ने कश्मीर में राजा के लिए एक राजोचित पोशाक का प्रचलन करवाया था। इसमें एक लम्बा कोट शामिल था। कहा जाता है कि एक भूतपूर्व मन्त्री को छोटा कोट पहनने के कारण राजा का कोप भाजन बनना पड़ा था। जाड़े में ऊनी कंबलों का व्यवहार किया जाता था। सामान्यतः सूती कपड़े का व्यवहार सबसे अधिक होता था। उच्च वर्गीय लोग रेशमी और मलमल के कपड़े पहनते थे। अरब के यात्री इसकी पुष्टि करते हैं कि पुरुष और स्त्री दोनों ही आभूषण के प्रेमी थे। स्त्री पुरुष दोनों ही सोने के बाजूबन्द और कर्णफूल पहनते थे, जो कभी-कभी बहुमूल्य नगीनों से निर्मित होते थे। एक चीनी लेखक चाउ जूं कुआ का कथन है कि गुजरात में स्त्री-पुरुष दोनों ही दोहरे-दोहरे कर्णफूल पहनते थे और उनके कपड़े चुस्त होते थे। उनके सिर पर पगड़ियाँ होती थीं और पैरों में लाल रंग के जूते होते थे। इस काल के एक दूसरे प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो के विवरण से भी ज्ञात होता है कि मालाबार में स्त्री पुरुष दोनों ही केवल लुंगी का प्रयोग करते थे। इस सम्बन्ध में राजा भी अपवाद नहीं था और यह भी कि वहाँ पर दर्जी का पेशा अज्ञात था। कईलौन में भी लुंगी ही स्त्री-पुरुषों की पोशाक थी। यद्यपि दक्षिण भारतीय राजाओं की पोशाक में कपड़े कम होते थे, किन्तु वे आभूषणों के विशेष प्रेमी थे। चाउ जूं कुआ के अनुसार मालाबार का राजा अपनी प्रजा के समान ही सूती लुंगी पहनता था एवं नंगे पैर रहता था। किन्तु बाहर जाते समय और हाथी पर सवारी के समय वह अपने सर पर मोती जवाहरात से सुसज्जित स्वर्ण मुकुट धारण करता था एवं स्वर्ण के भुजबन्द तथा पायल पहनता था। मार्को पोलो कहता है कि यह राजा सोने, मोती और जवाहरात की शक्ल में जो कुछ पहनता था उसका मूल्य एक नगर के निष्कृति धन अथवा रक्षा शुल्क से भी अधिक था। जहाँ तक भोजन का संबंध है, अनेक क्षेत्रों ओर वर्गों में शाकाहार का नियम था। उस काल के प्रमुख स्मृतिकारों ने विस्तार से उन अवसरों का वर्णन किया है जबकि माँस खाना वैद्य था। इससे मालूम पड़ता है, कि मयूर, घोड़ा व गधा, मुर्गा और सुअर का माँस खाना वैध माना जाता था।अरब लेखकों ने भारतीयों द्वारा मशीनी चीजों का व्यवहार न करने की प्रशंसा की है। इससे उनके आदर्श जीवन की तस्वीर प्रकट होती है। इस काल की साहित्यिक रचनाओं में मदिरापान के अनेक उल्लेख मिलते हैं। मदिरापान समारोहों, विवाहों, प्रतिभोजों और भ्रमणों के अवसर पर किया जाता था, जो जनता के कुछ वर्गों में बहुत लोकप्रिय था। राजा की यात्रा के समय उसके साथ चलने वाली स्त्रियाँ भी मदिरापान का खुलकर आनन्द लेती थीं। कुछ स्मृतिकारों ने तीन उच्च जातियों के लिए मदिरापान वर्जित बताया है। कुछ अन्य स्मृतियों में ब्राह्मणों के लिए मदिरापान निषिद्ध बताया है। कुछ अपवादों के साथ क्षत्रियों और वैश्यों के लिए मदिरापान का आनंद लेने की अनुमति दी गयी है। समकालीन साहित्य से प्रकट होता है कि नगरों के लोग आमोद-प्रमोद प्रिय थे। मेलों और उत्सवों के अतिरिक्त बगीचों की सैर, तैराकी आदि दूर तक लोकप्रिय थे। भेड़ों, मुर्गों व अन्य जानवरों के बीच लड़ाई के अतिरिक्त मल्ल युद्ध भी जनता में लोकप्रिय थे। समाज के उच्चवर्ग के लोग चौसर और शिकार खेलने के शौकीन थे। चौगान (एक प्रकार का भारतीय पोलो) शाही मनोरंजन का साधन था। शिक्षा, ज्ञान और विज्ञानपहले से चली आ रही शिक्षा व्यवस्था में अब तक जो विकास हुआ था, बिना अधिक परिवर्तन के इस काल में चलती रही। उस समय सामूहिक शिक्षा के विषय में कोई सोच भी नहीं सकता था। लोगों ने जीवन-यापन के लिए जो आवश्यक समझा, उसे ही सीखा। लिखना-पढ़ना कुछ ही लोगों तक, मुख्य रूप से ब्राह्मण और उच्च वर्गीय लोगों के बीच सीमित था। कभी-कभी उच्च शिक्षा की व्यवस्था मन्दिरों में भी की जाती थी। सामान्यतः विद्यार्थी को शिक्षक के घर में या शिक्षक के साथ निवास करके उच्च शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती थी। ऐसी स्थिति में वह अपने गुरु को शुल्क अथवा विद्या अध्ययन समाप्त होने पर गुरू दक्षिणा देता था। विद्यार्थियों में, खासकर बहुत निर्धन विद्यार्थी जो शुल्क देने में असमर्थ थे, गुरू की सेवा करते थे। व्याकरण और वेदों की विविध शाखाओं का अध्ययन पढ़ाई के मुख्य विषय थे। शिल्प या पेशे की शिक्षा देने की जिम्मेदारी प्रायः संघों या विशिष्ट परिवारों पर छोड़ दी जाती थी। उदाहरणार्थ एक व्यापारी द्वारा अपने पुत्र को सावधानी के साथ अपने पेशे के लिए प्रशिक्षित करने का विस्तृत वर्णन हमें मिलता है।शिक्षा विशेष रूप से नियमित थी जिसमें लौकिक विषयों पर जोर दिया जाता था। यह शिक्षा कुछ बौद्ध विहारों में प्रदान की जाती थी। उनमें से बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय सर्वप्रसिद्ध था। अन्य शिक्षा के केन्द्र विक्रमशिला और उदयन्तपुरी थे, जो बिहार में ही थे। इन शिक्षण संस्थानों में दूरवर्ती स्थानों से विद्यार्थी आते थे, जिनमें तिब्बत भी शामिल था। इनका खर्च चलाने के लिए राजाओं ने उदारता से मुद्रा और भूमिदान किया था। नालंदा को दो सौ गाँव अनुदान में मिले थे। कश्मीर शिक्षा का दूसरा प्रसिद्ध केन्द्र था। उस काल में कश्मीर में अनेक शैव सम्प्रदाय और ज्ञान के केन्द्र थे। दक्षिण भारत में मदुरई और श्रंगेरी में कई महत्वपूर्ण मठ स्थापित किये गये थे। अनेक शिक्षण केन्द्रों ने धर्म और दर्शन जैसे विषयों पर वाद-विवाद करने के लिए प्रोत्साहन दिया। भारत के विभिन्न भागों में स्थापित मठों और अन्य शिक्षण केन्द्रों ने शीघ्र और स्वतन्त्र रूप से भारत के एक भाग से दूसरे भाग तक जाने के विचारों का समर्थन किया। दर्शनशास्त्र की शिक्षा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती थी, जब तक की दार्शनिक देश के विविध भागों में स्थापित अनेक ज्ञान के केन्द्रों की यात्रा करके वहाँ के लोगों से शास्त्रार्थ न कर ले। इस प्रकार पूरे देश में विचारों के आदान-प्रदान से भारतीय सांस्कृतिक एकता को बहुत बल मिला। इस काल में देश में विज्ञान के विकास की गति मंद पड़ गयी और अब यह देश विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी नहीं रह गया। इस प्रकार शल्य चिकित्सा की अवनति हुई, क्योंकि शवों की चीरफाड़ करने के लिए निम्न जाति के लोग ही योग्य समझे जाते थे। वस्तुतः शल्य चिकित्सा नापियों का पेशा बन गया। फिर भी गणित क्षेत्र में बहुत कुछ प्रगति हुई। भास्कर द्वितीय द्वारा लिखित प्रामाणिक पाठ्य-पुस्तक लीलावती बहुत दिनों तक इस काल में चलती रही। धातुओं, विशेषकर पारा के प्रयोग से औषधि विज्ञान के क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई थी। वनस्पति विज्ञान और घोड़े, हाथियों आदि जानवरों के उपचार के लिए बहुत-सी पुस्तकें लिखी गयीं। उत्तम नस्ल के घोड़ों की वंशवृद्धि के लिए कोई उपाय नहीं किया गया, इसलिए मध्य एशिया, अरब और ईरान से घोड़ों का आयात किया जाता था। इन क्षेत्रों पर मुसलमान शासकों का अधिकार जमने के बाद भारतीय राजाओं को अच्छे घोड़ों को पाने में बहुत-सी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था। इस काल में भारतीय विज्ञान की स्थिरता के अनेक कारण थे। अनुभव बताता है कि संपूर्ण समाज के विकास के साथ विज्ञान के विकास का घनिष्ठ संबंध है। जैसा कि देखा गया है कि इस काल में समाज कठोर और स्वभाव में संकीर्ण होता जा रहा था। आवागमन के साधनों के पतन और धार्मिक कट्टरता में वृद्धि के कारण शहरी जीवन के विकास में बाधा पहुँची। विकास के पतन का दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि भारतीय वैज्ञानिकों ने बाहरी दुनिया में हो रही वैज्ञानिक विकास की धारा से अपने को सर्वथा अलग रखा। इसकी झलक हमें मध्य एशिया के वैज्ञानिक एवं विद्वान अलबरुनी की रचनाओं से मिलती है जिसने ग्यारहवीं शताब्दी के आरम्भ में दस वर्षों तक भारत में निवास किया था। यद्यपि अलबरुनी भारतीय विज्ञान और ज्ञान का बड़ा प्रशंसक था, उसने देश के विद्वानों अर्थात् ब्राह्मणों की संकीर्ण प्रवृत्ति का भी उल्लेख किया है वह कहता है, ‘वे ढीठ, मूर्ख, दंभी, आत्माभिमानी और संकीर्ण प्रवृत्ति के हैं। वे स्वभाव से ही अपने ज्ञान को दूसरे को बाँटने के मामले में कंजूस हैं और इस बात का अधिकाधिक ध्यान रखते हैं कि कहीं अन्य कोई जाति के किसी व्यक्ति, विशेषकर किसी विदेशी को उनका ज्ञान प्राप्त न हो जाये। उनका विश्वास है, कि उनके अतिरिक्त सृष्टि के किसी भी जीवन को विज्ञान का ज्ञान नहीं है।‘‘ वह यह भी सिखाता है कि उनके पूर्वज संकीर्ण दृष्टिकोण के नहीं थे। धार्मिक गतिविधियाँ और विश्वासइस काल में बौद्ध और जैन धर्मां का निरन्तर हृास और हिन्दू धर्म का पुनर्जागरण और विस्तार हुआ। बौद्धिक स्तर पर बौद्ध और जैन धर्मों के सिद्धान्तों को केवल चुनौती ही नहीं दी गयी बल्कि ऐसे अवसर भी आए जबकि मारपीट और बल प्रयोग के द्वारा बौद्ध और जैन धर्मों के मन्दिरों को अधिकृत कर लिया गया। इस काल में बौद्ध धर्म का प्रभाव पूर्वी भारत तक सीमित रहा। बंगाल के पाल शासक बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। दसवीं शताब्दी के बाद उनके पतन से बौद्ध धर्म को भी धक्का पहुँचा लेकिन इससे ज्यादा गम्भीर बौद्ध धर्म के आंतरिक मतभेद थे। बुद्ध ने स्वयं एक व्यवहारिक दर्शन का प्रचार किया था। जिसमें पुजारी वर्ग की भूमिका न्यूनतम थी तथा ईश्वर तथा उसके अस्तित्व के बारे में अधिक अटकलबाजी की गुंजाइश नहीं थी। ईसवीं युग के प्रारम्भ की शताब्दियों में महायान मत का विकास हुआ, जिसमें बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजा जाता था। धीरे-धीरे इनकी पूजा-परिपाटी और जटिल तथा भव्य होती गई। साथ-साथ यह विश्वास मजबूत होता गया कि पूजक मंत्रों को पढ़कर अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। उनका यह भी विश्वास था कि इन कार्यकलापों तथा विभिन्न प्रकार के कष्ट सहने से उन्हे हवा में उड़ने और अदृश्य होने जैसी दैवी शक्तियाँ प्राप्त हो सकती थीं। मनुष्य इस प्रकार से प्रकृति पर नियंत्रण के लिए हमेशा से इच्छुक रहा है, पर उसकी ये इच्छाएँ केवल आधुनिक विज्ञान के विकास से पूरी हुई हैं। कई हिन्दू योगियों ने भी इस प्रकार की चेष्टा की। इनमें सबसे प्रसिद्ध गोरखनाथ थे। गोरखनाथ के शिष्यों को नाथपंथी कहा जाता है तथा एक समय ये सारे उत्तर भारत में लोकप्रिय थे। इनमें से कई योगी नीची जाति के थे और उन्होंने वर्ण-व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तन्त्र कहा जाता है और इसकी सदस्यता बिना जातिभेद सभी के लिए खुली थी।इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म का पतन नहीं हुआ, लेकिन उसने कई ऐसे रूप धारण कर लिए जो हिन्दू धर्म से बहुत भिन्न नहीं थे। विशेषकर व्यापारी वर्गों में जैन धर्म लोकप्रिय बना रहा। गुजरात के चालुक्य राजाओं ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। यह वही समय था जबकि दिलवाड़ा और आबू पर्वत जैसे अत्यंत भव्य मन्दिरों का निर्माण किया गया था। मालवा के परमार राजाओं ने भी अनेक जैन तीर्थकरों और महावीर की विशाल प्रतिमाओं का निर्माण कराया। महावीर को अब भगवान के रूप में पूजा जाने लगा। भव्य जैनालय विभिन्न क्षेत्रों में बनवाए गए जो यात्रियों के लिए विश्रामालय के काम में लाए जाते थे। दक्षिण भारत में नवीं एवं दसवीं शताब्दियों में जैन धर्म अपने विकास की चरम सीमा पर पहुँचा। कर्नाटक के गंगा शासक जैन धर्म के प्रमुख संरक्षक थे। इस काल में वसाढ़ी (जैन मन्दिर) और महास्तम्भ कई भागों में स्थापित किए गए। श्रावण बेलगोला में महावीर की विशाल प्रतिमा भी इसी काल में बनी। यह मूर्ति 18 मीटर ऊँची तथा एक ही चट्टान से काटकर बनाई गई है। इसमें महावीर को तपस्या की मुद्रा में खड़ा दिखाया गया है। वे अपने चारों और के वातावरण से अनभिज्ञ हैं, उनके पाँव में साँप लिपटे हुए हैं तथा चीटियों ने मिट्टी के घरौदे बना लिये हैं। जैन धर्म के चार वरों (शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास) के सिद्धान्त ने जैन धर्म को लोक प्रिय बनने में मदद की। कालांतर में जैन धर्म में बढ़ती हुई कट्टरता और राजकीय संरक्षण का अभाव जैन धर्म के पतन का कारण बना। विविध रूपों में हिन्दू धर्म में पुनर्जागरण और विस्तार हुआ। शिव और विष्णु प्रमुख देवता बन गए और उनकी सर्वश्रेष्ठता प्रभावित करने के लिए भव्य मन्दिर बनाये गये। इस क्रम में स्थानीय देवी-देवताओं के साथ-साथ जनजातियों के देवी-देवताओं को भी शामिल कर लिया था, जनजातियों द्वारा हिन्दू धर्म स्वीकार कर लिया गया था। अब जनजातियों के देवता शिव या विष्णु के अधीन साथी बन गए थे। पूर्वी भारत में बुद्ध की संघनी तारा, शिव की सहचारी-दुर्गा और काली आदि स्वयं पूजा की अधिष्ठातृ बन गयीं। इस प्रकार शिव और विष्णु की सार्थक पूजा का आरंभ सांस्कृतिक संयोग का एक परिणाम था। यह उल्लेखनीय है कि विघटन के युग में धर्म ने रचनात्मक योगदान दिया। लेकिन धार्मिक पुनर्जागरण ने भी ब्राह्मणों की शक्ति और दर्प को बढ़ा दिया। इसके परिणामस्वरूप ऐसे जनआन्दोलन हुए जिन्होंने मानवीय समानता और स्वतन्त्रता के तत्वों पर बल दिया। यह पहले ही बताया जा चुका है कि उत्तर भारत में तन्त्रवाद का विकास हुआ जिसमें जाति का विचार किए बिना उसका सदस्य बना जा सकता था। लेकिन इससे कहीं और अधिक महत्वपूर्ण और स्पष्ट आधार दक्षिण भारत में भक्ति आन्दोलन के विकास को मिला। भक्ति आन्दोलन का नेतृत्व लगातार लोकप्रिय संतों ने किया था जिन्हें नयनार और अलवार के नाम से पुकारते हैं। इन संतों ने तपस्या को अस्वीकार किया। वे धर्म के ओर से उदासीन नहीं थे, बल्कि औपचारिक पूजा उनके लिए भगवान और भक्त के बीच सदा कायम रहने वाला प्रेम था। उनकी पूजा के मुख्य पात्र शिव और विष्णु थे। वे तमिल और तेलुगू भाषाओं में बोल और लिख सकते थे, जो जनसाधारण की भाषा थी। ये संत एक जगह से दूसरी जगह अपने प्रेम और भक्ति के संदेशों को लेते गए। उनमें से कुछ निम्न वर्गो के थे और कुछ ब्राह्मण थे। उनमें कुछ औरतें भी थीं। उनमें से लगभग सभी ने जातिभेद की उपेक्षा की। फिर भी किसी ने जाति व्यवस्था का प्रभावशाली ढंग से विरोध नहीं किया। निम्न जाति के लोगों को बौद्धिक पांडित्य और पूजा से वंचित रखा गया। परन्तु भक्ति के मार्ग को बिना किसी जातीय भेदभाव के, सबके लिए खुला छोड़ दिया गया। भक्ति आन्दोलन ने, न केवल हिन्दू धर्म के विभिन्न पक्षों को ही जीता बल्कि बहुतेरे बौद्धों और जैनियों को भी अपना अनुयायी बनाया। जनजातियों ने भी भक्ति आन्दोलन को स्वीकार किया। दूसरा लोकप्रिय आन्दोलन जिसका उदय बारहवीं शताब्दी में हुआ, वह था लिंगायत या वीर शैव आन्दोलन। इसके संस्थापक बासव और उसका भतीजा चन्नाबासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरान्त उन्होंने अपने मत की स्थापना की। लिंगायत शिव के पुजारी थे। उन्होंने जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध किया और उपवास प्रीतिभोज, तीर्थयात्रा और बलि प्रथा को अस्वीकार किया। सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दी। इस प्रकार दक्षिण भारत और उत्तर भारत के दोनों भागों में हिन्दू धर्म का पुर्नजागरण और विस्तार दो रूपों में हुआ। यदि एक ओर नये सिरे से वेदों और वैदिक पूजा पर बल दिया गया और इनके साथ-साथ शक्तिशाली साहित्यिक और बौद्धिक आन्दोलन पर भी जोर दिया तो दूसरी ओर उत्तर भारत में तंत्र और दक्षिण भारत में भक्ति जैसे लोकप्रिय आन्दोलन का आरम्भ हुआ। भक्ति और तंत्र दोनों ने जातीय विषमता का अनादर किया और उनके दरवाजे सबसे लिए खुले थे। हिन्दू दर्शन को पुनः प्रतिपादित करने वाले शंकर ने बौद्धिक स्तर पर बौद्ध और जैन धर्मों को सबसे भयंकर चुनौती दी। संभवतः शंकर का जन्म नौवीं शताब्दी में केरल में हुआ। उनका जीवन अंधकार रूपी पर्दे से ढका हुआ है। उनके जीवन से संबंधित अनेक दंत कथाएँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि जैन धर्म के अनुयायी हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गये, जिससे उन्हें मदुरई छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। उसके पश्चात् उन्होंने उत्तर भारत की विजय-यात्रा आरम्भ की, जहाँ उन्होंने अपने विरोधियों को शास्त्रार्थ में बुरी तरह पछाड़ा, उनकी विजय यात्रा पूरी हुई और लौटने पर मदुरई के राजा ने उत्साह के साथ उनका स्वागत किया और जैनियों को अपने राजदरबार से निकाल बाहर किया। शंकर का दर्शन अद्वैतवाद या जीव-ब्रह्म की एकता का सिद्धान्त कहलाया। शंकर के अनुसार परमात्मा और उसकी सृष्टि एक हैं। उनमें जो अंतर नजर आता है वह वास्तव में सत्य नहीं है और इस अंतर के उदय का कारण हमारा अज्ञान है। मोक्ष का सीधा मार्ग, स्वयं का ईश्वर के प्रति समर्पण है। ज्ञान शक्ति के आधार पर यह जाना जा सकता है कि ईश्वर और उसकी सृष्टि एक है और अभिन्न है। यह दर्शन वेदांत दर्शन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार शंकर इस विचार का समर्थन करते हैं कि वेद सत्यज्ञान के मूल-स्रोत हैं। शंकर द्वारा प्रतिपादित ज्ञान के मार्ग को कम लोग ही समझ सकते हैं। इस प्रकार का यह जनसमूह को प्रभावित नहीं कर सका। ग्यारहवीं शताब्दी में एक दूसरे प्रसिद्ध विद्वान रामानुज ने वेदों की परम्परा को भक्ति से जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने यह तर्क प्रस्तुत किया कि मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान की अपेक्षा ईश्वर की कृपा अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जाति-भेद के बिना भक्ति का मार्ग सबके लिए खुला है। इस प्रकार रामानुज ने भक्ति पर आधारित लोकप्रिय आन्दोलन और वेदों पर आधारित उच्चवर्गीय आन्दोलन के बीच सेतु निर्माण के प्रयत्न किये। रामानुज द्वारा स्थापित परम्परा का कुछ विचारकों ने अनुसरण किया जिसमें माधवाचार्य (दसवीं शताब्दी), उत्तर भारत में रामानंद बल्लभाचार्य तथा अन्य लोग थे। इस प्रकार भक्ति सोलहवीं शताब्दी के प्रारंभ में हिन्दू समाज के सभी वर्गों के लिए ग्राह्य हो गई। | |||||||||
| |||||||||