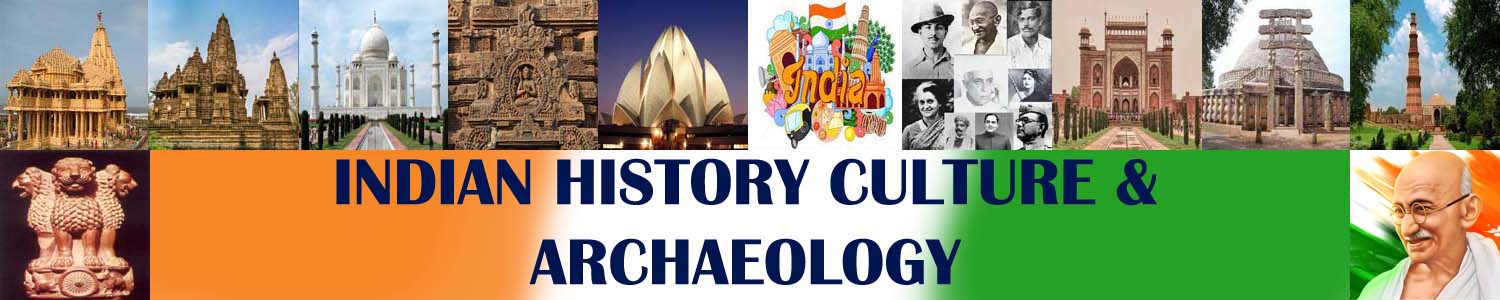| |||||||||
|
20वीं सदी में स्वतंत्रता आन्दोलन का प्रारंभ एवं गांधी युग
राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा और अंतिम चरण 1919 में शुरु हुआ जब विशाल जन-आंदोलन का युग आंरभ हुआ। इस काल में भारतीय जनता ने संभवतः विश्व इतिहास के सबसे बड़े जन-संघर्ष लड़े और भारत की राष्ट्रीय क्रांति विजयी हुई।
जैसा कि हमने पीछे के अध्याय में देखा, प्रथम महायुद्ध (1914-18) के दौरान एक नई स्थिति विकसित हो रही थी। राष्ट्रवाद की ताकत बढ़ी थी। राष्ट्रवादियों को युद्ध के बाद बड़े राजनीतिक लाभ मिलने की आशाएँ थीं और ये आशाएँ पूरी न हो पाने पर वे लड़ने को भी तैयार थे। महायुद्ध के बाद के वर्षों में आर्थिक स्थिति और बिगड़ी। पहले तो कीमतें बढ़ीं और फिर आर्थिक गतिविधियाँ मंद होने लगी। युद्ध के दौरान विदेशी आयात के रुक जाने के कारण भारतीय उद्योग फले-फूले थे, मगर अब उनको घाटे होने लगे और वे बंद होने लगे। इसक अलावा, भारत में अब विदेशी पूँजी बड़े पैमाने पर लगाई जाने लगी। भारतीय उद्योगपति चाहते थे कि सरकार आयातों पर भारी कस्टम ड्यूटी लगाकर तथा मदद देकर उनके उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करे। अब उन्हें भी महसूस होने लगा कि केवल एक मजबूत राष्ट्रवादी आंदोलन तथा एक स्वाधीन भारतीय सरकार के द्वारा ही ये लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। बेरोजगारी तथा मँहगाई की मार से पीड़ित मजदूर तथा दस्तकार भी राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हो उठे। अफ्रीका, एशिया और यूरोप में कुछ जीते हासिल करके देश लौटे भारतीय सैनिकों ने भी अपने आत्मविश्वास तथा दुनिया के बारे में अपना ज्ञान ग्रामीण क्षेत्रों में फैलाया। बढ़ती गरीबी तथा भारी करों के बोझ से कराहते किसान भी नेतृत्व पाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। नगरों के शिक्षित भारतीय भी बढ़ती बेरोजगारी से त्रस्त थे। इस तरह भारतीय समाज के सभी वर्ग आर्थिक कठिनाइयाँ महसूस कर रहे थे और इन कठिनाइयों को सूखों, मँहगाई और महामारियों ने और बढ़ा दिया था। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी राष्ट्रवाद के पुनरोदय के अनुकूल थी। प्रथम महायुद्ध ने पूरे एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रवाद को बहुत बल पहुँचाया था। अपने युद्ध-प्रयासों में जन-समर्थन पाने के लिए मित्र राष्ट्रों अर्थात् ब्रिटेन, अमरीका, फ्रांस, इटली और जापान ने दुनिया के सभी राष्ट्रों के लिए जनतंत्र तथा राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का एक नया युग आरंभ करने का वचन दिया था। लेकिन युद्ध के बाद उन्होंने अपना उपनिवेशवाद खत्म करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उल्टे, पेरिस शांति सम्मेलन तथा दूसरी सभी संधियों में युद्धकालीन वचन भुला, बल्कि तोड़ दिए गए। अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तथा पूर्वी एशिया में युद्ध में हारने वाली शक्तियों, अर्थात् जर्मनी और तुर्की के सारे उपनिवेशों को विजेताओं ने आपस में बाँट लिया। इससे एशिया और अफ्रीका में हर जगह जुझारू और भ्रममुक्त राष्ट्रवाद उठ खड़ा होने लगा। भारत में ब्रिटिश सरकार ने सांविधानिक सुधारों के कुछ प्रयास बेदिली से किए, मगर साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि उसका राजनीतिक सत्ता छोड़ने या उसमें भारतीयों को साझेदार बनाने का कोई इरादा नहीं था। महायुद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह भी हुआ कि गोरों की प्रतिष्ठा घटी। साम्राज्यवाद के आंरभ से ही यूरोपीय शक्तियों ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए जातीय-सांस्कृतिक श्रेष्ठता का स्वांग रचा था। लेकिन युद्ध के दौरान दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ धुआंधार प्रचार किया तथा अपने विरोधियों द्वारा उपनिवेशों में बर्बर और असभ्य व्यवहार का पर्दाफाश किया। स्वाभाविक तौर पर उपनिवेशों की जनता ने दोनों पक्षों पर विश्वास किया और गोरों की श्रेष्ठता का भय उनके मन से उठने लगा। रूसी क्रांति के प्रभाव से भी राष्ट्रीय आंदोलनों को बहुत बल मिला। रूस में ब्लादिमीर इल्यिच लेनिन के नेतृत्व में वहाँ की बोल्शेविक (कम्युनिस्ट) पार्टी ने जार का तख्ता पलट दिया और वहाँ दुनिया के पहले समाजवादी राज्य, सोवियत संघ की स्थापना की घोषणा की। चीन और एशिया के दूसरे भागों में अपना साम्राज्यवादी आधिकारों को एकतरफा तौर पर छोड़कर, एशिया में जार के पुराने उपनिवेशों को आत्मनिर्णय का आधिकार देकर और अपनी सीमा में रहने वाली उन सभी एशियाई जातीयताओं को, जो पुराने शासन के अधीन उसके दमन का शिकार रही थीं, समान अधिकार देकर, नई सोवियत सत्ता ने उपनिवेशों की जनता में बिजली की लहर दौड़ा दी। रूस की क्रांति ने उपनिवेशों की जनता में एक नई जान फूँकी। इसने उपनिवेशों की जनता को यह महान पाठ पढ़ाया कि साधारण जनता में बेपनाह शक्ति निहित होती है। अगर निहत्थे किसान और मजदूर अपने यहाँ के अत्याचारियों के खिलाफ एक क्रांति कर सकते हैं तो गुलाम राष्ट्रों की जनता भी अपनी आजादी के लिए लड़ सकती है, बशर्ते कि वह भी उतनी ही एकताबद्ध, संगठित तथा आजादी के लिए लड़ने पर दृढ़ हो। भारत का राष्ट्रवादी आंदोलन इस बात से भी प्रभावित हुआ कि एशिया और अफ्रीका के दूसरे भाग भी युद्ध के बाद राष्ट्रवादी आंदोलनों से आंदोलित हो रहे थे। भारत की नहीं बल्कि आयरलैंड, तुर्की, मिश्र तथा उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के दूसरे अरब देशों, ईरान, अफगानिस्तान, बर्मा, मलाया, इंडोनेशिया, हिंदचीन, फिलीपीन, चीन और कोरिया में भी राष्ट्रवाद की लहर आगे बढ़ी। राष्ट्रवादी और सरकार विरोधी भावनाओं की उठती लहर से परिचित ब्रिटिश सरकार ने एक बार फिर गुड़ खिलाकर डंडे मारने की, अर्थात कुछ छूट और दमन की नीति अपनाने का फैसला किया। इस नीति में गुड़ का काम मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों से लिया गया। मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारब्रिटिश सरकार के भारत मंत्री एडविन मांटेग्यू तथा वायसराय लार्ड चेम्सफोर्ड ने 1918 में संविधान सुधारों की एक योजना सामने रखी जिनके आधार पर 1919 का भारत सरकार कानून बनाया गया। इस कानून में प्रांतीय विधायी परिषदों का आकार बढ़ा दिया गया तथा निश्चित किया गया कि उनके अधिकांश सदस्य चुनाव जीतकर आएँगे। दुहरी शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय सरकारों को अधिक अधिकार दिए गए। इस प्रणाली में वित्त, कानून और व्यवस्था आदि का कुछ विषय ‘आरक्षित’ घोषित करके गर्वनर के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखे गए तथा शिक्षा, जन-स्वास्थ्य तथा स्थानीय स्वशासन जैसे कुछ विषयों को हस्तांतरित घोषित करके उन्हें विधायिकाओं के सामने उत्तरदायी मंत्रियों के नियंत्रण में दे दिया गया। इसका अर्थ यह भी था कि जिन विभागों में काफी धन खर्च होता तो वे हस्तांतरित तो होंगे मगर उनमें भी वित्त पर पूरा नियंत्रण गर्वनर का होगा। इसके अलावा, गर्वनर अपनी समझ से विशिष्ट किसी भी आधार पर मंत्रियों की आज्ञा को रद्द कर सकता था। केंद्र में दो सदनों की व्यवस्था थी। निचले सदन अर्थात लेजिस्लेटिव असेंबली में कुल 144 सदस्यों में 41 सदस्य नामजद होते थे। ऊपरी सदन अर्थात कौंसिल आफ स्टेट्स में 26 नामजद तथा 34 चुने हुए सदस्य होते थे। गर्वनर-जनरल ओर उसकी एक्जीक्यूटिव कौंसिल पर विधान मंडल का कोई नियंत्रण न था। दूसरी ओर केंद्र सरकार का प्रांतीय सरकारों पर अबाध नियंत्रण था। इसके अलावा वोट का अधिकार बहुत अधिक सीमित था। 1920 में निचले सदन के लिए कुल 909,874 तथा ऊपरी सदन के लिए 17,364 मतदाता थे।मगर भारतीय राष्ट्रवादी इन मामूली छूटों से बहुत आगे बढ़ चुके थे। वे अब राजनीतिक सत्ता की छाया मात्र से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। अगस्त 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंबई में एक विशेष सत्र बुलाया ताकि सुधार के प्रस्तावों पर विचार किया जा सके। इस अधिवेशन के अध्यक्ष हसन इमाम थे। इस सत्र ने इन प्रस्तावों को “निराशाजनक और असंतोषजनक” बतलाकर इनकी जगह प्रभावी स्वशासन की माँग रखी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस कुछ वयोवृद्ध नेता सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने के पक्ष में थे। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर दंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की। ये लोग “उदारवादी” कहे गए तथा भारत की राजनीति में आगे चलकर उनकी बहुत नगण्य भूमिका रही। रोलट कानूनभारतीयों को संतुष्ट करने के प्रयास करते समय भी भारत सरकार दमन के लिए तैयार थी। युद्ध के पूरे काल में राष्ट्रवादियों का दमन जारी रहा था। आतंकवादियों तथा क्रांतिकारियों को खोज-खोज कर फाँसी पर लटकाया या जेलों में बंद किया गया था। अबुलकलाम आजाद जैसे दूसरे अनेक राष्ट्रवादी भी सींखचों के पीछे बंद रखे गए थे। अब सरकार ने स्वयं को ऐसी भयानक शक्तियों से लैस करने का फैसला किया जो कानून के शासन के स्वीकृत सिद्धांतों के प्रतिकूल थी, ताकि वह सरकारी सुधारों से संतुष्ट न होने वाले राष्ट्रवादियों को कुचल सके। मार्च 1919 में सरकार ने केंद्रीय विधान परिषद् के एक-एक भारतीय सदस्य द्वारा विरोध के बावजूद रौलट एक्ट बनाया। इस कानून में सरकार को अधिकार प्राप्त था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में मुकदमा चलाए और दंड किए बिना जेल में बंद कर सके। कैदी को अदालत में प्रत्यक्ष उपस्थित करने का जो कानून ब्रिटेन में नागरिक स्वाधीनताओं के बुनियाद था उसे भी निलंबित करने का अधिकार सरकार ने रौलट कानून से प्राप्त कर लिया।महात्मा गाँधी ने नेतृत्व संभालारौलट कानून बादल से बिजली की तरह लोगों पर गिरा। युद्ध के दौरान सरकार ने भारत की जनता से जनतंत्र का विस्तार करने का वादा किया था, मगर यह कानून तो एक बेरहम मजाक था। जैसे कि भूखे आदमी को भोजन की आशा हो मगर उसे कंकड़ परोसे गए हों। लोकतांत्रिक प्रगति तो नहीं हुई, मगर नागरिक स्वतंत्रताएँ और भी कम कर दी गई। देश में असंतोष फैल गया और इस कानून के खिलाफ एक शक्तिशाली आंदोलन उठ खड़ा हुआ। इस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गाँधी नामक एक नए नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाल ली। इस नए नेता ने पुराने नेताओं की एक बुनियादी कमजोरी को खूब पहचाना। दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद से लड़ते हुए उन्होंने संघर्ष का एक नया रुप असहयोग और एक नई तकनीक सत्याग्रह का विकास किया था जिसे अब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आजमाया जा सकता था। इसके अलावा उन्हें भारतीय किसानों की समस्याओं तथा मानसिकता की बुनियादी समझ भी थी और उनके साथ हमदर्दी भी। इसलिए वे किसानों को आकर्षित करके राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्या धारा में लाने में समर्थ रहे। इस तरह वे भारतीय जनता के सभी वर्गों को उभारकर और उनमें एकता कायम करके एक जुझारु राष्ट्रीय जन-आंदोलन खड़ा करने में समर्थ रहे।गाँधीजी और उनके विचारमोहनदास करमचंद गाँधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ब्रिटेन में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। न्याय की उच्च भावना से प्रेरित होकर उन्होंने उस नस्लवादी अन्याय, भेदभाव और हीनता के खिलाफ संघर्ष किया जिसका शिकार दक्षिण अफ्रीका के उपनिवेशों में भारतीयों को होना पड़ रहा था। भारत से दक्षिण अफ्रीका पहुँचे मजदूरों और व्यापारियों को मत देने का अधिकार नहीं था उन्हें पंजीकरण कराना तथा चुनाव-कर देना पड़ता था। उनको गंदी और भीड़ भरी उन बस्तियों में ही रहना होता था जो उनके लिए निर्धारित थीं। कुछ दक्षिण अफ्रीकी उपनिवेशों में एशियाई और अफ्रीकी लोग रात के नौ बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते थे और न ही सार्वजनिक फुटपाथों का प्रयोग कर सकते थे। गाँधीजी इन स्थितियों के विरोध में चलने वाले संघर्ष के शीघ्र ही नेता बन गए और 1893-94 में वे दक्षिण अफ्रीका के नस्लवादी अधिकारियों के खिलाफ एक बहादुराना मगर असमान संघर्ष चला रहे थे। लगभग दो दशक लंबा यही वह संघर्ष था जिसके दौरान उन्होंने सत्य और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह नामक तकनीक का विकास किया। उनके अनुसार एक आदर्श सत्याग्रही सत्यप्रेमी और शांतिप्रेमी होता है, मगर वह जिस बात को गलत समझता है उसे स्वीकार करने से दृढ़तापूर्वक अस्वीकार कर देता है। वह गलत काम करने वालों के खिलाफ संघर्ष करते हुए हँसकर कष्ट सहन करता है। यह संघर्ष उसके सत्यप्रेम का ही अंग होता है। लेकिन बुराई का विरोध करते हुए भी वह बुरे से प्रेम करता है। एक सच्चे सत्याग्रही को प्रकृति में घृणा के लिए कोई स्थान नहीं होता। इसके अलावा वह एकदम निडर होता है। चाहे जो परिणाम हो, वह बुराई के सामने नहीं झुकता। गाँधीजी की दृष्टि में अहिंसा कायरों और कमजोरों का अस्त्र नहीं है। केवल निडर और बहादुर लोग ही इसका उपयोग कर सकते हैं। वे हिंसा को कायरता से अधिक स्वीकार्य सकझते थे। 1920 में अपने साप्ताहिक पत्र “यंग इंडिया” में एक प्रसिद्ध लेख में वे लिखते हैं कि “अहिंसा हमारी प्रजाति का धर्म है जैसे हिंसा पशु का धर्म है,“ परंतु “अगर केवल कायरता और हिंसा में किसी एक को चुनना हो तो मैं हिंसा को चुनने की सलाह दूँगा............. भारत कायरतापूर्वक, असहाय होकर अपने सम्मान का अपहरण होते देखता रहे, इसके बजाए मैं उसे अपने सम्मान की रक्षा के लिए हथियार उठाते देखना अधिक पसंद करुँगा।” एक जगह अपने पूरे जीवन-दर्शन की व्याख्या इस प्रकार की है -सत्य और अहिंसा ही वह अकेला धर्म है जिसका मैं दावा करना चाहता हूँ। मैं किसी भी परामानवीय शक्ति का दावा नहीं करता, ऐसी कोई शक्ति मुझमें नहीं है। गाँधीजी के दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी था कि वे विचार और कर्म में कोई अंतर नहीं रखते थे। उनका सत्य-अहिंसा-दर्शन जोशीले भाषणों और लेखों के लिए न होकर रोजमर्रा के जीवन के लिए था। इसके अलावा साधारण जनता की संघर्ष की क्षमता पर गाँधीजी को अटूट भरोसा था। उदाहरण के लिए, 1915 में जब मद्रास में उनका स्वागत किया गया तो दक्षिण अफ्रीका में अपने साथ संघर्ष करने वाले साधारण लोगों के बारे में उन्होंने कहा - आप कहते हैं कि इन महान स्त्री-पुरुषों को प्रेरणा मैंने दी, मगर मैं इस सम्मान को स्वीकार नहीं कर सकता। उल्टे, जरा से भी इनाम की आशा किए बिना श्रद्धा के साथ कोई काम करने वाले इन सीधे-सादे लोगों ने ही मुझे प्रेरणा दी, मुझे अपनी जगह पर अडिग रखा, तथा जिन्होंने अपने बलिदान के द्वारा, अपनी महान श्रद्धा के द्वारा तथा महान ईश्वर में अपने महान विश्वास के द्वारा मुझसे वह सब कराया जो मैं कर सका। इसी तरह 1942 में जब उनसे पूछा गया कि वे “साम्राज्य की शक्ति का सामना” कैसे कर सकेंगे, तो उन्होंने उत्तर दिया : “लाखों-लाख मूक जनता की शक्ति के द्वारा।” गाँधीजी 46 वर्ष की आयु में 1915 में भारत लौटे। पूरे एक वर्ष तक उन्होंने देश का भ्रमण किया और भारतीय जनता की दशा को समझा। फिर उन्होंने 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की जहाँ उनके मित्रों और अनुयायियों को रहकर सत्य-अहिंसा को समझना तथा व्यवहार करना पड़ता था। उन्होंने संघर्ष की अपनी नई विधि के साथ यहाँ प्रयोग भी करना आरंभ किया। चंपारन का सत्याग्रह (1917)गाँधीजी ने सत्याग्रह का अपना पहला बड़ा प्रयोग बिहार के चंपारन जिले में 1917 में किया। यहाँ नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय निलहे बहुत अधिक अत्याचार करते थे। किसानों को अपनी जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना तथा निलहों द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना पड़ता था। इसी तरह की परिस्थितियाँ पहले बंगाल में भी रही थीं मगर 1859-61 के काल में एक बड़े विद्रोह के द्वारा वहाँ के किसानों ने निलहे साहबों से मुक्ति पा ली थी।गाँधीजी के दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों की कहानी सुनकर चंपारन के अनेक किसानों ने उन्हें वहाँ आकर उनकी सहायता का निमंत्रण दिया। गाँधीजी बाबू राजेन्द्र प्रसाद, मजहरुल-हक, जे. बी. कृपलानी, नरहरि पारिख और महादेव देसाई के साथ 1917 में वहाँ पहुँचे और किसानों की हालत की विस्तृत जाँच-पड़ताल करने लगे। जिले के अधिकारियों ने जल-भुनकर उन्हें चंपारन छोड़ने का आदेश दिया, मगर उन्होंने आदेश का उल्लंघन किया और जेल-मुकदमें के लिए तैयार रहे। सरकार ने मजबूर होकर पिछला आदेश रद्द कर दिया और एक जाँच समिति बिठाई एक सदस्य स्वयं गाँधीजी थे। अंततः किसान जिन समस्याओं से पीड़ित थे उनमें कमी हुई। इस तरह भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की पहली लड़ाई गाँधीजी ने जीत ली। चंपारन में उन्होंने वह भयानक गरीबी भी देखी जो भारतीय किसानों के जीवन का अंग थी। अहमदाबाद में मजदूरों की हड़तालसन् 1918 में गाँधीजी ने अहमदाबाद के मजदूरों और मिल मालिकों के एक विवाद में हस्तक्षेप किया। उन्होंने मजदूरों को मजदूरी में 35 प्रतिशत वृद्धि की माँग करने तथा इसके लिए हड़ताल पर जाने की राय दी। लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि हड़ताल के दौरान मजदूर मालिकों के खिलाफ हिंसा का प्रयोग न करें। मजदूरों के हड़ताल जारी रखने के संकल्प को बल देने के लिए उन्होंने आमरण अनशन किया। उनके अनशन ने मिल मालिकों पर दबाव डाला और वे नर्म पड़कर मजदूरी 35 प्रतिशत बढ़ाने पर सहमत हो गए।सन् 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की फसल चौपट हो गई। मगर सरकार ने लगान छोड़ने से एकदम इनकार कर दिया और पूरा लगान वसूल करने पर उतारू हो गई। गाँधीजी ने किसानों का साथ दिया और उन्हें राय दी कि जब तक लगान में छूट नहीं मिलती, वे लगान देना बंद कर दें। जब यह खबर मिली कि सरकार ने केवल उन्हीं किसानों से लगान वसूलने के आदेश दिए हैं जो लगान दे सकते हों, तभी यह संघर्ष वापस लिया गया। सरदार वल्लभभाई पटेल उन्हीं अनेकों नौजवानों में एक थे जो खेड़ा के किसान-संघर्ष के दौरान गाँधीजी के अनुयायी बने थे। इन अनुभवों ने गाँधीजी को जनता के घनिष्ठ संपर्क में ला दिया और वे जीवन भर उनके हितों की सक्रिय रूप से रक्षा करते रहे। वे वास्तव में भारत के ऐसे पहले राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने अपने जीवन और जीवन-पद्धति को साधारण जनता के जीवन से एकाकार कर लिया था। जल्द ही वे गरीब भारत, राष्ट्रवादी भारत और विद्रोही भारत के प्रतीक बन गए। गाँधीजी को तीन दूसरे लक्ष्य भी जान से प्यारे थे। इनमें पहला था हिंदू-मुसलमान एकता, दूसरा था छुआछूत विरोधी संघर्ष और तीसरा था देश की स्त्रियों की सामाजिक स्थिति को सुधारना। अपने लक्ष्यों को उन्होंने एक बार संक्षेप में इस प्रकार रखा था - मैं ऐसे भारत के लिए काम करूँगा जिसमें सबसे निर्धन व्यक्ति भी इसे अपना देश समझे और इसके निर्माण में उसकी प्रभावी भूमिका हो-एक ऐसा भारत जिसमें लोगों का कोई उच्च वर्ग और निम्न वर्ग न हों, जिसमें सभी समुदाय पूरे सद्भाव के साथ रहते हों . . . . . इस प्रकार के भारत में छुआछूत नामक कोढ़ के लिए कोई जगह नहीं होगी . . . . . स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार होंगे . . . . . मेरे सपनों का भारत यही है। गाँधी जी एक धर्मप्राण हिंदू थे, मगर उनका सांस्कृतिक-धार्मिक दृष्टिकोण संकुचित न होकर बहुत व्यापक था। उन्होंने लिखा है : “भारतीय संस्कृति न तो पूरी तरह हिंदू है, न ही इस्लामी और न ही कोई और संस्कृति। यह सबका समन्वय है।” वे चाहते थे कि भारतीय अपनी संस्कृति में पूरी तरह लीन हों मगर साथ ही दूसरी विश्व-संस्कृतियों से जो कुछ अच्छे तत्व मिलते हों उन्हें स्वीकार करें। उन्होंने लिखा है - मैं चाहता हूँ कि जितनी स्वतंत्रता के साथ संभव हो सभी देशों की संस्कृतियों की बयारें मेरे घर में से गुजरें। लेकिन इनमें से किसी बयार के आगे लड़खड़ा जाना मुझे मंजूर नहीं है। दूसरे जनगण के घर में किसी घुसपैठिए, किसी भिखारी या किसी दास की तरह रहना मुझे मंजूर नहीं है। रोलट कानून के विरुद्ध सत्याग्रहदूसरे राष्ट्रवादियों की तरह गाँधीजी को भी रोलट कानून से धक्का लगा। फरवरी, 1919 में उन्होंने एक सत्याग्रह सभा बनाई जिसके सदस्यों ने इस कानून का पालन न करने तथा गिरफ्तारी और जेल जाने का सामना करने की शपथ ली। संघर्ष का यह एक नया रूप था। राष्ट्रवादी आंदोलन, चाहे नरमपंथियों के नेतृत्व में हुआ हो या गरमपंथियों के, अभी तक आंदोलनों तक ही सीमित था। बड़ी सभाएँ और प्रदर्शन, सरकार से सहयोग करने से इनकार, विदेशी वस्त्रों तथा स्कूलों का बहिष्कार, या व्यक्तिगत आतंकवादी कार्यवाही, अभी तक राजनीतिक कार्य के यही रूप राष्ट्रवादियों को ज्ञात थे। सत्याग्रह ने फौरन ही आंदोलन को एक नए और उच्चतर स्तर तक उठा दिया। अब मात्र आंदोलन करने तथा अपने असंतोष और क्रोध को मौखिक रूप से अभिव्यक्त करने की जगह अब राष्ट्रवादी सक्रिय कार्य भी कर सकते थे।इसके अलावा इस विधि को किसानों, दस्तकारों और शहरी गरीबों के राजनीतिक समर्थन पर अधिकाधिक निर्भर रहना था। गाँधी जी ने राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं से गाँवों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने समझाया कि भारत वहीं बसता है। उन्होंने राष्ट्रवाद को अधिकाधिक साधारण जनता की और मोड़ा खादी (यानी घर में सूत कातकर घर में बुना गया कपड़ा) इस रूपांतरण का प्रतीक थी और जल्द ही यह सभी राष्ट्रवादियों का लिबास बन गई। श्रम की महिमा और आत्मनिर्भरता का महत्व समझाने के लिए गाँधीजी स्वयं रोज सूत कातते थे। उन्होंने कहा कि भारत की मुक्ति तभी संभव है जब जनता नींद से जाग उठे और राजनीति में सक्रिय हो। जनता ने भी गाँधीजी के आह्वान का जोरदार उत्तर दिया। 1919 में मार्च और अप्रैल महीनों में भारत में अभूतपूर्व राजनीतिक जागरण आया। लगभग पूरा देश एक नई शक्ति से भर उठा। हड़तालें, काम रोको अभियान, जुलूस और प्रदर्शन होने लगे। हिंदू-मुसलमान एकता के नारे हवाओं में गूँजने लगे। पूरे देश में बिजली की लहर दौड़ गई। भारतीय जनता अब विदेशी शासन के अपमान को और सहने को तैयार नहीं थी। जलियाँवाला बाग का हत्याकांडसरकार इस जन-आंदोलन को कुचल देने पर अमादा थी। बंबई, अहमदाबाद, कलकत्ता, दिल्ली तथा दूसरे नगरों में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर बार-बार लाठियों और गोलियों से प्रहार हुआ। गाँधीजी ने 6 अप्रैल 1919 को एक शक्तिशाली हड़ताल का आह्वान किया। जनता ने अभूतपूर्व उत्साह से इसका अनुसरण किया। सरकार ने इस जन-प्रतिरोध का सामना, खासकर पंजाब में, दमन से करने का निश्चय किया। इस समय सरकार ने आधुनिक इतिहास का एक सबसे भयंकर राजनीतिक अपराध भी किया। पंजाब मे अमृतसर में 13 अप्रैल, 1919 को एक निहत्थी मगर भारी भीड़ अपने लोकप्रिय नेताओं डॉ. सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जलियाँवाला बाग में जमा हुई। अमृतसर के फौजी कमांडर जनरल डायर ने शहर की जनता को आतंक द्वारा वश में करने का निश्चय किया। जलियाँवाला बाग बहुत बड़ा बाग था, मगर इसमें से निकलने का केवल एक रास्ता था, शेष तीन ओर से यह मकानों से घिरा था। डायर ने बाग को फौज द्वारा घेर लिया और निकास-द्वार पर एक फौजी दस्ता खड़ा कर दिया। उसके बाद उसने अपने फौजियों को राइफलों और मशीनगनों द्वारा अंदर घिरी भीड़ पर गोली बरसाने का हुक्म दिया। वे तब तक गोली बरसाते रहे जब तक कि गोलियाँ खत्म न हो गईं। हजारों लोग मरे और घायल हुए। इस हत्याकांड के बाद पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया और लोगों पर अत्यंत जंगली किस्म के अत्याचार ढाए गए। एक उदारवादी वकील शिवस्वामी अय्यर ने, जिन्हें सरकार ने नाइट (Knight) की उपाधि दी थी, पंजाब के अत्याचारों के बारे में लिखा है -जलियाँवाला बाग में लोगों को बिखरने का अवसर दिए बिना सैकड़ों निहत्थे लोगों का कत्ले-आम, गोलीबारी में घायल सैकड़ों लोगों की दशा के प्रति जनरल डायर की बेरूखी, जो लोग बिखरकर भागने लगे थे उन पर मशीनगनों से गोलीबारी, बोगों पर सार्वजनिक रूप से कोड़े बरसाना, हजारों छात्रों की उपस्थिती जताने के लिए 16 मील दूर प्रतिदिन जाने का आदेश, 500 छात्रों और प्रोफेसरों की गिरफ्तारी और नजरबंदी, 5 से 7 वर्ष के स्कूली बच्चों को भी झंडे की सलामी के लिए परेड में उपस्थित रहने के लिए बाध्य करना........ एक विवाह मंडली पर कोड़ों की बारिश, डाक पर सेंसर, छः सप्ताहों तक बादशाही मस्जिद पर ताला, किसी ठोस कारण के बिना लोगों की गिरफ्तारी और नजरबंदी...........इस्लामिया स्कूल के 6 सबसे बड़े बच्चों पर कोड़ों की मार, केवल इसलिए कि वे स्कूली बच्चे थे और बड़े बच्चे थे, गिरफ्तार लोगों को खुलेआम बंद रखने के लिए बड़े पिंजड़े का निर्माण, दंड के नए-नए रूपों का आविष्कार जैसे सड़क पर रेंगकर चलने के आदेश, कूँदते हुए चलने के आदेश आदि जो नागरिक या सैनिक किसी भी कानून-प्रणाली के लिए अज्ञात हैं, लोगों को एक ही बेड़ी में आपस में जकड़कर रखना और उन्हें खुले ट्रकों में 15-15 घंटों तक रखना, निहत्थे नागरिकों के खिलाफ हवाई जहाजों और लेविस गनों तथा वैज्ञानिक युद्धप्रणाली के नवीनतम ताम-झाम का उपयोग, लोगों को बंधक बनाना, गैरहाजिर लोगों को हाजिर कराने के लिए उनकी संपत्ति को जब्त और नष्ट करना, हिंदू-मुस्लिम एकता के परिणाम जताने के लिए एक हिंदू और एक मुसलमान को एक ही बेड़ी में जकड़कर रखना, भारतीय घरों का पानी और बिजली काट देना, भारतीय घरों से पंखे हटाकर, यूरोपीयों को उपयोग के लिए दे देना, भारतीयों के सभी वाहनों को लेकर उपयोग के लिये यूरोपीयों को देना.......... ये सब उस मार्शल लॉ प्रशासन की अनेक घटनाओं में से कुछ-एक हैं जिसने पंजाब में आतंक राज कायम किया है तथा जनता को हिलाकर रख दिया है। पंजाब की घटनाएँ जब लोगों को ज्ञात हुई तो पूरे देश में भय की एक लहर सी दौड़ गई। साम्राज्यवाद तथा विदेशी शासन जिस सभ्यता का दावा करते थे उसके पर्दे में छिपे घिनौने चेहरे और बर्बरता का जीता-जागता रूप लोगों ने देखा। जनता ने इस कष्ट का वर्णन महान कवि और मानवतावादी रचनाकार रवींद्रनाथ ठाकुर ने किया है जिन्होंने इसके विरोध में अपनी ‘नाइट’ की उपाधि लौटा दी थी। उन्होंने घोषणा की कि - वह समय आ गया है जब सम्मान के प्रतीक अपमान अपने बेमेल संदर्भ में हमारी शर्म को उजागर करते हैं और मैं, जहाँ तक मेरा सवाल है, सभी विशिष्ट उपाधियों से रहित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़े होना चाहता हूँ जो अपनी तथाकथित क्षुद्रता के कारण मानव जीवन के अयोग्य अपमान को सहने के लिए बाध्य हो सकते हैं। खिलाफत और असहयोग आंदोलन (1919-22)खिलाफत आंदोलन से राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई धारा बही। हम देख चुके हैं, कि शिक्षित मुसलमानों की नई पीढ़ियाँ तथा पारंपरिक मौलवियों और धर्मशास्त्रियों का एक भाग अधिकाधिक उग्रपंथी और राष्ट्रवादी बनते जा रहे थे। लखनऊ समझौते ने हिंदू और मुसलमानों की साझी राजनीति गतिविधियों के लिए पहले ही जमीन तैयार कर रखी थी। रौलट कानून विरोधी राष्ट्रीय आंदोलन ने समूची भारतीय जनता को एकसमान प्रभावित किया था और हिंदू-मुसलमान दोनों को राजनीतिक आंदोलन में ले आया था।उदाहरण के लिए राजनीतिक गतिविधियों के क्षेत्र में हिंदू-मुसलमान एकता की मिसाल दुनिया के सामने रखने के लिए मुसलमानों ने कट्टर आर्यसमाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद को आमंत्रित किया था कि वे दिल्ली की जामा मस्जिद के मिंबर से अपना उपदेश दें। इसी तरह अमृतसर में सिखों ने अपने पवित्र स्थान स्वर्ण मंदिर की चाबियाँ एक मुसलमान नेता डॉ. किचलू को सौंप दी थीं। अमृतसर में यह राजनीतिक एकता सरकार के दमन के कारण थी। हिंदुओं और मुसलमानों को एक ही बेड़ियाँ पहनाई गई थीं, एक साथ जमीन पर रेंगकर चलने के आदेश दिए गए थे और एक साथ ही पानी पीने को कहा गया था जबकि एक हिंदू आम तौर पर किसी मुसलमान के हाथों से पानी नहीं पीता था। इस वातावरण में मुसलमान के बीच राष्ट्रवादी प्रवृत्ति ने खिलाफत आंदोलन की शक्ल ले ली। ब्रिटेन तथा उसके सहयोगियों ने तुर्की की उस्मानिया सल्तनत के साथ जो व्यवहार किया था और जिस तरह उसके टुकड़े करके प्रेस को हथिया लिया था, राजनीतिक-चेतना प्राप्त मुसलमान उसके आलोचक थे। यह कार्य भूतपूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री लायड जार्ज के वादे के विपरीत था कि “हम तुर्की को एशिया माइनर और थ्रेस की उस समृद्ध और प्रसिद्ध भूमि से वंचित करने के लिए युद्ध नहीं कर रहे हैं जो नस्ली दृष्टि से मुख्य रूप से तुर्क है।” मुसलमानों का यह भी मत था कि तुर्की के सुलतान को अनेक लोग खलीफा अर्थात् धार्मिक मामलों में मुसलमानों के प्रमुख मानते थे और उनकी स्थिति पर आँच नहीं आनी चाहिए। शीघ्र ही अली भाइयों (मुहम्मद अली और शौकत अली), मौलाना आजाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में एक खिलाफत कमेटी गठित हो गई और देशव्यापी आंदोलन छेड़ दिया गया। दिल्ली में नवंबर 1919 में आयोजित अखिल-भारतीय खिलाफत सम्मेलन ने फैसला किया कि अगर उनकी माँगें न मानी गईं तो वे सरकार से सहयोग करना बंद कर देंगे। इस समय मुस्लिम लीग पर राष्ट्रवादियों का नेतृत्व था। उसने राजनीतिक प्रश्नों पर राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके आंदोलन का पूरा-पूरा समर्थन किया। अपनी तरफ से लोकमान्य तिलक और महात्मा गाँधी समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं ने भी खिलाफत आंदोलन को हिंदू-मुसलमान एकता स्थापित करने का मुसलमान जनता को राष्ट्रीय आंदोलन में लाने का सुनहरा अवसर जाना। वे समझते थे कि हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई, पूँजीपति और मजदूर, किसान और दस्तकार, महिलाएँ और युवक, विभिन्न क्षेत्रों के आदिवासी तथा अन्य लोग, अर्थात् भारतीय जनता के सभी अंग अपनी विभिन्न माँगों के लिए संघर्ष करते हुए उसके अनुभव के द्वारा तथा विदेशी शासन को अपना विरोधी समझने के बाद ही राष्ट्रीय आंदोलन में आएँगे। गाँधीजी ने खिलाफत आंदोलन को “हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर जाना जो कि आगे सौ वर्षों तक नहीं मिलेगा।” उन्होंने 1920 के आरंभ में घोषणा की कि खिलाफत का प्रश्न संविधानिक सुधारों तथा पंजाब के अत्याचारों से अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि अगर तुर्की के साथ शांति-संधि की शर्तें भारतीय मुसलमानों को संतुष्ट नहीं करती तो वे असहयोग आंदोलन छेड़ेंगें। वास्तव में, गाँधीजी शीघ्र ही खिलाफत आंदोलन के एक नेता के रूप में उभरे। इस बीच सरकार ने रौलट कानून को रद्द करने पंजाब के अत्याचारों की भरपाई करने या राष्ट्रवादियों की स्वशासन की आकांक्षा को संतुष्ट करने से इनकार कर दिया था। जून 1920 में इलाहाबाद में सभी दलों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें स्कूलों, कॉलेजों और अदालतों के बहिष्कार का एक कार्यक्रम किया गया। खिलाफत आंदोलन ने 31 अगस्त, 1920 को एक असहयोग आंदोलन का आरंभ किया। सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ। कुछ ही सप्ताह पहले इसे एक भयानक नुकसान हुआ था जब 1 अगस्त को 64 वर्ष की आयु में लोकमान्य तिलक का निधन हो गया था। जल्द ही इस कमी को गाँधीजी, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने पूरा कर दिया। कांग्रेस ने गाँधीजी की इस योजना को स्वीकार कर लिया कि जब तक पंजाब तथा खिलाफत संबंधी अत्याचारों की भरपाई नहीं होती और स्वराज्य स्थापित नहीं होता, सरकार से असहयोग किया जाए। लोगों से आग्रह किया गया कि वे सरकारी शिक्षा संस्थाओं, अदालतों और विधानमंडलों का बहिष्कार करें, विदेशी वस्त्रों का त्याग करें, सरकार से प्राप्त उपाधियाँ और सम्मान वापस करें तथा हाथ से सूत कातकर और बुनकर खादी का इस्तेमाल करें। बाद में सरकारी नौकरी से इस्तीफा तथा कर चुकाने से इनकार करने को भी इस कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया। फौरन ही कांग्रेस वालों ने चुनाव से नाम वापस ले लिए और जनता ने भी अधिकांशतः उसका बहिष्कार ही किया। सरकार तथा उसके कानूनों के इस अत्यंत शांतिपूर्ण उल्लंघन के इस निर्णय को दिसंबर 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में अनुमोदित भी कर दिया गया। गाँधीजी ने नागपुर में घोषणा की कि “ब्रिटिश जनता यह बात चेत ले कि अगर वह न्याय नहीं करना चाहती तो साम्राज्य को नष्ट करना प्रत्येक भारतीय का परम कर्तव्य होगा।” नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किए गए। प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों को अब भाषायी आधार पर पुनर्गठित किया गया। कांग्रेस का नेतृत्व अब 15 सदस्यों की एक वर्किंग कमेटी को सौंपा गया जिसमें अध्यक्ष और सचिव शामिल थे। इससे कांग्रेस एक निंरतर विद्यमान राजनीतिक संगठन के रूप में काम करने लगी और उसके प्रस्तावों को लागू करने के लिए उसे एक उपकरण भी मिल गया। कांग्रेस का संगठन अब गाँवों, छोटे कस्बों और मुहल्लों तक भी फैकने वाला था। सदस्यता शुल्क घटाकर प्रति वर्ष चार आने (आज के 25 पैसे) कर दिया गया ताकि निर्धन ग्रामीण और नगर के निर्धन लोग भी उसके सदस्य बन सकें। अब कांग्रेस का चरित्र बदल गया। वह विदेशी शासन से मुक्ति के राष्ट्रीय संघर्ष में जनता की संगठनकर्ता और नेतृत्वकर्ता बन गई। प्रसन्नता की एक लहर चारों ओर फैल गई। राजनीतिक स्वाधीनता भले ही बाद में आए, अब जनता ने गुलामी की मनोवृत्ति को त्यागना आरंभ कर दिया था। मानों कि भारत अब किसी और हवा में साँस ले रहा हो। उन दिनों का उल्लास और उत्साह कुछ विशेष ही था, क्योंकि अब सोया हुआ शेर उठने ही वाला था। इसके अलावा, हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे थे। साथ ही, कुछ पुराने नेताओं ने अब कांग्रेस छोड़ भी दी थी। राष्ट्रीय आंदोलन में जो नया मोड़ आया था, वह उन्हें पसंद न था। वे आंदोलन तथा राजनीतिक कार्यकलाप के उसी पुराने ढर्रे में विश्वास करते थे जो कानून की चारदीवारी का रत्ती भर भी उल्लंघन न करे। वे जनता के संगठन हड़तालों, कामबंदियों, सत्याग्रह, कानून शिकनी, गिरफ्तारी और जुझारु संघर्ष के दूसरे रुपों के विरोध में थे। इस काल में जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ी उनमें मुहम्मद अली जिन्ना, जी. एस खपर्डे, विपिनचन्द्र पाल, और एनी बेसेंट प्रमुख थे। 1921-22 में भारतीय जनता एक अभूतपूर्व हलचल के दौर से गुजरी। हजारों की संख्या में छात्रों ने सरकारी स्कूल-कॉलेज छोड़कर राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश ले लिया। यही समय था जब अलीगढ़ के जामिया मिल्लिया इस्लामिया (राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय), बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ का जन्म हुआ। जामिया मिल्लिया बाद में दिल्ली चला गया। इन राष्ट्रीय कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आचार्य नरेंद्र देव, डॉ. जाकिर हुसैन और लाला लाजपतराय जैसे विख्यात व्यक्ति शिक्षक का कार्य करते थे। सैकड़ों वकीलों ने अपनी मोटी कमाई वाली वकालतें छोड़ दीं। इनमें देशबन्धु चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरु, राजेन्द्र प्रसाद, सैफुद्दीन किचलू, सी. राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, टी. प्रकाशम और आसफ अली जैसे लोग शामिल थे। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज्य कोश स्थापित किया गया और छः माह के अंदर इसमें एक करोड़ रुपया जमा हो गया। स्त्रियों ने बहुत उत्साह दिखाया और अपने गहनों, जेवरों को खुलकर दान किया। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार एक जन-आंदोलन बन गया। पूरे देश में विदेशी वस्त्रों की बड़ी-बड़ी होलियाँ जलाईं गईं। खादी स्वतंत्रता का प्रतीक बन गई। जुलाई 1921 में एक प्रस्ताव पारित करके खिलाफत आंदोलन ने घोषणा की कि कोई मुसलमान ब्रिटिश भारत की सेना में नहीं भरती होगा। सितंबर में ‘राजद्रोह’ का आरोप लगाकर अली भाइयों को कैद कर लिया गया। गाँधीजी ने फौरन आह्वान किया कि इस प्रस्ताव को सैकड़ों सभाओं में पढ़कर सुनाया जाए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 50 सदस्यों ने ऐसी ही एक घोषणा की कि जो सरकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से भारत का उत्पीड़न कर रही है उसकी सेवा कोई भारतीय न करे। ऐसा ही एक बयान कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी जारी किया। कांग्रेस ने अब आंदोलन को और ऊँचे स्तर तक ले जाने का फैसला किया। इसने हर एक प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को अनुमति दी कि अगर उसकी राय मे उस प्रांत की जनता तैयार हो तो वह नागरिक अवज्ञा आंदोलन या ब्रिटिश कानूनों के उल्लंघन का आंदोलन आरंभ कर सकती है और इसमें करों का भुगतान रोकने का आंदोलन भी शामिल किया जा सकता है। सरकार ने एक बार फिर दमन का सहारा लिया। तब तक कांग्रेस और खिलाफत के स्वयंसेवक निचले स्तरों पर हिंदू और मुसलमान राजनीतिक कार्यकर्ताओं को एकताबद्ध करने के लिए साथ-साथ ड्रिल का आयोजन करने लगे थे। ऐसे सारे ड्रिल गैरकानूनी घोषित कर दिए गए। 1921 के अंत तक गाँधीजी को छोड़कर सारे महत्वपूर्ण राष्ट्र वादी नेता तथा 3,000 दूसरे लोग जेलों में बंद किए जा चुके थे। नवंबर 1921 में ब्रिटिश सिंहासन के उत्तराधिकारी प्रिंस आफ वेल्स जब भारत-भ्रमण पर आए तो उनका स्वागत बड़े-बड़े विरोध-प्रदर्शनों द्वारा किया गया। सरकार ने उनसे निवेदन किया था कि जनता और राजा-महाराजाओं में वफादारी की भावना जगाने के लिए वे भारत की यात्रा पर आए। बंबई में एक प्रदर्शन को कुचलने का प्रयास सरकार ने किया और इसमें 53 लोग मारे गए तथा लगभग 400 घायल हुए। दिसंबर 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में कांग्रेस ने अपना “यह दृढ़ मत दोहराया कि जब तक पंजाब और खिलाफत की गलतियों की भरपाई नहीं की जाती और स्वराज्य स्थापित नहीं होता . . . . . वह पहले से भी अधिक जोरदार ढंग से अहिंसक असहयोग का आंदोलन जारी रखेगी।” इस प्रस्ताव में सभी भारतीयों और खासकर छात्रों, से आग्रह किया गया था कि वे “स्वयंसेवक संगठनों में भर्ती होकर चुपचाप और बिना किसी प्रदर्शन के अपनी गिरफ्तारी दें। ऐसे सभी सत्याग्रहियों कों “मनसा-वाचा-कर्मणा अहिंसक रहने”, हिंदुओं मुसलमानों, सिखों, पारसियों, ईसाइयों और यहूदियों में एकता की भावना मजबूत बनाने, तथा स्वदेशी का व्यवहार करने और केवल खादी पहनने की शपथ लेनी पड़ती थी। हिंदू स्वयंसेवकों को सक्रिय रूप से छुआछूत से लड़ने की शपथ भी लेनी होती थी। प्रस्ताव में जनता से यह भी आग्रह किया गया था कि जहाँ भी संभव हो, वह अहिंसक रहकर व्यक्तिगत या सामूहिक अवज्ञा आंदोलन चलाए। लोग अब संघर्ष के अगले आह्वान का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। आंदोलन भी अब जनता में गहरी जड़ें जमा चुका था। संयुक्त प्रांत तथा बंगाल के हजारों किसानों ने असहयोग के आह्वान का पालन किया था। संयुक्त प्रांत के कुछ भागों में बँटाईदारों ने जमींदारों की अनुचित माँगें पूरी करने से इनकार कर दिया था। पंजाब में गुरूद्वारों पर भ्रष्ट मंहतों का कब्जा खत्म करने के लिए सिख अकाली आंदोलन नामक एक अहिंसक आंदोलन चला रहे थे। असम में चाय-बगानों के मजदूरों ने हड़ताल की। मिदनापुर के किसानों ने यूनियन बोर्ड के कर देने से इनकार कर दिया था। चिराला की पूरी जनता नगरपालिका के कर चुकाने से इनकार कर के शहर छोड़ चुकी थी। पेडन्नापाडु में गाँवों के सारे अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया था। डुग्गीराला गोपालकृष्णय्या के नेतृत्व में गुंटूर जिले में एक शक्तिशाली आंदोलन उठ खड़ा हुआ था। उत्तरी केरल के मलाबार क्षेत्र में मोपला कहे जाने वाले मुस्लिम किसानों ने एक शक्तिशाली जमींदार-विरोध आंदोलन छेड़ रखा था। फरवरी 1919 में वायसराय ने विदेश सचिव को पत्र लिखा कि ‘‘शहरों के निम्न वर्गो पर असहयोग आंदोलन का गहरा प्रभाव पड़ा है..........कुछ क्षेत्रों में, खासकर असम घाटी के कुछ भागों, सयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा और बंगाल में किसान भी प्रभावित हुए हैं।’’ 1 फरवरी, 1922 को महात्मा गाँधी ने घोषणा की कि अगर सात दिनों के अंदर राजनीतिक बंदी रिहा नही किए जाते और प्रेस पर सरकार का नियंत्रण समाप्त नहीं होता तो वे करों की गैर-अदायगी समेत एक सामूहिक नागरिक अवज्ञा आंदोलन छेड़ेंगे। लेकिन संघर्ष की यह लहर शीघ्र ही उतरने लगी। संयुक्त प्रांत के गोरखपुर, जिले में चौरी चौरा नामक गाँव में 3,000 किसानों के एक कांग्रेसी जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाई। क्रुद्ध भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला करके उसमें आग लगा दी जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इसके पहले भी देश के विभिन्न भागों में भी भीड़ द्वारा हिंसा की कुछ घटनाएँ हो चुकी थीं। गाँधीजी को भय था कि जन उत्साह और जोश के इस वातावरण में आंदोलन आसानी से एक हिंसक मोड़ ले सकता है। उन्हें पूरा विश्वास था कि राष्ट्रवादी कार्यकर्ता अभी भी अहिंसा के पाठ को समझ और व्यवहार में अपना नहीं सके हैं और यह समझ न हो तो नागरिक अवज्ञा आंदोलन सफल नहीं हो सकता। हिंसा से उनका कोई संबंध न था, इस बात के अलावा शायद उन्हें यह भी विश्वास था कि अंग्रेज आसानी से किसी भी हिंसक आंदोलन को कुचल सकते हैं, क्योंकि जनता में भारी सरकारी दमन के प्रतिरोध की शक्ति अभी भी विकसित नहीं हो सकी थी। इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को रोक देने का फैसला किया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 12 फरवरी को गुजरात के बारडोली नामक स्थान पर अपनी मीटिंग की और एक प्रस्ताव द्वारा उन सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी जिनसे कानून का उल्लंघन हो सकता था। उसने कांग्रेसजन से आग्रह किया कि वे अपना समय चरखा को लोकप्रिय बनाने, राष्ट्रीय विद्यालय चलाने, छुआछूत मिटाने तथा हिंदू-मुसलमान एकता को प्रोत्साहित करने जैसे रचनात्मक कार्यों में लगाएँ। बारडोली के प्रस्ताव में पूरे देश को सकते में डाल दिया। आश्चर्यचकित राष्ट्रवादियों में इसकी मिली जुली प्रतिक्रिया हुई। कुछ को तो गाँधीजी में पूरी श्रद्धा थी और उन्हें विश्वास था कि आंदोलन पर यह रोक संघर्ष की गाँधीवादी रणनीति का ही एक भाग है, परंतु दूसरों ने, खासकर राष्ट्रवादियों ने आंदोलन रोके जाने के निर्णय का विरोध किया। सुभाषचंद्र बोस कांग्रेस के एक अत्यंत लोकप्रिय युवा नेता थे, उन्होंने अपनी आत्मकथा “दि इंडियन स्ट्रगल” में लिखा है - जिस समय जनता का उत्साह अपनी चरम सीमा को छूने वाला था, उस समय पीछे हट जाने का आदेश देना राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं था। महात्माजी के प्रमुख सहयोगी देशबंधु दास, पंडित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपतराय, जो सब जेलों में थे, भी इस सामूहिक खिन्नता में भागीदार थे। मैं उस समय देशबंधु के साथ था और मैनें देखा कि जिस तरह महात्मा गाँधी बार-बार गोलमाल कर रहे थे, उस पर वे क्रोध और दुख से आपे से बाहर हो रहे थे। जवाहर लाल नेहरू जैसे दूसरे युवक नेताओं ने भी ऐसी ही प्रतिक्रिया व्यक्त की। लेकिन जनता ओर नेतागण, दोनों को गाँधीजी में आस्था थी और वे सार्वजनिक रूप से उनके आदेश का उल्लंघन नहीं करना चाहते थे। खुलकर विरोध किए बिना उन्होंने उनके फैसले को स्वीकार कर लिया। इस तरह पहला असहयोग आंदोलन और नागरिक अवज्ञा (सिविल डिसओबीडिएंस) आंदोलन लगभग समाप्त ही हो गया। इस नाटक का आखिरी अंक यह था कि स्थिति का पूरा लाभ उठाकर सरकार ने तीखा प्रहार करने का निश्चय किया। उसने 10 मार्च, 1922 को महात्मा गाँधी को गिरफ्तार कर के उन पर सरकार के प्रति असंतोष भड़काने का आरोप लगाया। गाँधीजी को छः वर्षों की कैद की सजा सुनाई गई। अदालत में उन्होंने जो बयान दिया उसके कारण यह मुकदमा ऐतिहासिक बन गया। अभियोग पक्ष के आरोपों को स्वीकार करते हुए उन्होंने आंदोलन से निवेदन किया कि “कानून में जिस बात को स्वेछापूर्वक किया गया अपराध समझा जाता है और जो मुझे किसी नागरिक का परम कर्तव्य लगता है, उसके लिए मुझे जितनी कड़ी सजा दी जा सकती है, दी जाए।” उन्होंने ब्रिटिश शासन के एक समर्थक से उसके एक कट्टर आलोचक के रूप में अपने रूपांतरण की विस्तार से व्याख्या की और कहा - अनिच्छापूर्वक मैं इस निश्कर्ष पर पहुँचा कि राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से भारत पहले जितना असहाय था, उससे उसे कहीं अधिक असहाय ब्रिटेन के साथ संबंध ने बना दिया है। निहत्थे भारत के पास किसी भी आक्रमण के प्रतिरोध की शक्ति नहीं है।...... वह इतना निर्धन हो चुका है कि अकालों के प्रतिरोध के लिए उसमें शायद ही कोई शक्ति बची है।......... नगरवासियों को शायद ही पता हो कि भारत की आधे पेट खाकर जीवित रहने वाली जनता किस तरह जीवनहीन होती जा रही है। शायद ही उन्हें पता हो कि जो क्षुद्र आराम उन्हें प्राप्त है, वह उस काम की दलाली है जो वे विदेशी शोषकों के लिए करते हैं और यह कि ये मुनाफा और दलाली जनता से चूसी जाती है। शायद ही उन्हें महसूस होता हो कि ब्रिटिश भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार जनता के शोषण के लिए चलाई जाती है। कोई भी लफ्फाजी आंकड़ों का कोई भी खल उस साक्ष्य को नहीं मिटा सकते जो अनेक ग्रामों में हडिडयों के ढाँचों के रूप में दिखाई देता है।........... मेरे विचार में कानून के प्रशासन को चेतन या अचेतन रूप से शोषक के लाभार्थ भ्रष्ट किया जा रहा है। इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि अंग्रेजों तथा देश के प्रशासन में लगे उनके भारतीय सहयोगियों को यह नहीं मालूम है कि वे वही अपराध कर रहे हैं जिसका वर्णन करने का मैंने प्रयास किया है। मुझे विश्वास है कि अनेक अंग्रेज और भारतीय अधिकारी ईमानदारी के साथ यह मानते हैं कि वे दुनिया की सबसे अच्छी प्रणालियों में से एक को यहाँ लागू कर रहे हैं और यह कि भारत धीमी गति से ही सही, निरंतर प्रगति कर रहा है। वे यह नहीं जानते कि एक ओर आतंकवाद की एक सूक्ष्म पर प्रभावशाली प्रणाली और शक्ति के संगठित प्रदर्शनों और दूसरी ओर जवाबी आक्रमण या आत्मरक्षा की सारी शक्तियों से (भारतीयों के) वंचित कर दिए जाने के कारण जनता को शक्ति हीन बना दिया है तथा उनमें अनुकरण की आदत पैदा कर दी है। निष्कर्ष रूप में गाँधीजी ने यह मत व्यक्त किया कि “बुराई के साथ असहयोग उतना ही पुनीत कर्तव्य है जितना कि भलाई के साथ सहयोग।” न्यायाधीश ने कहा कि वह गाँधीजी को वही दंड दे रहा है जो 1908 में लोकमान्य तिलक को दिया गया था। खिलाफत का प्रश्न भी बहुत जल्द ही अप्रासंगिक हो गया। तुर्की की जनता मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में उठ खड़ी हुई और उसने नवंबर 1922 में सुलतान को सत्ता से वंचित कर दिया। कमाल पाशा ने तुर्की के आधुनिकीकरण के लिए तथा उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए अनेक कदम उठाए। उसने खिलाफत (खलीफा का पद) समाप्त कर दिया और संविधान से इस्लाम को निकालकर राज्य को धर्म से अलग कर दिया उसने शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया, स्त्रियों को व्यापक अधिकार दिए, यूरोपीय ढंग से कानून बनाए और खेती के विकास के तथा आधुनिक उद्योग-धंधों की स्थापना के लिए कदम उठाए। इन सभी कदमों ने खिलाफत आंदोलन की बुनियाद ही नष्ट कर दी। असहयोग आंदोलन में खिलाफत के आंदोलन की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके कारण नगरों के मुसलमान राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए और इस तरह देश में उन दिनों राष्ट्रवादी उत्साह तथा उल्लास का जो वातावरण था उसे बनाने में इसका भी एक हद तक योगदान था। परिणामस्वरूप ऐसा कहा जाता है कि धार्मिक चेतना का राजनीति में समावेश हुआ और अंततः सांप्रदायिक शक्तियाँ मजबूत हुई। यह बात कुछ हद तक सही भी है। राष्ट्रवादी आंदोलन द्वारा केवल मुसलमानों की एक माँग उठाना कोई गलत नहीं था। समाज के विभिन्न अंग अपनी विशिष्ट माँगों और अनुभवों के द्वारा स्वतंत्रता की आवश्यकता को समझें, ऐसा अपरिहार्य था। फिर भी मुसलमानों की धार्मिक राजनीतिक चेतना को ऊपर उठाकर धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक चेतना के स्तर तक ले जाने में राष्ट्रवादी नेतृत्व कुछ सीमा तक असफल रहा। इसके साथ ही यह भी ध्यान रहे कि खलीफा के प्रति मुसलमानों की चिंता से भी बड़े पैमाने पर उनकी भावनाओं का प्रतिनिधित्व खिलाफत आंदोलन ने किया। वास्तव में यह मुसलमानों में साम्राज्यवाद-विरोधी भावनाओं के प्रसार का ही एक पक्ष था। खिलाफत आंदोलन में इन भावनाओं को ही ठोस अभिव्यक्ति मिली। आखिरकार, जब कमाल पाशा ने 1924 में खिलाफत को समाप्त कर दिया तो भारत में कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। यहाँ यह बात ध्यान रहे कि देखने में असहयोग और नागरिक अवज्ञा आंदोलन तो असफल रहे थे, मगर इसके कारण राष्ट्रीय आंदोलन अनेक अर्थों में और मजबूत हुआ था। राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय आंदोलन अब देश के दूर-दराज के स्थानों तक पहुँच चुके थे। लाखों-लाख किसान, दस्तकार और शहरी गरीब राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए थे। भारतीय समाज के सभी वर्गों का राजनीतिकरण हुआ था। स्त्रियाँ आंदोलन में उतरी थीं। लाखों-लाख स्त्री-पुरुषों के इसी राजनीतिकरण तथा सक्रियता ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी चरित्र प्रदान किया। ब्रिटिश शासन दो धारणाओं पर आधारित था - प्रथम, अंग्रेज भारतीयों के भले के लिए ही भारत में शासन कर रहे थे और, द्वितीय यह अजेय था और इसे उखाड़ फेंकना असंभव था। जैसा कि हम देख चुके हैं, पहली धारणा को चुनौती नरमपंथी राष्ट्रवादियों ने दी थी जिन्होंने औपनिवेशिक शासन की एक शक्तिशाली अर्थशास्त्रीय आलोचना सामने रखी थी। अब राष्ट्रीय आंदोलन के सामूहिक चरण में यह हुआ कि इस आलोचना को भाषणों, पर्चों, नाटकों, गीतों, प्रभातफेरियों और समाचारपत्रों के द्वारा जोशीले आंदोलनकारियों ने जन-जन तक पहुँचा दिया। ब्रिटिश शासन की अजेयता की धारणा को चुनौती सत्याग्रह और जनसंघर्ष से मिली। जैसा कि “भारत : एक खोज” में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है - उनकी (गाँधीजी की) शिक्षा का मूल तत्व निर्भीकता थी......... शारीरिक साहस ही नहीं बल्कि मन में भी भय का अभाव.......... परंतु भारत में ब्रिटिश शासन का प्रमुख आवेग भय था - व्यापक, दमतोड़, गलाघोंटू भय, सेना, पुलिस, चारों ओर फैली खूफिया पुलिस का भय, अधिकारी वर्ग का भय, दमनकारी कानूनों और जेल का भय, बेरोजगारी और भुखमरी का भय जो हमेशा आस-पास मंडराते रहते थे। यही वह सर्वव्यापी भय था कि जिसके खिलाफ गाँधीजी की शांत और दृढ़ वाणी गूँजी - भय न करो। असहयोग आंदोलन का एक प्रमुख परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता के मन से भय की भावना उड़ गई। भारत में ब्रिटिश सत्ता की हैवानी ताकत अब उनके लिए डर का कारण न रही। जनता मे ऐसा बेपनाह आत्मश्विस और आत्मसम्मान जागा जो किसी भी हार या धक्के से नष्ट न हो। इसे गाँधीजी ने इस घोषणा द्वारा व्यक्त किया कि “1920 में जो संघर्ष आरंभ हुआ वह एक समझौता विहीन संघर्ष है, चाहे वह एक माह चले या एक साल, या कई माह या कई साल।” स्वराज्यवादी1922-28 के दौरान भारतीय राजनीति में बड़ी-बड़ी घटनाएँ घटीं। असहयोग आंदोलन के रोके जाने से तात्कालिक रूप में राष्ट्रवादियों के बीच हताशा की भावना फैली। इसके अलावा जिन नेताओं को यह फैसला करना था कि आंदोलन को निष्क्रिय बनने से कैसे बचाया जाए, उनके बीच गहरे मतभेद उभर आए। इनमें से एक विचार के प्रतिनिधि चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरु थे जिन्होंने बदली हुई परिस्थितियों मे एक नए प्रकार की राजनीतिक गतिविधि का सुझाव दिया। उनका कहना था कि राष्ट्रवादियों को विधानमंडलों का बहिष्कार समाप्त करके उनमें भाग लेना चाहिए, सरकारी योजनाओं के अनुसार उनके चलने में बाधा डालनी चाहिए, उनकी कमजोरियों को सामने लाना चाहिए, उनको राजनीतिक संघर्ष का क्षेत्र बनाना चाहिए, तथा इस प्रकार जन-उत्साह जगाने में उनका उपयोग करना चाहिए। “अपरिवर्तनवादी” कहे जाने वाले सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉ. अंसारी, बाबू राजेंद्र प्रसाद तथा दूसरे लोगों ने विधानमंडलों में जाने का विरोध किया। उन्होंने चेतावनी दी कि संसदीय राजनीति में भाग लेने से जनता के बीच काम की उपेक्षा होगी, राष्ट्रवादी उत्साह कमजोर पड़ेगा और नेताओं के बीच प्रतिद्वंदिता पैदा होगी। इसलिए ये लोग चरखा चलाने, चरित्र-निर्माण, हिंदू-मुस्लिम एकता, छुआछूत का खात्मा तथा गाँवों में और गरीबों के बीच निचले स्तरों पर कार्य, जैसे रचनात्मक कार्यों पर जोर देते रहे। उनका कहना था कि इससे देश धीरे-धीरे जन-संघर्ष के एक और दौर के लिए तैयार होगा।दिसंबर 1922 में दास और मोतीलाल नेहरु ने कांग्रेस-खिलाफत स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। इसके अध्यक्ष दास थे और मोतीलाल नेहरु इसके सचिवों में से एक थे। नई पार्टी को कांग्रेस के अंदर ही एक समूह के रूप में काम करना था। इसने कांग्रेस के कार्यक्रम को ही स्वीकार किया, मगर एक बात को छोड़कर कि यह पार्टी कौंसिल के चुनावों में भाग लेगी। स्वराज्यवादियों तथा “अपरिवर्तनवादियों” के बीच अब एक तीखा राजनीतिक विवाद उठ खड़ा हुआ। गाँधीजी इस बीच स्वास्थ्य-संबंधी आधार पर 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिए गए थे, मगर वे भी इनमें एकता कायम करने में असफल रहे। लेकिन दोनों ही पक्ष सूरत में 1907 में हुए विभाजन के कड़वे अनुभव को दोहराने से बचना चाहते थे। गाँधीजी की सलाह पर दोनों समूहों ने कांग्रेस में ही रहकर अलग-अलग ढंग से काम करने का फैसला किया। स्वराज्यवादियों को तैयारी के लिए बहुत कम समय मिला था, मगर नवंबर 1923 के चुनावों में उन्हें अच्छी सफलता मिली। केंद्रीय धारा-सभा की चुनाव से भरी जाने वाली 101 सीटों में से 42 उन्होंने जीत लीं। दूसरे भारतीय समूहों के सहयोग से उन्होंने केंद्रीय धारा-सभा में तथा अनेक प्रांतीय परिषदों में सरकार को बार-बार हराया। स्वशासन, नागरिक स्वाधीनताओं और औद्योगिक विकास के प्रश्नों पर अपने प्रभावशाली भाषणों के द्वारा उन्होंने आंदोलन चलाया। मार्च 1925 में एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता विट्ठलभाई पटेल को केंद्रीय धार-सभा का अध्यक्ष (स्पीकर) चुनवाने में भी वे सफल रहे। जिस समय राष्ट्रीय आंदोलन फिर से शक्ति जुटाने में लगा था ऐसे समय में उन्होंने राजनीतिक शून्य को भरा। उन्होंने 1919 के सुधार कानून के खोखलेपन को भी उजागर किया। लेकिन वे भारत की निरंकुश सरकार की नीतियाँ बदलवाने में असफल रहे, और पहले मार्च 1926 और फिर जनवरी 1930 में उन्हें केंद्रीय धारा-सभा का बहिष्कार करना पड़ा। इस बीच “अपरिवर्तनवादी” शांति के साथ रचनात्मक कार्यों में लगे रहे। इस कार्य के प्रतीक रुप में पूरे देश में सैकड़ों आश्रम स्थापित हुए जिनमें युवा स्त्री-पुरुष चरखा और खादी को प्रोत्साहित करते थे तथा निचली जातियों और आदिवासी जनता के बीच काम करते थे। ऐसे सैकड़ों राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज स्थापित हुए जिनमें युवक-युवतियों को उपनिवेश-विरोधी विचारधारा में प्रशिक्षित किया जाता था। इसके अलावा रचनात्मक कार्य करने वालों ने नागरिक अवज्ञा आंदोलनों के संगठनकर्ताओं के रूप में उसकी रीढ़ की हड्डी का काम किया। स्वराज्यवादी और “अपरिवर्तनवादी” भले ही अपने-अपने ढंग से काम रहे हों, मगर उनके बीच कोई बुनियादी मतभेद नहीं था। फिर चूँकि दोनों के परस्पर अच्छे संबंध थे और दोनों ही एक-दूसरे के साम्राज्यवाद-विरोधी चरित्र को स्वीकार करते थे, इसलिए बाद में, जब एक नए राष्ट्रीय संघर्ष का समय आया तो दोनों आसानी से एकजुट हो गए। इस बीच जून 1925 में चितरंजन दास के निधन से राष्ट्रीय आंदोलन और स्वराज्यवादियों को एक और गहरा धक्का लगा। असहयोग आंदोलन में जब उतार आया और जनता में कुंठा की भावना भर गई ऐसी स्थिति में सांप्रदायिकता अपना घिनौना सिर उठाने लगी। सांप्रदायिक तत्वों ने स्थिति का फायदा उठाकर अपने विचारों का प्रचार किया और 1923 के बाद देश में एक के बाद एक कई सांप्रदायिक दंगे हुए। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दिसंबर 1917 में स्थापित फिर सक्रिय हो उठीं। नतीजा यह हुआ कि हम सबसे पहले भारतीय है, यह भावना काफी पहले से चली आ रही थी इसको गहरा धक्का लगा। स्वराज्यवादी पार्टी के नेता मोतीलाल नेहरु और दास कट्टर राष्ट्रवादी थे, मगर सांप्रदायिकता ने इस पार्टी को भी विभाजित कर दिया। “प्रत्युत्तरवादी” (रिस्पांसिविस्ट) कहे जाने वालों के एक वर्ग ने सरकार को अपना सहयोग करने का प्रस्ताव रखा ताकि तथाकथित हिंदू हितों की रक्षा की जा सके। इस गुट में मदनमोहन मालवीय, लाला लातपतराय और एन. सी. केलकर शामिल थे। उन्होंने मोतीलाल नेहरु पर हिंदुओं को धोखा देने, हिंदू-विरोधी होने, गौहत्या का पक्ष लेने तथा गौमाँस खाने का आरोप लगाया। सत्ता के फेंके हुए टुकड़ों को हथियाने के लिए लड़ने में मुस्लिम संप्रदायवादी भी पीछे नहीं रहे। गाँधीजी ने बार-बार जोर देकर कहा था कि ‘‘हिंदू-मुस्लिम एकता हर काल में और सभी परिस्थितियों में हमारी आस्था होनी चाहिए,’’ उन्होंने ही हस्तक्षेप करके स्थिति सुधारने की कोशिश की। सांप्रदायिक दंगों के रूप में देखी गई दरिंदगी का प्रायश्चित करने के लिए उन्होने दिल्ली में मौलाना मुहम्मद अली के घर में सितंबर 1924 में 21 दिनों का उपवास किया। लेकिन उनके प्रयासों को कोई विशेष सफलता नहीं मिली। देश में स्थिति सचमुच गंभीर थी। राजनीतिक उदासीनता आम बात थी, गाँधीजी ने राजनीति से संन्यास ले लिया था, स्वराज्यवादी बँट चुके थे और सांप्रदायिकता फल-फूल रही थी। मई 1927 में गाँधीजी ने लिखा - ‘‘प्रार्थना और प्रार्थना का प्रत्युत्तर मेरी अकेली आशा है।’’ लेकिन राष्ट्रीय उभार की शक्तियाँ चुपके-चुपके बढ़ रही थीं। नवंबर 1927 में जब साइमन कमीशन के गठन की घोषणा हुई तो भारत इस अंधेरे से फिर बाहर निकला और रातनीतिक संघर्ष का एक नया युग आंरभ हुआ। | |||||||||
| |||||||||