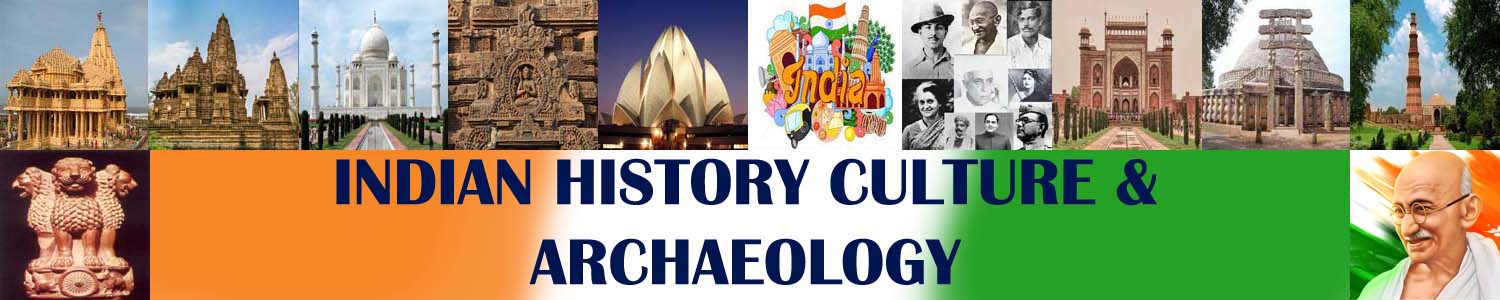| |||||||||
|
भारत में यूरोपीयों का प्रवेश और ब्रिटिश शासन की स्थापना
यूरोप में पूर्वी व्यापार में नया दौरयूरोप के साथ भारत के व्यापारिक संबंध बहुत पुराने, यूनानियों के जमाने के हैं। मध्यकाल में यूरोप और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भारत का व्यापार अनेक मार्गों से चलता था। एशिया में इस व्यापार का अधिकांश भाग अरब व्यापारियों और जहाजियों द्वारा चलाया जाता था, और इसके भूमध्यसागरीय और यूरोपीय भाग पर इटली वालों का लगभग एकाधिकार था। एशिया का माल यूरोप तक पहुँचने से पहले अनेक राज्यों से और हाथों से गुजरता था। फिर भी यह व्यापार बहुत लाभदायक होता था।1453 में उस्मानिया सल्तनत ने जब एशिया माइनर को जीत लिया और कुस्तुंतुनिया पर अधिकार कर लिया तो पूर्व और पश्चिम के बीच के पुराने व्यापारिक मार्ग तुर्कों के नियंत्रण में आ गए। इसके अलावा यूरोप और एशिया के व्यापार पर वेनिस और जेनेवा के व्यापारियों का अधिकार था और वे पश्चिमी यूरोप के नए राष्ट्रों, खासकर स्पेन और पुर्तगाल, को इन पुराने व्यापारिक मार्गां से होने वाले व्यापार में भागीदार नहीं बनाना चाहते थे। इसलिए पश्चिमी यूरोप के देश और व्यापारी भारत और इंडोनेशिया के स्पाइस आईलैंड (मसाले के द्वीप) के लिए नए और अधिक सुरक्षित समुद्री मार्गों की तलाश करने लगे, स्पाइस आईलैण्ड (मसाले के द्वीप) को तब ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था। उनकी मंशा व्यापार पर अरबों और वेनिसवासियों के एकाधिकार को तोड़ना, तुर्कों की शत्रुता मोल लेने से बचना और पूर्व के साथ सीधे व्यापार-संबंध स्थापित करना था। चूँकि 15वीं सदी में जहाज-निर्माण और समुद्री यातायात में बहुत प्रगति हुई थी, इसलिए वे यह काम करने में अच्छी तरह समर्थ थे। इसके अलावा पुनर्जागरण ने पश्चिमी यूरोप के लोगों में दुस्साहसी कार्य करने की भावना खूब भर दी थी। इस दिशा में पहला कदम पुर्तगाल और स्पेन ने उठाया। इन देशों के नाविकों ने अपनी-अपनी सरकारों की सहायता से और उनकी आज्ञा पर भौगोलिक खोजों का एक महान युग आंरभ किया। 1494 में स्पेन का कोलंबस भारत को खोजने निकला था लेकिन यह अमरीका की खोज कर बैठा। 1498 में पुर्तगाल के वास्को डि गामा ने यूरोप से भारत तक का एक नया और पूरी तरह से समुद्री मार्ग ढूंढ निकाला। वह केप ऑफ गुड होप होते हुए अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर कालीकट पहुँचा। वह जिस माल को लेकर वापस लौटा वह पूरी यात्रा की कीमत के 60 गुना दामों पर बिका। इन और ऐसे ही दूसरे समुद्री मार्गों की खोजों ने विश्व के इतिहास में एक नए अध्याय का सूत्रपात किया। 17वीं और 18वीं सदियों में विश्व व्यापार में बेहद बढ़ोत्तरी हुईं यूरोप को अब एक खूब लंबा-चौड़ा अमरीकी महाद्वीप उपलब्ध हो गया और यूरोप और एशिया के संबंध पूरी तरह बदल गए। 15वीं सदी के मध्य में अफ्रीका में यूरोपीय देशों ने प्रवेश किया तो उससे भी उनको आरंभिक पूंजी निर्माण का एक प्रमुख स्रोत प्राप्त हुआ। आंरभ में विदेशियों को अफ्रीकी सोने और हाथी दाँत ने आकर्षित किया। परंतु बहुत जल्द ही गुलामों का व्यापार अफ्रीका के साथ व्यापार का प्रमुख भाग बन गया। 16वीं सदी में इस व्यापार पर स्पेन और पुर्तगाल का एकाधिकार रहा। बाद में इस व्यापार में डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज व्यापारी छा गए। खासकर 1650 के बाद अनेक वर्षों तक हजारों अफ्रीकियों को गुलाम बनाकर वेस्ट इंडीज और उत्तरी तथा दक्षिण अमरीका...... में बेचा जाता रहा। कारखानों का माल लेकर गुलामों का व्यापार करने वाले जहाज यूरोप से अफ्रीका पहुँचते, अफ्रीका के तटों पर नीग्रो लोगों से माल की अदला-बदली करते, फिर इन दासों को लेकर अटलांटिक पार करते, वहाँ बागानों और खदानों की औपनिवेशिक पैदावार से उनकी अदला-बदली करते, और फिर इस माल को यूरोप में बेच देते। तिकोने व्यापार से होने वाला यही बेपनाह मुनाफा था जिस पर इग्लैंड और फ्रांस की व्यापारिक श्रेष्ठता स्थापित हुईं पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमरीका की समृद्धि अधिकांशतः गुलामों के इसी व्यापार पर और गुलामों के मेहनत से चलने वाले बागानों पर निर्भर थी। इसके अलावा दास-व्यापार और दासों की मेहनत से चल रहे बाजारों के मुनाफे से ही वह पूँजी बनी जो 18वीं और 19वीं सदी की...... औधोगिक क्रांति में काम आईं। बाद में भारत से ले जाई गई दौलत ने भी ऐसी ही भूमिका निभाई। 16वीं सदी में ही यूरोप के व्यापारियों और सैनिकों ने एशियाई देशों में घुसने और फिर उनको अधीन बनाने का लंबा सिलसिला शुरू किया। बेहद मुनाफा देनेवाले पूर्वी व्यापार पर लगभग एक सदी तक पुर्तगाल का एकाधिकार रहा। भारत में भी पुर्तगाल ने कोचीन, गोवा, द्यू और दमण में अपने व्यापारिक केंद्र खोले। पुर्तगालियों ने आरंभ से ही व्यापार के साथ शक्ति का भी प्रयोग किया। इस काम में उन्हें समुद्र पर राज करने वाले अपने हथियारबन्द जहाजों की श्रेष्ठता से मदद मिली। जमीन पर भारत और एशिया की सैनिक शक्ति बहुत अधिक थी, मगर उनके मुकाबले मुट्ठी भर पुर्तगाली सैनिक और जहाजी समुद्र में अपनी स्थिति बनाए रखने में सफल रहे। मुगलों की जहाजरानी के लिए खतरे पैदा करके वे मुगल सम्राटों से ही अनेक व्यापार संबंधी छूटें लेने में सफल रहे। गोवा पर 1510 में अधिकार करने वाला अलफांसों डि अलबुकर्क जब वायसराय था तब फारस की खाड़ी में स्थित हरमुज से लेकर मलाया में स्थित मलक्का तक और इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड तक एशिया के पूरे समुद्र तट पर पुर्तगालियों ने अधिकार जमा लिया। उन्होंने भारत के तटीय क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया और अपना व्यापार तथा अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाने और यूरोपीय प्रतिद्वदियों से अपने व्यापारिक एकाधिकार को सुरक्षित रखने के लिए लगातार लड़ाइयाँ लड़ते रहे। समुद्री डकैती और लूटपाट में भी वे पीछे न रहे। अमानवीय अत्याचार करने और अव्यवस्था फैलाने में भी उनका हाथ रहा। उनके बर्बर व्यवहार के बावजूद भारत में कुछ इलाकों पर कब्जा लगभग एक सदी तक बना रहा। इसका कारण यह था कि खुले समुद्र पर उनका राज चलता था, उनके सैनिक और प्रशासक कड़े अनुशासन के पाबंद थे और चूँकि दक्षिणी भारत मुगल साम्राज्य से बाहर था इसलिए मुगलों की ताकत का सामना उनको नहीं करना पड़ा। 16वीं सदी के उत्तरार्द्ध में इंग्लैण्ड और हालैण्ड और बाद में फ्रांस उभरती हुई व्यापारिक और प्रतिद्वन्दी शक्तियाँ थीं, लोगों ने विश्व-व्यापार पर स्पेनी और पुर्तगाली एकाधिकार के खिलाफ एक कड़ा संघर्ष छेड़ दिया। इस संघर्ष में स्पेन और पुर्तगाल की हार हुई। अब अंग्रेज और डच, व्यापारी केप आफ गुड होप होकर भारत जाने वाले रास्ते का प्रयोग करने लगे और पूर्व में अपना साम्राज्य बनाने की दौड़ में शामिल हो गए। अंत में इंडोनेशिया पर डचों का और भारत, श्रीलंका और मलाया पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 1602 में डच ईस्ट कंपनी की स्थापना हुई और डच सांसद ने एक चार्टर स्वीकार करके कंपनी को युद्ध छेड़ने, संधियाँ करने, इलाके जीतने और किले बनाने का अधिकार दे दिए। डचों की खास दिलचस्पी भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा और स्पाइस आईलैंड जैसे द्वीपों में थी जहाँ मसाले खूब पैदा होते थे। जल्द ही उन्होंने मलय जलडमरूमध्य और इंडोनेशियाई द्वीपों से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया और 1623 में इन क्षेत्रों पर अधिकार करने के प्रयास कर रहे अंग्रेजों को हराया। उन्होंने पश्चिमी भारत में गुजरात के सूरत, भड़ौंच, कैंबे और अहमदाबाद, केरल के कोचीन, मद्रास के नागपत्तनम्, आन्ध्र के मसुलीपट्टम, बंगाल के चिन्सूरा, बिहार के पटना और उत्तर प्रदेश के आगरा नगरों में भी व्यापार-केन्द्र खोले। 1658 में उन्होंने पुर्तगालियों से श्रीलंका को भी जीत लिया। एशियाई व्यापार पर भी अंग्रेज व्यापारियों की लालच भरी निगाहें जमीं थीं। पुर्तगालियों की सफलता, मसालों, मलमल, रेशम, सोने, मोतियों, दवाओं, पोर्सलीन, और एवोनी से भरे उनके जहाजों और इनसे प्राप्त भारी मुनाफों ने अंग्रेज व्यापारियों की भी आँखें चकाचौंध कर दीं और वे भी इस मुनाफा देने वाले व्यापार में शामिल होने के लिए बेचैन हो गए। 1599 मे मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से जाने जाने वाले कुछ व्यापारियों ने पूर्व से व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई। इस कंपनी को, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है, 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबैथ ने एक रायल चार्टर के द्वारा पूर्व से व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दे दिया। 1608 में इस कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्टरी खोलने का निश्चय किया, तब व्यापारिक केंद्रों को फैक्टरी नाम से ही जाना जाता था। कंपनी ने तब कैप्टन हाकिंस को जहाँगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए भेजा। परिणामस्वरूप एक शाही फरमान के द्वारा पश्चिमी तट की अनेक जगहों पर अंग्रेज कंपनी को फैक्टरियाँ खोलने की आज्ञा मिल गईं। मगर इस छूट से ही अग्रेंज संतुष्ट न थे। 1615 में उनका दूत, सर टामस रो, मुगल दरबार में पहुँचा। रो मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्टरियाँ खोलने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमान जारी कराने में सफल रहा। 1622 में जब सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने एक पुर्तगाली, राजकुमारी से शादी की तो पुर्तगालियों ने उसे बंबई का द्वीप दहेज में दे दिया। अंततः गोवा, द्यू और दमण को छोड़कर पुर्तगालियों के हाथ से भारत में उनके कब्जे वाले सारे इलाके निकल गए इंड़ोनेशिया के द्वीपों से हो रहे मसालों के व्यापार में भागीदारी को लेकर अग्रेंज कंपनी की डच कंपनी से ठन गईं इन दो शक्तियों के बीच रह-रहकर होने वाली लड़ाई 1654 में आरंभ हुई और यह 1667 में तब समाप्त हुई जब अग्रेंजों ने इंडोनेशिया पर सारे दावे छोड़ दिए और बदले में डचों ने भारत की अग्रेंज बस्तियों को न छूने का वादा किया। कम्पनी के व्यापारिक प्रभाव का विस्तार (1600-1744)भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत बहुत ही मामूली रही। 1623 तक इसने सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा और मसुलीपट्टम में फैक्टरियाँ स्थापित कर ली थी। आंरभ से उसने व्यापार और कूटनीति के साथ-साथ युद्धों का भी सहारा लेने और जिन क्षेत्रों में फैक्टरियाँ स्थापित की थीं, उन पर कब्जा करने के भी प्रयास किए।दक्षिण भारत में परिस्थितियाँ अंग्रेजां के अधिक अनुकूल थीं क्योंकि वहाँ उन्हें किसी शक्तिशाली भारतीय सरकार का सामना नहीं करना पड़ा। विजयनगर का महान साम्राज्य 1565 में ही नष्ट हो चुका था और उसकी जगह अनेक छोटे और कमजोर राज्य खड़े हो गए थे। उन्हें लालच देकर बहलाना या अपनी सैनिक शक्ति से डराना आसान था। अग्रेंजों ने दक्षिण में अपनी पहली फैक्टरी मसुलीपट्टम में 1611 में स्थापित की। पर जल्द ही उनकी गतिविधियों का केंद्र मद्रास हो गया जिसका पट्टा 1639 में वहाँ के स्थानीय राजा ने उन्हें दे दिया था। राजा ने उनको उस जगह की किलेबंदी करने, उसका प्रशासन चलाने और सिक्के ढालने की अनुमति इस शर्त पर दी कि बंदरगाह से प्राप्त चुंगी का आधा भाग राजा को दिया जाएगा। यहाँ अग्रेंजों ने अपनी फैक्टरी के इर्द-गिर्द एक छोटा सा किला बनाया जिसका नाम फोर्ट सेंट जार्ज पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि मुनाफे के लालची व्यापारियों की यह कंपनी शुरु से ही इस नीति पर अड़ी थी कि भारतीय उन्हें इस देश को जीतने का खर्च स्वंय दें। उदाहरण के लिए, कंपनी के कोर्ट आफ डायरेक्टर्स ने 1683 में मद्रास के अधिकारियों को लिखा कि हम चाहते हैं कि आप धीरे-धीरे नगर . . . .(मद्रास) को किलाबंद करें और किले को इतना मजबूत बनाएँ कि वह किसी भारतीय राजा या भारत में डच शक्ति के आक्रमण के सामने अडिग रहे . . . . पर हम आपसे यह भी चाहते हैं कि आप अपना काम इस प्रकार (लेकिन पूरी विनम्रता के साथ ) जारी रखें कि नगर निवासी ही सारी मरम्मत और किलाबंदी का पूरा खर्च उठाएँ।. . . . 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाल से बंबई का द्वीप प्राप्त किया और उसकी तत्काल किलेबंदी कर दी। बंबई के रूप में अंग्रेंजों का एक बड़ा और आसानी से रक्षा कर सकने योग्य बंदरगाह प्राप्त हुआ। इस कारण से और क्योंकि उस वक्त उभरती हुई मराठा शक्ति अंग्रेजों के व्यापार के लिए खतरे पैदा कर रही थी, पश्चिमी तट पर कंपनी के हेडक्वार्टर के रूप में सूरत का स्थान जल्द ही बंबई ने ले लिया। पूर्वी भारत में अँग्रेज कंपनी ने अपनी आरंभिक फैक्टरियों में एक की स्थापना 1633 में उड़ीसा में की थी। 1651 में उसे बंगाल के हुगली नगर में व्यापार की इजाजत मिल गई तब कंपनी ने जल्द ही पट्रना बालासोर, ढाका और बंगाल-बिहार के दूसरे स्थानों पर भी फैक्टरियाँ खोल ली। अब उसकी इच्छा थी कि बंगाल में उसकी एक स्वतंत्र बस्ती होनी चाहिए। अब वह भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के सपने देख रही थी ताकि मुगलों को मजबूर करके व्यापार में मनमानी करने की छूट ले ली जाए, भारतीयों को अपना माल सस्ता बेचने और कंपनी का माल मँहगा खरीदने के लिए मजबूर किया जा सके, प्रतिद्वंदी यूरोपीय व्यापारियों को बाहर रखा जाए और कंपनी का व्यापार भारतीय राजाओं की नीतियों से स्वतंत्र रहकर जारी रहे। राजनीतिक सत्ता स्थापित करके कंपनी भारतीय राजस्व पाने और इस तरह इस देश को इसी के साधनों से जीतने की आशा कर सकती थी। उस समय ऐसी योजनाएँ खुलकर सामने रखी गईं 1687 में कंपनी के डायरेक्टरों ने मद्रास के गवर्नर को सलाह दी कि............वह एक ऐसी नागरिक और सैनिक शक्ति स्थापित करे और राजस्व का सुरक्षित और इतना बड़ा स्रोत बनाए कि भारत में एक बड़े, मजबूत और हमेशा-हमेशा के लिए सुरक्षित ब्रिटिश राज्य की नींव डाली जा सके। 1689 में उन्होंने घोषणा की कि - हमारे राजस्व में वृद्धि हमारा उतना ही बड़ा उद्देश्य है जितना कि हमारा व्यापार। जिस समय बीसियों दुर्घटनाएँ हमारे व्यापार में बाधा डाल रही हों उस समय यही वस्तु है जो हमारी शक्ति को बनाए रख सकेगी। यही वस्तु है जो भारत में हमें एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगी . . . 1686 में जब अंग्रेजों ने हुगली को तहस-नहस कर दिया और मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी तब दोनों के बीच शत्रुता की शुरूआत हो गई पर अंग्रेजों ने स्थिति को पूरी तरह गलत समझा था और मुगलों की शक्ति को कम करके आंका था। औरगंजेब के शासन में मुगल साम्राज्य अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मामूली ताकत पर बहुत भारी था। युद्ध का अंत अंग्रेजों के लिए घातक रहा। उन्हें बंगाल स्थित उनकी फैक्टरियों से खदेड़ दिया गया और वे गंगा के मुहाने के एक द्वीप में शरण लेने के लिए बाध्य हो गए जो बीमारियों का गढ़ था। उनकी सूरत, मसुलीपट्टम और विशाखापतनम स्थित फैक्टरियों पर भी कब्जा हो गया और बंबई स्थित...... उनके किले पर घेरा पड़ गया। यह देखकर कि अंग्रेज अभी भी मुगल शक्ति से लड़ने में समर्थ नहीं हैं, उन्होंने एक बार फिर झुककर दरबार में हाजिरी बजाई और प्रार्थना की कि “उन्होंने जो अपराध किए हैं, उन्होंने क्षमा किया जाए।” उन्होंने भारतीय शासकों के संरक्षण में व्यापार करने की इच्छा प्रगट की। जाहिर है कि उन्हें सबक मिल चुका था। मुगल सम्राट से व्यापार संबंधी छूटें लेने के लिए एक बार फिर उन्होंने चापलूसी और विनम्रता का सहारा लिया। मुगल अधिकारियों ने अंग्रेजों की बदमाशी को फौरन माफ कर दिया। वे यह तो जान भी नहीं सकते थे कि अहानिकर दिखने वाले ये विदेशी व्यापारी एक दिन देश के लिए गंभीर खतरा बन जाएँगें। इसके बजाए उन्होंने यह मान लिया कि कंपनी के द्वारा किए जा रहे विदेशी व्यापार से भारतीय दस्तकारों और व्यापारियों को लाभ होता है और इस तरह सरकारी खजाने की आमदनी बढ़ती है। इसके अलावा जमीन पर कमजोर होने के बावजूद अंग्रेज समुद्रों में काफी मजबूत थे और इसलिए वे ईरान, पश्चिम एशिया, उत्तरी और पूर्वी अफ्रीका तथा पूर्वी एशिया के साथ होने वाले भारतीय व्यापार और जहाजरानी को पूरी तरह तहस-नहस करने में समर्थ थे। इसलिए औरंगजेब ने 1,50,000 रुपये हर्जाना लेकर उन्हें फिर से सूतानाटी, कलिकाता और गोविंदपुरी की जमींदारी प्राप्त कर ली और वहाँ उन्होंने अपनी फैक्टरी के इर्द-गिर्द फोर्ट विलियम नाम का किला बनाया। यही गाँव जल्द ही बढ़कर एक नगर बन गया जिसे अब कलकत्ता कहा जाता है। 1717 में कंपनी ने सम्राट फर्रुखसियर से एक फरमान प्राप्त किया जिसमें 1691 में उन्हें प्राप्त विशेषाधिकारों को दोबारा मान्यता दी गई और उन्हें गुजरात और दक्कन तक भी बढ़ा दिया गया था। लेकिन 18वीं सदी पूर्वार्द्ध में बंगाल पर मुर्शिद कुली खान और अली वर्दी खान जैसे शक्तिशाली नवाबों का शासन था। वे अंग्रेज व्यापारियों पर कड़ा नियंत्रण रखते थे तथा अपने विशेषाधिकारों के दुरूपयोग से उन्हें रोकते थे। उन्होंने अंग्रेजों को कलकत्ता की किलेबंदी को मजबूत बनाने और नगर पर स्वतंत्र रूप से शासन करने की छूट भी नहीं दी। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब का एक जमींदार होकर रह गईं। कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ तो पूरी न हुई, मगर उसका व्यापार पहले से बहुत अधिक फला-फूला। भारत से इंग्लैंड में होने वाला प्रतिवर्ष आयात 1708 में 5,00,000 पौंड का था, मगर 1740 तक वह 1,7,95,000 पौंड का हो गया। मद्रास, बंबई और कलकत्ता की अंग्रेज बस्तियाँ विकसित हो रहे नगरों का केंद्र बन गईं। बड़ी संख्या में भारतीय व्यापारी और बैंकर इन नगरों की ओर आकर्षित हुए। ऐसा अंशतः इस कारण कि मुगल साम्राज्य के बिखरने से इन नगरों के बाहर अनिश्चित और असुरक्षा की परिस्थितियाँ थीं। 18वीं सदी के मध्य तक मद्रास की जनसंख्या बढ़कर तीन लाख, कलकत्ता की दो लाख और बंबई की सत्तर हजार हो चुकी थी। 1600 के चार्टर में केप आफ गुड होप के पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार कंपनी को 15 वर्षों के लिए दिया गया था। इस कंपनी का स्वरूप एक पूरी तरह बंद निगम या इजारदारी जैसी थी। भारत में कंपनी की कोई फैक्टरी एक किलाबंद क्षेत्र जैसी होती थी जिसके अन्दर गोदाम, दफ्तर और कंपनी के कर्मचारियों के लिए घर होते थे। ध्यान दें कि इन फैक्टरियों में उत्पादन का कोई काम नहीं होता था। कंपनी के कर्मचारियों को बहुत कम वेतन मिलता था। उनकी वास्तविक आमदनी का स्त्रोत देश के ही अंदर का वह व्यापार था जिसकी छूट उन्हें कंपनी देती थी और इसी आमदनी के लिए ये कर्मचारी भारत में नौकरी करने के लिए बेचैन रहते थे। हाँ, भारत और यूरोप के बीच व्यापार करने का अधिकार केवल कंपनी के लिए सुरक्षित था। दक्षिण में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के टकरावनए-नए क्षेत्र और राजनीतिक सत्ता स्थापित करने की अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की जो महत्वकांक्षा 17वीं सदी के अंत में औरंगजेब के हाथों धूल चाटने लगी थी, वह 1740 के दशक में दोबारा उभरी जब मुगल साम्राज्य का पतन कुछ-कुछ स्पष्ट होने लगा। नादिरशाह के हमले के बाद केंद्रीय सत्ता का पतन खुलकर सामने आ गया था। लेकिन पश्चिमी भारत में विदेशी घुसपैट की बहुत गुंजाइश न थी, क्योंकि वहाँ जोशीले मराठों का प्रभुत्व था। पूर्वी भारत में अली वर्दी खान ने कड़ा नियंत्रण कायम कर रखा था। लेकिन दक्षिण भारत में परिस्थितियाँ विदेशी दुस्साहसकारियों के लिए धीरे-धीरे अनुकूल होती जा रही थीं। वहाँ औरगंजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय सत्ता नहीं रह गई थीं और 1748 में निजाम-उल-मुल्क आसफजाँह की मौत के बाद उसका मजबूत शासन भी नहीं रह गया था। इसके अलावा चौथ वसूलने के लिए मराठों सरदार हैदराबाद और दक्षिण के दूसरे भागों पर लगातार हमले करते रहते थे। इन हमलों के कारण राजनीतिक परिस्थितियाँ अनिश्चित हो गई थीं और प्रशासन नष्ट हो गया था। कर्नाटक में गद्दी के लिए भाई-भाई से लड़ रहा था।इन परिस्थितियों में विदेशियों को अपना राजनीतिक प्रभाव फैलाने और दक्षिण भारतीय राज्यों के मामलों पर नियंत्रण स्थापित करने में सहायता मिली। लेकिन व्यापारिक और राजनीतिक दावे सामने रखने में अंग्रेज अकेले न थे। वे 17वीं सदी के अंत तक अपने पुर्तगाली और डच प्रतिद्वंदियों को तो नष्ट कर चुके थे, पर फ्रांस एक नया प्रतिद्वंदी बनकर खड़ा हो गया था। 1744 से 1763 अर्थात् लगभग 20 वर्षों तक भारतीय व्यापार, संपत्ति और क्षेत्र पर अधिकार के लिए फ्रांसीसीयों और अंग्रेजों में भयानक युद्ध होते रहे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। पूर्वी तट पर कलकत्ता के पास चन्द्रनगर में और पांडिचेरी में उसने एक मजबूत स्थिति बना ली थी। पांडिचेरी को पूरी तरह किलाबंद किया गया था। पूर्वी तथा पश्चिमी तटों के बंदरगाहों में फ्रांसीसी कंपनी की कुछ और फैक्टरियाँ भी थीं। इसने हिंद महासागर में मॉरीशस और रियूनियन के द्वीपों पर भी कब्जा कर रखा था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बुरी तरह फ्रांस सरकार पर निर्भर थी जो अनुदान, कर्जे और दूसरी सुविधाएँ देकर उसकी सहायता करती रहती थी। फलस्वरूप, उस पर सरकार का बहुत अधिक नियंत्रण था और वही 1723 के बाद डायरेक्टरों की नियुक्ति करती रहती थी। कंपनी पर सरकार का यह नियंत्रण उसके लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुआ। उस समय फ्रांस में एक निरंकुश, अर्धसामंती और अलोकप्रिय सरकार थी जो भ्रष्टाचार, निकम्मापन और अस्थायित्व की मारी हुई थी। भविष्योन्मुखी न होकर यह सरकार पतित, परंपराओं में जकड़ी हुई और आम तौर पर समय की आवश्यकताओं को समझने से दूर थी। इस तरह की सरकार का नियंत्रण कंपनी के हितों के लिए घातक ही हो सकता था। 1742 में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैण्ड का युद्ध भड़क उठा। यूरोप का यह इग्लैण्ड-फ्रांस युद्ध जल्द ही भारत तक पहुँच गया और यहाँ दोनों ईस्ट इंडिया कंपनियाँ टकराने लगीं। 1748 में फ्रांस और इंग्लैण्ड का सामान्य युद्ध समाप्त हो गया। फिर भी भारत में व्यापार और क्षेत्रीय अधिकार की प्रतिद्वंद्विताएँ बनी रहीं, और इनका फैसला इस पार या उस पार होना ही था। इस समय पांडिचेरी में फ्रांसीसी गवर्नर-जनरल डुप्ले था जिसने यह नीति निकाली कि भारतीय शासकों के आपसी झगड़ों में अनुशासित और आधुनिक फ्रांसीसी सेना के द्वारा हस्तक्षेप किया जाए और एक के खिलाफ दूसरे का साथ देकर विजेता से मुद्रा, व्यापार और क्षेत्र संबंधी लाभ लिए जाएँ। इस तरह फ्रांसीसी कंपनी के लाभ के लिए और भारत से अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए उसने स्थानीय राजाओं, नवाबों और सरदारों के साधनों और सेनाओं का उपयोग करने की योजना बनाईं इस रणनीति की सफलता में केवल एक ही बात बाधक हो सकती थी, अर्थात् भारतीय शासकों द्वारा ऐसी विदेशी हस्तक्षेप की अनुमति देने से इनकार, पर भारतीय शासक देशभक्ति की भावना से प्रेरित न होकर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और लाभ की संकुचित भावना से प्रेरित थे। अपने देशी शत्रुओं से हिसाब चुकाने के लिए विदेशियों की सहायता माँगने में उन्हें कोई हिचक न थी। 1748 में कर्नाटक और हैदराबाद में एक ऐसी, स्थिति पैदा हो गई कि डुप्ले के षड्यंत्रकारी दिमाग को खुलकर खेलने का मौका मिला। कर्नाटक में चाँदा साहब ने नवाब के खिलाफ षड्यंत्र करना आरंभ कर दिया और हैदराबाद में निजामुल-मुल्क आसफजाह के मरने पर उसके बेटे नासिर जंग और पोते मुजफ्फर जंग में सत्ता के लिए गृहयुद्ध छिड़ गया। इस स्थिति को डुप्ले ने लाभ उठाया और चाँदा साहब तथा मुजफ्फर जंग से इस बात का गुप्त समझौता कर लिया कि वह अपने प्रशिक्षित फ्रांसीसी और भारतीय सेनिकों द्वारा उनकी सहायता करेगा। 1749 में इन तीन सहयोगियों ने अंबूर के युद्ध में अनवारउद्दीन को हराकर मार डाला। उसका बेटा मुहम्मद अली त्रिचुरापल्ली भाग गया। शेष कर्नाटक चाँदा साहब के अधिकार में आ गया और उसने पुरस्कारस्वरूप फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के निकट 80 गाँव दे दिए। फ्रांसीसी हैदराबाद में भी सफल रहे। नासिर जंग मारा गया और मुजफ्फर जंग निजाम अर्थात् दकन का सूबेदार बन गया। नए निजाम ने पांडिचेरी के निकट जमीनें और मसुलीपट्टम की प्रसिद्ध नगर फ्रांसीसी कंपनी को पुरूस्कार में दे दिए। उसने कंपनी को पाँच लाख रुपए दिए और उसकी सेनाओं को भी पाँच लाख रुपए दिए। डुप्ले को बीस लाख रुपयों के साथ एक जागीर भी मिली जिसकी वार्षिक आय एक लाख रुपए थी। इसके पूर्वी तट पर कृष्णा नदी से लेकर कन्या कुमारी तक के मुगल क्षेत्रों का उसे आनरेरी गवर्नर भी बना दिया गया। डुप्ले ने अपने सर्वश्रेष्ठ अफसर बुसी को फ्रांसीसी सेना की एक टुकड़ी के साथ हैदराबाद में नियुक्त किया। दिखावे के लिए इस नियुक्ति का उद्देश्य था शत्रुओं से निजाम की रक्षा करना, पर वास्तव में यह उसके दरबार में फ्रांसीसी प्रभाव बनाए रखने के लिए था। जब मुजफ्फर जंग अपनी राजधानी की ओर बढ़ रहा था तब एक दुर्घटना में वह मारा गया। बुसी ने फौरन निजामुल-मुल्क के तीसरे बेटे सलाबतजंग को गद्दी पर बिठा दिया। बदले में नए निजाम ने फ्रांसीसियों को आंध्र का वह क्षेत्र पुरस्कार में दे दिया जिसे उत्तरी सरकार कहा जाता है। इसमें चार जिले मुस्तफानगर, एल्लौर, राजामुंद्री और चिकाकोल शामिल थे। दक्षिण भारत में अब फ्रांसीसियों की शक्ति चरम सीमा पर थी। डुप्ले की योजनाओं को आशा से भी अधिक सफलता मिली थी। फ्रांसीसियों ने अपना काम भारतीय शासकों को मित्र बनाने से आंरभ किया था और अब अंत में उनको अपना आश्रित बना लिया था। लेकिन अंग्रेज अपने प्रतिद्वंदी की सफलताओं को खामोश बैठे नहीं देख रहे थे। फ्रांसीसी प्रभाव को कम करके और अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए वे नासिर जंग और मुहम्मद अली से मिलकर षड़यंत्र कर रहे थे। 1750 में उन्होंने मुहम्मद अली की ओर से अपनी पूरी ताकत लगा देने का निश्चय किया। नौजवान राबर्ट क्लाइव तब कंपनी की सेवा मे एक क्लर्क था। उसने प्रस्ताव किया कि कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर हमला करके त्रिचुरापल्ली में घिरे मुहम्मद अली पर फ्रांसीसीयों का दबाव कम किया जा सकता है। यह प्रस्ताव मान लिया गया। तब क्लाइव ने केवल 200 अंग्रेज और 300 भारतीय सैनिकों को लेकर अर्काट पर हमला किया और उसे जीत लिया। जैसी कि आशा थी, चाँदा साहब और फ्रांसीसीयों ने मजबूर होकर त्रिचुरापल्ली का घेरा उठा लिया। फ्रांसीसी सेनाओं की कई बार हार हुईं अब फ्रांसीसियों का सितारा डूब रहा था क्योंकि उनकी सेना और उनके जनरल अंग्रेजों का सामना नहीं कर पा रहे थे। अंत में भारतीय युद्ध के भारी खर्चों से परेशान होकर और अमरीकी उपनिवेशों के हाथ से निकल जाने के डर से फ्रांसीसी सरकार ने समझौता-वार्ता आरंभ की और 1754 में उसने अंग्रेजों की यह माँग मान ली की भारत से डुप्ले को वापस बुला लिया जाए। यह बात भारत में फ्रांसीसी कंपनी के भविष्य के लिए बहुत घातक सिद्ध हुईं। दोनों कंपनियों का यह अस्थायी समझौता 1756 में टूट गया जब इंग्लैण्ड और फ्रांस के बीच एक और युद्ध छिड़ गया। युद्ध के एकदम आरंभ में ही अंग्रेज बंगाल पर नियंत्रण करने में सफल रहे। इसका वर्णन इसी अध्याय में आगे किया गया है। इस घटना के बाद भारत में फ्रांसीसियों के लिए कुछ बचा ही नहीं। बंगाल की अथाह संपत्ति ने युद्ध का पलड़ा अंग्रेजों के पक्ष में झुका दिया। इस युद्ध की निर्णायक मुठभेड़ 22 जनवरी 1760 को वांडीवाश में हुई जब अंग्रेज जनरल आयर कूट ने लल्ली को हरा दिया। एक साल के अंदर-अंदर भारत में फ्रांसीसियों के हाथ से सब कुछ जाता रहा। युद्ध का अंत 1763 में पेरिस समझौते के साथ हुआ। इसके अनुसार फ्रांसीसियों को भारत स्थित उनकी सारी फैक्टरियाँ लौटा दी गईं, पर अब वे उनकी किलाबंदी नहीं कर सकते थे और न ही वहाँ सैनिक रख सकते थे। अब वे केवल व्यापार केंद्रों के रूप में काम कर सकती थीं। इसके बाद फ्रांसीसीयों को भारत में अंग्रेजों के संरक्षण में रहना था। दूसरी और अंग्रेज हिंद महासागर पर छा चुके थे। सभी यूरोपीय प्रतिद्वन्दियों को एक-एक करके हराने के बाद अब वे भारत-विजय के काम मे लग गए। फ्रांसीसियों और उनके भारतीय सहयोगियों के साथ अपने युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने कुछ महत्वपूर्ण और बहुमूल्य पाठ सीखे। पहला यह कि देश में राष्ट्रवादी भावना के अभाव के कारण वे भारतीय शासकों के आपसी झगड़ों का फायदा उठाकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ पूरी कर सकते थे। दूसरे, पश्चिमी तर्ज पर प्रशिक्षित यूरोपीय या भारतीय पैदल सेना आधुनिक अस्त्रों से लेस होकर और तोपखाने का सहारा लेकर पुरानी तर्ज वाली भारतीय सेनाओं को घमासान युद्धों में आसानी से हरा सकती थी। तीसरे, यह सिद्ध हो गया कि यूरोपीय तर्ज पर प्रशिक्षित और हथियारबंद भारतीय सैनिक यूरोपीय सैनिक जैसा ही अच्छा सैनिक बन सकता है और चूँकि भारतीय सैनिकों में भी राष्ट्रवादी भावना का अभाव था, इसलिए जो भी उसे अच्छा पैसा दे, वह उन्हें अपनी सेवा में रख सकता था। अंग्रेजों ने अब अंग्रेज अफसरों की देख-भाल में “सिपाही” कहे जाने वाले भारतीय सैनिकों की एक शक्तिशाली सेना बनाने का काम आरंभ कर दिया। इस सेना को अपना प्रधान साधन बनाकर और भारतीय व्यापार और क्षेत्रों के बेपनाह साधनों को अपने अधिकार में लाकर अब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्धों और क्षेत्रीय प्रसार के एक नए युग में कदम रखा। बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकारभारत मे ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ 1757 के प्लासी के युद्ध से माना जा सकता है जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजउद्दौला को हरा दिया। इसके पहले दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों के साथ अंग्रेजों के टकराव तो पूर्वाभ्यास मात्र थे। इन टकरावों से प्राप्त अनुभव का बंगाल में अच्छी तरह उपयोग किया गया।बंगाल तब भारत का सबसे उपजाऊ और धनी प्रांत था। इसके उद्योग-धंधे और व्यापार बहुत विकसित थे। प्रांत से ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके कर्मचारियों के लाभदायक व्यापारिक हित जुड़े थे। 1717 में मुगल सम्राट के एक शाही फरमान द्वारा अंग्रेजों को बहुमूल्य विशेषाधिकार मिले हुए थे। इस फरमान के अनुसार कंपनी को बिना कर चुकाएँ बंगाल से अपने सामान का आयात-निर्यात करने की आजादी मिली हुई थी और इन मालों की आवाजाही पर पास या दस्तक जारी रखने का उसे अधिकार था। कंपनी के कर्मचारियों को भी निजी व्यापार की छूट दी थी, हालाँकि उनको फरमान की सुरक्षा प्राप्त न थी। उनको वही कर देने पड़ते थे जो भारतीय व्यापारियों को। यह फरमान कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच झगड़े की जड़ बना हुआ था। इसका एक नतीजा यह था कि बंगाल की सरकार को राजस्व की हानि होती थी। दूसरे, कंपनी को दस्तक जारी करने का जो अधिकार मिला था, उसका दुरुपयोग कंपनी के कर्मचारी अपने निजी व्यापार पर भी कर न चुकाने के लिए करते थे। मुर्शिद कुली खान से लेकर अली वर्दी खान तक बंगाल के सभी नवाबों ने 1717 के फरमान की अंग्रेजों की व्याख्या पर आपत्ति की थी। उन्होंने कंपनी को खजाने में एकमुश्त रकमें देने के लिए मजबूर कर दिया था और दस्तकों के दुरुपयोग को सख्ती से बंद करा दिया था। इस मामले में कंपनी को भी नवाब का अधिकार मानना पड़ा था, मगर उसके कर्मचारी इस अधिकार से बचने और उसका उल्लंघन करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। पानी तब सर से ऊपर आ गया जब 1756 में युवक और जल्द क्रोधित हो जाने वाला सिराजुद्दौला अपने दादा अली वर्दी खान की जगह गद्दी पर बैठा। उसने अंग्रेजों से माँग की कि वे जिन शर्तों पर मुर्शिद कुली खान के जमाने में व्यापार करते थे, उन्हीं शर्तों पर अब भी व्यापार करें। अंग्रेजों ने जो दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों को हराकर खुद को ताकतवर महसूस करते थे, इस बात को मानने से इनकार कर दिया। वे अपने मालों पर नवाब को कर चुकाने को तैयार नहीं हुए, उल्टे उन्होंने उन भारतीय मालों पर भारी महसूल लगा दिए जो कलकत्ता आते थे। (कलकत्ता तब उनके नियंत्रण में था।) युवक नवाब स्वाभाविक था कि क्रोधित हो उठता। उसे शंका थी कि कंपनी उसकी शत्रु है और बंगाल की गद्दी की लड़ाई में उसके दुश्मनों का साथ दे रही है। बात तब हद से आगे बढ़ गई, जब नवाब से आज्ञा लिए बगैर कंपनी ने कलकत्ता की किलाबन्दी शुरू कर दी क्योंकि उसे तब चंद्रनगर में जमे फ्रांसीसियों के साथ युद्ध की आशंका थी। सिराज ने सही तौर पर इस हरकत को अपनी प्रभुता पर एक चोट समझा। कोई भी स्वतंत्र शासक अपनी धरती पर व्यापारियों की किसी निजी कंपनी को किले खड़ा करने और निजी युद्ध चलाने की छूट भला कैसे देता। दूसरे शब्दों में, सिराज इस पर तैयार था कि यूरोपीय लोग व्यापारी बनकर ही रहें और मालिक बनने की कोशिश न करें। उसने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों, दोनों को आज्ञा दी कि वे कलकत्ता और चंद्रनगर की अपनी किलेबंदियाँ गिरा दें और एक दूसरे से लड़ने से बाज आएँ। फ्रांसीसी कंपनी ने तो इस आज्ञा का पालन किया पर अंग्रेज कंपनी ने इसे मानने से इनकार कर दिया क्योंकि कर्नाटक में मिली विजय ने उसकी महत्वाकांक्षाओं और आत्मविश्वास दोनों को बढ़ा दिया था। वह नवाब की इच्छा के खिलाफ भी बंगाल में जमे रहने और अपनी शर्तों पर व्यापार करने पर अड़ी थी। इस कंपनी ने अपनी सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने के ब्रिटिश सरकार के अधिकार को स्वीकार किया था। ब्रिटेन मे ब्रिटिश सरकार ने उसके व्यापार और उसकी ताकत पर जो अंकुश लगाया था उसे कंपनी ने भीगी बिल्ली बनकर स्वीकार कर लिया था। 1693 में उसका चार्टर समाप्त हो जाने पर संसद ने पूर्व में व्यापार करने का अधिकार उससे छीन लिया था और तब कंपनी ने ब्रिटेन के सम्राट, संसद और राजनेताओं को भारी रिश्वत दी थी (केवल एक वर्ष में उसने 80 हजार पौंड घूस में दिए थे)। फिर भी अंग्रेज कंपनी माँग कर रही थी कि बंगाल के नवाब की चाहे जो आज्ञा हो, उसे बंगाल में मुक्त व्यापार के पूरे अधिकार मिलने चाहिए। यह नवाब की प्रभुता के लिए सीधे-सीधे एक चुनौती थी। कोई भी शासक संभवतः इस बात को स्वीकार न करता। सिराजुद्दौला में इतनी राजबुद्धि थी कि वह अंग्रेजों की चालों के दूरगामी प्रभावों को समझ सके। उसने उनसे अपने देश के कानून मनवाने का निर्णय किया। जोश मे आकर मगर बेकार की जल्दीबाजी में और र्प्याप्त तैयारी किए बिना सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार की अंग्रेज फैक्टरी पर कब्जा कर लिया, फिर कलकत्ता की ओर कूच किया और 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। तब अपनी आसानी से मिली इस जीत की खुशी मनाने वह कलकत्ता से वापस आ गया और अपने जहाजों में बैठकर भागते अंग्रेजों पर उसने कोई ध्यान नही दिया। यह एक गलती थी क्योंकि उसने दुश्मन की ताकत को कम करके आँका था। अंग्रेज अधिकारियों ने समुद्र के निकट फुल्टा में शरण ली जिसे उनकी जहाजरानी संबंधी श्रेष्ठता ने सुरक्षित बना दिया था। यहाँ अब वे मद्रास में सहायता मिलने की प्रतीक्षा करने लगे और इस बीच वे नवाब के दरबार के प्रमुख लोगों के साथ साजिश और गद्दारी का ताना-बाना बुनते रहे। इनमें प्रमुख थे-मीर जाफर जो मीर बख्शी के पद पर था, मानिकचंद जो कलकत्ता का अधिकारी था, अमीचंद जो एक धनी व्यापारी था, जगतसेठ जो बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर था और खादिम खान जिसकी कमान में नवाब की सेना का एक बड़ा भाग था। मद्रास से एडमिरल वाटसन और कर्नल क्लाइन की कमान में एक बड़ी....... नौसैनिक और सैनिक सहायता भी आ पहुँची। क्लाइव ने 1757 के आरंभ में दोबारा कलकत्ता को जीत लिया और नवाब को मजबूर करके अंग्रेजों की सारी माँगें मनवा लीं। अंग्रेज फिर भी संतुष्ट न हुए। उनका उद्देश्य इससे कहीं बहुत अधिक था। उन्होंने सिराजुद्दौला की जगह किसी पिट्ठू को बिठाने का फैसला किया। बंगाल की गद्दी पर युवक नवाब की जगह मीर जाफर को बिठाने की जो साजिश नवाब के दुश्मनों ने रची थी, उसमें शामिल होने के बाद अंग्रेजों ने नवाब के सामने ऐसी माँगें रखीं जिन्हें पूरा करना अंसभव था। दोनों पक्षों को लग गया कि उन्हें जल्द ही एक निर्णायक युद्ध लड़ना होगा। 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद से 20 मील दूर प्लासी के मैदान में उनकी सेनाएँ आमने-सामने हुईं। प्लासी का यह निर्णायक युद्ध केवल कहने को युद्ध था। अंग्रेज पक्ष के केवल 29 लोग मरे जबकि नवाब के लगभग 500 लोग मारे गए। मीर जाफर और राय दुर्लभ जैसे गद्दारों की कमान में नवाब की काफी सेना लड़ाई में उतरी ही नहीं। नवाब के सैनिकों का एक बहुत छोटा-सा हिस्सा ही मीर जाफर और मोहनलाल की अगुआई में बहादुरी से और अच्छी तरह लड़ता रहा। नवाब को मजबूर होकर भागना पड़ा। मगर वह पकड़ा गया और मीर जाफर के बेटे मीरन के हाथों मारा गया। बंगाल के कवि नवीनचन्द्र सेन के अनुसार प्लासी के युद्ध के बाद “भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात” का आरंभ हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया और फिर उससे अपना इनाम माँगने लगे। कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार का निर्विवाद अधिकार मिल गया। उसे कलकत्ता के पास चौबीस परगना की जमींदारी भी मिली। कलकत्ता पर हमले के हर्जाने के रूप में मीर जाफर ने कंपनी को और नगर के व्यापारियों को एक करोड़ सतहत्तर लाख रुपए दिए। साथ ही कंपनी के अधिकारियों को ‘उपहारों’ अर्थात् रिश्वतों के रूप में बड़ी-रकमें दी गईं। उदाहरण के लिए क्लाइव को बीस लाख रुपए से अधिक की रकमें मिलीं। क्लाइव ने बाद में अनुमान लगाया कि पिट्ठू नवाब से कंपनी और उसके नौकरों को तीन करोड़ रुपए से अधिक मिले हैं। इसके अलावा यह भी मान लिया गया कि ब्रिंटश व्यापारियों और अधिकारियों को अपने निजी व्यापार पर कोई कर नहीं देना होगा। प्लासी के युद्ध का असीम ऐतिहासिक महत्व रहा। इसने बंगाल तथा अंततः पूरे भारत पर अंग्रेजों के अधिकार का रास्ता खोल दिया। इसने अंग्रेजों की प्रतिष्ठा बढ़ाई और एक ही बार में अंग्रेजों को भारतीय साम्राज्य के प्रमुख दावेदारों की कतार में ला खड़ा किया। बंगाल से प्राप्त भारी राजस्व के सहारे उन्होंने शेष भारत की विजय का खर्च उठाया। बंगाल पर उनके नियंत्रण की अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की लड़ाई में निर्णायक भूमिका रही। अंतिम बात यह है कि प्लासी की विजय ने कंपनी और उसके नौकरों को इस योग्य बनाया कि वे बंगाल की असहाय जनता को लूटकर बेपनाह दौलत जमा कर सकें। जैसा कि ब्रिटिश इतिहासकार एडवर्ड थांप्सन और जी. टी. गैरेट ने लिखा है - किसी क्रांति का आयोजन करना दुनिया का सबसे लाभदायी खेल समझा गया है। अंग्रेजों के मन में सोने का ऐसा लालच भर गया जो कोर्तेस और पिजारो के काल के स्पेनवासियों के बाद कभी देखने को नहीं मिला था। अब खास तौर पर बंगाल को तब तक चैन नहीं मिलने वाला था जब तक उसके खून की एक-एक बूँद न निचुड़ जाए। हालांकि मीर जाफर ने कंपनी की सहायता से गद्दी पाई थी, मगर जल्द ही वह इस सौदे पर पछताने लगा। कंपनी के अधिकारियों की उपहार और रिश्वत संबंधी माँगों ने जल्द ही उसका खजाना खाली कर दिया और इस बारे में पहल खुद क्लाइव ने की। जैसा कि कर्नल मालसन ने लिखा है, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य था कि “जितना लूट सको, लूटो और यह कि मीर जाफर सोने की एक ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो।” खुद कंपनी के लालच का कोई मुकाबला न था। कंपनी के डायरेक्टरों ने यह मानकर कि उनके हाथ कामधेनु गाय लग गई है और यह कि बंगाल की दौलत कभी खत्म न होगी, यह आज्ञा जारी की कि बंबई और मद्रास प्रेंसिडेंसियों का भी बंगाल खर्च उठाए और अपने राजस्व से कंपनी के भारत से होने वाले पूरे निर्यात का माल खरीदे। कंपनी अब भारत के साथ व्यापार ही नहीं कर रही थी बल्कि बंगाल के नवाब पर अपने नियंत्रण का फायदा उठाकर प्रांत की दौलत भी लूट रही थी। मीर जाफर को जल्द ही पता चल गया कि कंपनी और उसके अधिकारियों की सारी माँगें पूरी कर पाना असंभव था। अब ये अधिकारी भी अपनी आशाएँ पूरी न कर पाने के कारण नवाब की आलोचना करने लगे थे। इसलिए उन्होंने अक्टूबर 1760 में मीर जाफर को मजबूर किया कि वह अपने दामाद, मीर कासिम के हक मे गद्दी छोड़ दे। मीर कासिम ने अपने आकाओं की इस कृपा के बदले कंपनी को बर्दबान, मिदनापुर और चटगाँव जिलों की जमींदारी सौंप दी और बड़े अंग्रेज अधिकारियों को अच्छे अच्छे उपहार दिए जिनकी कुल कीमत 29 लाख रुपए थी। फिर भी मीर कासिम अंग्रेजों की इच्छाएँ पूरी न कर सका और जल्द ही वह बंगाल में उनकी स्थिति और उनकी चालों के लिए खतरा बन गया। वह एक योग्य, कुशल और शक्तिशाली शासक था और खुद को विदेशी नियंत्रण से मुक्त कराने पर अड़ा हुआ था। उसने महसूस किया कि अपनी आजादी बनाए रखने के लिए एक भरा हुआ खजाना और एक कुशल सेना की आवश्यकता थी। इसलिए उसने सार्वजनिक अव्यवस्था को संभालने, राजस्व प्रशासन से भ्रष्टाचार मिटाकर अपनी आय बढ़ाने और यूरोपीय तर्ज पर एक आधुनिक और अनुशासित सेना खड़ी करने की कोशिशें कीं। यह सब अंग्रेजों को पसंद न था। उन्हें सबसे ज्यादा नापसंद यह बात थी कि नवाब 1717 के फरमान का कंपनी के नौकरों द्वारा दुरुपयोग रोकने की कोशिश कर रहा था जबकि इन नौकरों की माँग थी कि उनका माल चाहे निर्यात के लिए हो या यहीं उपयोग के लिए, उस पर कोई चुंगी न लगाई जाए। इससे हानि भारतीय व्यापारियों को होती थी क्योंकि उन्हें वे कर भी देने पड़ते थे जिनसे विदेशी पूरी तरह मुक्त थे। इसके अलावा कंपनी के नौकर गैरकानूनी ढंग से अपने भारतीय व्यापारी मित्रों को दस्तकें (पास) बेच देते थे और ये भारतीय इस तरह अंदर के करों के भुगतान से बच जाते थे। इस दुरुपयोगों के कारण ईमानदार भारतीय व्यापारी बेईमानी से भरी प्रतियोगिता में बर्बाद होने लगे और नवाब के हाथ से राजस्व का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत जाता रहा। साथ ही, कंपनी और उसके नौकर भारतीय अधिकारियों और जमींदारों को उपहार और घूस देने के लिए बाध्य करते थे। वे भारतीय दस्तकारों, किसानों और व्यापारियों को अपना माल अंग्रेजों को सस्ता बेचने और अंग्रेजों को माल मँहगा खरीदने पर मजबूर करते थे। जो लोग ऐसा न करते उन्हें अकसर कोड़े मारे जाते या जेल भेज दिया जाता। हाल ही में एक ब्रिटिश इतिहासकार पर्सीवल स्पियर ने इस काल को “खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूट-पाट का युग” बताया है। वास्तव में अपनी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध बंगाल, धीरे-धीरे नष्ट हो रहा था। मीर कासिम को लगा कि अगर ये बदमाशियाँ जारी रही तो वह कभी बंगाल को शक्तिशाली न बना सकेगा और न ही खुद को कंपनी के चुंगल से मुक्त कर सकेगा। इसलिए उसने यह कड़ा कदम उठाया कि आंतरिक व्यापार पर सभी महसूल खत्म कर दिए और इस तरह अपनी प्रजा को वे छूटें दे दीं जो अंग्रेजों ने बलपूर्वक प्राप्त की थीं। मगर विदेशी व्यापारी अपने और भारतीय व्यापारियों के बीच समानता हो, ‘यह बर्दाश्त करने को अब तैयार न थे। उन्होंने भारतीय व्यापारियों पर दोबारा महसूल लगाए जाने की माँग की। एक और लड़ाई अब सामने नजर आ रही थी। सच्चाई यह थी कि अब बंगाल के दो स्वामी नहीं हो सकते थे। मीर कासिम तो यह समझता था कि वह एक स्वतंत्र शासक है, मगर अंग्रेज यह माँग कर रहे थे कि वह उनके हाथों की कठपुतली बना रहे क्योंकि उन्होंने ही उसे गद्दी पर बिठाया था। अनेक लड़ाइयों के बाद मीर कासिम 1763 में हरा दिया गया। तब वह अवध भाग गया जहाँ उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और भगोड़े मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ एक समझौता किया। कंपनी की सेना के साथ इन तीनों सहयोगियों की मुठभेड़ 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में हुई जिसमें ये तीनों हारे। यह भारतीय इतिहास के सबसे निर्णायक युद्धों में से एक था क्योंकि इसने दो बड़ी भारतीय शक्तियों की संयुक्त सेना पर अग्रेंजी सेना की श्रेष्ठता सिद्ध कर दी। इस युद्ध ने अग्रेंजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का निर्विवाद शासक बना दिया और अवध भी उनकी दया का मुहताज हो गया। इस बीच 1765 में क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनकर लौट आया था। उसने बंगाल में सत्ता पाने और शासन के सारे अधिकार नवाब से छीनकर कंपनी को दिलाने का यह अवसर न चूकने का फैसला किया। 1763 में अग्रेंजों ने मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया था। और कंपनी तथा उसके अधिकारियों के लिए बड़ी-बड़ी रकमें ली थी। मीर जाफर के मरने पर उन्होंने उसके दूसरे बेटे निजामुद्दौला को गद्दी पर बिठाया और बदले में उससे 20 फरवरी 1765 को एक नई संधि पर दस्तखत करा लिए। इस संधि के अनुसार नवाब को अपनी अधिकांश सेना भंग कर देना था और बंगाल का शासन एक नायब सूबेदार के सहारे चलाना था जिसकी...... नियुक्ति कंपनी करती और जिसे कंपनी की स्वीकृति के बिना नहीं हटाया जा सकता था। इस तरह कंपनी ने बंगाल के प्रशासन (निजामत) पर पूरा अधिकार जमा लिया। कंपनी की बंगाल कौंसिल के सदस्यों ने एक बार फिर नए नवाब से लगभग 15 लाख रुपए झटक लिए। शाह आलम द्वितीय अभी भी साम्राज्य का नाममात्र का प्रमुख था। उससे कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी (अर्थात् राजस्व वसूल करने का अधिकार) प्राप्त कर लिया। इस तरह बंगाल के ऊपर उसके नियंत्रण को कानूनी मान्यता मिल गई और इस सबसे समृद्ध भारतीय प्रांत का पूरा राजस्व उसके हाथों में आ गया। बदले मे कंपनी ने शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए दिए और उसे कोरा और इलाहाबाद जिले भी जीतकर दे दिए। सम्राट 6 वर्षों तक इलाहाबाद के किले में अंग्रेजों का लगभग कैदी बनकर रहा। अवध के नवाब शुजाउद्दौला को भी लड़ाई के हर्जाने के रूप में कंपनी को पचास लाख रुपए देने पड़े। इसके अलावा, दोनों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए। इसके अनुसार अगर नवाब पर बाहरी हमला होता तो कंपनी उसकी सहायता करती, शर्त यह थी कि नवाब को अपनी सहायता के लिये भेजी गई सेना के...... बदले में कंपनी को धन देना पड़ता। इस समझौते के द्वारा अवध का नवाब भी कंपनी का आश्रित बनकर रहा गया। 1766, 1767 और 1768 के केवल तीन वर्षों में ही बंगाल से 57 लाख पौंड की दौलत ले ली गई। दोहरी शासन-प्रणाली के दुरुपयोग और संपत्ति की लूट ने उस बदनसीब प्रांत को निर्धन और खोखला बना दिया। 1770 में बंगाल में एक अकाल पड़ा और यह मानव इतिहास के सबसे भयानक अकालों में से एक था। लाखों लोग मर गए और बंगाल की लगभग एक-तिहाई जनता इसके दुष्प्रभावों का शिकार हुई। हालाँकि अकाल का कारण वर्षा का न होना था, मगर कंपनी की नीतियों ने इसके दुष्प्रभावों को और भयानक बना दिया था। वारेन हेस्टिंग्ज (1772-85) और कार्नवालिस (1786-93) के युद्ध1772 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की एक प्रमुख शक्ति बन चुकी थी, और अब आगे-विजय से पहले इसके इंग्लैंड में बैठे डायरेक्टर और भारत में इसके अधिकारी बंगाल में अपनी स्थिति को मजबूत बना लेना चाहते थे। फिर भी भारतीय राजाओं के आपसी मामलों में दखल देने की उनकी आदत ने और इलाका तथा धन के उनके लालच ने जल्द ही उनको अनेक युद्धों में उलझा दिया।1766 में उन्होंने मैसूर के हैदर अली पर हमले में हैदराबाद के निजाम का साथ दिया। पर हैदर अली ने मद्रास कौंसिल को अपनी शर्तों पर शांति की संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। फिर 1775 में अंग्रेजों का मराठों से टकराव हुआ। तब मराठों में शासन के लिए एक कड़ा संघर्ष चल रहा था जिसमें बालक पेशवा माधवराव द्वितीय के समर्थक नाना फड़नीस के नेतृत्व में एक ओर थे और रघुनाथ राव के समर्थक दूसरी ओर थे। बंबई के ब्रिटिश अधिकारियों ने रघुनाथ राव की ओर हस्तक्षेप का निश्चय किया। उन्हें आशा थी कि उनके देशवासियों ने बंगाल और मद्रास में जो कुछ कर दिखाया था, वैसा ही कुछ काम वे कर सकेंगे और नतीजे में उनके धन-लाभ होगा। इस कारण वे मराठों के साथ एक लंबी लड़ाई में उलझ गए जों 1772 से 1782 तक चली। यह भारत में ब्रिटिश शक्ति के लिए बहुत अशुभ घड़ी थी। सभी मराठा सरदार पेशवा और उसके प्रधानमंत्री नाना फड़नीस की ओर से एक हो गए। दक्षिण भारत के शासक अपने बीच अंग्रेजों की उपस्थिति से बहुत दिनों से चिढ़े हुए थे और इस घड़ी का फायदा उठाकर हैदर अली और निजाम ने कंपनी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इस तरह अब अंग्रेजों को मराठों, मैसूर और हैदराबाद के शक्तिशाली गठजोड़ का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा 1776 में अमरीका की जनता ने विद्रोह कर दिया था और इस लड़ाई में अंग्रेजों की हार पर हार हो रही थी। फ्रांसीसी अपनी पुराने प्रतिद्वन्दियों की इन कठिनाइयों का फायदा उठाना चाहते थे और उसका भी मुकाबला अंग्रेजों को करना पड़ रहा था। पर भारत में इस समय अंग्रेजों का नेतृत्व जोशीला और अनुभवी गवर्नर-जनरल वारेन हेस्टिंग्ज कर रहा था। उसने पूरे विश्वास और दृढ़ता के साथ अपने कदम उठाए। युद्ध मे जीत किसी ‘पक्ष’ की नहीं हुई और युद्ध थम सा गया। 1782 की सल्बई की संधि के साथ शांति स्थापित हुई। इस संधि के अनुसार स्थिति को जैसी वह थी, वैसी ही बनाए रखना था। इससे अंग्रेज भारतीय शासकों की मिली-जुली शक्ति का सामना करने से बच गए। इस युद्ध में जिसे प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध कहा जाता है, किसी की जीत नहीं हुई। मगर इससे अंग्रेज 20 वर्षों के लिए मराठों की ओर से निश्चित हो गए जो तब भारत की सबसे बड़ी शक्ति थे। इस समय का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने बंगाल प्रेसीडेंसी में अपनी स्थिति को मजबूत बनाया जबकि मराठे आपसी झगड़ों में अपनी शक्ति बर्बाद करते रहे। इसके आलावा सल्बई की संधि के कारण अंग्रेज मैसूर पर दबाव डालने में सफल रहे, क्योंकि मराठों ने उनसे वादा किया कि हैदर अली से अपनी खोई हुई जमीन वापस लेने में वे अंग्रेजों की सहायता करेंगे। अंग्रेज फिर एक बार भारतीय शासकों में फूट डालने में सफल रहे। इस बीच 1780 में हैदर अली से युद्ध एक बार फिर आंरभ हो गया। अपने पुराने कारनामे दोहराते हुए हैदरअली ने कर्नाटक में अंग्रेज सेनाओं को बार-बार हराया और उन्हें बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण करने पर बाध्य कर दिया। जल्द ही लगभग पूरा कर्नाटक उसके कब्जे में आ गया। पर अंग्रेजों की शक्ति और कूटनीति ने एक बार फिर उन्हें बचा लिया। वारेन हेस्टिंग्ज ने निजाम को गुंटूर का जिला देकर तोड़ लिया और उसे ब्रिटिश विरोधी गठजोड़ से अलग करा दिया। 1781-82 में उसने मराठों से शांति-समझौता कर लिया और इस तरह सेना का एक बड़ा भाग मैसूर के साथ युद्ध के लिए मुक्त हो गया। जुलाई 1781 में आयरकूट की कमान में ब्रिटिश सेना ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराकर मद्रास को बचा लिया। दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद उसके बेटे टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा चूँकि दोनों में से कोई पक्ष दूसरे को हराने की स्थिति में न था, इसलिए उन्होंने मार्च 1784 में शांति-संधि कर ली और एक-दूसरे को जीते हुए सारे इलाके लौटा दिए। इस तरह यह तो सिद्ध हो गया कि अंग्रेज अभी इतने कमजोर हैं कि मराठों या मैसूर को नहीं हरा सकते, पर भारत में अपने बल-बूते पर खड़े होने की योग्यता उन्होंने निश्चित ही दिखा दी थी। मैसूर के साथ अंग्रेजों का तीसरा टकराव उनके लिए अधिक लाभप्रद सिद्ध हुआ। 1784 की संधि ने टीपू और अंग्रेजों के झगड़े की जड़ को समाप्त नहीं किया था, बल्कि युद्ध को केवल टाल भर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी टीपू के जानी दुश्मन थे। वे उसे दक्षिण में अपना सबसे शक्तिशाली शत्रु समझते थे जो दक्षिण भारत की जीत में उनके लिए प्रमुख बाधक बना हुआ था। टीपू भी अंग्रेजों से सख्त नफरत करता था और अपनी स्वाधीनता के लिए सबसे बड़ा खतरा समझकर उन्हें भारत से बाहर खदेड़ने पर अड़ा हुआ था। दोनों के बीच 1789 में फिर युद्ध भड़क उठा और अंततः 1792 में टीपू की हार हुई। श्रीरंगपट्टम में हुई संधि के अनुसार टीपू ने अपना आधा राज्य अंग्रेजों और उसके सहयोगियों को दे दिया और 330 लाख रुपए हर्जाना भी दिया। लार्ड वेलेजली के काल में अंग्रेजों का प्रसारभारत में ब्रिटिश शासन का दूसरा बड़ा प्रसार लार्ड वेलेजली (1798-1805) के काल में हुआ। वह 1798 में ऐसे समय में भारत आया था जब अंग्रेज पूरी दुनिया में फ्रांस के साथ जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे।इस समय तक अंग्रेजों की नीति यह थी कि अपने लाभों और साधनों की स्थिति को सुदृढ़ बनाया जाए और नए इलाके तभी जीते जाएँ जब बड़े भारतीय शासकों को दुश्मन बनाए बिना सुरक्षापूर्वक ऐसा कर पाना संभव हो। वेलेजली ने फैसला किया कि समय आ चुका है कि जितने अधिक भारतीय राज्य ब्रिटिश नियंत्रण में लाए जाएँ। 1797 तक दो प्रमुख भारतीय शक्तियों अर्थात् मैसूर और मराठों की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। भारत में राजनीतिक परिस्थितियाँ प्रसार के लिए अनुकूल थीं क्योंकि प्रसार करना अब आसान भी था और लाभप्रद भी। अपने राजनीतिक उद्देश्य पूरे करने के लिए वेलेजली ने तीन उपायों का सहारा लिया-सहायक संधि प्रथा, खुला युद्ध और पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों का इलाका हड़पना। किसी भारतीय शासक को पैसा लेकर ब्रिटिश सेना भी मदद देने की नीति तो बहुत पुरानी थी, फिर भी वैलेजली ने इस नीति को एक निश्चित रूपरेखा दी और इसका दुरुपयोग भारतीय शासकों को कंपनी के अधीन बनाने के लिए किया। उसकी सहायक संधि प्रथा की नीति के अनुसार किसी सहयोगी भारतीय राज्य के शासक को ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखनी पड़ती थी तथा उसके रख-रखाव के लिए अनुदान देना पड़ता था। यह सब कहने को उसकी सुरक्षा के लिए किया जाता था, मगर वास्तव में यह उस भारतीय शासक से कंपनी को खिराज दिलवाने का एक ढंग था। कभी-कभी कोई शासक वार्षिक अनुदान न देकर अपने राज्य का कोई भाग दे देता था। सहायक संधि के अनुसार आम तौर पर भारतीय शासक को यह भी मानना पड़ता था कि वह अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजीडेंट रखेगा, अंग्रेजों की स्वीकृति के बिना किसी और यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रखेगा...... और गवर्नर-जनरल से सलाह किए बिना किसी दूसरे भारतीय शासक से कोई वार्ता नहीं करेगा। इसके बदले अंग्रेज उस शासक की दुश्मनों से रक्षा करने का वचन देते। वे सहयोगी के अंदरूनी मामलों में दखल न देने का भी वादा करते, पर यह वादा ऐसा था जिसे कभी-कभी ही पूरा किया गया। वास्तव में सहायक संधि पर हस्ताक्षर करके कोई भारतीय राज्य अपनी स्वाधीनता लगभग गवाँ ही बैठता था। वह आत्म रक्षा के, कूटनीतिक संबंध बनाने के, विदेशी विशेषज्ञ रखने के तथा पड़ोसियों के साथ आपसी झगड़े के अधिकार ही खो बैठता था। वास्तव में उस भारतीय शासक की बाहरी मामलों में सारी प्रभुता समाप्त हो जाती और वह ब्रिटिश रेजीडेंट के अधिकाधिक अधीन होता जाता जो राज्य के रोजमर्रा के प्रशासन में हस्तक्षेप करता रहता था। इसके अलावा इस प्रथा के कारण सुरक्षा प्राप्त राज्य अंदर से खोखला होने लगता था। अंग्रेजों की दी हुई सहायक सेना का खर्च बहुत अधिक होता था और वास्तव में वह उस राज्य की क्षमता से काफी बाहर होता था। मनमाने ढंग से तय किए गए और बनावटी ढंग से बढ़ाए जाने वाले इस अनुदान के कारण उस राज्य की अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न और जनता निर्धन हो जाती थी। इस सहायक संधि प्रथा के कारण सुरक्षा प्राप्त राज्य की सेनाएँ भी भंग कर दी गईं। लाखों सैनिक और अधिकारी अपनी पैतृक जीविका से वंचित हो गए जिससे देश में बदहाली और गरीबी फैल गई। इसके अलावा सुरक्षाप्राप्त राज्यों के शासक अपनी जनता के हितों को अनदेखा तथा उनका दमन करने लगे क्योंकि अब उन्हें जनता का डर नहीं रहा गया था। चूँकि अंग्रेजों ने उन्हें अन्दरूनी और बाहरी दुश्मनों से रक्षा का वचन दिया था, इसलिए उनमें अब अच्छे शासक बनने का कोई लोभ नहीं रह गया। दूसरी तरफ सहायक संधि की प्रथा अंग्रेजों के लिए अत्यन्त लाभदायक थी। अब वे भारतीय राज्यों के खर्च पर एक बड़ी सेना रख सकते थे। अब वे अपने खुद के क्षेत्र से बहुत दूर लड़ाईयाँ लड़ सकते थे क्योंकि कोई भी युद्ध होता तो या तो उनके सहयोंगियों के क्षेत्र में होता या उनके शत्रुओं के। वे अपने सुरक्षा प्राप्त सहयोगी की रक्षा और विदेशी संबंधों के मामलों पर पूरा नियंत्रण रख रहे थे, उसकी जमीन पर एक शक्तिशाली सेना रखते थे और जब भी चाहे उसे ‘अयोग्य’ घोषित करके उसका शासन समाप्त कर उसके क्षेत्र को हड़प सकते थे। जहाँ तक अंग्रेजों का सवाल था, सहायक संधि की यह प्रथा, एक ब्रिटिश लेखक के शब्दों में, “अपने सहयोंगियों को बकरों की तरह तब तक खिला-पिलाकर मोटा रखने की प्रथा थी जब तक वे जिबह करने के काबिल न हो जाएँ।” लार्ड वैलेजली ने 1798 और 1880 में हैदराबाद के निजाम के साथ सहायक संधियाँ कीं। सहायक सेनाओं के खर्च के नाम पर नगद पैसा देने के बजाए निजाम ने कंपनी को अपने राज्य का एक भाग दे दिया। 1801 में अवध के नवाब को सहायक संधि के लिए मजबूर किया गया। एक बड़ी सहायक सेना के बदले में नवाब को मजबूर होकर अपना लगभग आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा जिसमें रूहेलखंड का इलाका और गंगा-यमुना का दोआबा आ जाते थे। उसकी अपनी सेना लगभग पूरी तरह भंग कर दी गई और अंग्रेजों को यह अधिकार मिल गया कि वे उसके राज्य के किसी भी भाग में अपनी सेना तैनात कर सकें। वेलेजली मैसूर, कर्नाटक और सूरत के साथ और भी कड़ाई से पेश आया। निश्चित ही मैसूर का टीपू सुल्तान कभी सहायक संधि के लिए तैयार नहीं हुआ। उल्टे उसे 1792 में अपना जो आधा राज्य देना पड़ा था, उसी को वह कभी भूल न सका। वह अंग्रेजों के साथ अपने अवर्श्यभावी युद्ध के लिए अपनी सेना को लगातार मजबूत बनाता रहा। उसने क्रांतिकारी फ्रांस के साथ गठजोड़ की बात भी चलाई। उसने एक ब्रिटिश-विराधी गठजोड़ बनाने के लिए अफगानिस्तान, अरब और तुर्की को भी अपने दूत भेजे। ब्रिटिश सेना ने 1799 में टीपू पर हमला किया और एक संक्षिप्त मगर भयानक युद्ध के बाद फ्रांसीसी सहायता पहुँचने के पहले ही उसे हरा दिया। टीपू ने अभी भी गिड़गिड़ाकर शांति की भीख माँगने से इनकार कर दिया। उसने गर्वपूर्वक घोषणा की कि “काफिरों का दयनीय दास बनकर और उनके पेंशन प्राप्त राजाओं और नवाबों की सूची में शामिल होकर जीने से अच्छा एक योद्धा की तरह मर जाना हैं।” अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम की रक्षा करते हुए वह 4 मई 1799 को बहादुरी की मौत मरा। उसकी सेना अंत तक वफादार बनी रही। टीपू का लगभग आधा राज्य अंग्रेज और उनके सहयोगी निजाम के बीच बँट गया। मैसूर राज्य का शेष भाग उन राजाओं के वंशजों को वापस दे दिया गया जिनसे हैदर अली ने राज्य छीना था। नए राजा को मजबूर करके एक विशेष सहायक संधि पर हस्ताक्षर कराए गए कि गवर्नर-जनरल आवश्यकता समझे तो राज्य का शासन खुद संभाल ले। वास्तव में मैसूर को कंपनी पर पूरी तरह आश्रित बना दिया गया। 1801 में लार्ड वेलेजली ने कर्नाटक के पिट्ठू नवाब पर एक नई संधि लाद दी और उसे मजबूर किया कि वह पेंशन लेकर अपना राज्य कंपनी को सौंप दें। अब मैसूर से मालाबार समेत जो क्षेत्र छीने गए थे, उनमें कर्नाटक को मिलाकर मद्रास प्रेसिडेंटी बनाई गई जो 1947 तक जारी रही। इसी तरह तंजौर और सूरत राज्य भी हड़प लिए गए और उनके शासकों को पेंशन देकर किनारे कर दिया गया। अब एक प्रमुख शक्ति के रूप में केवल मराठे ही ब्रिटिश प्रभुत्व से बचे हुए थे। अब वेलेजली ने उनकी ओर ध्यान देना आंरभ किया और उनके अंदरूनी मामलों में खुलकर हस्तक्षेप करने लगा। इस समय मराठा साम्राज्य पाँच बड़े सरदारों का एक महासंघ था। ये थे पूना का पेशवा, बड़ौदा का गायकवाड़, ग्वालियर का सिंधिया, इंदौर का होलकर और नागपुर का भांसले। पेशवा इस महासंघ का नाममात्र का प्रमुख था। लेकिन ये सभी सरदार आपसी झगड़ों में कट-मर रहे थे और बढ़ते हुए विदेशियों के खतरे की ओर से बेखबर थे। वेलेजली ने बार-बार पेशवा और सिंधिया के आगे सहायक संधि का प्रस्ताव रखा था। मगर दूरदर्शी नाना फड़नीस ने इस जाल में फँसने से इंकार कर दिया था। मगर 25 अक्टूबर 1802 को जब दीवाली के दिन होल्कर ने पेशवा और सिंधिया की मिली-जुली सेना को हरा दिया जो कायर पेशवा बाजीराव द्वितीय भागकर अंग्रेजों की शरण में जा पहुँचा और वर्ष 1802 के अंतिम दिन उसने बसाई में एक सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। यह जीत कुछ आसानी से ही मिल गई थी। मगर एक बात पर वेलेजली गलत था - अभिमानी मराठा सरदार बिना लड़ाई के अपनी स्वाधीनता की परंपरा छोड़ने वाले नहीं थे। मगर संकट की इस घड़ी में भी वे साझे शत्रु के खिलाफ एकजुट नहीं हुए। जब सिंधिया और भोंसले अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तब होल्कर चुपचाप दूर खड़ा था और गायकवाड़ अंग्रेजों की मदद कर रहा था। फिर जब होल्कर ने तलवार उठाई तो भोंसले और सिंधिया ने अपना बदला चुकाया। दक्षिण में आर्थर वेलेजली की कमान में ब्रिटिश सेना ने असाय में सितंबर 1803 में और फिर अरगाँव में नवंबर में सिंधिया और भोंसले की मिली-जुली सेना को हराया। उत्तर में लार्ड लेक ने नवंबर की पहली तारीख को लसवाड़ी में सिंधिया की सेना को तहस-नहस कर दिया और अलीगढ, दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। भारत का अंधा सम्राट एक बार फिर कंपनी का पेंशनखोर हो गया। मित्र मराठा राज्यों को शांति की बातचीत चलानी पड़ी। अब वे दोनों कंपनी के अधीनस्थ सहयोगी बन गए। उन्होंने अंग्रेजों को अपने राज्यों के कुछ भाग दिए, अपने दरबारों में अंग्रेज रेजिडेंट रखे और अंग्रजों की सहमति के बिना यूरोपीयों को सेवा में न रखने का वचन दिया। अब उड़ीसा के समुद्र तट पर और गंगा-यमुना के दोआबा पर अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार हो गया। पेशवा उनके हाथों की कठपुतली बनकर रह गया। वेलेजली ने अब अपना ध्यान होल्कर पर केंद्रित किया। पर यशवंतराज होल्कर अंग्रेजों के लिए काफी भारी साबित हुआ और अंत तक ब्रिटिश सेना से लड़ता रहा। होल्कर के सहयोगी भरतपुर के राजा लेक को, जब उसने राजा के किले को तोड़ने की असफल कोशिश की, भारी नुकसान पहुँचाया। इसके अलावा होल्कर परिवार के साथ अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर सिंधिया उससे हाथ मिलाने की बात सोचने लगा। दूसरी ओर, ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डरों को पता चला कि युद्ध के जरिए प्रसार की नीति बहुत मँहगी पड़ रही थी और उनका मुनाफा इससे कम हो रहा था। कंपनी का कर्ज जों 1797 में 170 लाख पौंड था 1860 तक बढ़कर 310 लाख पौंड हो चुका था। इसके अलावा ब्रिटेन के वित्तीय साधन ऐसे समय में खत्म हो रहे थे जब नेपोलियन यूरोप में एक बार फिर एक बड़ा खतरा बन रहा था। ब्रिटिश राजनेताओं और कंपनी के डायरेक्टरों को लगा कि अब आगे प्रसार रोक देने, बर्बाद कर देने वाले खर्च बंद कर देने और भारत में ब्रिटेन को जो कुछ हाल में उपलब्ध हुआ था उसे ही सुरक्षित करने और मजबूत बनाने का समय आ चुका है। इसलिए वेलेजली को भारत से वापस बुला लिया गया और कंपनी ने 1806 में राजघाट की संधि के द्वारा होल्कर के साथ शांति स्थापित कर ली और उसे उसके राज्य का एक बड़ा भाग लौटा दिया। वेलेजली की प्रसार की नीति सफलता के निकट पहुँची ही थी कि रोक दी गई थी। फिर भी इसका नतीजा यह हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी थी। कंपनी की न्यायिक सेवा के एक युवक अधिकारी हेनरी रोबरक्ला ने 1805 में लिखा - भारत में मौजूद हर अंग्रेज गर्व से भरा हुआ अकड़ा हुआ है। वह अपने को एक विजित जनता का विजेता मानता है और अपने नीचे के हर व्यक्ति को कुछ श्रेष्ठता की भावना के साथ देखता है। लार्ड हेस्टिंग्ज के काल में प्रसारद्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध ने मराठा सरदारों की शक्ति को तोड़ दिया था, पर उनके साहस को नहीं तोड़ सका था उन्होंने 1817 में अपनी खोई स्वाधीनता और प्रतिष्ठा को फिर से पाने का एक और हताशपूर्ण प्रयत्न किया। मराठा सरदारों का एक संयुक्त मोर्चा बनाने में पहल पेशवा ने की जो ब्रिटिश रेजिडेंट के कड़े नियंत्रण में छटपटा रहा था। पेशवा ने नवंबर 1817 में पूना में अंग्रेज रेजिडेंट पर हमला किया। अप्पा साहब ने नागपुर स्थित रेजीडेंसी पर हमला किया और माधवराज होल्कर युद्ध की तैयारी करने लगा।गवर्नर-जनरल लार्ड हेस्टिंग्ज 1813-22 ने पूरी ताकत के साथ जवाबी हमला किया। उसने सिंधिया को ब्रिटिश अधीनता स्वीकार करने को मजबूर किया और पेशवा, भोंसले और होल्कर की सेनाओं को हराया। पेशवा को गद्दी से उतारकर और पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर में बिठा दिया गया। उसका राज्य हड़पकर बंबई की विस्तारित प्रेसीडेंसी बनाई गई। होल्कर और भोंसले ने सहायक सेना रखना स्वीकार कर लिया। मराठों के गर्व को संतुष्ट करने के लिए पेशवा की जमीन पर सतारा का छोटा-सा राज्य बनाया गया और उसे छत्रपति शिवाजी के एक वंशज को दे दिया गया जो पूरी तरह अंग्रेजों पर निर्भर होकर सतारा शासन चलाता रहा। दूसरे भारतीय राज्यों के शासकों की तरह अब मराठा सरदार भी ब्रिटिश सत्ता की दया पर आश्रित हो गए। राजपूताना के राज्य कई दशकों से सिंधिया और होल्कर के प्रभुत्व में थे। मराठों के पतन के बाद वे लोग भी अपनी स्वाधीनता का फिर से दावा करने में असमर्थ थे और उन्होंने तत्काल ही अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। इस तरह 1818 तक पंजाब और सिंध को छोड़कर पूरा भारतीय उपमहाद्वीप अंग्रेजों के नियंत्रण में आ चुका था। इस पूरे क्षेत्र के एक भाग पर सीधे अंग्रेजों का शासन था और बाकी भाग पर अनेक भारतीय शासक राज्य कर रहे थे जिन पर अंग्रेजों का पूरा-पूरा जोर चलता था। इन राज्यों के पास अपनी सेनाएँ नहीं के बराबर थीं और उनके कोई स्वतंत्र विदेशी संबंध नहीं थे। उनके राज्यों में उन्हीं पर नियंत्रण रखने के लिए जो ब्रिटिश सेना तैनात थी उसके भारी खर्च उनको उठाने पड़ते थे। वे अपने अंदरुनी मामलों में स्वायत्त तो थे, मगर इस सिलसिले में भी रेजिडेंट के रूप में अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार.........करते थे। वे लगातार आजमाइश की हालत में बने रहे। ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ बनाने का कामपूरे भारत को जीतने का काम अंग्रेजों ने 1818 से 1857 तक के काल में किया। सिंध और पंजाब भी जीत लिए गए तथा अवध, मध्य प्रांत और बहुत सारे छोटे-छोटे राज्यों का अधिग्रहण कर लिया गया।सिंध की विजययूरोप और एशिया में अंग्रेजों और रूसियों की शत्रुता बढ़ रही थी और अंग्रेजों को भय था कि अफगानिस्तान या फारस के रास्ते रूसी भारत पर हमला कर सकते हैं। सिंध की विजय इसी का परिणाम थी। रूस को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अफगानिस्तान और फारस में अपना प्रभाव बढ़ाने का फैसला किया। उसने यह भी महसूस किया कि यह नीति तभी सफल हो सकेगी जब सिंध को ब्रिटिश नियंत्रण में लाया जाए। सिंध नदी के व्यापारिक उपयोग की संभावनाएँ भी इस लालच का एक कारण थीं।1832 की एक संधि के द्वारा सिंध की सड़कों और नदियों को ब्रिटिश व्यापार के लिए खोल दिया गया था। सिंध के अमीर कहलाने वाले सरदारों से 1839 में एक सहायक संधि पर हस्ताक्षर कराए गए। अंत में पहले के इन वादों को भुलाकर कि उनके राज्य पर कोई आँच नहीं आएगी, सर चार्ल्स नैपियर ने 1843 मे एक संक्षिप्त अभियान के बाद सिंध का अधिग्रहण कर लिया। इससे पहले नेपियर ने अपनी डायरी में लिखा था कि “हमें सिंध पर कब्जा करने का कोई हक नहीं हैं, फिर भी हम ऐसा करेंगे और यह बदमाशी का एक बहुत ही लाभदायक, उपयोगी और मानवीय उदाहरण होगा।” यह काम करने के बदले उसे पुरूस्कारस्वरूप सात लाख रुपए मिले। पंजाब की विजयजून 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता फैल गई, और वहाँ ताबड़तोड़ सरकारें आईं और गईं। स्वार्थी और भ्रष्ट नेताओं का बोलबाला हो गया। अंत में सत्ता बहादुर और देशभक्त मगर एकदम अनुशासनहीन सेना के हाथों में आई। इसके बाद अंग्रेज सतलज पार पाँच पानियों के देश को लालच भरी निगाहों से देखने लगे, हालाँकि उन्होंने 1809 में रणजीतसिंह के साथ स्थायी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए थे।अंग्रेजों के युद्धोन्मादी कार्यों और पंजाब के भ्रष्ट सरदारों के साथ उनकी साजिशों के कारण पंजाब की सेना भड़क उठी। 1845 के बसंत में यह समाचार पंजाब पहुँचा कि पुल बनाने के काम में आने वाली नावें बंबई से सतलज किनारे स्थित फिरोजपुर के लिए भेजी गई हैं। आगे के इलाकों में बैरकें बनाई गई हैं और उनमें अतिरिक्त सेना रखी गई है और पंजाब से लगने वाली सीमा के लिए अतिरिक्त रेजीमेन्टे भेजी जा रही हैं। पंजाब की सेना को विश्वास हो गया कि अंग्रेज पंजाब पर कब्जा करने पर आमादा थे, और फिर पंजाब की सेना ने जवाबी कारवाईयाँ की। जब दिसंबर में सेना ने सुना कि प्रधान सेनापति लार्ड गफ और गवर्नर-जनरल लार्ड हार्डिग्ज फिरोजपुर की ओर बढ़ रहे हैं तब उसने भी हमला करने का फैसला किया। इस तरह 13 दिसंबर 1845 को दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। इस विदेशी खतरे के आगे हिंदू, मुसलमान और सिख फौरन एक हो गए। पंजाब की सेना बहुत बहादुरी और उदाहरणीय साहस के साथ लड़ी। लेकिन उसके कुछ नेता पहले ही गद्दार बन चुके थे। प्रधानमंत्री राजा लालसिंह और प्रधान सेनापति मिस्सर तेजसिंह का शत्रु के साथ गुप्त पत्रव्यवहार जारी था। पंजाब की सेना हार स्वीकार करने और 8 मार्च 1846 को लाहौर में एक अपमानजनक समझौते पर हस्ताक्षर करने को बाध्य हो गई। अंग्रेजों ने जलंधर के दौआब को हड़प लिया और पचास लाख रूपए नगद लेकर जम्मू और कश्मीर को राजा गुलाबसिंह डोंगरा के हवाले कर दिया। पंजाब की सेना को घटाकर 20,000 पैदल और 12,000 घुडसवार सेना तक सीमित कर दिया गया और एक भारी ब्रिटिश सेना लाहौर में तैनात कर दी गई। बाद में 16 दिसंबर 1846 को एक और समझौता हुआ जिसके अनुसार राज्य के एक-एक विभाग के सारे मामलों में लाहौर स्थित अंग्रेज रेजिडेंट को पूरा अधिकार दे दिया गया। इसके अलावा राज्य के किसी भी भाग में सेना तैनात करने की छूट अंग्रेजों को मिल गई। अब अंग्रेज रेजिडेंट ही पंजाब का वास्तविक शासक बन बैठा और पंजाब अपनी स्वाधीनता खोकर एक अधीन राज्य बन गया। लेकिन भारत में खुलकर साम्राज्यवादी आक्रमणों का समर्थन करने वाला ब्रिटिश अधिकारियों का भाग अभी भी असंतुष्ट था और वह पंजाब पर सीधे-सीधे ब्रिटिश शासन लादना चाहता था। इसका अवसर उसे 1848 में मिला जब स्वतंत्रता-प्रेमी पंजाबियों ने अनेकों स्थानीय विद्रोह छेड़ दिए। इनमें से दो प्रमुख विद्रोहों के नेता मुल्तान के मूलराज और लाहौर के पास के छतरसिंह अटारीवाला थे। एक बार फिर पंजाबियों की निर्णायक हार हुई। इस अवसर का फायदा उठाकर लार्ड डलहौजी ने पंजाब को हड़प लिया। इस तरह भारत का अंतिम स्वाधीन राज्य भी भारत के ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी की अधिग्रहण की नीति (1848-56)लार्ड डलहौजी 1848 मे गर्वनर-जनरल बनकर भारत आया। वह शुरू से ही इस बात पर आमादा था कि जितने बड़े इलाके पर संभव हो, प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन स्थापित किया जाए। उसने घोषणा की थी कि “भारत के सभी देशी राज्यों का खात्मा अब कुछ ही समय की बात है।” उसकी नीति का उद्देश्य भारत को ब्रिटेन का निर्यात बढ़ाना था। दूसरे साम्राज्यवादी आक्रमणकारियों की तरह डलहौजी को भी विश्वास था कि भारत के देशी राज्यों के लिए ब्रिटेन का निर्यात इसलिए घट रहा था कि इन राज्यों के भारतीय शासक उनका शासन ठीक से नहीं चला रहे हैं। इसके अलावा वह समझता था कि “भारतीय सहयोगी” भारत में ब्रिटिश विजय में जितने सहायक हो सकते थे उतने हो चुके हैं और अब उसने छुटकारा पाने में ही लाभ है।लार्ड डलहौजी ने अपनी अधिग्रहण की नीति के लिए जिस साधन का सहारा लिया, वह था राज्य विलय का सिद्धान्त (डाक्ट्रिन आफ लैप्स)। इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी सुरक्षाप्राप्त राज्य का शासक बिना एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी के मर जाए तो उसका राज्य उसके दत्तक उत्तराधिकारी को नहीं सौंपा जाएगा जैसी कि सदियों से इस देश में परंपरा चलती आ रही थी। इसके बजाए, अगर उत्तराधिकारी गोद लेने के काम को पहले से अंग्रेज अधिकारियों की सहमति प्राप्त न होगी तो वह राज्य ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाएगा। 1848 में सतारा और 1854 में नागपुर और झाँसी समेत अनेक राज्यों का इसी सिद्धान्त के अनुसार अधिग्रहण कर लिया गया था। डलहौजी ने अनेक भूतपूर्व शासकों के अधिकारों को मान्यता देने और उन्हें पेंशन देने से भी इनकार कर दिया। इस तरह कर्नाटक और सूरत के नवाबों और तंजौर के राजा की उपाधियाँ छीन ली गईं। इसी तरह भूतपूर्व पेशवा बाजीराव द्वितीय, जिसे बिठूर का राजा बना दिया गया था, जब मरा तो डलहौजी ने उसका वेतन या पेंशन उसके दत्तक पुत्र नाना साहब को देने से इनकार कर दिया। लार्ड डलहौजी की निगाहें अवध के साम्राज्य को हड़पने पर लगी थीं। पर इस काम में कुछ बाधाएँ थीं। पहली यह कि बक्सर की लड़ाई के बाद से ही अवध के नवाब अंग्रेजों के सहयोगी रहे थे। इसके अलावा इन तमाम वर्षों में वे अंग्रेजों के सबसे अधिक आज्ञाकारी भी रहे थे। अवध के नवाब के कई उत्तराधिकारी थे और इसलिए उस पर राज्य विलय का सिद्धान्त भी लागू नहीं किया जा सकता था। अवध के नवाब को राज्य से वंचित करने के लिए किसी और बहाने की जरूरत थीं। अंत में, लार्ड डलहौजी ने अवध की जनता की दशा सुधारने के विचार का सहारा लिया। नवाब वाजिद अली शाह पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने अपना शासन ठीक से नहीं चलाया है और सुधार लागू करने से इनकार कर दिया है इसके बाद उनके राज्य को 1856 में हड़प लिया गया। निःसंदेह अवध के शासन का पतन वहाँ की जनता के लिए कष्ट का कारण था। अवध के नवाब भी अपने समय के दूसरे शासकों की तरह स्वार्थी और अय्याशियों में डूबे हुए थे और प्रशासन ठीक से चलाने या जनता की भलाई करने की चिंता करते थे। पर इस हालात के लिए अंततः अंग्रेज भी जिम्मेदार थे जो 1801 से ही अवध पर नियंत्रण किए हुए थे और परोक्ष रूप से वहाँ राज्य कर रहे थे। वास्तव में डलहौजी का लालच इस कारण से था कि अवध अपनी बेपनाह दौलत के साथ मैनचेस्टर में तैयार मालों के लिए एक अच्छा बाजार बन सकता था, यही चीज थी जो उसकी तथाकथित ‘मानवतावादी’ भावनाओं के पीछे काम कर रही थी। और ऐसे ही कारणों से कच्चे कपास की ब्रिटेन की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए डलहौजी ने 1853 में निजाम के बरार का कपास-उत्पादक प्रांत ले लिया था। यह बात हमें स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि देशी राज्यों के बने रहने या हड़पे जाने का उस समय कोई अधिक महत्व नहीं रह गया था। वास्तव में तब कोई भारतीय राज्य था भी नहीं। सुरक्षाप्राप्त देशी राज्य भी उसी तरह ब्रिटिश साम्राज्य के भाग थे जिस तरह कंपनी के प्रत्यक्ष शासन वाले इलाके। अगर कुछ राज्यों पर ब्रिटिश नियंत्रण का स्वरूप बदला गया तो केवल अंग्रेजों की सुविधा के लिए। वहाँ की जनता के हित का इस परिवर्तन से कोई संबंध न था। | |||||||||
| |||||||||