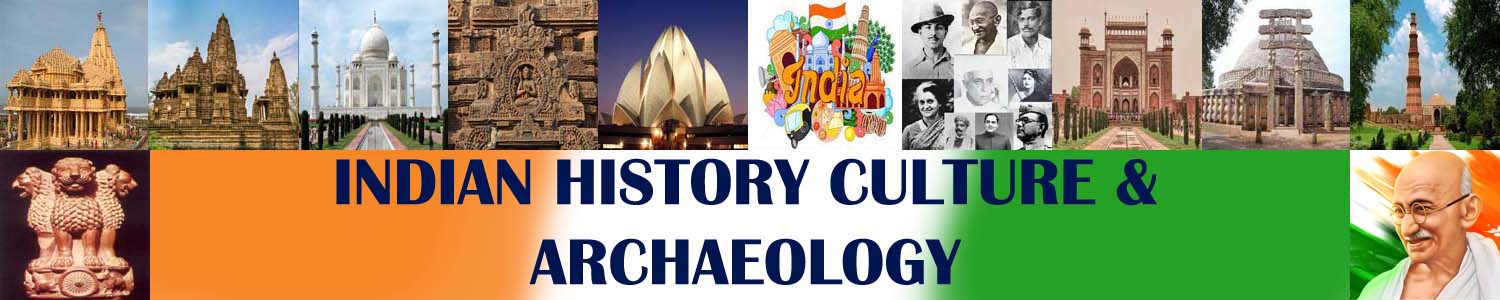| |||||||||
|
1858 ई. के बाद भारत में प्रशासनिक व्यवस्था
1857 के विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश प्रशासन को गहरा धक्का दिया और उसका पुनर्गठन अनिवार्य बना दिया। विद्रोह के बाद के दशकों में भारत सरकार के ढाँचे और नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था और सरकार में परिवर्तन के लिए भारत में उपनिवेशवाद के एक नए चरण का आरंभ अधिक महत्वपूर्ण था।
19वीं सदी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति का प्रसार और विकास हुआ। धीरे-धीरे यूरोप के दूसरे देश अमरीका और जापान का भी औद्योगीकरण हुआ और विश्व की अर्थव्यवस्था में ब्रिटेन की उत्पादन संबंधी और वित्तीय श्रेष्ठता समाप्त हो गई। अब बाजारों, कच्चे माल के स्त्रोतों और विदेशी पूँजी-निवेश के अवसरों के लिए दुनिया भर में तेज प्रतियोगिता आरंभ हो गई। उपनिवेशों और अर्ध-उपनिवेशों के लिए प्रतियोगिता और कड़ी और तीखी हो गई, क्योंकि नई औपनिवेशिक विजयों के लिए क्षेत्र कम होते गए। ब्रिटेन को अब विश्व पूँजीवाद में अपनी प्रमुख स्थिति बनाए रखने के लिए नए-नए विकसित हो रहे देशों की चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए उसने अपने वर्तमान साम्राज्य पर अपने नियंत्रण को मजबूत बनाने और उसे और फैलाने के लिए जोरदार कोशिशें आरंभ कर दीं। इसके अलावा 1850 के बाद रेलवे में और भारत सरकार को दिए गए ऋणों के रूप में बहुत अधिक ब्रिटिश पूँजी लगी थी। कुछ पूँजी चाय के बागानों, कोयला खदानों, जूट मिलों, जहाजरानी व्यापार और बैंकिंग में भी लगी थी। इस ब्रिटिश पूँजी को आर्थिक और राजनीतिक खतरों से सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक था कि भारत के ब्रिटिश शासन को और ठोस बनाया जाए। परिणामस्वरूप साम्राज्यवादी नियंत्रण को और भी सख्त बनाया गया और साम्राज्यवादी विचारधारा भी और मजबूती से स्थापित हुई इसको लिटन, डफरिन, लांसडाउन, एल्गिन और सबसे बढ़कर कर्जन के वायसराय-काल की प्रतिक्रियावादी नीतियों में भी देखा जा सकता था। प्रशासन1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक कानून ने शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सम्राट को दे दिया। इसके पहले भारत पर सत्ता कंपनी के डायरेक्टरों और बोर्ड आफ कंट्रोल की थी, पर अब शासन का भार एक ब्रिटिश सरकार के मन्त्री जिसे भारत मन्त्री अथवा सेक्रेटरी आफ स्टेट कहा जाता था को दे दिया और उसकी सहायता के लिए एक कौंसिल नियुक्त कर दी गई। यह भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य और इस प्रकार संसद के प्रति उत्तरदायी होता था इस तरह भारत पर सत्ता अंततः संसद के ही हाथों में थी।इस कानून के अनुसार भारत का शासन पहले की ही तरह एक गवर्नर-जनरल को चलाना था, हालाँकि अब उसे वायसराय अर्थात् सम्राट के व्यक्तिगत प्रतिनिधि की पदवी दे दी गई। समय के साथ-साथ नीतियों और उनको लागू करने के मामले में वायसराय अधिकाधिक ब्रिटिश सरकार के अधीन होता गया। प्रशासन के तमाम छोटे-छोटे मामलों पर भी भारत सचिव का नियंत्रण होता था। इस तरह भारत के मामलों पर अंतिम और व्यापक नियंत्रण जिस अधिकारी का था, वह भारत से हजारों मील दूर लंदन में बैठा होता था। इस स्थिति में सरकार की नीतियों पर भारतीय जनमत का प्रभाव पहले से भी कम हो गया। दूसरी ओर ब्रिटिश उद्योगपतियों, व्यापारियों और बैंकरों का भारत सरकार पर प्रभाव और भी बढ़ गया। इस तरह भारतीय प्रशासन 1858 के पहले की तुलना में और भी प्रतिक्रियावादी हो गया क्योंकि अब उदारतावाद का दिखावा भी धीरे-धीरे बंद कर दिया गया। भारत के लिए 1858 के कानून में व्यवस्था थी कि गवर्नर-जनरल के साथ एक एक्जिक्यूटिव कौंसिल (कार्यकारी परिषद) होगी, जिसके सदस्य विभिन्न विभागों के प्रमुख और गवर्नर-जनरल के अधिकारिक सलाहकार होंगे। यही कौंसिल सारे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करके बहुमत से निर्णय लेती थी, हालाँकि गवर्नर-जनरल कौंसिल के किसी भी महत्वपूर्ण फैसले को रद्द कर सकता था। 1861 के इंडियन कौंसिल्स एक्ट में गवर्नर-जनरल की कौंसिल को कानून बनाने की गरज से और भी बड़ा बना दिया गया और इसलिए उसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल नाम दिया गया। गवर्नर-जनरल को एक्जीक्यूटिव कौंसिल में 6 से 12 सदस्य तक बढ़ाने का अधिकार था, जिनमें से कम से कम आधे का गैर-अधिकारी होना अनिवार्य था। ये भारतीय भी हो सकते थे और अंग्रेज भी। इंपीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल को कोई वास्तविक अधिकार प्राप्त नहीं थे, इसलिए उसे आरंभिक कोटि का या कमजोर संसद भी नहीं माना जा सकता। यह मात्र एक सलाहकार समिति थी जो सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार नहीं कर सकती थी और वित्तीय प्रश्नों पर तो हर्गिज नहीं कर सकती थी। बजट पर तो इसका कतई नियंत्रण नहीं था। यह प्रशासन के कामों पर विचार नहीं कर सकती थी और सदस्य उनके बारे में कोई सवाल नहीं कर सकते थे। दूसरे शब्दों में लेजिस्लेटिव कौंसिल का एक्जिक्यूटिव पर कोई नियंत्रण न था। इसके अलावा इसके द्वारा पारित कोई भी विधेयक गवर्नर-जनरल के अनुमोदन के बिना कानून नहीं बन सकता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि भारत सचिव इसके द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को रद्द कर सकता था इस तरह लेजिस्लेटिव कौंसिल का एकमात्र महत्वपूर्ण काम यह था कि वह सरकारी कदमों पर हाँ करे और यह आभास कराए कि ये सभी कदम एक संसदीय संस्था द्वारा बनाए गए कानून हैं। सिद्धान्ततः भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने के लिए कुछ गैर-अधिकारी भारतीय सदस्य भी कौंसिल में शामिल कर लिए गए थे। लेकिन लेजिस्लेटिव कौंसिल में भारतीय सदस्यों की संख्या बहुत कम थी और वे भारतीय जनता द्वारा चुने हुए न होकर गवर्नर-जनरल द्वारा नामजद किए जाते थे फिर गवर्नर-जनरल भी हमेशा ही इसके लिए राजा-महाराजाओं और उनके मंत्रियों, बड़े जमींदारों, बड़े व्यापारियों या सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों का ही चयन करता था वे भारतीय जनता या विकसित हो रही राष्ट्रवादी भावना का कोई प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। भारत की सरकार अभी भी 1858 के पहले की तरह विदेशी और निरंकुश सरकार बनी रही। फिर यह सब आकस्मिक भी न था बल्कि सोची-समझी नीति का अंग था। 1861 में संसद में इंडियन कौंसिल बिल पेश करते हुए भारत सचिव चार्ल्स वुड ने कहा था - “सारे अनुभव हमें यही बतलाते हैं कि जब एक विजेता जाति दूसरी जाति पर शासन करती है तो एक निरंकुश सरकार ही शासन का सबसे नरम रूप हो सकती है।” प्रांतीय प्रशासनशासन की सुविधा के लिए अंग्रेजों ने भारत को प्रांतों में बाँट रखा था। इनमें से बंगाल, मद्रास और बंबई प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था। इन प्रेसिडेंसियों का प्रशासन एक गवर्नर तीन सदस्यों वाली एक कौंसिल की सहायता से चलाता था और उनकी नियुक्ति सम्राट करता था। प्रेसिडेंसियों की सरकारों को दूसरी प्रांतीय सरकारों से अधिक अधिकार और शक्तियाँ प्राप्त थीं। इन दूसरे प्रांतों का शासन गवर्नर-जनरल द्वारा नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ कमिश्नर चलाते थे।1833 के पहले प्रांतीय सरकारों को बहुत स्वायत्तता प्राप्त थी। पर 1833 में उनसे कानून बनाने के अधिकार ले लिए गए थे और उनके व्यय पर सख्त केंद्रीय नियंत्रण लगा दिया गया था। पर अनुभवों से जल्द ही पता चल गया कि भारत जैसे विशाल देश का शासन सख्त केंद्रीकरण के सिद्धान्त पर कुशलतापूर्वक नहीं चलाया जा सकता। अति-केंद्रीकरण की यह बुराई वित्त के मामलों में सबसे अधिक स्पष्ट थी। पूरे देश से और अनेक स्त्रोतों से राजस्व जमा होकर केंद्र में पहुँचता था और तब केंद्र उसे प्रांतीय सरकारों में बाँटता था। प्रांतों के व्यय की छोटी-छोटी बातों पर भी केन्द्र सरकार का सख्त नियंत्रण होता था। लेकिन यह प्रणाली व्यवहार में बहुत बर्बादी का कारण सिद्ध हुई। प्रांतीय सरकारों द्वारा राजस्व के कुशलतापूर्वक संग्रह पर निगरानी रखना या उनके खर्च पर पर्याप्त नियंत्रण रखना केंद्रीय सरकार के लिए संभव न था। इसलिए अधिकारियों ने सार्वजनिक वित्त का विकेंद्रीकरण करने का फैसला किया। प्रांतीय वित्त को केंद्रीय वित्त से अलग करने की दिशा में पहला कदम 1870 में लार्ड मेयो ने उठाया। पुलिस, जेल, शिक्षा, चिकित्सा सेवाओं और सड़कों जैसी कुछ सेवाओं के प्रशासन के लिए प्रांतीय सरकारों को निर्धारित रकम दे दी जाती थी और उनको इस धन का अपनी इच्छानुसार उपयोग करने को कहा जाता था। 1877 में लार्ड मेयो की इस योजना को लार्ड लिटन ने और फैलाया। उसने प्रांतीय सरकारों को भू-राजस्व, उत्पादन शुल्क, सामान्य प्रशासन और कानून तथा न्याय-व्यवस्था जैसी कुछ और सेवाएँ भी सौंप दीं। इस अतिरिक्त व्यय का भार उठाने के लिए प्रांतीय सरकार को उस प्रांत विशेष से स्टैंप, उत्पादन कर तथा आय कर जैसे कुछ स्त्रोतों से प्राप्त आय का एक निश्चित भाग दिया जाने लगा। इस व्यवस्था में 1882 में और भी परिवर्तन किए गए। प्रांतों को निर्धारित धन देने की प्रणाली समाप्त कर दी गई और उसके बजाए यह किया गया कि किसी प्रांत को कुछ स्त्रोतों से प्राप्त आय का एक निश्चित भाग दिया जाएगा। इस तरह राजस्व के सारे स्रोतों से प्राप्त आय का एक निश्चित भाग दिया जाएगा। इस तरह राजस्व के सारे स्रोतों को तीन भागों में बाँट दिया गया सामान्य, प्रांतीय, तथा वे जिनसे प्राप्त आय केंद्र और प्रांतों के बीच बँटनी थी। वित्तीय विकेंद्रीकरण के ऊपर वर्णित विभिन्न कदमों का अर्थ यह नहीं था कि एक वास्तविक प्रांतीय स्वायत्तता का आरंभ हो गया था या प्रांतीय प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी होने लगी थी। इसके बजाए उनकी प्रकृति प्रशासकीय पुनर्गठन की थी जिसका उद्देश्य व्यय कम कराना और आय को बढ़ाना था। सिद्धान्त और व्यवहार दोनों में केन्द्र सरकार का वर्चस्व बना रहा और केंद्र का प्रांतीय सरकारों पर प्रभावी और व्यापक नियंत्रण जारी रहा। यह अपरिहार्य था क्योंकि केंद्रीय और प्रांतीय, दोनों ही सरकारें पूरी तरह भारत सचिव और ब्रिटिश सरकार के अधीन थीं। स्थानीय संस्थाएँवित्तीय कठिनाइयों के कारण सरकार ने प्रशासन का और भी विकेंद्रीकरण किया और नगरपालिकाओं तथा जिला परिषदों के द्वारा स्थानीय शासन को प्रोत्साहित किया। औधोगिक क्रांति ने 19वीं सदी में यूरोपीय अर्थव्यवस्था और समाज को धीरे-धीरे बदलकर रख दिया था। यूरोप के साथ भारत के बढ़ते संपर्कों तथा साम्राज्यवाद और आर्थिक शोषण की नई विधियों के कारण आवश्यक हो गया था कि अर्थव्यवस्था, सफाई-व्यवस्था और शिक्षा के क्षेत्र में यूरोप में हुई प्रगति को भारत में भी लागू किया जाए। इसके अलावा उभरता हुआ भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन भी नागरिक जीवन में आधुनिक सुधारों को लागू किए जाने की माँग कर रहा था। इस तरह जनता के लिए शिक्षा, सफाई व्यवस्था, जल की आपूर्ति, बेहतर सड़कों तथा अन्य नागरिक सुविधाओं की जरूरत अधिकाधिक महसूस की जा रही थी। सरकार अब इनको और अनदेखा नहीं कर सकती थी। लेकिन सेना और रेलवे पर हो रहे भारी खर्चो के कारण वित्त-व्यवस्था पहले ही डाँवाडोल हो रही थी। चूँकि गरीब जनता पर करों का बोझ पहले ही बहुत अधिक था और इसमें और बढ़ोत्तरी करने से सरकार के खिलाफ जन असंतोष बढ़ने का डर था, इसलिए सरकार नए कर लगाकर आय भी नहीं बढ़ा सकती थी। दूसरी तरफ सरकार ऊँचे वर्गों, खासकर ब्रिटिश नागरिक अधिकारियों, बागानों के मालिकों और व्यापारियों पर कर लगाना नहीं चाहती थी, पर अधिकारियों को लग रहा था कि अगर जनता को यह लगे कि उन पर लगे नए करों से प्राप्त आमदनी का इस्तेमाल उसी के कल्याण के लिए होना है, तो वह कर देने में नहीं हिचकिचाएगी। इसलिए निर्णय किया गया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई और जल-आपूर्ति जैसे विषय स्थानीय सस्थाओं को दे दिए जाएँ और वे स्थानीय कर लगाकर उनका खर्च निकालें। अनेक अंग्रेजों ने एक और आधार पर भी स्थानीय संस्थाओं की स्थापना के लिए जोर डाला। उनका मत था कि किसी न किसी रूप में प्रशासन से भारतीयों को जोड़ने से वे राजनीतिक रूप से असंतुष्ट नहीं होगें। भारत में सत्ता पर अंग्रेजों के एकाधिकार को खतरे में डाले बिना भारतीयों को केवल स्थानीय संस्थाओं के स्तर पर ही जोड़ा जा सकता था।सबसे पहले 1864 और 1868 के बीच स्थानीय संस्थाओं की स्थापना हुई। पर लगभग हर मामले में इनके सदस्य नामजद होते थे और इनका अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट होता था। इसलिए ये संस्थाएँ किसी भी तरह स्थानीय स्वशासन नहीं कही जा सकती थीं और प्रबुद्ध भारतीयों ने भी उन्हें ऐसा नहीं माना। वे इन्हें जनता से नए कर उगाहने का साधन मात्र समझते थे। इस दिशा में बहुत हिचकते हुए एक अपर्याप्त कदम 1882 में लार्ड रिपन की सरकार ने उठाया। एक सरकारी प्रवास में ग्रामीण और नगरीय स्थानीय संस्थाओं द्वारा, जिनके अधिकांश सदस्य गैर-अधिकारी हों, स्थानीय मामलों के प्रबंध की एक नीति निर्धारित की गई। जहाँ भी अधिकारियों कों चुनाव-प्रणाली लागू करना संभव लगे वहाँ इन गैर-अधिकारी सदस्यों को जनता द्वारा चुने जाना था। इस प्रस्ताव में किसी स्थानीय संस्था के अध्यक्ष के रूप में किसी गैर-अधिकारी के चुनाव की छूट भी दी गई। लेकिन सभी जिला परिषदों और अनेक नगरपालिकाओं में चुने हुए सदस्य अल्प मत में होते थे। इसके अलावा वे बहुत थोड़ें से मतदाताओं द्वारा चुने जाते थे, क्योंकि मत देने का अधिकार बहुत ही सीमित था। जिलों के अधिकारी ही जिला परिषदों के अध्यक्ष बने रहे, हालाँकि धीरे-धीरे गैर-अधिकारी नगरपालिका समीतियों के अध्यक्ष बनने लगे। सरकार ने स्थानीय संस्थाओं की गतिवधियों पर कड़ा नियंत्रण लगाने और उनको अपने विवेक के अनुसार निलंबित या भंग करने का अधिकार अपने हाथ में रखा। नतीजा यह हुआ कि कलकत्ता, मद्रास और बंबई के प्रेसिडेंसी नगरों को छोड़कर हर जगह स्थानीय संस्थाएँ सरकारी विभाग बनकर रह गई और स्थानीय स्वशासन के अच्छे उदाहरण न बन सकीं। तो भी राजनीतिक रूप से जागरूक भारतीयों ने रिपन के प्रस्ताव का स्वागत किया और इन स्थानीय संस्थाओं में सक्रिय रूप से इस आशा के साथ भाग लिया कि समय आने पर उनको स्थानीय स्वशासन के कारगर साधन के रूप में परिवर्तित किया जा सकेगा। सेना में परिवर्तन1858 के बाद सेना का सावधानी के साथ पुनर्गठन किया गया जिसका प्रमुख उद्देश्य एक और विद्रोह न होने देना था। शासकों ने देखा कि उनकी संगीनें ही उनके शासन का एकमात्र सुरक्षित आधार थीं। भारतीय सैनिकों की विद्रोह की क्षमता को अगर एकदम समाप्त न किया जा सके तो उसे यथासंभव कम करने के लिए अनेक कदम उठाए गए। पहली बात यह कि सेना पर यूरोपीय सैनिकों का वर्चस्व सावधानी के साथ सुनिश्चित किया गया। सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपीयों का भाग बढ़ा दिया गया। बंगाल की सेना में अब यह अनुपात एक और दो का तथा मद्रास और बंबई की सेनाओं में दो और पाँच का था। इसके लिए भौगोलिक और सैनिक महत्व के स्थानों पर यूरोपीय सेनाओं को तैनात किया गया। तोपखाने (और बाद में बीसवीं सदी में टैंकों तथा बख्तर-बंद गाड़ियों) जैसे सेना के महत्वपूर्ण विभाग पूरी तरह यूरोपीय के हाथों में रखे गए। अधिकारी वर्ग से भारतीयों को बाहर रखने की पुरानी नीति का सख्ती से पालन किया जाने लगा। 1914 तक कोई भी भारतीय कभी सूबेदार के पद से ऊपर नहीं उठ सका। दूसरे, सेना के भारतीय अंग का संगठन “संतुलन और जवाबी संतुलन” तथा “बांटों और राज करो” की नीति के आधार पर किया गया ताकि किसी ब्रिटिश-विरोधी विद्रोह के लिए एकजुट होने का उनको अवसर न मिल सके। सेना की भर्ती में जाति, क्षेत्र और धर्म के आधार पर भेदभाव किए जाने लगे। यह कहानी गढ़ी गई कि भारतीयों में कुछ “लड़ाकू” जातियाँ और कुछ “गैर-लड़ाकू” जातियाँ हैं। अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सैनिकों ने ही आरंभ में अंग्रेजों की भारत-विजय में सहायता की थी, पर 1857 के विद्रोह में उनके भाग लेने के कारण उनको “गैर-लड़ाकू” घोषित कर दिया गया। अब बड़ी संख्या में सेना में उनको भर्ती करना बंद कर दिया गया। दूसरी ओर, विद्रोह को कुचलने में सहायता देने वाले पंजाबियों, गोरखों और पठानों को “लड़ाकू” जाति घोषित किया गया और उनको बड़ी संख्या में भर्ती किया जाने लगा। 1875 तक ब्रिटिश भारत की सेना का आधा भाग पंजाबियों का था। साथ ही भारतीय रेजीमेन्टों को तमाम जातियों और वर्गों का मिश्रण बना दिया गया कि वे सभी एक-दूसरे को संतुलित करती रहें। सैनिकों की सांप्रदायिक, जातिगत, कबीलाई और क्षेत्रीय निष्ठाओं को प्रोत्साहित किया गया ताकि उनके बीच राष्ट्रवाद की भावना न फैल सके। उदाहरण के लिए, अनेक रेजीमेण्टों में जातियों और संप्रदायों के आधार पर कंपनियाँ बनाई गईं। भारत सचिव चार्ल्स वुड ने 1861 में वायसराय कैनिंग को एक पत्र में लिखा -मैं एक ऐसी बड़ी सेना कभी देखना नहीं चाहता जिसकी भावनाएँ और पूर्वाग्रह और संपर्क वैसे ही हों, जिसे अपनी शक्ति का भरोसा है और जो मिलकर विद्रोह करने को इतनी उत्सुक हो। अगर एक रेजीमेंट विद्रोह करे तो दूसरी रेजीमेंट को उससे इतना कटा हुआ देखना पसंद करुँगा कि वह उस पर गोली चलाने के लिए भी तैयार हो। इस तरह भारतीय सेना शुद्ध रूप से भाड़े की सेना बनी रही। इसके अलावा उसे बाकी जनता के जीवन और विचारों से अलग रखने के सारे प्रयास किए गए। हर संभव उपाय द्वारा उसे राष्ट्रवादी विचारों से दूर रखा गया। समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं और राष्ट्र वादी प्रकाशनों को सैनिकों तक नहीं पहुँचने दिया जाता था। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, ऐसे सभी उपाय अंततः नाकाम रहे और भारतीय सेना के अंगों ने भारत के स्वाधीनता-संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय सेना आगे चलकर बहुत ही खर्चीली सैनिक शक्ति बन गई। 1904 में भारतीय राजस्व का लगभग 52 प्रतिशत इस पर खर्च हो रहा था। इसका कारण यह था कि यह एक से अधिक उद्देश्य पूरे कर रही थी। उस समय सबसे और महत्वपूर्ण उपनिवेश होने के नाते भारत की रूसी, फ्रांसीसी और जर्मन साम्राज्यवादियों से लगातार रक्षा करनी पड़ती थी। इससे भारतीय सेना की संख्या में बहुत वृद्धि हुई। दूसरे, भारतीय सैनिकों को केवल भारत की रक्षा ही नहीं करनी पड़ती थी। भारतीय सेना एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश सत्ता और शासन को फैलाने और मजबूत बनाने का प्रमुख साधन थी। अंतिम बात यह कि सेना का ब्रिटिश भाग कब्जा बनाए रखने वाली सेना का काम कर रहा था। देश पर ब्रिटिश अधिकार की आखिरी जमानत यही था। मगर इसका खर्च भारत के राजस्व से पूरा किया जाता था और यह भारत के लिए बहुत बड़ा बोझ था। सार्वजनिक सेवाएँहम ऊपर देख चुके हैं, कि भारत सरकार पर भारतीयों का नियंत्रण नहीं के बराबर था। कानून बनाने या प्रशासन की नीतियाँ निर्धारित करने में उनकी कोई भूमिका नहीं रखी गई थी। साथ ही उन्हें नौकरशाही से अलग रखा जाता था जो इन नीतियों को लागू करती थी। प्रशासन में अधिकार और उत्तरदायित्व के सारे पदों पर इंडियन सिविल सर्विस के सदस्य बैठे होते थे जिनकी भर्ती लंदन में होने वाली खुली वार्षिक प्रतियोगिता-परीक्षाओं के द्वारा की जाती थी। इन परीक्षाओं में भारतीय भी बैठ सकते थे। 1863 में यह परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ ठाकुर थे जो रवींद्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे। उसके बाद लगभग हर साल एक-दो भारतीय सिविल सर्विस के गौरवपूर्ण पदों पर पहुँचते रहे, मगर अंग्रेजों की अपेक्षा उनकी संख्या बहुत ही नगण्य थी। वास्तव में सिविल सर्विस के दरवाजे भारतीयों के लिए बंद ही रहे क्योंकि वे अनेक बाधाओं से ग्रस्त थे। यह परीक्षा अंग्रेजी के माध्यम से होती थी जो एक विदेशी भाषा थी। यह प्राचीन ग्रीक और लैटिन के ज्ञान पर आधारित थी जिसे इंग्लैण्ड में लंबे और खर्चीले अध्ययन के बाद ही प्राप्त किया जा सकता था। साथ ही सिविल सर्विस परीक्षा में बैठने की आयु जो 1859 में 23 वर्ष थी, 1878 में घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। अगर 23 वर्ष के भारतीय युवक के लिए सिविल सर्विस प्रतियोगिता में सफल होना कठिन था तो 19 वर्ष के भारतीय युवक के लिए यह असंभव ही था।इसी तरह प्रशासन के दूसरे विभागों जैसे पुलिस, सार्वजनिक निर्माण, चिकित्सा, डाक और तार, जंगल, इंजीनियरिंग, कस्टम और बाद में रेलवे में भी बड़े और अधिक वेतन वाले पद ब्रिटिश नागरिकों के लिए सुरक्षित रखे जाते थे। सभी महत्वपूर्ण पदों यूरोपीय का यह वर्चस्व आकस्मिक न था। भारत के शासकों का मत था कि भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था। इस तरह 1893 में भारत सचिव लार्ड किंबरले ने यह व्यवस्था रखी कि “सिविल सर्विस के सदस्यों में यूरोपीयों की हमेशा एक पर्याप्त संख्या का होना अत्यन्त आवश्यक है।” वायसराय लांसडाउन ने इस बात पर जोर दिया कि “अगर इस विशालकाय साम्राज्य को सुरक्षित रखना है तो इसकी सरकार का यूरापीयों के हाथों में होना एक अनिवार्यता है।” भारतीयों के दबाव में 1918 के बाद प्रशासकीय सेवाओं का धीरे-धीरे भारतीकरण किया गया। लेकिन नियंत्रण और अधिकार के पद फिर भी अंग्रेजों के हाथों में बने रहे। इसके अलावा लोगों को जल्द ही पता चल गया कि इन सेवाओं के भारतीकरण से उनके हाथों में राजनीतिक शक्ति तो आई ही नहीं है। इस सेवाओं में शामिल भारतीय ब्रिटिश शासन के एजेंट का काम करते थे और वफादारी के साथ ब्रिटेन के साम्राज्यवादी उद्देश्यों की पूर्ति करते थे। रजवाड़ों के साथ संबंध1857 के विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने भारतीय रजवाड़ों के प्रति नीति बदल दी। 1857 के पहले वे भारतीय राज्यों को हड़पने का कोई भी अवसर नहीं चूकते थे। यह नीति अब छोड़ दी गई। अनेक भारतीय शासक अंग्रेजों के वफादार ही नहीं रहे थे बल्कि विद्रोह को कुचलने में उनकी सक्रिय रूप से सहायता भी की थी। जैसा कि वायसराय कैनिंग ने कहा था, इन शासकों ने “तूफान में तरंगरोधकों” का काम किया था। उनकी वफादारी का इनाम अब इस घोषणा के रूप में दिया गया कि उनके उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार को मान्यता दी जाएगी तथा भविष्य में उनके राज्यों का कभी भी अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। इसके अलावा विद्रोह ने अनुभव के ब्रिटिश अधिकारियों को विश्वास करा दिया था कि जनता के विरोध या विद्रोह की स्थिति में ये रजवाड़े उनके कारगर सहयोगी हो सकते हैं। 1860 में कैनिंग ने लिखा था -बहुत पहले सर जान मालकोम ने यह बात कही थी कि अगर हम पूरे भारत को जिलों मे बांट दें तो भी वास्तविकता ऐसी नहीं है कि हमारा साम्राज्य पचास वर्षों तक भी जारी रह सके। पर अगर हम बिना किसी राजनीतिक सत्ता दिए, मात्र शाही उपकरणों के रूप में अनेक देशी रजवाड़ों को बनाए रखें तो भारत में हम तब तक बने रहेंगे जब तक कि समुद्र पर हमारा वर्चस्व बना रहेगा। इस मत की ठोस सच्चाई में मुझे कोई संदेह नहीं है और हाल की घटनाओं के बाद इस मत पर ध्यान देना पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। इसलिए रजवाड़ों को भारत में ब्रिटिश शासन के ठोस स्तंभ बनाकर रखने का निर्णय किया गया। जैसा कि ब्रिटिश इतिहासकार पी. ई. राबर्ट्स ने कहा है - “साम्राज्य के आधार के रूप में उनको बनाए रखना तब से ब्रिटिश नीति का एक सिद्धांत रहा है।” फिर भी रजवाड़ों को बनाए रखना रजवाड़ों के प्रति ब्रिटिश नीति का केवल एक पक्ष है। ब्रिटिश अधिकारियों का उन पर पूर्ण नियंत्रण इस नीति का दूसरा पक्ष है। 1857 के विद्रोह से पहले अंग्रेज व्यवहार में इन रजवाड़ों के आंतरिक मामलों में हमेशा दखल देते रहे थे, मगर फिर भी सिद्धान्त रूप में उनको सहयोगी और स्वाधीन शक्ति माना जाता रहा था। अब यह स्थिति एकदम बदल दी गई। अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए राजाओं को अब ब्रिटेन को सर्वोपरि शक्ति मानना पड़ता था। 1876 में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटेन की सत्ता पर जोर देने के लिए रानी विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्ञी का पद संभाल लिया। बाद में लार्ड कर्जन ने भी यह बात स्पष्ट की कि राजा-महाराजा अपने राज्यों का शासन केवल ब्रिटिश सम्राट के एजेंटों के रूप में करेंगे। राजाओं ने इस अधीनता की स्थिति को भी स्वीकार कर लिया और स्वेच्छापूर्वक साम्राज्य के पिछलग्गू बन गए क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें अपने राज्यों के शासक बने रहने का आश्वासन दिया गया था। अंग्रेजों ने सर्वोपरि शक्ति के रूप में रजवाड़ों के आंतरिक शासन पर निगरानी के अधिकार का भी दावा किया। वे रेजिडेन्टों के माध्यम से रजवाड़ों के रोजमर्रा के प्रशासन में दखल ही नहीं देते रहे, बल्कि मंत्रियों और दूसरे बड़े अधिकारियों को नियुक्त करने और हटाने के अधिकार पर भी उन्होंने जोर दिया। कभी-कभी शासकों को ही हटा दिया जाता था या उन्हें उनकी शक्तियों से वंचित कर दिया जाता था। इस तरह के हस्तक्षेप का एक कारण अंग्रेजों की इच्छा थी कि इन राज्यों में एक आधुनिक प्रशासन स्थापित किया जाए ताकि ब्रिटिश भारत से उनका पूर्ण एकीकरण हो सके। इसके अलावा अखिल भारतीय पैमाने पर रेलों, डाक-तार व्यवस्था, मुद्रा-प्रणाली और एक साँझे आर्थिक जीवन के विकास ने भी इस एकीकरण को और उसके फलस्वरूप हस्तक्षेप को और बढ़ाया। हस्तक्षेप का एक दूसरा कारण अनेक राज्यों में लोकतांत्रिक-जन आंदोलनों और राष्ट्रवादी आंदोलनों का उभरना था। एक ओर तो ब्रिटिश अधिकारियों ने राजाओं को इन आंदोलनों को दबाने में सहायता दी और दूसरी और उन्होंने इन राज्यों में प्रशासन के गंभीर दुरूपयोग को समाप्त करने के प्रयास भी किए। प्रशासन संबंधी नीतियाँभारत के प्रति अंग्रेजों का दृष्टिकोण और फलस्वरूप में उनकी नीतियाँ 1857 के विद्रोह के बाद और भी बदतर हो गई। 1857 के पहले उन्होंने, आधे दिल से और झिझक-झिझककर ही सही, भारत का आधुनिकीकरण करने की कोशिशें की थीं। पर अब वे समझ-बूझकर प्रतिक्रियावादी नीतियाँ अपनाने लगे। जैसा कि इतिहासकार पर्सीवल स्पियर ने लिखा है - “प्रगति के साथ भारत की सरकार का प्रेम भाव अब समाप्त हो गया।हम पहले ही देख चुके हैं कि प्रशासन में भारतीयों को प्रभावी ढंग से भाग लेने से रोकने के लिए किस प्रकार भारत और इंग्लैंड में प्रशासनिक संस्थाओं, भारतीय सेवा और सिविल सर्विस को पुनर्गठित किया गया था। पहले कम से कम यही कहा जाता था कि अंग्रेज भारतीयों को स्वशासन के लिए “प्रशिक्षित” और तैयार कर रहे हैं और अंततः राजनीतिक सत्ता भारतीयों को सौंप देंगे। पर अब यह बात खुलकर कही जाने लगी कि अपने सामाजिक और सांस्कृतिक दोषों के कारण भारतीय अपना शासन चला सकने में अयोग्य हैं और उन पर अंग्रेजों का शासन अनिश्चित काल तक बना रहना चाहिए। यह प्रतिक्रियावादी नीति अनेक क्षेत्रों में दिखाई पड़ी। बाँटों और राज करोअंग्रेजों ने भारत के ऊपर विजय भारतीय शासकों की फूट का लाभ उठाकर और उन्हें एक-दूसरे से लड़ाकर प्राप्त की थी। 1858 के बाद उन्होंने जनता के खिलाफ राजाओं को, एक प्रांत के खिलाफ दूसरे प्रांत को, एक जाति के खिलाफ दूसरी जाति को, एक समूह के खिलाफ दूसरे समूह को और सबसे अधिक मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को खड़ा करके बाँटों और राज करो की इस नीति को जारी रखने का फैसला किया।1857 के विद्रोह में हिंदुओं और मुसलमानों की जो एकता देखने को मिली थी, उसमें विदेशी शासक दरार डाल चुके थे। वे उभरते राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर बनाने के लिए इस एकता को तोड़ने पर अमादा थे। सच यह है कि उन्होंने इसका कोई अवसर नहीं छोड़ा। विद्रोह के फौरन बाद उन्होंने मुसलमानों का दमन करना, बड़े पैमाने पर उनकी जमीन-जायदाद जब्त करना आरंभ कर दिया और हिंदुओं को अपना तरफदार घोषित किया। 1870 के बाद यह नीति उलट दी गई, और उच्च तथा मध्य वर्गीय मुसलमानों को राष्ट्रवादी आंदोलन के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की गई। शिक्षित भारतीयों को धार्मिक आधार पर बाँटने के लिए सरकारी सेवाओं में सरकार ने बहुत चालाकी के साथ लोभ का इस्तेमाल किया। औद्योगिक-वाणिज्यिक पिछड़ेपन के कारण तथा सामाजिक सेवाओं के लगभग पूर्ण अभाव के कारण शिक्षित भारतीय तकरीबन पूरी तरह सरकारी सेवा पर निर्भर थे। उनके सामने दूसरे उपाय नहीं के बराबर थे। इस कारण उनके बीच सरकारी पदों के लिए तीखी प्रतियोगिता आरंभ हो गई। सरकार ने इस प्रतियोगिता का लाभ उठाकर प्रांतीय और सांप्रदायिक विद्वेष और घृणा को भड़काया। उसने वफादारी के बदले सांप्रदायिक आधार पर सरकारी कृपा का आश्वासन दिया और इस प्रकार शिक्षित मुसलमानों को शिक्षित हिंदुओं के खिलाफ उभारा। शिक्षित भारतीयों के प्रति शत्रुता1833 के बाद भारत सरकार ने आधुनिक शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया था। 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे और उसके बाद उच्च शिक्षा तेजी से फैली थी। 1857 के विद्रोह में शिक्षित भारतीयों के भाग लेने से इनकार करने पर अनेक अंग्रेज अधिकारियों ने उनकी प्रशंसा की थी, परंतु शिक्षित भारतीयों के प्रति यह अनुकूल सरकारी दृष्टिकोण जल्द ही उलट गया। कारण कि उनमें से अनेक लोग हाल में प्राप्त आधुनिक ज्ञान का उपयोग करके ब्रिटिश शासन के साम्राज्यवादी चरित्र का विश्लेषण करने लगे थे और उन्होंने प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की माँगें सामने रखी थीं। इसलिए जब जनता के बीच राष्ट्रवादी आंदोलन का संगठन करने लगे और उन्होंने 1855 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की तो अधिकारी उच्च शिक्षा के पक्के दुश्मन बन बैठे। अब सरकारी अधिकारी उच्च शिक्षा को फैलने से रोकने के लिए सक्रियतापूर्वक उपाय करने लगे। वे शिक्षित भारतीयों पर अब नाक-भौं सिकोड़ते तथा उनको ‘बाबू’ कहकर उनका मजाक उड़ाते।इस तरह जो भारतीय आधुनिक पश्चिमी ज्ञान प्राप्त कर चुके थे आधुनिकता के आधार पर प्रगति के पक्ष में थे, अंग्रेज उनके खिलाफ हो गए। ऐसी प्रगति भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बुनियादी हितों और नीतियों के खिलाफ थी। शिक्षित भारतीयों और उच्च शिक्षा के प्रति इस सरकारी विरोध से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश शासन के आरंभ में प्रगति की जो भी संभावनाएँ थी, वे इस समय तक समाप्त हो चुकी थीं। जमींदारों के प्रति दृष्टिकोणभविष्य के प्रति सचेत शिक्षित भारतीयों के प्रति शत्रुता की भावना रखने के साथ ही अंग्रेजों ने अब भारतीयों के सबसे प्रतिक्रियावादी वर्गों, जैसे राजाओं, जमींदारों और भूस्वामियों की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हम ऊपर पहले ही दिखा चुके है कि सरकार ने अब राजाओं के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल दिया था और उभरते हुए जन आंदोलनों और राष्ट्रवादी आंदोलनों के खिलाफ उनका उपयोग करने का प्रयास कर रही थी। इसी ढंग से जमींदारों और भूस्वामियों को भी खुश किया गया। उदाहरण के लिए, अवध के अधिकांश ताल्लुकदारों की जमीनें उन्हें लौटा दी गई। जमींदारों और भूस्वामियों को भारतीय जनता के परंपरागत और ‘स्वाभाविक’ नेता कहकर उछाला गया। उनके हितों और विशेषाधिकारों की रक्षा की जाने लगी। किसानों के खिलाफ जमीन पर उनके अधिकार को सुरक्षा दी गई और राष्ट्रवादी रूझान वाले शिक्षित वर्ग के खिलाफ उनका इस्तेमाल किया जाने लगा। 1876 में वायसराय लार्ड लिटन ने खुलकर घोषणा की कि “अब आगे इंग्लैंड के सम्राट एक शक्तिशाली देशी अभिजात वर्ग की आशाओं, आकांक्षाओं, सहानुभूतियों और हितों से संबद्ध समझा जाना चाहिए। बदले में जमींदारों और भूस्वामियों ने यह स्वीकार किया कि समाज में उनकी स्थिति तभी तक है जब तक ब्रिटिश शासन बना रहेगा,” और इस तरह वे इसके पक्के समर्थक हो गए।समाज-सुधार के प्रति दृष्टिकोणरूढ़िवादी वर्गों से सहयोग की इस नीति के अनुसार अंग्रेजों ने समाज-सुधारकों की सहायता करने की पुरानी नीति छोड़ दी। उनका मत था कि सती-प्रथा का उन्मूलन, विधवा-पुनविर्वाह की आज्ञा, आदि समाज-सुधार के कदम 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख कारण थे। इसलिए धीरे-धीरे उन्होंने रूढ़िवादियों का पक्ष लेना आरंभ कर दिया और समाज-सुधारकों का समर्थन बंद कर दिया।अपनी पुस्तक “भारत एक खोज” में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है - “भारत के प्रतिक्रियावादियों के साथ इस स्वाभाविक गठजोड़ के कारण ब्रिटिश शासन अनेक बुरी प्रथाओं और कर्मकांडों का रक्षक तथा समर्थक बन गया, हालाँकि वह अन्यथा इनकी निंदा करता था।” वास्तव में अंग्रेज इस मामले में सांप-छछूंदर वाली स्थिति में थे। अगर वे समाज-सुधार का समर्थन करें और इसके लिए कानून बनाएँ तो रूढ़िवादी भारतीय उनका विरोध करेंगे और यह कहेंगे कि एक विदेशी सरकार को भारतीयों के अंदरूनी सामाजिक मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी ओर, अगर वे ऐसे कानून न बनाएँ तो सामाजिक बुराइयों के बने रहने में सहायक होंगे और सामाजिक दृष्टि से प्रगतिशील भारतीय उनकी निंदा करेंगे। फिर भी यह ध्यान रहे कि अंग्रेज सामाजिक प्रश्नों पर हमेशा उदासीन ही नहीं रहे। यथास्थिति को बनाए रखकर उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक बुराइयों को सुरक्षित ही रखा। इसके अलावा, राजनीतिक लाभ के लिए जातिवाद और संप्रदायवाद को प्रोत्साहित करके उन्होंने सामाजिक प्रतिक्रिया को भी जमकर प्रोत्साहन दिया। सामाजिक सेवाओं का अत्यधिक पिछड़ापन19वीं सदी में यूरोप में शिक्षा, सफाई और जन स्वास्थ्य, जल-आपूर्ति और ग्रामीण सड़कों जैसी सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई थी, पर भारत में ये सेवाएँ अत्याधिक पिछड़ी बनी रहीं। भारत सरकार अपनी भारी आमदनी का अधिकांश भाग सेना, युद्धों और प्रशासकीय सेवाओं पर खर्च कर रही थी और सामाजिक सेवाएँ पैसे के लिए तरस रही थीं। उदाहरण के लिए, 1886 में भारत सरकार को कुल 47 करोड़ रूपयों का राजस्व प्राप्त हुआ। इसमें लगभग 19,41 करोड़ सेना पर और 17 करोड़ प्रशासन पर खर्च किए गए, मगर शिक्षा, चिकित्सा और जन-स्वास्थ्य पर 2 करोड़ रूपये से भी कम और सिंचाई पर केवल 65 लाख खर्च किए गए। सफाई, जल-आपूर्ति और जन-स्वास्थ्य पर झिझक-झिझककर जो थोड़े-बहुत कदम किए गए, वे भी आमतौर पर नगरों तक और उनमें भी तथाकथित सिविल लाइनों अर्थात नगरों के ब्रिटिश या आधुनिक भाग तक सीमित रहे। ये सेवाएँ मुख्यतः यूरापीय तथा नगरों के यूरोपीय भागों में रहने वाले थोड़े से उच्चवर्गीय भारतीयों के लिए ही थीं।श्रम संबंधी कानून19वीं सदी में आधुनिक कारखानों और बागानों के मजदूरों की हालत बहुत ही दयनीय थी। प्रतिदिन उनको 12 से 16 घंटों तक काम करना पड़ता और आराम के लिए सप्ताह में एक दिन की छुट्टी भी न मिलती। स्त्रियों और बच्चों को भी पुरूषों जितना ही काम करना पड़ता था। मजदूरी बहुत कम, प्रति माह 4 से 20 रूपये तक थी। कारखाने लोगों से भरे होते, उनमें प्रकाश और हवा की कमी होती और वे बेहद गंदे होते, मशीनों पर काम करना खतरे से भरा था और आए दिन दुर्घटनाएँ होती रहती थीं।यूँ तो भारत सरकार पूँजीपतियों की सर्मथक थी, फिर भी उसे आधुनिक कारखानों की बुरी स्थिति के प्रभावों को कम करने के लिए आधे मन से कुछ कदम उठाने पड़े जो एकदम अपर्याप्त थे। इन कारखानों में अनेक भारतीयों के थे। इस बारे में सरकार मानवीय भावनाओं से अंशतः ही प्रेरित हुई। ब्रिटेन के उद्योगपति फैक्टरी कानून बनाने के लिए सरकार पर लगातार दबाब डाल रहे थे। उन्हें डर था कि भारत में मजदूरी कम होन कारण भारतीय उद्योगपति भारतीय बाजार में उन्हें जल्द ही प्रतियोगिता में पीट देंगे। पहला इंडियन फैक्टरी एक्ट 1881 में बनाया गया। यह कानून मुख्यतः बाल-श्रम से संबंधित था। इसमें कहा गया कि 7 वर्ष से कम के बच्चों को कारखानों में नहीं लगाया जाएगा और 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों से प्रतिदिन 9 घंटें से अधिक काम नहीं लिया जाएगा। बच्चों को महीने में चार छुट्टियाँ भी मिलेंगी। इस कानून में खतरनाक मशीनों को अच्छी तरह अलग-थलग रखने की व्यवस्था थी थी। दूसरा इंडियन फैक्टरीज एक्ट 1891 में बनाया गया। इसमें सभी मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था थी। स्त्रियों के लिए प्रतिदिन काम के 11 घंटे निश्चित किए गए तथा बच्चों के लिए काम का समय घटाकर 7 घंटे कर दिया गया। मगर पुरूषों के काम के घंटों के लिए अभी भी कोई सीमा नहीं तय की गई। चाय और काफी के जिन बागानों के मालिक अंग्रेज थे उन पर इन दोनों में से कोई भी कानून नहीं लागू किया गया उल्टे विदेशी बागान-मालिकों को मजदूरों का अत्यधिक निर्मम शोषण करने में सरकार ने हर तरह की सहायता दी। अधिकांश चाय बागान असम में स्थित थे जिसकी आबादी बहुत कम थी जहाँ जलवायु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी। इसलिए बागानों पर काम करने के लिए बाहर से मजदूर लाने पड़ते थे। मगर बाहरी मजदूरों को बागानों के मालिक अच्छा वेतन देकर नहीं लाते थे। इसके बजाए धोखा-धड़ी करके और बलपूर्वक उन्हें भर्ती किया जाता और बागानों पर उन्हें लगभग गुलामों की तरह रखा जाता। भारत सरकार ने इन बागान मालिकों की पूरी सहायता की तथा उनकी सहायता के लिए 1863, 1865, 1870, 1873 और 1882 में दंड-कानून बनाए। कोई मजदूर किसी बाग पर जाकर काम करने के समझौते पर दस्तखत करने के बाद काम करने से इंकार नहीं कर सकता था। मजदूर द्वारा समझौता का कोई भी उल्लंघन एक दंडनीय अपराध था। बाग के मालिक का उसे गिरफ्तार करने तक का अधिकार था। फिर भी, उभरते हुए ट्रेड यूनियन आंदोलन के दबाव में 20वीं सदी में कुछ बेहतर श्रम कानून बने। तो भी भारतीय मजदूर वर्ग की हालत अत्यंत दयनीय बनी रही। औसत मजदूर को पूरा भोजन-वस्त्र भी नहीं मिलता था। ब्रिटिश शासन में भारतीय मजदूरों की हालत का वर्णन जर्मनी के प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार प्रोफेसर युर्गेन कुर्त्सीस्की ने 1938 में इन शब्दों में किया था - “आधा पेट खाकर रहने वाला, जानवरों की तरह प्रकाश, हवा और पानी से रहित घरों में रहने वाला भारतीय औद्योगिक मजदूर औद्योगिक पूँजीवाद की पूरी दुनिया में सबसे अधिक शोषित मजदूरों में से हैं।” प्रेस पर प्रतिबंधभारत में छापाखाने की शुरूआत अंग्रेजों ने की थी और इस तरह एक आधुनिक प्रेस की बुनियाद उन्होंने डाली थी। शिक्षित भारतीयों ने जल्द ही समझ लिया की जनमत को शिक्षित करने तथा आलोचना और निंदा के द्वारा सरकार की नीतियों को प्रभावित करने में प्रेस की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। सामाचार-पत्र आरंभ करने तथा उन्हें एक सशक्त राजनीतिक साधन बनाने में राममोहन राय, विद्यासागर, दादाभाई नौरोजी, जस्टिस रानाडे, सी. कर्झनकार मेनन, मदनमोहन मालवीय, लाला लाजपतराय, विपिनचन्द्र पाल और दूसरे भारतीयों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रेस धीरे-धीरे राष्ट्रवादी आंदोलन का एक प्रमुख अस्त्र बन गया।1835 में चार्ल्स मेटकाफ ने भारतीय प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया था। इस कदम का शिक्षित भारतीयों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया था। लेकिन राष्ट्र्रवादी धीरे-धीरे प्रेस का इस्तेमाल जनता में राष्ट्रवादी चेतना जगाने के लिए और सरकार की प्रतिक्रियावादी नीतियों की कड़ी आलोचना करने के लिए करने लगे। इससे अधिकारी भारतीय प्रेस के विरोधी हो गए और उसकी आजादी को कम करने का उन्होंने फैसला किया। इसके लिए 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बनाया गया। इस कानून ने भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों की आजादी पर कड़ी बंदिशें लगाई। भारतीय राष्ट्रवादी जनमत तब तक जागरूक हो चुका था और उसने इस कानून के बनाए जाने का जोरदार विरोध किया। इस विरोध का तात्कालिक प्रभाव पड़ा और इस कानून को 1882 में रद्द कर दिया गया इसके बाद लगभग 25 वर्षों तक भारतीय प्रेस को पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त रही। लेकिन 1905 में जुझारू स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के बाद 1908 और 1910 में कड़े प्रेस कानून फिर बनाए गए। जातीय शत्रुताभारतीयों पर हुकूमत बनाए रखने के लिए उनसे सामाजिक दूरी बनाए रखना आवश्यक है, यह मानकर अंग्रेज हमेशा भारतीयों से कटे-कटे रहे। वे स्वयं को जातीय दृष्टि से भी श्रेष्ठ मानते थे। 1857 के विद्रोह ने तथा विद्रोह के दौरान दोनों पक्षों द्वारा किए गए अत्याचारों ने भारतीयों और अंग्रेजों के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया। अब अंग्रेज खुलकर जातीय श्रेष्ठता के सिद्धान्त का प्रचार करने और जातीय दंभ दिखाने लगे। “केवल यूरोपीयों के लिए” आरक्षित रेलों के डिब्बे, रेलवे स्टेशनों के प्रतीक्षालय, पार्क, होटल, स्विमिंग पूल, क्लब आदि इस नस्लवाद के स्पष्ट उदाहरण थे। इससे भारतीय स्वयं को अपमानित महसूस करते। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में -“हम भारतीयों को नस्लवाद के सभी रूपों का ज्ञान ब्रिटिश शासन के आरंभ-काल से ही रहा है। इस शासन की पूरी विचारधारा भद्रजन और स्वामी जाति की रही है और सरकार का पूरा ढाँचा इसी विचारधारा पर आधारित रहा है, बल्कि स्वामी जाति का विचार साम्राज्यवाद में ही निहित है। इस बारे में कोई दुराव-छिपाव नहीं था तथा शक्ति संपन्न लोग खुलकर इसकी घोषणा करते थे। शब्दों से भी कहीं अधिक प्रभावी यह व्यवहार था जो इन शब्दों के साथ जुड़ा होता था और पीढ़ी-दर-पीढ़ी, साल-दर-साल एक राष्ट्र के रूप में भारत को और व्यक्तिगत रूप से भारतीयों को अपमान, घृणा और अपमानजनक व्यवहार का शिकार बनाया जाता रहा। हमसे कहा जाता कि अंग्रेज एक शासक जाति है और उन्हें हम पर शासन करने तथा हमें बंधन में रखने का ईश्वर-प्रदत्त अधिकार है और अगर हम विरोध करते तो हमें ‘शासक जाति के सिंह-समान गुणों’ की याद दिला दी जाती थी।” विदेशी नीतिब्रिटिश शासन में पड़ोसियों के साथ भारत के संबंध एक नए आधार पर विकसित हुए। इसके दो कारण थे। संचार के आधुनिक साधनों के विकास तथा देश के राजनीतिक और प्रशासकीय सुदृढ़ीकरण ने भारत सरकार को प्रेरित किया कि वह देश की प्राकृतिक भौगोलिक सीमाओं तक अपना विस्तार करें। यह सुरक्षा और आंतरिक दृढ़ता, दोनों के लिए आवश्यक थी। इसके फलस्वरूप सीमाओं पर अनिवार्य रूव से कुछ टकराव हुए। दुर्भाग्य से भारत सरकार प्राकृतिक और परंपरागत सीमाओं के बाहर भी कभी-कभी चली जाती थी। दूसरा और नया कारण भारत सरकार का विदेशी चरित्र था। एक स्वतंत्र देश की विदेश नीति विदेशियों द्वारा शासित किसी देश की विदेश नीति से मूलतः भिन्न होती है। एक स्वतंत्र देश की विदेशी नीति उसकी जनता की आवश्यकताओं और हितों पर आधारित होती है। जबकि एक पराधीन देश की विदेश नीति शासक देश के हितों की पूर्ति करती है। भारत के मामले में सरकार ने जिस विदेश नीति को अपनाया उसका संचालन लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार करती थी। एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश सरकार के दो प्रमुख लक्ष्य थे अपने बहुमूल्य भारतीय साम्राज्य की रक्षा करना और एशिया तथा अफ्रीका में ब्रिटेन के व्यापार और अन्य आर्थिक हितों को आगे बढ़ाना। इन दो लक्ष्यों के कारण अंग्रेजों ने भारत की प्राकृतिक सीमाओं से बाहर भी अपना प्रसार किया और नए इलाके जीते। इसके अलावा, इन लक्ष्यों के कारण ब्रिटिश सरकार का यूरोप के दूसरे साम्राज्यवादी राष्ट्रों से टकराव भी हुआ क्योंकि ये राष्ट्र भी एशिया और अफ्रीका मे अपने इलाके बढ़ाना और व्यापार फैलाना चाहते थे।भारतीय साम्राज्य की रक्षा करने, ब्रिटेन के आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने तथा दूसरी यूरोपीय शक्तियों को भारत से दूर रखने की धुन में भारत की ब्रिटिश सरकार ने अक्सर भारत के पड़ौसी देशों पर आक्रमण किए। दूसरे शब्दों में ब्रिटिश शासन के दिनों में पड़ौसियों के साथ भारत के संबंध अंततः ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आवश्यकताओं से निर्धारित होते थे। लेकिन भारत की विदेश नीति ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आवश्यकता पूरी तो करती थी, पर उसे लागू करने का खर्च भारत को बरदाश्त करना पड़ता था। ब्रिटिश हितों की पूर्ति के लिए भारत को अपने पड़ोसियों के साथ अनेक युद्ध करने पड़े, भारतीय सैनिकों को अपना खून बहाना पड़ा और उसके भारी खर्च पूरे करने को लिए भारतीयों को कर चुकाने पड़ते थे। नेपाल के साथ युद्ध (1814)भारतीय साम्राज्य को उसकी प्राकृतिक भौगोलिक सीमा तक फैलाने की अंग्रेजों की धुन के साथ सबसे पहले उनका उत्तर में स्थित नेपाल से टकराव हुआ। अक्टूबर 1814 में दोनों देशों की सीमा पुलिस के बीच झड़प हुई जिससे खुला युद्ध आरंभ हो गया। सैनिक शक्ति, धन और सामग्री, सभी दृष्टियों से अंग्रेज नेपालियों से श्रेष्ठ थे। अंत में नेपाल सरकार को ब्रिटेन की शर्तों पर शांति की बातचीत करनी पड़ी। उसे अपने यहाँ एक ब्रिटिश रेजीमेन्ट रखना पड़ा। उसे गढ़वाल तथा कुमाऊँ के जिले छोड़ने पड़े तथा तराई के क्षेत्रों पर भी अपना दावा त्यागना पड़ा। उसे सिक्किम से भी हट जाना पड़ा। इस समझौते से अंग्रेजों को अनेक लाभ हुए। उनका भारतीय साम्राज्य अब हिमांचल तक फैल गया। मध्य एशिया के साथ व्यापार में उन्हें अब अधिक सुविधा हो गई। उन्हें हिल-स्टेशन बनाने के लिए शिमला, मसूरी और नैनीताल जैसे महत्वपूर्ण स्थान भी मिल गए। इसके अलावा भारी संख्या में ब्रिटिश भारत की सेना में शामिल होकर गोरखों ने उसकी शक्ति और भी बढ़ा दी।बर्मा पर विजय19वीं सदी में तीन बार स्वतंत्र बर्मा से युद्ध करके अंततः उस पर कब्जा कर लिया। बर्मा और ब्रिटिश भारत का टकराव सीमा संबंधी झड़पों से आरंभ हुआ। उसे प्रसारवादी आकांक्षाओं ने और उकसाया। बर्मा के जंगल संबंधी संसाधनों पर ब्रिटिश व्यापारियों की लालची निगाहें बहुत पहले से गड़ीं थीं और वे उसकी जनता को भी अपने कारखानों के माल निर्यात करने के लिए बेचैन थे। ब्रिटिश अधिकारी भी बर्मा तथा शेष दक्षिण-पूर्व एशिया में फ्रांसीसीयों के व्यापारिक और राजनीतिक प्रभाव को बढ़ने से रोकना चाहते थे। 18वीं सदी में जब बर्मा और ब्रिटिश भारत अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे, तो दोनों की सीमाएँ आ मिलीं। सदियों के अंदरूनी कलह के बाद बर्मा में सम्राट अलौंगपाय ने 1752-60 में एकता स्थापित करने में सफलता पाई थी। इरावती नदी के तट पर स्थित अवा में शासन कर रहे उसके उत्तराधिकारी बोदावपाय ने बार-बार स्याम पर आक्रमण किया, अनेकों चीनी हमलों को नाकाम बनाया, 1785 में अराकान और 1813 में मणिपुर के सीमावर्ती राज्यों पर अधिकार किया और इस प्रकार बर्मा की सीमा को ब्रिटिश भारत की सीमा तक फैला दिया। पश्चिमी की ओर बढ़ना जारी रखते हुए उसने असम और ब्रह्मपुत्र घाटी के लिए एक खतरा पैदा कर दिया। अंततः 1822 में बर्मियों ने असम को जीत लिया। अराकान और असम पर बर्मा की विजय के बाद उसकी और बंगाल की अस्पष्ट सीमाओं पर लगातार झड़पों का एक युग आरंभ हो गया।1824 में ब्रिटिश भारत के शासकों ने बर्मा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। आरंभ में कुछ समय तक हारते रहने के बाद ब्रिटिश सेनाओं ने अंततः असम, कछार, मणिपुर और अराकान से बर्मियों को बाहर कर दिया। मई 1824 में ब्रिटिश नौसेना ने समुद्र के रास्ते रंगून पर अधिकार कर लिया और राजधानी अवा से 45 मील दूर तक पहुँच गए। यांदबों की संधि के द्वारा फरवरी 1826 में शांति स्थापित हुई। बर्मा की सरकार ने (1) लड़ाई के हर्जाने के रूप में एक करोड़ रूपए देने की, (2) अराकान और तेनासेरिम के समुद्र तटीय प्रांतों पर से अधिकार छोड़ने की, (3) असम, कछार और जयंतिया पर सारे दावे छोड़ देने की, (4) मणिपुर को स्वतंत्र राज्य स्वीकार करने की, (5) ब्रिटेन के साथ एक व्यापारिक संधि की बातचीत चलाने की, (6) अवा में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखने तथा कलकत्ता में एक बर्मी दूत नियुक्त करने की शर्ते मान लीं। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने बर्मा को उसके अधिकांश समुद्र तट से वंचित कर दिया और भावी प्रसार के लिए बर्मा में अपनी जड़ें मजबूत कर लीं। 1852 में जो दूसरा बर्मा युद्ध छिड़ा, वह लगभग पूरी तरह ब्रिटेन के व्यापारिक लोभ का परिणाम था। इमारती लकड़ी का व्यापार करने वाली ब्रिटिश फर्मों ने अब तक ऊपरी बर्मा के जंगलों की इमारती लकड़ी में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी थी। इसके अलावा अंग्रेजों को लगा कि बर्मा की विशाल जनसंख्या ब्रिटेन के सूती कपड़ों और दूसरे औधोगिक मालों की बिक्री के लिए एक बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध करा सकती है। अंग्रेज जो बर्मा के दो तटीय प्रांतों पर पहले ही कब्जा जमाए बैठे थे, अब बाकी देश के व्यापारिक संबंधों पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाह रहे थे। वे यह भी चाहते थे कि शांति से हो या युद्ध से, वे अपने व्यापारिक प्रतियोगियों, अर्थात फ्रांसीसियों या अमरीकियों के पैर जमाने से पहले बर्मा पर अपनी जकड़ को मजबूत बना लें। इस बार का युद्ध 1825-26 के युद्ध की अपेक्षा बहुत कम समय तक चला और अंग्रेजों की विजय भी बहुत निणार्यक रही। अंग्रेजों ने अब बर्मा के अकेले बचे तटीय प्रांज पेगू को भी हड़प लिया। फिर भी दक्षिणी बर्मा पर प्रभावी नियंत्रण जमाने से पहले अंग्रेजों को तीन साल तक जनता की एक भयानक छापामार लड़ाई का सामना करना पड़ा। अब बर्मा के पूरे समुद्र तट पर और उसके पूरे समुद्री व्यापार पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो चुका था। इस लड़ाई को लड़ने की मुख्य जिम्मेदारी भारतीय सैनिकों को उठानी पड़ी और इसका खर्च भारतीय धन से पूरा किया गया। पेगू के अधिग्रहण के बाद अनेक वर्षों तक बर्मा और ब्रिटेन के बीच शांति बनी रही। फिर भी अंग्रेज ऊपरी बर्मा में पैर फैलाने की कोशिशें करते रहे। ब्रिटेन के व्यापारियों और उधोगपतियों को खास लोभ इसका था कि बर्मा के रास्ते चीन से व्यापार संभव था। बर्मा में फ्रासीसियों का बढ़ता हुआ प्रभाव भी अंग्रेजों को जलन का शिकार बनाए हुए था। ब्रिटिश व्यापारियों को डर था कि कहीं उनके फ्रांसीसी और अमरीकी प्रतिद्वंदी बर्मा के विशाल बाजार पर अधिकार ना कर लें। अब ब्रिटेन में चैंबर ऑफ कामर्स ने तथा रंगून में बैठे ब्रिटिश व्यापारियों ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला कि वह ऊपरी बर्मा पर फौरन कब्जा करे। ब्रिटिश सरकार स्वयं भी इसके लिए इच्छुक थी। 13 नवंबर 1885 को अंग्रेजों ने बर्मा पर हमला किया। 28 नंवबर 1885 को सम्राट थिबाऊ ने आत्मसमर्पण कर दिया तथा उसके राज्य को जल्द ही भारतीय साम्राज्य में मिला लिया गया। बर्मा की विजय तो बहुत आसान रही पर उस पर शासन करना इतना आसान नहीं रहा। सेना के देशभक्त सैनिकों और अधिकारियों ने आत्मसमर्पण करने से इंकार कर दिया। उन्होंने घने जंगलों में शरण ले ली और वहीं से एक व्यापक छापामार युद्ध चलाते रहे। दक्षिण बर्मा की जनता भी विद्रोह के लिए उठ खड़ी हुई। जनविद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों को लगातार पाँच वर्षों तक 40,000 की सेना का प्रयोग करना पड़ा। इस लड़ाई तथा इसके बाद विद्रोह को कुचलने के अभियान का खर्च भी भारतीय खजाने से ही लिया गया। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद बर्मा में आधुनिक प्रकार का एक जोरदार राष्ट्रवादी आंदोलन उठ खड़ा हुआ। ब्रिटिश माल और प्रशासन के बहिष्कार का एक व्यापक अभियान चला और होमरूल की माँग सामने रखी गई। बर्मा के राष्ट्रवादियों नें जल्द ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हाथ मिला लिया। बर्मा के स्वाधीनता संग्राम को कमजोर कर सकने की आशा में 1935 में अंग्रेजों ने बर्मा को भारत से अलग कर दिया। बर्मी राष्ट्रवादियों ने इस कदम का विरोध किया। बर्मा का राष्ट्रवादी आंदोलन द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान ऊं आंग सान के नेतृत्व में अपनी चरम सीमा पर जा पहुँचा। अंततः 4 जनवरी 1948 को बर्मा ने अपनी स्वाधीनता प्राप्त की। अफगानिस्तान के साथ संबंधअफगानिस्तान के साथ संबंधों के स्थायी बनने से पहले भारत की ब्रिटिश सरकार के उससे दो युद्ध हुए। ब्रिटिश दृष्टिकोण से अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण थी। रूस की ओर से संभावित सामरिक चुनौती का सामना करने तथा मध्य एशिया में ब्रिटेन के व्यापारिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान भारत की सीमा के बाहर एक अगली चौकी का काम कर सकता था और कुछ नहीं तो वह दो शत्रु शक्तियों के बीच एक सुविधाजनक तटस्थ देश ही हो सकता था। अंग्रेज अफगानिस्तान में रूस के प्रभाव को कमजोर बनाना और समाप्त करना तो चाहते थे, पर वे अफगानिस्तान को मजबूत बनते भी नहीं देखना चाहते थे। वे उसे एक कमजोर तथा बँटा हुआ देश ही बनाए रखना चाहते थे ताकि आसानी से उस पर नियंत्रण कर सकें।अंग्रेज अफगानिस्तान के स्वतंत्र शासक दोस्त मुहम्मद को हटा कर उसकी जगह किसी ‘मित्र’ अर्थात् पिट्ठू शासक को बिठाना चाहते थे। उनकी निगाह अब शाह शुजा पर पड़ी जिससे 1809 में गद्दी छिन गई थी और जो लुधियाना में अंग्रेजों का पेंशनखोर बनकर रह रहा था। अंग्रेजों ने अफगानिस्तान की गद्दी के लिए उसी का समर्थन करने का निश्चय किया। अब उन्होंने बिना किसी कारण या बहाने के अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में दखल देने तथा इस छोटे से पड़ोसी देश पर हमला करने का निश्चय किया। यह हमला फरवरी 1839 में किया गया। अधिकांश अफगान कबीलों को अब तक रिश्वत देकर खरीदा जा चुका था। 7 अगस्त 1839 को काबुल पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ और उन्होंने फौरन गद्दी पर शाह शुजा को बिठा दिया। पर शाह शुजा को अफगानिस्तान की जनता घृणा की दृष्टि से देखती थी, खासकर इसलिए कि वह विदेशी संगीनों का सहारा लेकर फिर से शासक बना था। अनेक अफगान कबीलों ने विद्रोह कर दिया। फिर एकाएक 2 नवंबर 1841 को काबुल में विद्रोह छिड़ गया और हट्टे-कट्टे अफगान ब्रिटिश सेनाओं पर टूट पड़े। अंग्रेजों ने मजबूर होकर 11 दिसंबर 1841 को अफगान सरदारों से एक समझौता किया और बात मान ली कि वे अफगानिस्तान से चले जाएँगें और दोस्त मुहम्मद को फिर से गद्दी पर बिठाया जाएगा। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब अंग्रेज अफगानिस्तान छोड़ रहे थे, पूरे रास्ते भर उन पर जगह-जगह हमले हुए। 16,000 सैनिकों में से केवल एक ही जिंदा सीमा तक पहुँचा और अनेकों जीवित रहे पर युद्धबंदी बनकर। इस तरह अंग्रेजों का अफगान अभियान बुरी तरह असफल रहा। अब ब्रिटिश भारत की सरकार ने एक नए अभियान की तैयारी की। 16 सितंबर 1842 को उन्होंने दोबारा काबुल पर अधिकार कर लिया, पर उन्होंने पिछले अनुभव से अच्छी तरह सबक लिया था। हाल की हार और अपमान का बदला ले चुकने के बाद उन्होंने दोस्त मुहम्मद से समझौता कर लिया तथा काबुल को खाली करके उन्होंने दोस्त मुहम्मद को अफगानिस्तान का स्वतंत्र शासक मान लिया। प्रथम अफगान युद्ध में डेढ़ करोड़ रूपए से अधिक का खर्च आया था तथा लगभग 20,000 सैनिक मारे गए थे। अंग्रेजों ने अब अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में दखल न देने की नीति अपनाई। 1860 के दशक में क्रीमियाई युद्ध में हारने के बाद जब रूस ने मध्य एशिया पर ध्यान देना आरंभ किया तो अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को एक तटस्थ देश के रूप में मजबूत बनाने की नीति अपनाई। उन्होंने काबुल के अमीर को अपने अंदरूनी दुश्मनों पर काबू पाने तथा विदेशी शत्रुओं से अपनी स्वाधीनता बनाए रखने में हर तरह की सहायता दी। इस तरह हस्तक्षेप न करने तथा कभी-कभी सहायता देने की नीति अपनाकर उन्होंने अमीर को रूस के साथ हाथ मिलाने से रोके रखा। 1870 के बाद पूरी दुनिया में साम्राज्यवाद का पुनरूत्थान हुआ। अंग्रेजों और रूस की शत्रुता भी बढ़ी। अब एक बार फिर ब्रिटिश राजनेताओं ने अफगानिस्तान को अपने प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण में लाने की बात सोची ताकि वे मध्य एशिया में ब्रिटेन के प्रसार के लिए एक आधार का काम दे सकें। अफगान शासक शेर अली पर ब्रिटेन की शर्तें लादने के लिए उन्होंने 1878 में अफगानिस्तान पर एक और हमला किया। इसे ही दूसरा अफगान युद्ध कहा जाता है। मई 1879 में शांति स्थापित हुई जब शेर अली के बेटे याकूब खान ने गंदमक की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को वह सब कुछ मिल गया जो वे चाहते थे। उन्हें कुछ सीमावर्ती जिले मिल गए, कावुल में एक रेजीडेंट रखने का अधिकार मिल गया और अफगानिस्तान की विदेश नीति पर उनका नियंत्रण स्थापित हो गया। अंग्रेजों की सफलता बहुत समय तक नहीं बनी रही। चूँकि अफगानों के राष्ट्रीय स्वाभिमान को चोट पहुँची थी, इसलिए अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक बार फिर उठ खड़े हुए। विद्रोही अफगान सैनिकों ने 3 सितंबर 1879 को ब्रिटिश रेजिडेंट मेजर केवान्यारी तथा उसके सैनिक के अंगरक्षक पर हमला करके उन्हें मार डाला। अफगानिस्तान पर अंग्रेजों ने एक बार फिर हमला करके उस पर अधिकार कर लिया। पर अफगान अपनी बात स्पष्ट कर चुके थे। अंग्रेजों ने फिर एक बार अपनी नीति बदली तथा एक मजबूत और दोस्त अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में दखल न देने की पुरानी नीति अपनाई। दोस्त मुहम्मद के पोते अब्दुर्रहीम को अफगानिस्तान का नया शासक स्वीकार किया गया। अब्दुर्रहमान ने भी ब्रिटेन को छोड़कर किसी और शक्ति से राजनीतिक संबंध न रखने की बात मान ली। इस तरह अफगानिस्तान के अमीर का अपनी विदेश नीति पर नियंत्रण नहीं रहा और इस सीमा तक वह एक पराधीन शासक बन गया। पर साथ ही अपने देश के अंदरूनी मामलों पर उसका पूरा अधिकार बना रहा। प्रथम विश्वयुद्ध तथा 1917 की रूसी क्रांति ने आंग्ल-अफगान संबंधों को एक नया मोड़ दिया। अफगान अब ब्रिटिश नियंत्रण से पूर्ण स्वाधीनता की माँग करने लगे। हबीबुल्लाह ने, जो 1901 में अब्दुर्रहमान के बाद अमीर बना था, ब्रिटिश भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। 1921 में शांति स्थापित हुई और एक संधि के द्वारा अफगानिस्तान को अपने विदेशी मामलों में अपनी स्वाधीनता वापस मिल गई। | |||||||||
| |||||||||