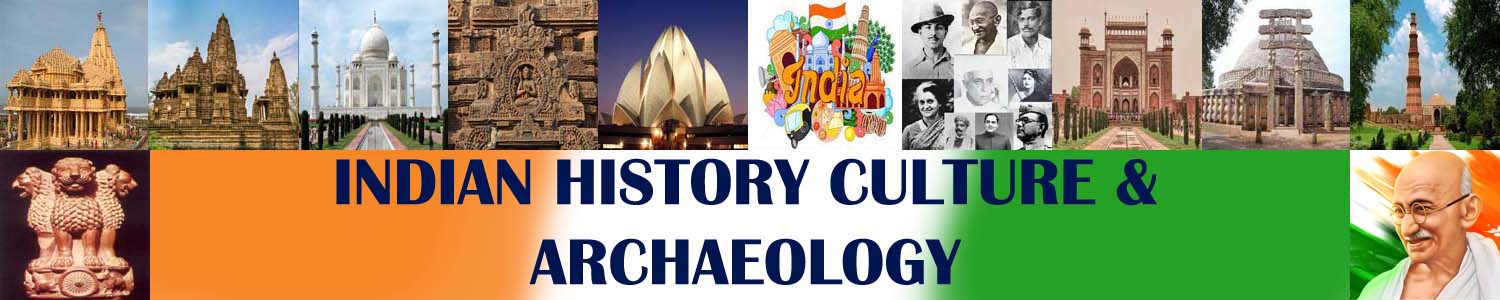| |||||||||
|
18वीं सदी में प्रशासनिक संगठन और सामाजिक तथा सांस्कृतिक नीति
जैसा कि हम जानते हैं कि 1784 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया था और उसकी आर्थिक नीतियाँ ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को देखते हुए निर्धारित की जाने लगी थीं। अब हम उस संगठन की चर्चा करेंगे जिसके जरिए कंपनी ने अपने नव प्राप्त उपनिवेश की शासन व्यवस्था का संचालन किया।
आरंभ में कंपनी ने भारत स्थित अपने इलाकों का प्रशासन भारतीयों के हाथों में छोड़ दिया था और तब उसकी गतिविधियाँ देख-रेख तक ही सीमित रह गई थीं। मगर उसने जल्द ही समझ लिया कि प्रशासन के पुराने तौर-तरीकों का अनुसरण करने से ब्रिटिश उद्देश्य ठीक से प्राप्त नहीं हो सकते। फलस्वरूप कंपनी ने प्रशासन के कुछ पहलुओं को अपने हाथों में ले लिया। वारेन हेस्टिंग्ज और कार्नवालिस के शासनकाल में ऊपर के प्रशासन में आमूल परिवर्तन किया गया और नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजी प्रशासन ढाँचे की तर्ज पर रखी गई। नए क्षेत्रों में ब्रिटिश सत्ता के विस्तार, नई समस्याओं, नई आवश्यकताओं, नए अनुभवों और नए विचारों के फलस्वरूप उन्नीसवीं सदी में प्रशासन की व्यवस्था में अधिक गंभीर परिवर्तन हुए। मगर इन परिवर्तनों के दौरान साम्राज्यवाद के व्यापक उद्देश्यों को कभी नहीं भुलाया गया। भारत में ब्रिटिश प्रशासन तीन खंभों पर टिका हुआ था। वे थे नागरिक सेवा (सिविल सर्विस), सेना और पुलिस। ऐसा दो वजहों से था। पहला कारण, ब्रिटिश भारत के प्रशासन का मुख्य लक्ष्य कानून और व्यवस्था को बनाए रखना तथा ब्रिटिश शासन को स्थायी बनाना था। कानून और व्यवस्था के अभाव में ब्रिटिश सौदागर और ब्रिटिश विनिर्माता अपनी वस्तुओं को भारत के कोने-कोने में बेचने की उम्मीद नहीं रख सकते थे। फिर विदेशी होने के कारण अंग्रेज भारतीय जनता का स्नेह पाने की आशा नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने भारत पर अपना नियत्रण बनाए रखने के लिए जन समर्थन के बदले शक्ति का सहारा लिया। ड्यूक आफ वेलिंग्टन ने अपने भाई लार्ड वेल्सली के मातहत भारत में काम किया था उसने यूरोप जाने पर लिखा - भारत में सरकार की व्यवस्था, सत्ता की नींव और उसे संभाले रखने तथा सरकार के कार्यकलापों को चलाने के तौर-तरीके समान उद्देश्य के लिए यूरोप में अपनाए गए और तौर-तरीकों से बिल्कुल भिन्न हैं .... वहाँ संपूर्ण सत्ता की नींव और उपकरण तलवार है।” नागरिक सेवा (सिविल सर्विस)नागरिक सेवा (सिविल सर्विस) का जन्मदाता लार्ड कार्नवलिस था। जैसा कि पहले के एक अध्याय में हम देख चुके हैं, आरंभ से ही पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार कर्मचारियों के जरिए होता था। कर्मचारियों को बहुत कम मजदूरी दी जाती थी मगर उन्हें अपना निजी व्यापार करने की इजाजत थी। बाद में जब कंपनी एक क्षेत्रीय शक्ति बन गई, तब उन्हीं कर्मचारियों ने प्रशासनिक कार्य करने आरंभ किए। वे तब अत्यंत भ्रष्ट हो गए। स्थानीय बुनकरों और दस्तकारों, सौदागरों और जमींदारों का उत्पीड़न कर, राजाओं और नवाबों से घूस और नजराना ऐंठकर और गैरकानूनी निजी व्यापार के जरिए उन्होंने अकथनीय संपदा इकट्ठी की, जिसको लेकर सेवानिवृत्त हो इंग्लैंड चले गए। क्लाइव और वारेन हैस्टिंग्ज ने उनके भ्रष्टाचार को समाप्त करने के प्रयास किए, मगर वे इस काम में आंशिक रूप से ही सफल रहे।कार्नवालिस 1786 में भारत का गवर्नर-जनरल बन कर आया। वह प्रशासन को स्वच्छ बनाने के लिए दृढ़-प्रतिज्ञ था मगर उसने महसूस किया कि कंपनी के कर्मचारी तब तक ईमानदारी और कुशलतापूर्वक काम नहीं कर सकते जब तक उन्हें पर्याप्त वेतन नहीं दिए जाते। इसीलिए उसने निजी व्यापार तथा अफसरों द्वारा नजराने और घूस लिए जाने के खिलाफ सख्त कानून बनाए। साथ ही उसने कंपनी के कर्मचारियों के वेतन भी बढ़ा दिए। उदाहरण के लिए, जिले के कलेक्टर का वेतन 1500 रुपए प्रति माह निर्धारित किया गया। इसके अतिरिक्त उसे अपने जिले की कुल वसूल की गई राजस्व रकम का एक प्रतिशत दिया जाना तय हुआ। वस्तुतः कंपनी की नागरिक सेवा, संसार में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली सेवा हो गई। कार्नवालिस ने यह भी निर्धारित किया कि नागरिक सेवा में पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर होगी जिससे उसके सदस्य बाहरी प्रभाव से मुक्त रहें। लार्ड वेल्सली ने 1800 में नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों को प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला। कंपनी के निदेशकों ने उसकी कार्रवाई को पसंद नहीं किया और 1806 में उन्होंने कलकत्ता के कॉलेज की जगह इंग्लैण्ड में हैलीवरी के अपने ईस्ट इंडियन कॉलेज में प्रशिक्षण का काम आरंभ किया। 1853 तक नागरिक सेवा में सारी नियुक्तियाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक करते रहे। बोर्ड आफ कंट्रोल के सदस्यों को खुश करने के लिए उन्होंने उन्हें कुछ नियुक्तियाँ करने का मौका दिया। निदेशकों ने इस लाभप्रद और बहुमूल्य विशेषाधिकार को बनाए रखने के लिए बहुत संघर्ष किया और जब संसद ने उनके अन्य आर्थिक और राजनीतिक विशेषाधिकार को छीन लिया तब भी उन्होंने इस विशेषाधिकार को छोड़ने से इनकार कर दिया। अंततोगत्वा 1853 में वे उसे खो बैठे जब चार्टर एक्ट ने यह कानूनी व्यवस्था लागू कर दी कि नागरिक सेवा में सारे प्रवेश प्रतियोगी परिक्षाओ द्वारा किए जाएँगे। कार्नवालिस के जमाने से ही भारतीय नागरिक सेवा की एक खास विशेषता थी - भारतीयों को बड़ी सख्ती से पूरी तरह अलग रखना। अधिकृत तौर पर 1793 में यह व्यवस्था की गई थी कि प्रशासन में उन सारे ऊँचे ओहदों पर जहाँ 500 पौंड सालाना से अधिक वेतन मिलता था, केवल अंग्रेज ही नियुक्त हो सकते हैं। इन नीति को सरकार की अन्य शाखाओं जैसे सेना, पुलिस, न्यायपालिका और इंजीनियरिंग में भी लागू किया गया। कार्नवालिस की जगह गवर्नर-जनरल बन कर भारत आने वाले जान शोर के शब्दों में - अंग्रेजों के बुनियादी सिद्धांत सारे भारतीय राष्ट्र को हर संभव तौर पर अपने हितों और फायदों के लिए गुलाम बनाना था। भारतवासियों को हर सम्मान, प्रतिष्ठा या ओहदे से वंचित रखा गया है जिन्हें स्वीकार करने के लिए छोटे-से-छोटे अंग्रेज की भी चिरौरी की जा सकती है। अंग्रेजों ने ऐसी नीति का अनुसरण क्यों किया? इसके लिए अनेक कारक संयुक्त रूप से जिम्मेदार थे। सर्वप्रथम, उन्हें विश्वास था कि ब्रिटिश विचारों, संस्थानों और व्यवहारों पर आधारित कोई प्रशासन केवल अंग्रेज कार्यकर्ताओं द्वारा ही पूरी तरह स्थानीय किया जा सकता हैं और फिर भारतीय लोगों की योग्यता और ईमानदारी पर उनको भरोसा नहीं था। उदाहरण के लिए, चार्ल्स ग्रांट ने भारतीय जनता की निंदा करते हुए यह कहा कि वह “मनुष्यों की अत्यंत पतित और निकृष्ट नस्ल है जिसमें नैतिक जिम्मेदारी की नाममात्र की भावना रह गई है . . . और जो अपने दुर्गुणों के कारण विपन्नता में धंसी हुई हैं।” इसी तरह कार्नवालिस का विश्वास था कि “हिंदुस्तान का हर निवासी भ्रष्ट है।” उल्लेखनीय है कि यह आलोचना कुछ हद तक तत्कालीन भारतीय अफसरों और जमींदारों के एक छोटे वर्ग पर जरूर लागू होती थी। मगर यह आलोचना अगर नहीं तो समान रूप से भारत स्थित ब्रिटिश अफसरों पर भी लागू होती थी। वस्तुतः कार्नवालिस ने उन्हें ऊँचे वेतन देने का प्रस्ताव इसीलिए रखा था कि उन्हें प्रलोभन से दूर रखने में सहायता मिले और वे ईमानदार तथा आज्ञाकारी बन सकें। मगर उसने पर्याप्त वेतन का यह उपाय भारतीय अफसरों के बीच से भ्रष्टाचार हटाने के लिए लागू करने के बारे में कभी नहीं सोचा। वास्तव में, सेवाओं के उच्च वेतनमानों से भारतीयों को वंचित रखने की नीति जानबूझ कर अपनाई गई थी इन सेवाओं की जरूरत उस समय भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना करने तथा उसे मजबूत बनाने के लिए थी। जाहिर है कि यह काम भारतीयों पर नहीं छोड़ा जा सकता था जिसमें अंग्रेजों की तरह ब्रिटिश हितों के लिए न सहज सहानुभूति थी और न उनकी समझदारी। वस्तुतः इन नियुक्तियों को लेकर उनके बीच बहुत दिनों तक विवाद का विषय बना रहा। ऐसी स्थिति में अंग्रेज भारतवासियों को कैसे इन जगहों पर आने देते। मगर छोटे ओहदों के लिए भारतवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया क्योंकि वे अंग्रेजों की अपेक्षा कम वेतन पर तथा आसानी से उपलब्ध थे। भारतीय नागरिक सेवा (इंडियन सिविल सर्विस) धीरे-धीरे दुनिया की एक अत्यंत कुशल और शक्तिशाली सेवा के रूप में विकसित हो गई। उसके सदस्यों को काफी अधिकार थे और बहुधा वे नीति-निर्माण के कार्य में भाग लेते थे। उन्होंने आजादी, ईमानदारी और कठिन परिश्रम की कतिपय परंपराएँ विकसित कीं यद्यपि इन गुणों ने स्पष्टतया भारतीय हितों को नहीं बल्कि ब्रिटिश हितों को साधा। उनकों यह विश्वास हो गया कि भारत पर शासन करने करने का उन्हें लगभग दैवी अधिकार मिल गया है। भारतीय नागरिक सेवा (इंडियन सिविल सर्विस) को बहुधा ‘इस्पात का चौखटा’ कहा गया है जिसने भारत में ब्रिटिश शासन का पोषण किया और लंबी अवधि तक बनाए रखा कालक्रम से भारतीय जीवन में जो कुछ भी प्रगतिशील और उन्नत बातें थीं उनकी वह विरोधी बन गईं और इस प्रकार वह उदीयमान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के हमले का निशाना बनीं। सेनाभारत में ब्रिटिश राज के दूसरे महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में सेना थी। उसने तीन महत्वपूर्ण कार्य किए। वह भारतीय शक्तियों को जीतने के लिए औजार बनीं। उसने विदेशी प्रतिद्वन्दियों से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा की और सदा वर्तमान आंतरिक विद्रोह के खतरे से ब्रिटिश प्रभुसत्ता की रक्षा की और एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा का भी यह प्रमुख हथियार थी।कंपनी की अधिकांश सेना भारतीय सिपाहियों की थी जिन्हें मुख्य रूप से उन क्षेत्रों से भर्ती किया गया था जो अभी उत्तर प्रदेश और बिहार में हैं। उदाहरण के लिए, 1857 में भारत में कंपनी की फौज में 3,11,400 सैनिक थे जिनमें से 2,65,900 भारतीय थे। मगर उसके अफसर निश्चित रूप से कार्नवालिस के जमाने से केवल अंग्रेज होते थे। 1856 में सेना में केवल तीन ऐसे भारतीय थे जिनको 300 रुपए प्रति माह वेतन मिलता था और सबसे ऊँचा भारतीय अफसर एक सूबेदार था। बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों को काम पर लगाना पड़ता था क्योंकि ब्रिटिश सैनिक अपेक्षाकृत अधिक खर्चीले थे। इसके अलावा, ब्रिटेन की जनसंख्या इतनी कम थी कि वह शायद भारत को जीतने के लिए बड़ी संख्या में सैनिक नहीं दे सकती थी। संतुलन के लिए फौज के सारे अफसर अंग्रेज रखे जाते थे और भारतीय सैनिकों को नियंत्रण में रखने के लिए ब्रिटिश सैनिकों को एक निश्चित संख्या में रखा जाता था। आज इस पर बड़ा अचरज होता है कि मुट्ठी भर विदेशी ऐसी फौज के जरिए भारत को जीत और नियंत्रित कर सके, जिसमें भारतीयों का बहुमत था। ऐसा दो कारणों से संभव हुआ। एक ओर उस समय देश में आधुनिक राष्ट्रीयता का अभाव था। बिहार या अवध के किसी सैनिक ने न यह सोचा और न ही वह यह सोच सकता था कि मराठों या पंजाबियों को हराने में कंपनी की सहायता कर वह भारत विरोधी हो रहा है। दूसरी ओर, भारतीय सैनिक की यह बड़ी पुरानी परंपरा रही थी कि वह जिससे वेतन पाए उसकी निष्ठापूर्वक सेवा करे। इसे आम तौर से नमक हलाली कहा जाता था। दूसरे शब्दों में, भारतीय सैनिक भाड़े का एक बढ़िया सिपाही था और कंपनी एक अच्छा वेतनदाता थी। उसने अपने सैनिकों को नियमित रूप से और अच्छा वेतन दिया। यह एक ऐसी चीज थी जो भारतीय शासक और सरदार उस समय नहीं कर रहे थे। पुलिसपुलिस ब्रिटिश शासन का तीसरा स्तम्भ थी। उसका सृजन करने वाला भी कार्नवालिस ही था। उसने जमींदारों को पुलिस कार्यों से मुक्त कर दिया और कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक नियमित पुलिस दल की स्थापना की। इसके लिए उसने थानों की पुरानी भारतीय व्यवस्था को लिया और उसे आधुनिक बनाया। दिलचस्प बात यह है कि पुलिस व्यवस्था के मामले में भारत ब्रिटेन से आगे हो गया। उस समय तक ब्रिटेन में पुलिस व्यवस्था विकसित नहीं हुई थी। कार्नवालिस ने थानों की व्यवस्था स्थापित की। हर थाने का प्रधान दरोगा होता था। दरोगा भारतीय होता था। बाद में, पुलिस के जिला सुपरिटेंडेंट (अधीक्षक) का पद बनाया गया। सुपरिटेंडेंट जिले में पुलिस संगठन का प्रधान हो गया। पुलिस में भी भारतीयों को सभी ऊँचे ओहदों से अलग रखा गया। गाँवों में पुलिस की जिम्मेदारियों को चौकीदार निभाते थे जिनका भरण-पोशण गाँव वाले करते थे। पुलिस धीरे-धीरे डकैती जैसे प्रमुख अपराधों को कम करने में सफल हो गई। पुलिस ने विदेशी नियंत्रण के विरूद्ध बड़े पैमाने पर षड्यंत्रों को भी रोका और जब राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ तब पुलिस का इस्तेमाल उसे दबाने के लिए किया गया। लोगों के साथ व्यवहार में भारतीय पुलिस ने असहानुभूतिपूर्ण रूख अपनाया। संसद की एक समिति ने 1813 की अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि “पुलिस ने शांतिप्रिय निवासियों को उसी तरह लूटा-मारा जैसे डकैत करते थे जबकि डकैतों को दबाने के लिए उसका आयोजन किया गया था” और गवर्नर-जनरल बैंटिक ने 1832 में लिखा -जहाँ तक पुलिस का सवाल है, वह जनता का रक्षक होने की स्थिति से कोसों दूर है। इस संबंध में जनता की भावना को बिना निम्नलिखित तथ्य का सहारा लिए मैं अच्छी तरह नहीं रख सकता। हाल के एक रेगुलेशन से बढ़कर कुछ भी अधिक लोकप्रिय नहीं हो सकता। इस रेगुलेशन के अनुसार अगर कोई डकैती हुई हो तो पुलिस को तब तक जाँच करने की मनाही है जब तक लुटे गए व्यक्ति उसे नहीं बुलाएँ - कहने का मतलब यह है कि गड़ेरिया भेड़िए से बड़ा भुक्खड़ हिंसक पशु है। न्यायिक संगठनदीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्ज ने आरंभ किया मगर कार्नवालिस ने 1793 में इसे और सुदृढ़ बनाया। हर जिले में एक दीवानी अदालत कायम की गई जिसका प्रमुख जिला जज होता था जो नागरिक सेवा का सदस्य होता था। इस तरह कार्नवालिस ने दीवानी जज और कलेक्टर के ओहदों को अलग-अलग कर दिया। जिला अदालत के फैसलों के खिलाफ अपील पहले दीवानी अपील की चार प्रांतीय अदालतों में हो सकती थी। अपील की आखिरी सुनवाई सदर दीवानी अदालत ही कर सकती थी। जिला अदालत के नीचे रजिस्ट्रार की अदालतें थी जिनके प्रधान यूरोपवासी होते थे और अनेक छोटी अदालतें थीं जिनके प्रधान भारतीय जज होते थे जिन्हें मुंसिफ और अमीन कहा जाता था। फौजदारी मुकदमों का निबटारा करने के लिए कार्नवालिस ने बंगाल प्रेसिडेंसी को चार डिवीजनों में बाँट दिया। उसने उनमें से हर एक में एक क्षेत्रीय न्यायालय (कोर्ट आफ सर्किट) स्थापित किया जिनके प्रधान नागरिक सेवा के लोग होते थे। इन अदालतों के नीचे छोटे-छोटे मुकदमों को फैसला करने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय मजिस्ट्रेट होते थे। क्षेत्रीय न्यायालय (कोर्ट्स आाफ सर्किट) के फैसलों के खिलाफ सदर निजामत अदालत में अपील की जा सकती थी। फौजदारी अदालतों ने मुस्लिम फौजदारी कानून को संशोधित किया और कम सख्त रूप में उनको लागू किया जिससे शरीर के अंगों को काटने या इस प्रकार की अन्य सजाएँ देने की मनाही कर दी। दीवानी अदालतों ने उस पारंपरिक कानून को लागू किया जो किसी क्षेत्र या जनता के किसी हिस्से के बीच बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा था। विलियम बैंटिक ने 1831 में अपील कर प्रांतीय अदालतों तथा क्षेत्रीय न्यायालय को खत्म कर दिया। उनका काम पहले कमीशनों और बाद में जिला जजों और जिला कलेक्टरों को सौंप दिया गया। बैंटिक न न्यायायिक सेवा में काम करने वाले भारतीयों के दरजे और अख्तियार बढ़ा दिए। उसने भारतीयों को डिप्टी मजिस्ट्रेट सबार्डिनेट जज और प्रिंसिपल सदर अमीन नियुक्त किए। सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत की जगह 1865 में कलकत्ता, मद्रास और बंबई में उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) स्थापित किए गए।अधिनियम (enactment) तथा पुराने कानूनों को संहिताबद्ध (codification) करने की प्रक्रियाओं के द्वारा अंग्रेजों ने कानूनों की एक नई प्रणाली स्थापित की। भारत में न्याय की परंपरागत प्रणाली मुख्य रूप से प्रचलित कानून पर आधारित थी जो लंबी परंपरा और रिवाज से निकली थी यद्यपि अनेक कानून शास्त्रों और शरियत तथा शाही फरमानों पर आधारित थे। हालाँकि अंग्रेज आम तौर से प्रचलित कानून को लागू करते रहे, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने कानूनों की एक नई प्रणाली विकसित की। उन्होंने रेगुलेशन लागू किए, तत्कालीन कानूनों को संहिताबद्ध किया और उन्हें बहुधा न्यायिक व्याख्याओं के द्वारा सुव्यवस्थित करके आधुनिक बनाया। 1833 के चार्टर एक्ट के कानून बनाने के सारे अख्तियार कौंसिल की सहमति से गवर्नर-जनरल को दे दिए। इस सबका मतलब था कि अब भारतीय उत्तरोत्तर मानव-निर्मित कानूनों के तहत रहेंगे जो अच्छे-बुरे कुछ भी हो सकते हैं। मगर वे स्पष्ट रूप से मानवीय तर्क की उपज थे। दूसरे शब्दों में, लोग उन कानूनों के तहत नहीं रहेंगे जिनका आँख मूँद कर पालन करना पड़ता था और उनके औचित्य पर इसलिए उंगली नहीं उठाई जाती थी क्योंकि वे दैवी और इसीलिए पवित्र माने जाते थे। सरकार ने 1833 में लार्ड मैकाले के नेतृत्व में भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग, (Law Commission) नियुक्त किया। उसके परिश्रम के फलस्वरूप भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) पश्चिमी देशों में लाई गई दीवानी प्रक्रिया और दंड प्रक्रिया संहिताएँ और कानून की अन्य संहिताएँ आईं। अब सारे देश में एक ही प्रकार के कानून लागू हो गए और उन्हें न्यायालयों की समरूप प्रणाली के जरिए लागू किया गया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत को न्यायिक रूप से एक सूत्रबद्ध किया गया। कानून का शासनअंग्रेजों ने कानून के शासन या विधि-शासन (Rule of Law) की आधुनिक अवधारणा को लागू किया। इसका तात्पर्य था कि उनका प्रशासन कम से कम सैद्धान्तिक रूप में कानूनों के अनुसार चलाया जाएगा, न कि शासक की सनक या वैयक्तिक इच्छा के अनुसार। कानूनों ने प्रजा के अधिकारों, विशेषाधिकारों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था। बेशक, व्यवहार में अफसरशाही और पुलिस को मनमाने अख्तियार थे और उन्होंने जनता के अधिकारों और स्वतंत्रताओं में हस्तक्षेप किया। कानून का शासन कुछ हद तक व्यक्ति की वैयक्तिक स्वतंत्रता की गारंटी था। यह सही है कि भारत के पिछले शासक आम तौर से रीति-रिवाज से बँधे होते थे, मगर उन्हें अपनी इच्छानुसार कोई भी प्रशासनिक कदम उठाने का कानूनी अधिकार था और उनसे बड़ी कोई ऐसी सत्ता नहीं थी जिसके सामने उनकी कारर्वाइयों को चुनौती दी जा सके। कभी-कभी भारतीय शासकों और सरदारों ने अपनी इच्छानुसार इस शक्ति का प्रयोग किया। दूसरी ओर, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत प्रशासन मुख्य रूप से कानूनों के आधार पर न्यायालयों द्वारा उनकी की गई व्याख्या के अनुसार चलाया जाता था। कानून बहुधा त्रुटिपूर्ण होते थे। कानून जनता द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा नहीं बल्कि विदेशी शासकों द्वारा निरंकुश तरीकों से बनाए जाते थे। कानून सरकारी कर्मचारियों तथा पुलिस के हाथों में काफी अख्तियार दे देते थे। मगर शायद एक विदेशी राज के अंतर्गत यह अवर्श्यभावी था। विदेशी राज स्वभावतः लोकतांत्रिक या स्वतंत्रतावादी नहीं हो सकता।कानून के सम्मुख समानताअंग्रेजी राज के दौरान भारतीय विधिप्रणाली कानून के सम्मुख समानता की अवधारणा पर आधारित थी। इसका मतलब था कि कानून की निगाहों में सारे मनुष्य बराबर हैं। जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के एक ही कानून सब लोगों पर लागू होता था। पहले न्यायप्रणाली जाति के भेदभावों का ख्याल करती थी और तथाकथित उच्च जाति और निम्न जाति के बीच भेदभाव करती थी। एक ही अपराध के लिए एक गैर-ब्राह्मण की अपेक्षा एक ब्राह्मण को हल्का दंड दिया जाता था। इसी प्रकार जमींदारों और सामंतों को वास्तविक रूप से उतना कड़ा दंड दिया जाता था जितना एक आम आदमी को। वस्तुतः उनके खिलाफ उनकी कार्यवाहियों के लिए अक्सर मुकदमा नहीं चलाया जाता था। अब दीन-हीन लोग भी न्यायालय में जा सकते थे।मगर कानून के सम्मुख समानता के इस उत्कृष्ट सिद्धांत का एक अपवाद भी था। वह यह कि यूरोपवासियों और उनके वंशजों के लिए अलग-अलग अदालत और यहाँ तक कि अलग कानून भी थे। उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमों की सुनवाई केवल यूरोपीय जज ही कर सकते थे। अनेक अंग्रेज अधिकारियों, सैनिक अधिकारियों, बागान मालिकों और सौदागरों ने भारतीय लोगों के साथ अंहकारी, निष्ठुर और यहाँ तक क्रूर व्यवहार किया लेकिन जब उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के प्रयास हुए तब उन्हें अप्रत्यक्ष और अनुचित संरक्षण दिया गया और फलस्वरूप मुकदमों की सुनवाई करने वाले अनेक यूरोपीय जजों ने उन्हें हल्की सजा दी या ऐसे ही रिहा कर दिया जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है,उनके खिलाफ मुकदमों की सुनवाई केवल यूरोपीय जज ही कर सकते थे। फलस्वरूप प्रायः न्याय की हत्या होती थी। व्यवहार में एक अन्य प्रकार की कानूनी समानता उभर कर आई। न्याय काफी महँगा हो गया क्योंकि कोर्ट फीस का भुगतान करना पड़ता था, वकील करने पड़ते थे और गवाहों के खर्च को पूरा करना होता था। आम तौर से कचहरियाँ दूर शहरों में होती थीं। मुकदमें वर्षो तक चलते थे। जटिल कानून अशिक्षित और गैर-जानकार किसानों की समझदारी से बाहर थे। निरपवाद रूप से धनी लोग कानूनों और कचहरियों को अपने पक्ष में मोड़ सकते थे। किसी गरीब आदमी को निचली अदालत से अपील सुनने वाली सबसे बड़ी अदालत तक न्याय की लंबी प्रक्रिया में ले जाने और फलस्वरूप उसे पूरी तरह बर्बाद करने की धमकी ही उसे घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देती थी। इसके अलावा पुलिस तथा शेष प्रशासकीय तंत्र के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार न्याय नहीं मिलने देता था। अधिकारी बहुधा धनी लोगों का पक्ष लेते थे। बिना सरकारी कार्यवाही से डरे जमींदार रैयतों पर अत्याचार करते थे। इसके विपरीत, अंग्रेजी राज्य के पहले जो न्याय प्रणाली थी वह अपेक्षाकृत अनौपचारिक, शीघ्र और कम-खर्चीली थी। इस प्रकार यद्यपि नई न्याय-प्रणाली उस हद तक प्रगतिशील थी जिस हद तक वह कानून के शासन और कानून के सम्मुख समानता के प्रशासकीय सिद्धान्तों तथा विवेकपूर्ण और मानवोचित मानव निर्मित कानूनों पर आधारित थी, तथापि वह कुछ अन्य दृष्टियों से बहुत खराब थी। उदाहरण के लिए, वह अब अधिक खर्चीली हो गई थी और लोगों को न्याय पाने में काफी विलंब होता था। सामाजिक और सांस्कृतिक नीतिहम देख चुके है कि ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन और विनियमन ब्रिटिश व्यापार और उद्योग के हितों में किया और व्यवस्था और सुरक्षा की गारंटी के लिए एक आधुनिक प्रशासन व्यवस्था की स्थापना की। 1813 तक अंग्रेजों ने देश के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में गैर-हस्तक्षेप की नीति अपनाई, मगर 1813 के बाद उन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति के रूपांतरण के लिए संक्रिय कदम उठाए। इसके पहले उन्नीसवीं सदी के दौरान ब्रिटेन में नए हितों और नए विचारों का उदय हुआ था। औद्योगिक क्रांति अठारहवीं सदी के मध्य में आरंभ हुई थी जिसके फलस्वरूप औद्योगिक पूँजीवाद का विकास ब्रिटिश समाज के सभी पहलुओं को तेजी से बदल रहा है। उदीयमान औद्योगिक हितों ने भारत को अपनी वस्तुओं के लिए बड़े बाजार के रूप में बदलना चाहा। ऐसा केवल शांति बनाए रखने की नीति के जरिए नहीं हो सकता था बल्कि भारतीय समाज के आंशिक रूपांतरण और आधुनिकीकरण की आवश्यकता थी और इस प्रकार, इतिहासकारों थाम्पसन और गैर्रेट के शब्दों में, “पुरानी बटमारी की मनोदशा और तरीके आधुनिक उद्योगवाद तथा पूँजीवाद की मनोदशा तथा तरीके में बदल गए।”विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने भी मानवीय प्रगति की नई प्रत्याशाएँ उत्पन्न कर दीं। अठारहवीं और उन्नीसवीं सदियों दौरान ब्रिटेन तथा यूरोप में नए विचारों का एक नया ज्वार देखा गया जिसने भारतीय समस्याओं के प्रति ब्रिटिश दृष्टिकोण को प्रभावित किया। सारे यूरोप में ‘‘सोच-विचार, तौर-तरीकों और नैतिकता के नए दृष्टिकाण सामने आ रहे थे।“ 1789 की महान फ्रांसीसी क्रांति ने अपने स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के संदेश द्वारा शक्तिशाली जनतांत्रिक भावनाएँ उत्पन्न कीं और आधुनिक राष्ट्रीयता की शक्ति को फैलाया। नई प्रवृति का चिंतन के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व बेकन, लाक, वाल्तेयर, रूसो, कांट-ऐडम स्मिथ और बेंथम और साहित्य के क्षेत्र में वर्ड्सवर्थ, बायरन, शैली और चार्ल्स डिकेंस ने किया। नया चिंतन अठारहवीं शताब्दी की बौद्धिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न हुआ था स्वभावतया इस नए चिंतन का प्रभाव भारत में महसूस किया गया तथा उसने सरकार की शासकीय धारणाओं को भी कुछ हद तक प्रभावित किया। नए चिंतन की तीन मुख्य विशेषताएँ थीं - विवेकशीलता या तर्क और विज्ञान में विश्वास मानवतावाद या मनुष्य के प्रति प्रेम, मानव की प्रगति करने की क्षमता में आस्था विवेकशील और वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस बात का सूचक था कि केवल वही चीज सही मानी जाएगी जो मानव तर्क के अनुकूल हो और व्यवहार में जिसकी परीक्षा की जा सके। सत्रहवीं, अठारहवीं और उन्नीसवीं सदियों की वैज्ञानिक प्रगति तथा उद्योग में विज्ञान के प्रयोग से प्राप्त उत्पादन की विशाल शक्तियाँ मानवीय तर्कशक्ति का प्रकट प्रमाण थीं। मानवतावाद इस धारणा पर आधारित था कि प्रत्येक मानव प्राणी अपने आप ही साध्य है और इसी रूप में उसका सम्मान किया जाना चाहिए और उसे महत्व दिया जाना चाहिए। किसी भी मनुष्य को यह अधिकार नहीं हो सकता कि वह दूसरे मनुष्य को अपने सुख का माध्यम समझे। मानवतावादी दृष्टिकोण ने व्यक्तिवाद, उदारतावाद और समाजवाद के सिद्धान्तों को जन्म दिया। प्रगति के सिद्धान्त के अनुसार सभी समाजों को समय के साथ अवश्य बदलना होता है। कोई भी चीज न जड़ थी और न जड़ हो सकती है। इसके अलावा मनुष्य में प्रकृति और समाज को विवेकशील तथा उचित रूपरेखा के अनुसार फिर से ढालने की क्षमता है। यूरोप में चिंतन की नई लहरों का पुराने दृष्टिकोण से टकराव हुआ। भारत संबंधी नीति निर्धारित करने वालों तथा भारतीय प्रशासन चलाने वालों के बीच दृष्टिकोण में संघर्ष हुआ। पुराने दृष्टिकोण को रूढ़िवादी या परंपरागत दृष्टिकोण कहा जाता था। यह दृष्टिकोण भारत में यथासंभव कम से कम परिवर्तन करने का पक्षपाती था। इस दृष्टिकोण के शुरू के काल में प्रतिनिधि वारेन हेस्टिंग्स और प्रसिद्ध लेखक तथा सांसद एडमंड वर्क थे और बाद के प्रतिनिधि प्रसिद्ध अफसर मुनरो, मैलक, एल्फिस्टन और मेटकाफ थे। रूढ़िवादियों का कहना था कि भारतीय सभ्यता यूरोपीय सभ्यता से भिन्न थी मगर अवर्श्यभावी रूप से उससे निकृष्ट नहीं थी। उनमें से अनेक भारतीय दर्शन और संस्कृति की इज्जत और प्रशंसा करते थे। यह महसूस करते हुए कि कुछ पश्चिमी विचारों और रिवाजों को लागू करना जरूरी हो सकता है उन्होंने प्रस्ताव किया कि उन्हें बहुत सावधानीपूर्वक और धीरे-धीरे लागू किया जाए। सामाजिक स्थिरता को सर्वोपरि रखते हुए, उन्होंने तेज बदलाव के किसी भी कार्यक्रम का विरोध किया। उन्होंने महसूस किया कि व्यापक या जल्दबाजी में किए गए परिवर्तन देश में तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न करेंगे। इंग्लैंड और ब्रिटिश शासन के बिल्कुल अंत तक भारत में रूढ़िवादी दृष्टिकोण प्रभावशाली बना रहा। वस्तुतः भारत में ब्रिटिश अफसरों का बहुमत आम तौर से रूढ़िवादी दृष्टिकोण वाला था। रूढ़िवादी दृष्टिकोण की जगह पर 1800 तक बड़ी तेजी से नया दृष्टिकोण आने लगा था जो भारतीय समाज और संस्कृति का कटु आलोचक था। भारतीय सभ्यता को गतिहीन कहकर उसकी निंदा की गई और उसे घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा। भारतीय रीति-रिवाजों को असभ्यता का प्रतीक माना गया, भारतीय संस्थानों को भ्रष्ट और पतनोन्मुख बतलाया गया तथा भारतीय चिंतन को संकीर्ण और अवैज्ञानिक कहा गया। ब्रिटेन के अधिकांश अफसरों और लेखकों तथा राजनेताओं ने इस आलोचनात्मक दृष्टि का प्रयोग भारत की राजनीतिक और आर्थिक दासता को उचित बतलाने तथा यह घोषित करने के लिए किया कि वह उन्नति करने योग्य नहीं है और इसलिए उसे स्थायी रूप से ब्रिटिश संरक्षण में रहना चाहिए। मगर थोड़े से अंग्रेज जिन्हें ‘रेडिकल्स’ (Radicals) कहा जाता था संकुचित आलोचना और साम्राज्यवादी दृष्टिकोण की सीमा से बाहर गए उन्होंने विकसित मानवतावादी और विवेकशील चिंतन को भारतीय स्थिति पर लागू करने का प्रयत्न किया। विवेक बुद्धि के सिद्धांत के फलस्वरूप उनकी धारणा थी कि यह आवश्यक नहीं है कि भारत हमेशा पतित बना रहे क्योंकि विवेक, बुद्धि और विज्ञान के रास्ते चलकर सभी समाजों में उन्नति करने की क्षमता है और इस प्रकार ब्रिटिश समाज के श्रेष्ठतर तत्वों का प्रतिनिधित्व करने वाले ‘रेडिकल्स’ ने भारत को विज्ञान तथा मानवतावाद के आधुनिक प्रगतिशील संसार का भाग बनाना चाहा। उनके अनुसार आधुनिक पाश्चात्य विज्ञान, दर्शन और साहित्य को अपनाकर वस्तुतः व्यापक और नए तरीके से परिवर्तन के जरिए भारत की कुरीतियों का निराकरण हो सकता है। उन्नीसवीं सदी के तीसरे दशक में भारत आने वाले कुछ अफसर भी रेडिकल दृष्टिकोण से गंभीर रूप से प्रभावित थे। यही नहीं, 1830 के बाद इंग्लैण्ड में सुधारक व्हिग सत्तारूढ़ थे। मगर यहाँ पर इस बात पर बल देने की जरूरत है कि ऐसे ईमानदार और लोकहितैषी अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी और ब्रिटिश प्रशासन पर उनका प्रभाव कभी निर्णायक नहीं रहा। ब्रिटिश भारत के प्रशासन में शासक तत्व साम्राज्यवादी और शोषक बने रहे। वे नए विचारों को तभी ग्रहण करते और सुधारवादी उपायों को तभी और उसी हद तक लागू करते थे, जब व्यापारिक हितों और मुनाफे की प्रवृत्तियों से वे नहीं टकराते थे। भारत का आधुनिकीकरण उस हद तक ही हो सकता था जिससे कि अपेक्षाकृत आसानी से और पूरे तौर पर ब्रिटिश भारत के संसाधनों का अपने हित में शोषण कर सकें। इस प्रकार भारत के आधुनिकीकरण को अनेक अंग्रेज अधिकारियों, व्यवसायियों और राजनेताओं ने स्वीकार कर लिया था क्योंकि हिंदुस्तानियों को ब्रिटिश वस्तुओं का बेहतर ग्राहक बनाना था तथा उन्हें विदेशी शासन स्वीकार करने के लिए तैयार करना था। जैसा कि उन्होंने ब्रिटेन में किया उस तरह जनतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए प्रयास करने के बदले उन्होंने भारत में एक अपेक्षाकृत अधिक सत्तावादी शासन की माँग की जिसे उन्होंने पितृ सत्तावादी कहा इस दृष्टि से वे रूढ़िवादियों के साथ थे। रूढ़िवादी भी पितृसत्तावाद के कट्टर हिमायती थे जिसके अंतर्गत भारतीय जनता के साथ बच्चों जैसा व्यवहार किया जाएगा और उन्हें प्रशासन से अलग रखा जाएगा। भारत स्थित ब्रिटिश प्रशासकों की मूल दुविधा यही थी कि कुछ सीमा तक आधुनिकीकरण के बिना भारत में ब्रिटिश हितों को नहीं साधा जा सकता था परंतु पूर्ण आधुनिकीकरण ऐसी शक्तियों को जन्म देता जो उनके हितों के विरूद्ध जाती और काफी आगे चलकर देश में ब्रिटिश प्रभुत्व के लिए खतरे पैदा कर देतीं। इसलिए, उन्हें आंशिक आधुनिकीकरण की अत्यंत सावधानी से संतुलित नीति अपनानी पड़ी। इस नीति का मतलब था - कुछ छेत्रों में आधुनिकीकरण करना और अन्य क्षेत्रों में उसके रास्ते में रोड़े अटकाना या उसे नहीं होने देना। दूसरे शब्दों में, आधुनिकीकरण को भी उपनिवेशवादी सीमा के भीतर रहना था। भारतीय समाज और संस्कृति के आधुनिकीकरण की नीति को ही ईसाई धर्म प्रचारकों तथा विलियम विल्बर-फोर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स ग्रांट जैसे धर्मपरायण लोगों ने बढ़ावा दिया, जो चाहते थे कि भारत में ईसाई धर्म फैले। उन्होंने भी भारतीय समाज के प्रति आलोचनात्मक रूख अपनाया मगर उन्होंने धार्मिक आधार पर ऐसा किया। उनका उत्कट विश्वास था कि ईसाई धर्म ही एकमात्र सच्चा धर्म है और अन्य सारे धर्म झूठे हैं। उन्होंने पश्चिमीकरण के एक कार्यक्रम को इस उम्मीद से समर्थन दिया कि उसके परिणामस्वरूप अंततोगत्वा देश ईसाई धर्म को अपना लेगा। उन्होंने सोचा कि पाश्चात्य ज्ञान की रोशनी अपने धर्मों में लोगों के विश्वास को खत्म कर देगी और उन्हें ईसाई धर्म का स्वागत करने तथा उसे अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। इसलिए उन्होंने देश में आधुनिक स्कूल, कॉलेज और अस्पताल खोले। मगर धर्मप्रचारकों को विवेकशील ‘रेडिकल्स’ का बहुधा अनचाहे सहायक होना पड़ता था। ‘रेडिकल्स’ का वैज्ञानिक दृष्टिकोण न केवल हिंदू या मुस्लिम पौराणिक गाथाओं की बल्कि ईसाई पौराणिक गाथाओं की भी जड़ें खोदता था। जैसा कि प्रोफेसर एच.एच. डाडवेल ने बतलाया है - “अपने ही देवताओं की मान्यता पर शंका प्रकट करने की शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने (पाश्चात्य प्रभाव में आए भारतीयों ने) बाइबल की प्रमाणिकता और उसके वृत्तांत की सच्चाई पर भी संदेह व्यक्त किया।” धर्मप्रचारकों ने पितृसत्तावादी साम्राज्यवादी नीतियों का भी समर्थन किया क्योंकि वे कानून तथा व्यवस्था और ब्रिटिश प्रभुत्व को अपने धार्मिक प्रचार के काम के लिए आवश्यक समझते थे। यह आशा दिलाकर कि ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले ब्रिटिश वस्तुओं के अच्छे ग्राहक होंगे, उन्हांने ब्रिटिश सौदागरों और विनिर्माताओं से उनका समर्थन प्राप्त करना चाहा। ‘रेडिकल्स’ को राजा राममोहन राय और उसी तरह के अन्य भारतीयों ने अपना पूर्ण समर्थन दिया। ऐसे भारतीय इस तथ्य के प्रति सचेत थे कि उनका देश और समाज काफी नीचे गिर गया है। वे जाति संबंधी पूर्वाग्रहों तथा अन्य सामाजिक कुरीतियों से ऊब गए थे और उनका विश्वास था कि भारत की मुक्ति विज्ञान और मानवतावाद के द्वारा ही हो सकती है। हम इन भारतीयों के दृष्टिकोण और गतिविधियों के बारे में अगले अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत सरकार ने व्यापक रूप से आधुनिकीकरण के बदले सावधानी और धीमी गति से नए परिवर्तन लाने की जो नीति अपनाई उसके लिए जिम्मेदार अन्य कारणों में भारत स्थित ब्रिटिश अधिकारियों में रूढ़िवादी दृष्टिकोण का बोलबाला और यह धारणा थी कि भारतीयों के धार्मिक ख्यालों तथा सामाजिक रिवाजों में हस्तक्षेप करने से भारतीय जनता के बीच क्रांतिकारी प्रतिक्रिया हो सकती है। यहाँ तक कि अत्यंत कट्टर ‘रेडिकल्स’ ने भी इस चेतावनी की ओर ध्यान दिया क्योंकि ब्रिटिश शासक वर्ग के अन्य सदस्यों के साथ उन्होंने भी भारत में ब्रिटिश शासन की सुरक्षा और स्थायित्व की कामना की, जिसके सामने हर अन्य विचार का महत्व गौण था। वस्तुतः आधुनिकीकरण की नीति को 1858 के बाद धीरे-धीरे छोड़ दिया गया क्योंकि भारतीय योग्य शिष्य सिद्ध हुए और वे अपने समाज के आधुनिकीकरण तथा अपनी संस्कृति पर जोर देने की दिशा में बढ़े। उन्होंने माँग की कि उन पर स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रीयता के आधुनिक सिद्धान्त के अनुसार शासन किया जाए। ब्रिटिश लोगों ने सुधारकों को अपना समर्थन देना क्रमशः बंद कर दिया। धीरे-धीरे उन्होंने समाज के कट्टरपंथियों का पक्ष लेना शुरू किया। उन्होंने जातिवाद तथा सांप्रदायिकता को भी बढ़ावा दिया। लोकोपकारी कार्रवाइयाँभारतीय समाज को उसकी कुरीतियों से मुक्त करने के लिए किए गए ब्रिटिश सरकार के प्रयास कुल मिलाकर बहुत कम थे और इसलिए उनका कुछ विशेष परिणाम नहीं हुआ। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी 1829 में सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित करने की कार्यवाई। विलियम बैंटिक ने घोषित किया कि पति की चिता पर विधवा के जल मरने की कार्यवाई में जो भी सहयोगी होंगे उन्हें अपराधी माना जाएगा। इससे पहले ब्रिटिश शासकों ने सतीप्रथा को रोकने के प्रश्न पर उदासीन रूख अपनाया था। उन्हें डर था कि सती प्रथा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से रूढ़िवादी भारतीय नाराज हो जाएँगे। जब राममोहन राय और अन्य प्रबुद्ध भारतीयों तथा धर्मप्रचारकों ने इस अमानवीय प्रथा को खत्म करने के लगातार आंदोलन किए तब जाकर सरकार सती प्रथा को रोकने के लोकोपकारी कदम उठाने के लिए सहमत हुई। भूतकाल में अकबर और औरंगजेब, पेशवाओं और जयपुर के राजा जयसिंह ने इस कुप्रथा को दबाने के लिए प्रयास किए लेकिन वे असफल रहे। कुछ भी हो, इस प्रथा को गैरकानूनी घोषित करने के लिए बैंटिक प्रशंसा का पात्र है। इस कुप्रथा के कारण 1815 और 1818 के बीच केवल बंगाल में ही 800 महिला ने अपनी जान गँवाई थी। बैंटिक इसलिए भी प्रशंसा का पात्र है कि उसने सती प्रथा के रूढ़िवादी समर्थकों के विरोध के सामने झुकने से इनकार कर दिया।पैदा होते ही लड़कियों को मार देने की प्रथा कुछ राजपूत खानदानों तथा अन्य जातियों में प्रचलित थी। इसके मुख्य कारण थे लड़ाइयों में बड़ी संख्या में मरने के कारण नौजवानों की कमी तथा ऊसर क्षेत्रों में जीविकोपर्जन में कठिनाइयाँ। यह प्रथा पश्चिम और मध्य भारत में दहेज की कुप्रथा के भंयकर रूप में विद्यमान होने के कारण प्रचलित थी। शिशु हत्या को रोकने के संबंध में कानून 1795 और 1802 में बनाए गए थे मगर उन्हें सख्ती से बैंटिक और हार्डिंग ने ही लागू किया। हार्डिंग ने नर बलि की प्रथा को खत्म करने के लिए भी कानून बनाया। यह प्रथा गांड नाम की आदिम जाति में प्रचलित थी। भारत सरकार ने 1856 में हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए कानून पास किया। सरकार ने पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर और अन्य सुधारकों द्वारा इसके पक्ष में लगातार आंदोलन चलाने के बाद यह कार्यवाई की । इस कानून के तात्कालिक प्रभाव कुछ विशेष नहीं हुए। इन सब सरकारी सुधारों ने भारतीय समाजव्यवस्था को सतही तौर पर ही प्रभावित किया तथा जनता के विशाल बहुमत के जीवन पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। शायद एक विदेशी सरकार के लिए इससे अधिक कुछ करना संभव भी नहीं था। आधुनिक शिक्षा का प्रसारअंग्रेज आधुनिक शिक्षा आरंभ करने में अधिक सफल रहे। निःसंदेह आधुनिक शिक्षा का प्रसार केवल सरकार के प्रयास से ही नहीं हुआ। ईसाई धर्मप्रचारकों और बड़ी संख्या में प्रबुद्ध भारतीयों ने भी इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।अपने शासन के पहले 60 वर्षों के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रजा की शिक्षा में नाममात्र दिलचस्पी ली। वह मुनाफा कमाने वाली एक व्यापारिक संस्था रही, परंतु इसके दो बहुत ही छोटे अपवाद रहे। वारेन हेस्टिंग्ज ने 1781 में मुस्लिम कानून और संबद्ध विषयों के अध्ययन और पढ़ाई के लिए कलकत्ता मदरसा कायम किया। जोनाथन डंकन ने 1791 में हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए वाराणसी में संस्कृत कॉलेज स्थापित किया। वह वाराणसी मे रेजिडेंट था। दोनों संस्थाओं की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि उनसे कंपनी की अदालतों में न्याय-प्रशासन के लिए योग्य भारतीय नियमित रूप से मिल सकें। धर्मप्रचारकों और उनके समर्थकों तथा अनेक लोकोपकारी व्यक्तियों ने कंपनी पर तुरंत दबाव डालना आरंभ किया कि वह भारत में आधुनिक धर्मनिरपेक्ष पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दे। यद्यपि अनेक भारतीयों सहित समाजसेवी लोगों की धारणा थी कि आधुनिक ज्ञान ही देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कुरीतियों की सर्वोत्तम दवा है, लेकिन धर्मप्रचारकों को विश्वास था कि आधुनिक शिक्षा अपने धर्मों में लोगों की आस्था को खत्म कर देगी और वे ईसाई धर्म ग्रहण करने के लिए प्रेरित होंगे। एक मामूली सी शुरुआत 1813 में की गई जब चार्टर ऐक्ट में विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा देश में आधुनिक विज्ञानों के ज्ञान को प्रोत्साहित करने का सिद्धांत शामिल कर लिया गया। ऐक्ट ने कंपनी को इस उद्देश्य के लिए एक लाख रुपए खर्च करने का निर्देश दिया। मगर 1833 तक कंपनी के अधिकारियों ने इस काम के लिए यह तुच्छ रकम भी नहीं दी। वर्षों तक देश में इस प्रश्न को लेकर काफी वादविवाद चलता रहा कि यह खर्च किस दिशा में किया जाए। कुछ लोगों का कहना था कि यह रकम केवल आधुनिक पाश्चात्य अध्ययनों कों प्रोत्साहन देने के लिए खर्च की जाए, अन्य लोंगों की इच्छा थी कि पाश्चात्य विज्ञान और साहित्य की पढ़ाई छात्रों को नौकरियों के लिए तैयार करने के लिए दी जाएँ, मगर मुख्य जोर परंपरागत भारतीय विद्या के प्रसार पर दिया जाए। जो लोग पाश्चात्य विद्या का प्रसार चाहते थे, उनके बीच इस मुद्दे पर विवाद खड़ा हो गया कि आधुनिक स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा का कौन सा माध्यम अपनाया जाए। कुछ लोगों ने भाषाओं (जिन्हें उस समय Vernaculars कहा जाता था) के प्रयोग की सिफारिश की जबकि अन्य लोगों ने अंग्रेजी के इस्तेमाल की वकालत की। दुर्भाग्यवश, इस प्रश्न को लेकर काफी उलझन पैदा हो गई। अनेक लोग माध्यम के रूप में अंग्रेजी तथा अध्ययन के विषय में अंग्रेजी के बीच, तथा माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं और अध्ययन की मुख्य विषयवस्तु के रूप में परंपरागत भारतीय विद्या के बीच भेद नहीं कर पाए। दोनों विवाद 1835 में तब खत्म हुए, जब भारत सरकार ने निर्णय किया कि जो भी सीमित संसाधन वह देने को तैयार है, उसे वह पाश्चात्य विज्ञान तथा पाश्चात्य साहित्य को केवल अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पढ़ाने के लिए लगाएगी। लार्ड मैकाले उस उसय गवर्नर-जनरल की कौंसिल का विधि सदस्य था, उसने एक प्रसिद्ध आलोकपात्र (minute) में वह तर्क दिया कि भारतीय भाषाएँ इतनी विकसित नहीं हैं कि इस उद्देश्य को पूरा कर सकें और “प्राच्य विद्या यूरोपीय विद्या से बिल्कुल निकृष्ट है।” यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि मैकाले के विचार विज्ञान तथा चिंतन के क्षेत्रों में भारत की भूतकालीन उपलब्धियों के प्रति पूर्वाग्रह तथा अज्ञान से भरे हुए थे, फिर भी उसका यह दावा सही था कि भौतिक तथा सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्रों में यूरोपीय ज्ञान तत्कालीन भारतीय ज्ञान से श्रेष्ठतर था। एक जमाना था जब भारतीय ज्ञान सबसे अधिक उन्नत था वह बहुत दिनों से गतिहीन हो गया था तथा वास्तविकता से उसका कोई संपर्क नहीं रह गया था। इसीलिए राजा राममोहन राय के नेतृत्व में उस समय के अधिकांश प्रगतिशील भारतीयों ने जोरदार ढंग से पाश्चात्य ज्ञान के अध्ययन की वकालत की। वे पाश्चात्य ज्ञान को “आधुनिक पश्चिम के वैज्ञानिक तथा लोकतांत्रिक चिंतन के खजाने की कुंजी” के रूप में देखते थे। उन्होंने यह भी माना कि परंपरागत शिक्षा ने अंधविश्वास, डर और सत्तावाद को जन्म दिया है। दूसरे शब्दों में, उन्होंने माना कि देश की मुक्ति आगे बढ़ने में है न कि पीछे जाने में। वस्तुतः उन्नीसवीं और बीसवीं सदियों के किसी भी प्रमुख भारतीय ने इस दृष्टिकोण को कभी नहीं छोड़ा। इसके अतिरिक्त आधुनिक इतिहास के संपूर्ण काल में पाश्चात्य ज्ञान को ग्रहण करने के लिए उत्सुक भारतीयों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह आधुनिक ढर्रे पर अपनी शैक्षिक गतिविधियों का प्रसार करें। भारत सरकार ने, विशेषकर बंगाल में, 1835 के निर्णय पर तेजी से कार्यवाई की और अपने स्कूलों और कॉलेजों में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया। उसने बड़ी संख्या में प्राथमिक स्कूल खोलने के बदले थोड़े से अंग्रेजी स्कूल और कॉलेज खोले। लोक शिक्षा की उपेक्षा करने के कारण बाद में इस नीति की तीव्र आलोचनाएँ हुईं। वस्तुतः आधुनिक और उच्चतर शिक्षा संस्थान खोलने पर जोर देने की नीति गलत नहीं थी। अगर और कुछ नहीं तो प्राथमिक स्कूलों के लिए शिक्षकों को शिक्षित और प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में स्कूलों और कॉलेजों की आवश्यकता थी। मगर उच्च शिक्षा के प्रसार के साथ ही आम जनता को शिक्षित करने का काम भी हाथ में लिया जाना चाहिए था। सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वह शिक्षा पर मामूली रकम से अधिक खर्च नहीं करना चाहती थी। शिक्षा पर खर्च की कमी को पूरा करने के लिए अधिकारियों ने तथाकथित “अधोगामी निस्यंदन सिद्धान्त” या नीचे की ओर छन कर जाने का सिद्धान्त (Downward filtration theory) का सहारा लिया। चूँकि शिक्षा के मद में दी गई धनराशि के द्वारा मुट्ठी भर लोगों को ही शिक्षित किया जा सकता था, इसलिए यह तय हुआ कि उसे उच्च और मध्यम वर्गों के थोड़े से लोगों को शिक्षित करने पर खर्च किया जाए। उन लोगों से यह आशा की जाती थी कि वे जनसाधारण को शिक्षित करने और उनके बीच आधुनिक विचारों का प्रचार करने का काम अपने ऊपर लेंगे। इस प्रकार यह समझा गया कि शिक्षा और आधुनिक विचार उच्च वर्गों से छिन कर या निकल कर निचले वर्गों के लोगों को प्राप्त होंगे। यह नीति ब्रिटिश शासन के बिल्कुल अंत तक चली हालाँकि इसे सरकारी तौर पर 1854 में छोड़ दिया गया था। यहाँ इस बात का उल्लेख आवश्यक है कि यद्यपि शिक्षा रिसकर नीचे नहीं गई किंतु आधुनिक विचार बहुत हद तक आम लोगों के बीच फैले हालाँकि शासकों ने जिस रूप में चाहा था, उस रूप में ऐसा नहीं हुआ। स्कूलों और पाठ्यपुस्तकों के जरिये नहीं बल्कि राजनीतिक दलों, पत्र-पत्रिकाओं और सार्वजनिक मंचों के माध्यम से शिक्षित भारतीयों का बुद्धिजीवियों ने ग्रामीण और शहरी जनता के बीच जनतंत्र, राष्ट्रीयता, साम्राज्यवाद विरोध और सामाजिक और आर्थिक समानता तथा न्याय के विचारों का प्रचार किया। यदि शिक्षा इन विचारों का वाहक बनी भी तो ऐसा उसने परोक्ष रूप से ही किया। इसने लोगों को भौतिक और समाजविज्ञानों तथा मानविकी में कुछ साहित्य उपलब्ध कराया। इससे उनकी सामाजिक विवेचन की क्षमता बढ़ी। अन्यथा इस शिक्षा का ढाँचा और खाका, इसके लक्ष्य तथा पद्धतियों और पाठ्यक्रम की रचना साम्राज्यवाद को सुरक्षित रखने के लिए की गई थी। भारत में शिक्षा के विकास में भारत मंत्री (Secretary of State) की 1854 की शिक्षा विषयक विज्ञप्ति (Educational Dispatch) एक और महत्वपूर्ण कदम थी। इस विज्ञप्ति ने भारत सरकार से जन शिक्षा की जिम्मेदारी लेने को कहा इस प्रकार उसने “अधोगामी निस्यंदन सिद्धान्त” को कम से कम कागजी तौर पर तो छोड़ दिया। लेकिन व्यवहार में, सरकार ने शिक्षा के प्रसार के लिए कुछ भी नहीं किया और उस पर नाममात्र खर्च किया। विज्ञप्ति द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग बने और 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में संबद्धकारी (Affiliating) विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। प्रसिद्ध बंगला उपन्यासकार बंकिमचन्द्र चटर्जी 1858 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम दो स्नातकों में से थे। सभी बड़े-बड़े दावों के बावजूद, कंपनी और बाद में ब्रिटिश राज के अधीन भारत सरकार ने भारत में पाश्चात्य विद्या या किसी भी अन्य विद्या के प्रसार में वस्तुतः कोई गंभीर दिलचस्पी नहीं ली। यहाँ तक कि जो सीमित प्रयास किया गया, वह उन कारकों का परिणाम था, जिनका लोक कल्याण की भावनाओं से कोई संबंध नहीं था। इस दिशा में आधुनिक शिक्षा के पक्ष में प्रगतिशील भारतीयों, विदेशी ईसाई धर्म प्रचारकों और लोकोपकारी अफसरों तथा अन्य अंग्रेजों का आंदोलन कुछ महत्व रखता है। मगर सबसे महत्वपूर्ण कारण था, प्रशासन का खर्च कम करने की चिंता। इसके लिए सरकार शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाना चाहती थी जिससे प्रशासन और ब्रिटिश व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की छोटे कर्मचारियों की बड़ी और बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा किया जा सके। शिक्षित भारतीय अपेक्षाकृत सस्ते पड़ते थे। इन कामों के लिए पर्याप्त संख्या में अंग्रेजों को बाहर से लाना बहुत ही खर्चीला था और शायद संभव भी नहीं था। सस्ते क्लर्कों की संख्या बढ़ाने पर जोर देने के फलस्वरूप स्कूलों और कॉलेजों में आधुनिक शिक्षा दी जाने लगी जिसने वहाँ शिक्षा प्राप्त करने वालों को कंपनी को प्रशासन में काम करने लायक बनाया। साथ ही इन संस्थानों ने अंग्रेजी पर जोर दिया जो स्वामियों और प्रशासन की भाषा थी। अंग्रेजों की शिक्षा नीति का एक अन्य प्रयोजन इस धारणा से निकला था कि शिक्षित भारतीय इंग्लैण्ड में बनी वस्तुओं के बाजार का भारत में विस्तार करेंगे। अंत में, पाश्चात्य शिक्षा भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करेगी, विशेषकर इस कारण से कि उसने भारत के ब्रिटिश विजेताओं और उनके प्रशासन की महिमा का गान किया था। उदाहरण के लिए, मैकाले ने निर्देश दिया था - हमें ऐसा वर्ग बनाने के लिए जी-जान से प्रयत्न करना चाहिए जो हमारे और उन करोड़ों लोगों के बीच, जिन पर हम शासन करते हैं, द्विभाषिए का काम कर सके, यह उन लोगों का वर्ग हो जो रक्त और रंग की दृष्टि से भारतीय मगर रुचि, विचारों, आचरण तथा बुद्धि की दृष्टि से अंग्रेज हो। इस प्रकार अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा का उपयोग देश में अपनी राजनीतिक सत्ता को मजबूत बनाने के लिए करना चाहा। परंपरागत भारतीय शिक्षा प्रणाली धीरे-धीरे सरकारी समर्थन के अभाव और उससे भी अधिक, 1844 की सरकारी घोषणा के कारण समाप्त हो गई, जिसके अनुसार सरकारी रोजगार के लिए आवेदन करने वालों को अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूलों को अधिक लोकप्रिय बना दिया और अधिकाधिक छात्रों को परंपरागत स्कूलों को छोड़ने को लिए बाध्य कर दिया। शिक्षा प्रणाली की एक मुख्य कमजोरी थी, आम जनता की शिक्षा की उपेक्षा। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में जन-साक्षरता की स्थिति 1821 की तुलना में 1921 में शायद ही अच्छी थी। 1911 में 94 प्रतिशत और 1921 में 92 प्रतिशत भारतीय निरक्षर थे। शिक्षा के माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं की जगह अंग्रेजी के ऊपर अधिक जोर ने जनता में शिक्षा का प्रसार नहीं होने दिया। उसमें शिक्षित लोगों और जनता के बीच भाषा तथा संस्कृति की खाई पैदा करने की प्रवृत्ति भी नजर आने लगी। चूँकि छात्रों को स्कूलों तथा कॉलेजों में फीस देनी पड़ती थी, इसलिए शिक्षा काफी मँहगी थी, अतः धनी वर्गों और शहरी लोगों का इस पर एकाधिकार हो गया था। लगभग एक सौ साल तक यह शिक्षा इतनी सीमित थी कि यह परंपरागत शिक्षा की क्षति की भरपाई करने में भी असफल रही। प्रारंभिक शिक्षा नीति में एक सबसे बड़ी खामी थी लड़कियों की शिक्षा की बिल्कुल अवहेलना। लड़कियों की शिक्षा के लिए धन की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी। ऐसा अंशतः इसलिए हुआ कि सरकार चिंतित थी कि रुढ़िवादी भारतीयों की भावनाओं को चोट न पहुँचे। इससे भी बढ़कर यह बात थी कि विदेशी अधिकारियों की नजर में स्त्री-शिक्षा की कोई तात्कालिक उपयोगिता नहीं थी क्योंकि स्त्रियों को सरकारी दफ्तरों में क्लर्क नहीं बनाया जा सकता था। परिणाम यह हुआ कि 1921 में भी केवल 2 प्रतिशत भारतीय स्त्रियाँ लिख-पढ़ सकती थीं और 1919 में केवल 490 लड़कियाँ बंगाल प्रेसिडेंसी के हाई स्कूलों की चार उच्च कक्षाओं में पढ़ रही थीं। कंपनी के प्रशासन ने वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा की भी उपेक्षा की। 1857 तक देश में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में केवल तीन ही मेडिकल कॉलेज थे। उच्चतर तकनीकी शिक्षा देने के लिए केवल एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में था। उसके दरवाजे केवल यूरोपवासियों तथा यूरोपियन लोगों के लिए खुले हुए थे। इन कमजोरियों में से अधिकांश की जड़ में वित्तीय समस्या थी। सरकार शिक्षा पर कभी एक मामूली रकम से अधिक खर्च करने को तैयार नहीं थी। यहाँ तक कि 1886 में भी उसने अपनी लगभग 47 करोड़ रुपयों की निवल आय में से एक करोड़ रुपए ही शिक्षा पर खर्च किए। | |||||||||
| |||||||||